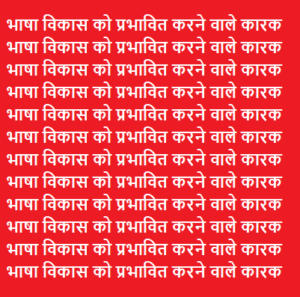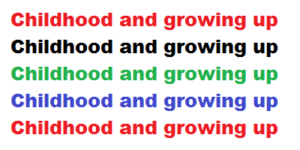वृद्धि एवं विकास के अर्थ , परिभाषाये , सिधांत , अंतर , सम्बन्ध , प्रभावित करनेवाले कारक , शिक्षकों की भूमिका एवं , शैक्षिक महत्व
| Vridhi evan vikaas ke arth , paribhaashaaye , sidhaant , antar , sambandh , prabhaavit karanevaale kaarak , shikshakon kee bhoomika evan ,shaikshik mahatv | Meaning, definitions, principles, differences, relationships, influencing factors, role of teachers and educational importance of growth and development. |
इस पेज में वृद्धि एवं विकास के अर्थ ,वृद्धि एवं विकास के परिभाषाये , वृद्धि एवं विकास के सिधांत , वृद्धि एवं विकास के अंतर सम्बन्ध , वृद्धि एवं विकास के प्रभावित करनेवाले कारक ,वृद्धि एवं विकास के शिक्षकों की भूमिका ,वृद्धि एवं विकास शैक्षिक महत्व का वर्णन किया गया है |
प्रश्न – वृद्धि एवं विकास के अर्थ , परिभाषाये , सिधांत , अंतर , सम्बन्ध , प्रभावित करनेवाले कारक , शिक्षकों की भूमिका एवं ,शैक्षिक महत्व का वर्णन करे ?
उतर –
01. वृद्धि एवं विकास के प्रस्तावना
वृद्धि तथा विकास एक सतत् प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ बनाती है। यह प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही माता के गर्भ में प्रारम्भ हो जाती है तथा जीवन पर्यन्त चलती रहती है। वास्तव में, गर्भाधान के साथ ही वृद्धि और विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है तथा जन्म के उपरान्त शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था में निरन्तर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया का अत्यंत महत्व है । आयु के बढ़ने के साथ-साथ वृद्धि तथा विकास के फलस्वरूप बालक की योग्यताओं तथा क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। इसलिए शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय बालकों की आयु तथा उनके विकास की अवस्था का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों का ज्ञान कराता है जिससे विभिन्न आयु के बालकों के विकास तथा उनके द्वारा विभिन्न विषयों के ज्ञान को हृदयंगम करने की क्षमता का समुचित ढंग से आंकलन किया जा सके।
02 वृद्धि एवं विकास के अर्थ
(Meaning of Growth and Developement
VRIDHI AEVM VIKAS KE ARTH
प्रायः वद्धि तथा विकास को समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निःसंदेह ये दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर ही संकेत करते हैं परंतु मनोवैज्ञानिक दष्टि से इन दोनों में कुछ अंतर है। वृद्धि तथा विकास के अर्थों को समझने के लिए इनके अंतर को समझना आवश्यक होगा । सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि (Celluar Multiplication) के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है । निःसंदेह विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, परंतु यह वृद्धि से व्यापक होता है ।
विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। गर्भाधान से लेकर शैशवास्था, बाल्यावस्था किशोरावस्था से होते हए प्रौढावस्था तक पहुँचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लम्बाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जा सकता है। वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है। बालक में होने वाली वृद्धि को अन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। परंतु कभी-कभी बालक के अंगों के आकार में वृद्धि होने पर भी उसकी कार्यक्षमता में अपेक्षित प्रगति नहीं होती है तथा कहा जाता है कि वृद्धि तो हो रही है, परंतु विकास ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। स्पष्ट है कि विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता को इंगित में करता है। विकास शरीर की अनेक संरचनाओं (Structures) तथा कार्यों (Functions) को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आंतरिक शरीर रचना सम्बन्धी परिवर्तन (Internal Physiological Change) तथा इनसे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं (Psychological Process) एकीकृत होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता व मितव्ययता से कार्य करने के योग्य बनाती हैं। अतः अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जा सकता है।
विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएँ प्रकट होती हैं। विकास के अंतर्गत दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएँ होती हैं जो निरन्तर जीवन पर्यन्त चलती रहती हैं। ये हैं-वृद्धि (Growth अथवा Evolution) तथा क्षय (Atrophy अथवा Involution)। ये दोनों प्रक्रियाएँ गर्भकाल से प्रारम्भ हो जाती हैं तथा मृत्यु पर समाप्त हो जाती हैं। प्रारम्भिक वर्षों में वृद्धि की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, जबकि क्षय प्रक्रिया अत्यंत मन्द गति से चलती है। जीवन के अन्तिम वर्षों में क्षय प्रक्रिया तीव्र गति से चलती है, जबकि वृद्धि प्रक्रिया की गति अत्यंत मन्द हो जाती है ।
(03) वृद्धि एवं विकास के परिभाषाएँ
VRIDHI AEVM VIKAS KE PRIBHASHA
मेरीडिथ के अनुसार-
“कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास को भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में।”
Some writers reserve the use of ‘growth’ to designate increments in size and of ‘development’ to mean differntiation.
-Meridith
हरलॉक के शब्दों में-
“विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है वरन् इसमें प्रौढावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएँ तथा नवीन योग्यताएँ प्रकट होती हैं।”
Development is not limited to growing larger. Instead, it consists of a progressive series of changes towards the goal of maturity. Development results in new characteristics and new abilities on the part of the individual.
-Hurlock
मनरों के अनुसार-
“विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था मे परिपक्वता तक गुजरता है।”
(04) वृद्धि तथा विकास के सिद्धान्त
(04) Principles of Growth and Development
(04) VRIDHI AEVM VIKAS KE SIDHANT
वृद्धि तथा विकास के सम्बन्ध में मनौवैज्ञानिकों के द्वारा अनेक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों से सिद्ध हो गया है कि वृद्धि तथा विकास के फलस्वरूप आने वाले परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धान्तों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धान्तों का अनुपालन करती है। इन सिद्धान्तों को वद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धान्तों के नाम से पुकारा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययनकर्ता के लिए वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को संचालित करने वाले सिद्धान्तों को जानना अत्यंत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण होगा। वृद्धि तथा विकास के कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्नवत् हैं
1. निरन्तरता का सिद्धान्त (Principle of Continuity)
2. व्यक्तिगतता का सिद्धान्त (Principle of Individuality)
3.परिमार्जितता का सिद्धान्त (Principle of Modifyability)
4. निश्चित तथा पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धान्त (Principle of Definite and Predictable Pattern
5. समान-प्रतिमान का सिद्धान्त (Principle of Uniform Pattern)
6. समन्वय का सिद्धान्त (Principle of Integration)
7. वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धान्त
(Principle of Interaction between Heredity and Enviornment)
DETAILS
1. निरन्तरता का सिद्धान्त
(Principle of Continuity)
निरन्तर विकास के सिद्धान्त के अनुसार वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरन्तर अविराम गति से चलती रहती है। कभी यह मन्द गति से चलती है तथा कभी तीव्र गति से चलती है । वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव निहित रहता है। वृद्धि तथा विकास को अलग-अलग सोपानों में नहीं बाँटा जा सकता है। उदाहरणार्थ, प्रारम्भिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र रहती है और उसके बाद के वर्षों में धीमी हो जाती है, परंतु विकास प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती रहती है। निरन्तर विकास के सिद्धान्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि वद्धि तथा विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है।
ii व्यक्तिगतता का सिद्धान्त
(Principle of Individuality)-
विकास की व्यक्तिगतता का सिद्धान्त बताता है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न-भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति से विकास करता है। एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा चारित्रिक आदि विभिन्नताओं का होना विकास की व्यक्तिगतता को इंगित करता है। यही कारण है कि आयु के समान होने पर भी बालक परस्पर भिन्न होते है |
iii परिमार्जितता का सिद्धान्त
(Principle of Modifyability)
विकास की परिमार्जित का सिद्धान्त यह बताता है कि विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन सम्भव होता है । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। विकास का यह सिद्धान्त शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना जाता है । शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा बालक के विकास को वांछित दिशा में अधिक तीव्र गति से अग्रसर करने का प्रयास किया जाता है |
iv. निश्चित तथा पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धान्त
(Principle of Definite and Predictable Pattern)
प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति, के विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिरूप का अनुसरण करते है । यद्यपि किसी भी प्रजाति के सदस्यों में परस्पर व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती परन्तु ये भिन्नताएँ बहुत कम होती हैं तथा उस प्रजाति की सामान्य प्रवृत्ति (General Trend) को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। व्यक्तियों के किसी समूह के विकास का अनेक वर्षों तक अवलोकन करने पर विकास के विभिन्न पक्षों के विकासात्मक प्रतिमानों को जाना जा सकता है। विकास के इन प्रतिमानों के आधार पर अन्य व्यक्तियों के विकास का पूर्वकथन (Prediction) किया जा सकता है। इस सिद्धान्त को विकास क्रम या विकास दिशा का सिद्धान्त (Principle of Developmental Direction) के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। उदाहरणार्थ, शारीरिक विकास के क्षेत्र में वृद्धि व विकास के क्रमबद्ध व पूर्वकथनीय प्रतिरूप के होने के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं । जन्म पूर्व जीवन (Prenatal Life) में शारीरिक वृद्धि मस्तकोधमुखी क्रम (CEPHALOCAUDAL SEQUENCE) का अनुसरण करती है। जिसका अर्थ है कि सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र (Head Region), फिर धड़ क्षेत्र (Trunk Region), तथा सबसे अन्त में पैर क्षेत्र (Leg Region) में शरीर की वृद्धि तथा शरीर के विभिन्न अंगों का नियन्त्रण होता है। जन्म के उपरान्त भी शारीरिक विकास में यह क्रम बना रहता है। बालक शरीर के ऊपरी अंगों अर्थात सिर का नियन्त्रण सबसे पहले सीखता है. फिर हाथो का नियन्त्रण सीखता है, फिर धड़ का नियन्त्रण सीखता है तथा सबसे अन्त में शरीर के निम्न भाग अर्थात् पैरों का नियन्त्रण करना सीख पाता है। मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि पक्षों में भी विकास के निश्चित प्रतिमानों को देखा जा सकता है |
v. समान-प्रतिमान का सिद्धान्त
(Principle of Uniform Pattern)
समान-प्रतिमान के सिद्धान्त के अनुसार समान प्रजाति (Race) के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो चाहे अथवा मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है । उदाहरणार्थ, संसार के समस्त भागों में मानव प्रजाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है तथा मानव शिशुओं के विकास के प्रतिमानों में किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है।
vi. समन्वय का सिद्धान्त (Principle of Integration)—
इस सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है.। बालक पहले सम्पूर्ण अंगों को तथा फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है । तत्पश्चात् वह इन समस्त भागों में समन्वय स्थापित करना सीखता है। जब तक शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनके भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता है तब तक उचित विकास नहीं हो पाता है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों को सरल व सहज बनाता है।
vii. वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धान्त
(Principle of Interaction between Heredity and Enviornment)
इस सिद्धान्त के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अन्तक्रिया का परिणाम होता है। केवल वंशानुक्रम अथवा केवल वातावरण बालक के विकास की दिशा व गति को निर्धारित नहीं करते हैं वरन् दोनों की अन्तःक्रिया के द्वारा विकास की दिशा व गति का नियंत्रण होता है । वास्तव में, वंशानुक्रम उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिससे आगे बालक का विकास करना सम्भव नहीं होता, जबकि वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर व सम्भावनाओं को निर्धारित करता है। अच्छे वंशानक्रम के अभाव में अच्छा वातावरण निष्फल हो सकता है तथा अच्छे वंशानुक्रम के बावजद दुषित वातावरण बालक को कुपोषण या गम्भीर रोगों का शिकार बना सकता है अथवा उसकी जन्मजात योग्यताओं को कुंठित कर सकता है।
इस सब्जेक्ट से सम्बन्धित विडिओ देखने के लिए इसे क्लिक करे >>
इस सब्जेक्ट से सम्बन्धित PDF के लिए इसे क्लिक कर टेलीग्राम join करे >>
(05) विकास के पक्ष
विकास के पक्ष -(Aspects of Development)
विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास के उपरोक्त वर्णित विवेचन से स्पष्ट है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक के व्यवहार में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं । बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास को अग्रांकित पक्षों में विभक्त किया जा सकता है |
1. शारीरिक विकास (Physical Development)
2. मानसिक विकास (Mental Development)
3. सामाजिक विकास (Social Development)
4. संवेगात्मक विकास (Emotional Development)
5. नैतिक विकास (Moral Development)
शैक्षिक दष्टि से विकास के इन सभी पक्षों का अत्यधिक महत्व है। विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में इस विभिन्न पक्षों का विकास किस प्रकार से होता है तथा विकास की गति को किसे प्रकार से वांछित दिशा में तीव्र गति से बढ़ाया जा सकता है, इसका अध्ययन करना शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक मानसिक सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास की विस्तृत चर्चा अध्याय आठ, नौ, दस, ग्यारह तथा बारह में की गई है।
(06) विकास के अवस्थाएँ
VIKAS KE AVSTHAYE
Stages of Development
यद्यपि विकास की अवस्था अथवा सोपान अथवा स्तर जैसे शब्द का प्रयोग तकनीकी दृष्टि से भ्रामक है। फिर भी, प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया को कुछ अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है। विकास की अवस्था शब्द युग्म से संकेत मिलता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर विकास प्रक्रिया में कुछ निश्चित परिवर्तन आ जाते हैं । वास्तव में विकास एक सतत् प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त चलती है। परंतु व्यावहारिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए यह मान लिया जाता है कि विकास की प्रक्रिया में बालक विकास की कुछ अवस्थाओं अथवा सोपानों से होकर गुजरता है।
विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न सोपानों अथवा अवस्थाओं को बताया है।
सामान्य रूप से मानव विकास को निम्नांकित अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है
i. गर्भावस्था (Prenatal)
ii. शैशवावस्था (Infancy)
iii. बाल्यावस्था (Childhood)
iv. किशोरावस्था (Adolesence)
v. प्रौढावस्था (Adulthood)
माता व पिता के मिलन के फलस्वरूप माता के द्वारा गर्भ धारण करने से लेकर शिशु के जन्म तक का समय गर्भावस्था कहलाती है। शिशु के जन्म के उपरान्त के प्रथम पाँच वर्ष का काल शैशवास्था या शैशवकाल कहलाता है। पाँच वर्ष की आयु से लेकर बारह वर्ष की आयु तक ही अवधि बाल्यावस्था या बाल्यकाल कहलाती है। बारह वर्ष की आयु से लेकर अट्ठारह वर्ष की आयु तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। अट्ठारह वर्ष की आयु के उपरान्त का काल प्रौढकाल या प्रौढ़ावस्था कहलाती है।
शैक्षिक दृष्टि से इनमें से मध्य की तीन अवस्थाओं अर्थात् शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था का अत्यधिक महत्त्व है।
(07) वृद्धि एवं विकास में अंतर pdf
(08) वृद्धि एवं विकास में सिधांत pdf
(09) वृद्धि एवं विकास में सम्बन्ध pdf
(10) वृद्धि एवं विकास के प्रभावित करनेवाले कारक
(11) वृद्धि एवं विकास के स्तर
(12) वृद्धि एवं विकास में शिक्षकों की भूमिका pdf
(13) वृद्धि एवं विकास के शैक्षिक महत्व pdf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
###############################
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
***********************************************
नोट – इस पेज में आप Meaning of growth and development , definitions of growth and development , principles of growth and development , differences of growth and development ,relationships of growth and development , influencingof growth and development , factors of growth and development, role of teachers of growth and development , and educational importance of growth and development. वृद्धि एवं विकास के अर्थ ,वृद्धि एवं विकास के परिभाषाये , वृद्धि एवं विकास के सिधांत , वृद्धि एवं विकास के अंतर सम्बन्ध , वृद्धि एवं विकास के प्रभावित करनेवाले कारक ,वृद्धि एवं विकास के शिक्षकों की भूमिका ,वृद्धि एवं विकास शैक्षिक महत्व का वर्णन है इस टॉपिक से सम्बन्धित कोए स्म्श्य है तो आप निचे कमेंट करे |