वैदिक कालीन भारत मे शिक्षा
Vaidik Kalin Bharat Me Shiksha
| प्रश्न | वैदिक कालीन भारत मे शिक्षा | Vaidik Kalin Bharat Me Shiksha |
| विषय | बी.एड. , डी.एल.एड एवं अन्य |
वैदिक-शिक्षा का अर्थ
वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ। जैसे- विद्या, ज्ञान, प्रबोध एवं विनय आदि। शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक एवं संकुचित दोनों अर्थों में किया गया। व्यापक अर्थ में मनुष्य को उन्नत तथा सभ्य बनाना शिक्षा है, शिक्षा की यह प्रक्रिया जीवन-पर्यन्त चलती है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का मतलब औपचारिक शिक्षा से है । प्रत्येक बालक प्रारम्भिक जीवन के कुछ वर्षों में गुरुकुल में निवास करके ब्रह्मचर्य – जीवन व्यतीत करते हुए गुरु से शिक्षा प्राप्त करता था । व्यक्ति का सर्वागीण विकास गुरुकुल में होता था । वह धर्म की राह पर चलकर मोक्ष पाता था ।
वैदिक काल में शिक्षा को महत्त्व दिया जाता है। आर्यों का विश्वास था शिक्षा से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास हो सकता है। शिक्षा प्रकाश का स्त्रोत मानी गयी। शिक्षा सभी का जीवन के सभी क्षेत्रों में पथ-प्रदर्शन करती है। वैदिककाल में अशिक्षित व्यक्ति समाज के लिए कलंक था। माता-पिता बच्चों को शिक्षित करना अपना पुनीत कर्त्तव्य समझते थे । भर्तृहरि ने नीतिशतक में लिखा है- विद्या विहीनः पशु अर्थात् विद्या के बिना मनुष्य पशु-तुल्य है। वैदिककाल में शिक्षा सार्वजनिक थी। स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से शिक्षा आवश्यक थी । शिक्षा प्राप्त करके लोग पुरुषार्थों को प्राप्त करते थे ।
वैदिक कालीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य
प्राचीन भारत में शिक्षा के कुछ विशिष्ट उद्देश्य थे। जिन्हें शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा के उद्देश्य माना है। शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है और उसे सामाजिकता का प्रशिक्षण देती है। डॉ० ए० एस० अल्तेकर ने प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए लिखा है- “ईश्वर भक्ति एवं धार्मिक भावना का विकास, चरित्र-निर्माण, व्यक्ति का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्त्तव्य – पालन की शिक्षा, सामाजिक कुशलता में वृद्धि तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कहे जा सकते हैं।”
- 01. ज्ञान तथा अनुभव पर बल-
- 02. चित्तवृत्तियों का निरोध करना-
- 03. धार्मिकता का समावेश –
- 04. चरित्र का निर्माण करना-
- 05. व्यक्तित्व का विकास-
- 06. नागरिक और सामाजिक कर्त्तव्य-
- 07. राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार –
- 08. राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार –
01. ज्ञान तथा अनुभव पर बल-
प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना था। छात्रों की मानसिक योग्यता का मापदण्ड उनके प्राप्त किये जाने वाले ज्ञान से था । उपाधि-पत्र नहीं थे। अर्जित किये गये ज्ञान का प्रमाण वे विद्वत्परिषदों में शास्त्रार्थ करके देते थे। “छान्दोग्य उपनिषद्” में हमें श्वेतकेतु और कमलायन के उदाहरण मिलते हैं जिनको बारहवर्ष के अध्ययन के उपरान्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं समझा गया। प्राचीनकाल में शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं था, वरन् मनन, स्मरण और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान आत्मसात् करना था। डॉ० आर० के० मुकर्जी ने लिखा है- “शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात् करना था । ”
02. चित्तवृत्तियों का निरोध करना-
शिक्षा का उद्देश्य छात्रों की चित्त-वृत्तियों का निरोध करना था। उस समय शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्त्व दिया जाता था । क्योंकि शरीर नश्वर है। आत्मा अनश्वर है । आत्मा के उत्थान के लिए जप, तप और योग पर बल दिया जाता था। ये कार्य चित्त की प्रवृत्ति निरोध अर्थात् मन पर नियन्त्रण करके ही सम्भव थे। छात्रों को विभिन्न प्रकार के अभ्यासों द्वारा चित्त-वृत्तिय का निरोध करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। जिससे मन इधर-उधर भटक कर उनकी मोक्ष-प्राप्ति में बाधा उपस्थित न करे। डॉ० आर० के० मुकर्जी के शब्दों में “चित्तवृत्तियों का निरोध, शिक्षा का उद्देश्य अर्थात् मन के उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता है ।
03. धार्मिकता का समावेश –
शिक्षा का उद्देश्य – छात्रों में ईश्वर – भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश करना था । इस प्रकार की शिक्षा को सार्थक माना जाता था, जो संसार में व्यक्ति की मुक्ति को सम्भव बनाये – “सा विद्या या विमुक्तये व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती थी जब वह ईश्वर – भक्ति और धार्मिकता की भावना से पूर्ण हो । इस भावना को व्रत, यज्ञ, उपासना, धार्मिक उत्सवों आदि के द्वारा विकसित किया जाता था। डॉ० ए० एस० अल्तेकर ने लिखा है- “सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था ।”
04. चरित्र का निर्माण करना-
प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना था । व्यक्ति के चरित्र को उसके पाण्डित्य से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था । “मनुस्मृति” में लिखा है- “केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान् ब्राह्मण, सम्पूर्ण वेदों के ज्ञाता, पर चरित्रहीन विद्वान् से कहीं अधिक श्रेष्ठ है।” गुरुकुलों के उत्तम वातावरण, सदाचार उपदेशों, महापुरुषों के उदाहरणों, महान विभूतियों के आदर्शों के द्वारा छात्रों के चरित्र का निर्माण किया जाता था। डॉ० वेद मित्र का कथन है- “छात्रों के चरित्र का निर्माण करना, शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था । ”
05. व्यक्तित्व का विकास-
शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था । आत्म-संयम, आत्म-सम्मान, आत्म-विश्वास आदि सद्गुणों को उत्पन्न किया जाता था । गोष्ठियों और वाद-विवाद सभाओं का आयोजन करके विवेक, न्याय और निष्पक्षता की शक्तियों को जन्म देकर उनको बलवती बनाया जाता था।
06. नागरिक और सामाजिक कर्त्तव्य-
पालन की भावना का विकास – छात्रों में नागरिक और सामाजिक कर्त्तव्यों का पालन करने की भावना लाना शिक्षा का उद्देश्य था । व्यक्ति से यह आशा की जाती थी वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते समय अपने नागरिक और सामाजिक कर्त्तव्यों का पालन करे। इसके लिए छात्रों को गुरु द्वारा विभिन्न प्रकार के उपदेश दिये जाते थे, जैसे अतिथियों का सत्कार करना, दीन-दुःखियों की सहायता करना, वैदिक साहित्य की निःशुल्क शिक्षा देना, दूसरों के प्रति निःस्वार्थता का व्यवहार करना, और पुत्र, पिता एवं पति के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करना । इससे मनुष्य का जीवन सर्वथा ही आदर्श बन जाता था ।
07. सामाजिक कुशलता लाना –
शिक्षा का उद्देश्य छात्रों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना था । शिक्षा केवल व्यक्ति का मानसिक विकास ही नहीं करती वरन् सामाजिक कुशलता में उनकी उन्नति करती है । जिससे वह सरलता से जीविका का उपार्जन करके अपने सुख में वृद्धि कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रो को रुचि और वर्ण के अनुसार उद्योग व व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी । “शिक्षा पूर्णतया सैद्धान्तिक और साहित्यिक नहीं थी, वरन् किसी न किसी शिल्प से सम्बद्ध थी । ”
08. राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार –
प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण उसका प्रसार करना था । उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय में दक्ष बनाता था । ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता था और आर्य वैदिक साहित्य के किसी न किसी भाग का अध्ययन करता था । इन कार्यों से किसी को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता था, लेकिन ऐसा करके वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी राष्ट्रीय संस्कृति को सुरक्षित रखते थे, उसका प्रसार करते थे । इन उद्देश्यों से लौकिक और पारलौकिक जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं ।


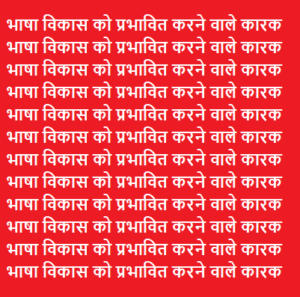
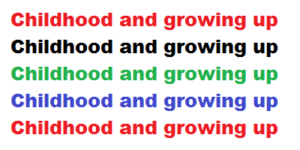
2 thoughts on “वैदिक कालीन भारत मे शिक्षा | Vaidik Kalin Bhart Me Shiksha”
Hai
Test 2