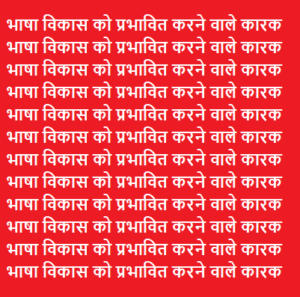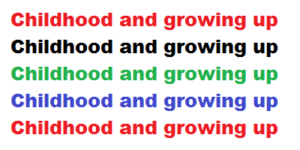सृजनात्मकता के अर्थ परिभाषा तत्व विशेषताएं प्रभावित करने वाले कारक
Srjanaatmakata Ke arth Paribhaasha Tatv Visheshataen Prabhaavit Karane Vaale Kaarak
प्रश्न- सृजनात्मकता के अर्थ परिभाषा तत्व विशेषताएं प्रभावित करने वाले कारको का वर्णन करे |
उत्तर –
(01) सृजनात्मकता के प्रस्तावना
वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक विकास के आधुनिक युग में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत नित प्रतिदिन नूतन आविष्कार हो रहे हैं। इनमें से अधिकांश आविष्कारों के पीछे जहाँ वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम छिपा है वहीं उनकी सजनात्मकता का भी योगदान कम नहीं है। पहले यह माना जाता था कि केवल लेखक, कवि, चित्रकार, संगीतकार आदि व्यक्ति ही सृजनात्मक होते हैं परन्तु अब यह माना जाने लगा है कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति हो सकती है। वास्तव में ससार के समस्त प्राणियों में सजनात्मकता पाई जाती है – किसी व्यक्ति में कम मात्रा में सृजनात्मकता होती है तथा किसी व्यक्ति में अधिक मात्रा में सृजनात्मकता होती है। मानवीय जीवन को सुखमय बनाने के लिए नवीन आविष्कार करने तथा समस्याओं का सामाधान खोजने के कार्य में सृजनात्मकता अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूसरे विश्वयुद्ध के उपरान्त ‘सृजनात्मकता’ के प्रत्यय पर मनोवैज्ञानिकों व शिक्षाशास्त्रियों ने विशेष ध्यान दिया। वर्तमान समय में तीव्र गति से हो रहे वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक प्रगति व विकास तथा आधुनिकीकरण ने मानव जीवन को इतना जटिल तथा समस्याग्रस्त बना दिया है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। आज के समस्याग्रस्त जटिल समाज तथा प्रतियोगितापूर्ण संसार में सृजनात्मक व्यक्तियों की अत्यन्त माँग है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपलब्धियों को अधिकाधिक अर्जित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मक व्यक्तियों को खोजना एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है।
(02) सृजनात्मकता के अर्थ–
MEANING OF DEFINITION
सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के Creativity के हिंदी रूपांतरण है| सृजनात्मकता के अर्थ है – किसी नये चीज को उत्पन्न या रचना करना | नवीन क्रियाओ या नवीन विचारो या खोज करने की शक्ति को सृजनात्मकत कहते है |
(03)सृजनात्मकता के परिभाषाये
(Definition of Creativity)
भिन्न-भिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सृजनात्मकता (Creativity) को भिन्न-भिन्न ढंग से परिभाषित किया है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत सृजनात्मकता की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नवत हैं –
डीहान तथा हेविंगहर्ट के अनुसार –
“सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे। यह नवीन वस्तु सम्पूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसने उसे प्रस्तुत किया है।”
ड्रैवहल के के अनुसार –
“सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है।”
क्रो एवं क्रो के अनुसार –
“सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है।”
कोल और ब्रूस के के अनुसार –
सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समय व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है।”
Creativity is an ability and activity of man’s mind to grasp, express and appreciate in the form of an original product.”
– Cole and Bruce
उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सृजनात्मकता का सम्बन्ध प्रमुख रूप से मौलिकता या नवीनता से है। समस्या पर नये ढंग से सोचने तथा समाधान खोजने के प्रयास से सृजनात्मकता परिलक्षित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने तथा विचार करने में समर्थ बनाती है। प्रचलित ढंग से हटकर किसी नये ढंग से चिन्तन करने तथा कार्य करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है।
(04)सृजनात्मकता के तत्व
(Elements of Creativity)
सृजनात्मकता की परिभाषाओं के अवलोकन तथा विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सृजनात्मकता को संवेदनशीलता, जिज्ञासा, कल्पना, मौलिकता, खोजपरकता, लचीलापन, प्रवाह, विस्तृतता, नवीनता आदि के संदर्भ में समझा जा सकता है। सृजनात्मकता के कुछ समानार्थी यह विभिन्न प्रत्यय वैज्ञानिक अनुसंधानों, कलाकृतियों, संगीत, रचना, लेखन व काव्य कला, चित्रकला, भवन निर्माण आदि सृजनात्मक कार्यों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। सृजनात्मकता के चार प्रमुख तत्व निम्नवत् हैं –
(i) प्रवाह (Fluency) –
प्रवाह से तात्पर्य किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों या प्रत्युत्तरों को प्रस्तुत से है। प्रवाह को पुनः चार भागों – वैचारिक प्रवाह (Ideational Fluency), अभिव्यक्ति प्रवाह (Expressional Fluency), साहचर्य प्रवाह (Associative Fluency) तथा शब्द प्रवाह (Word Fluency) में बाँटा जा सकता है। वैचारिक प्रवाह में विचारों के स्वतंत्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे किसी कहानी के अनेकानेक शीर्षक वताना, किसी वस्तु के अनेकानेक उपयोग बताना. किसी वस्तु को सुधारने के अनेकानेक तरीके बताना आदि आदि। अभिव्यक्ति प्रवाह में मानवीय अभिव्यक्तियों के स्वतंत्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे दिये गये चार शब्दों से वाक्य बनाना, दिये गये अपूर्ण वाक्य को पूरा करना आदि आदि । साहचर्य प्रवाह से तात्पर्य दिये गये शब्दों या वस्तओं में परस्पर साहचर्य स्थापित करने से है। जैसे किसी दिये गये शब्द के अधिकाधिक पर्यायवाची या विलोम शब्द लिखना । शब्द प्रवाह का सम्बन्ध शब्दों से होता है। जैसे दिये गये प्रत्ययों तथा उपसर्गों (Prefix and Suffix) से शब्द बनाना। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी सृजनशील परीक्षण के किसी पद (item) पर प्रवाह को प्रायः उस पद पर दिये गये प्रत्युत्तरों की संख्या से व्यक्त किया जाता है। परीक्षण पर व्यक्ति के कुल प्रवाह प्राप्तांक को ज्ञात करने के लिए सभी पदों के प्रवाह अंकों का योग कर लिया जाता है।
(ii) विविधता (Flexibility) –
विविधता से अभिप्राय किसी समस्या पर दिये प्रत्युत्तरो या विकला में विविधता के होने से है। इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प या उत्तर एक दूसरे से कितने भिन्न-भिन्न हैं। विविधता की तीन विमाएं – आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता (Figural Spontaneous Flexibility, आकृति अनुकूलन विविधता (Figural Adaptive Flexibility) तथा शाब्दिक स्वतः स्फूर्त विविधता (Semantic Spontaneous Flexibility) हो सकती हैं। आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता से तात्पर्य किसी वस्तु या आकृति में सुधार करने के उपायों की विविधता से है। आकृति अनुकूलन विविधता से अभिप्राय किसी वस्तु या आकृति के रूप में किसी दिये गये रूप में परिवर्तित करने की विधियों की विविधता से है। शाब्दिक स्वतः स्फूर्त विविधता में वस्तओं या शब्दों के प्रयोग में विविधता को देखा जाता है। सृजनात्मकता के परीक्षणों के किसी पद (item) पर विविधता को प्रायः उस पद पर व्यक्ति के द्वारा दिये गये प्रत्युत्तरों के प्रकार (Type of Responses) की संख्या से व्यक्त किया जाता है। परीक्षण पर किसी व्यक्ति के कल विविधता प्राप्तांक को ज्ञात करने के लिए उसके द्वारा विभिन्न पदों पर प्राप्त विविधता अंकों को जोड़ लिया जाता है।
(iii) मौलिकता (Originality) –
मौलिकता से अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्पो या उत्तरो का असामान्य (Uncommon) अथवा अन्य व्यक्तियों के उत्तरों से भिन्न होने से है। इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति द्वारा दिये गये विकल्प या उत्तर सामान्य या प्रचलित (Popular) विकल्पी या उत्तरा से कितने भिन्न हैं। दूसरे शब्दों में मौलिकता मुख्य रूप से नवीनता (Newness) से सम्बन्धित हाता है। जो व्यक्ति अन्यों से भिन्न विकल्प प्रस्तुत करता है वह मौलिक कहा जा सकता है। वस्तुओं के नय उपयाग बताना, कहानी, कविता या लेख के शीर्षक लिखना, परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम बताना, नवीन प्रतीक खोजना आदि मौलिकता के कुछ उदाहरण हैं।
iv) विस्तारण (Elaboration)–
विस्तारण से तात्पर्य दिये गये विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या, व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुतिकरण से होता है। विस्तारण को दो भागों – शाब्दिक विस्तारण (Semantic Elaboration) तथा आकृति विस्तारण (Figural Elaboration) में बांटा जा सकता है। शाब्दिक विस्तारण में किसी दी गई संक्षिप्त घटना, क्रिया, कार्य, परिस्थिति आदि को विस्तृत करके प्रस्तुत करने के लिए कहा .. जाता है जबकि आकृति विस्तारण में किसी दी गई रेखा या अपूर्ण चित्र में कुछ जोड़कर उससे एक पूर्ण एवं सार्थक चित्र बनाना होता है।
(05)सृजनात्मकता के विशेषताएं
- (i) विचारों तथा अभिव्यक्ति में मौलिकता
- (ii) अन्वेषणात्मक तथा जिज्ञासा प्रकृति
- (iii) दूरदृष्टि
- (iv) स्वतंत्र निर्णय क्षमता
- (v) उच्च आकांक्षा
- (vi) गैर परम्परागत विचारों में रुचि
- (vii) अभिव्यक्ति में प्रवाह
- (viii) विस्तारण क्षमता
- (ix) सृजन का गौरव
- (x) अभिव्यक्ति में स्वः स्फूर्तता
- (xi) जोखिम उठाने को तत्पर
- (xii) अभिव्यक्ति में विविधता
(06) सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक
(1) आनुवंशिकता-
(2) वातावरण-
(3) पारिवारिक वातावरण-
(4) विद्यालय का वातावरण-
(5) जिज्ञासा-
(6) समस्या समाधान व ज्ञान प्राप्ति का अवसर-
(7) उत्साहपूर्ण वातावरण पैदा करके ( Creating an encourage climate )
8) बहुत से क्षेत्रों में रचनात्मकता को उत्साहित करना ( Encourage Creative in many medias )
(9) विविधिता की प्रेरणा (Encouraging variety of approach )
(10) लचीलता तथा सक्रियता को उत्साहित करना ( Encouraging activeness and flexibility )
(11) आत्म विश्वास को उत्साहित करना ( Encouraging self trust )
(12) श्रेणीं कृतियों के अध्ययन की प्रेरणा ( Encourage to study master pieces )
(13) स्वयं भी एक रचनात्मक रूचियों वाला व्यक्ति हो ( Being a creative person one self )
(1) आनुवंशिकता-
बालक वंशानुगत रूप से अन्य शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों की तरह सृजनात्मक क्षमता भी अपने माता-पिता या पूर्वजों से प्राप्त करता है। प्रायः गायक या कलाकार का पुत्र भी गायक बनता है, परन्तु यह आवश्यक नही कि ऐसा हो ही। कई मामलों में यह गण बालकों को उचित वातावरण नहीं मिलने पर नहीं भी विकसित हो सकता है।
(2) वातावरण-
समुचित वातावरण बालक में सृजनात्मक क्षमता का विकास करता है। उपर्यक्त वातावरण मिलने पर बालक अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त प्रदान कर पाता है अन्यथा वातावरण के अभाव में सृजनात्मक क्षमता कुंठित हो जाती है। अतः माता-पिता व शिक्षक का कर्तव्य है कि बालकों के लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें।
(3) पारिवारिक वातावरण-
बालकों में सृजनात्मकता के विकास को उसका पारिवारिक वातावरण भी प्रभावित करता है। कठोर व तानाशाही पारिवारिक अनुशासन सृजनात्मकता को अवरुद्ध करता है। अतः सृजनात्मकता के उचित विकास के लिए आवश्यक है कि परिवार का वातावरण स्वतन्त्र, लचीला, एवं जनतन्त्रीय होना चाहिए जिससे बालक को स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का अवसर मिले। साथ ही बालक को कुछ समय के लिये पारिवारिक कार्यों से मुक्त रखा जाना चाहिए, नहीं तो सृजनात्मकता अवरूद्ध हो जायेगी।
(4) विद्यालय का वातावरण-
विद्यालय का वातावरण भी सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक होता है। विद्यालय में अगर जनतान्त्रिक वातावरण नहीं होता तथा छात्रों के मध्य शिक्षक द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो छात्रों में धनात्मक अभिवृत्ति का विकास नहीं हो पाता जिससे उनकी सृजनात्मकता अवरुद्ध हो जाती है। अतः आवश्यक है कि विद्यालय का वातावरण प्रजातान्त्रिक हो जिससे बालकों में धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास हो सके जो सृजनात्मकता के विकास में सहायक है।
(5) जिज्ञासा-
जिज्ञासा भी बालकों में सृजनात्मकता के विकास के लिए अहम कारक है। बालक अगर किसी बात को जानने की जिज्ञासा रखता है तथा उसकी जिज्ञासा शान्त नहीं की जाती अथवा उसे डाँट कर चुप करा दिया जाता है तो इससे उसकी सृजनात्मकता बाधित होती है। अतः आवश्यक है कि बालकों की जिज्ञासा को सन्तुष्ट किया जाये।
(6) समस्या समाधान व ज्ञान प्राप्ति का अवसर-
बालक को जितना समस्या समाधान का अवसर मिलता है उसके ज्ञान में उतनी ही वृद्धि होती है। ज्ञान वृद्धि से सृजनात्मकता प्रभावित होती है। साधारणतया उच्च बुद्धि के बालकों में उच्च सजनात्मक क्षमता पायी जाती है। अतः बालकों को यथासंभव उचित समस्या वाली परिस्थिति प्रदान की जानी चाहिए।
(7) उत्साहपूर्ण वातावरण पैदा करके ( Creating an encourage climate ) –
रचनात्मका का विकास करने के लिए खोज के अवसर प्रदान करने चाहिएं और ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिसमें बच्चा आने आपकों स्वतन्त्र समझें।
(8) बहुत से क्षेत्रों में रचनात्मकता को उत्साहित करना ( Encourage Creative in many medias ) –
अध्यापक विधार्थियों को इस बात के लिए उत्साहित करे कि जितने भी क्षेत्रों में सम्भव हो सके, अपने विचारों तथा भावनओं को प्रकट करे । प्रायः अध्यापक यह समझता है कि रचनात्मकता कविताएं, कहानियां, उपन्यास या जीवनियां लिखने तक ही सीमित है। वास्तव में और भी क्षेत्र हैं जैसा कि कला, चित्रकारी, शिल्प, संगीत या नाटक आदि जिसमें नए ढंग से बच्चों को अपने विचार प्रकट करने के लिए उत्साहित किया जा सकता है।
(9) विविधिता की प्रेरणा (Encouraging variety of approach ) –
अध्यापक को विविध उत्तरों को प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चों के कार्य तथा प्रयत्न में किसी परिवर्तन या विविधता के चिन्ह का स्वागत करना चाहिए और उसे प्रेरणा देनी चाहिए।
(10) लचीलता तथा सक्रियता को उत्साहित करना ( Encouraging activeness and flexibility ) –
अध्यापक को चाहिए कि वह सक्रियता तथा लचीलता को उत्साहित करे और बढ़ावा दे। बुद्धिमान बच्चे पढ़ाई की बहुत सी प्रभावी तथा कुशल विधियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार क सुन्दर अपवादों का स्वागत किया जाए तथा इनका अच्छी तरह मूल्यांकन किया जाए।
(11) आत्म विश्वास को उत्साहित करना ( Encouraging self trust ) –
अध्यापक बच्चों को अपने विचारों में विश्वास तथा सत्कार की भाक्ना के लिए उत्साहित करे। उसे चाहिए कि वह बच्चों के रचनात्मक चिन्तन का पुरस्कार उनके प्रश्नों का सत्कार करते हुए काल्पनिक विचारों के प्रति सम्मान प्रकट करके उनकी स्वाचालित पढ़ाई को प्रोत्साहन दे।
(12) श्रेणीं कृतियों के अध्ययन की प्रेरणा ( Encourage to study master pieces ) –
अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को श्रेष्ठ – कृतियां के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करे, उन्हें मौलिक रचना करने के लिए कहें, उन्हे बताए कि वे अपने अनुभवो को प्रयोग करने के लिए नए और अच्छे रूप पैदा करें।
(13) स्वयं भी एक रचनात्मक रूचियों वाला व्यक्ति हो ( Being a creative person one self ) –
एक प्राचीन स्वयं सिद्ध कथन है कि ( What a teacher does speaks more loudly then what he says ) रचनात्मक रूचियों वाला अध्यापक अपने विधार्थियों को अपने कार्य से चकित करता है और विधार्थियो को नवीनता का सत्कार करना सिखा सकता है। वह अध्यापक जो स्वयं सीख रहा है और अपने विषय क्षेत्र के ज्ञान को जानने का पूर्ण प्रयत्न कर रहा है, अपने शिष्य का अनुकरण करने के लिए एक नमूना प्रदान करता है|
समाप्त – The End
@@ @@@ @@@@ @@@
## #### ##### ### #####
^^ ^^^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^
- सृजनात्मकता के तत्व ,
- सृजनात्मकता के विशेषताएं ,
- सृजनात्मकता के प्रभावित करने वाले कारक ,
- srjanaatmakata ke tatv ,
- srjanaatmakata ke visheshataen ,
- srjanaatmakata ke prabhaavit karane vaale kaarak ,
- srjanaatmakata ke arth
- srjanaatmakata ke paribhaasha ,
- meaning of creativity definition of creativity,
- elements of creativity,
- Characteristics of creativity,
- Factors influencing creativity
- सृजनात्मकता के अर्थ परिभाषा तत्व विशेषताएं प्रभावित करने वाले कारक
- Srjanaatmakata Ke arth Paribhaasha Tatv Visheshataen Prabhaavit Karane Vaale Kaarak