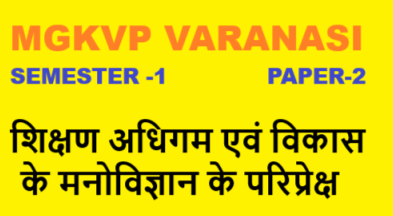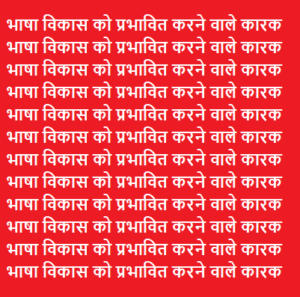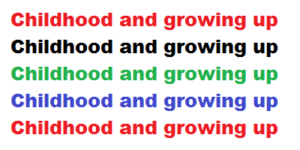शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष
shikshan adhigam evan vikaas ke manovigyaan ke paripreksh
| विषय | शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष |
| SUBJECT | shikshan adhigam evan vikaas ke manovigyaan ke paripreksh |
| SUBJECT | Perspectives from the psychology of teaching, learning and development |
| UNIVERSITY | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय |
| COURSE | बी.एड प्रथम सेमेस्टर |
| PAPER | २ |
| CODE | 102 |
| lnfo | इस पेज में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष सिलेबस , नोट्स एवं क्वेश्चन पेपर को शामिल किया गया है | |
VVI NOTES के इस पेज में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष सिलेबस , शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष नोट्स , शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष क्वेश्चन पेपर , शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष सीरिज , शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष प्रश्न उत्तर ,शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष गेस पेपर , शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष गाइड ,शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष बुक ,शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष प्रश्न ,शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष क्वेश्चन पेपर इत्यादी को सामिल किया गया है |
शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष सिलेबस
| विषय | शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष
shikshan adhigam evan vikaas ke manovigyaan ke paripreksh Syllabus |
| SUBJECT | Perspectives from the psychology of teaching, learning and development Syllabus |
| पेपर कोड | 102 |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय |
| कोर्स | बी.एड |
| सेमेस्टर | प्रथम सेमेस्टर |
| FULL MARKS | |
| lnfo | यहाँ महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के पेपर -102 शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष के सिलेबस दिया गया है | |
Unit-1
A. Educational Psychology: Meaning, Scope and its relevance. Individual
difference: Meaning, types, causes and educational implications.
B. Psychology of development: meaning of development, difference between development & growth, characteristics related to cognitive, social and emotional development during childhood & adolescence and their educational implications.
Unit-2
A. Psychology of learning: meaning, factors affecting learning, transfer of learning: meaning, types and its educational implications, Motivation: meaning, various techniques for motivating the students.
B. Theories of learning: Classical, Operant, Gestalt and Cognitive theory
of Piaget and Bruner, Main features and their educational implications.
Unit-3
A. Psychology of intelligence: meaning, concept, theories of intelligence: cognitive, associative and unitive. IQ, EQ and SQ: their implications for organizing teaching-learning processes. Use of intelligence tests and its limitations. Indian concept of intelligence.
B. Psychology of Adjustment: meaning, process of adjustment, characteristics of a well adjusted person. Stress: concept, coping mechanism and its educational implications for teacher & learner. Ensuring wellness life style: determinants of wellness and scales to measure wellness life style.
Unit-4
A. Psychology of personality : meaning, its Indian and Western conceptualizations; development of personality, measurement of personality.
B. Psychology of exceptional children: creative, gifted, slow learner and mentally retarded children, their characteristics and implications for providing education.
(2) शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष नोट्स
| विषय | शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष नोट्स
shikshan adhigam evan vikaas ke manovigyaan ke paripreksh Notes |
| SUBJECT | Perspectives from the psychology of teaching, learning and development Question- Answer |
| पेपर कोड | 102 |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय |
| कोर्स | बी.एड |
| सेमेस्टर | प्रथम |
| FULL MARKS | |
| lnfo | यहाँ महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के पेपर -102 शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष के नोट्स दिया गया है | |
लघु उत्तरीय प्रश्न
(Short Answer Type Questions)
निर्देश- प्रश्न संख्या 1 (a से j) लघु उत्तरीय प्रश्न है। परीक्षार्थियों को सभी दस प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। (10 × 4 = 40 अंक)
प्रश्न a (i) शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर –
शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति एवं स्वरूप विज्ञान पर आधारित है। मनोविज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को व्यावहारिक रूप में पुष्टि, इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। क्रो एवं क्रो के शब्दों में- “शिक्षा मनोविज्ञान को एक व्यावहारिक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि यह मानव व्यवहार के सम्बन्ध में वैज्ञानिक विधि से निर्धारित किये गये सिद्धान्तों एवं तथ्यों के अनुसार अधिगम की व्याख्या करने का प्रयास है।”
प्रश्न a (ii) शिक्षा में मनोविज्ञान के महत्त्व की विवेचना कीजिए।
उत्तर —
शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्त्व निम्न प्रकार से है। जॉन डीवी के कथनानुसार, “बगैर मनोविज्ञान के शिक्षा की कोई क्रिया नहीं चल सकती।” स्किनर का कथन है कि “शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है।” एक अन्य वैज्ञानिक के अनुसार, “शिक्षा की समस्या का व्यावहारिक समापन मनोविज्ञान से होता है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों का विकास तथा उन्नति मनोविज्ञान की सहायता से ही की जा सकती है। ”
प्रत्येक बालक का अपना अलग व्यक्तित्व होता है। इस कारण भी मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान है।
मॉण्टेसरी का कहना है कि “शिक्षक में जितना ही अधिक प्रयोगात्मक विज्ञान का ज्ञान होता है उतना ही अधिक उसमें पढ़ाने की योग्यता एवं क्षमता होती है।”
प्रश्न a (iii) शिक्षा मनोविज्ञान की समस्याओं की विवेचना कीजिए।
उत्तर –
शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं-
(1) मानवीय मूल्यांकन की समस्याएँ –
शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय छात्र होता है और उसका परीक्षण शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है। इस स्थिति में एक छात्र दूसरे छात्र के व्यवहारों को वैज्ञानिक नियमों के अनुकूल नियंत्रित करने में सदैव असमर्थ रहता है। दूसरी बात यह है कि हम चाहे जितना प्रयास कर लें, एक कुशल मनोवैज्ञानिक भी अपने आचार-विचार, भावना, बुद्धि, चातुर्य तथा व्यक्तित्व से परीक्षणदाता को प्रभावित करता है। अतः प्राप्त आँकड़ों की सत्यता संदिग्ध हो जाती है।
(2) मानवीय व्यवहार सम्बन्धी नैतिक सीमाएँ –
शिक्षा मनोविज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण सीमा है कि नवीन मानवतावादी दृष्टिकोण के अन्तर्गत बालक को पशु की भाँति कैद करके परीक्षण किये जाते हैं। अब इन परीक्षणों के विरुद्ध आवाज उठने लगी है जिससे कि कठिन प्रायोगिक परिस्थितियों में न तो इन प्रयोज्यों को रखा जा सकता है और न ही प्रयोग की वस्तु की भाँति समझा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत सीमित है।/
(3) शिक्षा सम्बन्धी समस्याएँ –
शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वोच्च सीमा है। उसकी सफलता शिक्षकों पर ही निर्भर करती है और यदि शिक्षक अपने कर्त्तव्य का उचित पालन नहीं कर पाता है तो इनकी उपयोगिता स्वयं समाप्त हो जाती है ।
(4) प्रयोगशाला सम्बन्धी समस्याएँ–
शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसके समस्त गुण धर्मों का प्रायोगिक परिस्थितियों में परीक्षण किया जाना आवश्यक है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगशालाओं का अभाव पाया जाता है। फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मौलिक अनुसंधानों की अपेक्षा करना व्यर्थ है।
प्रश्न a (iv) शिक्षा मनोविज्ञान के सम्बन्ध में अनुशासन का क्या स्थान है?
उत्तर—
शिक्षा को मनोविज्ञान से प्रभावित होने के कारण अब दमनात्मक अनुशासन के स्थान पर मुक्त्यात्मक अनुशासन को स्थान दिया जाने लगा है जिससे बालकों की अपनी रुचियों, अभिवृत्तियों, भावनाओं एवं विचारों को व्यक्त करने का पूर्ण अवसर दिया जाता है और उनमें ‘आत्म-अनुशासन’ की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। वर्तमान समय में अनुशासनहीनता की समस्याओं के कारणों को खोजकर मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्हें स्नेह, प्रशंसा, सहानुभूति, पुरस्कार आदि के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता है।
प्रश्न a (v) शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक की भूमिका बताइए ।
उत्तर –
शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रभाव के परिणामस्वरूप शिक्षक का स्थान एक मित्र, सहायक तथा निर्देशक के समान माना जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में बालक की स्थिति एक पौधे के समान तथा शिक्षक की स्थिति बालकरूपी पौधे का उपयुक्त विकास करने वाले माली के समान होती है। स्किनर ने कहा है, “शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ही आवश्यक उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण है कक्षा-शिक्षण एवं बालकों के दैनिक सम्पर्क में मनोविज्ञान का प्रयोग किये बिना वह अपने कार्य को कुशलता से सम्पन्न नहीं कर सकता है।
प्रश्न a (vi)अधिगम को प्रभावित करने वाले कोई तीन तत्त्व लिखिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ।
अथवा
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए ।
अथवा
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें।
उत्तर-
अधिगम को प्रभावित करने वाले तीन कारक हैं-
(1) शारीरिक तथा मानसिक वातावरण-
स्वस्थ व्यक्ति की ज्ञानेन्द्रियाँ तथा उसकी बुद्धि ठीक तरह कार्य करती है, जबकि इसके विपरीत यदि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ है तो वह सीखने के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। इसका कारण यह है कि ज्ञानेन्द्रियाँ तथा बुद्धि सीखने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। विद्यालयों में मध्यान्तर में विश्राम की व्यवस्था, पोषाहार देना, छात्रों में अच्छी आदत डालना ।
(2) अभिप्रेरणा –
अधिगम में ‘अभिप्रेरण’ का विशेष महत्त्व है। कक्षा में छात्रों की मानसिक क्रिया अधिक करने के लिए अभिप्रेरण की आवश्यकता होती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि छात्रों को सीखने के लिए अधिक मानसिक क्रियाओं पर बल देना चाहिए, जो शिक्षक अभिप्रेरण के माध्यम से कर सकता है। अतः यदि छात्रों को उचित अभिप्रेरण प्रदान किया जाय तो इन्हें अधिगम सबसे ज्यादा होगा। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की विधियों का प्रयोग समय तथा परिस्थिति के अनुसार कक्षा में करता है। ये प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं-
(अ) पुरस्कार व दण्ड-
प्रायः यह देखा है कि उचित स्थान पर तथा उचित समय पर प्रशंसा करना लाभकारी सिद्ध होता है। इसके विपरीत अवांछनीय कार्यों के लिए निन्दा करना भी सिद्ध हुआ है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि कमजोर तथा पिछड़े लोगों की निन्दा करना उत्साहवर्द्धक नहीं है। प्रशंसा निन्दा से अधिक उत्साहवर्द्धक होती है।
(ब) प्रतियोगिता-
हर छात्र में योग्य तथा बड़ा बनने की भावना उसके मस्तिष्क के किसी भी भाग में छिपी रहती है। प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र की इस भावना को जागृत कर सकते हैं तथा उसे पढ़ने के लिए तत्पर कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना होगा कि यह अभिप्रेरण छात्रों की सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए तथा स्वस्थ प्रतियोगिता ही उनके लिए हितकर है।
उपर्युक्त दोनों ही विधियों से अभिप्रेरणा छात्रों को दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा उनको कक्षा में अभिप्रेरित किया जा सकता है।
(3) उचित वातावरण-अधिगम और वातावरण का एक-दूसरे से निकट का सम्बन्ध है। यदि स्कूल अथवा परिवार का अच्छा, शान्त, स्नेहपूर्ण तथा रुचिकर वातावरण है तो बच्चा अपने कार्य को शीघ्र सीख लेता है। यदि विद्यालय का वातावरण दूषित वायुमण्डल में है, वहाँ खेलने और मनोरंजन की सामग्री का अभाव है और वहाँ ईर्ष्या, शत्रुता का वातावरण है तो इन परिस्थितियों में छात्र उपयुक्त मात्रा में सीख नहीं सकता है।
प्रश्न a (vii) पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त स्पष्ट कीजिए।
उत्तर—
पियाजे के सिद्धान्त के आधारभूत प्रत्यय – पियाजे के सिद्धान्त के कुछ आधारभूत प्रत्यय निम्न हैं-
(1 ) निर्माण और खोज –
बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय-समय पर खोज और निर्माण करते रहते हैं, जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यय नहीं किया होता है। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। नवीनता या खोज का उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। उदाहरणार्थ- एक चार साल का बालक विभिन्न आकार के बालकों को क्रमानुसार लगा देता है तो यह उसके बौद्धिक विवृद्धि की खोज और निर्माण से सम्बन्धित है।
(2) कार्य क्रिया का अर्जन-
कार्य क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार के मानसिक क्रम से है, जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणीयता है। प्रत्येक कार्य क्रिया का एक तर्कपूर्ण उद्देश्य होता है; उदाहरणार्थ – एक मिट्टी के चक्र को दो भागों में तोड़ना तथा दो टूटे हुए भागों को पुनः पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना एक कार्य क्रिया है। पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुँच जाता है तब तक वह भिन्न-भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न वर्गों में कार्य क्रियाओं का अर्जन करता रहता है एवं उसकी विकास अवस्था से दूसरी में पदार्पण के लिए निम्न दो तथ्य आवश्यक हैं-
(क) सात्मीकरण –
सात्मीकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित एक विचार या वस्तु किसी नये विचार या वस्तु का समावेश हो जाना। पियाजे के विचार से तात्पर्य बालक के प्रत्यक्षात्मक- गत्यात्मक समन्वय से है।
(ख) व्यवस्थापन तथा सन्तुलन स्थापित करना-व्यवस्थापन का अर्थ नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना है या अपने विचारों एवं क्रियाओं को नये विचारों एवं वस्तुओं में विद्यमान करना है। मानसिक विवृद्धि में सात्मीकरण और व्यवस्थापन में उपस्थित उत्पन्न तनाव का हल निहित होता है। यह तनाव नई परिस्थितियों में पुरानी अनुक्रियाओं के समय उत्पन्न होते हैं या उस समय उत्पन्न होते हैं जब बालक नयी अनुक्रियाओं को नवीन समस्याओं के समाधान में फिट करता है, जिससे उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार का व्यवस्थापन सन्तुलित कहलाता है।
प्रश्न a (viii) शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं क्या हैं?
उत्तर-
शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था–
पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है और पढ़ाने की तैयारी करता है। इस अवस्था में वे सभी क्रियायें आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था को ‘शिक्षण नियोजन व्यवस्था’ भी कहा जाता है। शिक्षण की इस व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षक शिक्षण-योजना का चयन करता है, उसका नियोजन करता है ताकि अभीष्ट उद्देश्यों को वह प्राप्त कर सके। इस समय शिक्षक अपने शिक्षण को सुनियोजित तथा सफल बनाने के लिए चिन्तन करता है, सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करता है और दूसरों से विचार-विमर्श करता है। इसलिए इसे प्रयात्नात्मक या करने की अवस्था भी कहते हैं। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है-
1. शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण-
शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व अपने अध्यापन के उद्देश्य निर्धारित करता है। वह उद्देश्यों को व्यावहारिक परिवर्तन के सन्दर्भ में परिभाषित करता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान, पूर्व व्यवहार तथा अनुभव, कक्षा स्तर, आयु, मानसिक योग्यताओं आदि के आधार पर वह उद्देश्य बनाता है।
2. पाठ्यवस्तु के सम्बन्ध में निर्णय लेना –
शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के पश्चात् शिक्षक उस पाठ्यवस्तु के सम्बन्ध में निर्णय लेता है जिसे वह विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करके उनके व्यवहार में परिवर्तन करना चाहता है। इस निर्णय को शिक्षक निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए लेता है-
(i) शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है?
(ii) विद्यार्थियों का पूर्व व्यवहार क्या है ?
(iii) विद्यार्थियों को उसे सीखने की आवश्यकता क्यों है ?
(iv) विद्यार्थियों को किस स्तर की प्रेरणा प्रभावशाली हो सकती है?
(v) पाठ्यवस्तु से सम्बन्धित ज्ञान का मूल्यांकन कौन-कौन सी विधियों द्वारा करें ?
3. प्रस्तुतीकरण के लिए पाठ्य-वस्तु के तत्त्वों की व्यवस्था-विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत पाठ्य-वस्तु के सम्बन्ध में निर्णय लेने के पश्चात् शिक्षक पाठ्य-वस्तु के अवयवों को तर्कपूर्ण एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करता है जिससे पाठ्य वस्तु की व्यवस्था सीखने के स्थानान्तरण में सहायक सिद्ध हो जाये।
4. शिक्षण युक्तियों का चुनाव-शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले ही इस बात का निर्णय करना चाहिए कि पाठ्य-वस्तु के किन-किन शिक्षण बिन्दुओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण के समय कौन-सी शिक्षण-युक्तियाँ, प्रविधियाँ, उदाहरण तथा सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा? कक्षा में कब प्रश्न करेगा, व्याख्यान देगा और किस समय कौन-सी श्रव्य-दृश्य सामग्री का प्रयोग करेगा ? शिक्षक को पहले से योजना बना लेनी चाहिए कि वह शिक्षण कैसे और किन प्रविधियों के माध्यम से करेगा।
5. शिक्षण युक्तियों का विवरण-शिक्षक को यह भी निश्चित करना चाहिए वह कक्षा शिक्षण के समय किन-किन विधियों तथा प्रविधियों का कब और कैसे प्रयोग करेगा? दूसरे शब्दों में वह कब और किस प्रकार का प्रश्न विद्यार्थियों से पूछेगा ? कब और कहाँ चार्ट अथवा मानचित्र का प्रयोग करेगा? कब भाषण देगा? कब और कैसे श्यामपट्ट का प्रयोग करेगा तथा कब मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा ? आदि आदि ।
व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न b (i) व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धान्त
उत्तर-
व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धान्त–
व्यक्तित्व के अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिकों ने किया है। सिद्धान्तों की भिन्नता का आधार व्यक्तित्व के सम्बन्ध में बनाई गई आधारभूत मान्यताओं का अन्तर है। व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख प्रकार सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-
(i)शरीर रचना सम्बन्धी सिद्धान्त-कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के रूप, रंग, आकार तथा शरीर के गठन के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या तथा वर्गीकरण किया है। इस सिद्धान्त की पृष्ठभूमि जीव विज्ञान से प्रभावित है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक शैलडन महोदय थे। उन्होंने शरीर रचना एवं व्यक्तित्व के बीच सम्बन्ध स्थापित किए और पाया कि दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है ।
(ii) मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त- इस सिद्धान्त के प्रवर्तक फ्रॉयड थे। उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में अपना अनूठा व्यापक सिद्धान्त दिया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त के प्रतिपादन में अचेतन, हृदं अहं तथा अत्यहं आदि प्रत्ययों को आधार माना गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार पानी में तैरते हुए बर्फ का केवल 1/9 भाग ऊपर रहता है और बाकी 8/9 भाग पानी में डूबा रहता है उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क का 1/9 भाग चेतन अवस्था और बाकी भाग अचेतन अवस्था में रहता है। फ्रॉयड के अनुसार मनुष्य का अचेतन मन अधिक महत्त्वपूर्ण एवं जटिल होता है। इनके अनुसार अचेतन अनेक अनजानी परन्तु शक्तिशाली व जीवन्त शक्तियों का संचय होता है जो व्यक्ति के चेतन व्यवहार पर नियन्त्रण रखता है।
(iii) विशेषक सिद्धान्त-व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धान्त का प्रतिपादन कैटिल ने किया है। उसने व्यक्तियों के गुण एवं विशेषताओं आदि का सांख्यिकीय विधि से कारक विश्लेषण किया तथा कुछ सामान्य गुणों को ज्ञात किया जिसे व्यक्तित्व विशेषक कहते हैं। संवेगात्मक स्थिरता, बुद्धि सामाजिकता आदि कुछ कारक कैटिल ने सुझाये हैं।
है
(iv) माँग सिद्धान्त – इस सिद्धान्त का प्रतिपादन मुरे ने किया है। इस सिद्धान्त की मान्यता कि मनुष्य अपनी अन्तर्निहित आवश्यकताओं तथा बाहरी दबावों के कारण उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। माँग दबाव की परिस्थिति हमेशा व्यक्ति में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न करती रहती है। फलतः व्यक्ति नये-नये कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तथा वह अपने पुराने उद्देश्यों को भी बनाये रखता है। मुरे के अनुसार, “व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के दबावों को समग्र रूप उसके अन्दर कुछ माँगों को उत्पन्न करता है और ये माँगें ही व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती हैं।” मुरे ने इन माँगों को व्यक्तित्व माँग का नाम दिया। उन्होंने लगभग चालीस इस प्रकार की माँगों का पता लगाया। मुरे के अनुसार, “कोई माँग मानव मस्तिष्क की एक परिकल्पित शक्ति है जो व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण, अन्तर्बोध तथा मानसिक-शारीरिक क्रियाओं को इस प्रकार संगठित करती है कि वह व्यक्ति असन्तुष्टि की परिस्थिति से निकल सके।” मुरे द्वारा बताई गई माँगों में कुछ माँगें इस प्रकार हैं जैसे, प्रदर्शन की माँग, सानिध्य की माँग, परोपकार की माँग, स्वायत्तता की माँग, सम्प्राप्ति की माँग आदि।
प्रश्न b (ii) विस्मरण के शैक्षिक निहितार्थ को समझाइए ।
उत्तर-
विस्मृति कम करने के उपाय —
किसी बात की कम विस्मृति का अर्थ है-उसे अधिक समय तक स्मरण रखने या स्मृति में धारण रखने (Retention) की क्षमता न होना। अतः विस्मृति को कम करने या धारण-शक्ति में उन्नति करने के लिए निम्नांकित उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है-
1. पाठ की विषय-वस्तु – कोलेसनिक का मत है- पाठ की विषय-वस्तु अर्थपूर्ण, क्रमबद्ध और बालक की मानसिक योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की विषय-वस्तु की विस्मृत की गति और मात्रा बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त, पाठ में आवश्यकता से अधिक तथ्य, तिथियाँ और विस्तृत सूचनाएँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी विस्मृति की गति और मात्रा बहुत तीव्र होती है।
2. पूरे पाठ का स्मरण-बालक को पूरा पाठ सोच-समझकर याद करना चाहिए। जब तक उसे पूरा पाठ याद न हो जाय, तब तक उसे स्मरण करने का कार्य स्थगित नहीं करना चाहिए। साथ ही उसे पाठ को आंशिक रूप से स्मरण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाठ का भूल जाना आवश्यक है।
3. पाठ का अधिक स्मरण-पाठ स्मरण हो जाने के बाद भी बालक को उसे कुछ समय तक और स्मरण करना चाहिए। इसका कारण बताते हुए नन ने लिखा है- “पाठ स्मरण’ हो जाने के बाद जितना अधिक स्मरण किया जाता है, उतना ही अधिक वह स्मृति में धारण रहता है।”
4. बालक का स्मरण करने में ध्यान-पाठ को स्मरण करते समय बालक को अपना पूर्ण ध्यान उस पर केन्द्रित रखना चाहिए। वुडवर्थ के शब्दों में इसका कारण यह है कि-“सीखने वाला जितना अधिक ध्यान देता है, उतनी ही जल्दी वह सीखता है और बाद में उतनी ही अधिक देर में वह भूलता है।”
5. अधिक समय तक स्मरण रखने का विचार-बालक को पाठ यह विचार करके स्मरण करना चाहिए कि उसे उसको बहुत समय तक याद रखना है। तभी वह उसे शीघ्र भूलने की सम्भावना का अन्त कर सकता है। बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वील्ड ने लिखा है- “अधिक समय तक स्मरण रखने के विचार से याद किया हुआ पाठ अधिक समय तक स्मरण रहता है।”
प्रश्न b (iii) वृद्धि और विकास के सिद्धान्त को समझाइए ।
है।
उत्तर-
अभिवृद्धि का अर्थ
वृद्धि और विकास शब्दों को कई बार पर्यायवाची रूप में प्रयोग कर लिया जाता है क्योंकि इन दोनों शब्दों का सम्बन्ध गर्भाधान के समय से लेकर मानव में आये परिवर्तनों की व्याख्या करने से होता । इन परिवर्तनों में शिक्षा एवं वातावरण का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। इन दोनों शब्दों का प्रयोग सीखने से सम्बन्धित कर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या की जाती है। वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शरीर, आकार, भार आदि में वृद्धि के सन्दर्भ में किया जाता है। इस वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों और शरीर की साधारण वृद्धि भी शामिल होती है। इस प्रकार की वृद्धि की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसका मापन किया जा सकता है तथा इसका आकलन भी किया जा सकता है।
विकास का अर्थ
विकास का अर्थ बालक के कद या भार में परिवर्तन होने से नहीं है, विकास में एक निश्चित क्रम होता है जो बालक को परिपक्वता की ओर बढ़ाता है। इसमें प्रगति निहित होती है। बालक की प्रगति उसके भविष्य को निश्चित करती है। अतः निश्चित परिवर्तनशील प्रगति को ही विकास माना जाता है। जैसा मुनरो महोदय ने लिखा है, “परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था, जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है।”
हरलॉक के अनुसार, “विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा इसके प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएँ और नवीन योग्यताएँ प्रकट होती हैं।”
प्रश्न b (iv) किशोरावस्था में बौद्धिक विकास सम्बन्धी विलक्षणताओं को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
किशोरावस्था में मानसिक विकास शारीरिक विकास की अपेक्षा कुछ विलम्ब से होता है। पूर्ण किशोरावस्था में बुद्धि का विकास कुछ मन्द रहता है। किशोरावस्था के अन्तिम चरण (17 से 19 वर्ष) में बुद्धि का तीव्र गति से विकास होता है। वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की अवस्था में अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। वह विकास 14 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच अधिक होता है। इस अवस्था में किशोर में ध्यान केन्द्रित करने की शक्ति, क्षमता, चिन्तन, कल्पना शक्ति तथा विभिन्न प्रकार की रुचियाँ, लड़कियों में सुन्दर बनने, नृत्य, संगीत, नाटक, कविता, रेडियो सुनना एवं लड़के में स्वस्थ बनने, विभिन्न प्रकार के खेलों तथा लड़के और लड़कियों की एक-दूसरे में रुचि उत्पन्न हो जाती है। किशोर के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, परिवार का वातावरण, माता-पिता की शिक्षा, समाज, शारीरिक स्वास्थ्य, विद्यालय, शिक्षक, वंशानुक्रम आदि हैं।
प्रश्न b (v) किशोरों की क्या समस्याएँ हैं?
उत्तर –
किशोरावस्था की संवेगात्मक तथा सामाजिक समस्याएँ निम्न प्रकार हैं-
(1 ) अस्त-व्यस्त मनोदशा – किशोर की मनोदशा अस्त-व्यस्त रहती है। उसमें अनेक गलत बातों की स्पष्टता दिखायी देती है, जैसे-कठोरता, उद्दण्डता, कल्पना आदि।
(2) अपराधी प्रवृत्ति – किशोर समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगते हैं। वे नशीली वस्तुओं का भी प्रयोग करने लगते हैं।
(3) अनियन्त्रित व्यवहार – किशोरावस्था में प्रजनन अवयवों की तीव्रता से वृद्धि तथा विकास उसके व्यवहार को चिड़चिड़ा बना देता है तथा क्रोध, घृणा और उदासीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में किशोर स्वयं अपने व्यवहार पर नियन्त्रण नहीं रख पाता है।
(4) स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेने में कठिनाई-किशोर को स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेने के अवसर प्रदान नहीं किये जाते हैं, जिनके कारण उसे मानसिक कष्ट होता है।
प्रश्न b (vi) किशोरावस्था की आवश्यकताएँ बताइए।
उत्तर-
किशोरावस्था की आवश्यकताएँ
1. सुरक्षा व स्वतंत्रता के बीच सन्तुलन की आवश्यकता होती है
2. ऊर्जा व संवेग को प्रयोग हेतु कई कार्यों व कारणों की आवश्यकता होती है।
3. बालक व बालिकाओं के लिए अलग स्वास्थ्य व चुस्त-दुरुस्त रहने हेतु शारीरिक शिक्षा के प्रोग्राम की आवश्यकता होती है।
4. इस अवस्था में संगीत, नृत्य आदि की आवश्यकता होती है।
5. किशोर को करीब आठ घण्टे सोने की आवश्यकता होती है।
प्रश्न c (i) व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है?
अथवा व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ
उत्तर-
व्यक्तिगत भिन्नता मानव के व्यक्तित्व सम्बन्धी विभिन्न गुणों की भिन्नता है। प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व अनेक गुणों के द्वारा निर्मित होता है। ये गुण अथवा विशेषताएँ विभिन्न विधियों के माध्यम से मापी जा सकती हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नताओं में उन सभी गुणों अथवा विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें मापा जा सकता है तथा जिनके आधार पर व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग किया जाता है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है- “औसत समूह के मानसिक, शारीरिक विशेषताओं के सन्दर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता अथवा अन्तर को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं।”
प्रश्न c (ii) पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं?
अथवा
पिछड़े बालक के सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
पिछड़े बालक –
बर्ट के अनुसार “अपनी विद्यालयी शिक्षा के बीच जो बालक अपनी उम्र के लिए सामान्य से नीचे की कक्षा का कार्य करने में अक्षम होता है, पिछड़ा बालक होता है।”
पिछड़ा बालक न तो औसत होता है और न ही मन्द बुद्धि होता है। ऐसा बालक कक्षा में बार- बार समझाने पर भी समझ नहीं पाता व कक्षा का सामान्य कार्य भी नहीं कर पाता है।
स्कोनेल एवं स्कोनेल के अनुसार “पिछड़ा बालक अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में शैक्षिक रूप से पिछड़ापन दर्शाते हैं।”
प्रश्न c (iii) पिछड़े बालक के लक्षण एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए ।
उत्तर-
पिछड़े बालक के लक्षण / विशेषताएँ
इन बालकों में सामान्य बालकों से भिन्न कुछ लक्षण पाये जाते हैं। ये लक्षण निम्न हैं-
(1) इन बालकों की अधिगम गति मन्द होती है।
(2) विद्यालयी अनुभवों का वे ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते।
(3) उनकी अकादमिक उपलब्धि नगण्य होती है।
(4) असफलता के कारण वे सांवेगिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं और उनमें कुण्ठा का जन्म हो जाता है।
(5) वे असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं।
प्रश्न c (iv) बुद्धि के सिद्धान्त की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
उत्तर-
एक सत्तात्मक सिद्धान्त-इस सिद्धान्त के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक कार्यों के मूल में होती है। इस सिद्धान्त के समर्थक बुद्धि को एक अखण्ड व अविभाज्य इकाई मानते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण होगा। इस सिद्धान्त के समर्थक डॉ० जॉनसन का मानना है कि महान् वैज्ञानिक न्यूटन एक महान् कवि भी बन सकते थे यदि वे कविता करने की ओर अपना ध्यान लगाते। विभिन्न परीक्षणों ने सिद्ध कर दिया है कि यदि मनुष्य किसी एक कार्य को अच्छी तरह कर लेता है तो यह आवश्यक नहीं कि वह दूसरे कार्यों को भी अच्छी तरह कर सके।
बहुकारक सिद्धान्त-इस सिद्धान्त के प्रतिपादक थार्नडाइक हैं। इस सिद्धान्त में बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है, जिसमें कई योग्यताएँ निहित हैं। व्यक्ति को किसी भी बौद्धिक क्रिया में विभिन्न कारक मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। थार्नडाइक ने बुद्धि के सामान्य कारक को स्वीकार नहीं किया बल्कि इसके बदले बौद्धिक योग्यता में निहित विशिष्ट क्रियाओं को मान्यता दी।
संघ सत्तात्मक सिद्धान्त – इस सिद्धान्त के प्रतिपादक बिने हैं। बुद्धि का निर्माण कई प्रकार की शक्तियों से मिलकर होता है। ये शक्तियाँ हैं-प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना आदि। ये शक्तियाँ एक-दूसरे से पूर्णतया भिन्न होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धान्त को दोषपूर्ण बताया है तथा कहा कि मानसिक शक्तियाँ अन्योन्याश्रित हैं।
द्विसत्तात्मक सिद्धान्त – द्विसत्तात्मक सिद्धान्त के प्रतिपादक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार बुद्धि में दो कारक माने जाते हैं-एक सामान्य कारक व दूसरा विशिष्ट कारक। सामान्य कारक जन्मजात होता है और सभी क्रियाओं में पाया जाता है। वह कारक मनुष्य में सदैव ही एवं एक समान रहता है। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य कारक की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है।
प्रश्न c (v)किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए।
उत्तर-
विकास की अवस्थाओं में किशोरावस्था, बाल्यकाल तथा युवावस्था का सन्धि काल है। इस अवस्था में बालक अपने को बालक नहीं समझता, बड़े लोग उसे बड़ा नहीं समझते। इसलिए वह संक्रमण काल की अवस्था में रहता है।
किशोरावस्था अंग्रेजी शब्द एडोलेसैंस से विकसित हुआ है, इस शब्द का अर्थ है- परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। स्टेनले हॉल ने इस अवस्था के बारे में कहा है- “किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है।”
जरशील्ड के अनुसार, “किशोरावस्था, विकास की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था में प्रवेश करता है।” ई० किलपेट्रिक ने कहा है, “इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है।” कुछ विद्वान् किशोरावस्था को अटपटी तथा समस्याओं की अवस्था मानकर चलते हैं। बिग्गी तथा हस्ट ने कहा है, “किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त करनेवाला
एक शब्द परिवर्तन है। यह परिवर्तन शरीरक्रिया वैज्ञानिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है।”
किशोरावस्था मानद का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। प्रत्येक मानव को इस अवस्था से गुजरना पड़ता है।
प्रश्न : c(vi) “किशोरावस्था प्रबल दबाव तथा तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। ” इस कथन की विवेचना कीजिए ।
अथवा
किशोरावस्था को तूफानी अवस्था क्यों कहते हैं?
अथवा
किशोरावस्था तनाव की अवस्था है।’ स्पष्ट करें।
उत्तर-
किशोरावस्था मानव विकास की प्रमुख एवं सन्धिकाल की अवस्था है जिसमें अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप बालक का सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही बदल है। किशोरावस्था के विषय में हैडो कमेटी ने इस प्रकार कहा है- ” 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार शुरू हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार को बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाय एवं इसकी शक्ति तथा धारा के साथ-साथ नयी यात्रा प्रारम्भ की जाय तो हमारा विचार है कि यह सौभाग्य की ओर ले जायगी।” स्टेनले हॉल ने इस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था बताया है। जर्सील्ड के अनुसार, “किशोरावस्था में मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर बढ़ता है। ”
किशोरावस्था के परिवर्तन के विषय में मनोवैज्ञानिकों ने (1) क्रमिक तथा (2) त्वरित विकास की धारणाओं का विकास किया है। क्रमिक विकास की धारणा के अन्तर्गत किशोरावस्था में विकास धीरे-धीरे होता है। थार्नडाइक के अनुसार, “किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन एकदम न होकर धीरे-धीरे होते हैं।” किंग के अनुसार, “एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के बाद होता है किन्तु पहली ऋतु में दूसरी के आने के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। इसी प्रकार बालक की अवस्थाएँ भी एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं।” त्वरित विकास की धारणा के अन्तर्गत स्टेनले हॉल ने यह मत प्रतिपादित किया कि किशोरावस्था में होनेवाले परिवर्तन एकाएक प्रकट होते हैं। हॉल के अनुसार, “किशोरों के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन एकदम छलांग मारकर आते हैं। ”
प्रश्न c (vii)वृद्धि एवं विकास में अन्तर कीजिए।
अथवा
अभिवृद्धि एवं विकास में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।
अथवा
वृद्धि एवं विकास में विभेद कीजिए।
उत्तर-
वृद्धि एवं विकास के अन्तर को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं-
1. वृद्धि शब्द तादाद या परिमाण सम्बन्धी
परिवर्तनों (Quantitative Changes) के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ आकार, लम्बाई, ऊँचाई और भार आदि में होनेवाले परिवर्तन को वृद्धि कहकर पुकारते हैं।
2. वृद्धि एक तरह से सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है। विकास के परिमाण और तादाद सम्बन्धी पक्ष के परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है।
3. वृद्धि शब्द व्यक्ति के शरीर के किसी भी अवयव तथा व्यवहार के किसी भी पहलू होने वाले परिवर्तनों को प्रकट कर सकता है।
4. वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक द्वारा परिपक्वता (Maturity) ग्रहण करने के साथ-साथ यह समाप्त हो जाती है
5. वृद्धि के फलस्वरूप होनेवाले परिवर्तन बिना कोई विशेष प्रयास किये दृष्टिगोचर हो सकते हैं। साथ ही इन्हें भली-भाँति मापा भी जा सकता है।
विकास
1. विकास शब्द वृद्धि की तरह केवल परिमाण सम्बन्धी परिवर्तनों को व्यक्त न कर ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है।
2. विकास शब्द अपने-आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका ही एक भाग है। यह व्यक्ति में होनेवाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है।
3. विकास किसी एक अंग-प्रत्यंग में अथवा व्यवहार के किसी एक पहलू में होने वाले परिवर्तनों को नहीं, बल्कि व्यक्ति में आनेवाले सम्पूर्ण परिवर्तनों को इकट्ठे रूप में व्यक्त करता है।
4. विकास एक सतत प्रक्रिया (Continuous Process) है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर समाप्त न होकर यह आजीवन चलती है।
5. विकास शब्द कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आनेवाले गुणात्मक परिवर्तनों (Qualitative Changes) को भी प्रकट करता है। इन परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप में मापना कठिन नहीं है। इन्हें केवल अप्रत्यक्ष तरीकों, जैसे-व्यवहार करते हुए बालक का निरीक्षण करना आदि से ही मापा जा सकता है।
प्रश्न c (viii) एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं?
अथवा
बालकों को अभिप्रेरित करने वाली तकनीकों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
उत्तर-
शिक्षा में अभिप्रेरणा प्रदान करने की विधियाँ
शिक्षण-कार्य की सफलता के लिए शिक्षक को बालकों को सीखने व ज्ञानार्जन के लिए अभिप्रेरणा देनी चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने इसके लिए अनेक विधियाँ बतायी हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं-
(1) बालकों की रुचियों का अध्ययन-बालकों को पढ़ाने से पूर्व उनकी रुचियों का अध्ययन करना चाहिए तथा उन्हीं रुचियों के अनुकूल उन्हें विषयों को पढ़ाना चाहिये तथा विषयों के पढ़ाने में शिक्षण-विधि का प्रयोग करना चाहिए।
( 2 ) स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास – बालकों को अधिकाधिक ज्ञानार्जन तथा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिये प्रेरित करने हेतु उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता या ईर्ष्या एवं द्वेष से रहित प्रतियोगिता का विकास करना चाहिए। इस सन्दर्भ में वॉगन एवं डिसरेन ने कहा है, “शिक्षाशास्त्र के सम्पूर्ण इतिहास में प्रतियोगिता को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिये प्रयोग किया गया है।”
(3) प्रशंसा-बालकों की उनके अच्छे कार्यों के लिये हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। इससे उन्हें अभिप्रेरणा प्राप्त होती है।
(4) प्रोत्साहन पढ़ने-लिखने व अच्छे व्यवहार तथा आचरण के लिये छात्रों को उनके समक्ष महान पुरुषों, विद्वानों तथा वैज्ञानिकों के उदाहरण प्रस्तुत कर प्रोत्साहन प्रदान करते रहना चाहिए।
(5) स्पष्ट एवं आकर्षक लक्ष्य छात्रों को सीखने या अध्ययन के लिये अभिप्रेरित करने हेतु उनके समक्ष शिक्षा के लक्ष्यों को स्पष्ट एवं आकर्षक बनाकर रखना चाहिए।
(6) पुरस्कार-किसी अच्छे कार्य के लिये किसी छात्र को पुरस्कार देने से उसे आगे के लिये तो अभिप्रेरणा मिलती ही है इससे पुरस्कृत छात्र को देखकर अन्य छात्रों को भी अच्छे कार्यों की अभिप्रेरणा मिलती है।
(7) दण्ड- कभी-कभी अच्छे कार्यों के लिये अभिप्रेरित करने के लिए दण्ड की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन दण्ड मनोवैज्ञानिक दण्ड देना चाहिए वरना दण्डित छात्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
प्रश्न d. (i) व्यक्तित्व के मापन हेतु प्रयुक्त किसी एक प्रक्षेपी तकनीकी का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
रोर्शा का स्याही-धब्बा परीक्षण-इस परीक्षण की रचना स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन दोश ने सन् 1921 में की थी। यह परीक्षण सबसे अधिक सफल परीक्षण माना जाता है। यह परीक्षण निम्न प्रकार से किया जाता है-
(i) परीक्षण सामग्री- इस परीक्षण में दस कार्ड होते हैं। इन कार्डों पर रचनाहीन स्याही के धब्बों जैसी आकृतियाँ बनी होती हैं। इन दस कार्डों में से पाँच कार्डों पर बिल्कुल काली आकृतियाँ, दो कार्डों पर काली तथा लाल आकृतियाँ तथा शेष तीन कार्डों पर भिन्न-भिन्न आकृतियाँ होती हैं। सभी
कार्डों की आकृतियाँ कोई विशेष अर्थ नहीं रखतीं ।
(ii) परीक्षण का आयोजन – जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना होता है, उस व्यक्ति को ये दस कार्ड एक-एक करके दिये जाते हैं व उस कार्ड पर तथा छपी आकृति के बारे में उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया को नोट किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि उस कार्ड की आकृति उन्हें किस प्रकार की लगती है या उन्हें उस आकृति में क्या दिखाई दे रहा है। प्रत्येक कार्ड को देखने के लिए व्यक्ति जितना समय चाहता है, उसे उतना ही समय दिया जाता है। इस कार्ड को वह व्यक्ति किसी भी कोण से देख सकता है, एक ही कोण से देखने का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।
इन आकृतियों को देखकर मनुष्य की प्रतिक्रियाओं, उसके कार्डों को पकड़ने का ढंग तथा चेहरे के भावों का लेखा-जोखा रखा जाता है।
प्रश्न d (ii) शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएँ दीजिए।
अथवा
शिक्षा मनोविज्ञान की भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणा में अन्तर बताइए ।
उत्तर –
शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएँ –
1. “शिक्षा मनोविज्ञान का सम्बन्ध मानवीय व्यवहार के अध्ययन, मानवीय, व्यक्तिगत, उसके विकास और शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया के निर्देशन से है। ”
2. “शिक्षा-मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन है।”
3. “शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक वातावरण के सन्दर्भ में शिक्षार्थियों या विशिष्ट व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन है । ”
क्रो एण्ड क्रो- “शिक्षा मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक अधिगम सम्बन्धी अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है।”
आर. एच. भाटिया- “शैक्षणिक वातावरण में छात्रों या व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं।”
डॉ. माथुर-“शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक ज्ञान है जो शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करता है।”
शिक्षा मनोविज्ञान की भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणा में यह अन्तर है कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान सम्पूर्ण जीवन से जोड़कर देखते हैं, जबकि भारतीय मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का अहम् पहलू मानते हैं।
प्रश्न d (iii) शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए।
अथवा
शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में लिखिए।
अथवा
शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
अथवा
शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र।
उत्तर-
किसी भी विज्ञान अथवा शास्त्र के व्यवस्थित एवं सही अध्ययन के लिए आवश्यक है कि उस विज्ञान के विषय क्षेत्र का सही-सही निर्धारण किया जाय। विषय-क्षेत्र के सही निर्धारण के बाद सम्बन्धित शास्त्र का अध्ययन करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है।
शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ सम्बन्धी विवेचना द्वारा स्पष्ट है कि इस विज्ञान के अन्तर्गत शैक्षिक वातावरण में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस स्थिति में स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अनेक उन तथ्यों का भी अध्ययन किया जाता है, जिनका अध्ययन मुख्य रूप से सामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है, परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तथ्यों का भी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है।
प्रश्न d (iv) अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता बताइए ।
अथवा
शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापकों के लिए क्या उपयोग है?
अथवा
शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है?
उत्तर-
अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता
अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है-
(1) शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है।
(2) शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बाल- स्वभाव तथा व्यवहार के ज्ञान से परिचित कराता है।
(3) शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन बनाये रखने के मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है।
(4) शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक् दृष्टिकोण प्रदान करता है।
(5) शिक्षा मनोविज्ञान मापन तथा मूल्यांकन की नवीन विधियों से अध्यापक को परिचित कराता है।
प्रश्न d (v) शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता।
अथवा
शिक्षा मनोविज्ञान की एक शिक्षा के लिए क्या प्रासंगिकता है?
उत्तर-
शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता —
शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करनेवाला विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य
के बारे में उन तथ्यों का पता लगाता है जिससे कि वह अपनी परिस्थितियों की सहायता से अपनी आन्तरिक शक्तियों का अधिकतम विकास कर ले। इसके उद्देश्यों को देखने से पता चलता है कि यह विषय न केवल शिक्षार्थी और शिक्षक बल्कि शिक्षा के प्रशासक, अधिकारी, प्रबन्धक, शिक्षा समिति के सदस्य और अभिभावकों के लिए अत्यन्त उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह शिक्षा का एक सबल आधार है।
अध्यापक की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता – अध्यापक को अपने अध्ययन कार्य में शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता मिलती है। इससे उसे कई लाभ होते हैं जो नीचे दिये जा रहे हैं-
(1) अध्यापक विद्यार्थी के स्वभाव, गुण, शक्ति, रचना आदि की जानकारी करने में लाभ उठाता है।
(2) अध्यापक विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास की स्थितियों को जानने और तद्नुकूल शिक्षा देने में लाभ उठाता है।
(3) अध्यापक विद्यार्थी को उसके पर्यावरण के साथ समुचित ढंग से अनुकूलन और समायोजन करने में सहायता देता है। यह भी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता कही जाती है।
(4) अध्यापक विद्यार्थी के व्यक्तित्व सम्बन्धी भिन्नताओं को समझता है और उसके विकास में योगदान देता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान के कारण सम्भव है।
(5) अध्यापक अपने-आपको शिक्षा मनोविज्ञान से समझता है और विद्यार्थी के साथ अच्छा व्यवहार करता है तथा अपने कार्य को सरल एवं सफल बनाता है।
प्रश्न d (vi) पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त के शैक्षिक निहितार्थ को समझाइए |
उत्तर –
पियाजे के सिद्धान्त तथा अनुसन्धान का शिक्षण में बहुत महत्त्व है। वह खोज द्वारा सीखने को बल देते हैं। उनके सिद्धान्त यह स्पष्ट कर देते हैं कि सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जबकि विद्यार्थी की रुचि और कौतूहल के अनुरूप होता है। अतएव पाठ्यक्रम इत्यादि इस प्रकार बनाना चाहिए कि जो सिखाया जाना है, उसमें रुचि और कौतूहल में पूर्ण तालमेल हो ।
पियाजे की खोजों में यह निहित है कि औपचारिक सीखने की स्थितियों में उस सीमा तक सफलता मिलने की आशा है जिस तक कि वह सीखने के प्रकार की है जो प्राकृतिक रूप से होता है।
विभिन्न आयु पर जो ज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें तथा विद्यालय के अनुभवों में तालमेल लाने के लिए पियाजे के अनुसन्धान निम्न सुझाव प्रस्तुत करते हैं-
सर्वप्रथम विद्यार्थी संवेदनात्मक-गामक काल में और मूर्त संक्रिया के काल के प्रारम्भ में मुख्य रूप से खेल और छानबीन द्वारा सीखते हैं। वह कुछ शाब्दिक तथा ज्ञानात्मक नमूने भी प्राप्त कर लेते हैं किन्तु यह बहुत अल्प ढंग से ही समावेशित होते हैं। ऐसे स्तर पर बालकों को यथावत् संप्रत्यय सामग्री को, जैसी कि बहुधा हम अपने विद्यालय के पाठ्यक्रम में पाते हैं, समझने में कठिनाई होती है। संप्रयात्मक चिन्तन की तैयारी के काल में भी वह ऐसी सामग्री को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। अतएव इन आयु-स्तर पर हमें चाहिए कि बालकों को भरा-पूरा एवं प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करें जो बालकों को छानबीन कर सीखने को प्रोत्साहित करे।
बाद के स्तरों पर पियाजे के अनुसार बालक औपचारिक शिक्षण से अधिक लाभान्वित हो सकता है। यह लगभग उसी प्रकार का शिक्षण होगा जो विद्यालयों में दिया जाता है। अतएव हम कह सकते हैं कि पियाजे का सिद्धान्त खोज कर सीखने को बल देता है किन्तु साथ ही साथ यह पढ़ने- लिखने और गणित को एक-दूसरे से विलग करके शिक्षण देने पर भी बल देता है। यह वैसा ही शिक्षण है जैसे कि वर्तमान विद्यालयों में दिया जा रहा है। रटने और अभ्यास की विधियों पर इस प्रकार के शिक्षण में बल दिया जाता है। इस तरह से पियाजे के सिद्धान्त में शिक्षण के लिए ये निहिताएँ हैं कि प्रारम्भ में बालकों को खोज इत्यादि से सिखाने पर बल दिया जाये फिर जैसे-जैसे वह बड़ा होता जाय, उसे अधिक ज्ञानात्मक शिक्षण दिया जाये।
प्रश्न e (i) बुद्धि से आप क्या समझते हैं?
अथवा
मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गयी बुद्धि की चार परिभाषाएँ लिखिए।
उत्तर-
बुद्धि का अर्थ व परिभाषा —
प्रायः यह सुनने में आता है कि वह मनुष्य अधिक बुद्धिमान अथवा उसकी बुद्धि अधिक तेज है या वह व्यक्ति कम बुद्धि अथवा मन्द बुद्धि का है। प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में बुद्धि क्या है व उसका स्वरूप क्या है। यहाँ पर हम बुद्धि के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गयी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे जिनके आधार पर बुद्धि का अर्थ ज्ञात किया जा सकता है-
स्टर्न के शब्दों में, “जीवन की नवीन अवस्थाओं एवं समस्याओं के अनुसार समायोजन करने की शक्ति बुद्धि है।”
वर्ट के अनुसार, “बुद्धि एक स्वाभाविक प्रकृतिदत्त मानसिक योग्यता है।”
विने के अनुसार, “किसी समस्या को समझने, उसका हल निकालने, अपने परिस्थिति विशेष के अनुकूल बनाने तथा आत्म-आलोचना करने की योग्यता का सामूहिक रूप बुद्धि है । ”
थर्स्टन के शब्दों में, “बुद्धि में शाब्दिक आगमन, तर्क शक्ति, निगमन्तर तर्कशक्ति, स्मरण शक्ति, वाक्शक्ति, वस्तु प्रेक्षण शक्ति, संख्या की गणना तथा प्रतिबोधक गति सम्मिलित है।”
थार्नडाइक ने कहा है, “उत्तम अनुक्रिया करने एवं नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजित करने की योग्यता ही बुद्धि है।”
प्रश्न e (ii) गेने ने सीखने के बारे में कितनी बातें बतायी हैं?
अथवा
गेने द्वारा प्रस्तुत अधिगम के अधिक्रम का विवरण दीजिये।
उत्तर-
(1) सीखना व्यवहार में परिवर्तन है-हम वह क्रिया सीखते हैं, जो हमें नहीं आती। जब हमें वह क्रिया आ जाती है तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है।
(2) मानव के संस्कार तथा उसकी कार्यक्षमता में परिवर्तन होता है-जब किसी व्यवहार को कोई सीखने वाला सीखता है तो वह व्यवहार अनुभवजन्य होने के कारण संस्कार बन जाता है।
(3) प्रदर्शन तथा निलम्बन की क्षमता-अधिगम में भी परिवर्तन होता है। प्रायः यह देखा गया है कि साक्षात्कार या प्रयोगात्मक परीक्षा में अभ्यर्थी अपना सम्पूर्ण श्रेष्ठ प्रभाव छोड़ देता है परन्तु . जब वह अपने कार्य पर लगता है तो उसमें साक्षात्कार जैसी कार्य-कुशलता के दर्शन नहीं होते।
(4) परिपक्वता से आये परिवर्तन सीखना नहीं है-गेने की धारणा का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन होते हैं, वे सीखना या अधिगम नहीं कहलाते।
सीखना, मानव विकास की अनिवार्यता है। जो व्यक्ति जितना शीघ्र सीखता है, उतना ही विकसित माना जाता है। वुडवर्थ के शब्दों में, “एक क्रिया सीखना कही जा सकती है जहाँ तक कि वह व्यक्ति को अच्छे-बुरे, किसी भी प्रकार से विकसित करती है और उसके अनुभवों तथा परिवेश को पहले से भिन्न बताती है।” हिलगार्ड ने इसी आधार पर सीखने की व्याख्या की है-“सीखना वह क्रिया है जिससे कोई क्रिया आरम्भ होती है अथवा सामना की गई परिस्थिति से प्रतिक्रिया के द्वारा परिवर्तित की जाती है बशर्ते क्रिया में परिवर्तन के लक्षण स्वाभाविक प्रतिक्रिया की प्रवृत्तियों अथवा जीव की अस्थायी दशाओं के आधार पर न समझायी जा सके। इसलिये सीखना मानव विकास की पहली शर्त है । ”
प्रश्न e (iii) सृजनात्मक बालक की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
सृजनात्मक बालक की प्रवृत्ति प्रत्येक बालक में पायी जाती है। समाज के अन्तर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्य एवं व्यवसाय में उनकी रचनात्मकता देखने को मिलती है। जैसे—बढ़ई लकड़ी से मनचाही मेज बना सकता है, चित्रकार मनचाहे रंगों से नवीन कलाकृति की रचना करता है। कवि, कविता रचता है और गीतकार गीत रच सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में सृजन की सम्भावनायें होती हैं और उनका विकास किया जाना चाहिए।
सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रियेटिविटी का पर्यायवाची है। इसके समान्तर विधायिकता उत्पादकता शब्दों का प्रयोग होता है। उत्पादकता में प्राडक्टीविटी का बोध होता है जो किसी वस्तु के उत्पादन का आभास कराता है। विधायिकता में एकत्रीकरण का बोध होता है। एक और शब्द- खोज, इसे डिस्कवरी के सन्दर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। ये सभी शब्द सृजनात्मकता के इर्द-गिर्द घूमते हैं और उस आशय को पूरा नहीं करते। सृजनात्मकता के बिल्कुल समानान्तर शब्द भी है। सृजन शून्य का भाव है और सृजन में विद्यमान में से नवीनता की, मौलिकता की सृष्टि करनी पड़ती है। डॉ० कामिल बुल्के ने क्रियेटिव शब्द के समानान्तर अर्थ- सृजनात्मकता, रचनात्मक सृजक बताये हैं। भारत सरकार के तकनीकी कोश में क्रियेटिविटी को सृजनशीलता कहा गया है। डॉ० रघुवीर ने क्रियेट का अर्थ-सृजन, उत्पन्न करना, सर्जन करना, बनाना कहा है।
सृजनात्मक का अर्थ मौलिकता से लिया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रास्ट के अनुसार – “मौलिकता क्या है?” यह मुक्त साहचर्य है । जब कविता की पंक्तियाँ या उसके विचार आपको उद्वेलित करते हैं, आपको साधारण कारण के लिए बाध्य करते हैं, यह दो वस्तुओं का सम्बन्ध होता है, परन्तु आप साहचर्य को देखने की कामना नहीं करते, आप तो उसका आनन्द उठाते हैं।
इसी प्रकार मेडेनिक ने कहा है- “सृजनात्मकता चिन्तन में साहचर्य के तत्त्वों का मिश्रण रहता है जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संयोगशील होते हैं या किसी अन्य रूप में लाभदायक होते
नवीन संयोग विचार जितने कम होंगे, सृजनात्मकता की सम्भावना उतनी ही अधिक होगी।
प्रश्न e (iv) बुद्धि के स्पीयरमैन के सिद्धान्त का विवेचन कीजिए ।
उत्तर-
स्पीयरमैन कृत द्वि-कारक सिद्धान्त- इस सिद्धान्त के समर्थक स्पीयरमैन थे। इनके अनुसार प्रत्येक प्रकार की क्रिया में एक सामान्य तत्त्व ‘G’ (General) होता है जो सभी क्रियाओं में विद्यमान नहीं..
रहता।
इस प्रकार ‘सामान्य बुद्धि’ नाम की कोई चीज अवश्य है जो सभी क्रियाओं में विद्यमान रहती है और उसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट समस्याओं का सामना करता है। उदाहरणस्वरूप का किसी व्यक्ति की हिन्दी की योग्यता में कुछ तो उसकी सामान्य बुद्धि होती है और कुछ भाषा सम्बन्धी ‘विशिष्ट योग्यता’ होती है अर्थात् G+s1 या गणित में उसकी योग्यता का कारण होगा G + s2 ।
इस प्रकार कई विशिष्ट योग्यताएँ हो सकती हैं। ‘G’ तत्त्व न्यूनाधिक रूप से सभी विशिष्ट क्रियाओं में विद्यमान रहता है। इस प्रकार इस व्यक्ति की पूर्ण बुद्धि (जिसे यदि ‘A’ की संज्ञा दी जाय) को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है- G+s1, + so2 + S3 + ….=A
स्पीयरमैन कृत इस द्वि-कारक सिद्धान्त की विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना हुई है।
(i) स्पीयरमैन के कथनानुसार ‘बुद्धि’ को प्रकट करनेवाले दो तत्त्व होते हैं परन्तु जैसा कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है, इसमें दो नहीं बल्कि कई तत्त्व होते हैं। (G, S1, S2, S3, आदि)।
(ii) स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक कार्य में कुछ विशिष्ट योग्यता का होना आवश्यक है। परन्तु यह धारणा उचित नहीं जान पड़ती क्योंकि इसका यह अर्थ हो जाता है कि विभिन्न कार्यों में एक ‘सामान्य तत्त्व’ के अतिरिक्त और कुछ भी सामान्य नहीं होता और नर्सिंग कम्पाउण्डर तथा डॉक्टर के व्यवसाय को एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता। वास्तव में S1, S2, S3, S4 …. के तत्त्व एक-दूसरे से अलग नहीं होते। ये एक-दूसरे की सीमा को पार करके कई सामान्य तत्त्वों को जन्म देते हैं।
प्रश्न e (v) बुद्धि-लब्धि क्या है? उचित उदाहरण द्वारा इसके सूत्र को निर्धारित कीजिए।
अथवा
एक व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष है और मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धि-लब्धि निकालिए।
उत्तर-
किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा की मात्रा को व्यक्त करना बुद्धि-लब्धि द्वारा ही सम्भव है। अर्थात् बुद्धि-लब्धि किसी व्यक्ति की मानसिक अभिवृद्धि की मात्रा या उपलब्धि को व्यक्त करती है। बुद्धि-लब्धि ज्ञात करने के लिये मानसिक आयु में वर्षायु से (वास्तविक आयु) भाग देकर 100 से गुणा कर देते हैं।
बुद्धि-लब्धि = मानसिक आयु वर्षायु /(वास्तविक आयु) × 100 = 16/20*100=80
बुद्धि-लब्धि = 80
= MA/CA*100
जैसे यदि किसी 10 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 11 वर्ष है तो उसकी बुद्धि-लब्धि 110
बुद्धि-लब्धि =11/10*100
प्रश्न e (vi) बुद्धि के दो तत्त्व सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
दो तत्त्व सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन महोदय ने किया। उनके अनुसार बुद्धि का निर्माण निम्नलिखित दो तत्त्वों से होता है-
(i) सामान्य तत्त्व-सुविधा की दृष्टि से इसे ‘G’ Factor (General Factor) भी कहा जाता है। यह वह तत्त्व है जो व्यक्ति की समस्त क्रियाओं में निहित होता है। इसी तत्त्व के प्रभाव से व्यक्ति विभिन्न कार्यों के सम्पादन में सफल होता है। भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने अथवा कार्यों को करने में सामान्य तत्त्व ही सहायक होता है। यह तत्त्व सभी लोगों में समान रूप से पाया जाता है और जन्म से ही प्राप्त होता है।
(ii) विशिष्ट तत्त्व- इस तत्त्व को सुविधा के लिए ‘S’ factor (Specific Factor) भी कहा जाता है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए जिसमें विशेष बुद्धि एवं निपुणता की जरूरत पड़ती है उसमें विशिष्ट तत्त्व सहायक होता है। उदाहरण के लिए कला-कौशल, शिल्प आदि में सिद्धहस्तता एवं तकनीकी विषयों में निपुणता अथवा विशेषता ‘S’ Factor के द्वारा ही प्राप्त होती है। यह तत्त्व सभी व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न रूप में पाया जाता है। प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग विशिष्ट तत्त्व होते हैं। जिस व्यक्ति में किसी कार्य से सम्बन्धित अधिक ‘S’ Factor पाये जाते हैं तो वह व्यक्ति उस कार्य विशेष में अधिक निपुण हो जाता है। व्यक्ति में यह तत्त्व जन्मजात न होकर अर्जित किया हुआ होता है।
प्रश्न (vii) शिक्षा में बुद्धि परीक्षण का उपयोग बताइए।
अथवा बुद्धि परीक्षण की शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
बुद्धि परीक्षण की शैक्षिक उपयोगिता- शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश में तो कम लेकिन दूसरे देशों में बुद्धि परीक्षण का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसी के आधार पर विद्यालय में प्रवेश, वर्गीकरण, मार्गदर्शन आदि संभव होता है। हम नीचे इनकी उपयोगिता पर विचार कर रहे हैं-
1. बुद्धि परीक्षणों के आधार पर विद्यार्थियों का चुनाव सरलता से किया जाता है।
2. इसकी सहायता से विद्यार्थियों का वर्गीकरण अच्छी तरह से किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण करके विद्यार्थियों की बुद्धि के अनुसार अच्छी शिक्षा व्यवस्था की सकती है।
4. विद्यार्थियों की बुद्धि-लब्धि जानकर उसके अनुसार शिक्षा विधि और योजना भी करते हैं।
5. विद्यार्थियों के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करके उन्हें जीवन में सफलता के साधन बताये जा सकते हैं।
6. शैक्षणिक मार्ग-प्रदर्शन देना इन परीक्षणों की सहायता से ही हो सकता है। इससे पढ़ाई- लिखाई की कठिनाई दूर की जा सकती है।
7. व्यावसायिक मार्ग-प्रदर्शन विशिष्ट योग्यता को पता लगा कर दी जाती है जो इन परीक्षणों के द्वारा होता है।
8. छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता जानकर इन्हें छात्रवृत्ति भी देते हैं जिससे वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।
प्रश्न (viii) संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं?
उत्तर-
समायोजन करने की योग्यता के रूप में बालक के संवेगात्मक समायोजन और स्थिरता की दिशा में बुद्धि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस सम्बन्ध में मेल्टजर ने अपने विचार प्रकट करते लिखा है- “सामान्य रूप से अपनी ही उम्र के कुशाग्र बालकों की अपेक्षा निम्न बुद्धि स्तर के बालकों में कम संवेगात्मक संयम पाया जाता है। विचार शक्ति, तर्क शक्ति आदि मानसिक शक्तियों के सहारे ही व्यक्ति अपने संवेगों पर अंकुश लगाकर उनको अनुकूल दिशा देने में सफल हो सकता है। अतः प्रारम्भ से ही बालकों की मानसिक शक्तियाँ, बालकों के संवेगात्मक विकास को दिशा प्रदान करने में लगी रहती है। ”
प्रश्न f (i) विकलांग बालक का क्या अर्थ है? ये कितने प्रकार के होते हैं? विकलांग बालकों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए?
उत्तर-
विकलांग बालक का अर्थ-
विकलांग बालक उस बालक को कहते हैं जो जन्म से या किसी दुर्घटना के कारण किसी अंग से विहीन हो गया हो या उसका अंग ठीक से कार्य न कर रहा हो। शरीर के किसी अंग या उसमें कार्यक्षमता के अभाव में बालक को जीवन के सामान्य कार्यों को करने में कुछ कठिनाई का अनुभव होने लगता है। शिक्षा प्राप्त करने में भी वह अभाव बाधक हो सकता है, लेकिन संवेगात्मक असन्तुलन तो वह उत्पन्न कर ही देता है
विकलांग बालकों के प्रकार-
विकलांग बालक कई प्रकार के होते हैं, उनकी मुख्य श्रेणियाँ इस प्रकार हैं-
(1) अंगहीन, (2) बहरे और आंशिक बधिर, (3) अन्धे और आंशिक अन्धे, (4) वाणी-दोषयुक्त, (5) कोमल, (6) मिरगी ग्रस्त ।
विकलांगों की शिक्षा-उपर्युक्त सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में असुविधा होती है। इनकी शिक्षा का विशेष प्रबन्ध होना चाहिए –
(1) अंगहीन की शिक्षा,
(2) श्रवण-दोष युक्त बालकों की शिक्षा,
(3) दृष्टि-दोष युक्त बालकों की शिक्षा,
(4) वाणी-दोषयुक्त बालकों की शिक्षा,
(5) कोमल बालकों की शिक्षा,
(6) मिरगी के रोग वाले बालकों की शिक्षा ।
इनकी शिक्षा से सम्बन्धित विचारणीय दशाएँ इस प्रकार हैं-
(1) सरलता एवं सुविधा, (2) समरूपता या एकरूपता, (3) रोचकता, (4) शीघ्रता, (5) यथार्थता अथवा प्रतिपन्नता, (6) ध्यान का अभाव, (7) परिवर्तन में विरोध ।
विकलांग बच्चों की शिक्षा के प्रसंग में कुछ नियम तथा सिद्धान्त ध्यान देने योग्य हैं,
जैसे- (1) संकल्प की दृढ़ता का नियम, (2) प्रथम अवसर के प्राप्त करने का नियम, (3) संलग्नता का नियम, (4) अभ्यास का नियम, (5) स्नायु-विज्ञानवादी विचारधारा, (6) मनोविश्लेषणवादी ।
प्रश्न f (ii) मन्द बुद्धि बालक की विशेषताएँ तथा उनके लिए शिक्षा का स्वरूप बताइए।
अथवा
मन्द बुद्धि बालकों की शिक्षा हेतु प्रमुख सुझावों को बताइए।
अथवा
सीखने में अक्षम बालकों की क्या विशेषताएँ होती हैं?
अथवा
शिक्षण योग्य मंदितमना बालकों को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए?
अथवा
मानसिक मन्द बालकों की क्या विशेषताएँ हैं?
अथवा
मन्द अधिगामकों की क्या विशेषताएँ हैं?
उत्तर-
मन्द बुद्धि बालक-मन्द बुद्धि बालक वे होते हैं, जिनमें औसत से कम मानसिक योग्यता होती है। ऐसे बालकों की बुद्धि-लब्धि साधारण बालकों की बुद्धि-लब्धि से कम होती है। क्रो एवं को के अनुसार, “जिन बालकों की बुद्धि-लब्धि 70 से कम होती है, उन्हें मन्द बुद्धि बालक कहा जाता है।” स्किनर के अनुसार, “जो छात्र एक वर्ष का निर्धारित पाठ्यक्रम वर्ष भर में पूरा कर लेते हैं, वे सामान्य छात्र कहलाते हैं और जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते, वे मन्दबुद्धि छात्रों की श्रेणी में आते हैं।”
मन्द बुद्धि बालक की विशेषताएँ-
मन्द बुद्धि बालक की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं-
(1) इसकी बुद्धि-लब्धि 50 से 75 के मध्य होती है।
(2) विद्यालय के सामान्य कार्य को अन्य बालकों के समान पूरा करने की क्षमता का अभाव।
(3) किसी कार्य के परिणामों की चिन्ता किये बिना भावना के आवेग में आकर कार्य करना।
(4) कठिन या जटिल समस्याओं को ठीक प्रकार से न समझना।
(5) आत्मविश्वास की कमी।
मन्द बुद्धि बच्चों की शिक्षा-
मन्द बुद्धि बालकों की शिक्षा का स्वरूप वही होना चाहिए, जैसा कि पिछड़े बालकों के लिए होता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है-
(1) मन्द बुद्धि बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षक के लिए पर्याप्त धैर्य रखना आवश्यक है।
(2) उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए।
(3) उन्हें आत्म-मूल्यांकन करने का प्रशिक्षण दिया जाय।
(4) उन पर कुछ उत्तरदायित्व भी डाले जाय।
(5) उन्हें उचित निर्णय लोने का प्रशिक्षण दिया जाय।
प्रश्न f (iii) प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? इनकी विशेषताएँ बताइए ।
उत्तर-
प्रतिभाशाली बालक
1. टरमन व ओडम- “प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व में लक्षणों, विद्यालय-उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं।”
2. क्रो एवं क्रो – “प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं–
(i) वे बालक, जिनकी बुद्धि-लब्धि 130 से अधिक होती है और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं।
(ii) वे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में से एक या अधिक में विशेष योग्यता रखते हैं।”
प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएँ
निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त बालक को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं-
1. बुद्धि परीक्षाओं में उच्च बुद्धि-लब्धि (130+से 170+तक)
2. सामान्य अध्ययन में रुचि ।
3. सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता ।
4. विशाल शब्द कोश
5. अमूर्त विषयों में रुचि ।
6. मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता ।
7. आश्चर्यजनक अन्तर्दृष्टि का प्रमाण ।
8. विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता ।
9. अध्ययन में अद्वितीय सफलता।
10. पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि ।
प्रश्न f (iv)व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं?
उत्तर-
व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ –
वैयक्तिक भिन्नता से अभिप्राय है- प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अन्तर पाया जाना। इसी अन्तर के कारण व्यक्ति, दूसरे से भिन्न माना जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में 19वीं सदी में फ्रांसिस गाल्टन, पियर्सन, कैटेल, टर्मन आदि ने व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया तथा उनके कारणों की खोज की। स्किनर के शब्दों में, “बालक भी प्रत्येक सम्भावना के विकास का एक विशिष्ट काल होता है। यह काल वैयक्तिक भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न अवधि का होता है। यदि उचित समय पर इस सम्भावना को विकसित करने का प्रयत्न न किया गया तो उसके नष्ट हो जाने का भय रहता है।”
कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। यहाँ तक कि जुड़वाँ बच्चों में भी असमानता पायी जाती है। इस दृष्टि से वैयक्तिक भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है।
स्किनर ने लिखा है, “व्यक्तिगत विभिन्नता में सम्पूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है, जिसका माप किया जा सकता है।”
स्किनर की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की इस परिभाषा के अनुसार उनमें व्यक्तित्व के वे सभी पहलू आ जाते हैं, जिनका माप किया जा सकता है। माप किये जा सकने वाले ये पहलू कौन-से हैं, इनके सम्बन्ध में टायलर ने लिखा है, “शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति सम्बन्धी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। ”
प्रश्न f (v) व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।
उत्तर-
व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अन्तर- दोनों प्रकार के परीक्षणों की तुलना करने पर हमें उनमें निम्नलिखित अन्तर दिखायी पड़ते हैं—
व्यक्तिगत परीक्षण
1. एक समय में केवल एक व्यक्ति की जाँच हो सकती है।
2. छोटी-बड़ी सभी आयु के लिए उपयुक्त है।
3. इसमें समय और धन भी अधिक लगता है।
4. इसके प्रयोग के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति की जरूरत होती है।
5. यह परीक्षण अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक होता है।
सामूहिक परीक्षण
1. एक समय में बहुत से व्यक्तियों की जाँच हो सकती है।
2. छोटी आयु या सीमित आयु तक के लिए अधिक उपयुक्त है।
3. इसमें समय और धन कम लगता है।
4. इसका प्रयोग कुछ मनोविज्ञान का ज्ञान रखनेवाला कर सकता है।
5. यह अपेक्षाकृत कम विश्वसनीय एवं प्रामाणिक होता है।
प्रश्न g (i) “किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है।” स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
जी० स्टेनले हाल का मानना है कि “किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन का वह काल है, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का नया जन्म होता है।” इस दशा में बालक में तीव्र शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों की तीव्रता के कारण ही हाल ने इस अवस्था को तूफान व दबाव का काल कहा है। इस अवस्था में किशोरों में अस्थिरता, सांवेगिकता व अनिश्चितता का बाहुल्य पाया जाता है जिसके फलस्वरूप उनमें असामान्यता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। किलपैट्रिक का मानना है-“इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है।” इस अवस्था में अनोखे शारीरिक, मानसिक व सांवेगिक परिवर्तन होते हैं। अतः यह अवस्था कभी-कभी समस्यात्मक बन जाती है। इस अवस्था में होनेवाले परिवर्तन से अवगत होते हुए भी माता- पिता कभी उसको बालक समझते हैं तो कभी प्रौढ़ तथा उसी के अनुरूप व्यवहार भी करते हैं। कभी- कभी उससे प्रौढ़-जैसा कार्य करने की अपेक्षा करते हैं और न कर पाने पर उसे ताड़ना देते हैं कि तुम इतने बड़े हो गये हो फिर भी यह काम नहीं कर सकते हो। बड़ों के समान जब वह कार्य करता है तो उसे यह कहकर डाँट दिया जाता है कि तुम अभी बच्चे हो। इस प्रकार का व्यवहार किशोर को असमञ्जस में डाल देता है।
|
प्रश्न g (ii)विकास की विभिन्न अवस्थाएँ क्या हैं? उनका नाम अवधि के साथ दीजिए।
अथवा
आयु के अनुसार मानव विकास की अवस्थाओं के नाम लिखिए।
उत्तर-
बालक का विकास यूँ तो हम गर्भावस्था से कह सकते हैं किन्तु देखा जाये तो उसका वास्तविक विकास जन्म लेने के पश्चात् ही होता है। विकास की प्रक्रिया में बालक को कुछ सोपानों या अवस्थाओं में होकर गुजरना पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों में इस सम्बन्ध में मतभेद अवश्य है किन्तु विकास की अवस्थाओं में सबका विश्वास है। हमारे प्राचीन ग्रन्थों-भरतकृत ‘स्मृति’ और श्रीमद्भगवत में विकास की अवस्थाओं का वर्णन है। पाश्चात्य शिक्षाशास्त्री रूसो ने विकास को चार अवस्थाओं में विभक्त करने का प्रारम्भिक प्रयास किया था। डॉ0 अरनैस्ट जोन्स के अनुसार विकास की निम्न चार अवस्थाएँ हैं-
1. शैशवावस्था- जन्म से 5 वर्ष तक ।
2. बाल्यावस्था- 6 से 12 वर्ष तक ।
3. किशोरावस्था- 13 से 18 वर्ष तक ।
4. प्रौढ़ावस्था- 19 वर्ष से उपरान्त ।
प्रश्न g (iii) बुद्धि की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर—
(i) यह व्यक्ति का जन्मजात गुण एवं शक्ति है।
(ii) यह अमूर्त चिन्तन की योग्यता देती है।
(iii) यह विभिन्न बातों को सीखने में मदद करती है।
(iv) यह व्यक्ति की कठिन समस्याओं तथा जटिल परिस्थितियों को सरल बनाती है।
(v) इस पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है।
(vi) व्यक्ति को अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है।
(vii) व्यक्ति को नयी दशाओं से सामञ्जस्य करने का गुण प्रदान करती है।
(viii) व्यक्ति को अच्छे-बुरे, उचित-अनुचित, सही- गलत, नैतिक-अनैतिक कार्यों में भेद की योग्यता देती है।
(ix) बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यान्तर तक ही होता है।
(x) लिंग-भेद के कारण लड़कों तथा लड़कियों की बुद्धि में बहुत ही कम अन्तर होता है।
प्रश्न g (iv) ‘प्रयत्न-भूल’ और ‘सूझ’ द्वारा सीखने में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
प्रयत्न-भूल और सूझ में निम्नलिखित अन्तर है-
1. प्रयत्न एक शारीरिक क्रिया है और सूझ मानसिक क्रिया है।
2. सीखने की दृष्टि से पहले मानसिक क्रिया होती है तत्पश्चात् शारीरिक ।
3. जिस क्रिया में केवल शरीर के अंग कार्य करते हैं वह प्रयत्न, जिसमें केवल मस्तिष्क कार्य करता है वह सूझ और जिसमें शरीर और मस्तिष्क दोनों ही कार्य करते हैं वह इन दोनों का मिश्रित रूप, उसे भूल एवं प्रयत्न भी कह सकते हैं।
4. ‘प्रयत्न और भूल’ द्वारा सीखी हुई बात में स्थायित्व कम होता है और ‘सूझ’ द्वारा सीखी हुई बातों में स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है।
5. छोटी आयु में ‘प्रयत्न और भूल’ द्वारा सीखने का सिद्धान्त कार्य करता है तथा मानसिक विकास के साथ-साथ बड़ी आयु में ‘सूझ’ द्वारा सीखने का सिद्धान्त ।
प्रश्न g (v) थार्नडाइक के अधिगम के नियमों का वर्णन कीजिए।
अथवा
थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के तीन नियम कौन-कौन से हैं?
अथवा
थार्नडाइक के सीखने के नियम को स्पष्ट कीजिए ।
अथवा
थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के तीन नियम कौन-कौन से हैं?
अथवा
थार्नडाइक के अधिगम सिद्धान्त के शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन कीजिए।
उत्तर —
थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने (अधिगम) के तीन नियम-
1. तत्परता का नियम- जब मनुष्य सीखने की तीव्र इच्छा करता है तो वह शीघ्र सीख जाता है, साथ ही साथ उसे सीखने में आनन्द भी मिलता है।
कक्षा में प्रश्न करते समय शिक्षकों को केवल उन्हीं बालकों से प्रश्न करने चाहिए जो उत्तर देने के लिए तैयार हों। चतुर और मनोवैज्ञानिक अध्यापक इस परिस्थिति का निराकरण बड़ी सरलता से कर सकता है।
2. अभ्यास का नियम- इस नियम के दो भाग हैं- उपयोग और अनुपयोग। किसी कार्य को बार-बार करने से उसे करने की आदत पड़ जाती है। अभ्यास छोड़ देने से आदत भूलती जाती है। अतः अभ्यास सीखने के लिए आवश्यक है। अभ्यास के नियम का तात्पर्य यह हुआ कि शिक्षक को उपयुक्त अवसर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में अभ्यास देते रहना चाहिए। शिक्षकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बालक कभी गलत बात का अभ्यास न करे, नहीं तो गलत बात के बैठ जाने से उससे पीछा छुड़ाना सरल न होगा।
3. प्रभाव का नियम- इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। जिन कार्यों से हमें आनन्द मिलता है उन्हें हम सीख लेते हैं, इसके विपरीत कष्टदायक कार्य हम नहीं सीख पाते हैं। अभिभावक तथा अध्यापकों को इस नियम का प्रयोग मनोवैज्ञानिक सावधानी के अनुसार करना चाहिए।
प्रश्न h (i) ‘प्रयास एवं त्रुटि से सीखना’ विधि को समझाइए ।
अथवा
अधिगम सिद्धान्तों के शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन कीजिए।
उत्तर –
सर्वप्रथम जब हम कोई नवीन वस्तु को सीखने का प्रयास करते हैं तो हम एकाएक नहीं सीख जाते। हमको कई बार प्रयास करना पड़ता है और कई बार हम भूलते हैं, अन्त में क्रमशः हम सीख जाते हैं।
प्रयास एवं त्रुटि से सीखने की विधियाँ-
(1) अनायास प्रक्रिया का होना।
(2) असंतोषजनक प्रतिक्रियाओं की अवहेलना।
(3) स्थानापन्न उत्तेजना।
(4) स्थानापन्न प्रतिक्रिया ।
(5) प्रतिक्रिया का मिश्रण ।
शिक्षा में उपयोगिता –
(1) प्रयास एवं त्रुटि की विधि में बहुत शक्ति की आवश्यकता है।
(2) इस विधि से बहुत देर में सफलता मिलती है।
(3) यह विधि गणित, ग्रामर आदि के लिए अच्छी सिद्ध होती है।
(4) बहुत छोटे बच्चों के लिए एवं मन्द बुद्धि बालकों के लिये इस विधि की उपयोगिता अधिक है।
(5) यह विधि शिक्षकों को कम उपयोग में लाना चाहिए।
प्रश्न h (ii) पॉवलव के ‘सम्बन्ध प्रतिक्रिया सिद्धान्त’ का वर्णन कीजिए।
अथवा
पॉवलव के अनुबंध सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
प्राचीन अनुबंधन सिद्धान्त का जन्मदाता रूसी शरीर विज्ञानशास्त्री पॉवलव है, जिसने सबसे पहले उद्दीपक और अनुक्रिया के सम्बन्ध में अनुबंधन के द्वारा व्यक्त किया है। इस सिद्धान्त का सम्बन्ध शरीर विज्ञान से है। इस सिद्धान्त पर व्यवहारवादियों का विशेष विश्वास है।
जब कोई स्वाभाविक अनुक्रिया कृत्रिम या अस्वाभाविक उद्दीपन के द्वारा होने लगे तो इसे अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। इस अनुबंधित अनुक्रिया में स्वाभाविक उद्दीपन का प्रतिस्थापन अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपन से हो जाता है। जैसे-मांस को देखकर कुत्ते के मुँह से लार टपकना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, किन्तु यदि मांस को दिखाने के साथ-साथ घण्टी बजाने का क्रम भी चलता रहे तो कुछ दिन के बाद केवल घण्टी की ध्वनि पर ही कुत्ता लार टपकाना सीख जाता है। कुत्ते का लार टपकना घण्टी की ध्वनि से जो अस्वाभाविक उद्दीपन है, सम्बन्धित हो जाता है। इस प्रकार घण्टी की ध्वनि सुनकर लार टपकना अनुबंधित अनुक्रिया है। दूसरे शब्दों में, भोजन के लिए कुत्ता घण्टी की ध्वनि से अनुबंधित हो गया।
प्रश्न h (iii) गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम के सन्दर्भ में किसी एक प्रयोग का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
पूर्ण विधि-गेस्टाल्टवादी प्रत्यक्षीकरण को महत्त्व देते हैं। ये मानते हैं कि बालक जो कुछ भी सीखता है वह पूर्ण रूप से सीखता है। अतः छात्रों को समस्या का पूर्ण ज्ञान कराना आवश्यक है। समाधान तो वह स्वयं खोज लेंगे। कुछ विद्वान् इस विधि को मेधावी छात्रों के लिए ही उपयुक्त मानते हैं।
प्रश्न h (iv) ‘सीखने में पठार’ से आप क्या समझते हैं?
उत्तर-
सीखने में पठार का अर्थ- जब हम कोई चीज सीखते हैं तो सीखने में हमारी क्रमशः उन्नति नहीं हुआ करती है। इस विधि में प्रतिदिन उन्नति करते चले जाते हैं, पर कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि हम उतनी उन्नति के साथ नहीं सीख पा रहे हैं, जितनी कि पहले सीखते थे। इस प्रकार सीखने की उन्नति में रुकने को पठार कहते हैं।
पठारों के कारण –
डब्ल्यू0 डब्ल्यू0 क्रूज का कहना है कि पठार आने के कारण रुचि का अभाव, समझने की कमी, गलत विधि, आदतों का पुनर्संगठन, थकान आदि हो सकते हैं। हालिंग बर्थ के अनुसार पठारों के कारण पठारों के कारण –
(1) विद्यार्थी का परिश्रम करना छोड़ना,
(2) गलत पद्धति को अपनाना,
(3) निरुत्साह होना ।
मोटे तौर पर पठार आने के कुछ कारण दिये जा रहे हैं-
1. ज्ञानावरोध – बालक जब किसी चीज को सीखता है तो उसका ज्ञान विकसित होता है, परन्तु एक सीमा वह आ जाती है कि अधिक ज्ञानार्जन उसके लिए असम्भव हो जाता है। इस प्रकार के अवरोध को ज्ञानावरोध कहते हैं।
2. उत्साहावरोध – सीखते-सीखते उत्साह की क्रमशः कमी हो जाती है। कार्यक्षमता भी कम हो जाती है।
3. शारीरिक क्षमतावरोध – मनुष्य मनः शारीरिक प्राणी है। शारीरिक क्षमता की कुछ सीमा हुआ करती है। जब शारीरिक क्षमता की सीमा पूर्ण हो जाती है तो यह स्वाभाविक है कि मानसिक क्षमता भी कम हो जाती है।
प्रश्न h (v)’अन्तर्दृष्टि द्वारा सीखने’ के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।
अथवा
अधिगम के गेस्टाल्टवादी सिद्धान्त के प्रमुख बिन्दु क्या हैं?
उत्तर –
‘अन्तर्दृष्टि द्वारा सीखने’ के सिद्धान्त को ‘गेस्टाल्ट’ का सिद्धान्त भी कहा जाता है। इसके अनुसार, “ मनुष्य के प्रयास उसके मस्तिष्क पर आधारित होते हैं।”
वस्तु के अंगों या विभिन्न भागों को देखकर उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
इस सिद्धान्त के कई गुण हैं, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं-
1. इससे बालकों की बुद्धि का विकास किया जाता है। यह सिद्धान्त व्यर्थ के प्रयासों में विश्वास नहीं करता है। बालक को अपना पाठ बुद्धिमत्ता के साथ सीखना चाहिए।
2. यह ज्ञान को स्थायी बनाता है, शक्ति की बचत होती है। बालक की क्षमता बढ़ती है।
3. बालक की बुद्धि तीक्ष्ण बनती है, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान में बालक को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है।
4. यह सिद्धान्त Motivation पर बल देता है जो कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए परम आवश्यक है।
5. शिक्षक को पूर्ण अंश की ओर चलना चाहिए। जब शिक्षक को पौधा पढ़ाना हो तो उसे चाहिए कि वह बालक को सम्पूर्ण पौधा दिखाये और उसके पश्चात् पौधे के विभिन्न भागों को समझाये।
प्रश्न h (vi) सीखने के शास्त्रीय और क्रिया प्रसूत अनुकूलन के बीच तुलनात्मक
अथवा
स्किनर द्वारा प्रस्तुत किये गये अधिगम सिद्धान्त के प्रमुख बिन्दुओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धान्त (शास्त्रीय अनुबन्ध सिद्धान्त ) – कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे अनुबन्धन का सिद्धान्त भी कहा है। इसे क्लैसिकल कण्डीशनिंग का सिद्धान्त भी कहते हैं। यह सिद्धान्त भी शरीर की क्रिया पर आधारित है और इस दृष्टि से इसे शरीर विज्ञान का सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार अधिगम एक अनुकूल अनुक्रिया है या अनुबंधन है। अब हमें मालूम करना चाहिए कि अनुकूलित अनुक्रिया क्या है?
प्रो० बर्नार्ड ने लिखा है कि “अनुकूलित अनुक्रिया उत्तेजना की पुनरावृत्ति द्वारा व्यवहार का स्वचालन है जिसमें उत्तेजनाएँ निश्चित अनुक्रिया के साथ लगी रहती हैं और बाद में वे उत्तेजनाएँ व्यवहार के लिए कारण बन जाती हैं जिसके साथ वे मात्र पहले रूप में लगी हुई थीं।”
स्किनर का क्रिया-प्रसूत अनुबन्ध —
व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बी०एफ० स्किनर द्वारा प्रयोगशाला में पशुओं पर अधिगम के क्षेत्र में काफी महत्त्वपूर्ण प्रयोग किये गये हैं। स्किनर ने अपने प्रयोगों के आधार पर अधिगम के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, उसे अनुबद्ध अनुक्रिया- सिद्धान्त या क्रिया-प्रसूत अनुबन्ध का सिद्धान्त कहते हैं। बी०एफ० स्किनर ने व्यवहार को दो श्रेणियों में रखा है-
1. प्रतिकृत व्यवहार – वे अनुक्रियाएँ होती हैं जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण होती हैं। इनमें एक ज्ञात उद्दीपक एक निश्चित अनुक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे- ‘भोजन’ उद्दीपक ‘लार टपकने’ की अनुक्रिया को उत्पन्न करता है।
2. क्रिया-प्रसूत व्यवहार -जब प्राणी के व्यवहार में बिना किसी ज्ञात उद्दीपक के स्वतः स्फूर्त ढंग से अनुक्रिया उत्पन्न होती है तो उसे क्रिया-प्रसूत व्यवहार कहते हैं, अर्थात् वे अनुक्रियाएँ जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण नहीं होतीं, क्रिया-प्रसूत व्यवहार कहते हैं, अर्थात् वे अनुक्रियाएँ जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण नहीं होतीं, ‘क्रिया-प्रसूत’ व्यवहार कहलाती हैं
स्किनर के अनुसार मानव-व्यवहार का तीन-चौथाई से भी अधिक अंश क्रिया-प्रसूत व्यवहार की श्रेणी में रखा जा सकता है। स्किनर ने जिस प्रकार के अनुबन्धन का तरीका अपनाया, उसमें प्राणी द्वारा क्रिया उत्पन्न करने पर विशेष बल दिया। इसके अन्तर्गत अधिगम-स्थिति को इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि जब तक सीखनेवाला वांछित व्यवहार न करे, तब तक उसे पुरस्कार न मिले। यहाँ सीखनेवाले को यह अवसर दिया जाता है कि वह अधिगम-स्थिति में सक्रियता की भूमिका कर सके।
प्रश्न i (i) टी० ए० टी० परीक्षण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
अथवा
व्यक्तित्व के टी० ए० टी० परीक्षण का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
टी० ए० टी० परीक्षण —
मरे द्वारा प्रतिपादित TAT एक ऐसा प्रक्षेपीय परीक्षण है जिसे शोध मूल्य के दृष्टिकोण से रोशार्क परीक्षण के तुरन्त बाद रखा गया है। इस परीक्षण में 30 कार्ड तथा 1 सादा कार्ड कुल 31 कार्ड होते हैं। इनमें से 19 कार्ड तथा 1 सादा कार्ड का चयन व्यक्ति की उम्र एवं यौन के अनुरूप किया जाता है और व्यक्ति उसके चित्रों एवं दिखलाये गये दृश्यों के आधार पर कहानी लिखता है। इन कहानियों का विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा TAT का प्रयोग रोगियों के व्यक्तित्व को समझने में काफी किया गया है। TAT का प्रयोग शोध उद्देश्यों से भी काफी किया गया है तथा इसका उपयोग उपलब्धि आवश्यकता तथा सम्बन्धन आवश्यकता को मापने के लिए भी काफी किया गया है।
प्रश्न i (ii) प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं?
उत्तर-
भूमिका-
प्रत्येक विद्यालय में सामान्य बालकों की संख्या अधिक होती है। परन्तु पढ़ने आनेवाले छात्रों में असामान्य छात्रों की भी संख्या होती है। इनकी अपनी शारीरिक और मानसिक विशेषताएँ होती हैं। इनमें से कुछ मन्द बुद्धि तो कुछ अत्यन्त प्रखर बुद्धिवाले बालक होते हैं। कुछ बालकों में शारीरिक दोष भी पाया जाता है। ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। इन बालकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है-
(1) प्रतिभाशाली बालक,
(2) मन्द बुद्धि वाले बालक,
(3) पिछड़े बालक और
(4) समस्यात्मक बालक ।
प्रतिभाशाली बालक का अर्थ-
बालकों में व्यक्तिगत भेद पाये जाते हैं। प्रतिभाशाली बालक साधारण बालकों से भिन्न होते हैं। जिन बालकों की बुद्धि-लब्धि (I.Q.) सामान्य बुद्धि-लब्धि से अधिक होती है, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जिन बालकों की बुद्धि-लब्धि 130 या 140 से अधिक होती है, उनको प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होता है।
प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा – प्रतिभाशाली बालक की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है-
(1) कॉलसनिक- “प्रतिभाशाली शब्द उस बालक के लिए प्रयोग किया जाता है जो वय-वर्ग में किसी एक योग्यता में श्रेष्ठ होता है। जो उसे असाधारण रूप से हमारे समाज के जीवन के गुण तथा कल्याण के लिए योग देनेवाला बनाता है।”
(2) स्किनर – “प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन एक प्रतिशत बालकों के लिए किया जाता है, जो सबसे अधिक बुद्धिमान् होते हैं।
प्रश्न i (iii) प्रतिभाशाली बालकों हेतु निर्देशन के प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर-
प्रतिभाशाली बालकों के निर्देशन हेतु अधोलिखित सोपानों को प्रस्तुत किया गया है-
(1) प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए परीक्षण, निरीक्षण, गृहकार्य, व्यवहारों तथा विशेषताओं का उपयोग करते हैं।
(2) बुद्धि-परीक्षण भी देते हैं तथा बुद्धि-लब्धि ही मुख्य आधार होता है।
(3) प्रतिभाशाली बालकों की समस्या समाधान हेतु समुचित आयामों का चयन करते हैं।
(4) प्रतिभाशाली बालकों की कक्षा की व्यवस्था पृथक् रूप में की जाती है।
(5) शैक्षिक गति वृद्धि तथा प्रोन्नति हेतु पाठ्यक्रम को कम समय में पूरा करने का प्रयास किया जाता है। सामान्य बालकों के साथ अध्ययन करने से उन्हें सन्तोष नहीं होता है। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती है।
प्रश्न 1 (iv) समस्यात्मक बालकों के निर्देशन हेतु सुझाव दीजिए।
उत्तर-
कुछ बालक सामाजिक तथा भावात्मक दृष्टि से सामान्य से भिन्न प्रकार के होते हैं। उनका समायोजन नहीं होता और वे समाज, विद्यालय तथा साथियों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं और मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से सामान्य होते हैं। इस प्रकार के बालकों का व्यक्तित्व तथा व्यवहार असामान्य होता है। कुछ असामान्य व्यवहार इस प्रकार के होते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, अन्य साथियों से स्वयं को रुष्ट कर लेना, गृहकार्य नहीं करना, कक्षा से भाग जाना, विद्यालय में देर से आना आदि। ऐसे बालक अपने से बड़ों का आदर-सम्मान नहीं करते तथा इनका आचरण भी सामान्य नहीं होता है।
इन छात्रों की समस्याओं का अध्ययन मनोविज्ञान की दृष्टि से करने से कारणों का बोध होता है। इसके लिए एकल अध्ययन प्रविधि को प्रयुक्त किया जाता है तभी कारणों की पहचान होती है। किस अवस्था से बालक में गलत आदतों तथा व्यवहार का संचार हुआ। कभी-कभी विकास के साथ-साथ भी हो जाता है। इन छात्रों के लिए निर्देशन व्यक्तिगत दिया जाता है। बालक के कारणों का निदान करने के पश्चात् ही निर्देशन तथा परामर्श की व्यवस्था की जाती है। सामूहिक निर्देशन से इन बालकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है।
प्रश्न i (v)विकलांग बालकों हेतु शिक्षा-व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
उत्तर-
विकलांग बालकों हेतु शिक्षा —
1. अपंग बालकों हेतु शिक्षा
(1) इनके लिए पृथक् कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए।
(2) इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
(3) शारीरिक दृष्टि से अपंग बालकों के बैठने हेतु विशेष प्रकार की कुर्सी व मेज की व्यवस्था की जानी चाहिए। इनके मन से हीन भावना को समाप्त कर इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए।
2. वाक् दोषी बालकों की शिक्षा-
(1) इन्हें बोलने का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
(2) इन्हें हस्तकार्य की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
(3) सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।
3. पूर्ण बहरे तथा अपूर्ण बहरे बालकों की शिक्षा –
(1) ऐसे बालकों के लिए मूक-बधिर शिक्षालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
(2) बधिर बालक, गणना की खोज कार्य करने में निपुण किये जा सकते हैं।
4. सम्पूर्ण अन्धे बालकों की शिक्षा-
(1) अन्धे बालकों की ब्रेल विधि द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।
(2) इनके लिए विशेष अन्ध विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
(3) अर्द्ध अन्धे बालकों के लिए मोटे व बड़े अक्षरों में छपी पुस्तकों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
(4) कक्षा में रोशनी का समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए।
प्रश्न j (i) स्मृति स्तर के शिक्षण को उदाहरण की सहायता से समझाइए ।
उत्तर- यह शिक्षण के स्तर की प्रथम अवस्था है। स्मृति स्तर विचारहीन प्रक्रिया होती है। इसमें तथ्यों तथा सूचनाओं को याद करना मुख्य लक्ष्य होता है। इस स्तर पर अध्यापक का उद्देश्य छात्रों की स्मृति का विकास करना होता है। वह स्मृति के आवश्यक तत्त्वों-अधिगम, धारण, प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान के विकास के लिए विभिन्न रीतियों का प्रयोग करता है।
स्मृति स्तर पर शिक्षण में अध्यापक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इस स्तर पर छात्र निष्क्रिय अधिगमकर्त्ता के रूप में रहता है। वह कठोर अनुशासन का पालन करते हुए केवल तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों, सिद्धान्तों, नियमों तथा विचारों को हृदयंगम करता रहता है। अध्यापक स्वयं ही पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित, क्रमिक एवं सुसंगठित रूप प्रदान करने के लिए परिश्रम करता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच किसी प्रकार की अन्तःक्रिया नहीं होती। समस्त शिक्षण का कार्य यांत्रिक ढंग से सम्पन्न होता रहता है।
प्रश्न j (ii) समंजन का शैक्षिक निहितार्थ क्या है?
अथवा
समंजन प्रक्रिया की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
उत्तर-
समायोजन/समंजन के शैक्षिक निहितार्थ —
बालक के जीवन के प्रारम्भ के वर्ष परिवार के बाद विद्यालय में व्यतीत होते हैं। यही कारण है कि बालक के समायोजन को विद्यालय का वातावरण प्रभावित करता है, इनको निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है-
(1) सहानुभूति व्यवहार-यदि किसी बालक में कुसमायोजन की भावना जाग्रत हो रही है और यदि अध्यापक को उसका पता चल जाये तो उसका कर्त्तव्य है कि वह प्रधानाध्यापक से मिलकर बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से उसके अन्दर पनप रहे कुसमायोजन को समाप्त करने का प्रयास करे।
(2) हीनता की भावना न आने देना-सभी मनुष्य एक-समान नहीं होते हैं। सभी सुन्दर नहीं होते। कुछ शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। अर्थात् कक्षा में कुछ मन्द बुद्धि बालक, कुछ शारीरिक रूप से विकलांग जैसे-लँगड़े तथा तुतलाने वाले बालक होते हैं। कुछ अध्यापक तथा कक्षा के अन्य बालक विकलांग बालकों को चिढ़ाते हैं उन्हें लँगड़ा आदि कहकर सम्बोधित करते हैं। इस प्रकार की बातों से उनमें हीनता की भावना आ जाती है वह स्वयं को कोसने लगते हैं और तनावग्रस्त रहने लगते हैं। स्कूल जाने में संकोच करने लगते हैं। इसी कारण उनमें कुसमायोजन की भावना उत्पन्न हो जाती है।
(3) पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ-बालक की वर्तमान आयु के अनुरूप ही विद्यालय का पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए जिससे बालकों की स्वाभाविक रुचि पढ़ाई की ओर हो। इस प्रकार होने से बालक स्कूल जाने में प्रसन्नता का अनुभव करता है और सुचारु रूप से पढ़ाई करता है जिससे अंक प्राप्त करके उसे सन्तुष्टि की प्राप्ति होती है जो उसके समायोजन को स्वस्थ बनाने में सहायता करती है।
उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर अध्यापक बालक के उचित समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
(4) अध्यापक का व्यवहार-बालकों के लिए अध्यापक आदर्श समान होता है। वे उसी का अनुकरण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यापक का स्वयं का व्यवहार समायोजित होना चाहिए। यदि अध्यापक किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में अपने को समायोजित कर लेता है तो यही गुण बालक भी अपने में समाहित कर लेता है। उसी कारण अध्यापक का खुद का व्यवहार समायोजित होना अति आवश्यक है
(5) कठोर अनुशासन- अगर विद्यालय का अनुशासन कठोर है तो भी बालक कुसमायोजित हो जाता है। अत्यधिक दण्ड मिलने के कारण घर से तो स्कूल के लिए निकल पड़ता है पर वह स्कूल न पहुँचकर इधर-उधर घूमता रहता है और वह गलत आदतों का शिकार हो जाता है; जैसे-सिगरेट, बीड़ी आदि पीना सीख जाता है और उसका व्यवहार कुसमायोजित हो जाता है।
प्रश्न j (iii) बुद्धि के थर्स्टन के सिद्धान्त को समझाइए ।
अथवा
बुद्धि के थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को समझाइए ।
उत्तर-
ग्रुप-तत्त्व सिद्धान्त (समूह तत्त्व सिद्धान्त ) – जो सभी तत्त्व प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते परन्तु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं उन्हें ‘ग्रुप-तत्त्व’ की संज्ञा दी गयी है। इस सिद्धान्त के समर्थकों में थर्स्टन का नाम प्रमुख है। प्रारम्भिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रारम्भिक तत्त्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो उन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करता है और उन्हें अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग करता है। मानसिक क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं। उनमें अपना एक प्रारम्भिक तत्त्व होता है। थर्स्टन
उनके साथियों नये ऐसे नौ तत्त्वों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं-
(a) मौखिक तत्त्व – इसका सम्बन्ध शब्दों तथा विचारों के साथ है।
(b) स्थान- सम्बन्धी तत्त्व-इसका सम्बन्ध व्यक्ति के किसी स्थान-विशेष में किसी चीज के परिमाण आदि के बारे में है।
(c) अंक सम्बन्धी तत्त्व-अंकों से सम्बद्ध हिसाब-किताब को शीघ्र एवं शुद्ध रूप से करना ।
(d) स्मृति तत्त्व- जल्दी से याद करने की योग्यता ।
(e) शाब्दिक-प्रवाह सम्बन्धी तत्त्व-तेजी के साथ पृथक् शब्दों पर सोचने की योग्यता ।
(f) निगमन तर्क तत्त्व – इसका सम्बन्ध चिन्तन की निगमन प्रणाली से है।
(g) आगमन-तर्क तत्त्व – यह चिन्तन की आगमन प्रक्रिया से सम्बन्धित है।
(h) प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी तत्त्व-इसका सम्बन्ध प्रत्यक्षीकरण से है।
(i) समस्या समाधान सम्बन्धी योग्यता तत्त्व- समस्याओं को हल करने की योग्यता से इसका सम्बन्ध है।
प्रश्न j (iv) मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई व्यक्तित्व की चार परिभाषाएँ दीजिए।
अथवा
व्यक्तित्व के सम्प्रत्यय को समझाइए ।
उत्तर-
(1) मार्टन प्रिन्स-मार्टन प्रिन्स ने व्यक्तित्व की संग्राही परिभाषा दी है। इनके अनुसार, “व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जैविक जन्मजात विन्यासों एवं प्रवृत्तियों का योग है।” इस परिभाषा में व्यक्तित्व के आन्तरिक एवं बाह्य पक्षों को समान महत्त्व प्रदान किया गया है।
(2) कारमाइकेल एवं वारेन के अनुसार, “व्यक्तित्व मानव के विकास की किसी भी अवस्था में मानव का सम्पूर्ण मानसिक संगठन है। यह मानव चरित्र के प्रत्येक पहलू को छाती से लगाता है। बुद्धि, स्वभाव, कौशल, नैतिकता एवं मानव की जीवन सारणी में निर्मित प्रत्येक दृष्टिकोण।”
(3) जे0 पी0 गिलफोर्ड के अनुसार, “हम व्यक्तित्व को गुणों के संगठित नमूनों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये व्यक्तित्व को एक रूप में लेते हैं। व्यक्तित्व के कारण ही मनुष्य एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।”
(4) वाटसन के अनुसार, “विश्वसनीय सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु एक लम्बे समय तक देखी गयी आदतों एवं आदत तत्त्वों के योगफल को ही व्यक्तित्व कहते हैं।”
प्रश्न j (v)व्यक्तित्व पर स्कूल का क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर-
एक निश्चित आयु में आकर बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया जाता है। दाखिल होने के बाद दिन में काफी समय बच्चों को स्कूल में ही रहना पड़ता है। स्कूल में बच्चे अन्य बच्चों और शिक्षकों के निकट सम्पर्क में आते हैं। इस सम्पर्क के परिणामस्वरूप उनमें सामाजिक आदान-प्रदान होता है। इस प्रकार के आदान-प्रदान का व्यक्तित्व पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। बच्चों के व्यक्तित्व पर पड़ने वाले स्कूल के प्रभाव को दो भागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम प्रभाव है शिक्षक का प्रभाव और दूसरा प्रभाव है सहपाठियों का प्रभाव।
(अ) शिक्षक का प्रभाव-
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के व्यक्तित्व पर अपने शिक्षक का विशेष प्रभाव पड़ता है। प्रायः सभी बच्चे अपने शिक्षक को एक आदर्श व्यक्ति माना करते हैं। इसलिये अधिकांश बच्चे जान-बूझकर या अनजाने में ही अपने शिक्षक का अनुसरण करने लगते हैं।
(ब) सहपाठियों का प्रभाव-
परिवार में जो स्थान छोटे-बड़े भाई-बहनों का होता है, स्कूल में वही स्थान सहपाठियों का होता है। बच्चों के व्यक्तित्व पर उनके सहपाठियों का गहरा प्रभाव पड़ता है।
प्रश्न j (vi) समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? समस्यात्मक बालक के क्या कारण हैं?
उत्तर-
प्रत्येक कक्षा में कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने उग्र व्यवहार के कारण शिक्षक के लिए सिर-दर्द बन जाते हैं। ऐसे बालकों का व्यवहार असामान्य होता है, जिसके कारण वे सब के लिए एक समस्या बन जाते हैं। समस्यात्मक बालक की परिभाषा देते हुए वेलेण्टाइन ने लिखा है-“समस्यात्मक बालक वे बालक हैं, जिनके व्यवहार या व्यक्तित्व में किसी प्रकार की आर्थिक असामान्यता पायी जाती है।”
यदि एक बालक समस्यात्मक है तो आवश्यक नहीं कि वह पिछड़ा हुआ भी हो। सामान्य स्तर के बालक भी समस्यापूर्ण हो सकते हैं। समस्या का सम्बन्ध निष्पत्ति की अपेक्षा व्यवहार से है।
समस्यात्मक बालक के कारण–
एक बालक के समस्यात्मक होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
(1) माता-पिता की मृत्यु बाद बालक का बुरी संगत में पड़ जाना।
(2) सौतेली माता की उपेक्षा तथा कठोर व्यवहार।
(3) बालकों की मूल प्रवृत्तियों का दमन करने से उनमें भावना-ग्रन्थियों का पड़ जाना।
(4) अत्यधिक अश्लील और अपराधी फिल्में देखना।
(5) सामूहिक रूप से किसी बालक का अपमान करना।
प्रश्न j (vii) व्यक्तित्व मापन हेतु प्रयुक्त किसी एक प्रक्षेपी प्रविधि का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
प्रक्षेपण विधियाँ —
मनुष्य के मूल्यांकन करने की सभी विधियों में यह सर्वाधिक विश्वसनीय तथा वैध विधि है। वर्तमान समय में इन्हीं विधियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। एल० फ्रेंक ने सबसे पहले प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया था। फ्रेंक के अनुसार, “प्रक्षेपण द्वारा हमें यह मालूम होता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को किस प्रकार समझाता है। इन विधियों द्वारा व्यक्तियों को आन्तरिक या प्राइवेट जीवन का आभास मिलता है। ”
इस विधि के माध्यम से अचेतन व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि अन्य विधियाँ केवल चेतन व्यवहार का ही अध्ययन करती हैं। संक्षेप में प्रक्षेपण का अर्थ हम इस वाक्य द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी विशेष वस्तु अथवा क्रिया में व्यक्ति के विशेष गुण के अनुसार किसी विशेष तथ्य को देखना ही प्रक्षेपण कहलाता है। प्रक्षेपण विधियों की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—
(1) रचनाहीन सामग्री-इन विधियों में प्रयुक्त होनेवाली सामग्री रचनाहीन सामग्री होती है। इनकी कोई विशेष आकृति नहीं बनती।
( 2 ) सम्पूर्ण व्यक्तित्व – इन विधियों के माध्यम से सम्पूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। अन्य विधियों के माध्यम से ऐसा सम्भव नहीं होता। वे व्यक्ति के व्यक्तित्व के अलग गुणों का अध्ययन करती हैं।
( 3 ) अचेतन व्यवहार से सम्बन्धित- इन विधियों के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
( 5 ) मानसिक रोगों का अध्ययन-इन विधियों के माध्यम से मानसिक रोगों का अध्ययन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था में भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है।
रोर्शा का स्याही धब्बा परीक्षण-इस परीक्षण की रचना स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोर्शा ने सन् 1921 में की थी। यह सबसे अधिक सफल परीक्षण माना जाता है। यह परीक्षण निम्न प्रकार किया जाता है—
(i) परीक्षण सामग्री-इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। इन कार्डों पर रचनाहीन स्याही के धब्बों-जैसी आकृतियाँ बनी होती हैं। इन 10 कार्डों में से 5 कार्डों पर बिल्कुल काली आकृतियाँ, 2 कार्डों पर काली तथा लाल आकृतियाँ तथा शेष 3 कार्डों पर भिन्न-भिन्न आकृतियाँ होती हैं। सभी 10 कार्डों की आकृतियाँ कोई विशेष अर्थ नहीं रखतीं।
(ii) परीक्षण का आयोजन-जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना होता है, उस व्यक्ति को ये 10 कार्ड एक-एक करके दिये जाते हैं व उस कार्ड पर तथा छपी आकृति के बारे में उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया को नोट किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि उस कार्ड की आकृति उन्हें किस प्रकार की लगती है या उन्हें उस आकृति में क्या दिखायी दे रहा है। प्रत्येक कार्ड को देखने के लिए व्यक्ति जितना समय चाहता है, उसे उतना ही समय दिया जाता है। इस कार्ड को वह व्यक्ति किसी भी कोण से देख सकता है, एक ही कोण से देखने का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।
प्रश्न j (viii) स्मृति के शैक्षिक निहितार्थ को समझाइए |
उत्तर-
शैक्षिक निहितार्थ —
आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार-स्मृति व्यक्ति का जन्मजात गुण है। इसीलिए व्यक्तियों की स्मृति या स्मरण-शक्ति में अन्तर पाया जाता है। पर विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका
है कि प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा स्मृति में उन्नति की जा सकती है। इसका कारण बताते हुए वुडवर्थ ने लिखा है- “सीखने या स्मरण करने की प्रक्रिया एक नियंत्रित क्रिया होने के कारण प्रशिक्षण से अत्यधिक प्रभावित होती है।”
अब प्रश्न यह है कि स्मृति की उन्नति के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण या अभ्यास की आवश्यकता है? इसका उत्तर देते हुए एवेलिंग (Aveling) ने अपनी पुस्तक “Directing Mental Energy” में लिखा है- “वास्तव में स्मृति में उन्नति हमारी स्मरण करने की विधियों में उन्नति के अतिरिक्त और कुछ नहीं।” इस कथन की सत्यता के बावजूद कुछ उपाय या नियम ऐसे हैं, जो स्मृति की उन्नति में सहायता देते हैं, यथा-
(1) दृढ़ निश्चय-बालक जिस बात को याद करना चाहते हैं, उसे याद करने के लिए उनमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए।
(2) स्पष्ट ज्ञान-बालक जिस बात को स्मरण करना चाहते हैं, उसका लाभ और उद्देश्य उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए।
(3) प्रोत्साहन – बालकों को पाठ याद करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
(4) पहले से समझना-बालकों को जो पाठ याद करने के लिए दिया जाये, उसका कार्य उन्हें पहले ही पूर्ण रूप से समझा दिया जाना चाहिए।
(5) रुचि उत्पन्न करना-बालकों को स्मरण करने के लिए जो पाठ दिया जाये, उसमें उनकी रुचि होनी चाहिए या रुचि उत्पन्न की जानी चाहिए।
प्रश्न j (ix) अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ।
उत्तर-
1. सीखने की इच्छा-यदि बच्चे में सीखने की इच्छा है तो नया ज्ञान उसे सरल तीरके से सिखाया जा सकता है। बालक यदि सीखने के लिए तैयार नहीं है तो शिक्षक के सामने बहुत गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। सीखने की इच्छा, रुचि तथा अभिप्रेरणा बहुत सीमा तक अधिगम को प्रभावित करते हैं
2. शैक्षिक योग्यता या निष्पत्ति-विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का अधिगम पर बहुत प्रभाव प्रड़ता है। यदि विद्यार्थी किसी विषय में पिछड़ा है तो उस विषय से सम्बन्धित नवीन ज्ञान सीखने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यदि विद्यार्थी की किसी विषय में शैक्षिक योग्यता सामान्य से अधिक है तो विद्यार्थी नया ज्ञान सुगमता से सीख लेता।
3. आकांक्षा का स्तर बालक की महत्वाकांक्षा पर अधिगम की सफलता काफी कुछ निर्भर करती है। जब तक विद्यार्थी में महत्वाकांक्षा नहीं होगी, वह सीखने के लिए प्रयत्नशील नहीं होगा
4. बुद्धि-सीखना बहुत कुछ सीखने वाले की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालक कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र सीख लेते हैं।
5. संवेगात्मक स्थिति-सीखने में संवेगात्मक स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है। संवेगात्मक रूप से स्वस्थ विद्यार्थी शीघ्रता से सीखता है।
प्रश्न j (x) सांवेगिक बुद्धि।
उत्तर-
संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है सांवेगिक बुद्धि के चार घटक हैं— संवेग महसूस करना, संवेग समझना, संवेग प्रबंधित करना और संवेगों का उपयोग करना। 1990 तक मनोवैज्ञानिक पीटर सेलोवी और जॉन मेयर ने सांवेगिक बुद्धि का प्रथम सिद्धान्त प्रस्तुत किया। गोलमैन के अनुसार, “संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति के स्वयं के एवं दूसरों के संवेगों को पहचानने की वह क्षमता है जो हमें प्रेरित कर सकने और हमारे संवेगों को स्वयं में अपने सम्बन्धों के दौरान भली प्रकार से साधने में सहायक होती है।”
प्रश्न j (xi) तनाव से बचने के उपाय।
उत्तर-
तनाव दूर करने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं—
(i) पर्याप्त नीद लेना,
(ii) नकारात्मकता से बचना,
(iii) व्यायाम और योग में समय देना,
(iv) मित्रों और परिजनों के साथ समय बिताना,
(v) अहंकार को समाप्त करना,
(vi) यथार्थवादी बनना,
(vii) स्वस्थ आहार लेना चाहिए,
(viii) हाथों को गर्म पानी से धोना,
(ix) ड्राइंग करना या आर्ट बनाना,
(x) हँसने वाली परिस्थिति में अपने को समायोजित करना।
प्रश्न j (xii) व्यक्तित्व की भारतीय अवधारणा।
उत्तर-
उपनिषद में दिए गए “व्यक्तित्व” के प्राचीन भारतीय मॉडल में पाँच कोश शामिल हैं। वे हैं— अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय । प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएँ होती हैं जो उसे दूसरे व्यक्तियों से पृथक् करती हैं। व्यक्ति के इन गुणों का संगठन ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। ‘अन्नमय’ मानव तंत्र का एक भाग ‘अन्न’ अर्थात् भोजन से पोषित होता है। ‘प्राणमय’ वह खण्ड है जो ‘प्राण’ अर्थात् ‘बायोएनर्जी’ द्वारा पोषित होता है। ‘मनोमय’ ‘शिक्षा’ से पोषित खण्ड है। ‘विज्ञानमय’ ‘अहंकार’ से पोषित है और ‘आनंदमय’ भावनाओं से पोषित खण्ड है। त्रिगुण की अवधारणा का उपयोग आधुनिक युग में भी व्यक्तिव की अवधारणा को समझाने के लिए किया गया है। चेतना का विकास स्पष्टतः त्रिगुण की इस अवधारणा में निहित है। इन्हें (सत्व) स्थिरता कहा जाता है; रजस को सक्रियता और तमस को जड़ता कहा जाता है।
प्रश्न j (xiii) विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं?
उत्तर- “विशिष्ट बालक” वह हैं जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय व्यवस्थाओं में संशोधन अथवा विशेष शैक्षिक सेवाएँ अथवा पूरक शिक्षण चाहता है जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं-
(i) शारीरिक विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट बालक,
(ii) मानसिक रूप से विशिष्ट बालक,
(iii) सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक,
(iv) संवेगात्मक विकास की दृष्टि से विशिष्ट बालक ।
क्रूशैंक के अनुसार, “एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, बौद्धिक संवेगात्मक एवं सामाजिक रूप, सामान्य बुद्धि एवं विकास की दृष्टि से इतने अधिक विचलित होते हैं कि नियमित कक्षा-कार्यक्रमों से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं तथा जिसे विद्यालयों में विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है।
प्रश्न j (xiv) प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान।
उत्तर-
प्रतिभाशाली बच्चे समाज और देश की धरोहर होते हैं। इन बालकों की शिक्षा व्यवस्था उनके विशिष्ट आवश्यकताओं, रुचियों एवं उनके वास्तविक शैक्षिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए । इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु नवोदय विद्यालय, दक्षिणा फाउंडेशन, विद्याज्ञान, सितारे फाउन्डेशन मिलकर कार्य कर रहे हैं। प्रतिभाशाली बालकों के शैक्षिक प्रावधान के अंतर्गत् योग्य एवं नेक अध्यापक, सहगामी क्रियाओं की विशेष व्यवस्था, पुस्तकालय की सुविधा, विस्तृत पाठ्यक्रम, उत्तरदायित्व का कार्य तथा प्रोजेक्ट विधि का उपयोग किया जाना चाहिए।
******* ******* ******** ***** ****** ****** ***** ** **
—— ——- —- —- —— —– —— —— —— —- ——
/// //// //// ///// //// ///// //////// ///// //// ///////
दीर्घ उतरिय प्रश्न
LONG QUESTION ANSWER
निर्देश – प्रश्न संख्या २ से ९ दीर्घ उतरीय प्रश्न है | परिक्षार्थियो को प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल चार प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है | प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित है | 4*15=60
प्रश्न 2 (i) शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है?
अथवा
शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए एवं उसके स्वरूप एवं विषय विस्तार की व्याख्या कीजिए।
अथवा
शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप बताइए तथा इसके विषय विस्तार का वर्णन कीजिए।
अथवा
शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसके विषय क्षेत्र का भी वर्णन कीजिए।
उत्तर –
शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ —
शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है— शिक्षा और मनोविज्ञान। साधारण रूप से इसका अर्थ हुआ ‘शिक्षा की क्रिया का मनोविज्ञान।’ शिक्षा का तात्पर्य सीखना है अर्थात् अपने चारों ओर हम क्या देखते-सुनते हैं और तदनुकूल हम क्या करें यही शिक्षा है। अंग्रेजी में ‘एजूकेशन’ (Education) शब्द का मूलतः अर्थ है- आन्तरिक शक्तियों को बाहर के वातावरण में प्रकट करने की क्रिया जिससे हम उस वातावरण से परिचित हो जायें और फलस्वरूप आगे बढ़ सकें। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा जीवन की एक सार्थक क्रिया है और उसकी सार्थकता पर्यावरण के साथ परिचय या अनुकूलन में पायी जाती है या सीखने में होती है। अतएव शिक्षा सीखना है, आन्तरिक शक्तियों का प्रकाशन और विकास है।
यह शिक्षा की क्रिया कैसे होती है यह मनुष्य की अपनी विशेषताएँ बताती हैं। मनुष्य के पास ‘मन’ और ‘शरीर’ होता है। मन से वह सोचता-विचारता है और शरीर से क्रिया करता है। मनुष्य जब मन से सोचता-विचारता और शरीर से क्रिया करता है तो उसे उसका ‘व्यवहार’ कहते हैं। इस प्रका से ‘व्यवहार’ की जानकारी हमें कैसे होती है? इसके लिए एक विशेष विषय है जिसे ‘मनोविज्ञान
अर्थात् मन का विज्ञान या वस्तुनिष्ठ एवं विशेष ज्ञान ‘देने वाला विषय’ कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि हर एक मनुष्य के मन और शरीर की क्रिया का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। शिक्षा भी और शरीर की एक विशिष्ट क्रिया है और इसका अध्ययन भी मनोविज्ञान करता है परन्तु उसे केवल मनोविज्ञान न कहकर शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि “शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ उस विषय से होता है जो मनुष्य की सीखने-सिखाने की मन तथा शरीर से की गयी क्रिया का विशेष ढंग से अध्ययन करता है।”
शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा —
जब शिक्षा मनोविज्ञान एक विषय है तो निश्चित ही उसकी कुछ परिभाषा विद्वानों एवं विशेषज्ञों द्वारा अवश्य दी गयी होगी जिसे यहाँ जानना जरूरी है तभी हम उसके स्वरूप एवं विषय-क्षेत्र को अच्छी तरह से जान सकते हैं। कुछ शिक्ष -मनोविज्ञानियों द्वारा दी गयी परिभाषाएँ नीचे दी जा रही हैं-
डब्ल्यू. जी. ट्रो- “शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन है।”
सी. ई. स्किनर – “शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, इसका तात्पर्य है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार के अध्ययन या मानवीय व्यक्तित्व से उसकी अभिवृद्धि, विकास तथा शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्देशन से सम्बन्ध रखता है।”
प्रो. क्रो एवं क्रो- “शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से बुढ़ापे तक व्यक्ति के सीखने से सम्बन्धित अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है।”
शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप –
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप पर विचार कर सकते हैं। उक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप के सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं-
(अ) शिक्षा मनोविज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन या विज्ञान है। यह बालक और अन्य शिक्षा लेने वाले व्यक्तियों के शिक्षा सम्बन्धी क्रियाओं अथवा व्यवहार का अध्ययन करता है।
(आ) शैक्षिक क्रिया या व्यवहार व्यक्ति की वातावरण के प्रति की गयी वह अनुक्रिया है जो वह सीखने या अनुभव ज्ञान ग्रहण करने के विचार से करता है। शिक्षा मनोविज्ञान इसी का अध्ययन है
(इ) शिक्षा मनोविज्ञान जिन शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है उसमें विद्यालय, शिक्षक, प्रबन्धक, प्रशासक, क्रीड़ा-प्रांगण, कक्षा, पुस्तक और अन्य सामग्री, विद्यालय के कर्मचारी, विद्यालय की कार्यविधि तथा सीखने वालों की समस्त मानसिक एवं शारीरिक क्रियाएँ होती हैं जो विभिन्न स्थितियों के कारण की जाती हैं।
(ई) शिक्षा मनोविज्ञान इन सभी का अध्ययन, विश्लेषण एवं व्याख्या के ढंग से करता है जिसमें वैज्ञानिकता पायी जाती है।
(उ) शिक्षा मनोविज्ञान हर एक विद्यार्थी के उन अनुभवों की व्याख्या करता है जो विद्यालय के बाहर भी होते हैं और जिनका प्रभाव उसकी सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है।
(ऊ) शिक्षा विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम में होने वाले परिवर्तन को भी प्रकट करती है जिससे कि उसे अभिवृद्धि एवं विकास कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान इस बात की जानकारी कराता है। (ए) शिक्षा मनोविज्ञान व्याख्या और विश्लेषण करने वाला अध्ययन है, इसलिए इसे निश्चयात्मक या विधायक विज्ञान कहा जाता है।
(ऐ) शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय की शैक्षिक स्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। इस दृष्टि से वह केवल छात्र-व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी कहा जाता है।
(ओ) शिक्षा मनोविज्ञान कुछ विशिष्ट विधियों का प्रयोग करता है। इस प्रकार उसका अपना एक विशेष स्थान है।
शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव –
शिक्षा की क्रिया एवं व्यवस्था पर शिक्षा मनोविज्ञान का प्रभाव आधुनिक युग में बहुत पड़ा। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री पेस्टॉलॉजी ने तो यहाँ तक कहा है कि “मैं शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ।” इस दिशा में उसने बहुत प्रयत्न किया और सफल भी रहा क्योंकि बाद के शिक्षाशास्त्री उसके विचारों और कार्यों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रभाव शिक्षा पर पड़ने से निम्नलिखित परिणाम मिले हैं-
(1) शिक्षा बाल केन्द्रित या विद्यार्थी केन्द्रित हो गयी अर्थात् सीखने वाले को प्रथम स्थान शिक्षा में दिया जाने लगा।
(2) शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की निजी विशेषताओं के अनुरूप दी जाने लगी, सबको अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि एवं आवश्यकता के आधार पर शिक्षा मिलने लगी।
(3) शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रयत्न किया जाने लगा। मानसिक,शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक सभी प्रकार का विकास होने लगा।
(4) शिक्षा के लिए सभी को सुविधा, अवसर एवं अधिकार मिला कि वह अपना व्यक्तिगत विकास करे।
(5) शिक्षा क्रियाशील हो गयी केवल सूचना, सिद्धान्त या सूक्ष्म बातें नहीं बतायी जाने लगीं।
(6) शिक्षा की नयी विधियाँ बनायी गयीं जैसे— खेल विधि, योजना विधि, किण्डर गार्टन विधि, मॉण्टेसरी विधि, डाल्टन विधि आदि। अभिनय, यात्रा, सेवा, सैनिक क्रिया आदि पर भी बल दिया गया।
(7) शिक्षा के क्षेत्र में नये सिद्धान्त निकाले गये जैसे—सीखने का सिद्धान्त, अवधान का सिद्धान्त, स्मृति के सिद्धान्त। इससे शिक्षा आगे बढ़ी।
शिक्षा मनोविज्ञान का विषय-क्षेत्र –
इसके विषय में नीचे लिखी चीजें शामिल हैं–
(1) बालक का विकास-
शिक्षा मनोविज्ञान के अन्तर्गत हम बालक के विकास का अध्ययन करते हैं। बालक की विभिन्न अवस्थाओं जैसे—शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि का अध्ययन एवं इन अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। बालक के वंशानुक्रम का प्रभाव उस पर किस प्रकार पड़ता है तथा उसका वातावरण किस प्रकार उसको प्रभावित करता है अर्थात् उसकी योग्यताएँ, अतिक्षमताएँ, बुद्धि, आदि के विकास पर वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव किस प्रकार और कहाँ तक पड़ता है, इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के विषय-क्षेत्र में ही आता है। बालक के विकास के आधारभूत तत्त्व क्या हैं तथा किस प्रकार उनको वांछित दिशा प्रदान की जाय, बालक के सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास को किस प्रकार सामान्य रूप से विकसित किया जाय इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अन्तर्गत ही होता है।
(2) अधिगम-
अधिगम शिक्षा का आधार है। अतः अधिगम किस प्रकार होता है यह जानना अति आवश्यक है। अधिगम की प्रकृति क्या है और इसके सिद्धान्त क्या हैं? इसको जानने के लिए प्रयोग, निरीक्षण एवं सत्यापन किया जाता है, यह कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही आता है। सीखने में अवधान, स्मरण, विस्मरण, संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण, चिन्तन, कल्पना, तर्क आदि मानसिक क्रियाओं का प्रभाव एवं उनका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अन्तर्गत ही किया जाता है। सीखने की गति को कैसे बढ़ाया जाय या सीखने की गति को किस प्रकार स्थानान्तरित किया जाय यह शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही आता है। इनके ज्ञान से शिक्षा की प्रक्रिया या शिक्षा में सुधार किया जाता है तथा शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर ही शिक्षा दी जाती है।
(3) व्यक्तित्व एवं समायोजन-
व्यक्तित्व का अर्थ स्वरूप, उसके घटकों तथा उसके विकास एवं उससे सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन भी इसके अन्तर्गत होता है। इसके अन्तर्गत, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का स्वरूप क्या होता है? उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से हैं तथा अस्वस्थ बालकों (मानसिक रूप से) के क्या लक्षण हैं, उनका उपचार क्या है आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट बालकों जैसे मानसिक रूप से पिछड़े बालकों एवं अपराधी बालकों, समस्या बालकों का अध्ययन करना और उनके लिए उचित निदान ढूँढ़ना शिक्षा मनोविज्ञान का ही कार्य है।
(4) मापन एवं मूल्यांकन –
बालक क्या है? अर्थात् उसमें विभिन्न गुण किस मात्रा में विद्यमान है? यह जानना शिक्षाविद् के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी के आधार पर वह छात्र को वांछित लक्ष्य की ओर ले जा सकेगा। बालक की उपलब्धियों, बुद्धि, अभिरुचियों आदि का मापन करके ही बालक को निर्देश दिये जाते हैं तथा बालक के स्वरूप का ज्ञान होता है। इस प्रकार मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। मापन एवं मूल्यांकन की विधियों की खोज तथा उनका शिक्षा में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विषय-वस्तु है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का निर्माण तथा उसकी वैधता एवं विश्वसनीयता आदि की परीक्षा की जाती है, जिससे बालक का मापन सम्भव हो सके।
(5) अध्ययन विधियाँ –
शिक्षा मनोविज्ञान के अन्तर्गत कई विधियों का प्रयोग होता है क्योंकि प्रत्येक विधि की अलग-अलग उपयोगिता एवं सीमायें हैं। अध्ययन की विधियों की खोज करना एवं प्रचलित विधियों में सुधार करना भी शिक्षा मनोविज्ञान के विषय-क्षेत्र में आता है।
शिक्षा मनोविज्ञान अभी विकास की प्रक्रिया में है और यह विषय अपेक्षाकृत नया है, अतः इसके विषय-क्षेत्र का विस्तार अभी हो रहा है। ऊपर दिये गये विषय शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण भाग का निर्माण करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र की व्यापकता पर पील ने इस प्रकार मत व्यक्त किया है कि “शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वह विज्ञान है जो शिक्षक को अपने शिष्यों के विकास, उनकी क्षमताओं के विस्तार एवं सीमाओं, उनकी सीखने की प्रक्रियाओं तथा उनके सामाजिक सम्बन्धों को समझने में सहायता करता है। ”
प्रश्न 2 (ii) मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान के विकास ने शिक्षा प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है?
अथवा
शिक्षा और मनोविज्ञान के सम्बन्ध की विवेचना कीजिए तथा यह बताइए कि मनोविज्ञान ने शिक्षा सिद्धान्त और व्यवहार को कहाँ तक प्रभावित किया है?
अथवा
शिक्षा और मनोविज्ञान के सम्बन्धों को स्पष्ट कीजिए।
अथवा
शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
उत्तर –
शिक्षा एवं मनोविज्ञान का अर्थ —
शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों मानव अनुभव एवं व्यवहार से सम्बन्धित हैं। एक ओर मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का अध्ययन करता है तो दूसरी ओर शिक्षा अनुभव एवं व्यवहार का परिमार्जन करती है। इस प्रकार दोनों का सम्बन्ध ‘मानव व्यक्तित्व’ से है और इसलिए जहाँ मनोविज्ञान ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं व अंगों को प्रभावित किया है वहाँ शिक्षा ने भी मनोविज्ञान को विषय-वस्तु, क्षेत्र तथा अन्य बातों को प्रभावित कर उसे (मनोविज्ञान को) अपनी एक व्यावहारिक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे महत्त्वपूर्ण विज्ञान को जन्म देने में सहायता की है। यहाँ पर हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान के पारस्परिक सम्बन्ध को समझने के लिए दोनों के पारस्परिक प्रभावों को निम्नलिखित दो उप-शीर्षकों में प्रस्तुत कर रहे हैं।
मनोविज्ञान का शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रभाव —
मनोविज्ञान ने शिक्षा के विभिन्न अंगों को किस प्रकार प्रभावित किया है इसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा रहा है-
(1) शिक्षा का अर्थ-
शिक्षा के मनोविज्ञान से प्रभावित होने के कारण उसके अर्थ में पर्याप्त अन्तर आ गया है। परम्परागत रूप से शिक्षा का तात्पर्य विभिन्न विषयों से सम्बन्धित ज्ञान व सूचनाओं को बालकों के मस्तिष्क में प्रेषित करने का प्रयास करता है भले ही उस ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को कितनी ही कठिनाइयों, संयम-नियम का सामना क्यों न करना पड़े। यद्यपि मनोविज्ञान का कार्य शिक्षा के अर्थ को परिभाषित करना नहीं है, किन्तु मनोविज्ञान ने बालक के व्यवहार व आचरण के सम्बन्ध में जो मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त व नियम प्रस्तुत किये हैं उनसे अवगत होकर शिक्षाशास्त्रियों व शिक्षा दार्शनिकों ने शिक्षा के परम्परागत अर्थ को अस्वीकार करते हुए उनके नवीन व आधुनिक अर्थ को प्रस्तुत किया है। यह अर्थ विषय केन्द्रित न होकर बाल केन्द्रित है जिसमें बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए बाहर से किसी विचार व वस्तु को आरोपित नहीं किया जाता, बल्कि उसे ‘आत्म प्रकाशन’ या ‘आत्माभिव्यक्ति’ का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। शिक्षा में ‘मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति’ का विकास करने वाले सुप्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री पेस्टॉलॉजी ने शिक्षा की मनोवैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए लिखा है, “शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। ”
(2) शिक्षा के उद्देश्य –
मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना नहीं है क्योंकि यह एक ‘विषायक विज्ञान’ होने के नाते ‘क्या होना चाहिए’ का अध्ययन करके ‘क्या है’ का अध्ययन करता है। किन्तु मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है अथवा वह मन की उड़ान मात्र है क्योंकि मनोविज्ञान बालक की आवश्यकताओं, मूलप्रवृत्तियों, संवेगों, इच्छाओं एवं रुचियों से अच्छी तरह अवगत होता है। इस सन्दर्भ में क्रो एवं क्रो ने लिखा है, “यद्यपि मनोविज्ञान शिक्षा के लक्ष्य निश्चित नहीं कर सकता, किन्तु वैज्ञानिक मनोविज्ञान हमें एकदम बता सकता है कि कोई लक्ष्य निराशाजनक रूप से बादलों में है या उसको पाया जा सकता है।”
इसके साथ-साथ जैसा कि जेम्स ड्रेवर ने लिखा है, “शिक्षा का उद्देश्य पूरा करने के लिए मनोविज्ञान इतना निश्चित करके समाप्त नहीं हो जाता कि यह सम्भव है अथवा असम्भव ।” बल्कि मनोविज्ञान यह भी निश्चित रूप से बता सकता है कि उन्हें किन साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः उद्देश्य प्राप्ति की प्रक्रिया में शिक्षक के लिए मनोविज्ञान सबसे अधिक सहायक होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने में मनोविज्ञान सबसे अधिक सहायक सिद्ध होता है।’
(3) पाठ्यक्रम –
पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं पाठ्यक्रमेय विषयों के छात्रों की धारणा में भी मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है। प्राचीन काल में जहाँ ‘पुस्तकीय ज्ञान’ को अत्यधिक महत्त्व देने के कारण बालकों को सभी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ते थे, वहाँ वर्तमान समय में मनोविज्ञान को शिक्षा में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने के कारण इस बात पर बल दिया जाने लगा है कि पाठ्यक्रम को जीवनोपयोगी बनाने के लिए उसे बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, अभिवृत्तियों एवं मानसिक योग्यताओं के अनुकूल बनाया जाए। इस दृष्टिकोण से अब यह माना जाने लगा है कि पाठ्यक्रम निर्माताओं को ‘बाल मनोविज्ञान’ का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बाल विकास की प्रत्येक अवस्था की अलग-अलग आवश्यकताएँ एवं विशेषताएँ होती हैं। अतः प्रत्येक अवस्था का पाठ्यक्रम निर्धारण करने के लिए उस अवस्था के बालकों की आवश्यकताओं एवं विशेषताओं से अवगत होना आवश्यक हो जाता है। यह मनोविज्ञान द्वारा ही सम्भव होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के निर्माण में मनोविज्ञान की सहायता अमूल्य बन चुकी है।
(4) शिक्षण विधियाँ –
शिक्षा में मनोविज्ञान को स्थान मिलने के फलस्वरूप शिक्षण विधियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब बालक की रुचि को जागृत करके उन्हें मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जाता है। ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ मनोवैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा निर्धारित की गई हैं। इन विधियों में बालक की रुचि एवं स्वभाव को सामने रखते हुए ‘करके सीखने’, ‘खेल द्वारा सीखने आदि पर बल दिया जाता है। किण्डरगार्टन, मॉण्टेसरी, प्रोजेक्ट, डाल्टन आदि नवीन शिक्षण-विधियाँ मनोविज्ञान पर ही आधारित हैं जिनमें बालकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार जैसा कि रायबर्न ने लिखा है, “मनोविज्ञान के ज्ञान की प्रगति होने के कारण ही शिक्षण-विधियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं।”
(5) बालक या शिक्षार्थी –
शिक्षा में मनोविज्ञान को स्थान प्राप्त होने के पूर्व शिक्षा ‘विषय- प्रधान’ तथा ‘शिक्षक-प्रधान’ थी। किन्तु अब मनोविज्ञान के प्रभाव के परिणामस्वरूप वह ‘बाल-केन्द्रित’ हो गयी है। अब जैसा कि पेस्टालॉजी ने लिखा है, “शिक्षा का मुख्य लक्ष्य अध्यापन नहीं है, बल्कि विकास है अर्थात् बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, प्रगतिशील और व्यवस्थित विकास करना है।” ऐसा तभी सम्भव है जबकि शिक्षा योजना बालकों की रुचियों, मूलप्रवृत्तियों, रुझानों, क्षमताओं एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर निर्मित की जाए। रूसो ने तो यहाँ तक लिखा है कि “बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को अद्योपान्त पढ़ना पड़ता है।” आज शिक्षा बालक के लिए है न कि बालक शिक्षा के लिए। इस प्रकार मनोविज्ञान के प्रभाव के परिणामस्वरूप शिक्षा योजना में बालक को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
(6) शिक्षक-
शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रभाव के परिणामस्वरूप शिक्षक का स्थान एक मित्र, सहायक तथा निर्देशक के समान माना जाता है। शिक्षा-प्रक्रिया में बालक की स्थिति एक पौधे के समान तथा शिक्षक की स्थिति बालक-रूपी पौधे का उपयुक्त विकास करने वाले माली के समान होती है। जिस प्रकार पौधे के विकास के लिए उपयुक्त खाद, मिट्टी, हवा, पानी, रोशनी आदि आवश्यक तत्त्वों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार बालक के विकास के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण की आवश्यकता होती है। इस वातावरण का निर्माण शिक्षक द्वारा ही किया जा सकता है। किन्तु यह वातावरण तभी निर्मित हो सकता है, जबकि उसे बालक के मन व स्वभाव का अच्छी तरह ज्ञान हो। स्किनर के अनुसार, “शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ही आवश्यक, उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण है। कक्षा शिक्षण एवं बालकों के दैनिक सम्पर्क में मनोविज्ञान का प्रयोग किये बिना वह अपने कार्य की कुशलता में सम्पन्न नहीं कर सकता है।” शिक्षक के लिए न केवल शिक्षार्थी का ज्ञान आवश्यक है, बल्कि उसे मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा स्वयं अपने स्वभाव, बुद्धि स्तर, व्यवहार योग्यता आदि का भी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। इस सन्दर्भ में स्किनर ने लिखा है, “शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। इससे वह स्वयं अपनी दुर्बलता को कम करने का प्रयास कर सकता है और शिक्षण कार्य को अधिक से अधिक सफल बना सकता है।” इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए स्किनर ने यहाँ तक कहा है, “शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है।’
(7) विद्यालय –
विद्यालयों का शैक्षिक एवं सामाजिक वातावरण स्वस्थ एवं उपयोगी बनाने में मनोविज्ञान ने महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। प्राचीन व परम्परागत रूप से चलने वाले विद्यालयों की स्थिति ‘कारागार’ के समान थी जहाँ विद्यार्थियों की स्थिति कैदियों के समान तथा शिक्षक की स्थिति जेलर के समान थी। किन्तु जब से शिक्षा में मनोविज्ञान को स्थान प्राप्त हुआ है तब से इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जाने लगा है, जहाँ बालकों के विकास के लिए स्वतंत्र एवं स्वाभाविक वातावरण प्राप्त हो। मनोविज्ञान पर आधारित इन नवीन विद्यालयों के सम्बन्ध में के. जी. सैयदेन ने ठीक ही लिखा है, “नवीन विद्यालय बालक के प्रति अपने दृष्टिकोण में परम्परागत विद्यालय से भिन्न है। नवीन विद्यालय बालक की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्त्व देता है। यह इस मनोवैज्ञानिक तत्त्व पर विश्वास करता है कि बालक का वास्तविक विकास तभी सम्भव होगा जब उसकी जन्मजात शक्तियों एवं योजनाओं को वातावरण से पूर्ण स्वतंत्रता मिले।” इसी प्रकार रॉयन ने लिखा है, “आधुनिक समय में अनेक विद्यालयों में हम मित्रता और सहर्ष का वातावरण पाते हैं। अब उनमें परम्परागत औपचारिकता, मजबूरी, मौन, ताण्डव एवं दण्ड के प्रायः दर्शन नहीं होते हैं।” जॉन एडम्स ने भी यहाँ तक कहा है, “शिक्षा को मनोविज्ञान ने बाँध लिया है। मनोविज्ञान सिद्धान्तों की उपयोगिता को जाँचने के लिए सबसे अच्छा विद्यालय है।”
(8) अनुशासन –
प्राचीन समय में बालकों को अनुशासित रखने में दमन, दण्ड एवं बाध्यता का बोलबाला था। उनकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों, सुकोमल भावनाओं, सरल इच्छाओं एवं विकसित बुद्धि को कोई स्थान नहीं दिया जाता था । किन्तु शिक्षा के मनोविज्ञान से प्रभावित होने के कारण अब ‘दमनात्मक अनुशासन’ के स्थान पर ‘मुक्त्यात्मक अनुशासन’ को स्थान दिया जाने लगा है जिसमें बालकों को अपनी रुचियों, अभिवृत्तियों, भावनाओं एवं विचारों को व्यक्त करने का पूर्ण अवसर दिया जाता है और उनमें ‘आत्म अनुशासन’ की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। वर्तमान समय में अनुशासनहीनता की समस्याओं के कारणों को खोजकर मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्हें स्नेह, प्रशंसा, सहानुभूति, पुरस्कार आदि के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता है। अनुशासन के इस मनोवैज्ञानिक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए मूलर ने लिखा है, “अपने सबसे नवीन एवं सम्यक् रूप में अनुशासन का तात्पर्य यह है कि बालक तथा बालिकाओं को एक प्रजातांत्रिक सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना, अनुशासन का प्रयोजन व्यक्ति को ज्ञान, शक्ति, आदतें, रुचियों एवं आदर्शों को जो उसके स्वयं की उसके मित्रों तथा सम्पूर्ण समाज की भलाई के लिए निर्मित होते हैं, प्राप्त करने में सहायता करना है।”
(9) समय सारणी –
मनोविज्ञान के अनुसार समय-सारणी के अन्तर्गत जिन पाठ्य विषयों एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं को रखा जाए उनके सम्बन्ध में यह विचार किया जाए कि अधिक परिश्रम की आवश्यकता वाले विषयों को वे समय निर्धारित किये जाएँ जिनमें बालक थके न हों और मस्तिष्क में ताजगी हो। इस दृष्टिकोण से गणित, भाषा आदि को सबसे अच्छा समय देना चाहिए और सरल विषयों एवं पाठ्य-सहगामी क्रियाओं को वह समय दिया जाय जिसमें बालक थकान अनुभव कर रहे हों। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए समय-सारिणी में अवकाश, खेलकूद आदि के लिए भी समय निश्चित किया जाए।
(10) मूल्यांकन –
शिक्षा में मनोविज्ञान की प्रविष्टि के पूर्व बालकों के अर्जित ज्ञान एवं प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु मौखिक एवं लिखित परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता रहा। मनोविज्ञान की दृष्टि से इससे बालकों की योग्यता का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता। अतः परम्परागत परीक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करने हेतु अब शिक्षा मनोविज्ञान ने अनेक नवीन विधियाँ जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा आदि की खोज की। इनके द्वारा बालकों को उपलब्धियों की माप एवं मूल्यांकन भली-भाँति विश्वसनीय ढंग से किया जाता है।
शिक्षा का मनोविज्ञान के विषय-क्षेत्र पर प्रभाव —
जिस प्रकार मनोविज्ञान ने शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित किया है उसी प्रकार शिक्षा ने भी मनोविज्ञान के विषय-क्षेत्र आदि को प्रभावित किया है, जैसे-
(1) मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति-शिक्षा एवं मनोविज्ञान के परस्पर प्रभाव के परिणामस्वरूप मनोविज्ञान की एक नवीन शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई जिसका अध्ययन शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों विषयों के अन्तर्गत किया जाने लगा है। वस्तुतः शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य सम्बन्ध ‘सीखने की प्रक्रिया’ से है। यह शिक्षा के ‘मनोवैज्ञानिक पहलुओं’ के वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत शैक्षिक व्यवहारों व क्रियाओं का शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है।
(2) मनोविज्ञान की अध्ययन-वस्तु का समृद्ध होना- जब शिक्षा तथा मनोविज्ञान के परस्पर प्रभाव के परिणामस्वरूप मनोविज्ञान की एक नवीन शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का विकास हुआ
तो मनोविज्ञान की अध्ययन वस्तु का समृद्ध व विस्तार होना स्वाभाविक हो गया और इस प्रकार शिक्षा के विकास के साथ ही मनोविज्ञान ने शैक्षिक क्षेत्र में भी अपने लिए अध्ययन सामग्री प्राप्त कर ली। अब मनोवैज्ञानिक केवल ‘मानव व्यवहार’ मात्र का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह सीखने वाली परिस्थितियों का भी गम्भीर रूप से अध्ययन करने लगा है।
(3) शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक शोधों का सूत्रपात – शिक्षा एवं मनोविज्ञान के परस्पर बचाव के परिणामस्वरूप केवल मनोविज्ञान की एक नवीन शाखा शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म तथा उसकी विषय-सामग्री का विस्तार ही नहीं हुआ, बल्कि शिक्षा से सम्बन्धित अनेक समस्याओं पर मनोवैज्ञानिकों ने शोध-कार्य प्रारम्भ कर दिये हैं, जैसे समस्यात्मक बालकों का अध्ययन, पिछड़े एवं प्रतिभाशाली बालकों को शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन आदि।
प्रश्न 3 (i) विकास और अभिवृद्धि में क्या अन्तर है? किशोरावस्था के सांवेगिक एवं सामाजिक विकास की विशेषताओं और समस्याओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर –
वृद्धि एवं विकास में अन्तर —
वृद्धि एवं विकास ये दोनों शब्द प्रायः बिना कोई भेदभाव किये पर्यायवाची रूप में काम में लाये जाते हैं। दोनों यह प्रकट करते हैं कि गर्भाधान के समय से किसी विशेष समय तक किसी प्राणी में कितना कुछ परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में वातावरण की शक्तियों और शिक्षा का बहुत हाथ । इनकी कृपा से हमारे व्यक्तित्व के सभी पहलुओं-शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि का सब ओर से वृद्धि एवं विकास होता है। इस तरह से वृद्धि और विकास दोनों शब्दों का प्रयोग बालक में आयु के बढ़ने के साथ-साथ होनेवाले परिवर्तनों के लिए किया जाता है और इसीलिए यह आवश्यक रूप से वंशानुक्रम और वातावरण की उपज कहा जाता है।
वृद्धि एवं विकास के अन्तर को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं-
वृद्धि
1. वृद्धि शब्द तादाद या परिमाण सम्बन्धी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ आकार, लम्बाई, ऊँचाई और भार आदि में होनेवाले परिवर्तन को वृद्धि कहकर पुकारते हैं
2. वृद्धि एक तरह से सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है। विकास के परिमाण और तादाद सम्बन्धी पक्ष के परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है।
3. वृद्धि शब्द व्यक्ति के शरीर के किसी भी अवयव तथा व्यवहार के किसी भी पहलू होने वाले परिवर्तनों को प्रकट कर सकता है।
4. वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ-साथ यह समाप्त हो जाती है।
5. वृद्धि के फलस्वरूप होनेवाले परिवर्तन बिना कोई विशेष प्रयास किये दृष्टिगोचर हो सकते हैं। साथ ही इन्हें भली-भाँति मापा भी जा सकता है।
6. वृद्धि के साथ-साथ सदैव विकास होना भी आवश्यक नहीं है। मोटापे के कारण एक बालक के भार में वृद्धि हो सकती है, परन्तु इस वृद्धि से उसकी कार्यक्षमता एवं कार्य- कुशलता में कोई वृद्धि नहीं होती और इस तरह से उसकी वृद्धि विकास को साथ लेकर नहीं चलती है।
विकास–
1. विकास शब्द वृद्धि की तरह केवल परिमाण सम्बन्धी परिवर्तनों को व्यक्त न कर ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है।
2. विकास शब्द अपने-आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका ही एक भाग है। यह व्यक्ति में होनेवाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है।
3. विकास किसी एक अंग-प्रत्यंग में अथवा व्यवहार के किसी एक पहलू में होने वाले परिवर्तनों को नहीं, बल्कि व्यक्ति में आनेवाले सम्पूर्ण परिवर्तनों को इकट्ठे रूप में व्यक्त करता है।
4. विकास एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर समाप्त न होकर यह आजीवन चलती है।
5.विकास शब्द कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आनेवाले गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रकट करता है। इन परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप में मापना कठिन नहीं है। इन्हें केवल अप्रत्यक्ष तरीकों, जैसे – व्यवहार करते हुए बालक का निरीक्षण करना आदि से ही मापा जा सकता है।
6. दूसरी ओर विकास वृद्धि के बिना भी सम्भव हो सकता है। कई बार यह देखा जाता है कि कुछ बच्चों की ऊँचाई, आकार एवं भार में समय गुजरने के साथ-साथ कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखायी देता, परन्तु उनकी कार्यक्षमता तथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक योग्यता में बराबर प्रगति होती रहती है।
किशोरों की सामाजिक तथा संवेगात्मक विशेषताएँ —
किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य अस्थिरता का काल है। मनोवैज्ञानिक और शिक्षाशास्त्री इस अवस्था को ‘विकट अवस्था’ या ‘समस्या की अवस्था’ कहते हैं। अस्थिरता के इस काल में व्यक्ति बचपन की आदतों को छोड़कर परिपक्व व्यवहार की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार वह बाल्यावस्था की अभिवृत्तियों का परिपक्व अभिवृत्तियों में परिवर्तन करने लगता है। किशोरावस्था परिपक्वता की देहली पर होता है जहाँ उसे ऐसे निर्णय और समायोजन करने पड़ते हैं जिनका प्रभाव उसके आगे के जीवन पर दिखायी पड़ता है। कुहलेन के अनुसार, “वह स्वयं के प्रति अनिश्चय और अपनी स्थिति के प्रति असुरक्षा का अनुभव करता है। ”
1. अस्थिरता – कोल और ब्रूस के अनुसार, “किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिह्न संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है।” संवेगात्मक अस्थिरता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। किशोरावस्था में आकर किशोर की बाल्यकालीन सांवेगिक स्थिति समाप्त हो जाती है और वह शैशवकालीन सांवेगिक अस्थिरता की पुनरावृत्ति करता हुआ प्रतीत होता है। वैलेन्टाइन के अनुसार, “अस्थिरता किशोर का सामान्य चिह्न है— संवेगों और रुचियों की स्थिरता।”
किशोर वातावरण की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति को नवीन दृष्टिकोण से देखता है और अपने ढंग से समझने का प्रयत्न करता है।
किशोर बालक में संवेगों की अस्थिरता का कारण उसका भावप्रधान होना है। थोड़े ही समय में वह असीम उमंगों से भर जाता है और थोड़े ही समय बाद घोर उदासीनता की स्थिति में पहुँच जाता है इसका कारण यह है कि उसमें शारीरिक और मानसिक शक्तियों का संचार इतनी तीव्रता से होता है कि वह समस्त कार्यों को एकबारगी समाप्त कर लेना चाहता है। अस्थिरता का प्रदर्शन वह सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना में भी करता है। किशोर के विचार और निश्चय स्थिरता नहीं प्राप्त कर पाते।
2. तीव्र सांवेगिकता – किशोरावस्था में पदार्पण करते ही किशोरों में तीव्र सांवेगिकता पैदा हो जाती है। उसके प्रत्येक संवेग तीव्रतर रूप से प्रकट होते हैं। क्रोध की स्थिति में अधिक क्रोध प्रकट करना, विषमलिंगियों के प्रति अधिक आकृष्ट होना या सामाजिक स्वीकृति का भय आदि सब कुछ तीव्र रूप में दिखायी पड़ता है। किशोरों के संवेगों का तीव्र रूप निम्नलिखित कारणों से प्रकट होता है-
(i) प्रतिकूल पारिवारिक सम्बन्ध।
(ii) अभिभावकों का कठिन नियन्त्रण और निरीक्षण।
(iii) किशोर की इच्छापूर्ति में बाधक कठिनाइयाँ।
(iv) ऐसी परिस्थितियाँ जिससे वह अपने को असहाय पाता है।
(v) अधिक व्यवहार की सामाजिक प्रत्याशा।
(vi) नये वातावरण के साथ समायोजन।
(vii) मित्रों या परिवार के साथ संघर्ष।
(viii) विषमलिंगियों के साथ सामाजिक समायोजन।
(ix) व्यवसाय की समस्याएँ।
3. पलायन या प्रत्याक्रमण —
वह आदर्श व्यक्तियों से प्रेरणा ग्रहण करता है जिससे उसमें उच्च विचार जैसा आदर्श पैदा हो जाता है और इन्हें ही वह व्यवहार में प्रकट करना चाहता है। किशोर के आदर्शवादी विचार समाज की जटिल परिस्थितियों के कारण छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, उसे पराजय तथा निराशा का सामना करना पड़ता है। पराजय तथा निराशा की यह स्थिति या तो उसे पलायनवादी बना देती है या आक्रमणकारी। पलायन की स्थिति में या वह आत्महत्या कर लेता है या दिवास्वप्नों के मनोराज्य से अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। आक्रमणकारी होने की स्थिति में उसमें क्रोध पैदा होता है और उसका अपने माता-पिता, शिक्षकों तथा मित्रों से मतभेद होने लगता है। ई० बी० हरलॉक ने लिखा है कि “प्रारम्भिक किशोरावस्था उथल-पुथल का काल है। यह माता-पिता, अध्यापकों और मित्रों से अनेक मतभेदों का काल है और नवकिशोर प्रारम्भिक अवस्था की अपेक्षा अधिक सांवेगिकता का अनुभव करता है। वास्तव में किशोर एक जटिल व्यक्ति है।”
प्रश्न 3 (ii)विशिष्ट बालक को परिभाषित कीजिए। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कीजिए।
उत्तर —
विशिष्ट बालक वह है जो अन्तः वैयक्तिक, भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से अन्तर- व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। क्रो व क्रो के शब्दों में, “वह बालक, जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुँचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो विशिष्ट बालक कहलाता है।
कक्षा में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक विशिष्ट बालक की विशेषताएँ होती हैं। उनको आधार या कसौटी मानकर इनकी पहचान की जा सकती है ।
ये विधियाँ निम्न हैं-
(i) सामूहिक परीक्षण – सामूहिक परीक्षणों में बुद्धि के परीक्षण देकर कक्षा के बालकों की बुद्धिलब्धि (I.Q.) देखी जा सकती है।
(ii) व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण – सामूहिक परीक्षण के आधार पर चुने हुए बालकों को बुद्धि से सम्बन्धित व्यक्तिगत परीक्षण करके बुद्धिस्तर का ज्ञान हो सकता है।
(iii) उपलब्धि परीक्षण-बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि जानने के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये वस्तुनिष्ठ परीक्षण देने चाहिए। इसके परिणाम के आधार पर विशिष्ट बालकों का पता लगाया जा सकता है।
प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएँ
स्किनर व हेरीमैन (Skinner and Herriman) ने प्रतिभाशाली बालक में निम्न विशेषताएँ बतायी हैं—
(1) बुद्धि परीक्षाओं में उच्च बुद्धि लब्धि। (130 से 170 तक)।
(2) मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता व तीव्र चिन्तन ।
(3) विशाल शब्दकोश ।
(4) दैनिक कार्यों में विभिन्नता ।
(5) सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठता।
(6) सामान्य अध्ययन में रुचि ।
(7) अमूर्त विषयों में चिन्तन व रुचि ।
(8) अध्ययन अद्वितीय सफलता।
(9) आश्चर्यजनक अन्तर्दृष्टि का परिणाम।
(10) मन्दबुद्धि व सामान्य बालकों में अरुचि।
(11) पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि।
(12) विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता।
(13) किसी विशेष विषय या कार्य में प्रवीणता।
(14) समस्त कार्य व शिक्षा के लिये योग्यता तथा कोई भी बौद्धिक कार्य करने में सक्षम।
(15) टरमन के शब्दों में- “इनके माँ-बाप बच्चे उच्च कुल के होते हैं। ये बालक अच्छी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति वाले परिवार में अधिक मात्रा में पाये जाते हैं।
(16) पढ़ाई में अच्छे होने के साथ वे कला, गायन आदि में भी रुचि लेते हैं, ऐसा हालिगबर्थ का मानना है।”
प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का स्वरूप
प्रतिभावान बालकों की शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए इसके लिए हेविगर्ट्स ने अपनी पुस्तक “A Survey of the Education of Gifted Children’ में लिखा, “प्रतिभावान बालकों के लिये शिक्षा का सफल कार्यक्रम नहीं हो सकता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न योग्यताओं का विकास करना न हो।” इस कथन के अनुसार प्रतिभावान बालकों के कार्यक्रम का स्वरूप निम्नवत् होना चाहिए—
(1) सामान्य रूप से पदोन्नति-
कुछ मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि प्रतिभावान बालकों को एक वर्ष में दो बार कक्षोन्नति दी जानी चाहिए। इसके विपरीत दूसरे मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि ऐसा करना, उनको सीखने की प्रक्रिया के ‘क्रमिक विकास’ के लाभ से वंचित करना है। उनका विचार है कि यह आवश्यक नहीं है कि उनकी सब विषयों में विशेष योग्यता हों। ऐसी दशा में उच्च शिक्षा में पहुँचकर, उसमें असमायोजन उत्पन्न हो सकता है। क्रो व क्रो का सुझाव है, “प्रतिभावान बालक का सामान्य रूप से विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन करना चाहिए।” दूसरे शब्दों में, इनके अनुसार प्रतिभावान बालकों को वर्ष के अन्त में उसी प्रकार पदोन्नति दी जानी चाहिए, जिस प्रकार अन्य बालकों को दी जाती है। I
(2) विशेष एवं विस्तृत पाठ्यक्रम —
एक वर्ष में दो बार उन्नति देने की बजाय प्रतिभावान बालकों के लिए विशेष एवं विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। इस पाठ्यक्रम में हो अधिक व कठिन विषय होने चाहिए, ताकि वे अपनी विशेष योग्यताओं के कारण अधिक ज्ञान का अर्जन कर सकें। इस सम्बन्ध में स्किनर ने लिखा है- “इन बालकों के पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे उनकी मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता और तर्क, चिन्तन और रचनात्मक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनको खोज, मौखिक और स्वतन्त्र कार्यों, क्रियात्मक और प्रयोगात्मक कार्यों के लिए उत्तम अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।”
(3) शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान—
प्रतिभावान बालकों के प्रति शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। उसे उनको नियमित रूप से परामर्श एवं निर्देशन देना चाहिए। इन विधियों का अनुसरण करके ही वह उनको उनकी विशेष योग्यताओं के अनुसार प्रगति करने के लिये अनुप्रभावित एवं अनुप्रेरित कर सकता है।
(4) चुनाव व वर्गीकरण—
प्रतिभावान बालकों की उचित शिक्षा हेतु सर्वप्रथम यह पता लगाना आवश्यक हैं कि किस ‘कक्षा’ (Class) में कौन-कौन से बालक प्रतिभावान हैं। इन बालकों का चुनाव निम्न आधार पर किया जा सकता है, जैसे –
(1) बुद्धि परीक्षाएँ,
(2) व्यक्तित्व परीक्षाएँ,
(3) उपलब्धि व निष्पत्ति परीक्षाएँ,
(4) पूर्व कक्षाओं के प्राप्तांक,
(5) शिक्षकों एवं माता-पिता की सम्मतियाँ आदि।
(5) नेतृत्व का अवसर व प्रशिक्षण-प्रतिभाशाली बालकों को अन्य बालकों एवं लोगों का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे वे व्यावहारिक जीवन में प्रवेश कर मानव कल्याण कर सके। क्रो व क्रो के अनुसार, “क्योंकि हम प्रतिभाशाली बालक से नेतृत्व की आशा करते हैं, इसलिए उनको विशिष्ट परिस्थितियों में नेतृत्व का अवसर और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।” जैसे—मानीटर, स्काउट, कम्पनी हेड आदि।
(6) संस्कृति की शिक्षा-बहुत से शिक्षाशास्त्रियों ने प्रतिभावान बालकों को अपनी संस्कृति
और उसके विकास की शिक्षा देने का सुझाव दिया है। इस सन्दर्भ में हॉलिगबर्थ ने अपनी पुस्तक ‘An Enriched Curriculum for Rapid Learners’ में लिखा है, “प्रतिभावान बालकों को सभ्य समाज में स्थान देने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें विशेष प्रकार से संस्कृति के उद्भव व विकास के विषय में जो अब तक हो चुका है, बताना चाहिए क्योंकि अब वे संस्कृति को समझने लगते हैं व उन पर संस्कृति का प्रभाव भी पड़ने लगता है, बल्कि साधारण वस्तुओं, भोजन, रक्षा, आदि इसी प्रकार की वस्तुएँ, सम्पत्ति है। इस माध्यम से उन्हें उत्तेजित किया जा सकता है और उनकी ‘बौद्धिक उत्सुकता’ को सन्तुष्ट किया जा सकता है।”
(7) सामान्य बालकों के साथ शिक्षा-कुछ शिक्षा विशेषज्ञों का मत है कि प्रतिभावान बालकों को सामान्य बालकों से पृथक् विशिष्ट कक्षाओं एवं विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके विरोध में दूसरे मनोवैज्ञानिकों का मत है कि इससे उनमें घमण्ड की भावना आ जाती है और वे सबके साथ समायोजन नहीं कर पाते। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सामान्य व कम बुद्धि के बालकों के साथ मिलने-जुलने का अवसर प्रदान किया जाए जिससे मधुर सम्बन्ध बन सके। ऐसा करने से उनमें न तो अभिमान की भावना आयेगी और न ही भविष्य में सामान्य लोगों के साथ रहने में कोई परेशानी होगी।
( 8 ) विशेष अध्ययन की सुविधाएँ—प्रतिभावान बालकों की सामान्य विषयों के अध्ययन में विशेष रुचि होती है। उनकी इस रुचि का विकास करने के लिए एवं उनको अधिक अध्ययन के लिए प्रोत्साहन करने के विचार में विभिन्न विषयों की पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय होना चाहिए। इस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएँ उनके अधिक ज्ञान का अर्जन करने में अपूर्व सहायता दे सकती है।
( 9 ) पाठ्य सहभागी क्रियाओं का आयोजन—प्रतिभावान बालकों में रुचियों का बाहुल्य होता है। उनकी सन्तुष्टि केवल अध्ययन से ही नहीं हो सकती। अतः विद्यालय को अधिक से अधिक पाठ्य सहभागी क्रियाओं का उत्तम आयोजन करना चाहिए, जैसे— सरस्वती यात्राएँ, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, स्काउटिंग आदि।
(10) सामाजिक अनुभवों के अवसर—प्रतिभावान बालकों को सामान्य बालकों की सामाजिक क्रियाओं से पृथक् नहीं रखना चाहिए। इन क्रियाओं में भाग लेकर उनको सामाजिक अनुभव प्राप्त होते हैं। ये अनुभव उनको निश्चित रूप से सहायता प्रदान करते हैं ताकि वे अनुभवों से सामाजिक समायोजन कर सकें। क्रो व क्रो के अनुसार, “प्रतिभावान बालक को सामाजिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर दिये जाने चाहिए, ताकि वह सामाजिक असमायोजन से अपनी रक्षा कर सकें।
(11) व्यक्तित्व का पूर्ण विकास-प्रतिभाशाली बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के साथ व्यक्तित्व विकास भी तीव्र गति से किया जाए। Seheiffle ने अपनी पुस्तक ‘The Gifted Child in the Regular Classroom’ में लिखा है, “प्रतिभावान बालक की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सदैव उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होना चाहिए। इस दिशा में परिवार, विद्यालय और समाज को एक-दूसरे को इस प्रकार सहयोग देना चाहिए कि प्रारम्भिक बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो जाए।”
प्रश्न 3 (iii) किशोरावस्था की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर –
किशोरावस्था की समस्याएँ
किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएँ निम्न प्रकार हैं-
(1 ) आत्म-सम्मान, आत्म-स्वीकृति तथा सुरक्षा की समस्या-
ये तीनों ही बातें किशोर को अधिक चिन्तित रखती हैं। आत्म-सम्मान की दृष्टि से वह घर में या समूह में जहाँ कहीं भी रहता है, सम्मान चाहता है। इसी दृष्टि से वह कक्षा मॉनीटर, कैप्टन या छात्र संघ का पदाधिकारी बनने की इच्छा रखता है। वह चाहता है कि उसके द्वारा किये गये कार्यों की दूसरे सराहना करें, माता-पिता, अध्यापकों एवं संगी-साथियों का स्नेह मिले। जो किशोर अत्यधिक गरीब होते हैं उन्हें असुरक्षा की भावना हर समय सताती रहती है। परिणामस्वरूप वे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति ‘उसके समायोजन को बेहतर बनाती है तथा इनकी पूर्ति न होने पर उसका व्यक्तित्व दोषपूर्ण बन जाता है।
(2) स्वतन्त्रता की समस्या-इस अवस्था में किशोर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है ‘तथा अपने भविष्य की कल्पनाओं को साकार करने के लिए वह पूर्ण स्वतन्त्रता चाहता है और किसी की सलाह को अपने रास्ते में हस्तक्षेप समझता है, लेकिन किशोर इतना समर्थ नहीं होता कि उसे ‘भविष्य सम्बन्धी निर्णय लेने में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाय, यह उचित नहीं। माता-पिता व अध्यापकों के मार्गदर्शन की तो आवश्यकता उसे पड़ेगी ही। इस तथ्य को समझे बिना किशोर अपने लक्ष्य को पाने में उलझकर रह जाता है। अतः उसे चाहिए कि वह अपनी सीमाओं और क्षमताओं को समझे तथा दूसरों के सहयोग से अपनी मंजिल प्राप्त करे। दूसरों से प्राप्त सहयोग को उसे अपनी प्रतिष्ठा या अहं का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए।
(3) सुख एवं आनन्द की चाह -इस अवस्था को सुखद अवस्था भी कहा जाता है। किशोर अत्यधिक सुख एवं आनन्द की कामना करता है। उसे सिनेमा देखना, होटलों में जाना, कहानी-उपन्यास पढ़ना या लिखना, गाने सुनना, अभिनय करना अच्छा लगता है। विपरीत सेक्स से दोस्ती करना उसकी सबसे प्रबल इच्छा रहती है। लड़के, लड़कियों से तथा लड़कियाँ, लड़कों से बात करने की हर समय इच्छुक रहती हैं। उन्हें सेक्स सम्बन्धी जानकारी अच्छी लगती है तथा वे इसकी पूर्ति सेक्स सम्बन्धी साहित्य पढ़कर, पशुओं की मैथुन क्रिया देखकर, चलचित्रों में नग्न चित्र देखकर तथा मित्रों से इस सम्बन्ध में बात करके करते हैं तथा अपनी इस भावना का प्रदर्शन शौचालयों की दीवारों पर गन्दी बातें लिखकर व चित्र बनाकर करते हैं। सम-लिंगीय मैथुन, भिन्न-लिंगीय मैथुन, हस्त मैथुन, अश्लील बातें करना, प्रेम-पत्र लिखना आदि में इनकी प्रबल रुचि होती है।
(4) आत्म-निर्भर बनने की समस्या-किशोर यह अहसास करने लगता है कि अब वह बड़ा हो गया है तथा उसे माता-पिता पर बोझ नहीं बनना चाहिए। दूसरे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उसे धन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वह आत्म-निर्भर होना चाहता है तथा किसी अच्छे व्यवसाय को अपनाना चाहता है। यह विचार पहले तो कल्पना लगती है, फिर बेकार की बात लगती है और अन्त में वह लक्ष्य-प्राप्ति के लिए गम्भीर हो जाता है। देखने में आता है कि निर्धन परिवारों के किशोर अपने माता-पिता का व्यवसाय अपनाने में रुचि नहीं रखते जबकि उच्च परिवारों के किशोर अपने माता- पिता का व्यवसाय अपनाने में रुचि रखते हैं। कुछ किशोरों में यह भावना इतनी हावी रहती है कि उनके व्यवहार में यह स्पष्ट दिखायी देती है। बड़े शहरों में किशोर अपने लक्ष्य के लिए अधिक बेचैन रहते हैं।
(5) बिछुड़ने का भय या स्नेह की लालसा-ये दोनों ही भावनाएँ किशोर पर हर समय छायी रहती हैं। अपनी भावनात्मक सन्तुष्टि के लिए वे अपने दोस्तों पर अधिक निर्भर रहते हैं। वे दूसरों से स्नेह लेना चाहते हैं और दूसरों को भी स्नेह देना चाहते हैं। उनका कोई दोस्त उनसे अगर थोड़े समय के लिए भी रूठ जाय या बिछुड़ जाय तो उन्हें सहन नहीं होता। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। समूह में अपना स्थान बना लेने पर वे सुरक्षित महसूस करते हैं तथा इसके विपरीत यदि उन्हें समूह में उचित स्थान नहीं मिलता या तिरस्कार मिलता है तो वे दुःखी होते हैं जो कभी-कभी घातक भी सिद्ध होता है। किशोर अपने माता-पिता से एक बार तो दूर रह सकता है लेकिन अपने संगी-साथियों से दूर रहने की कल्पना से ही डरने लगता है।
(6) नैतिक मूल्यों में बँधे रहने की समस्या- किशोर नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक मूल्यों को बन्धन महसूस करता है। उसे एक ही समय पर बहुत से मूल्यों में बँधना होता है। माता-पिता का कठोर अनुशासन, स्कूल का वातावरण, दोस्तों की भावनाएँ आदि उसे एक साथ निभानी पड़ती हैं
(7) वीर-पूजा – किशोरों में वीर-पूजा की भावना विकसित हो जाती है। वे आदर्श पुरुष का अनुकरण प्रारम्भ कर देते हैं। अपने को अपने आदर्श पुरुष के अनुरूप बनाने का प्रयास करने लगते हैं |आदर्श पुरुषों के लिए विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित हो सकते हैं। सिनेमा का अभिनेता या अभिनेत्री ऐतिहासिक वीर-पुरुष या धार्मिक नेता, राजनैतिक नेता या विद्वान् उनके आदर्श पुरुष हो सकते हैं। भारत में आजकल अधिकांश किशोर या किशोरी का आदर्श पुरुष सिने-जगत् का अभिनेता या अभिनेत्री होती है। वे उसी के अनुरूप बनने के लिए वैसे ही वस्त्र पहनना, उसी की तरह बाल रखना तथा उसी की भाँति बोलना प्रारम्भ कर देते हैं। कॉलेजों में किशोर या किशोरियों के आदर्श पुरुष कोई अध्यापक या अध्यापिका होती हैं जो उनको अधिक प्रभावित करते हैं। किशोर अपने आदर्श व्यक्ति का गुणगान करते नहीं थकते हैं। कभी-कभी इस वीर-पूजा की परिणति प्रेम के रूप में भी देखी जा सकती है।
(8) विद्रोह की भावना-किशोर में स्वाभिमान की भावना का विकास हो जाता है। अब वह माता-पिता या अध्यापक के नियन्त्रण को पसन्द नहीं करता है। बी० एन० झा ने लिखा है कि किशोर में नवीन जीवन-दर्शन के प्रादुर्भाव से उसमें आत्मसम्मान की प्रबल प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। वह अपने को बन्धनों से मुक्त रखना पसन्द करता है। कॉलसनिक का कथन है कि किशोर, प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है क्योंकि वे उसकी स्वतन्त्रता पर नियन्त्रण रखना चाहते हैं। प्रौढ़ों के नियन्त्रण के विरोध में किशोर विद्रोह प्रारम्भ कर देते हैं। माता-पिता या अध्यापक की आज्ञा का विरोध करने लगते हैं।
|
(9) विशेष रुचियाँ-आयु में वृद्धि के साथ रुचियों में भी परिवर्तन होता है। स्ट्रांग के अनुसार, 15 वर्ष की आयु तक किशोरों की रुचियाँ परिवर्तित होती रहती हैं किन्तु इसके बाद उनमें स्थिरता आने लगती है। किशोर और किशोरी में कुछ समान रुचियाँ होती हैं तथा कुछ असमान रुचियाँ। समान रुचियाँ सामान्यतः कहानी, नाटक, उपन्यास का पढ़ना, शरीर को सुन्दर बनाना, नवीन फैशन के वस्त्र पहनना, विषमलिंगी के साथ प्रेम करना, रेडियो सुनना, सिनेमा देखना आदि हैं। दोनों की रुचियों में भिन्नता इस प्रकार हैं-लड़के खेल-कूद, व्यायाम तथा भावी व्यवसाय के चयन में अधिक रुचि लेते हैं किन्तु लड़कियों की विशिष्ट रुचियाँ संगीत, कला, अभिनय, श्रृंगार करने के कार्यों में दिखायी देती हैं।
(10) यौन-विकास- किशोरावस्था का महत्त्वपूर्ण लक्षण यौनिक विकास है। इस काल में किशोर या किशोरी के यौन अंगों में पर्याप्त वृद्धि होने से उनमें प्रजनन शक्ति आ जाती है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि शैशवावस्था की यौन भावना की पुनरावृत्ति किशोरावस्था में आरम्भ होती है। इसीलिए किशोर-काल को यौन भावना का जागृति काल कहते हैं। यौन भावना का इस काल में विस्फोट-सा होता है। किशोर पर काम प्रवृत्ति का ज्वार-सा चढ़ जाता है। किशोर में यौन-विकास की तीन प्रमुख अवस्थाएँ होती हैं, जो इस प्रकार हैं-
(i) स्व-प्रेम- किशोर-काल में यौन-विकास की प्रारम्भिक अवस्था स्व-प्रेम की होती है। स्व-प्रेम के दो रूप होते हैं-एक रूप के अनुसार किशोर अपने को सबसे अधिक सुन्दर मानता है। इस सुन्दरता को बढ़ाने के लिए वह सौन्दर्य-प्रसाधनों का प्रयोग करता है। बार-बार दर्पण में अपने शरीर को देखकर आनन्दित होता है। कभी अपने बालों को सँवारता है तो कभी बार-बार वस्त्र बदलकर देखता है कि कौन-सा वस्त्र उसके शरीर की सुन्दरता को अधिक बढ़ाता है। फ्रॉयड ने इस स्थिति को Narcisism की स्थिति कहा है। दूसरे रूप में, किशोर अपने लिङ्ग-अवयवों का स्पर्श करके यौनिक आनन्द की अनुभूति करता है। अब उसको लिङ्ग-अवयवों का स्पर्श करने पर गुदगुदी-सी अनुभव होती है। ऐसा करने से किशोर में हस्तमैथुन (Masturbation) जैसी गन्दी आदत का विकास हो जाता है। यह हस्तमैथुन की आदत केवल लड़कों में ही नहीं होती है अपितु लड़कियाँ भी इसकी शिकार बनती हैं। आजकल मनोवैज्ञानिक हस्तमैथुन को स्वाभाविक क्रिया मानते हैं, किन्तु फिर भी इस प्रकार की अप्राकृतिक कार्यों का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।
(ii) समलिङ्गीय कामुकता-यौन-विकास की दूसरी अवस्था समलिङ्गी कामुकता की है। इस अवस्था में समान लिङ्ग के व्यक्तियों में परस्पर प्रेम होता है। लड़के, लड़कों के साथ और लड़कियाँ, लड़कियों के साथ रहना, घूमना, खाना, बातचीत करना पसन्द करते हैं। वे आपस में चुम्बन लेते हुए भी देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि दोनों लिङ्ग के व्यक्ति परस्पर अपने समलिङ्ग के गुणों को उत्तेजित
करने के कार्य में संलग्न पाये जाते हैं। समलिङ्गीय कामुकता के लिए कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं। एक कारण समलिङ्गीय कामुकता का लड़के-लड़कियों को एक-दूसरे से दूर रखने से सम्बन्धित है। जब विषमलिङ्ग के साथ मेल-जोल बढ़ाने का अवसर नहीं मिलता तो किशोरावस्था में बालक काम-प्रवृत्ति की सन्तुष्टि समलिङ्गीय प्रेम के द्वारा करते हैं। भारतीय समाज में यही स्थिति है। यहाँ लड़कों को लड़कियों से पृथक् रखा जाता है। अतएव वे समलिङ्ग को ही कामुकता की सन्तुष्टि का साधन मानने लगते हैं। समलिङ्गीय कामुकता उन विद्यालयों में भी पायी जाती है जहाँ सहशिक्षा का अभाव रहता है। सहशिक्षा के अभाव के कारण विषमलिङ्ग के प्रति आकृष्ट होने तथा प्रेम करने का अवसर नहीं मिलता है। रेम्जे, झिंगरन और किंसे ने अपने अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि समलिङ्गीय कामुकता प्रारम्भिक किशोरावस्था में अधिक पायी जाती है। किंसे का मत है कि लगभग एक-चौथाई किशारों में समलिङ्गीय कामुकता का प्रभाव रहता है। समलिङ्गीय कामुकता शीघ्र परिपक्व होनेवाले लड़कों में देर से परिपक्व होनेवालों की अपेक्षा अधिक पायी जाती है। कभी-कभी समलिङ्गीय कामुकता की प्रवृत्ति किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार की अवस्था शोचनीय होती है। इस प्रकार का अप्राकृतिक कार्य प्राकृतिक विषमलिङ्गी कामुकता में बाधक बन जाता है।
(iii) विषम-लिङ्गी कामुकता – यौन प्रवृत्ति की परिपक्व अवस्था विषमलिङ्गी कामुकता है जो उत्तर किशोरावस्था में विकसित होती है । यौन सम्बन्धों की यह प्राकृतिक एवं स्वाभाविक दशा है। इस स्थिति में किशोर लड़के, लड़कियों की और लड़कियाँ लड़कों की ओर आकृष्ट होती हैं, वे परस्पर बातचीत करते, आपस में मिलते-जुलते हैं। घनिष्ठता और बढ़ने पर वे सिनेमा देखने, चुम्बन करते तथा आलिंगन करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ शादी से पूर्व ही सम्भोग क्रिया में रत पाये जाते हैं। यह स्थिति भयानक होती है और उनको सभी समाज में हेय दृष्टि से देखते हैं। शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने के भय से अभिभावक लड़के-लड़कियों के मिलने पर नियन्त्रण लगाते हैं, जिसके कारण लड़कों- लड़कियों में अनुशासनहीनता फैलती है। यदि लड़कों-लड़कियों को सामूहिक रूप में कार्य करने को प्रोत्साहित किया जाय तो उनमें यौन-सम्बन्धों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण पैदा किया जा सकता है।
इकाई-II
प्रश्न 4 (i) अनुबन्ध क्या है? सीखने के स्किनर सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
अथवा
स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के क्रिया-प्रसूत अनुकूलन सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
अथवा
अनुबद्ध अनुक्रिया-सिद्धान्त ( क्रिया-प्रसूत अनुबन्ध का सिद्धान्त ) की व्याख्या तथा मूल्यांकन कीजिए। इसके शैक्षिक निहितार्थ बताइए।
अथवा
अधिगम के स्किनर द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त में प्रमुख बिन्दुओं को समझाइए । यह सिद्धान्त थार्नडाइक के सिद्धान्त से किस प्रकार भिन्न है? इसके सिद्धान्त के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं?
अथवा
सीखने के सक्रिय अनुबंधन सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर –
स्किनर का क्रिया-प्रसूत अनुबन्ध
व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बी०एफ० स्किनर द्वारा प्रयोगशाला में पशुओं पर अधिगम के क्षेत्र में काफी महत्त्वपूर्ण प्रयोग किये गये हैं। स्किनर ने अपने प्रयोगों के आधार पर अधिगम के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, उसे अनुबद्ध अनुक्रिया-सिद्धान्त या क्रिया-प्रसूत अनुबन्ध का सिद्धान्त कहते हैं।
एफ० स्किनर ने व्यवहार को दो श्रेणियों में रखा है-
1. प्रतिकृत व्यवहार तथा
2. क्रिया-प्रसूत व्यवहार ।
1. प्रतिकृत व्यवहार-ये अनुक्रियाएँ होती हैं जो किसी ज्ञात उंद्दीपन के कारण होती हैं। इनमें एक ज्ञात उद्दीपक एक निश्चित अनुक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे ‘भोजन’ उद्दीपक ‘लार टपकने’ की अनुक्रिया को उत्पन्न करता है।
2. क्रिया-प्रसूत व्यवहार -जब प्राणी के व्यवहार में बिना किसी ज्ञात उद्दीपक के स्वतः स्फूर्त ढंग से अनुक्रिया उत्पन्न होती है तो उसे क्रिया-प्रसूत व्यवहार कहते हैं, अर्थात् वे अनुक्रियाएँ जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण नहीं होतीं, क्रिया-प्रसूत व्यवहार कहते हैं, अर्थात् वे अनुक्रियाएँ जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण नहीं होतीं, क्रिया-प्रसूत व्यवहार कहलाती हैं।
स्किनर के अनुसार मानव-व्यवहार का तीन चौथाई से भी अधिक अंश क्रिया-प्रसूत व्यवहार की श्रेणी में रखा जा सकता है। स्किनर ने जिस प्रकार के अनुबन्धन का तरीका अपनाया, उसमें प्राणी द्वारा क्रिया उत्पन्न करने पर विशेष बल दिया। इसके अन्तर्गत अधिगम-स्थिति को इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि जब तक सीखने वाला वांछित व्यवहार न करे, तब तक उसे पुरस्कार न मिले। यहाँ सीखने वाले को यह अवसर दिया जाता है कि वह अधिगम-स्थिति में सक्रियता की भूमिका कर सके।
स्किनर ने अपना प्रारम्भिक प्रयोग एक कबूतर पर किया था। भूखे कबूतर ने स्वतः क्रिया द्वारा यह सीख लिया कि दाहिनी ओर सिर घुमाकर चौंच मारने से दाना (प्रबलक) मिल जाता है।
क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन में अनुक्रिया को अधिक महत्त्व दिया गया है। इसमें पहले कुछ क्रियाएँ या व्यवहार करना पड़ता है। उसके फलस्वरूप उद्दीपन प्रकट होता है। इसलिए इसमें अधिगम का स्वरूप अउ (R-S) सूत्र में प्रदर्शित करते हैं।
स्किनर के उपर्युक्त प्रयोग से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं-
(i) प्रयोग के आरम्भ से सही अनुक्रिया के बीच कबूतर मनचाहा व्यवहार (जैसे घूमना, इधर-उधर चोंच मारना, बायें सिर घुमाना आदि) करने के लिए स्वतन्त्र है, किन्तु उसे दाना (पुनर्बलक) तभी दिया जाता है जब वह प्रयोगकर्त्ता द्वारा निर्धारित अन्त्य व्यवहार को करता है।
(ii) इस प्रकार के पूर्व-नियोजित कौशल को सिखाने में अधिक समय नहीं लगता।
(iii) प्रयोगकर्त्ता इच्छित व्यवहार होने पर कबूतर को हर बार दाना देता है। मनोवैज्ञानिक शब्दावली में इसे इच्छित अनुक्रिया को पुनर्बलित करना कहेंगे। जब भी सही अनुक्रिया होती है, तब उसे पुनर्बलित किया जाता है, किन्तु गलत अनुक्रिया होने पर उसे दण्ड नहीं दिया जाता है।
क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन के अन्तर्गत होनेवाले कुछ प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाएँ अग्रलिखित हैं-
1. रूपण या व्यवहार- रचना – क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन में रूपण सबसे महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगमकर्त्ता में वांछित व्यावहारिक परिवर्तन लाने के लिए समयानुकूल समुचित पुनर्बलन प्रदान करने से यह सम्बन्धित है। रूपण के प्रक्रम में वांछित व्यवहार तक पहुँचने के लिए एक के बाद एक पुनर्बलन दिया जाता है। वांछित व्यवहार अथवा अन्त्य व्यवहार तक अधिगमकर्त्ता को पहुँचाने के लिए अर्थात् अधिगमकर्त्ता के व्यवहार का वांछित रूपण करने के लिए स्किनर ने तकनीक विकसित किया है।
उदाहरण के लिए, यदि हम कबूतर को निश्चित स्थान पर चोंच मारकर उत्तोलक दबाना सिखाना चाहते हैं, तब इसके लिए हमें क्रम से व्यवहार के इस रूप तक पहुँचना होगा, जब तक कबूतर अन्त्य व्यवहार न करे अर्थात् उत्तोलक को न दबाये, तब तक प्रतीक्षा करना उचित नहीं होगा। इसके स्थान पर अन्त्य व्यवहार तक पहुँचने के प्रक्रम में आने वाली प्रक्रियाओं पर हमें ध्यान देना होगा। पहले, जब कबूतर उत्तोलक के समीप आता है, उसे पुनर्बलन देना चाहिए। इससे उसमें उत्तोलक के समीप रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जायेगी। तत्पश्चात् जब कबूतर उत्तोलक के अत्यन्त समीप आ जाता है, उसे पुनर्बलन देना चाहिए। फिर जब वह उत्तोलक को दबाता है, तभी उसे पुनर्बलन देना चाहिए।
इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध रीति से एक के बाद एक पद पर पुनर्बलन देने से कबूतर अन्त्य व्यवहार के और समीप आ जाता है और अन्त में उसके व्यवहार को मनोवांछित व्यवहार में रूपान्तरित कर दिया जाता है।
रूपण की प्रक्रिया में अनुबन्धन के निम्नलिखित तीन सिद्धान्त प्रयुक्त होते हैं-
(अ) सामान्यीकरण-अधिगमकर्त्ता में एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति को उसी प्रकार की दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकृत कर प्रयुक्त करने की क्षमता होती है। सामान्यीकरण
दो प्रकार का हो सकता है-
(i) उद्दीपन सामान्यीकरण-यह तब होता है जब किसी एक उद्दीपन द्वारा एक अनुक्रिया होती है और उसी प्रकार के किसी अन्य उद्दीपन से भी वही अनुक्रिया हो। उद्दीपन सामान्यीकरण में परिस्थितियाँ या उद्दीपन बदलते हैं, किन्तु अनुक्रिया वही रहती है। उदाहरण के लिए, वाटसन के प्रयोग में एक बालक जोर की आवाज से डरता है, फिर दूध, बिल्ली और यहाँ तक कि रोएंदार कोट पहने हुए अपनी माँ से भी डरता है।
सामान्य घरेलू व्यवहार में भी हम देखते हैं कि छोटे बच्चे अपने पिता के रूप, रंग एवं पहनावे वाले किसी भी पुरुष को पापा या पिताजी कह बैठते हैं।
(ii) अनुक्रिया सामान्यीकरण-रूपण की प्रक्रिया में अनुक्रिया सामान्यीकरण का अधिक महत्त्व है, क्योंकि इसी के सहारे रूपण सम्भव हो पाता है। अनुक्रिया सामान्यीकरण में अनुक्रियायें बदलती हैं। उद्दीपन वही रहता है। उदाहरण के लिए स्किनर के प्रयोग में हमने देखा कि अनुक्रिया सामान्यीकरण के द्वारा ही कबूतर उत्तोलक दबाने की क्रिया के समीप धीरे-धीरे पहुँचता है (पहले उत्तोलक के समीप आना, गर्दन दाहिनी ओर घुमाना और अन्त में सही तरीके से चोंच मारना) ।
(ब) आदत प्रतिस्पर्द्धा-रूपण की प्रक्रिया में दूसरा सिद्धान्त आदत प्रतिस्पर्द्धा का है। सही आदत अथवा अनुक्रिया को अन्य अनुक्रियाओं से प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है। सही अन्त्य व्यवहार तक होने वाली क्रियाओं की शृंखला में प्रत्येक पद पर अन्य व्यवहार भी होते रहते हैं, किन्तु सही व्यवहार को पुनर्बलित किया जाता है। दूसरे व्यवहारों को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। व्यवहारों और आदतों की इस होड़ में वांछित व्यवहार को पुनर्बलित कर सफल बना दिया जाता है।
(स) शृंखलन – रूपण में अन्तिम व तीसरा सिद्धान्त श्रृंखलन का है। रूपण की प्रक्रिया में व्यवहार का प्रत्येक अंश दूसरे अंश से श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। एक अनुक्रिया करने से जो संकेत मिलता है वह दूसरी श्रृंखला से अवश्य जुड़ी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कबूतर के प्रयोग में यदि कबूतर अपनी गर्दन सही दिशा से थोड़ा-सा भी झुकाता है तो उसे पुनर्बलन दिया जाता है। इस आदत के पुनर्बलित होने पर यह आदत दृढ़ हो जाती है। यहाँ से अन्त्य व्यवहार तक आनेवाली एक-एक क्रिया को एक के बाद एक पुनर्बलित करते हुए श्रृंखलाबद्ध कर दिया जाता है। इस तरह कबूतर का समस्त व्यवहार रूपान्तरित हो जाता है।
प्रभावकारी रूपण के तत्त्व-रूपण की तकनीक से ही हम प्राणी के व्यवहारों को सुनिश्चित उद्देश्यों के अनुरूप बदल सकते हैं। प्रभावकारी रूपण के लिए निम्नलिखित बातों का होना अत्यन्त आवश्यक है-
(i) अधिगमकर्त्ता द्वारा सक्रिय अनुक्रिया-प्रत्येक पद पर अधिगमकर्त्ता सक्रियता से भाग लेता है, न कि प्रयोगकर्त्ता या शिक्षक ।
(ii) तत्काल पुनर्बलन- जब भी अधिगमकर्त्ता द्वारा सर्वोत्तम व्यवहार होता है, उसे तत्काल पुनर्बलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में सही या वांछित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाता है।
है।
(iii) क्रमिक उपगमन-अधिगमकर्त्ता पहले जो कुछ भी करता है, उसे पुनर्बलित किया जाता ! अन्त्य व्यवहार तक पहुँचने के लिए जिन-जिन क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें छोटे-छोटे पदों में विभाजित कर दिया जाता है। हर पद पर पुनर्बलन देते हुए क्रमिक उपगमन के सहारे अधिगमकर्त्ता
अन्त्य व्यवहार तक पहुँचाया जाता है
को
(iv) प्रवीणता – प्रवीणता प्रगति पर आश्रित है। सरल एवं प्रथम पद पर सफल और पुनर्बलित होने के पश्चात् ही अधिगमकर्ता को दूसरा पद दिया जाता है अर्थात् जब तक पहले पद पर वह प्रवीण नहीं हो जाता, तब तक उसे दूसरा नया और पहले पद से जटिल पद नहीं दिया जाता।
2. विलुप्तीकरण-क्रिया-प्रसूत अनुबन्ध के अन्तर्गत होने वाली दूसरी महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया विलुप्तीकरण की है। वांछित अनुक्रिया होने पर पुनर्बलन को हटा लेने से या पुनर्बलन न देने से विलुप्तीकरण की प्रक्रिया होती है। मान लीजिए कि चोंच मारने पर दाना देकर इस अनुक्रिया को पुनर्बलित कर सिखा दिया गया है। अब चोंच मारने पर दाना देना बन्द कर दिया जाय तो चोंच मारने पर सीखी हुई अनुक्रिया का विलुप्तीकरण हो जायगा ।
3. सहज पुनः प्राप्ति-विलुप्तीकरण के पश्चात् यदि अधिगमकर्त्ता को प्रायोगिक परिस्थिति से कुछ समय के लिए हटा दें और पुनः वापस लाने पर सीखी हुई अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन दे दिया जाय तो पुराना अनुबंधित अधिगम सहज ही पैदा हो जाता है। इसी घटना को अनुबन्ध के सिद्धान्त में सहज पुनः प्राप्ति कहते हैं।
क्रिया-प्रसूत आदत की सहज पुनः प्राप्ति इन बातों पर निर्भर करती है; विलुप्तीकरण के पश्चात् कितना समय बीता है, पहले अधिगम के समय कितनी बार पुनर्बलन दिया गया था, अधिगम के समय दो पुनर्बलन के बीच समय का कितना अन्तराल दिया गया था।
4. पुनर्बलन – पुनर्बलन का संप्रत्यय क्रिया-प्रसूत अधिगम का प्राण है। इसे भली-भाँति समझे बिना क्रिया-प्रसूत अधिगम को समझना सम्भव नहीं है। पुनर्बलित करना सुदृढ़ करना है। पुनर्बलन किसी क्रिया के पश्चात् घटने वाली एक ऐसी घटना है जो उस क्रिया को पुष्ट करती है अर्थात् उस क्रिया के पुनः होने की सम्भावना बढ़ जाती है। किसी भी प्राणी को हम दो प्रकार से पुनर्बलित कर सकते हैं; कुछ देकर या कुछ उसके पास से हटाकर। अधिगमकर्त्ता को कुछ देकर पुनर्बलित करने को धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। अधिगमकर्त्ता के पास से कुछ हटाकर पुनर्बलित करने को ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं ।
स्किनर ने पुनर्बलन के व्यवहार को नियन्त्रित करने की एक विधि माना है, शास्त्रीय अनुबन्धन के प्रतिपादकों की तरह S-R सम्बन्ध को उत्पन्न करनेवाली एक काल्पनिक युक्ति नहीं। जिस घटना या वस्तु के द्वारा पुनर्बलन होता है, उसे पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन वे घटनाएँ हैं जिनके कारण अनुक्रिया की गति में वृद्धि होती है। स्किनर क्रिया-प्रसूत अनुबन्ध के सिद्धान्त का प्रयोग विद्यालयी अधिगम में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह उसने अभिक्रमित अधिगम की प्रणाली में करके दिखाया। स्किनर ने प्रचलित शिक्षा-पद्धति की निम्नलिखित कमियों का उल्लेख किया है-
(i) अवांछित उद्दीपनों से व्यवहार का नियन्त्रण – विद्यालयों का वातावरण दुःखद अनुभवों तथा भय से भरा होता है।
(ii) व्यवहार और पुनर्बलन के बीच अधिक अन्तर- वर्तमान में विद्यालयों में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक होती है कि सही व्यवहार को तुरन्त पुनर्बलित नहीं किया जा सकता। इसके अभाव में अधिगम की गति पर पुनर्बलन का प्रभाव नहीं पड़ पाता । अत्यन्त विलम्ब से दिया गया पुनर्बलन प्रभावहीन होता है।
(iii) तारतम्य का अभाव – वर्तमान शिक्षा पद्धति में विषय-वस्तु को छोटे-छोटे पदों में क्रमबद्ध करके रखने की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक पद पर पुनर्बलन नहीं दिया जा सकता है।
(iv) स्पष्ट उद्देश्यों का अभाव-कक्षा-शिक्षक प्रत्येक पाठ के व्यावहारिक उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट नहीं होते। उन्हें पता नहीं होता कि वे पाठ को किन व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पढ़ा रहे हैं। उपर्युक्त सभी दोषों को दूर करने में स्किनर के क्रिया-प्रसूत अनुबन्ध पर आधारित अभिक्रमित अधिगम शिक्षण दूर करने का स्पष्ट प्रयास करता है।
थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धान्त अथवा संयोजनवाद (सिद्धान्त)–
थार्नडाइक के सीखने के सिद्धान्त को अनेक नामों से पुकारा जाता है जैसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धान्त, प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धान्त, संयोजनवाद, अधिगम का सम्बन्ध सिद्धान्त ।
थार्नडाइक के अनुसार अधिगम अथवा सीखना सम्बन्ध स्थापित करता है। सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। अधिगम की व्याख्या करते हुए थार्नडाइक ने कहा है,
“अधिगम अथवा सीखना स्नायुमण्डल अथवा तन्त्रिकातन्त्र में परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच संयोग सम्बन्धों का बनना तथा सशक्त होने की बात है।” थार्नडाइक के अनुसार, “जब कोई प्राणी सीखता है तो उसके सामने एक परिवर्तन अथवा उद्दीपक होता है, जो प्राणी को एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट प्रकार के उद्दीपन का एक विशिष्ट अनुक्रिया से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है जिसे उद्दीपन अनुक्रिया सम्बन्ध कहते हैं।”
इस सिद्धान्त के अनुसार समस्त प्राणी प्रयास विधि के द्वारा सीखते हैं। इसमें वे सही अनुक्रिया का एक विशेष उद्दीपन के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की प्रक्रिया में प्राणी को
बहुत से प्रयास करने पड़ते हैं। प्राणी प्रयासों के द्वारा कार्य करता है तथा फलस्वरूप उनकी सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। प्रत्येक प्रयास के बाद उसकी भूलें कम होती रहती हैं।
स्किनर के सक्रिय अनुबन्धन का शैक्षिक महत्त्व- स्किनर का विचार था कि सक्रिय अनुबन्धन के द्वारा शिक्षण-प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसी सिद्धान्त के द्वारा पशु- पक्षियों को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। स्किनर के सक्रिय अनुबन्धन का शैक्षिक महत्त्व निम्नलिखित है-
(1) स्किनर ने अपने सिद्धान्त में पाठ्य-वस्तु को छोटे-छोटे पदों में बाँटने पर बल दिया। अभिक्रमित अधिगम में भी पाठ्य-वस्तु को छोटे-छोटे भागों में बाँटकर उनके फ्रेम्स बनाये जा सकते हैं। इससे अधिगम शीघ्र तथा प्रभावकारी ढंग से होता है।
(2) इस सिद्धान्त का पालन करते हुए शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहारों को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान कर सकता है।
(3) स्किनर के प्रयोगों से यह सिद्ध हो जाता है कि व्यक्ति को सन्तुष्टि प्रदान करने वाली सक्रियता आती है तथा अधिगम भी शीघ्र हो पाता है।
(4) यदि विद्यार्थियों को उनके प्रयासों के परिणामों का ज्ञान करा दिया जाये तो विद्यार्थी अपने कार्य में अधिक उन्नति कर सकते हैं।
(5) स्किनर का विचार था कि अनेक जटिल तथा मानसिक रोगियों को सक्रियता अनुबन्धन के द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है।
(6) स्किनर के इस सिद्धान्त का प्रयोग अभिक्रमित अधिगम के लिए किया गया है। इसी सिद्धान्त के द्वारा ही शब्द भण्डार में वृद्धि की जा सकती है।
(7) सक्रिय अनुबन्धन में पुनर्बलन का अत्यधिक महत्त्व है। पुनर्बलन के अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे-दण्ड, पुरस्कार तथा परिणाम का ज्ञान आदि।
प्रश्न 4 (ii) अधिगम से क्या तात्पर्य है? थार्नडाइक द्वारा दिये गये अधिगम के मुख्य नियम कौन-कौन-से हैं? इन नियमों का कक्ष शिक्षण में क्या महत्त्व है?
अथवा
अधिगम के मुख्य और गौण नियम कौन-कौन से हैं? इन नियमों का शैक्षिक महत्त्व समझाइए ।
उत्तर —
अधिगम का अर्थ —
सूक्ष्म रूप से अधिगम का अर्थ हुआ अनुभव और ज्ञान अर्जित करना। मनुष्य ऐसा क्यों करता है और ऐसा करने से उसे क्या मिलता है यह भी सन्दर्भ में विचारणीय है। मनुष्य अनुभव और ज्ञान इसलिए अर्जित करता है कि उसे अपने आगामी व्यवहारों को करने में सरलता होती है। अपने व्यवहार में कुशल और दक्ष भी हो जाता है। ऐसी दशा में अधिगम मनुष्य की प्रयोजनपूर्ण एवं उपयोगी क्रिया है जिसमें उसका शरीर एवं मन दोनों लगा हुआ पाया जाता है। एतदर्थ इसे प्रयोगपूर्ण एवं उपयोगी मनोशारीरिक क्रिया भी कहते हैं। यह अधिगम का अर्थ है। अंग्रेजी शब्द ‘Learning’ का अर्थ होता है कि किसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, जानने में सहायता लेना, निष्पादन की शक्ति प्राप्त करना। सीखना मनुष्य की सक्रिय एवं निष्क्रिय रूप में ज्ञान अर्जित करने की क्रिया है जिसके फलस्वरूप कार्यों का सफलतापूर्वक एवं कुशलतापूर्वक निष्पादन होता है। इससे हमें यह भी संकेत मिलता है कि Learning एक मनोशारीरिक क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है क्योंकि कार्य-निष्पादन में मन और शरीर दोनों निहित हैं।
अधिगम की परिभाषा —
नीचे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया विचार अधिगम के सम्बन्ध में प्रकट किया जा रहा है। इससे हमें उसके अर्थ का अच्छी तरह बोध होता है-
प्रो० गिलफोर्ड : “अधिगम व्यवहार के परिणामस्वरूप होनेवाला व्यवहार में परिवर्तन है।” प्रो० पारीक : “अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के कारण नये प्रकार के सपरिवर्तन को अर्जित करता है जो किसी सीमा तक प्राणी के सामान्य व्यवहार के प्रतिदर्श को स्थायी एवं प्रभावित करता है।”
प्रो० बर्नहार्ट : ” अधिगम किसी उद्देश्य की प्राप्ति अथवा किसी समस्या के समाधान के प्रयास में अभ्यास के कारण एक निश्चित परिस्थिति में व्यक्ति के कार्यों में एक स्थायी संपरिवर्तन के रूप में परिभाषित होता है।”
प्रो० क्रो और क्रो : “ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन अधिगम है।
प्रो० गुथरी : “अधिगम की योग्यता किसी परिस्थिति में बीते हुए अनुभव के कारण परिस्थिति के अनुसार भिन्न तौर पर अनुक्रिया करना है।”
अधिगम के नियम —
प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई नियम अवश्य कार्य करता है। नियमों का निर्माण कार्य के अनुभवों के आधार पर होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अन्तर्गत सीखने के नियमों का विशेष महत्त्व है डगलस और हालैण्ड के कथनानुसार, “सीखना निश्चित नियमों के साथ चलता है।” प्रत्येक बालक का सीखना नियमों के अनुसार पर आधारित होता है और शिक्षक स्वयं अपने शिक्षण में सीखने के नियमों का ध्यान रखता है। ये नियम मनोवैज्ञानिकों द्वारा पशुओं और बच्चों पर किये गये प्रयोगों के आधार पर निश्चित किये गये हैं।
अपने सम्बद्धवाद से सम्बन्धित प्रयोगों के आधार पर थार्नडाइक ने अधिगम के नियमों का उल्लेख किया है। इन्हें थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के नियम कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया इन्हीं नियमों के अनुसार पर आधारित होती है और शिक्षक स्वयं अपने शिक्षण में सीखने के नियमों का ध्यान रखता है। ये नियम मनोवैज्ञानिकों द्वारा पशुओं और बच्चों पर किये गये प्रयोगों के आधार पर निश्चित किये गये हैं।
अपने सम्बद्धवाद से सम्बन्धित प्रयोगों के आधार पर थार्नडाइक ने अधिगम के नियमों का उल्लेख किया है। इन्हें थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के नियम कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया इन्हीं नियमों के आधार चलती है। थार्नडाइक के सभी नियमों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है-
(1) अधिगम के मुख्य नियम तथा
(2) अधिगम के गौण नियम
अधिगम के मुख्य नियम —
1. अभ्यास का नियम –
इस नियम के अनुसार पशु और मनुष्य बार-बार के अभ्यास द्वारा सीखते हैं, किसी उद्दीपन के कारण अनुक्रियाएँ करता है और अनुक्रिया की पुनरावृत्ति अथवा अभ्यास के द्वारा उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सम्बन्ध दृढ़ हो जाता है। अभ्यास के द्वारा सीखी गयी अनुक्रिया दीर्घ काल तक स्थायी बनी रहती है, क्योंकि बार-बार के अभ्यास के कारण शरीर की मांसपेशियाँ तथा स्नायुतन्तु भी उस क्रिया को करने को अभ्यस्त हो जाते हैं। छोटा बच्चा अभ्यास के द्वारा ही खड़ा होना, चलना और दौड़ना सीखता है। इसी प्रकार विद्यालय में बालक अनेक क्रियाओं में निपुणता अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त करता है। इस नियम के दो उपनियम भी हैं-
(i) उपयोग का नियम —
थार्नडाइक के अनुसार, “उपयोग के नियम के अनुसार जब किसी परिस्थिति तथा अनुक्रिया के बीच सम्बन्ध स्थापित होता है तब अन्य बातों के समान रहने पर पुनरावृत्ति के कारण यह सम्बन्ध स्थापित होता है, तब अन्य बातों के समान रहने पर पुनरावृत्ति के कारण यह सम्बन्ध दृढ़ हो जाता है।”
(ii) अनुपयोग का नियम
इस नियम के अनुसार किसी परिस्थिति या उद्दीपन और अनुक्रिया में सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर एक अवधि तक उसका अभ्यास न करने के कारण उद्दीपन और अनुक्रिया का सम्बन्ध क्षीण हो जाता है। यदि किसी चीज को भुलाना हो तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
2. प्रभाव का नियम – जिन अधिगम अनुक्रियाओं को करने से संतोष, सुख या पुरस्कार प्राप्त होता है, हम उस कार्य को करना चाहते हैं। इस स्थिति में उद्दीपन और अनुक्रिया का सम्बन्ध दृढ़ होता है। यही प्रभाव का नियम है। इसके विपरीत जिंन अनुक्रियाओं को करने से हमें असन्तोष, दुःख या दण्ड प्राप्त होता है, उन्हें हम नहीं करना चाहते। इस स्थिति में उद्दीपन अनुक्रिया का सम्बन्ध क्षीण होता है
3. तत्परता का नियम सीखना उस समय अधिक अच्छी तरह होता है जब कोई क्रिया सीखने के लिए हम तत्पर या तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में समस्त प्राणी उस समय अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से अधिगम करते हैं जब वे अच्छी भावावस्था में होते हैं। विद्यालय में बालक की इच्छा या अनिच्छा का प्रभाव उसके सीखने पर अवश्य पड़ता है। वह जिस विषय या कार्य में तत्परतापूर्वक रत होता है, उसे कुशलता के साथ पूरा भी करता है। शिक्षक का यह दायित्व है कि वह कक्षा में कोई भी क्रिया सीखने से पूर्व यह अवश्य देख ले कि बालक उस क्रिया को सीखने के लिए तत्पर है या नहीं। यदि बालक कविता याद करने के लिए या मानचित्र बनाने के लिए तत्पर नहीं है या अनिच्छुक है तो उनके साथ सीखने के शेष प्रयत्न व्यर्थ ही होंगे। तत्परता में जिन निश्चित अंगों का प्रयोग किया जाता है, उनकी शारीरिक परिपक्वता भी सम्मिलित है। अभ्यास तथा प्रभाव के नियम का तत्परता के नियम से घनिष्ठ सम्बन्ध है ।
4. प्रसंगाधीनता का नियम – थार्नडाइक ने प्रभाव के नियम में सुधार करते हुए बताया कि जिस प्रकार हम सुखप्रद या संतोषजनक अनुभवों को याद रखते हैं उसी प्रकार कष्टप्रद अनुभवों को भी। उसने बताया कि कोई बात अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे सन्दर्भ या प्रसंग में याद आती है। यही प्रसंगाधीनता का नियम है। जिस प्रकार किसी क्रिया को पूरा करने वाली अनुक्रिया से हमारा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, उसी प्रकार उस क्रिया की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करनेवाली अनुक्रिया से भी सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।
अधिगम के गौण नियम —
सीखने के गौण नियमों का विवेचन थार्नडाइक ने एक ही स्थान पर क्रमबद्ध रूप से नहीं किया गौण नियमों का मुख्य नियमों से सम्बन्ध भी स्पष्ट नहीं है फिर भी ये नियम एक सीमा तक उपयोगी अवश्य हैं
1. बहुअनुक्रिया का नियम –
इस नियम के अनुसार जब हमारे सामने कोई समस्या उपस्थित होती है तब उसको हल करने के लिए हम कई प्रकार की अनुक्रियाएँ करते हैं। ऐसा करते समय हमें यह भी पता नहीं होता कि किस अनुक्रिया के द्वारा समस्या हल होगी। इन्हीं अनुक्रियाओं में से किसी उपयुक्त अनुक्रिया के द्वारा हमें अपने कार्य में सफलता मिल जाती है अर्थात् समस्या का हल निकल आता है। समस्या के हल के लिए प्राणी द्वारा अनेक प्रकार की अनुक्रिया करने के कारण इसे बहुअनुक्रिया का नियम कहते हैं। इनके मूल में प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत कार्य करता है।
2. मनोवृत्ति का नियम-
बालक को सिखाने में उसकी मनोवृत्ति का विशेष हाथ होता है।
जिस कार्य को करने में बालक की अभिवृत्ति नहीं होती है उसे या तो वह नहीं करता या ठीक प्रकार से नहीं करता। जो बालक गणित से दूर भागता है उसकी मनोवृत्ति गणित सीखने में नहीं हो सकती है। कक्षा में कोई भी ज्ञान देने से पूर्व बालक की मानसिक सजगता और रुचि का ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है।
3. आंशिक क्रिया का नियम-
इस नियम के अनुसार किसी समस्या में उपस्थित होने पर प्राणी आंशिक क्रियाओं को ही करके समस्या का हल ढूंढ़ लेता है। इसे ही आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। समस्या को हल करने के लिए प्राणी कई प्रकार की अनुक्रियायें करता है। परन्तु जिसमें सूझ या अन्तर्दृष्टि होती है वह जल्दी ही मुख्य अनुक्रिया को चुनकर समस्या को हल कर लेता है। इस प्रकार समय और श्रम की बचत भी होती है। कार्य को छोटी-छोटी इकाइयों या अंशों में बाँटकर करने से कार्य जल्दी समाप्त होता है। कक्षा में शिक्षक अपने पाठ को छात्रों के सम्मुख इकाइयों या अंशों में ही प्रस्तुत करता है। इस नियम पर खण्ड से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है।
4. आत्मसात का नियम –
नया ज्ञान प्राप्त करते समय हम उससे सम्बन्धित पूर्व अनुभवों का स्मरण करते हैं। पूर्व अनुभवों के आधार पर नये ज्ञान को सरलतापूर्वक आत्मसात करने में सुविधा होती है। इस प्रकार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। जब तक नवीन ज्ञान के लिए पूर्वज्ञान की पृष्ठभूमि नहीं होती तब तक नवीन ज्ञान को आत्मसात करना कठिन होता है। कक्षा में अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक नये पाठ को पढ़ने से पूर्व या नयी क्रिया को सिखाने से पूर्व बालकों के पूर्वार्जित अनुभवों की जानकारी प्राप्त कर ले।
5.साहचर्य परिवर्तन का नियम-
इस नियम के अनुसार प्राणी एक बार की गयी अनुक्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार की अनुक्रिया करने लगता है। वास्तव में अनुबन्धित अनुक्रिया को ही थार्नडाइक ने साहचर्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया है भोजन देखकर कुत्ते के मुँह से लार टपकती है। कुछ दिनों बाद बर्तन में उसे भोजन दिया जाता है, उसे भी देखकर लार टपकने लगती है।
शैक्षिक महत्त्व —
सीखने के मुख्य नियमों के समान ही गौण नियमों की उपयोगिता भी अधिक है। प्रायः देखने में आता है कि समस्या के हल के लिए कई प्रकार की अनुक्रियाएँ करनी पड़ती हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह समस्याओं के हल के लिए छात्रों को कई प्रकार की अनुक्रियाओं को करने का अवसर दे। सीखने में मनोवृत्ति का विशेष महत्त्व है। बालक उसी विषय या क्रिया को सीखना चाहता है जिसमें उसकी अभिवृत्तियों का झुकाव होता है। विषय के प्रति बालक की अभिवृत्ति का ज्ञान अध्यापक के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार पढ़ने के पूर्व नवीन ज्ञान की भित्ति खड़ी होती है। यह भी देखने में। आता है कि समस्या उपस्थित होने पर प्राणी सूझ के द्वारा केवल मुख्य अनुक्रियाओं को ही करता है। तथा साहचर्य परिवर्तन के द्वारा स्वाभाविक अनुक्रिया को वांछित अनुक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित करता है।। के नियमों का महत्त्व बताते हुए कहा है, “यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों या सिद्धान्तों का
इस प्रकार अधिगम में इसके नियम का महत्त्वपूर्ण स्थान है। डब्ल्यू0 एम0 रायबर्न ने अधिगम | अनुसरण किया गया है तो अधिगम अधिक संतोषजनक होगा।”
वास्तव में, सफल अधिगम की सभी आवश्यक विधियों की मुख्य बातों को थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य तथा गौण नियमों के भीतर सम्मिलित कर लिया है।
प्रश्न 4 (iii) पॉवलाव के सम्बन्ध अनुक्रिया सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं? इसकी शैक्षिक उपयोगिता का विवेचन कीजिए।
अथवा
पॉवलाव के अधिगम सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। पॉवलाव के सिद्धान्त | की शैक्षिक उपयोगिता की विवेचना कीजिए।
अथवा
अधिगम के पॉवलाव के सिद्धान्त का विस्तृत वर्णन कीजिए। यह सिद्धान्त थार्नडाइक के सिद्धान्त से किस प्रकार भिन्न है? वर्णन कीजिए।
अथवा
अधिगम की पॉवलाव की शास्त्रीय अनुबन्धन सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
ANSWER-
पॉवलाव का सम्बन्ध अनुक्रिया सिद्धान्त —
सम्बन्ध अनुक्रिया का अर्थ है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। उदाहरणार्थ, एक बालक अपने वास्तविक बाजार के रास्ते से स्कूल जा रहा है। रास्ते में हलवाई की दूकान पड़ती है दूकान
है पर सजी हुई रंग-बिरंगी मिठाइयों को देखकर बच्चे के मुँह में लार टपकने लगती है तथा धीरे-धीरे यह एक स्वाभाविक क्रिया बन जाती है अतः स्पष्ट है कि जब अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति अस्वाभाविक क्रिया होती है और बाद में बार-बार दोहराने पर जो स्वाभाविक उत्तेजक भी वही अनुक्रिया पैदा करने लगता है जो अस्वाभाविक उत्तेजक करता था तो वह अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धान्त कहलाता है।
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 1904 में रूसी शरीर शास्त्री पॉवलाव ने किया था उनके अनुसार सीखने की क्रिया अनुक्रिया से प्रभावित होती है।
एच. डब्ल्यू. बर्नार्ड ने सिद्धान्त की परिभाषा इस प्रकार दी है-
“अनुकूलित अनुक्रिया उत्तेजना की पुनरावृत्ति द्वारा व्यवहार का संचालन है जिसमें उत्तेजना पहले किसी अनुक्रिया के साथ होती है, किन्तु अन्त में वह स्वयं उत्तेजना बन जाती है।”
लेस्टर एन्डरसन के अनुसार, “उद्दीपन अनुक्रिया प्राणी की मूल प्रकृति का एक भाग है यानी सीखना है। जब मूल Stimulus के साथ एक नया Stimulus दिया जाता है और कुछ समय बाद जब मूल उद्दीपक को हटा लिया जाता है तब यह देखा जाता है कि नये उद्दीपक में भी वही अनुक्रिया होती है जो मूल उद्दीपन से होती थी। इस प्रकार अनुक्रिया उद्दीपन के साथ अनुकूलित हो जाती है।”
पॉवलाव द्वारा परीक्षण–
पॉवलाव ने इस क्रिया को जानने के लिए एक पालतू कुत्ते पर यह प्रयोग किया। इस कुत्ते की लार ग्रन्थि का ऑपरेशन किया गया जिससे लार एकत्रित की जा सके। लार काँच की नली के द्वारा एकत्र किया गया। प्रयोग का आरम्भ इस प्रकार किया गया-कुत्ते को खाना देते समय घण्टी बजाई जाती थी तथा खाना देखकर कुत्ते के मुँह में लार आना स्वाभाविक था। घण्टी बजती है परन्तु खाना नहीं दिया जाता है परन्तु कुत्ते के मुँह से लार टपकती है । इस प्रकार घण्टी के साथ अनुकूलित क्रिया होने लगती हैं। इस प्रकार एक साथ जो उत्तेजनाएँ दी जाती थीं, घण्टी का बजना तथा भोजन का दिया जाना साथ-साथ चलता रहा और काफी समय जब भोजन नहीं दिया गया केवल घण्टी बजी। परिणामतः अनुक्रिया वही हुआ जो भोजन के लिए दिये जाने साथ होता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब दो उत्तेजनाएँ साथ दी जाती हैं पहले नई तथा बाद में मौलिक, उस समय पहली क्रिया भी effective हो जाती है।
Conditioned Response इस आधार पर विकसित होती है-
(1) US -> UR (अस्वाभाविक क्रिया तथा अनुक्रिया)
भोजन (भार) (Unconditioned stimulus and Response)
(2) CU+ US→ UR (Condition Stimulus and Response)
घण्टी की आवाज + भोजन लार (Unconditions and stimulus Response)
(3) CS → CR Condition stimulus and
घण्टी की आवाज – Condition Response
पर लार
इस प्रकार स्पष्ट है कि जब किसी क्रिया को बार-बार दोहराया जाता है तो Condition Stimulus भी वही Response करने लगता है जो Uncondition Stimulus करता था इसमें भोजन (US) बदलकर ।
घण्टी के साथ भी कुत्ता वही Response करने लगता है जो कि वह भोजन दिखाने पर करता है।
सम्बन्ध अनुक्रिया सिद्धान्त के नियन्त्रक तत्व —
अब हमें यह देखना है कि (Conditioned Response) किस प्रकार प्रभावित होती है, वह कौन- कौन से तथ्य हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं-
(1) अनुक्रिया का प्रभुत्व-अर्थात् अनुकूलित अनुक्रिया में प्रक्रिया का प्रभुत्व रहता है। जैसे घण्टी के बजते ही कुत्ते का ध्यान आवाज की ओर केन्द्रित हो जाता है।
(2) उद्दीपकों में समय का सम्बन्ध-अन्य बातें समान रहने पर दो उद्दीपकों में भी समय का सम्बन्ध होना चाहिए जैसे भोजन तथा घण्टी का साथ-साथ बजना ।
(3) उद्दीपन की पुनः आवृत्ति-क्रिया के बार-बार करने पर वह स्वभाव में आ जाती है जैसे वाटसन के प्रयोग में रोएँदार बीजों से बालक डरता पाया गया।
(4) भावनात्मक पुनर्बलन-प्रेरक जितने अधिक शक्तिशाली होंगे अनुक्रिया उतनी अधिक होगी इसके अलावा अन्य तथ्य हैं जो प्रभाव डालते हैं-
(1) अभ्यास-अनुकूलित प्रक्रिया को जितना अधिक दोहराया जायेगा उतनी ही अनुकूलित प्रक्रिया अधिक दृढ़ होगी।
(2) समय-समय का भी प्रभाव पड़ता है कि मूल उत्तेजना तथा सम्बन्धित उत्तेजना में कितना समय दिया गया है।
(3) बाहरी बाधाएँ।
(4) प्रेरक ।
(5) बुद्धि।
(6) आयु।
(7) मानसिक स्वास्थ्य-यदि मानसिक रूप से स्वस्थ है जो उसमें Condition Response अधिक शीघ्र होगा।
प्रानुकूलित अनुक्रिया- इसमें अनुक्रिया का सम्बन्ध अन्य क्रिया से बढ़ा दिया जाता है Deconditioning कहलाती है। इसमें Unconditioning Stimulus की संख्या बढ़ जाती है। इसे नीचे स्पष्ट किया गया है-
(1) S1 → R1
भोजन लार टपकना
(2) S1 + S2 → R1
Conditioning
S2 → R2
घण्टी की आवाज
(3) S2 + S3 → R1
Deconditioning
बिजली की रोशनी
इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अस्वाभाविक उत्तेजना की संख्या बढ़ती गई और उसका प्रभाव भी बढ़ता गया।
शैक्षिक उपयोगिता
अनुकूलित अनुक्रिया का आधार व्यवहार है। वाटसन ने Conditioned के आधार पर ही यह मुझे कोई भी बालक दे दो मैं उसे जो चाहूँ बना सकता हूँ।” वह व्यक्ति के विकास में अनुकूलित देता ही है। विद्यालय में इस मत का उपयोग सरलता से किया जा सकता है।
(1) स्वभाव निर्माण-अनुकूलित प्रक्रिया धीरे-धीरे स्वभाव बन जाती है। स्वभाव का मानव जीवन से विशेष महत्त्व है। इससे समय की बचत होती है तथा कार्य में स्पष्टता होती है। बार- द्वार किया गया कार्य आदत बन जाता है। विद्यालय, परिवार तथा समाज में सिद्धान्त के आधार पर अनुशासन किया जा सकता है। विद्यालयों में अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
(2) अभिवृत्ति का विकास-इस सिद्धान्त के द्वारा बालकों में अच्छी अभिवृत्ति विकसित हो सकती है। बच्चों के समक्ष आदर्श उपस्थित कर उन्हें अनुकूलन प्रक्रिया ग्रहण करने की अनुप्रेरणा दे सकते हैं तथा अच्छी अभिवृत्ति के साथ अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सिद्धान्त का जितना प्रभाव अच्छी अभिवृत्ति विकसित करने पर पड़ता है उतना ही इसका प्रभाव विपरीत पड़ता है यदि किसी कार्य को ठीक प्रकार से ग्रहण न किया गया है। जैसे-एक कक्षा उदाहरण
यह बात स्पष्ट है-
मान लिया कोई विद्यार्थी किसी विषय में अरुचि रखता है तो वह अरुचि तथा घृणा उस विषय के पढ़ाने वाले अध्यापक से भी जुड़ जायेगी। अब यदि वह विद्यार्थी इस विषय को छोड़कर दूसरा विषय से लेता है, जिसको वह अच्छी प्रकार समझता है। परन्तु कुछ दिन बाद विषय को पढ़ाने के लिए वही पहले वाला अध्यापक आ जाता है तो उस अध्यापक के प्रति घृणा का सम्बन्ध उस दूसरे विषय से भी बुड़ जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि विषय को पढ़ाने से पहले अध्यापक को विद्यार्थी की रुचि का ध्यान रखना चाहिए जिससे वह उस विषय में अनुकूलित हो जाता है।
(3) अक्षर विन्यास तथा गुण शिक्षण-उस सिद्धान्त के अनुसार बच्चों में अक्षर विन्यास तथा पूण का विकास किया जा सकता है क्योंकि इस सिद्धान्त में अभ्यास पर अधिक बल देना आवश्यक है।
(4) मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार-यह सिद्धान्त उन बच्चों के लिए उपचार प्रस्तुत करता है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तथा संवेगात्मक रूप में अस्थिर होते हैं।
(5) अध्यापक का योग-उस सिद्धान्त के अनुसार अध्यापक का योग वातावरण का निर्माण करने में अधिक रहता है। अध्यापक को चाहिये कि वह बालकों को दण्ड व पुरस्कार का निर्णय तुरन्त करे इससे, अनुकूलित प्रक्रिया का सम्पादन शीघ्र होगा।
प्रश्न 5 (i) शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएँ कौन-सी हैं? शिक्षण की अन्तर्क्रियात्मक अवस्था का विस्तार से वर्णन करें।
ANSWER-
शिक्षण की प्रकृति को समझने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि शिक्षण क्या है? शिक्षण की अवधारणा में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं जो दूसरों को शिक्षा देने के लिए अपनाये जाते है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उत्तम ज्ञान देने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि विद्यार्थी प्रकरण को समझ सकें। अध्यापक का कर्त्तव्य है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षण का अर्थ है-अध्यापक और विद्यार्थी के नव्य चलने वाली अन्तर्क्रिया ।
शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों का पारस्परिक लाभ सन्निहित होता है। दोनों के अपने-अपने उद्देश्य होते हैं और शिक्षण के माध्यम से दोनों अपने-अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।
विश्व के महान अध्यापकों ने शिक्षण को अपनी-अपनी तरह से परिभाषित किया है। उनकी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षण में तीन मुख्य आयाम होते हैं-
प्रथम : अध्यापक
द्वितीय: विद्यार्थी
तृतीय : शिक्षा
व्यापक स्वरूप में शिक्षण वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के लिए अधिगम को आसान बनाती है।
शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएँ –
शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं-
1. शिक्षण ज्ञान, कौशल और गुणधर्म का विशिष्ट अनुप्रयोग है, जिससे वैयक्तिक और सामाजिक, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है।
2. शिक्षण की मुख्य विशेषता निर्देशन और परामर्श प्रदान करना है। /
3. अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अन्तर्क्रिया शिक्षण कहलाती है।
4. शिक्षण प्रभावकारी ढंग से विद्यार्थियों को ज्ञान देने की एक कला है।
5. शिक्षण एक विज्ञान है जो विभिन्न विषयों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों के कारण और वास्तविकताओं का ज्ञान होता है।
6. शिक्षण विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों का बोध कराता है।
7. शिक्षण निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।
8. यदि अध्यापक को अपने विषय का अच्छा ज्ञान होता है तो वह अच्छा शिक्षण कर सकता है। 9. शिक्षण बच्चों को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
10. शिक्षण का स्वरूप औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है।
11. शिक्षण में विद्यार्थियों को सूचना सम्प्रेषित की जाती है।
12. शिक्षण वह उपकरण है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने वातावरण और समाज के साथ समायोजन स्थापित करता है।
शिक्षण अधिगम में शिक्षकों की भूमिका-
विद्यालयों में शिक्षण शिक्षक-केन्द्रित है जहाँ शिक्षक ज्ञान का प्रसार करने वाले तथा छात्र उसे ग्रहण करने वाले होते हैं। छात्रों से यह अपेक्षा रहती है कि वे शिक्षकों अथवा पाठ्य पुस्तकों द्वारा दिये गये ज्ञान को स्मरण रखें तथा उसे परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करें। शैक्षणिक सत्र की समाप्ति के बाद छात्रों की उपलब्धि को उनके द्वारा परीक्षा में प्राप्त ग्रेड/अंकों के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है। बहुत से विद्यालयों में शिक्षण अधिगम का एक परिणाम यह भी देखने में आया है कि बच्चे प्रश्नों और उत्तरों को याद रखने के लिए, यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालयों में भी, गाइड पुस्तकों का सहारा लेते हैं। जानकारी का स्मरण अथवा याद करने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि छात्र ने उसे समझ लिया है तथा जीवन की विभिन्न स्थितियों में वह उसका प्रयोग कर सकेगा। सार्थक ज्ञान वही है, जब विद्यार्थी अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करे।
● विद्यार्थी अच्छी तरह तभी सीख पायेंगे जब-
• वे अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें।
• अधिगम उनके जीवन के दैनिक अनुभवों से सम्बद्ध हो।
• छात्र शिक्षक तथा छात्र-छात्र के बीच अन्तःसम्बन्धों को प्रोत्साहित किया जाये।
• शिक्षक की भूमिका ज्ञान के प्रसारक के बजाय बच्चों को ज्ञान सृजन कराने वाले उत्प्रेरक के रूप में बदल गयी है।
• विद्यार्थियों को अधिगम की विविध स्थितियाँ उपलब्ध करायें।
• यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा अधिगम प्रक्रिया में संलिप्त है।
• विद्यार्थियों को सहभागिता तथा एक-दूसरे से सीखने, वाद-विवाद के लिए प्रोत्साहित करें।
• जब विद्यार्थी चाहे तभी सहायता करें।
इस प्रकार सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्यापकों को एक चिन्तनशील व्यवहारकर्त्ता बनाने कों को इन बातों का प्रशिक्षण दिया जाय दिया जाना चाहिए।
* छात्रों के सन्दर्भ और आवश्यकताओं के अनुरूप अध्ययन परिवेश विकसित करना, अभिकल्पित करना तथा चयन करना।
* अधिगम तथा मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रबन्धकीय निर्णय लेना।
* सहयोगी अधिगम की व्यवस्था करना।
* छात्रों के अध्ययन कार्यों का आकलन।
शिक्षकों की भूमिका को बजाय ज्ञान के प्रसारक के, सूचना तथा ज्ञान सृजन को सुगम बनाने वाले रूप में स्थापित किये जाने की जरूरत है। शिक्षक उस तरह के शिक्षण अधिगम का सृजन करे जो दीखने के प्रजातान्त्रिक माहौल में आलोचनात्मक चिन्तन के विकास को सुगम बनाये, जहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र, समुदाय तथा वर्ग के भेदभाव किये बिना सभी बच्चे भाग ले सकें। अध्यापक छात्रों को ऐसे यार करें जिससे वे ज्ञान के विभिन्न स्रोतों को समन्वित कर सकें, जैसे- बच्चों के जीवन के अनुभव, ठ्य-पुस्तकों से अलग हटकर स्थानीय जानकारी आदि।
● शिक्षकों के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं-
• वे बच्चों का ख्याल कर सकें तथा उनके साथ रहना पसन्द करें।
• बच्चों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सन्दर्भों में समझ सकें।
• ग्रहणशील तथा निरन्तर सीखने वाले हों।
• शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों की सार्थकता की खोज के रूप में देखें तथा ज्ञान निर्माण मननशील अधिगम की लगातार उभरती प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें। ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों में नेहित बाह्य वास्तविकता के रूप में न देखकर उसके निर्माण को शिक्षण अधिगम के साझा सन्दर्भों और व्यक्तिगत अनुभवों के रूप में देखें। समाज के प्रति अपना दायित्व समझें और एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए कार्य करें।
• आत्ममूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, शिक्षकों की प्रतिपुष्टि और वर्ष के अन्त में औपचारिक मूल्यांकन जैसे कई प्रशिक्षण मूल्यांकन होते हैं। सभी मूल्यांकनों का उद्देश्य सम्बन्धित कार्यक्रमों में सुधार, शक्तियों और कमियों को समझना है।
● सीखने की स्थिति में बालक की भूमिका –
सीखने ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। छात्र सक्रिय रूप से अपने क्रियाकलापों / प्रदान की ई सामग्री के आधार पर नये विचारों को वर्तमान विचारों से जोड़कर अपने ज्ञान की रचना करते हैं। उदाहरण के लिए किसी घटना अथवा वस्तु के लिए पाठ, चित्र अथवा दृश्य सामग्री का उपयोग करने साथ सामूहिक चर्चा अथवा अन्तःक्रिया करना । उपयुक्त गतिविधियाँ छात्रों में विचारों की रचना एवं रचना में मदद करती हैं। सहयोगी अधिगम अर्थ सम्बन्धी विभिन्न विचारों के आदान-प्रदान व प्रतचीत के अवसर प्रदान करता है, जैसे-जैसे छात्र सीखता है वह व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से किसी वस्तु अथवा किसी घटना से सम्बन्धित अर्थ का निर्माण करता है। अर्थ निर्माण ही सीखना है। रक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिए जिनसे वे स्कूल में सिखाई जाने वाली वेजों का सम्बन्ध बाहरी दुनिया से जोड़ सकें, बच्चों को अपने शब्दों में जवाब देने और अपने अनुभव आधार पर उत्तर देने को प्रोत्साहित करना चाहिए। ‘चतुर अनुमान’ को एक कारगर शिक्षाशास्त्रीय उपन के रूप में प्रोत्साहित किये जाने की जरूरत है। शिक्षक द्वारा ऐसे अवसर प्रदान किये जाने हिए ताकि बच्चे प्रश्न पूछकर, पर्यवेक्षण करके, वाद-विवाद, खोज एवं चिन्तन कर अवधारणाओं को आत्मसात् करें या नये विचारों का सृजन करें।
● बच्चे विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। ये निम्न प्रकार हैं-
* बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं- अनुभव के माध्यम से, चीजें स्वयं करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने, विमर्श करने, पूछने, सुनने, सोचने व मनन करने से तथा भाषण गतिविधि या लेखन के माध्यम से एवं स्वयं को अभिव्यक्त करने से। बच्चों को विकास के मार्ग में इन सभी तरह के अवसर मिलने चाहिए।
* सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है।
* स्कूल के भीतर व बाहर, दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। इन दोनों जगहों में यदि सम्बन्ध रहे तो सीखने की प्रक्रिया मजबूत होती है।
* अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य, अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।
* बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों, उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना सीखने को कमजोर करना है। बच्चे बहुत से तथ्य याद तो रख सकते हैं, लेकिन सम्भव है कि वे न तो उन्हें समझ पायें, न ही उन्हें अपने आस-पास की दुनिया से जोड़ पायें।
* सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को रटकर और परीक्षा के बाद सीखे हुए को भूल न जायें बल्कि उसे समझ सकें और आत्मसात् कर सकें। साथ ही सीखने में विविधता व चुनौतियाँ होनी चाहिए ताकि वह बच्चों को रोचक लगे और उन्हें व्यस्त रख सकें। केवल दोहराव से ऊब पैदा होती है।
सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है आस पास का वातावरण, प्रकृति, चीजों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अन्तःक्रिया करना ।
सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की व दुबारा सीखने की तत्परता नई स्थितियों का सामना करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा तथा प्रशिक्षण में यह आवश्यक है कि ज्ञान सृजन की प्रक्रिया पर जोर दिया जाये।
स्कूलों में शिक्षण अधिगम सुन्दर, सुखद वातावरण में होना चाहिए। यदि बच्चे ऐसे वातावरण के निर्माण में सक्रिय भाग लें तो इसका महत्त्व और भी बढ़ जाता है।
अधिगम उस सामाजिक वातावरण/सन्दर्भ से बेहद प्रभावित होता है जहाँ से शिक्षक तथा छात्र आते हैं। स्कूल तथा कक्षा का सामाजिक परिवेश सीखने की प्रक्रिया, यहाँ तक कि पूरी शिक्षा प्रक्रिया पर असर डालता है।
प्रश्न 5 (ii) अधिगम के स्थानान्तरण से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए । एक अध्यापक के लिए उसकी क्या उपयोगिता है?
अथवा
अधिगम स्थानान्तरण क्या है? विभिन्न प्रकार के स्थानान्तरण तथा अधिगम स्थानान्तरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
अथवा
अधिगम के हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं? हस्तांतरण के विभिन्न प्रकारों एवं इनके शैक्षिक निहितार्थो की व्याख्या कीजिए।
ANSWER-
अधिगम के स्थानान्तरण का अर्थ-सभी शिक्षण और प्रशिक्षण की मुख्य कसौटी क्या है? उत्तर सीधा है कि जो कुछ लड़के ने पढ़ा-पढ़ाया है उसे काम में लाने की योग्यता उसमें अवश्य होनी चाहिए। मनोविज्ञान में इस कसौटी को ‘अधिगम का स्थानान्तरण’ कहा गया है। अधिगम के स्थानान्तरण का तात्पर्य विद्यालय में सीखे हुए ज्ञान, कौशल, क्रिया को सरलतापूर्वक जीवन की व्यावहारिक परिस्थितियों में प्रयोग करना है।
अधिगम स्थानान्तरण की परिभाषा – विभिन्न मनोविज्ञानियों ने इसकी परिभाषा दी है जिन्हें हम यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं-
प्रो० क्रो और क्रो- “जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य की आदत, ज्ञान या कौशलों का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह प्रशिक्षण (अधिगम) अन्तरण कहकर संकेत किया जाता है।”
प्रो० डब्ल्यू० बी० कोल्सनिक- “पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशलों, आदतों, अभिवृत्तियों अथवा अन्य अनुक्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना स्थानान्तरण है।”
प्रो० एच० सोरेन्सन- “अधिगम-अन्तरण के द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है जहाँ तक एक परिस्थिति में अर्जित योग्यताएँ दूसरी परिस्थिति में सहायता करती हैं। ”
सीखने के स्थानान्तरण के रूप
सीखने के स्थानान्तरण के निम्नलिखित रूप होते हैं-
1. धनात्मक स्थानान्तरण-जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल किंसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायक होता है तो इसे धनात्मक स्थानान्तरण कहते हैं; जैसे – गणित के ज्ञान का भौतिकशास्त्र की संख्यात्मक समस्याओं के हल करने में सहायक होना और कार चलाने के कौशल का जीप अथवा ट्रक चलाने के कौशल सीखने में सहायक होना। शिक्षा र के क्षेत्र में इस धनात्मक स्थानान्तरण का ही महत्त्व होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम सीखने के स्थानान्तरण की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य इसी धनात्मक स्थानान्तरण से होता है।
2. ऋणात्मक स्थानान्तरण-जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में बाधक होता है तो इसे ऋणात्मक स्थानान्तरण कहते हैं; जैसे – विज्ञान के ज्ञान और उसमें निहित कारण-कार्य सम्बन्ध का धर्म एवं दर्शन के अध्ययन में बाधक होना। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के स्थानान्तरण का कोई महत्त्व नहीं होता इसलिए इस पर कोई विचार नहीं किया जाता।
3. शून्य स्थानान्तरण-जब सीखने का स्थानान्तरण न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है तो उसे शून्य स्थानान्तरण कहते हैं
4. क्षैतिज स्थानान्तरण-जब किसी एक ही स्तर की कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल उसी कक्षा के किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने सहायक होता है तो इसे क्षैतिज स्थानान्तरण कहते हैं; जैसे – कक्षा 10 में सीखे हुए गणित के ज्ञान एवं कौशल का उसी कक्षा के विज्ञान की संख्यात्मक समस्याओं के हल करने में सहायक होना।
5. लम्बीय स्थानान्तरण- जब किसी पूर्व कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा वैशल उससे आगे की कक्षा में किसी क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायक ता है तो इसे लम्बीय स्थानान्तरण कहते हैं, जैसे- कक्षा 10 में सीखे जाने वाल गणित के ज्ञान एवं शल का कक्षा 11 में सीखे जाने वाले गणित के ज्ञान एवं कौशल के सीखने में सहायक होना।
6. एक पक्षीय स्थानान्तरण- जब शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल सी अंग द्वारा किसी दूसरे कौशल को सीखने में सहायक होता है तो इसे एक पक्षीय स्थानान्तरण कहते जैसे – बायें हाथ से कपड़ा सीने के कौशल का बायें हाथ से लिखना सीखने में सहायक होना।
7. द्विपक्षीय स्थानान्तरण-जब शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल शरीर दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल के या अन्य किसी कौशल को सीखने में सहायक होता है तो इसे द्विपक्षीय
स्थानान्तरण कहते हैं; जैसे दायें हाथ से लिखने के कौशल का बायें हाथ से लिखना अथवा तलवार चलाना सीखने में सहायक होता है।
सीखने के स्थानान्तरण का महत्त्व और शिक्षकों की भूमिका
शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के स्थानान्तरण का बड़ा महत्त्व है, उसकी बड़ी उपयोगिता है। अब इस तथ्य को सामने रखकर ही शिक्षा के किसी स्तर की शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं और इसी आधार पर उसकी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है और साथ ही ऐसी शिक्षण-अधिगम विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें पूर्व ज्ञान एवं कौशल के आधार पर नए ज्ञान एवं कौशल का विकास किया जाता है। इससे दुहरा लाभ होता है – एक यह कि पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल और अधिक स्थायी होता है और दूसरा यह कि नए ज्ञान एवं कौशल के सीखने में आसानी होती है और वह स्थायी होता है। अतः शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे सीखने के स्थानान्तरण के लिए उचित वातावरण तैयार करें, उसके लिए आवश्यक दशाओं का निर्माण करें।
(1) इसके लिए जहाँ तक अनुकूल पाठ्यचर्या के निर्माण का प्रश्न है, यह कार्य तो शिक्षा आयोजकों का है परन्तु शिक्षकों को इतना और करना होता है कि वे उस पाठ्यचर्या में जो सार्थक एवं उपयोगी है उससे सीखने वालों को अवगत कराएँ और इस विषय सामग्री को क्रम विशेष में संयोजित करें और तब उसे सीखने वालों के सामने प्रस्तुत करें। ।
(2) शिक्षकों को कुछ भी पढ़ाते-सिखाते समय शिक्षार्थियों को अपनी सामान्य बुद्धि के प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। इससे उनमें सामान्य योग्यता का विकास होगा जिसका स्थानान्तरण सरलता से किया जा सकेगा।
(3) शिक्षक शिक्षार्थियों को जो भी पढ़ाएँ-सिखाएँ उसे सही ढंग से पढ़ाएँ-सिखाएँ जिससे उन्हें उसका स्पष्ट ज्ञान हो, उस पर उनका अधिकार हो। उस स्थिति में ही सीखने का स्थानान्तरण सम्भव होगा ।
(4) शिक्षक शिक्षार्थियों को अपने पूर्व में सीखे ज्ञान एवं कौशल को नए सीखे जाने वाले ज्ञान एवं कौशल के सीखने में प्रयोग करने के लिए अभिप्रेरित करें।
(5) शिक्षक शिक्षार्थियों में सीखे ज्ञान एवं कौशल के प्रयोग की अभिवृत्ति का विकास करें।
(6) शिक्षकों को शिक्षार्थियों में उचित आदर्श और मूल्यों का विकास भी करना चाहिए। ये मनुष्य के व्यवहार को स्थायित्व प्रदान करते हैं।
(7) शिक्षकों को कुछ भी पढ़ाते-सिखाते समय शिक्षार्थियों को सामान्यीकरण के अवसर प्रदान करने चाहिए। इस सामान्यीकृत ज्ञान एवं कौशल का ही तो स्थानान्तरण होता है।
(8) शिक्षक किसी भी विषय को पढ़ाते अथवा कौशल को सिखाते समय ऐसी विधियों का प्रयोग करें जिनमें शिक्षार्थियों को अपने पूर्व में सीखे ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग करना पड़े।
(9) शिक्षकों को शिक्षार्थियों को अपने पूर्व में सीखे ज्ञान एवं कौशलों के प्रयोग के स्वतन्त्र अवसर प्रदान करने चाहिए।
इकाई – III
प्रश्न 6 (i) बुद्धि को परिभाषित कीजिए। थर्स्टन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि के सिद्धान्त का विस्तार से वर्णन कीजिए।
अथवा
बुद्धि से आप क्या समझते हैं? बुद्धि के बहुकारक सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
अथवा
बुद्धि क्या है? बुद्धि के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
अथवा
बुद्धि को परिभाषित कीजिए। बुद्धि के गिलफोर्ड के सिद्धान्त को समझाइए ।
अथवा
बुद्धि को परिभाषित कीजिए। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
अथवा
बुद्धि को परिभाषित कीजिए। गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
अथवा
बुद्धि क्या है? बुद्धि के समूह कारक सिद्धान्त के शैक्षिक निहितार्थों और सीमाओं की विवेचना कीजिए।
ANSWER-
बुद्धि का अर्थ
बुद्धि क्या है? इसका उत्तर आज भी कोई ठीक से नहीं दे सका है, फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर दिया है। बुद्धि भी मनुष्य की मानसिक योग्यता है जिससे मनुष्य अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सहायता लेता है। बुद्धि शब्द में बुद् और धि दो शब्द मिले हैं बुद् का अर्थ ऊपर या बाहर आना होता है और धि का अर्थ सन्तुष्ट करना होता है। अब दोनों शब्दों को मिलाकर बुद्धि का अर्थ होता है मनुष्य की क्षमता जो बाहर आये अर्थात् विभिन्न क्रियाओं में प्रकट हो और इसके फलस्वरूप वह अपने कार्य से सन्तुष्ट हो। बुद्धि अतएव व्यक्ति की जन्मजात मानसिक योग्यता है जो विभिन्न क्रियाओं को करने में प्रयुक्त होती है और तद्नुसार वह क्रिया में सफल होता है।
FIGGER-
अंग्रेजी में बुद्धि के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता है Intellect और Intelligence। इन दोनों में बारीक अन्तर पाया जाता है। शब्दकोश के अनुसार दोनों के मूल शब्द एक ही हैं जो लैटिन भाषा का Intelligere शब्द है जिसका अर्थ बोध करना, समझना अथवा आन्तरिक चुनाव करना है। इससे स्पष्ट है कि बुद्धि, जब कई चीजें सामने होती हैं तो उसे चुनकर अपना काम पूरा करने की क्षमता और योग्यता होती है। Intellect का अर्थ है अपने संज्ञानात्मक पहलू के साथ मन विशेषकर उच्चतर प्रक्रियाओं के सन्दर्भ में इस दृष्टि से हिन्दी में इसे प्रज्ञा अर्थात् बोध की विशेष प्रकार की अथवा उच्चतर मानसिक क्षमता। Intelligence का अर्थ है मन को सम्बद्ध करनेवाली क्रिया। यह एक प्रकार से मानसिक क्रिया हुई। परन्तु योग्यता के अर्थ में इसे प्रज्ञात्मक कौशल कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि बुद्धि मनुष्य की प्रज्ञा को अच्छी तरह से प्रयोग करने की योग्यता है अर्थात् प्रज्ञात्मक क्षमता है
बुद्धि की परिभाषाएँ
प्रो० बिने- “अच्छी तरह निर्णय करने, अच्छी तरह बोध करने और अच्छी तरह तर्क करने की योग्यता बुद्धि है।”
प्रो० बर्ट ने भी इस परिभाषा का समर्थन किया है। 1
प्रो० स्टर्न- “बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जो व्यक्ति को चैतन्य रूप से अपनी विचार-प्रक्रिया को नवीन आवश्यकताओं से समायोजित करने में सहायता करती है। ”
प्रो० स्पीयरमैन- “बुद्धि मनुष्य की सामान्य एवं विशेष कारकों से युक्त योग्यता है।”
प्रो० वेक्सलर- “उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तर्कयुक्त चिन्तन करने और अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की सम्पूर्ण या सार्वभौम क्षमता बुद्धि है।”
प्रो० स्टाडॉर्ड – “बुद्धि वह योग्यता है जिससे कठिनाई, जटिलता, अमूर्त्तता, मितव्ययता, उद्देश्य के प्रति अनुकूलता, सामाजिक मूल्य, मौलिकताओं के उद्गमन की विशेषताओं के साथ क्रिया करना
होता है तथा उन दशाओं के अन्तर्गत ऐसी क्रियाओं को करना जारी रखना होता है जो शक्ति के केन्द्रीकरण तथा शक्तियों के प्रतिरोध की माँग करती है।”
बुद्धि के सिद्धान्त
विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को निश्चित करने और उसकी व्याख्या करने के विभिन्न प्रयत्न किये हैं, लेकिन हम यहाँ पर गणितीय विश्लेषण कर सर्वमान्य सिद्धान्तों का वर्णन करेंगे। इससे पहले बुद्धि
किन बातों पर निर्भर करती है देखना होगा।
अब हम बुद्धि के प्रमुख सिद्धान्तों पर प्रकाश डालेंगे-
(1) एक-तत्त्व सिद्धान्त – इस सिद्धान्त का प्रतिपादन बिने महोदय ने किया था। उन्होंने इसका प्रचलन सन् 1911 में किया। बाद में इस सिद्धान्त का समर्थन टरमन, स्टर्स तथा एबिंग्हास ने किया इस सिद्धान्त के अनुसार बुद्धि केवल एक खण्डात्मक होती है जिसकी मात्रा मनुष्यों में मित्र-मित्र होती है। इसे सामान्य बुद्धि का नाम दिया जाता है। बुद्धि सर्वव्यापी मानसिक शक्ति है। सभी मानसिक क्रियाओं में इस महान् शक्ति-बुद्धि का एकच्छत्र राज्य है। इसके अनुसार वह व्यक्ति जो एक मानसिक कार्य सुचारु रूप से करता है वह अन्य मानसिक कार्य भी उसी प्रकार सुचारु रूप से करेगा। बुद्धि के एकच्छत्र राज्य की प्रवृत्ति के कारण ही इसे निरंकुशवादी सिद्धान्त भी कहते हैं। बुद्धि केवल एक ही तत्त्व से निर्मित है तथा समस्त क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है, यह सिद्धान्त दोषपूर्ण माना जाता है। हम यह नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति जो कला में निपुण है, वह विज्ञान में भी निपुण होगा। इस प्रकार, यह एकतत्त्व सिद्धान्त अथवा अखण्ड सिद्धान्त सर्वमान्य नहीं है। यदि हम इस सिद्धान्त से सहमत भी हो जायँ तब भी बुद्धि- मापन के लिए हमें इसे खण्डों में विभाजित करना पड़ेगा। प्रारम्भ में इस सिद्धान्त का बहुत स्वागत हुआ परन्तु यह सिद्धान्त, बुद्धि क्या है? इसका विशेष स्पष्टीकरण नहीं करता और मानसिक परीक्षण के आधार के रूप में भी यह अस्पष्ट है।
( 2 ) बहुकारक सिद्धान्त – इस सिद्धान्त के मुख्य समर्थक थार्नडाइक थे। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, इस सिद्धान्त के अनुसार बुद्धि कई तत्त्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्त्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती बल्कि ‘बुद्धि’ में कई स्वतन्त्र, विशिष्ट योग्यताएँ निहित रहती हैं जो विभिन्न कार्यों को सम्पादित करती हैं।
इस प्रकार एक-कारक एवं बहुकारक सिद्धान्त अतिवादी सिद्धान्त हैं। जिस प्रकार यह निश्चित नहीं है कि बुद्धि की अच्छी मात्रा द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो सकती है, उसी प्रकार यह भी निश्चित नहीं है कि विशिष्ट योग्यताओं से मनुष्य विशिष्ट क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है और शेष क्षेत्रों में पूर्ण रूप से असफल रहता है। गार्डनर मर्फी के विचारानुसार, “एक क्षेत्र की प्रतिभा का दूसरे क्षेत्र की प्रतिभा के साथ एक निश्चित सकारात्मक सम्बन्ध होता है। ”
इससे हम आसानी के साथ इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि सभी कार्यों में एक उभयनिष्ठ तत्त्व अवश्य होना चाहिए। यह सिद्धान्त इस निष्कर्ष की पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करने में असफल है और इसी के परिणामस्वरूप स्पीयरमैन कृत द्वि-कारक सिद्धान्त का जन्म हुआ।
( 3 ) स्पीयरमैन कृत द्वि-कारक सिद्धान्त -इस सिद्धान्त के समर्थक स्पीयरमैन थे। इनके अनुसार प्रत्येक प्रकार की क्रिया में एक सामान्य तत्त्व ‘G’ होता है जो सभी क्रियाओं में विद्यमान नहीं रहता।
इस प्रकार ‘सामान्य बुद्धि’ नाम की कोई चीज अवश्य है जो सभी क्रियाओं में विद्यमान रहती है और उसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट समस्याओं का सामना करता है। उदाहरणस्वरूप किसी व्यक्ति की हिन्दी की योग्यता में कुछ तो उसकी सामान्य बुद्धि होती है और कुछ भाषा सम्बन्धी ‘विशिष्ट योग्यता’ होती है अर्थात् G+ S1 या गणित में उसकी योग्यता का कारण होगा G+S2 | इस प्रकार कई विशिष्ट योग्यताएँ हो सकती हैं।
‘G’ तत्त्व न्यूनाधिक रूप से सभी विशिष्ट क्रियाओं में विद्यमान रहता है। इस प्रकार इस
व्यक्ति की पूर्ण बुद्धि (जिसे यदि ‘A’ की संज्ञा दी जाय) को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-
G+s1+ S2+ S3 = …….. =A
स्पीयरमैन कृत इस द्वि-कारक सिद्धान्त की विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना हुई है।
(i) स्पीयरमैन के कथनानुसार ‘बुद्धि’ को प्रकट करनेवाले दो तत्त्व होते हैं परन्तु जैसा कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है, इसमें दो नहीं बल्कि कई तत्त्व होते हैं। (G, S1, S2, S3 … आदि) ।
(ii) स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक कार्य में कुछ विशिष्ट योग्यता का होना आवश्यक है । परन्तु यह धारणा उचित नहीं जान पड़ती क्योंकि इसका यह अर्थ हो जाता है कि विभिन्न कार्यों में एक ‘सामान्य तत्त्व’ के अतिरिक्त और कुछ भी सामान्य नहीं होता और नर्सिंग कम्पाउण्डर तथा डॉक्टर के व्यवसाय को एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता। वास्तव में S1, S2, S3,
ये एक-दूसरे की सीमा को पार करके कई सामान्य तत्त्वों को जन्म देते हैं।
एक-दूसरे की सीमा को पार करके ‘ग्रूप’ के निर्माण से सम्बन्धित विचारधारा ने ग्रूप तत्त्व सिद्धान्त को जन्म दिया |
( 4 ) ग्रूप तत्त्व सिद्धान्त (समूह तत्त्व सिद्धान्त ) – जो सभी तत्त्व प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते परन्तु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं उन्हें ‘ग्रूप-तत्त्व’ की संज्ञा दी गयी है। इस सिद्धान्त के समर्थकों में थर्स्टन का नाम प्रमुख है। प्रारम्भिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रारम्भिक तत्त्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो उन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करता है और उन्हें अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग करता है। मानसिक क्रियाओं के कई ग्रूप होते हैं। उनमें अपना एक प्रारम्भिक तत्त्व होता है। थर्स्टन तथा उनके साथियों नये ऐसे नौ तत्त्वों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं-
(a) मौखिक तत्त्व – इसका सम्बन्ध शब्दों तथा विचारों के साथ है।
(b) स्थान-सम्बन्धी तत्त्व-इसका सम्बन्ध व्यक्ति के किसी स्थान-विशेष में किसी चीज के परिमाण आदि के बारे में है।
(c) अंक सम्बन्धी तत्त्व-अंकों से सम्बद्ध हिसाब-किताब को शीघ्र एवं शुद्ध रूप से करना ।
(d) स्मृति तत्त्व- जल्दी से याद करने की योग्यता ।
(e) शाब्दिक प्रवाह सम्बन्धी तत्त्व-तेजी के साथ पृथक् शब्दों पर सोचने की योग्यता ।
(f) निगमन तर्क तत्त्व-इसका सम्बन्ध चिन्तन की निगमन प्रणाली से है
(g) आगमन-तर्क तत्त्व-यह चिन्तन की आगमन प्रक्रिया से सम्बन्धित है।
(h) प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी तत्त्व-इसका सम्बन्ध प्रत्यक्षीकरण से है।
(i) समस्या समाधान सम्बन्धी योग्यता तत्त्व- समस्याओं को हल करने की योग्यता से इसका सम्बन्ध है।
(5) प्रतिदर्श सिद्धान्त-
इस सिद्धान्त के प्रवर्तक थॉम्पसन हैं। उनका कहना है कि मनुष्य में अनेक योग्यताएँ होती हैं किन्तु जब मनुष्य किसी कार्य को सम्पादित करता है तो उस कार्य के सम्पादन के लिए सभी योग्यताओं में से थोड़ा-थोड़ा प्रतिदर्श लेकर उस कार्य-विशेष के लिए एक नवीन योग्यता बना लेता है। कार्य सम्पादित होने के बाद नवीन संगठन विच्छेदित हो जाता है। इस तथ्य को हम यूँ भी स्पष्ट कर सकते हैं कि मानसिक योग्यताओं के विशाल समूह में से आवश्यकतानुसार न्यादर्श लेकर प्रस्तुत कार्य को सम्पादित करने के लिए उन प्रतिदर्शों के आधार पर मानसिक योग्यताओं का एक संगठन तैयार कर व्यक्ति उस कार्य को सम्पादित करता है। इस वीन संगठन में केवल उन्हीं मानसिक योग्यताओं से प्रतिदर्श लिये जाते हैं जिनके मध्य पर्याप्त सह-सम्बन्ध होता है। विभिन्न मानसिक योग्यताओं के परीक्षणों के फलांकों में पाया जानेवाला धनात्मक सह-सम्बन्ध विभिन्न न्यादर्शों के सभी स्वतन्त्र कारकों के प्रतिनिधित्व मिश्रण से प्राप्त होता है। एक सामान्य अनुभव है कि जटिल परीक्षणों में सरल परीक्षणों की अपेक्षा अधिक सह- सम्बन्ध पाया जाता है जिसकी व्याख्या थॉम्पसन के इस सिद्धान्त के आधार पर आसानी से की जा सकती है। स्पीयरमैन का सिद्धान्त इस दृष्टि से उपयोगी नहीं है। थॉम्पसन के सिद्धान्त के अन्तर्गत अंक प्राप्त करने का एक ठोस आधार होता है जिसके कारण व्यक्तियों की विभिन्न योग्यता का मापन सरलता से किया जा सकता है। साथ ही, थॉम्पसन, स्पीयरमैन के सामान्य तत्त्व (G) की एकच्छत्र सत्ता को स्वीकार नहीं करता परन्तु समूह कारक से वह सहमत है, जो कि स्पीयरमैन के विशिष्ट कारक (S) की तरह संकुचित नहीं है और न ही सामान्य कारक (G) की तरह विस्तृत ।
यादर्शों के पारस्परिक सह-सम्बन्ध को निम्न चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है-
( 6 ) क्रमिक महत्त्व सिद्धान्त-यह एक नवीन सिद्धान्त है जिसका प्रतिपादन बर्ट (Burt) तथा वर्नन (Vernon) ने किया। यह सिद्धान्त प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्त्व प्रदान करता है। इस महत्त्व क्रम में सामान्य मानसिक योग्यता सर्वप्रथम आती है तथा विशिष्ट योग्यताएँ निम्नतम स्तर पर। सामान्य मानसिक योग्यता दो प्रमुख खण्डों में विभक्त रहती है। फिर, ये प्रमुख
• खण्ड अन्य गौड़ खण्डों में विभक्त होते हैं और गौड़ खण्ड अनेक विशिष्ट खण्डों में विभक्त होते. हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार सामान्य मानसिक योग्यता दो खण्डों में विभक्त है-(1) क्रियात्मक, यान्त्रिक, प्रक्षेपण तथा शारीरिक अथवा K. M. तथा (2) शाब्दिक आंकिक तथा शैक्षिक अथवा V. D. जिनके वर्गीकरण में कारक-विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है। महत्त्व क्रम के अन्तिम स्तर में जिन विशिष्ट मानसिक योग्यताओं को रखा जाता है उनका विभिन्न ज्ञानात्मक क्रियाओं से अलग-अलग सम्बन्ध रहता है।
(7) गिलफोर्ड का बुद्धि सम्बन्धी सिद्धान्त और बुद्धि प्रतिमान जे० पी० गिलफोर्ड और इसके सहयोगियों ने बुद्धि परीक्षण से सम्बन्धित कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्त्वों या कारकों को प्रकाश में लानेवाला प्रतिमान विकसित किया है। उन्होंने अपने अध्ययन प्रयासों के द्वारा यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि हमारी किसी भी मानसिक प्रक्रिया अथवा बौद्धिक कार्य को तीन आधारभूत आयामों संक्रिया, सूचना-सामग्री या विषय-वस्तु तथा उत्पाद में बाँटा जा सकता है। संक्रिया से हमारा तात्पर्य हमारी उस मानसिक चेष्टा तत्परता और कार्यशीलता से होता है जिसकी मदद से हम किसी भी सूचना सामग्री या विषयवस्तु को अपने चिन्तन तथा मनन का विषय बनाते हैं या दूसरे शब्दों में, इसे चिन्तन तथा मनन का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि को काम में लाने का प्रयास कहा जा सकता है। हम जिस रूप में चिन्तन या मनन करते हैं अथवा चिन्तन और मनन के लिए जिस प्रकार की विषयवस्तु या सूचना – सामग्री की सहायता लेते हैं उसे बुद्धि को प्रयोग में लाने का दूसरा आधारभूत आयाम विषयवस्तु कहा जा सकता है तथा बौद्धिक संक्रिया के द्वारा सूचना-सामग्री या विषयवस्तु को लेकर जिस प्रकार की बौद्धिक प्रक्रिया की जाती है उसके परिणामस्वरूप जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद का नाम दिया जाता है। इन तीनों आधारभूत आयामों संक्रिया, विषयवस्तु तथा उत्पाद को भी उनके अपने विशिष्ट तत्त्वों या कारकों में विभाजित किया जा सकता है। गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि प्रतिमान में संक्रिया को उसे 5 विशिष्ट तत्त्वों, विषयवस्तु को 5 तथा उत्पाद को 6 विशिष्ट तत्त्वों में बाँटने का प्रयास किया है और फिर इन विशिष्ट तत्त्वों या कारकों की अन्तःक्रिया के माध्यम से बुद्धि में 5 5 6 150 तत्त्वों या कारकों की उपस्थिति का संकेत दिया है।
उपर्युक्त प्रतिमान के माध्यम से गिलफोर्ड ने यह बताने की चेष्टा की है कि मानव बुद्धि को अलग-अलग प्रकार की 150 मानसिक योग्यताओं का समूह कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में उसने बुद्धि में 150 विभिन्न तत्त्वों या कारकों की उपस्थिति की बात कही है और इन तत्त्वों तथा कारकों को 5 प्रकार की संक्रियाओं, 5 प्रकार की विषयवस्तु या सूचना-सामग्री तथा 6 प्रकार के उत्पाद की अन्तः क्रिया का प्रतिफल बताया है।
प्रश्न 6 (ii) समंजन किसे कहते हैं? समंजन की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए इस हेतु प्रयुक्त किन्हीं दो रक्षा युक्तियों को समझाइए ।
अथवा
समंजन किसे कहते हैं? इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक अध्यापक के लिए समाज के सम्प्रत्यय को समझने की क्या आवश्यकता है? उदाहरण की सहायता से समझाइए ।
अथवा
समंजन किसे कहते हैं? समंजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आपकी दृष्टि में एक सुसंजित व्यक्ति में क्या विशेषताएँ होनी आवश्यक है?
ANSWER–
समायोजन का अर्थ व परिभाषा –
एक छात्र अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना अपना लक्ष्य बनाता है, पर दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता और अपनी कम योग्यता के कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है। इससे वह निराशा और असन्तोष, मानसिक तनाव और संवेगात्मक संघर्ष का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में वह अपने मौलिक लक्ष्य को त्यागकर अर्थात् अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अपनी असफलता के प्रति ध्यान न देकर वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना अपना लक्ष्य बनाता है। अब यदि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो वह अपनी परिस्थिति या वातावरण से ‘समायोजन कर लेता है। पर यदि उसे सफलता नहीं मिलती है, तो उसमें ‘असमायोजन’ उत्पन्न हो जाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाना या परिस्थितियों के अनुकूल हो जाना ही समायोजन कहलाता। है। यह समायोजन व्यक्ति अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार करता है।
हर ‘समायोजन’ और ‘असमायोजन’ के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएँ दे रहे हैं, यथा-
1. गेट्स व अन्य-“समायोजन निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच सन्तुलित सम्बन्ध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है।”
2. बोरिंग, लैगफेल्ड व वेल्ड – “समायोजन वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में सन्तुलन रखता है।”
3. गेट्स व अन्य- “असमायोजन, व्यक्ति और उसके वातावरण में असन्तुलन का उल्लेख करता है |
इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समायोजन निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है साथ ही व्यक्ति, परिस्थिति तथा पर्यावरण के मध्य अपने को समायोजित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अत: समायोजन को सन्तुलित दशा कहा गया है।
समायोजन के लक्षण —
समायोजन करने वाले व्यक्ति में ये लक्षण पाये जाते हैं-
1. परिस्थिति का ज्ञान, नियन्त्रण तथा अनुकूल आचरण,
2. सन्तुलन,
3. पर्यावरण तथा परिस्थिति से लाभ उठाना,
4. समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान,
5. सन्तुष्टि एवं सुख,
6. सामाजिकता, आदर्श चरित्र, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, सन्तुलित तथा दायित्वपूर्ण,
7. साहसी एवं समस्या का समाधान युक्त। इसीलिये गेट्स ने कहा है-समायोजित व्यक्ति वह है जिसकी आवश्यकताएँ एवं तृप्ति सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के सदृश्य संगठित हों।
समायोजन की प्रक्रिया
व्यक्ति समायोजन करने के लिए अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है या पर्यावरण के अनुरूप अपना अनुकूलन करके स्वयं बदल जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने विचारों, सम्प्रत्ययों, अभिवृत्तियों, प्रत्यक्षण, भावनाओं, संवेग तथा क्रियाओं में परिवर्तन करता है।
स्पष्ट है कि व्यक्ति की आवश्यकता प्राप्ति के लक्ष्य में उसके विभिन्न वातावरण प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य प्राप्ति न होने पर व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। फलस्वरूप व्यक्ति में तनाव कम करने के लिए स्वयं में अथवा वातावरण में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यदि वह इस क्रिया में सफल रहता है तो समायोजित हो जाता है।
रक्षा युक्तियाँ
रक्षा युक्तियाँ निम्न प्रकार की हैं-
(1) शोधन-जब व्यक्ति की काम-प्रवृत्ति तृप्त न होने के कारण उसमें तनाव उत्पन्न करती है, जब वह कला, धर्म, साहित्य, पशुपालन, समाज-सेवा आदि में रुचि लेकर अपने तनाव को कम करता है।
(2) प्रक्षेपण- इस विधि में व्यक्ति अपने दोष का आरोपण दूसरे पर करता है। उदाहरणार्थ, यदि बढ़ई द्वारा बनाई गई किवाड़ टेढ़ी हो जाती है, तो वह कहता है कि लकड़ी गीली थी।
समायोजन के उपाय
बालकों को समायोजित करने में उसके माता-पिता तथा शिक्षक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक को समायोजित करने के लिए आवश्यक है कि उसे इच्छित लक्ष्यों की ओर उन्मुख किया जाए तथा उसके मानसिक तनावों को कम किया जाए। बालकों को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं-
1. छात्रों की ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए और शिक्षा को बाल-केन्द्रित बनाया जाए।
2. स्कूल का वातावरण पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होना चाहिए, जिससे छात्र प्रश्न पूछ सकें तथा | आत्म-अभिव्यक्ति कर सके तथा उसमें सुरक्षा की भावना हो।
3. छात्रों के लिए स्कूल में प्रयुक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाए।
4. छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और वात्सल्यपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।
5. शिक्षक का कार्य विद्यालय में शिक्षण के साथ-साथ स्वस्थ वातावरण पैदा करना भी है, जो बालक को समायोजन के लिए प्रेरित करता है।
6. माता-पिता घर पर स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का प्रयत्न करें तथा स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें।
7. विद्यालय में कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। अनुशासन दण्ड द्वारा भय दिखाकर नहीं बल्कि छात्रों में नियम पालन तथा उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करके स्थापित किया जाना चाहिए।
8. छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार विषय दिए जाएँ तथा उनकी शिक्षा सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए।’
प्रश्न 7 (i) बुद्धि से आप क्या समझते हैं? बुद्धि की परिभाषा दीजिए तथा बुद्धि के प्रकार बताइए।
ANSWERE-
बुद्धि का अर्थ –
बुद्धि क्या है? इसका उत्तर आज भी कोई ठीक से नहीं दे सका है, फिर भी मनोवैज्ञानिक ने उत्तर दिया है। बुद्धि भी मनुष्य की मानसिक योग्यता है जिससे मनुष्य अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सहायता लेता है। बुद्धि शब्द में बुद और धि दो शब्द मिले हैं। बुद् का अर्थ ऊपर या बाहर आना होता है और की धि का अर्थ सन्तुष्ट करना होता है। अब दोनों शब्दों को मिला कर बुद्धि का अर्थ होता है। मनुष्य क्षमता जो बाहर आवे अर्थात् विभिन्न क्रियाओं में प्रकट हो और इसके फलस्वरूप वह अपने कार्य से सन्तुष्ट हो। अतएव बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात मानसिक योग्यता है जो विभिन्न क्रियाओं को करने में प्रयुक्त होती है और तदनुसार वह क्रिया में सफल होता है।
बुद्धि की परिभाषा —
प्रो० बिने के अनुसार, “अच्छी तरह निर्णय करने, अच्छी तरह बोध करने और अच्छी तरह तर्क करने की योग्यता बुद्धि है।”
प्रो० स्टर्न के अनुसार, “बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जो व्यक्ति को चैतन्य रूप से अपनी विचार प्रक्रिया को नवीन आवश्यकताओं से समायोजित करने में सहायता करती है।”
स्पीयरमैन के अनुसार, “बुद्धि मनुष्य की सामान्य एवं विशेष कारकों से युक्त योग्यता है।”
बुद्धि के प्रकार —
बुद्धि के प्रकार पर कई ढंग से विचार किया जा सकता है। प्रो० टरमन ने बुद्धि-लब्धि का संकेत किया है और उसके अनुसार
(1) प्रतिभाशाली,
(2) उत्कृष्ट,
(3) सामान्य,
(4) मन्द,
(5) न्यून,
(6) मूढ़,
(7) जड़ बुद्धि आदि बताई गई हैं। इस प्रकार बुद्धि की मात्रा के आधार पर यह वर्गीकरण होता है। इसके अलावा निम्न प्रकार की बुद्धि बताई गई है-
1. अमूर्त्त बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि-सूक्ष्म प्रश्नों और जटिल समस्याओं को हल करने में अमूर्त बुद्धि पायी जाती है। वैज्ञानिक, गणितज्ञ, कवि, दार्शनिक की बुद्धि सूक्ष्म कहलाती है। अंक, शब्द, प्रतीक, संकेत आदि की सहायता से यह प्रकट होती है। अधिगम विचाराभिव्यक्ति, समस्या, हल, कला में हम अमूर्त बुद्धि से काम लेते हैं। विद्यालयीय शिक्षण में अध्यापक इसी की सहायता से ज्ञान देने में समर्थ होता है।
2. मूर्त्त बुद्धि-
कौशल, यंत्र, निर्माण के कार्यों में मूर्त्त बुद्धि पायी जाती है। बढ़ई, लुहार, मिस्त्री, राजगीर आदि इसी बुद्धि से काम करते हैं। मूर्त वस्तुओं की सहायता से काम करना इसी के कारण सम्भव होता है। इसमें कर्मेन्द्रियों की सहायता ली जाती है यद्यपि चिन्तन की क्रिया भी पायी जाती है। निष्पादन एवं हस्तकौशल इसी बुद्धि के आधार पर होता है।
3. सामाजिक बुद्धि-
यह व्यक्ति की उस योग्यता को संकेत करती है जिससे मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ समायोजन करने, सम्बन्ध बनाये रखने, आपसी व्यवहार करने, सुख-दुःख में भाग लेने में समर्थ होता है।
4. व्यावहारिक बुद्धि-
चरित्र और आचरण से व्यावहारिक बुद्धि पायी जाती है। किसके साथ कैसा व्यवहार मनुष्य को करना चाहिए यह व्यावहारिक बुद्धि बताती है। पिता का पुत्र के साथ, अध्यापक का छात्र के साथ, प्रशासक का नियोक्ता के साथ और इसके व्यक्तिक्रम रूप में भी व्यावहारिक बुद्धि होती है। दैनिक लेन-देन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। घर में और घर के बाहर इसी का प्रयोग किया जाता है।
5. यांत्रिक बुद्धि-
यंत्र के साथ और यंत्र की तरह काम करने में यांत्रिक बुद्धि पायी जाती है। मोटर चालक, इंजिन चालक, अन्य सवारियों के चालक इसी बुद्धि से काम करते पाये जाते हैं और उनमें यंत्र की तरह काम करने की आदत भी पायी जाती है। अतएव यहाँ हम यांत्रिक बुद्धि ही पाते हैं। रटन्त क्रिया भी यांत्रिक बुद्धि से सम्बन्धित होती है। क्रमबद्ध रूप में कार्य करने में भी यांत्रिक बुद्धि होती है जैसे दफ्तर में 10 बजे से 4 बजे तक काम करना, विद्यालय में 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई में लगे रहना भी यांत्रिक बुद्धि को बताता है। दैनिक समय सारिणी का अनुगमन यांत्रिक बुद्धि को बताता है।
प्रश्न 7 (ii) बुद्धि का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है? बुद्धि के मापन में कौन- कौन सी समस्यायें आती हैं? बुद्धि मापन के किसी एक परीक्षण का वर्णन कीजिए।
अथवा
बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धिलब्धि का प्रयोग शिक्षण प्रक्रियाओं के अध्ययन में किस प्रकार किया जा सकता है? उदाहरण देकर समझाइए ।
अथवा
बुद्धि परीक्षणों के उपयोग
ANSWER–
बुद्धि-मापन का तात्पर्य –
बुद्धि हमारी जन्मजात योग्यता है जो हमारे विचार-चिन्तन एवं सभी प्रकार के कामों में पायी जाती है। अतएव किस व्यक्ति में इस प्रकार की योग्यता कितनी मात्रा में है इसे ज्ञात करना ही बुद्धि-मापन है। मानसिक योग्यता की मात्रा को मालूम करना बुद्धि-मापन है। उदाहरण के लिए, एक 10 वर्ष का बालक कक्षा 5 में सब लड़कों से अधिक अंक प्राप्त करता है। सभी विषयों में वह 100 अंक में 60- 70 अंक पाता है तो हम उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। कोई दूसरा छात्र अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर बहुत देर में देता है, अशुद्ध उत्तर देता है। ऐसी हालत में उसमें बुद्धि की मात्रा कम पायी जाती है। उसके परीक्षाफल ही उसकी बुद्धि की माप बताते हैं। अतएव परीक्षणों के द्वारा हम व्यक्ति की सामान्य और विशेष योग्यता की जानकारी करते हैं तो उसे हम बुद्धि-मापन कहते हैं।
बुद्धि-मापन एक प्रकार से स्वाभाविक ढंग से भी होनेवाली क्रिया है। घर में हम किसी बालक कुछ चीज उठाने, उठाकर रखने, खोलने-बाँधने, लाने-देने को कहते रहते हैं। यदि हम उसे ठीक से करता हुआ देखते हैं तो सन्तुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि उसमें बुद्धि है और ठीक से न करने पर हम उसे धिक्कारते हैं कि उसमें बुद्धि नहीं है। अतएव बुद्धि का मापन व्यक्ति की कार्यकुशलता का बोधक होता है। अतः बुद्धि का मापन कार्यकुशलता की स्वीकृति और अस्वीकृति भी होती है। इसे जानने के कई साधन हैं जिन्हें हम मापन के साधन या परीक्षण कहते हैं। अतएव परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की बुद्धि की मात्रा को जानना ही बुद्धि का मापन होता है।
मानसिक एवं कालिक आयु –
मानसिक आयु एवं कालिक आयु है क्या? इसे क्यों जाना जाय? यह प्रश्न होना स्वाभाविक होता है। बुद्धि मानसिक योग्यता है अतएव बुद्धि की आयु को मानसिक आयु कहते हैं। आयु का तात्पर्य वर्ष से ज्ञात होता है अतएव कालिक आयु या शारीरिक आयु या वास्तविक आयु की तरह व्यक्ति की मानसिक योग्यता का भी समय होता है। इसे मानसिक आयु से संकेत करते हैं जो व्यक्ति की मानसिक उपलब्धि के आधार पर निश्चित की जाती है। कालिक आयु जन्म के बाद से वर्तमान समय तक की अवधि को कहते हैं अर्थात् व्यक्ति के जन्म से लेकर जीवित रहने की अवधि कालिक आयु है।
प्रो० बिने ने जब बुद्धि परीक्षण बनाया उस समय उन्होंने हरेक उम्र (Age) के लिए कुछ निश्चित प्रश्न बनाये, जैसे- 3 वर्ष के बालक के लिए 4 प्रश्न बनाये। 4 वर्ष के बालक के लिए 4 प्रश्न बनाये और इसी प्रकार अन्य आयु वालों के लिए भी प्रश्न तैयार किये। इस आधार पर यदि 3 वर्ष का बालक 4 प्रश्न के सही उत्तर दे देता तो उसकी मानसिक आयु 3 वर्ष की होती है और यदि वह 4 वर्ष के बालक के लिए दिये गये प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के सही उत्तर दे देता तो उसकी मानसिक आयु (3-1 = 23 ) वर्ष की होती है। इस ढंग से 3 वर्ष के बालक की इन दशा में आयु 31⁄2 वर्ष की हो गयी जबकि उसकी कालिक आयु 3 वर्ष की ही रही। कालिक आयु से मानसिक आयु कम भी होती है। यदि यही बालक 3 वर्ष की आयु वाले केवल 3 प्रश्नों का सही उत्तर देता और 4 वर्ष वालों के लिए बने प्रश्नों में से कुछ भी न कर सकता तो इसकी उम्र मानसिक आयु (3-4 = 23 ) वर्ष हुई। अतः अब ज्ञात हो गया कि व्यक्ति की मानसिक आयु उसकी कालिक आयु से बढ़ती-घटती रहती है या समान भी रहती है। मानसिक तथा कालिक आयु में मुख्य अन्तर आधार का है। मानसिक आयु व्यक्ति के निष्पादन, ज्ञान, योग्यता की कुशलता के आधार पर निश्चित की जाती है, जबकि कालिक आयु जन्म से जीवित रहने की तिथि तक की अवधि पर निश्चित की जाती है।
बुद्धि- लब्धि —
प्रो० एम० एल० टरमन ने सबसे पहले प्रो० बिने के बुद्धि परीक्षण का संशोधन अमेरिका में किया और बुद्धि-लब्धि का उपयोग किया। प्रो० सोरेन्सन का कथन है कि मानसिक आयु मानसिक परीक्षण से निर्धारित होती है। किसी भी कालिक आयु वाले बालक के लिए निर्धारित औसत प्राप्तांक मानसिक स्तर या मानसिक विकास का स्तर संकेत करता है। अतएव मनोवैज्ञानिक टरमन ने मानसिक आयु और कालिक आयु का एक अनुपात मालूम किया और उसे उसने बुद्धि-लब्धि कहा। इस आधार पर बुद्धि-लब्धि किसी भी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा कालिक आयु की अनुपात होती है। प्रो० ड्रेवर ने लिखा है कि “बुद्धि-लब्धि : मानसिक आयु की कालिक आयु के साथ अनुपात एक प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त।”
बुद्धि-लब्धि जानने का एक सूत्र भी प्रो० टरमन के द्वारा बताया गया है जो इस प्रकार है-
मानसिक आयु (Mental Age)
बुद्धि-लब्धि (I.Q.) = मानसिक आयु (Mental Age) * 100 / कालिक आयु (Chronological Age)
इस सूत्र से हम प्राप्तांकों की सहायता से मानसिक आयु मालूम कर लेते हैं। कालिक या वास्तविक आयु ज्ञात रहती ही है और पुनः बुद्धि-लब्धि मालूम करते हैं। 100 से गुणा क्यों करते हैं? जिससे कि संख्या प्रतिशत में आवे और छोटी पूर्णांक के रूप में प्रकट की जा सके। एक उदाहरण से इसे स्पष्ट किया जा सकता है-
मान लीजिये एक बालक की आयु 16 वर्ष है। उसको परीक्षण देने पर जो प्राप्तांक मिले उससे उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष की हुई तो उसकी बुद्धि-लब्धि क्या होगी ?
बुद्धि-लब्धि = 15 × 100 /16 = 94 (के करीब)
इसी प्रकार से यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 और कालिक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि-लब्धि क्या होगी?
बुद्धि-लब्धि = 20 x 100 /16 = 125
बुद्धि-लब्धि की उपयोगिता- मनोवैज्ञानिकों के परिणामों के आधार पर यह कहना सरल है कि बुद्धि-लब्धि क्यों मालूम की जाती है, इसकी क्या उपयोगिता है। बुद्धि-लब्धि से एक तो बालक की मानसिक स्थिति मालूम होती है, दूसरे उसके मानसिक विकास में सहायता मिलती है, तीसरे उसे आगे बढ़ने
के लिए यथोचित निर्देशन दिया जा सकता है जिससे उसे अधिक-से-अधिक सफलता मिल सके। अतएव स्पष्ट है कि बुद्धि-लब्धि की एक बड़ी शैक्षिक एवं व्यावहारिक उपयोगिता पायी जाती है।
परीक्षण की समस्याएँ
(1) इसका प्रभावीकरण बहुत ही कठिन, असम्भव एवं जटिल है।
(2) इसमें शब्द ज्ञान को इतना अधिक महत्त्व दिया गया है कि वह छात्रों के लिए दुष्कर हो जाता है। अधिक आयु की सभी परीक्षाएँ शाब्दिक योग्यता से अत्यन्त प्रभावित रहती हैं। अतः वे व्यक्ति जिनमें यह योग्यता नहीं होती, इस परीक्षा में कम अंक पाते हैं |
(3) इस परीक्षा को लागू करने का तरीका भी उचित नहीं है। क्योंकि जब किसी बालक को यह परीक्षा दी जाती है तब उसकी आधारीय आयु अज्ञात होने के कारण परीक्षक को या तो पिछली परीक्षा वेनी पड़ती है या आगे की परीक्षाएँ देनी होती हैं, जिसका बालक पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
(4) यह परीक्षण बालकों के लिए अवश्य ही सरल एवं उचित है पर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए यह किसी भी भाँति अनुरूप नहीं है।.
(5) यह परीक्षण सभी उद्देश्यों के लिए वैध नहीं है।
(6) इस परीक्षण से भेददर्शी अभियोग्यता का मापन नहीं होता।
(7) परीक्षण की फलांकन प्रक्रिया उचित नहीं है। कई परीक्षण पद ऐसे होते हैं जिनके कई उत्तर हो सकते हैं। लेकिन जिन उत्तरों को अंकन कुंजी में रखा गया है उनको ही स्वीकृत माना जाता है।
(8) इस परीक्षण में प्रयुक्त मानसिक आयु के सिद्धान्त में अनेक त्रुटियाँ हैं, जैसे-विभिन्न आयु-स्तरों पर मानसिक आयु की इकाइयों में असमानता, एक परीक्षण से प्राप्त मानसिक आयु-मानकों की दूसरे परीक्षण से प्राप्त मानकों से तुलना न होना तथा प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग न किया जाना आदि।
सामूहिक शाब्दिक परीक्षण —
ये परीक्षण ऐसे व्यक्तियों के लिए बनाये जाते हैं जो शिक्षित होते हैं अथवा जिन्हें भाषा का ज्ञान होता है। इस प्रकार के परीक्षणों में प्रयोग होनेवाली सामग्री निम्नलिखित है-
(1 ) समानता एवं विभिन्नता – प्रस्तुत साम्य शब्दों में से भिन्न अर्थ रखनेवाले शब्द के नीचे रेखा खींचिए- मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, विद्यालय।
(2) सादृश्य-कोष्ठक के बाहरवाले शब्दों में कोष्ठक के अन्दरवाले दो शब्दों का सम्बन्ध देखिये और उसके नीचे रेखा अंकित कीजिए- जूता, सिर, हाथ (पैर, बाल, घड़ी) ।
(3) आवश्यक-कोष्ठक के अन्दरवाले शब्दों के लिए जो आवश्यक हो, कोष्ठक के अन्दरवालों में रेखांकित कीजिए- (जल, आकाश, नादान, घट) मछली।
(4) विलोम शब्द – विलोम शब्द के नीचे रेखा खींचिए-
उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण, वैभव
जल-थल, नभ, धरती
उन्नति-पतन, उत्कर्ष
(5) तुलना -बताइये कौन बड़ा है ?
भक्ति अथवा ज्ञान (भक्ति)
गुरु अथवा गोविन्द (गुरु)
(6) पर्याय- प्रस्तुत शब्द का कोष्ठक में पर्याय शब्द ढूँढ़िये तथा उसे रेखांकित कीजिए- प्रस्तुत शब्द पृथ्वी।
(रवि, अंशुमाली, करुण, रजनीश, धरनि) ।
(7) दिशा बोध-स्कूल मेरे घर से 3 मील उत्तर में है तथा पोस्ट ऑफिस 3 मील पूर्व में है। यदि मन्दिर स्कूल से 4 मील पूर्व में हो तो पोस्ट ऑफिस किस ओर है?
(8) अंकगणितीय समस्याएँ-एक डायरी का मूल्य 6 रु० है तो 15 डायरियों का मूल्य क्या होगा?
(9) क्रमिक संख्या अथवा संख्याओं का क्रम प्रस्तुत संख्याओं को देखकर बताइये कि इनसे आगे कोष्ठक में कौन-सी संख्या आयेगी ?
आर्मी- अल्फा परीक्षण-
टरमन का स्टेनफोर्ड बिने परीक्षण सन् 1916 में प्रकाशित हुआ और उसके एक वर्ष बाद ही अमेरिका को प्रथम विश्वयुद्ध में शामिल होना पड़ा। परिणामस्वरूप यह अनुभव किया गया कि लाखों व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को छाँटकर बाहर निकाल दिया जाय जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हों तथा दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों की खोज की जाय जो फौज में अफसर बनने योग्य हों। इस कार्य के लिए शीघ्र ही ‘अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संस्था’ ने विशेषज्ञों की एक कमेटी बनायी, जिसे ऐसे परीक्षण निर्माण का कार्य सपिा गया जिसे एक ही समय में व्यक्तियों के बड़े समूह पर प्रशासित किया जा सके। राबर्ट एम० यर्क्स, जो येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इसके अध्यक्ष -नियुक्त किये गये। इस कमेटी के अन्य सदस्य थे टरमन, ओटिस आर्थर, हेनरी गोडार्ड, वैल्स, बिन्धम, हिपिल तथा हैन्स । परीक्षण निर्माण में कमेटी ने इस बात का ध्यान रखा कि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति की जन्मजात योग्यता का ही मापन सम्भव हो तथा जहाँ तक सम्भव हो सके परीक्षण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रभाव से पूर्णतया स्वतन्त्र हो । अन्ततः कमेटी की देखरेख में जिस प्रथम परीक्षण की रचना की गयी उसका नाम आर्मी- अल्फा परीक्षण रखा गया। इस परीक्षण में कुल 8 भाग हैं तथा प्रत्येक भाग में प्रश्नों की संख्या लगभग 12 से लेकर 40 तक है। प्रत्येक भाग में प्रश्नों को उनके क्रमिक कठिनाई स्तर के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है अर्थात्, प्रारम्भ में सबसे सरल तथा अन्त में सबसे कठिन प्रश्नों को रखा गया है। स्पष्ट है, सरल प्रश्नों को अधिकाधिक अभ्यर्थी हल कर लेंगे जबकि कठिन प्रश्नों को कुछ ही अभ्यर्थी हल कर सकेंगे। परीक्षण के प्रथम स्वरूप में निम्नलिखित निर्देश अभ्यर्थी को जोर से पढ़कर सुनाये जाते हैं-
“सावधान! दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखो जिसमें अंकों के चारों ओर वृत्त खींच दिये गये हैं। जब मैं ‘चलो’ कहूँ, तो दूसरे से लेकर पाँचवें वृत्त तक रेखा खींचो जो तीसरे वृत्त के नीचे से चले और पाँचवें वृत्त
“के ऊपर से ।” “चलो। ”
शेष अन्य 2 से लेकर 8 तक परीक्षणों में जिस प्रकार के प्रश्नों को रखा गया है, वे क्रमशः हैं- गणित सम्बन्धी 20 समस्याएँ, सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न, शब्दों के 40 युग्म जिनके माध्यम से यह निर्णय लिया जा सके कि वे पर्यायवाची हैं या विलोमार्थक, ऐसे शब्द जिन्हें वाक्यों में व्यवस्थित करना होता है, अंक सारणी की पूर्ति करना जैसे 5.6.8..11..15..20, अनुपातपूरक प्रश्न, जैसे- ठण्डी : बियर :: गर्म : … तथा सामान्य सूचना सम्बन्धी प्रश्न ।
परीक्षण के प्रशासन एवं अंकन की दृष्टि से परीक्षण की समय-सीमा 24 मिनट है तथा अधिकतम अंक 212 हैं। अंकों का वर्गीकरण इस प्रकार है, 135 श्रेष्ठ; 105-134 बेहतर 45-104 सन्तोषजनक। साथ ही, इसी क्रम में एक अफसर का सामान्य अंक 105 है तथा सिपाही का 60 माना गया है। परीक्षण परिणामों के आधार पर प्रज्ञांक (IQ.) भी प्रायः मशीन से निकाल लिया जाता है जिससे न तो अधिक समय ही व्यय होता है और न ही कुशल परीक्षकों की ही आवश्यकता होती है। इस प्रकार वह परीक्षण समूह बुद्धि-परीक्षण का एक उत्तम उदाहरण है।
प्रश्न 7 (iii) अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? एक अध्यापक के रूप में अपने विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेरित करेंगे?
ANSWER–
अधिगम में अभिप्रेरण का तात्पर्य
–
अधिगम या सीखना केवल एक मानसिक प्रक्रिया मात्र नहीं है। हमें अधिगम का तात्पर्य विद्यालय की परिस्थितियों में ज्ञान, अनुभव और कौशल के अर्जन से लेना चाहिए। अतः जब बालक या वयस्क ज्ञान कौशल के अर्जन की परिस्थिति का सामना करता है तो उसकी आन्तरिक दशा में एक अव्यवस्था (Disturbance) होती है। यह अव्यवस्था उसे एक निश्चित एवं धनात्मक दिशा में कार्य करने की ओर भाव-दशा उत्पन्न करे और क्रिया में लगाये, तो वहाँ हम अधिगम में अभिप्रेरण का होना पाते हैं। इस प्रकार आन्तरिक रूप से प्राप्त होता है और मनुष्य अपनी क्रिया में जुटा रहता है और उसे पूरा करके छोड़ता है।
अधिगम में अभिप्रेरण अभिप्रेरकों द्वारा उत्तेजित किया जाता है। ऊपर गणित या विज्ञान के कार्य को पूरा करने में अध्यापक की सहायता, निर्देशन एवं शिक्षण आदि अभिप्रेरक हैं। इसके अलावा कार्य होने पर विद्यालय के विद्यार्थी समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, पारितोषिक, प्रलोभन एवं जीवन में सफलता ये सब भी अभिप्रेरक हैं। ये सब न भी मिले यदि मनुष्य को आन्तरिक सुख, उसकी आकांक्षा की प्राप्ति हो जाय तो वहाँ भी अभिप्रेरक होते हैं। अब साफ-साफ मालूम हो गया होगा कि अधिगम में अभिप्रेरण का तात्पर्य उस आंतरिक भाव दशा से होता है जो विभिन्न अभिप्रेरको के द्वारा उपस्थित या उत्पन्न होती है और जिसके फलस्वरूप मनुष्य ज्ञान – कौशल के अर्जन में अन्त तक जुटा रहता है। इससे ज्ञान, अनुभव एवं कौशल आदि प्राप्त करने की इच्छा सन्तुष्ट होती है और एक आन्तरिक सन्तुलन उपस्थित होता है, ‘स्वान्तः सुख’ होता है, मन की अशान्ति और अव्यवस्था दूर होती है।
बालकों को कैसे अभिप्रेरित किया जाय?
विद्यालय अधिगम के लिए समुचित एवं सुव्यवस्थित संस्था है। यहाँ अध्यापक अधिगम के लिए नियुक्त होते हैं। इसलिए अध्यापक को अधिगम के लिए विद्यार्थी को तैयार एवं तत्पर करना होता है।
इसके लिए अध्यापक निम्नलिखित प्रयत्न करें-
(i) विद्यार्थी को अधिगम के लिए उत्सुक, जागृत और क्रियान्वित करें। उत्सुक और जिज्ञासु बनाने के लिए ऐसे ढंग से सामग्री एवं व्यवहार प्रस्तुत करें कि छात्र उसे ग्रहण करने को तैयार हो जाय
(ii) रोचक कार्यों से बालक की शक्ति को वह संचालित करें।
(iii) बालक को लगातार काम में लगाये रहें। पूरे सत्र के काम को विभिन्न खण्डों में बाँट कर उन्हें पूरा बता दिया जाय और एक-एक खण्ड को पूरा करने के लिए कहा जाय। एक खण्ड पूरा हो जाने पर दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा इस क्रम को लगातार पूरे वर्ष तक कराया जाय।
(iv) तनाव दूर करने की कोशिश करना भी अध्यापक के लिए जरूरी है। तनाव की स्थिति दूर करने में उचित निर्देशन, शिक्षण एवं सहायता देनी चाहिये। अध्यापक आवश्यकतानुसार स्वयं भी बालकों के साथ काम करें।
(v) पुरस्कार और दण्ड का भी प्रयोग अध्यापक करें। इससे भी प्रोत्साहन मिलता है। जो तरीका उचित हो उसी के द्वारा पुरस्कार या दण्ड दिया जाय ।
(vi) अवधान केन्द्रित करने का प्रयास भी अध्यापक करें। इसके लिए उन्हें बालकों की क्षमता, योग्यता, आवश्यकता, रुचि आदि के अनुसार कार्य करना जरूरी है।
(vii) लक्ष्य प्राप्ति में पूरा सहयोग देना अध्यापक की जिम्मेदारी है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक अभिप्रेरण पूरा नहीं होता है।
(viii) अध्यापक कक्षा एवं विद्यालय के पर्यावरण को ऐसे ढंग से आयोजित करे जिससे कि बालक शिक्षा कार्य में लगा रहे। कक्षा की शान्ति, छात्रों में परस्पर सहयोग, कक्षा में आवश्यक सामग्री का होना छात्र की ओर ध्यान रहना, सहानुभूति एवं सहायता, प्रशासकों की अभिवृत्ति बालकों के विकास की ओर होना, सभी साज-सज्जा व सामान की व्यवस्था शीघ्र करना एवं उदार दृष्टिकोण रखना, ये सब शिक्षा के लिए अभिप्रेरित करते हैं। परिचर्या, गोष्ठी, खेलकूद, प्रतियोगिता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, बौद्धिक प्रगति का विवरण, प्रकाशन, सम्भ्रान्त लोगों का आना-जाना अभिप्रेरण के साधन हैं। इन सब दृष्टान्तों से यह सिद्ध होता है कि प्रेरणा सीखने में व्यावहारिक रूप से सहायता करना है।
पुरस्कार और दण्ड द्वारा अभिप्रेरण –
पुरस्कार और दण्ड क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक अभिप्रेरक हैं। पुरस्कार वस्तु-रूप या प्रशंसा-रूप में दिया जाता है, इसके द्वारा व्यक्ति के गुणों को मान्यता मिलती है और उसको आत्म-सम्मान की अनुभूति होती है, आत्म सन्तुष्टि होती है। इस प्रकार आगे भी अच्छे कार्य एवं व्यवहार आदि वह करता है। अतः पुरस्कार व्यवहार के लिए अभिप्रेरक होता है।
दण्ड शारीरिक, आथक या मानसिक पीड़ा है। दण्ड पाकर व्यक्ति को अपने कार्य व्यवहार के लिए दुःखानुभूति होती है, जबकि पुरस्कार ऊँचा उठाता है। इस दृष्टि से दण्ड बुरे व्यवहार को रोकता है, सुधार के लिए प्रयत्न करता है। ऐसी स्थिति में दण्ड भी अच्छे व्यवहार का अभिप्रेरण देता है।
प्रश्न 7 (iv) तनाव (प्रतिबल Stress ) का क्या कार्य है? उचित उदाहरणों की सहायता से तनाव सहन करने की चार युक्तियों/तरीकों का वर्णन करें।
ANSWER—-
प्रतिबल से आशय-मनोवैज्ञानिक रूप से यदि प्रतिबल को देखा जाय तो यह जटिल ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और दैहिक प्रक्रियाओं से पूर्ण दिखायी देता है। इस रूप में प्रतिबल कई बार चिन्ता, अन्तर्द्वन्द्व, संवेग, कुण्ठा तथा उदोलन के समान प्रतीत होती है। वास्तव में प्रतिबल इन सबसे भिन्न अवस्था है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कुण्ठा और अन्तर्द्वन्द्व को प्रतिबल प्रकार के अन्तर्गत रखते हैं।
प्रतिबल के जटिल होने के दो स्तर है
(1) Biological Level जैसे किसी Infection से शारीरिक बीमारी हो और प्रतिबल उत्पन्न हो।
(2) Pesychological Level, जैसे- अपराध भावना मनोवैज्ञानिक प्रतिबल का एक स्रोत है। प्रतिबल व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पर घटित हो सकती है। युद्ध के कारण प्रतिबल की स्थिति व्यक्ति और समाज दोनों में उत्पन्न होती है।
प्रतिबल की परिभाषा –
कोलमैन के अनुसार, “कोई भी परिस्थिति जो व्यक्ति पर दबाव डालती है तथा जिसके कारण व्यक्ति को असमायोजन करना पड़ता है। सही प्रतिबल है । ”
प्रतिबल वह अवस्था है जो व्यक्ति पर इतना प्रभाव डालती है कि उसे समायोजन की आवश्यकता पड़ती है या उसे समायोजन करना पड़ता है। कोलमैन का विचार है कि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रतिबल की अनुपस्थिति में विकसित नहीं होता है। एक व्यक्ति का मानसिगक स्वास्थ्य उस अवस्था में तीव्र गति से विकसित होता है जब वह इन प्रतिबल परिस्थितियों के प्रति सन्तोषजनक ढंग से प्रतिक्रिया करता है।
सेली ने प्रतिबल को केवल एक प्रकार का शारीरिक प्रत्युत्तर माना है। आपके अनुसार प्रतिबल और प्रतिबल उद्दीपक Stressor दो भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं। प्रतिबल उद्दीपक शारीरिक और बाह्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। प्रतिबल में Pituitary Adrenal Involvement तथा Harmonal and Metabolic Processes का अध्ययन अनेक मनोज्ञानिक ने किया है।
काफर तथा एपली ने प्रतिबल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि “Stress is the state of the organism when he perceives that his well being (or intergrity) is endangered and that he must eleveate all of his energies to his protection.”
रोजन और उनके साथियों के अनुसार, “प्रतिबल का अर्थ उन उद्दीपक अवस्थाओं से हैं जो व्यक्तियों से कठिन समायोजन की माँग करती है। प्रतिबल से सम्बन्धित उद्दीपक जैविक, मनोवज्ञानिक, बाह्य, आन्तरिक, हानिकारक और बेचने वाले आदि कुछ भी हो सकते हैं।”
प्रतिबल के प्रकार
1. जैविक प्रतिबल-ऐसे प्रतिबल के अन्तर्गत वे सब कारक सम्मिलित रहते हैं, जिनसे शरीर की कार्यक्षमता पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे- दुर्घटना के कारण शरीर के अंगों का क्षतिग्रस्त होना, व्यक्ति का विकलांग होना, क्षयरोग, कैन्सर, कुष्ठरोग व दमा जैसे भयेंकर रोग से निरन्तर पीड़ित रहना। केवल यही नहीं, बल्कि ऐसे प्रतिबल के अन्तर्गत स्वाभाविक नींद का अभाव, विटामिन न्यूनता, अनेक ऐसे दैनिक व जीव-रासायनिक अभाव भी सम्मिलित हैं जिनमें वचन से शरीर के रोगों के कीटाणुओं के प्रति प्रतिरोधी-शक्ति क्षीण होती है व व्यक्ति के व्यवहार में विभिन्न दोष उत्पन्न होते देखे जाते हैं।
2. मनोवैज्ञानिक प्रतिबल-मनोवैज्ञानिक प्रतिबल के अन्तर्गत वे समस्त प्रबल कुण्ठाएं, कठोर अन्तर्द्वन्द्व तथा तीव्र मानसिक दबाव सम्मिलित रहते हैं, जनिके कारण व्यक्ति के मन में एक निरन्तर ऐसा संवेगात्मक तनाव बना रहता है, जसिके समाधान के प्रति व्यक्ति प्रायः अपने आपको अत्यन्त हताश व निराश अनुभव करता है। इसके अन्तर्गत बाल्यकाल में अपने माता-पिता के प्रेम का अभाव, मित्रों व …सायों के सहयोग का अभाव, जीवन में सुरक्षा भावना का अभाव व व्यक्तित्व की अपर्याप्तता तथा हीनता | जैसी मानसिक बाधाओं व अवरोधों का समावेश रहता है। मनोवज्ञानिक प्रतिबल की अभिव्यक्ति प्रयः व्यक्ति दुश्चिन्ता व मानसिक क्लेश के रूप में होती है। मनोवैज्ञानिक प्रतिबल के भी दो मुख्य रूप होते है|
(क) अहम् सम्बन्धित प्रतिबल – अहम् सम्बन्धित प्रतिबल ऐसे होते हैं, जिनके कारण व्यक्ति का आत्म-सम्मान, आत्म-सुरक्षा व प्रतिष्ठा आदि को धक्का पहुँचने का भय रहता है। इसका स्वरूप व्यक्ति के लिए प्रायः अति गम्भीर होता है, क्योंकि इससे उसकी आत्म- संरचना को भी आघात पहुँचने की आशंका हो जाती है। अतः ऐसे प्रतिबल के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया विशेष मानसिक विक्षोभ व विघटन की होती है।
(ख) अहम्-असम्बन्धित प्रतिबल-व्यक्ति की गम्भीर, प्रतिक्रिया अहम-असम्बन्धित प्रतिबल के प्रति नहीं होती। ऐसे प्रतिबल का दुष्प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक कष्टकारक नहीं होता है
कॉलमैन के अनुसार प्रतिबल की स्थिति से निपटने के मुख्य चरण क्रमशः निम्नलिखित होते हैं-
(1) प्रतिबल स्थिति के प्रति आवश्यक कार्य की रूपरेखा बनाना-इस चरण के अन्तर्गत व्यक्ति को अपने अनुभव, तर्क व विवेक के आधार पर प्रतिबल से निपटने के लिए आवश्यक कार्य की रूपरेखा तैयार करनी होती है। इस प्रक्रम में उसे ऐसे विभिन्न विकल्पों को बी सोचना होता है, जिसके द्वारा प्रतिबल का दुष्प्रभाव कम से कम ही हो सके। इस चरण के अन्तर्गत व्यक्ति को प्रत्येक विकल्प के गुण व दोषों का भी सन्तुलित रूप से आकलन करना होता है। तथा अनावश्यक व जोखिमपूर्ण विकल्प का यथासम्भव परित्याग करना ही श्रेयस्कर होता है
(2) प्रतिबल स्थिति का अंकन -प्रथम चरण में व्यक्ति के लिए प्रतिबल के स्वरूप तथा उसके भयंकरता का अंकन करना होता है। इसके अन्तर्गत व्यक्ति को धैर्य के साथ भावी संकट को एक भारी प्रतिबल तथा एक भयंकर संकट को एक साधार घटना समझने की भूल कर बैठता है। कल्पना से सामान्य संकट भी अति भयावह लगता है, अतः व्यक्ति को अपनी अतीत के अनुभवों के सन्दर्भ में ऐसी स्थिति का वस्तुपक आधार पर अंकन करना आवश्यक होता है।
( 3 ) प्रतिबल के प्रति आवश्यक कार्यवाही करना-इस चरण के अन्तर्गत सुविचारित विकल्प को कार्यरूप देकर प्रतिबल का सामना करने के लिए आगे बढ़ना होता है तथा इस प्रक्रम में व्यक्ति का अतीत के अनुभव के आधार पर अथवा प्रतिपुष्टि से समय-समय पर अपने विकल्प के प्रभावी रूप का अंकन करना होता है। प्रतिपुष्टि से यहाँ अभिप्राय पीछे किये गये कार्य के फल के सन्दर्भ में आगे के कार्य में आवश्यक संशोधन लाना होता है।
प्रतिबल के प्रति कार्यवाही के रूप-
प्रतिबल के प्रति व्यक्ति की कार्यवाही के मुख्यतः तीन रूप होते हैं-
(1) प्रतिबल स्थिति के प्रति विमुख हो जाना-यदि व्यक्ति सम्बन्धित प्रतिबल स्थिति का सामना करने में अपने आप को असमर्थ पाने का अनुभव करता है, तब उसके लिए ऐसे संघर्ष से हट जाना ही प्रायः अधिक हितकर होता है। यहाँ व्यक्ति का असाध्य संघर्ष से हटना प्रकृति के नियम- मुकाबला करो या फिर भाग जाओं के अनुकूल ही है।
(2) प्रतिबल की स्थिति के साथ मेल-मिलाप करना-यदि व्यक्ति प्रतिबल स्थिति पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता, तब उसके लिए एक ही अति उपयोगी विकल्प ऐसी स्थिति के साथ मेल-मिलाप कर लेना भी अधिक श्रेयस्कर रहता है। इस विकल्प के अंतर्गत व्यक्ति को अपने अकांक्षास्तर, सामाजिक व नैतिक स्तर तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में आवश्यक परिवर्तन करना होता है तथा परिस्थितियों की कटुता व प्रतिबल की कठोरता के साथ ताल-मेल बिठाना पड़ता है।
(3) प्रतिबल स्थिति के प्रत्यक्षतः सम्मुख होना-इस विकल्प के अन्तर्गत व्यक्ति सम्बन्धित प्रतिबल का अंटकर सामना करता है। इस प्रक्रम में अपने शारीरिक व मानसिक संसाधनों अपनी शक्ति व साहस को पूरी तरह से ऐसे मुकाबले के लिए सुसंगठित करता है |
इकाई – IV
प्रश्न 8 (i) व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? इसके मापन की किसी एक प्रक्षेपण विधि का वर्णन कीजिए।
अथवा
व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
अथवा
व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियाँ कौन-कौन सी हैं? उनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन कीजिए।
अथवा
व्यक्तित्व को परिभाषित करें। व्यक्तित्व मापन की किन्हीं दो विधियों की विस्तार से चर्चा कीजिए।
अथवा
व्यक्तित्व के सम्प्रत्यय को समझाइए। इसके मापन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।
अथवा
व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व के आकलन की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए।
ANSWER–
व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा —
व्यक्तित्व के स्वरूप के बारे में अनेक धारणाएँ हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में ‘व्यक्तित्व’ शब्द का प्रयोग शरीर की बनावट तथा सौन्दर्य के लिए किया जाता है। कुछ लोग ‘व्यक्ति व व्यक्तित्व’ को पर्यायवाची मानते हैं। कुछ लोग ‘व्यक्तित्व’ में केवल एक या दो गुणों का संगठन मानते हैं तो कुछ अनिश्चित गुणों व लक्षणों का संग्रह मानते हैं। जिस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों की व्यक्तित्व के विषय में विभिन्न धारणाएँ है उसी प्रकार विभिन्न विद्वानों व मनोवैज्ञानिकों में भी व्यक्तित्व के स्वरूप के सम्बन्ध में मतभेद है। सामान्यतः यह माना जाता है कि व्यक्तित्व विचित्र है, जटिल है, व्याख्या से परे है। व्यक्तित्व के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए जरूरी है कि इसके अर्थ व परिभाषाओं का अध्ययन किया जाये।
व्यक्तित्व अंग्रेजी के ‘Personality’ शब्द का रूपान्तर है। ‘पर्सनैलिटी’ शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ‘परसोना’ शब्द से हुई है जिसका तात्पर्य है — “नकाब या नकली चेहरा अर्थात् वह वेश-भूषा जिसे नाटक करते समय अभिनेता लोग पहनते हैं।” अगर शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाय तो ‘व्यक्तित्व का अर्थ-व्यक्ति के बाह्य गुणों का संगठन है।
‘व्यक्तित्व’ एक ऐसा शब्द है जिसके लिए मापन शब्द का प्रयोग सही नहीं है क्योंकि ‘विकास’ को मापा नहीं जा सकता उसका तो केवल मूल्यांकन ही किया जा सकता है। इसलिए व्यक्तित्व के विकास का भी मूल्यांकन ही सम्भव है। व्यक्तित्व मापन की कोई इकाई नहीं है। व्यक्तित्व के विकास के शारीरिक पक्ष या कुछ भार आदि का मापन किया जा सकता है लेकिन इससे सम्पूर्ण व्यक्तित्व का मापन नहीं किया जा सकता। व्यक्तित्व के मूल्यांकन में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है-
(अ) व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ –
ये विधियाँ निम्नलिखित हैं-
(1 ) साक्षात्कार विधि – एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ आमने-सामने होने वाली बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। यह व्यक्तिनिष्ठ विधि है।
साक्षात्कार विधि के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछता है। उन प्रश्नों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। आमने-सामने होने वाले इस वार्त्तालाप से व्यक्ति
की रुचियों, इच्छाओं व आशाओं का पता चल जाता है।
साक्षात्कार विधि का सबसे प्रमुख दोष है कि समय का अधिक प्रयोग कई बार व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर भी सही ढंग से नहीं दे पाता।
( 2 ) आत्मकथा-यह व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपनी जीवन-कथा लिखता है व दूसरे व्यक्ति उस आत्म-कथा लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। आत्मकथा में लेखक भूतकाल का अधिक वर्णन करते हैं। व्यक्ति आत्मकथा में अपने अनुभवों, रुचियों, इच्छाओं व लक्ष्यों का अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन करता है। इसमें कुछ भी हैं जैसे-
आत्मकथा में व्यक्ति असत्य बातें लिख देता है तथा अधूरी बातें भी लिख देता है। व्यक्ति अपने गुणों का बहुत बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन करता है।
( 3 ) व्यक्ति वृत्त विधि – इस विधि में व्यक्ति की पिछली जिन्दगी के तथ्यों को रिकार्ड करते हैं। इस विधि के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी तथ्यों को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करते हैं। यह एक प्रकार से व्यक्ति व व्यक्तित्व का पूर्ण इतिहास होता है। इस विधि द्वारा ज्यादातर समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जा सकता है।
इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि व्यक्ति से सम्बन्धित सामग्री को इकट्ठा करना तथा उसका रिकार्ड तैयार करना होता है। इस कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है। व्यक्ति-वृत्त विधि में व्यक्ति के व्यक्तित्व से सम्बन्धित सूचनाओं को दर्ज करने के लिए स्पष्टता व ईमानदारी का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक है।
( 4 ) प्रश्नावली विधि – इस विधि के माध्यम से कुछ प्रश्नों की एक सूची बना ली जाती है। इस सूची को व्यक्तियों में बाँटकर उनसे प्रश्नों के उत्तर माँगे जाते हैं। फिर उन उत्तरों का विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लिया जाता है। ये प्रश्न व्यक्तित्व के उसी पक्ष से सम्बन्धित होते हैं जिसका मूल्यांकन करना होता है। प्रश्नों की यह सूची एक समय में एक ही व्यक्ति को अथवा व्यक्तियों के समूह को दी जा सकती है। (ब)
वस्तुनिष्ठ विधियाँ
ये विधियाँ व्यक्ति के बाहरी व्यवहार से जुड़ी होती हैं। ये विधियाँ अधिक वैज्ञानिक व विश्वसनीय कही जाती हैं। प्रमुख विधियाँ हैं—
(1 ) निरीक्षण विधि-निरीक्षण द्वारा भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन यह लगातार चलनेवाली प्रतिक्रिया होती है। थोड़े समय के निरीक्षण से व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं हो सकता। यह
निरीक्षण भी दो प्रकार का होता है-
(a) नियन्त्रित निरीक्षण,
(b) अनियन्त्रित निरीक्षण।
(a) नियन्त्रित निरीक्षण-इस प्रकार के निरीक्षण के अन्तर्गत परिस्थितियों को नियन्त्रण में रख कर व्यक्ति का निरीक्षण किया जाता है और उस व्यक्ति को इस निरीक्षण के बारे में ज्ञात होता है।
(b) अनियन्त्रित निरीक्षण-इस प्रकार के निरीक्षण में व्यक्ति का गुप्त रूप से निरीक्षण किया जाता है और उसे इस सम्बन्ध में बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया जाता कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है। इस प्रकार के निरीक्षण से व्यक्ति का व्यक्तित्व प्राकृतिक रूप से खुल कर सामने आता है।
( 2 ) समाजमिति विधि-इस विधि द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है या व्यक्ति के सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। सर्वप्रथम इस विधि को जे० एल० मोरिनो ने जन्म दिया। इस विधि में बालकों से उनकी रुचियाँ जानी जाती हैं। इन तथ्यों के आधार पर सोशियोग्राम खींचा जाता है। इस सोशियोग्राम का विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन होता है।
लिए अन्य व्यक्तियों का मत एकत्रित किया जाता है। इस मानदण्ड मूल्यांकन विधि में प्रत्येक गुण
( 3 ) मानदण्ड मूल्यांकन विधि-इस विधि द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के को मूल्यांकित करने के लिए तैयार किये गये प्रश्नों के कथनों के उत्तरों को पाँच अथवा सात कोटियों में विभाजित कर दिया जाता है। इन पाँच या सात कोटियों पर सबसे किसी एक कोटि पर मत व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। सबसे अधिक मतों का तात्पर्य है इस व्यक्ति में उस कोटि का गुण होना।
( 4 ) व्यक्तित्व परिसूची – यह विधि प्रश्नावली विधि से मिलती-जुलती है। इस विधि में प्रश्न केवल व्यक्ति विशेष से ही सम्बन्धित होते हैं। प्रश्नावली विधि में व्यक्ति के अलावा अन्य सूचनायें भी एकत्र की जाती हैं। व्यक्तित्व परिसूची में प्रश्न उत्तम पुरुष को सम्बन्धित किये जाते हैं, यथा-म देशाटन को पसन्द करता हूँ।
इस विधि के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना कठिन होता है। कई बार प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त नहीं किये जा सकते। व्यक्ति अपने दोषों, कमियों व अवगुणों को छुपा लेते हैं। अतः यह विधि भी सम्पूर्ण नहीं कही जा सकती।
( 5 ) परिस्थिति परीक्षण-परिस्थिति परीक्षणों के अन्तर्गत व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उसकी विशेषताओं का मूल्यांकन किया जाता है। इस परीक्षण में वास्तविक परिस्थिति परीक्षण तैयार किये जाते हैं। यथा-बालकों को ईमानदारी की परीक्षा करनी हो तो ऐसी परिस्थिति पैदा की जानी चाहिए जिससे उसमें ईमानदारी के गुण का मूल्यांकन किया जा सके।
(स) प्रक्षेपण विधियाँ —
मनुष्य के मूल्यांकन करने की सभी विधियों में यह सर्वाधिक विश्वसनीय तथा वैध विधि है। फ्रेंक के अनुसार, “प्रक्षेपण द्वारा हमें यह मालूम होता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को किस प्रकार समझाता है। इन विधियों द्वारा उन व्यक्तियों को आन्तरिक या प्राइवेट जीवन का अभ्यास मिलता है।”
इस विधि के माध्यम से अचेतन व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि अन्य विधियाँ केवल चेतन व्यवहार का ही अध्ययन करती हैं। प्रक्षेपण विधियों की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
(1) रचनाहीन सामग्री-इन विधियों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री रचनाहीन सामग्री होती है। इनकी कोई विशेष आकृति नहीं बनती।
(2) सम्पूर्ण व्यक्तित्व- इन विधियों के माध्यम से सम्पूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। अन्य विधियों के माध्यम से ऐसा सम्भव नहीं होता। वे व्यक्ति के व्यक्तित्व के अलग गुणों का अध्ययन करती हैं।
(3) अचेतन व्यवहार से सम्बन्धित – इन विधियों के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
(4) मानसिक रोगों का अध्ययन-इन विधियों के माध्यम से मानसिक रोगों का अध्ययन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था में भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है।
प्रक्षेपण की दो प्रमुख विधियाँ प्रचलित हैं-
(अ) रोर्शा का स्याही-धब्बा परीक्षण- इस परीक्षण की रचना स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोर्शा ने सन् 1921 में की थी। यह परीक्षण सबसे अधिक सफल परीक्षण माना जाता है। यह परीक्षण निम्न प्रकार से किया जाता है—
(i) परीक्षण सामग्री-इस परीक्षण में दस कार्ड होते हैं। इन कार्डों पर रचनाहीन स्याही के धब्बों जैसी आकृतियाँ बनी होती हैं। इन दस कार्डों में से पाँच कार्डों पर बिल्कुल काली आकृतियाँ, दो कार्डों पर काली तथा लाल आकृतियाँ तथा शेष तीन कार्डों पर भिन्न-भिन्न आकृतियाँ होती हैं। सभी दस कार्डों की आकृतियाँ कोई विशेष अर्थ नहीं रखतीं।
(ii) परीक्षण का आयोजन- जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना होता है, उस व्यक्ति को ये दस कार्ड एक-एक करके दिये जाते हैं व उस कार्ड पर तथा छपी आकृति के बारे में उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया को नोट किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि उस कार्ड की आकृति उन्हें किस प्रकार की लगती है या उन्हें उस आकृति में क्या दिखाई दे रहा है। प्रत्येक कार्ड को देखने के लिए व्यक्ति जितना समय चाहता है, उसे उतना ही समय दिया जाता है। इस कार्ड को वह व्यक्ति किसी भी कोण से देख सकता है, एक ही कोण से देखने का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।
इन आकृतियों को देखकर मनुष्य की प्रतिक्रियाओं, उसके कार्डों को पकड़ने का ढंग तथा चेहरे के भावों का लेखा-जोखा रखा जाता है।
(iii) अनुक्रियाओं का विश्लेषण-परीक्षण के माध्यम से व्यक्तियों से प्राप्त अनुक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण के लिए अनुक्रियाओं का अंकन किया जाता है। इन अनुक्रियाओं के अंकन के लिए निम्नलिखित चार बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाता है-
(a) स्थिति-इस बिन्दु को उस सन्दर्भ में देखा जाता है कि व्यक्ति कार्ड पर छपी आकृति के किस भाग को अपनी प्रतिक्रिया का भाग बनाता है। क्या वह सारी आकृति के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया बता रहा है या उस आकृति के किसी एक भाग को देखकर। अगर व्यक्ति ने कार्ड की सम्पूर्ण आकृति को देखकर उत्तर दिया है तो उस प्रतिक्रिया को (W) शब्द द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि वह किसी आकृति को बढ़ा-चढ़ाकर कहता है तो उसे (D) शब्द द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। छोटी-छोटी बातों को गहराई से देखने पर (d) शब्द का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अगर व्यक्ति खाली स्थानों के बारे में प्रतिक्रिया बताता है तो उसे (S) शब्द के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है।
(b) विषय-वस्तु – इसमें मनुष्य कार्डों पर छपी आकृतियों में क्या कुछ देखता है, उसे नोट किया जाता है। यथा – व्यक्ति की आकृति, पशुओं की आकृति, वस्तुओं की या प्राकृतिक दृश्यों की आकृति । मानव की आकृति को देखने पर H, पशुओं की आकृति को देखने पर A, प्राकृतिक दृश्यों के लिए N. अन्य वस्तुओं जैसे- बर्तन, छतरी आदि के लिए आदि शब्दों का प्रयोग होता है
(c) निर्धारक तत्त्व-कार्डों पर छपी आकृतियों के प्रत्यक्षीकरण के लिए मनुष्यों को जिन कारणों ने सहायता पहुँचाई, उन्हें निर्धारक तत्त्व कहते हैं। जैसे-यदि आकृति ने ही उसे प्रतिक्रिया के लिए प्रोत्साहित किया हो तो F, उसके रंग को C, गति को M व रंगों के उतार-चढ़ाव को K अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है।
(d) मौलिकता-पहले से घोषित अथवा प्रचलित अनुक्रियाओं को व्यक्त करने पर P का अक्षर तथा मौलिक अनुक्रियाओं को 0 अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है।
(iv) परीक्षण की सत्यता व विश्वसनीयता- इस परीक्षण की विश्वसनीयता 67 से 97 तक है तथा सत्यता 49 मालूम की गई है।
(v) उपयोगिता-रोर्शा टेस्ट के परीक्षण की उपयोगिता निम्न प्रकार है-
(a) यह परीक्षण जटिल असामाजिक कार्यों के कारणों को जानने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। (b) इस परीक्षण से हमें व्यक्ति के संवेगात्मक, मानसिक व सामाजिक पक्षों के बारे में अधिक पता चलता है। (c) इससे व्यक्ति की बुद्धि का भी पता चलता है।
(vi) आलोचना-
(a) यह विधि छोटे बच्चों के लिए सही नहीं है।
(b) इस परीक्षण के संचालन के लिए कुशल व्यक्तियों की जरूरत होती है। सभी लोग इनका संचालन नहीं कर पाते।
(c) इसमें अधिक समय तथा धन की जरूरत होती है।
(d) इस परीक्षण में वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है।
(ब) थिमैटिक अन्तर्बोध परीक्षण- इस परीक्षण के जन्मदाता मारगन व मूरे थे। उन्होंने परीक्षण का निर्माण सन् 1925 में किया था। यह परीक्षण निम्न प्रकार किया जाता है-
(i) परीक्षण सामग्री- इस परीक्षण में भी तीस (30) चित्र होते हैं। इन चित्रों में से दस चित्र पुरुषों के, दस चित्र स्त्रियों के व दस दोनों के लिए होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 20 चित्र दिखाये जाते हैं। ये कार्ड दो बार में दिखाये जाते हैं।
(ii) परीक्षा लेने का ढंग-इस परीक्षण में चित्रों को एक-एक करके प्रस्तुत किया जाता है। ये चित्र अस्पष्ट होते हैं। इस परीक्षण में कोई उत्तर सही अथवा गलत नहीं होता। केवल मानव की मौलिक कल्पना को ही देखा जाता है। व्यक्ति को निश्चित समय में प्रत्येक कार्ड को देखकर कोई कहानी लिखनी होती है। चित्र की कहानी निम्न पक्षों को लेकर लिखी जाती है-
(a) चित्र में क्या हो रहा है?
(b) इसके क्या कारण हो सकते हैं?
(c) इसके परिणाम क्या हो सकते हैं?
इन कहानियों को लिखने से मनुष्य अपनी भावनाएँ, आकांक्षाएँ आदि इन कहानियों के द्वारा प्रदर्शित कर सकता है। अतः दूसरों के समक्ष स्वयं को प्रदर्शित करने में असमर्थ मनुष्य इन कहानियों के द्वारा स्वयं को प्रदर्शित कर देता है।
(iii) विश्लेषण तथा व्याख्या-इन कहानियों का विश्लेषण निम्न बातों के आधार पर होता है-
(a) कहानी के नायक का व्यक्तित्व क्या है?
(b) कहानी का कथानक ।
(c) कहानी की भाषा तथा शैली
(d) कहानी की विषय-वस्तु ।
(e) कहानी लिखते समय व्यक्ति का व्यवहार।
(f) कहानी का अन्त।
(iv) आलोचना – इस विधि में अयोग्य परीक्षक कई बार चित्रों को देखकर लिखी कहानियों का गलत अर्थ भी मान लेते हैं। इसका प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व की सम्पूर्ण व्याख्या पर पड़ता है। दूसरा इस परीक्षण के संचालन के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत होती है। यह परीक्षण बड़ों के लिए उपयुक्त है लेकिन बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होता है।
प्रश्न 8 (ii) व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व के ‘प्रकार सिद्धान्त’ की व्याख्या कीजिए।
अथवा
व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धान्तों का विवेचन कीजिए।
ANSWER-
व्यक्तित्व का अर्थ शारीरिक सौन्दर्य या अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। व्यक्तित्व के अन्दर बहुत गुण सम्मिलित होते हैं जो मानवीय गुण होते हैं अर्थात् यह मानवीय व्यवहार का प्रतिमान है जो कि परिस्थिति-विशेष प्रत्युत्तर में प्रयोग किये जाते हैं। व्यक्तित्व लैटिन भाषा के ‘पर्सनेअर’ शब्द से बना है जिसका अर्थ है ‘ध्वनि करने के सदृश्य’। यह एक पात्र की आवाज को व्यक्त करता है। ध्वनि को हम सुन सकते हैं पर देख या छू नहीं सकते। व्यक्तित्व को हम केवल समझ सकते हैं। यह गतिशील है और इसकी गति समाज में देखी जा सकती है। वैलेन्टाइन के अनुसार, “व्यक्तित्त्व दूसरे के समझने का दृष्टिकोण है।”
व्यक्तित्व की परिभाषाएँ
डेशील के अनुसार “व्यक्ति का व्यक्तित्व सम्पूर्ण रूप से उसकी प्रतिक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की आवश्यकताओं की उस ढंग की व्यवस्था है जिससे वह सामाजिक प्राणियों द्वारा आंकी जाती है। यह व्यक्ति के व्यवहारों का एक समायोजित संकलन है जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्थापन के लिए करता है।” यह परिभाषा व्यक्तित्व के सभी पक्षों पर प्रकाश डालती है। मानव व्यक्तित्व तभी पूर्णतः समझा जा सकता है, जब व्यक्ति अन्य प्राणियों के सम्पर्क में आकर प्रतिक्रियायें और प्रत्युत्तर करता है।
वारेन के अनुसार “व्यक्तित्व व्यक्ति का सम्पूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। ”
यह परिभाषा मानसिक एवं शारीरिक संगठन को एक-दूसरे से अलग कर देती है।
गार्डेन आलपोर्ट के अनुसार “व्यक्तित्व व्यक्ति के साथ उन मनो-शारीरिक संस्थान का गतिशील संगठन है जो वातावरण में उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं।”
व्यक्तित्व के सिद्धान्त
व्यक्तित्व के अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिकों ने किया है। सिद्धान्तों की भिन्नता का आधार व्यक्तित्व के सम्बन्ध में बनाई गई आधारभूत मान्यताओं का अन्तर है। व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-
(1) शरीर रचना सम्बन्धी सिद्धान्त,
(2) मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त,
(3) विशेषक सिद्धान्त,
(4) माँग सिद्धान्त।
शरीर रचना सम्बन्धी सिद्धान्त-कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के रूप, रंग, आकार तथा शरीर के गठन के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या तथा वर्गीकरण किया है। इस सिद्धान्त की पृष्ठभूमि जीवविज्ञान से प्रभावित है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक शैलडन महोदय थे। उन्होंने शरीर रचना एवं व्यक्तित्व के बीच सम्बन्ध स्थापित किए और पाया कि दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है-
(1) गोलाकृति शरीर वाले लोगों का व्यक्तित्व Visceretona प्रकार का कहलाता है। ये लोग भोजनप्रिय, आरामपसन्द, शौकीनमिजाज, परम्परावादी, सहनशील और सामाजिक प्रकृति के होते हैं।
(2) आयताकृति शरीर वाले लोग Somatotonia प्रकार के व्यक्तित्व वाले कहलाते हैं। ये रोमांचप्रिय, प्रभुत्ववादी, जोशीले, क्रोधित होने वाले और उद्देश्य केन्द्रित होते हैं।
(3) लम्बाकृति रचना वाले लोगों का व्यक्तित्व Cereprotonia प्रकार का कहलाता है। ये लोग एकान्तप्रिय, गुमसुम, जल्दी थकने वाले, अल्प निद्रा वाले तथा असामाजिक होते हैं।
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त – इस सिद्धान्त के प्रवर्तक फ्रायड थे। उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में अपना अनूठा व्यापक सिद्धान्त दिया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त के प्रतिपादन में अचेतन, इदं, अहं तथा अत्यहं आदि प्रत्ययों को आधार माना गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार पानी में तैरते हुए बर्फ का केवल 1/9 भाग ऊपर रहता है और बाकी 8/9 भाग पानी में डूबा रहता है उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क का 1/9 भाग चेतन अवस्था और बाकी भाग अचेतन अवस्था में रहता है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य का अचेतन मन अधिक महत्त्वपूर्ण एवं जटिल होता है। इनके अनुसार अचेतन अनेक अनजानी परन्तु शक्तिशाली व जीवन्त शक्तियों का संचय होता है जो व्यक्ति के चैतन व्यवहार पर नियन्त्रण रखता है।
फ्रायड के अनुसार यदि ये तीनों घटक एक सुसंगठित एवं समरस इकाई के रूप में कार्य करें तो व्यक्ति का समायोजन उसके वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से होता है। ऐसे लोगों का समायोजन ठीक प्रकार से होता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति में इन तीन घटकों के बीच उचित समायोजन नहीं होता है तो व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन करने में असफल रहता है। इस प्रकार फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व वास्तव में इदं, अहं एवं अत्यहं के बीच परस्पर समायोजना का परिणाम है।
विशेषक सिद्धान्त-व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धान्त का प्रतिपादन कैटिल ने किया है। उसने व्यक्तियों के गुण एवं विशेषताओं आदि का सांख्यिकीय विधि से कारक विश्लेषण किया तथा कुछ सामान्य गुणों को ज्ञात किया जिसे व्यक्तित्व विशेषक कहते हैं। संवेगात्मक स्थिरता, बुद्धि सामाजिकता आदि कुछ कारक कैटिल ने सुझाये हैं।
कोई भी व्यक्ति किसी दी गई परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा ? यह ज्ञात करने के लिए जिस आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है वही कैटिल के अनुसार व्यक्तित्व है। कैटिल के अनुसार व्यक्तित्व विशेषक एक मानसिक संरचना है तथा इसे व्यक्तित्व की व्यवहार प्रक्रिया की निरन्तरता तथा नियमितता से जाना जा सकता है। इसके अनुसार कुछ सामान्य विशेषक तथा कुछ विशिष्ट विशेषक होते हैं। सामान्य विशेषक वह विशेषक है जो सभी व्यक्तियों में पाये जाते हैं तथा उनकी मात्रा किसी में कम और किसी में अधिक होती है। विशिष्ट विशेषक विशेष प्रकार के लोगों में पाये जाते हैं और इन्हीं के कारण व्यक्तियों की विशिष्टता होती है।
माँग सिद्धान्त – इस सिद्धान्त का प्रतिपादन मुरे ने किया है। इस सिद्धान्त की मान्यता है कि मनुष्य अपनी अन्तर्निहित आवश्यकताओं तथा बाहरी दबावों के कारण उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। माँग दबाव की परिस्थिति हमेशा व्यक्ति में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न करती रहती है। फलतः व्यक्ति नये-नये कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तथा वह अपने पुराने उद्देश्यों को भी बनाये रखता है। मुरे के अनुसार, व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के दबावों को समग्र रूप उसके अन्दर कुछ माँगों को उत्पन्न करता है और ये माँगें ही व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। मुरे ने इन माँगों को व्यक्तित्व माँग का नाम दिया। उन्होंने लगभग चालीस इस प्रकार की माँगों का पता लगाया। मुरे के अनुसार, कोई माँग मानव मस्तिष्क की एक परिकल्पित शक्ति है जो व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण, अन्तर्बोध तथा मानसिक-शारीरिक क्रियाओं को इस प्रकार संगठित करती है कि वह व्यक्ति असन्तुष्टि की परिस्थिति से निकल सके। मुरे द्वारा बताई गई माँगों में कुछ माँगें इस प्रकार हैं जैसे, प्रदर्शन की माँग, सानिध्य की माँग, परोपकार की माँग, स्वायत्तता की माँग, संप्राप्ति की माँग आदि।
प्रश्न 9 (i) सृजनशीलता अथवा सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। सृजनात्मकता के तत्त्व अथवा आयाम की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
अथवा
सृजनशीलता किसे कहते हैं? इसकी पहचान कैसे की जाती है? सृजनशीलता के संवर्द्धन हेतु प्रयुक्त किन्हीं दो उपागमों का वर्णन कीजिए।
अथवा
विशेष कोटि के बालक किसे कहते हैं? सृजनशील एवं प्रतिभाशाली बालकों के मध्य विभेद कीजिए। सृजनशील बालकों की शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार नियोजित की जानी चाहिये?
अथवा
सृजनात्मकता को परिभाषित करें। अपनी कक्षा में बालकों की सृजनात्मकता को आप किस प्रकार से बढ़ावा देंगे?
अथवा
विशिष्ट बालक से क्या आशय है? सृजनशील एवं प्रतिभाशाली बालक के मध्य विभेद कीजिए। बालकों की सृजनशीलता के संवर्द्धन के लिए किन तकनीकियों का प्रयोग किया जा सकता है?
ANSWER-
विशिष्ट बालक –
जो बालक अपनी आयु समूह के मानदण्डों के अनुसार, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक और संवेगात्मक तथा अन्य किसी क्षमता में कम या अधिक होता है या सामान्य व्यक्ति से भिन्न प्रकार की क्षमताएँ रखता है उसे विशिष्ट या असाधारण कहा जाता है।
क्रो एण्ड क्रो के अनुसार, “विशिष्ट या असाधारण शब्द ऐसे गुणों या ऐसे गुणों वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है जो कि सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उन्हीं गुणों से इस सीमा तक भिन्न होते हैं कि व्यक्ति विशेष की ओर उसके साथियों को ध्यान देना पड़ता है, इसके कारण ही उनकी व्यावहारिक प्रतिक्रियाएँ तथा कार्य प्रभावित होते हैं।”
सृजनात्मकता का अर्थ
सृजनात्मकता कुछ नया निर्माण करने, नया ढूँढ़ने या रचना करने की योग्यता है। जो से निर्मित है उसमें बदलाव करने की योग्यता भी सृजनात्मकता में शामिल है।
यह प्रक्रिया अथवा सामान्य कार्य को किसी अलग अथवा नवीन तरीके से करने की प्रविधि सृजनात्मकता कहलाती है।
यद्यपि सृजनात्मकता कलाकारों, जैसे-कवि, लेखक, चित्रकार, अभिनेता, विद्वान आदि के जीवन में अधिक व्यापक रूप से विद्यमान रहती है, परन्तु यह कहना भी अतिशयोक्ति न होगी कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में सृजनात्मकता प्रदर्शित करता है। यह मानव प्रकृति में विद्यमान सार्वभौम प्रवृत्ति है। यदि वातावरण इस गुण के विकास के अनुकूल हो तो व्यक्ति की क्षमता का मौलिक विकास होता है।
सृजनात्मकता का आधार है चिन्तन । व्यक्ति कैसा एवं कितना चिन्तन करता है, यह उसकी सृजनशीलता को निर्धारित करता है। यदि व्यक्ति सामान्य प्रकार का चिन्तन अर्थात् अभिसारी चिन्तन करता है अर्थात् सामान्य तरीके से किसी बात पर विचार करता है तो उसे सृजनशीलता नहीं माना जा सकता। जब व्यक्ति चिन्तन की अपसारी प्रविधि अपनाता है अर्थात् किसी बात पर सामान्य से भिन्न तरीके अथवा विधि द्वारा विचार करता है तो परिणाम सृजनात्मकता के रूप में दिखाई देता है।
शिक्षा में सृजनात्मकता एक महत्वपूर्ण तत्व है। शिक्षा प्रक्रिया में ऐसे अवसर कक्षागत परिस्थितियों के छात्रों को दिये जायें, जिनमें उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता मिले।
यद्यपि सृजनात्मकता अपसारी चिन्तन की योग्यता पर आधारित है परन्तु मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि बुद्धि, ज्ञान व अभिप्रेरणा जैसे घटक भी सृजनात्मकता से जुड़े हुए हैं।
सृजनात्मकता के लिए एक निश्चित स्तर की बुद्धि-लब्धि (औसत) आवश्यक है।
गहन ज्ञान के बिना सृजनशील बनना सम्भव नहीं है।
उच्च अभिप्रेरणा मौलिक अथवा सृजनात्मकता कार्य के लिए आवश्यक शर्त है।
स्टेगनर एवं कार्बोसकी के अनुसार “किसी वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है।”
बी. एफ. स्किनर के अनुसार “सृजनात्मक चिंतन का अर्थ है कि व्यक्ति की भविष्यवाणियाँ या निष्कर्ष नवीन, मौलिक, अन्वेषणात्मक तथा असाधारण हों। सृजनात्मक चिंतक वह है जो नये क्षेत्र की खोज करता है, नये निरीक्षण करता है, नई भविष्यवाणियाँ करता है और नये निष्कर्ष निकालता है।”
सृजनात्मकता की परिभाषाएँ
सृजनात्मकता अथवा सृजनशीलता के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ दी हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है
कोल और ब्रूस के अनुसार- “सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है।”
डीहान तथा हेविंगहर्स्ट के अनुसार- “सृजनात्मकता वह विशेषता है, जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे। यह नवीन वस्तु सम्पूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है, जिसने उसे प्रस्तुत किया है।”
ड्रैवहल के अनुसार—“सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है, जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है।”
क्रो व क्रो—“सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है।”
टोरेन्स के अनुसार- “रचनात्मकता समस्याओं, कठिनाइयों, ज्ञान में अन्तराल, खोये हुए तत्व, अव्यवस्था आदि, कठिनाई की पहचान करना, हलों की खोज करना, अनुमान करना या कमियों के लिए परिकल्पनाएँ बनाना, इन परिकल्पनाओं का परीक्षण और पुनर्परीक्षण करना और सम्भवतः उन्हें सुधारना और परीक्षण करना और अन्त में परिणामों को देने की प्रक्रिया है।”
विशेष कोटि के बालक
विशिष्ट बालक की आम अवधारणा यह है कि वह सामान्य होते हुए भी प्रायः असामान्य गुणों से युक्त होता है। वैयक्तिक भिन्नता ही विशिष्टता का आधार है। मनोवैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि कोई भी दो बालक एक-दूसरे से भिन्न होते हैं, उनमें समानता के साथ-साथ कुछ भिन्नतायें होती हैं जो उन्हें अन्यों से अलग करती हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि 10-10% बालकों को समूह में औसत से भिन्न माना जाता है। एक बालक शारीरिक रूप से समान होने पर भी मानसिक रूप से भिन्न हो सकता है। यह भिन्नता अन्तः वैयक्तिक होती है।
अतएव कहा जा सकता है- “विशिष्ट बालक वह है जो अन्तःवैयक्तिक भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से अन्तर-व्यक्तिगत भिन्नता रखता है।” इसी बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है – “विशिष्ट बालक वह है जो उन बालकों से जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक गुणों में औसत हैं, भिन्न हैं।”
सृजनशील एवं प्रतिभाशाली बालकों के मध्य अन्तर
सृजनशील व्यक्ति –
(i) सृजनशील व्यक्ति में समस्याओं को संवेदन करने की क्षमता होती है।
(ii) सृजनात्मक व्यक्ति में कौतूहल होता है। वह विचारों को काम में लाता रहता है। उनमें एक उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की लग्न होती है जो उनको लगातार उस ओर प्रयास करने में व्यस्त रहती है।
(iii) सृजनशील व्यक्ति में स्वतन्त्र विचार, खतरा उठाने की अधिक प्रवृति, अधिक उद्योगशील एवं अधिक साहसी अधिक बहिर्मुखी एवं दूसरों की तुलना में अधिक जटिल ।
प्रतिभाशाली बालक –
(i) ये शारीरिक गुणों में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं।
(ii) पढ़ने लिखने में इनकी रुचि अधिक होती है।
(iii) इनकी ज्ञानेन्द्रियों का विकास शीघ्र होता है।
(iv) इनमें मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता दिखाई देती है। इनमें अवधान, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, विचार, तर्क तथा निर्णय शक्ति अधिक तीव्र होती है।
सृजनात्मकता के आयाम या उपागम –
सृजनात्मकता अपसारी चिन्तन की प्रक्रिया है। अपसारी चिन्तन अर्थात् सामान्य से अलग हटकर सोचना। इसलिए यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। सृजनात्मकता को मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन, नवीनता, खोजपरकता आदि के सन्दर्भ में समझा जा सकता है। सृजनात्मकता के सर्वमान्य चार महत्वपूर्ण आयाम अग्रलिखित हैं-
(1) प्रवाह-प्रवाह से तात्पर्य किसी उद्दीपक के प्रति अधिकाधिक विचारों या प्रत्युत्तरों को प्रस्तुत करने से है। जितनी अधिक प्रत्युत्तरों की संख्या होती है, व्यक्ति उतना ही अधिक सृजनशील माना जाता है। उदाहरण के लिए किसी कहानी के अनेकानेक शीर्षक बताना, किसी वस्तु के अनेकानेक उपयोग बताना, शब्दों से वाक्य बनाना, दिये गये अपूर्ण वाक्य को पूरा करना आदि।
(2) विविधता-विविधता से तात्पर्य किसी समस्या/उद्दीपके पर दिये गये विकल्पों अथवा प्रत्युत्तरों के एक-दूसरे विविध/अलग होने से है अर्थात् कई विकल्पों पर सोच सकने की क्षमता या बातचीत के सन्दर्भ बदलने की योग्यता जैसे यदि आप किसी व्यवसाय को चुनते हैं तो उस समय आप किन-किन पहलुओं पर ध्यान देंगे, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए । विविधता की तीन विमाएँ होती हैं। आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता से तात्पर्य किसी वस्तु या आकृति से सुधार करने के उपायों में विविधता से है। आकृति अनुकूल विविधता से तात्पर्य किसी वस्तु या आकृति के रूप में परिवर्तित करने की विधियों में विविधता से है। शाब्दिक स्वतः स्फूर्त विविधता में वस्तुओं या शब्दों के प्रयोग में विविधता को देखा जाता है।
(3) मौलिकता-मौलिकता से अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्पों या प्रत्युत्तरों का असामान्य, असाधारण, उपयोगी, प्रासंगिक तथा अन्य व्यक्तियों के उजरों से भिन्न होने से है। मौलिकता, नवीनता से सम्बन्धित होती है। जो व्यक्ति विकल्प प्रस्तुत करने (अन्यों से) में भिन्नता प्रदर्शित करता है, वह मौलिक कहा जाता है। जैसे दिये गये शब्दों पर कविता लिखना, कहानी, कविता या लेख के शीर्षक बताना।
(4) विस्तारण-विस्तार से तात्पर्य दिए गए भावों या विचारों की विस्तृत व्याख्या, व्यापक पूर्ति व गहन प्रस्तुतीकरण से है। शाब्दिक विस्तारण में किसी दी गई संक्षिप्त घटना, क्रिया, कार्य, परिस्थिति आदि को विस्तृत करके प्रस्तुत किया जाता है, जबकि आकृति विस्तारण में किसी दी गई आकृति, रेखा या अपूर्ण चित्र में कुछ जोड़कर उससे एक पूर्ण तथा सार्थक चित्र बनाना होता है।
सृजनात्मक बालक की पहचान –
सृजनात्मक बालक को सामान्य बालकों से अलग करना थोड़ा जटिल इसलिए है कि ऐसे बालक सामान्य बालकों जैसा ही व्यवहार करते पाये गये हैं। साथ ही बुद्धि के सम्बन्ध में भी ये भिन्न नहीं होते । इनकी पहचान कुछ चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है। मैककिनोन ने सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताएँ अपने अनुसन्धान में पायी जिनका विवरण निम्न प्रकार है-
(i) सृजनात्मक बालक अपने को दूसरों से भिन्न मानता है। ये अपने को खोजपूर्ण स्वतन्त्र और व्यक्तिगत समझते हैं।
(ii) सृजनात्मक बालक संवेगों और अनुभवों के प्रति खुले रहते हैं। ये इस बात की परवाह नहीं करते हैं अन्य लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। वे अपने अनुभवों और संवेगों को प्रदर्शित करते हैं।
(iii) एक भावुकं बुद्धि को रखते हैं।
(iv) स्व-जागरूकता को समझते हैं।
(v) विस्तृत रुचियों को रखते हैं।
(vi) सृजनात्मक लोग छोटे-छोटे विवरणों और घटनाओं में रुचि नहीं रखते हैं।
(vii) वे विवरणों और घटनाओं के अर्थों और प्रयोगों में रुचि लेते हैं।
(viii) ज्ञानात्मक लोच वाले होते हैं।
(ix) शाब्दिक कौशल में निपुण होते हैं।
(x) दूसरों के विचारों के आदान-प्रदान में रुचि लेते हैं।
(ix) जिज्ञासु होते हैं।
(xii) अपनी प्रतिभा को सुधारने में या बनाने में कोई रुचि नहीं रखते।
(xiii) ज्ञानात्मक लोच वाले होते हैं।
(xiv) दूसरों की प्रतिभाओं और आवेगों की परवाह नहीं करते हैं।
(xv) ये अनुभवों को आत्मसात करते हैं उनका मूल्यांकन नहीं करते हैं।
(xvi) सृजनात्मक व्यक्तियों को अधिक अन्तर्बोध होता है।
गोयल ने सृजनात्मक बालकों में निम्नलिखित विशेषताएँ पायीं-
(i) अधिक स्फूर्तिपूर्ण,
(ii) अधिक अन्तर्मुखी,
(iii) विचारों और क्रियाओं में अधिक स्वतन्त्र,
(iv) खुला मस्तिष्क,
(v) सहनीय अस्पष्टता
(vi) विरोधात्मक मूल्य की विचारणा ।
इन विभिन्न विशेषताओं के आधार पर सृजनात्मक बालकों की पहचान की जा सकती है। गेटजल्स और मेडन्स ने सृजनात्मक बालकों की पहचान विधियों को पाँच भागों में बाँटा है। ये निम्नलिखित हैं-
1. उपलब्धि-अत्यन्त उच्च श्रेणी की उपलब्धि, यथा, नोबल पुरस्कार या इसी प्रकार कोई अन्य कार्य सृजनात्मकता को बताता है।
2. मापनी-साथियों, अध्यापकों, निरीक्षकों, प्रधानाचार्यों अथवा मनोवैज्ञानिकों द्वारा मापनी की सहायता से सृजनात्मक बालकों का पता लगाया जा सकता है।
3. बुद्धि-बुद्धि-लब्धि परीक्षण में अति उच्च बुद्धि-लब्धि सृजनात्मक की द्योतक मानी जाती है।
4. व्यक्तित्व- सर्जनात्मक व्यक्तित्व विशेषताओं के आधार पर सर्जनात्मक बालकों की पहचान की जा सकती है।
5. सृजनात्मकता- परीक्षण-अंक- कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता परीक्षण बनाये हैं; जैसे- टोरेन्स, गिलफोर्ड, मेडनिक आदि। भारत में भी अनेक इस प्रकार के परीक्षण बनाये गये हैं, उदाहरणार्थ- पासी, बॉकर मेंहदी, कौल, मजूमदार आदि के परीक्षण ।
इस प्रकार इन विभिन्न विधियों से सृजनात्मक बालकों का पता लगाया जाता है। ऐसे बालकों का पता लग जाने पर उनकी शिक्षा का यथोचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अन्य बालकों में भी सृजनात्मक चिन्तन कौशल विकसित हो ।
सृजनात्मक बालकों की शिक्षा –
शिक्षा व्यक्ति को ऐसे अवसर प्रदान कर सकती है कि उसमें अन्तर्निहित सृजनशीलता प्रस्फुटित होकर जीवन की समस्याओं का समाधान करने तथा नवीन कार्य करने में सहायक हो सके। अतः शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों का निर्धारण करते समय सृजनात्मकता के महत्त्व को भी स्वीकार करना होगा। सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सुझाव दिये हैं, जिनमें से कुछ सुझाव निम्न हैं-
1. बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके अध्यापक भी सृजनात्मक प्रवृत्ति के हों। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अध्यापकगण साहित्य, कला आदि विभिन्न क्षेत्रों में तरह-तरह के सृजनात्मक कार्य प्रस्तुत करके अपने छात्रों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने में समर्थ होने चाहिए।
2. छात्रों में नवीन विचारों को ग्रहण करने तथा उनका सम्मान करने के साथ-साथ प्रतिक्रिया करने की स्वतन्त्रता तथा प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति कक्षा में विकसित की जानी चाहिए। मस्तिष्क उद्वेलीकरण
को बढ़ा दिया जाना चाहिए।
3. अध्यापक जो भी कुछ पढ़ाये, उसमें समस्या के स्तरों की पहचान का शिक्षण अवश्य हो । छात्र यह अवश्य जान ले कि समस्या किस स्तर की है ? जे० स्टेनली ग्रे ने इस सम्बन्ध में कहा है कि समस्या समाधान की योग्यता दो पदों पर है-एक व्यक्ति को सीखने की या अधिगम की बुद्धिवादी क्षमता या वृद्धि और दूसरा यह है कि क्या उस व्यक्ति ने क्षमता के भीतर अधिगम पा लिया है।
4. सृजनात्मक शिक्षा के लिए समस्या समाधान के सन्दर्भ में तथ्यों का अधिगम कराया जाये। इसमें क्या किया गया, क्या किया जाना चाहिए? आदि प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। 5. सृजनात्मकता के शिक्षण के लिए मौलिकता की उद्भावना विकसित करने के लिए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सृजन तथा मौलिकता से अभिप्राय ज्ञान के तथ्यों को नवीन रूप से ढालना है। 6. अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों का सही मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति विकसित करे। यह सृजन शक्ति को अधिक विकसित करता है।
7. छात्रों में चिन्तन की जाँच की विधि की कुशलता विकसित की जाए।
8. सृजनात्मकता के विकास के लिए यह आवश्यक है कि सृजनात्मक कार्यों में बालकों के उत्साह रुचि को बनाये रखा जाए। अतः अध्यापकों को अपने छात्रों की रुचि तथा उत्साह बनाये रखने के लिए यथा सम्भव प्रयास करने चाहिए।
9. जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे-सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, तकनीकी अथवा शैक्षिक आदि की विभिन्न समस्याओं को समझने तथा उनका तर्कसंगत तथा व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
10. विभिन्न क्षेत्रों के महान् अन्वेषकों के जीवन परिचय के साथ-साथ उनके जीवन में घटी विशेष तथा सार्थक घटनाओं से बालकों को अवगत कराना चाहिए, जिससे वे उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त कर सकें।
प्रश्न 9 (ii) विकास से क्या आशय है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त को समझाइए। इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है?
अथवा
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त की चर्चा उसके शैक्षिक निहितार्थ सहित कीजिए।
अथवा
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
ANSWER-
विकास का अर्थ
विकास का अर्थ है ‘बढ़ना’। यह समग्र, क्रमिक, सुसम्बद्ध एवं प्रगतिशील होता है। इससे परिपक्वता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विकास उन प्रगतिशील परिवर्तनों को कहते हैं जिनका प्रारम्भ नियमित एवं क्रमिक होता है तथा परिपक्वता प्राप्ति की ओर निर्देशित रहता है। प्रायः देखने में आता है कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रचना में परिवर्तन के कारण उसकी विभिन्न अवस्थाओं में नये-नये गुणों का आविर्भाव और पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। व्यक्ति को जीवित और सक्रिय बने रहने के लिए ये परिवर्तन आवश्यक हैं क्योंकि जीवन का अर्थ है ‘अविरल परिवर्तन’ । इन्हीं शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों, गुणों तथा विशेषताओं की नियमित और क्रमिक उत्पत्ति को मनोवैज्ञानिक भाषा में ‘विकास’ कहा जाता है और निहित क्षमताओं को साकार करने की प्रक्रिया ही विकासात्मक प्रक्रिया है।
विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्कीनर ने कहा है कि, “विकास नियमित और क्रमिक प्रक्रिया है।” ई0बी0 हरलॉक ने विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि, “विकास नियमित और क्रमबद्ध रूप में परिवर्तनों के प्रगतिशील क्रम को व्यक्त करता है। इसे कार्य हेतु अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए क्षमताओं को प्रकट करने और विस्तृत करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।” स्पष्ट है कि विकास परिवर्तनों की प्रक्रिया है और इसके फलस्वरूप ही व्यक्ति के भीतर नयी-नयी विशेषताओं और क्षमताओं का जन्म होता है।
पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए संज्ञानात्मक विकास को चार प्रमुख अवस्थाओं में विभक्त किया है। प्रत्येक अवस्था संज्ञानात्मक संरचनाओं में तालमेल बैठाने के बालक के प्रयासों के एक भिन्न रूप को अभिव्यक्त करती है। प्रत्येक अवस्था एक विशेष समयावधि में उपयुक्त होती है तथा प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व अवस्थाओं से अधिक उपयुक्त होती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की निम्न चार अवस्थाएँ बतायी हैं-
1. संवेगी पेशीय अवस्था – जन्म से 3 वर्ष तक
2. प्राक्संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक
3. ठोस संक्रिया की अवस्था – 7 से 12 वर्ष तक
4. औपचारिक संक्रिया की अवस्था – वयस्कावस्था के प्रारम्भ तक ।
1. संवेदी पेशीय अवस्था-यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष चलती है। इस अवस्था में शिशुओं का संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है।
पहली उप-अवस्था प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था – यह जन्म से 30 दिन तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियायें करता है। इन प्रतिवर्त क्रियाओं में चूसने का प्रतिवर्त सबसे प्रबल होता है
दूसरी उप- अवस्था प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था – यह अवस्था 1 से 4 माह की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्त क्रियायें उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती है, दोहराई जाती हैं और एक-दूसरे के साथ अधिक समन्वित हो जाती हैं। इन व्यवहारों को प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें दोहराई जाती है।
तीसरी उप-अवस्था गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था – यह अवस्था 4 से 8 महीने की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है न कि अपने शरीर की प्रतिवर्त क्रियाओं पर । इसके आलावा वह जान-बूझ कर कुछ ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है जो उसे सुनने या करने में रोचक तथा मनोरंजक लगती हैं।
चौथी उप-अवस्था गौण स्कीमैटा के समन्वय की अवस्था-यह अवस्था 8 से 12 माह तक चलती है। इस अवस्था में बालक उद्देश्य तथा उस तक पहुँचाने के साधन में अन्तर करना प्रारम्भ कर देता है। जैसे- यदि कोई खिलौना छिपा दिया जाता है, तो वह उसके लिए वस्तुओं को इधर-उधर हटाकर खोज जारी रखता है। इसके द्वारा शिशु वयस्कों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का अनुकरण भी प्रारम्भ कर देता है। इस अवधि में शिशु जो स्कीमा सीखते हैं, उनके वे एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में समामान्यीकरण करना भी प्रारम्भ कर देते हैं
पाँचवीं उप-अवस्था तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था-यह अवस्था 12 महीने से 18 महीने की अवधि की होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक की अपनी शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम हो जाती है और वह स्वयं कुछ वस्तुओं को लेकर प्रयोग करता है। बालक में उत्सुकता अभिप्रेरक अधिक प्रवृत्त हो जाता है तथा उनमें वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है।
छठी उप-अवस्था मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था – यह अन्तिम उप-अवस्था है जो 18 से 24 माह तक की अवधि की होती है। यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारम्भ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। इस गुण को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है।
2. प्राक्संक्रियात्मक अवस्था-संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। यह प्रारम्भिक बाल्यावस्था होती है। इस अवस्था को पियाजे ने 2 अवधियों में बाँटा है-
1. प्राक्संप्रत्यात्मक अवधि – 2 से 4 वर्ष तक
2. अन्तर्दर्शी अवधि – 4 से 7 वर्ष तक
प्रथम अवधि- प्राक्संप्रत्यात्मक अवधि – इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेते हैं। सूचकता से तात्पर्य इस बात से होता है कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिन्तन किसी चीज के लिए किया जाता है। पियाजे ने दो तरह की सूचकता पर बल डाला है-
(I) संकेत – किसी ठोस वस्तु के मानसिक चिन्तन का दूसरा नाम संकेत है। संकेत तथा ठोस में अधिक सादृश्यता होती है। जैसे- जब बालक अपनी माँ की आवाज को सुनता है तब उसके मन में माँ की एक प्रतिमा बनती है जो संकेत का उदाहरण है।
(II) चिह्न – चिह्न से वस्तुओं में, जिनका बालक मानसिक चिन्तन करते हैं, इतनी अधिक सादृश्यता नहीं होती है। चिह्न में वस्तुओं या घटनाओं का एक अमूर्त चिन्तन होता है। शब्द या भाषा के अन्य पहलू सब सामान्य चिह्न के उदाहरण हैं।
पियाजे नै संकेत तथा चिह्न को प्राक्संक्रियात्मक चिन्तन का महत्त्वपूर्ण साधन माना जाता है। इस अवस्था में बालकों को इस सूचकता का अर्थ समझना होता है तथा साथ ही साथ उसे अपने चिन्तन एवं कार्य में उसका प्रयोग करना सीखना होता है। इसे पियाजे ने लाक्षणिक कार्य की संज्ञा दी है। पियाजे ने यह भी बताया है कि बालकों में लाक्षणिक कार्य मूलतः दो तरह की क्रियाओं (अनुकरण एवं खेल) द्वारा होता है। अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा बालक सूचकता को सीखते हैं। उदाहरणस्वरूप, बालक जब माँ को ‘फूल को फूल’ कहने का अनुकरण है, तो वह धीरे-धीरे फूल एवं उसके अर्थ को समझ जाता है। खेल के माध्यम से भी बालक सूचकता के अर्थ को समझते हैं तथा उसका सही-सही प्रयोग अपने चिन्तन एवं क्रियाओं में करना सीखते हैं।
पियाजे ने प्राक्संक्रियात्मक चिन्तन की दो सीमाएँ बताई हैं जो निम्नवत् हैं-
(I) जीववाद – जीववाद के चिन्तन में एक ऐसी सीमा की ओर बताता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। जैसे- कार, पंखा, हवा, बादल आदि सब उसके लिए सजीव होते हैं।
(II) आत्मकेन्द्रित — इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सहीं मानता है। उसे कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है कि दुनिया की अधिकतर चीजें उसके इर्द-गिर्द चक्कर लगाती रहती हैं। जैसे- वह तेजी से दौड़ता है तो सूर्य भी तेजी से चलना प्रारम्भ कर देता है, उसकी गुड़िया वही देखती है जो वह देखता है, आदि-आदि। पियाजे ने यह भी बताया कि जैसे-जैसे बालकों का सम्पर्क अन्य बालकों एवं भाई-बहिनों से बढ़ता चला जाता है, उसके चिन्तन में आत्मकेन्द्रितता कम होती जाती है।
द्वितीय अवधि अन्तर्दर्शी अवधि – इस अवधि में बालकों का चिन्तन एवं तर्कणा पहले से अधिक परिपक्व हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप वह साधारण मानसिक प्रक्रियाओं में जोड़, घटाव (बाकी), गुणा तथा भाग आदि में सम्मिलित होती हैं, उन्हें वह कर पाता है। परन्तु, इन मानसिक प्रक्रियाओं के पीछे छिपे नियमों को वह नहीं समझ पाता है। अन्तर्दर्शी चिन्तन इस प्रकार एक ऐसा चिन्तन होता है जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। पियाजे ने अन्तर्दर्शी चिन्तन की भी एक सीमा बताई है और वह यह है कि 4 से 7 वर्ष के बालकों के चिन्तन पलटावी गुण नहीं होता है, जैसे- बालक तो यह समझता है कि 2 x 2 = 4 हुआ, परन्तु 4/2 = 2 कैसे हुआ नहीं समझ पाता।
3. ठोस संक्रिया की अवस्था-यह अवस्था 7 वर्ष से प्रारम्भ होकर 12 वर्ष तक चलती रहती है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि बालक दो वस्तुओं अर्थात् ठोस वस्तुओं के आधार पर वे आसानी से मानसिक संक्रियायें करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। परन्तु उन वस्तुओं को न देकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करके यदि समस्या उपस्थित की जाती है, तो वे ऐसी समस्याओं पर मानसिक संक्रियायें कर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में असमर्थ रहते हैं। जैसे यदि उन्हें तीन वस्तुएँ A, B, C दी जायें तो उन्हें देखकर वे आसानी से कह देंगे कि इनमें ‘A’, ‘B’, से बड़ा है और B, C से बड़ा है। अतः सबसे बड़ा A है। परन्तु यदि उनसे यह कहा जाए कि ‘जय’ ‘अन्’ है और ‘अनु’ बड़ा है। ‘मनु’ से, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इसका उत्तर देने में बालक असमर्थ रहता है। इसका कारण यह है कि इस समस्या में ठोस संक्रिया संभव नहीं है क्योंकि समस्या शाब्दिक कथन के रूप में उपस्थित की गई है। इस उदाहरण से यह भी स्पष्ट है कि इस अवस्था में बालकों का चिन्तन एवं तर्क प्राक्संक्रियात्मक अवस्था की तुलना में अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत हो जाती है। इस अवस्था के चिन्तन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें पलटावी गुण आ जाता है। जैसे- अब बालक यह समझने लगता है कि 2 x 2 = 4 हुआ तो 4/2 = 2 होगा।
इस अवस्था में बालकों में तीन महत्त्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाता है- संरक्षण, सम्बन्ध तथा वर्गीकरण। इस अवस्था में बालक, तरल, लम्बाई, भार तथा तत्त्व के संरक्षण से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करते पाए जाते हैं। वे क्रमिक सम्बन्धों से सम्बन्धित समस्याओं का भी समाधान करते पाए जाते हैं। अर्थात् दी गई वस्तुओं को उसकी लम्बाई या वजन के अनुसार घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाने की क्षमता आ जाती है। इसे पंक्तिबद्धता की संज्ञा दी जाती है। उसी तरह से इस अवस्था में वस्तुओं के गुण के अनुसार उसे किसी एक वर्ग या उपवर्ग में छाँटने की भी क्षमता विकसित हो जाती है।
इतना होने के बावजूद ठोस संक्रियात्मक चिन्तन की दो प्रमुख सीमाएँ बताई गयी हैं–
(i) इस अवस्था में बालक मानसिक संक्रियायें तभी कर पाते हैं जब वस्तु ठोस रूप में उपस्थित की गई हो।
(ii) इस अवस्था में चिन्तन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता है क्योंकि बालक दी गई समस्या के तार्किक रूप से संभावित सभी समाधानों के बारे में नहीं सोच पाता है।
4. औपचारिक संक्रिया की अवस्था-यह अवस्था 11 वर्ष से आरम्भ होकर वयस्कावस्था तक चलती है। इस अवस्था में किशोरों का चिन्तन अधिक लचीला होता है तथा प्रभावी भी हो जाता है। उसके चिन्तन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। अब वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोच कर एवं चिन्तन करके करने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था में समस्या के समाधान के लिए समस्या के एकांशों को ठोस रूप से उसके सामने उपस्थित होना अनिवार्य होता है। इस तरह किशोरों के चिन्तन में वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है।
पियाजे का मत है कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक परिवर्त्य होती है तथा यह किशोरों के शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। जिस बालकों का शिक्षा- स्तर काफी नीचा होता है, उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिन्तन भी काफी कम होता है। परन्तु, जिस बालक का शिक्षा स्तर काफी ऊँचा होता है, उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिन्तन अधिक मात्रा में पाया जाता है।
प्रश्न 9 (iii) शिक्षण किसे कहते हैं? इसके तीनों स्तरों को उदाहरणों की सहायता स्पष्ट कीजिए।
अथवा
शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के किन्हीं दो स्तरों को उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए।
ANSWER-
शिक्षण की परम्परागत अवधारणा —
पहले शिक्षण का अर्थ यह स्वीकार किया जाता था कि थोड़ा-सा ज्ञान बालक को लिखने, पढ़ने एवं गणित में दे दिया जाय। यह ज्ञान भी अध्यापक बालकों की स्मृति पर ही बल देकर प्रदान करते थे। जो शिक्षण-विधि वे अपनाते थे, वह रटने की विधि थी। वे बालकों पर कड़ा अनुशासन रखकर डण्डे के बल पर शिक्षा देना ही उत्तम समझते थे। एडम्स महोदय को परम्परागत शिक्षण के सम्बन्ध में एक “अध्यापक ने जॉन को लैटिन पढ़ायी” महत्त्वपूर्ण है। इस कथन के अनुसार पुराने अध्यापक लैटिन पर अधिक बल देते थे जबकि आधुनिक शिक्षण में जॉन (बालक) पर अधिक बल दिया जाता है। पुराने अध्यापक हर बालक को एक ही रास्ते पर एक ही ढंग से चलाते थे। उन्हें केवल इस बात की चिन्ता थी कि बालक किसी तरह लैटिन के निश्चित पाठ्यक्रम (निश्चित तथ्य एवं सूचनायें) को लें। इस बात पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी कि भिन्न-भिन्न बालकों की योग्यताओं में भी विभिन्नता हो सकती है, उनकी रुचियों और सामर्थ्यो में भी अन्तर हो सकता है। इस प्रकार संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षण के लिए केवल औपचारिक साधनों का प्रयोग होता है और शिक्षण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा व्यक्ति को एक निश्चित समय तक निश्चित तथ्य का शिक्षण दिया जाता है।
शिक्षण की आधुनिक अवधारणा–
19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से तो यह स्पष्ट रूप से माना जाने लगा कि शिक्षण प्रदान करने में बालक का विशेष महत्त्व है, रूसो, पेस्टालाजी, फ्रोबेल, हर्बर्ट स्पेन्सर, डीवी आदि के विचारों ने प्राचीन शिक्षण सिद्धान्तों एवं विधियों में क्रान्ति उत्पन्न कर दिया। शिक्षा विषय केन्द्रित से हटकर बाल- केन्द्रित होने लगी। एडम्स महोदय के उपर्युक्त कथन में लैटिन (विषय) की अपेक्षा ‘जॉन’ (बालक) का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाने लगा। विभिन्न बालकों की योग्यता, प्रवृत्ति, रुचि आदि के अनुसार शिक्षा प्रदान करना उत्तम समझा जाने लगा।
शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा में नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया और नवीन शिक्षण पद्धतियों का आविष्कार किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षण एक आनन्दपूर्ण प्रक्रिया है और बालक नयी वस्तुओं को सीखने में आनन्द करता है। इस प्रकार शिक्षण का अर्थ व्यापक हो गया। व्यापक अर्थ में शिक्षण और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधन निहित हैं। अपने व्यापक अर्थ में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, मनोरंजन और व्यवसाय में अपने वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त होता है।
शिक्षण का अर्थ और परिभाषाएँ –
1. योक्कम तथा सिम्पसन-“शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन से सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं
2. रायबर्न- “शिक्षण एक सम्बन्ध है जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है।”
3. बर्टन – “शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपन, मार्ग-दर्शन, निर्देशन और प्रोत्साहन है।”
बिग्गी ने शिक्षण-अधिगम की परिस्थितियों को निम्नलिखित तीन स्तरों में विभाजित किया है- 1. स्मृति-स्तर, 2. अवबोध-स्तर, 3. परावर्तन-स्तर ।
स्मृति स्तर के शिक्षण का स्वरूप
शिक्षण का प्रथम स्तर स्मृति-स्तर है। इस स्तर पर विचारहीनता पाई जाती है। इस स्तर पर ऐसी अधिगम परिस्थितियाँ विकसित की जाती हैं जिनसे छात्र पढ़ाई गई पाठ्यवस्तु को सरलता से कंठस्थ कर सके। विषयवस्तु को कंठस्थ कर लेने मात्र से ही शिक्षण की सफलता सिद्ध हो जाती है। स्मृति- स्तर रटने का स्तर है। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी के मस्तिष्क में ज्ञानात्मक स्तर पर तथ्यों एवं सूचनाओं को बलपूर्वक दूंसा जाता है। उसे केवल विषय के रटने की ओर प्रवृत्त किया जाता है। तथ्यों एवं सूचनाओं के रटने का सम्बन्ध बुद्धि से नहीं होता। मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक भी चीजें सरलता से याद कर लेते हैं। विद्यार्थी बलपूर्वक धारण किए हुए ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यास्मरण तथा पहचान करते हैं।
समृति स्तर पर शिक्षण में अध्यापक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इस स्तर पर छात्र निष्क्रिय अधिगमकर्त्ता के रूप में रहता है। वह कठोर अनुशासन का पालन करते हुए केवल तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों, सिद्धान्तों, नियमों तथा विचारों को हृदयंगम करता रहता है। अध्यापक स्वयं ही पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित, क्रमिक एवं सुसंगठित रूप प्रदान करने के लिए परिश्रम करता है। स्मृति स्तर के
(3) शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष पिछले साल के प्रश्न
| विषय | शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष प्रश्न
shikshan adhigam evan vikaas ke manovigyaan ke paripreksh Question Paper |
| SUBJECT | Perspectives from the psychology of teaching, learning and development Question |
| पेपर कोड | 102 |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय |
| कोर्स | बी.एड |
| सेमेस्टर | प्रथम |
| FULL MARKS | 50 |
| lnfo | यहाँ महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के पेपर -102 शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष प्रश्न दिया गया है | |