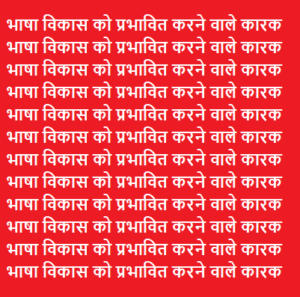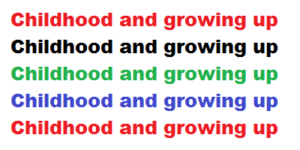शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान
Shiksha mein kriyaatmak anusandhaan
| विषय | शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान |
| SUBJECT | Shiksha Mein Kriyaatmak Anusandhaan |
| SUBJECT | Action Reseacher In Education |
| UNIVERSITY | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय |
| COURSE | बी.एड प्रथम सेमेस्टर |
| PAPER | 04 (FOUR) |
| CODE | 104 |
| lnfo | इस पेज में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान सिलेबस , नोट्स एवं क्वेश्चन पेपर को शामिल किया गया है | |
VVI NOTES के इस पेज में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान सिलेबस , शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान नोट्स , शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान क्वेश्चन पेपर , शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान सीरिज , शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान प्रश्न उत्तर ,शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान गेस पेपर , शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धानगाइड ,शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान बुक ,शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान प्रश्न ,शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान क्वेश्चन पेपर एत्याफी को सामिल किया गया है |
In this page of VVI NOTES, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth University B.Ed 1st Semester Action Research in Education Syllabus, Action Research in Education Notes, Action Research in Education Question Paper, Action Research in Education Series, Action Research in Education Question Answers, Action Research in Education Guess Paper, Action Research in Education Guide, Action Research in Education Book, Action Research in Education Questions, Action Research in Education Question Paper etc. have been included.
शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान सिलेबस
शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान | MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH, VARANASI
| विषय | शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान
Shiksha Mein Kriyaatmak Anusandhaan Shiksha mein kriyaatmak anusandhaan |
| SUBJECT | Action Reseacher In Education Syllabus |
| पेपर कोड | 104 |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय |
| कोर्स | बी.एड |
| सेमेस्टर | प्रथम सेमेस्टर |
| FULL MARKS | |
| lnfo | यहाँ महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के पेपर -१04 शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान के सिलेबस दिया गया है | यह विषय सभी स्टूडेंट्स का समान होता है | |
Unit-1
A. Action research: Meaning, importance, characteristics and objectives of action research.
B. Concept of fundamental and applied research, Difference between traditional (fundamental and applied) research and action research.
Unit-2
A. Action research for improving class room and school based programmes,
B. Role of stakeholders in action research projects. Role of action research in improving organizational climate.
Unit-3
A. Procedure of designing action research: Selection of problem, Formulation of action hypotheses and developing a suitable design for testing of such hypotheses.
B. Evaluation of results in action research and their usage.
Unit-4
A. Developing school based projects for action research; Format of a project and its implementation. Determining intervention based effects in terms of pre-post comparison: Precautions needed.
B. Formulating an action research based report for the benefit of other practitioners.
(2) शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान नोट्स
| विषय | शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान नोट्स
Shiksha mein kriyaatmak anusandhaan Notes |
| SUBJECT | Action Reseacher In Education Question- Answer |
| पेपर कोड | १04 |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय |
| कोर्स | बी.एड |
| सेमेस्टर | प्रथम |
| FULL MARKS | 50 |
| lnfo | यहाँ महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के पेपर -१04 समावेशी शिक्षा के नोट्स दिया गया है | |
लघु उत्तरीय प्रश्न
(Short Answer Type Questions)
निर्देश : इस खण्ड में प्रश्न संख्या 1 (a से j) लघु उत्तरीय प्रश्न है। परीक्षार्थियों को सभी दस (a से j) प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। (10 × 4 = 40 अंक)
प्रश्न a (i) क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक की भूमिका ।
उत्तर-क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा शिक्षक अपनी कक्षा के वातावरण में अपनी कार्य प्रणाली में सुधार तथा प्रगति करता है। शिक्षक शोध के पदों से परिचित होता है। शिक्षकों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति, शोध कार्य के लिए जागृत होती है। इसके द्वारा विद्यालय के प्रशासन में सुधार तथा परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्रियाकलापों का मूल्यांकन स्वयं करें एवं तद्नुसार प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर अपनी कमियों को जानें तथा अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास अपने स्तर से करें। क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों को संरचनात्मक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करके शिक्षा की लक्ष्य सिद्धि को सहज बनाने में सहायता प्रदान करता है। विद्यालय के शिक्षक को इस शोध पद्धति के अंतर्गत् अपनी क्रियाओं के विकास एवं सुधार के लिए अवसर उपलब्ध होता है, जिसके द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली को सुधारा जाता है।
प्रश्न a (ii) संगठनात्मक परिवेश के घटक।
उत्तर-संगठनात्मक परिवेश संगठनात्मक अवयवों जैसे संस्कृति, संरचना, प्रणाली, नेतृत्व व्यवहार और संगठन के सदस्यों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ आदि की अन्तः क्रिया द्वारा सृजित होता है। वैश्वीकरण के आरंभ होने से कार्य संस्कृति और संगठनात्मक परिवेश में असंख्य परिवर्तन हुए हैं, इसी प्रकार कार्यबल विविधता जैसे धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्ति, विस्थापित लोग, महिला-पुरुष मुद्दे, आयु सम्बन्धी कारक, अस्थायी अनियमित सुविधाएँ आदि किसी दूसरे व्यवसाय की कार्य संस्कृति की तुलना में समाज कार्य में कार्य संस्कृति पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। संगठनात्मक वातावरण को कॉर्पोरेट वातावरण के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह एक निगम की संस्कृति की मात्रा निर्धारित करता है। संगठन में कर्मचारियों की नौकरी से सन्तुष्टि, उत्पादकता और प्रेरक स्तरों पर इसका महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
प्रश्न a (iii) मौलिक अनुसंधान की अवधारणा ।
अथवा
मौलिक शोध की संकल्पना ।
उत्तर- मौलिक अनुसंधान को शुद्ध अनुसंधान के नाम से भी पुकारा जाता है। यह अनुसंधान का वह स्वरूप है जिसमें तथ्यों का निर्धारण तथा उनके आधार पर सम्बन्धों के निरूपण एवं विश्लेषण अत्यन्त कठोर तथा संरचित ढंग से सम्पन्न होते हैं तथा जिसका उद्देश्य सिद्धान्त प्रतिपादन एवं सिद्धान्त परीक्षण या सिद्धान्त परिष्करण की ओर बढ़ना है। इस प्रकार के शोधों का मुख्य मुद्दा होता है-सामान्यीकरण, अनुसिद्धान्तों, नियमों एवं उपनियमों का निरूपण । साधारण तौर पर इसे नियन्त्रित परिस्थितियों यथा- प्रयोगशालाओं में पूरा किया जाता है। मानवीय परिस्थितियों में भी इस प्रकार के शोध अधिकतर नियन्त्रित परिस्थितियों में सम्पन्न होते हैं, किन्तु चिन्तन की अनेकानेक धाराओं से सम्बद्ध मौलिक शोध चिन्तकों के विचारों की मीमांसात्मक व्याख्या एवं गवेषणात्मक अध्ययन पर आधारित होते हैं और उनमें प्रयोगशाला जैसी नियन्त्रित परिस्थिति का गठन सम्भव नहीं होता है।
आशय यह है कि मौलिक अनुसंधान की परिधि केवल इन्द्रियानुभविक विज्ञानों (Imperical Sciences) तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में होने वाले मौलिक शोध अग्रणी चिन्तकों एवं चिन्तन धाराओं के आलोचनात्मक अध्ययन को विशेष महत्त्व देते हैं तथा इनका गन्तव्य नवीन शैक्षिक धारणाओं एवं संकल्पनाओं को प्रकाश में लाना है।
प्रश्न a (iv) मौलिक अनुसंधान की विशेषताएँ ।
उत्तर- मौलिक अनुसंधान की विशेषताएँ निम्न हैं-
(1) मौलिक अनुसंधान को पूरा करने में साधारण तौर पर नियन्त्रित परिस्थितियाँ गठित की जाती हैं जिनके माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि किसी समग्र से चयनित प्रतिनिधि समूह के प्रेक्षण द्वारा सामान्यीकरण निर्मित हो ।
(2) मौलिक अनुसंधान का प्रमुख मुद्दा सिद्धान्त निरूपण, ज्ञान की सीमा में विस्तार लाना, नवीन अनुसिद्धान्तों का विकास तथा नवीन प्रणालियों, नियमों एवं सत्यों को विज्ञापित करना है ।
(3) यह सहजता से देखा जा सकता है कि मौलिक अनुसंधान का सन्दर्भ अपेक्षाकृत अमूर्त होता है तथा यह तथ्यों एवं चरों के परिमार्जन सम्बन्धी उच्चस्तरीय अवधारणा से मिलकर बनता है।
(4) उसके तहत अनुसंधान की समस्या अथवा प्रश्न से सम्बन्धित स्वरूप दो या दो से अधिक तथ्यों, चरों या सम्प्रत्ययों के मध्य का पता लगाने से सम्बन्धित होता है जिससे एक व्यापक व्याख्यात्मक परिप्रेक्ष्य कायम करने में मदद मिले। इसी परिप्रेक्ष्य को प्रायः सिद्धान्त (थियोरी) के नाम से पुकारा जाता है।
(5) अनुसंधान की परिकल्पना जो समस्या के प्रस्तावित समाधान के रूप में निर्मित होती है, इस प्रकार के अनुसंधान के तहत एक उच्चस्तरीय सम्बन्ध संरचना के आधार पर विकसित की जाती है तथा यह अध्ययन विशेष सम्बन्धित अनुक्षेत्र में सिद्धान्त निरूपण एवं सिद्धान्त- मूल्यांकन हेतु प्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है।
(6) मौलिक अनुसंधान के अन्तर्गत शोधकर्ता अपने अनुसंधान के समग्र गणना किये जाने योग्य समस्त इकाइयों या घटकों को परिभाषित करता है तथा उससे एक प्रतिनिधि (लघु समूह)
प्रेक्षण के लिए ले लेता है। इस प्रकार लघु समूह पर किये गये प्रेक्षण को पूरे समग्र पर सामान्यीकृत किया जाता है। यहाँ ध्यान रखना होगा कि इस अनुसंधान में समग्र तथा ‘प्रतिदर्श’ दोनों ही भिन्न- भिन्न धारणाएँ हैं तथा अधिकतर परिस्थितियों में शोधकर्ता एक सावधानीपूर्वक चुने गये प्रतिनिधि प्रतिदर्श पर ही प्रेक्षण करता है तथा बाद में इसे पूरे समग्र के सन्दर्भ में सामान्यीकरण करता है।
(7) मौलिक अनुसंधान की अन्य विशेषता यह है कि इसके तहत शोध के अभिकरण (रूपरेखा) या डिजाइन को अत्यन्त कठोरतापूर्वक विकसित एवं कार्यान्वित किया जाता है। शोध की यह रूपरेखा एक निर्देशक परिप्रेक्ष्य बन जाता है जिसके सन्दर्भ में अनुसंधान के चरों को परिभाषित करने, उनके मध्य सम्बन्ध उपकल्पित करने तथा उनके सत्यापन, परीक्षण या मूल्यांकन की ओर प्रवृत्त होने तथा सांख्यिकी निरूपण, आदि के प्रति पग उठाये जाते हैं।
प्रश्न a (v) व्यवहृत अनुसंधान की अवधारणा ।
उत्तर-व्यवहृत अनुसंधान को अनुसंधान का सामान्यतः प्रयुक्त स्वरूप कहा जा सकता है। यह मूलतः समस्यात्मक परिस्थितियों के वर्णन, उनकी व्याख्या एवं भावी कथन से सम्बन्धित शोध है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट की राय में भी शैक्षिक अनुसंधान का अधिकांश स्वरूप व्यवहृत होता है क्योंकि इसके तहत अधिकतर शिक्षण-अधिगम की प्रक्रियाओं एवं अनुदेशनात्मक सामग्रियों के बारे में सामान्यीकरण विकसित करने का प्रयास किया जाता है। शैक्षिक परिस्थितियों से जुड़े अधिकतर अध्ययन अपनी प्रकृति की दृष्टि से अन्तर्विद्यापरक हुआ करते हैं, अतः इन्हें इनके स्वरूप को लेकर व्यवहृत करना ही अधिक समीचीन होगा।
यहाँ ‘व्यवहृत’ पद का प्रयोग विशेष अर्थ का परिसूचक है। इसके अन्तर्गत किसी पूर्व निरूपित सिद्धान्त, मन, अनुसिद्धान्त अथवा नियम का एक विशिष्ट परिस्थिति में अनुप्रयोग किया जाता है। शैक्षिक अनुसंधान के तहत यह परिस्थिति शिक्षण, अधिगम या मूल्यांकन की प्रक्रिया
सम्बन्धित हो सकती है। इस प्रकार के अनुसंधान को, प्रयोगशाला या क्षेत्रीय परिस्थितियों में पूरा किया जा सकता है तथा इसके तहत वैज्ञानिक विधि के सोपानों का अनुसरण होता है।
प्रश्न a (vi) व्यवहृत अनुसंधान की विशेषताएँ ।
उत्तर-व्यवहृत अनुसंधान की विशेषताएँ निम्न प्रकार द्रष्टव्य हैं-
(1) व्यवहृत अनुसंधान का सम्बन्ध यथार्थ की मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार की परिस्थितियों से है क्योंकि इसमें पूर्व अन्वेषित ज्ञान या सिद्धान्त का अनुप्रयोग जीवन की अमूर्त घटनाओं अथवा प्रक्रियाओं के सन्दर्भ में किया जाता है जिससे उससे होने वाले गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सके।
(2) इस सम्बन्ध में विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि व्यवहृत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य एक प्रयोजनवादी समीक्षा या जाँच प्रस्तुत करना है जिससे पूर्व निरूपित नियमों, सिद्धान्तों तथा सामान्यीकरण का किन सम्भव दशाओं में उपयोग किया जा सकता है, इस बात का संकेत प्राप्त हो सके।
(3) व्यवहृत अनुसंधान का सन्दर्भ उन सभी तात्कालिक एवं दीर्घकालिक परिस्थितियों से सम्बद्ध है जिनमें पूर्व ज्ञात सत्यों तथ्यों एवं सिद्धान्तों का प्रयोग संगत कहा जा सकता है।
(4) इस प्रकार व्यवहृत अनुसंधान में जिन प्रश्नों को ध्यान में रखकर शोध कार्य पूरा होता है उनकी मूल प्रकृति, तथ्यों, सम्प्रत्ययों तथा सिद्धान्तों का विविध परिस्थितियों में अनुप्रयोग किये जा सकने की सम्भावना का पता लगाने से जुड़ी रहती है।
(5) ऐसे अनुसंधानों में शोध की परिकल्पना की संरचना की दृष्टि से अपेक्षाकृत मूर्त स्तर पर निरूपित होती है और अधिकतर परिस्थितियों में इसका स्वरूप यदि ऐसा किया जाए तो यह परिणाम घटित होगा अर्थात् एक सोपाधिक प्रतिज्ञप्ति की भाँति व्यक्त होता है।
(6) मौलिक अनुसंधान की भाँति इस प्रकार के शोधों में भी सर्वप्रथम समग्र को परिभाषित करना पड़ता है तथा उससे एक प्रतिनिधि समूह अर्थात् प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है। पूरा अध्ययन इस प्रतिदर्श पर सम्पन्न होता है तथा प्रेक्षित परिणामों को पूरे समग्र पर लागू किया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। इस दृष्टि से मौलिक एवं व्यवहृत अनुसंधानों में पर्याप्त समानता है।
(7) व्यवहृत अनुसंधान के अन्तर्गत शोध का अभिकल्प अर्थात् उसकी रूपरेखा तर्कबद्ध रूप के परिप्रेक्ष्य में प्रायः देखने को मिलता है। यहाँ इतना अन्तर अवश्य होता है कि वे विविध परिस्थितियाँ जिनमें सिद्धान्तों एवं नियमों को लागू किया जाता है, वे अत्यन्त गतिशील प्रकृति रखती हैं। अतः यदा-कदा इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शोध की रूपरेखा में परिवर्तन करना होता है।
प्रश्न b (i) क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा ।
उत्तर- क्रियात्मक अनुसंधान अनुसंधान की नवीनतम शाखा है। विद्यालयों की कार्य-पद्धति में सुधार तथा विकास लाने के लिए यह एक सराहनीय कदम है। इसके अन्तर्गत अनुसंधान कोई विशिष्ट व्यक्ति न होकर विद्यालयों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध रखने वाले लोग ही होते हैं। उनका . उद्देश्य उपाधि प्राप्त करना नहीं होता है। एम.एड., एम.ए. (शिक्षा) एम. फिल् तथा पी.एच डी. की उपाधि के लिए जो शोध ग्रन्थ तैयार हो रहे हैं अथवा जो शोधकार्य हो रहे हैं उन्हें क्रियात्मक अनुसंधान की दृष्टि से कदापि उपयोगी एवं सार्थक नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार के अनुसंधान विद्यालयों की कार्यप्रणाली के अधिक निकट नहीं होते हैं। अनुसंधानकर्ता भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो विद्यालय की क्रियाओं से सर्वथा दूर होता है, उसका विद्यालयी क्रियाओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसके अनुसंधान के परिणाम विद्यालय के अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, प्रबन्धकों तथा निरीक्षकों तक कठिनता से पहुँच पाते हैं और यदि पहुँच भी जाते हैं तो उनका क्रियान्वयन होना असम्भव हो जाता है। क्रियात्मक और मौलिक अनुसंधानों में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि मौलिक अनुसंधान नवीन सत्यों एवं सिद्धान्तों की स्थापना करता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिदिन की व्यावहारिक क्रियाओं में सुधार तथा विस्तार लाने का मार्ग ढूँढ़ता है। क्रियात्मक अनुसंधान में कार्य तथा व्यवहार पक्षों, उनकी उपादेयता तथा गुणवत्ता पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षक अपनी शिक्षण क्रिया, प्रधानाचार्य अपने विद्यालय का प्रबन्धन, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक क्रियाओं तथा व्यवस्थापक एवं विद्यालय निरीक्षक अपनी-अपनी गतिविधियों में उपयुक्त परिवर्तन, संशोधन तथा सुधार विधिवत् रूप में लाने की कोशिश करते हैं। वे अपनी समस्याओं को वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्लेषित करते हैं, उन पर अपेक्षित तटस्थता के साथ विचार करते हैं और उनका निराकरण तथा समाधान प्रयोगात्मक तरीके से प्राप्त करने के लिए सोचते हैं।
जे. बी. बेस्ट के अनुसार, “क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक प्रयोग पर केन्द्रित होता है, न कि किसी सिद्धान्त के विकास पर और न सामान्य प्रयोग पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय अनेक राष्ट्रों के सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि वे अपनी तात्कालिक समस्याओं को शीघ्र- से-शीघ्र कैसे हल करें, क्योंकि मौलिक अनुसंधान में अधिक समय तथा श्रम लगता था। इस प्रकार प्रतिरक्षा के क्षेत्र में संक्रियात्मक अनुसंधान का जन्म हुआ ।
प्रश्न b (ii) क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएँ । अथवा क्रियात्मक शोध की विशेषताएँ ।
उत्तर- स्टीफेन एम. कोरी (1953), जॉन डब्ल्यू. बेस्ट (1980) तथा कोहेन और मैनियन (1980) के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएँ निम्नलिखित बतायी गयी हैं-
(1) क्रियात्मक अनुसंधान परिस्थितिगत शोध है क्योंकि इसके तहत किसी विशिष्ट सन्दर्भ में समस्या का निदान एवं समाधान प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। दूसरे शब्दों में, यह मौके पर किया गया वह अध्ययन है जिसका प्रयोग किसी तात्कालिक परिस्थिति में मूर्त समस्या के सम्बन्ध में किया जाता है।
(2) क्रियात्मक अनुसंधान का सन्दर्भ सर्वथा अनौपचारिक एवं नमनीय होता है। यह यथार्थ अविरत परिप्रेक्ष्य से जुड़े रहने के कारण अत्यन्त गतिशील सन्दर्भों में सम्पन्न होता है।
(3) किसी दी हुई परिस्थिति में कार्यों एवं निर्णयों की गुणवत्ता को सुधारना ही क्रियात्मक ★ अनुसंधान का लक्ष्य होता है जिससे वह परिस्थिति बेहतर एवं उपयोगी सिद्ध हो सके।
(4) क्रियात्मक अनुसंधान के तहत समस्या का चयन यथार्थ के अत्यन्त मूर्त स्तर से होता है, अतः इसका स्वरूप उतना ही स्पष्ट एवं मूर्त रहता है जितना कि स्थानीय परिस्थिति का।
(5) क्रियात्मक अनुसंधान में शोध परिकल्पना प्रस्तावित कार्य तथा उसके प्रत्याशित परिणाम के रूप में निर्मित की जाती है। अतः इसे क्रियात्मक परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है तथा इसका स्वरूप आमतौर से एक सोपाधिक (सशर्त) प्रतिज्ञप्ति अर्थात् ‘ऐसा किया जाएगा तो यह होगा’ के रूप में प्रायः देखा जा सकता है।
(6) क्रियात्मक अनुसंधान का अभिकल्प अनुकूली स्वरूप रखता है जिससे इसके कार्यान्वयन में लचीलापन एवं परिवर्तन सम्भव होता है। चूँकि इस प्रकार के शोध का सन्दर्भ गतिशील होता है, इसकी रूपरेखा को व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित करते समय कठोरता नहीं बरती जा सकती है।
(7) क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य ‘सामान्यीकरण’ निर्मित करना नहीं होता है। इसके तहत यदि किसी प्रकार के सामान्यीकरण की गुंजाइश रहती भी है तो वह भावी परिस्थितियों से सन्दर्भित होने के कारण ‘उदग्र सामान्यीकरण’ के नाम से पुकारा जा सकता है, जबकि मौलिक तथा व्यवहृत अनुसंधान स्वरूपों में यह ‘पाश्विक सामान्यीकरण’ कहलाता है।
प्रश्न b (iv) क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता एवं महत्ता ।
अथवा
क्रियात्मक अनुसंधान का महत्त्व ।
उत्तर- क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता एवं इसका महत्त्व निम्नांकित दृष्टियों से विशेष रूप में दर्शाया जा सकता है-
1. विद्यालयों की कार्य-पद्धति में यथेष्ट सुधार तथा परिवर्तन लाने के लिए।
2. जनतन्त्रात्मक मूल्यों की सुरक्षा हेतु ।
3. वैज्ञानिक आविष्कारों, प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना-प्रौद्योगिकी के आविर्भाव के कारण उत्पन्न नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए।
4. विद्यालयों में यान्त्रिकता एवं रूढ़िवादिता का वातावरण समाप्त करने के निमित्त ।
5. शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबन्धकों तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक अथवा वस्तुनिष्ठ दृष्टि से अपनी कार्यप्रणालियों का मूल्यांकन करने एवं उनमें तदनुकूल परिवर्तन लाने के प्रति समर्थ एवं
क्षमतावान बनाना ।
6. छात्रों की बहुमुखी प्रगति हेतु विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावोत्पादक रीति से आयोजन करने के लिए।
7. विद्यालय की अनेकानेक समस्याओं; यथा-गुणवत्तापरक रूप में विद्यालय प्रबन्धन न कर पाने एवं उपयुक्त शिक्षण विधि के अनुप्रयोग की समस्या, अनुशासन की समस्या, पाठ्यक्रम- सहगामी क्रियाओं को प्रभावोत्पादक बनाने की समस्या, विविध विषयों के पढ़ने में अपेक्षित रुचि उत्पन्न करने की समस्या, विद्यालय के पुस्तकालय का सदुपयोग न कर सकने की समस्या, कुछ विशेष अवसरों पर छात्रों की उपस्थिति की समस्या तथा कक्षा से भाग जाने की समस्या, आदि का सहज समाधान प्राप्त करने हेतु ।
8. विद्यालय के अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को नित्य अपने अनुभवों को समेकित करने एवं उनसे लाभ उठाने में समर्थ बनाने की दृष्टि से ।
9. विद्यालय समाज का लघु रूप है। अतः सामाजिक परिवर्तनों को विद्यालय के पाठ्यक्रम तथा अन्य क्रियाओं द्वारा प्रतिबिम्बित करना चाहिए। इस दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।
2
10. शिक्षकों को परस्पर सहयोग एवं सहानुभूति के साथ कार्य करने का अभ्यासी बनाने के लिए।
11. छात्रों की उपलब्धियों का स्तर बढ़ाने के निमित्त ।
प्रश्न c (i) क्रियात्मक अनुसंधान की वर्तमान में आवश्यकता।
11
उत्तर- विद्यालय की कार्य-पद्धति में कठोरता एवं कठमुल्लेपन का अभाव होना चाहिए। विद्यालयों के अध्यापक, प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धक अपनी क्रियाओं का मूल्यांकन स्वयं करें तथा उनमें अपेक्षित सुधार लाने की चेष्टा अपने स्तर पर करें। जिस विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण नहीं है, जहाँ अध्यापकों एवं प्रधानाचार्य को अपनी कार्य-पद्धति में सुधार लाने की स्वतन्त्रता नहीं है, वह प्रजातन्त्र के विकास एवं गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वथा हानिकारक है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा प्रजातन्त्र की सुरक्षा निश्चित है, क्योंकि इसके अंतर्गत विद्यालय में सबको अपनी क्रियाओं में विकास एवं सुधार लाने के लिए समान अधिकार प्राप्त होता है। इसके द्वारा कार्य प्रणाली में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है।
प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्र की महती विशेषता यह होती है कि नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। वह सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त करने का दावेदार होता है। उसकी क्रियाओं में जो सामाजिक अथवा राष्ट्रीय हित की दृष्टि से की जाती है, कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न कर सकता। उसे अपनी क्रियाओं में सुधार एवं विस्तार लाते समय कोई बाधक नहीं बन सकता। हमारे विद्यालयों में प्रजातन्त्र के इस रूप को चरितार्थ करना होगा। परस्पर सहयोग एवं संगठन के साथ कार्य करने के लिए प्रत्येक अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबन्धक तथा निरीक्षक को कटिबद्ध होना चाहिए। उन्हें अपनी कार्य- प्रणालियों को वैज्ञानिक दृष्टि से आँकना चाहिए। वे अपने मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष बनेँ । निरन्तर इस बात की चेष्टा करें कि विद्यालय में वे जो कुछ करें वह शिक्षा के उद्देश्यों को सन्तुष्ट करने में सहायक हो। तभी प्रत्येक विद्यालय इस प्रकार के अनुसंधान द्वारा अपनी लक्ष्य सिद्धि को सुगम एवं सुंदर बना सकता है।
क्रियात्मक अनुसंधान का महत्त्व अन्य दृष्टियों से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। स्वाधीनता के उपरान्त अपने देश का पुनर्जन्म हुआ। नये राष्ट्र को नई समस्याएँ भी विरासत में मिलीं। शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयों का पुनर्गठन प्रारम्भ हुआ। शिक्षा के उद्देश्य पुनः निर्मित किये गये। पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए कदम उठाये गये। पाठ्य-पुस्तकों के नये स्वरूप सामने आये। शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग पद्धति में भी संशोधन लाया गया और अब भी इन सभी दिशाओं में प्रयत्न जारी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हम सुधार एवं विस्तार लाने की चेष्टा में सहगामी समस्याओं के प्रति उतना सचेत नहीं रह पाये हैं। विद्यालयों में शिक्षण-प्रणाली, पाठ्यक्रमों का अनुसरण एवं क्रियान्वयन, अनुशासन, विद्यालय प्रबन्ध तथा पुस्तकालयों के प्रयोग-विषयक अनेकानेक समस्याएँ, एक भयंकर होड़ के साथ बे-रोक-टोक बढ़ती चली जा रही हैं। यदि इन समस्याओं के प्रति हम सजग नहीं हुए तो शिक्षा के उद्देश्यों पर पानी फिर जायेगा। ‘क्रियात्मक अनुसंधान’ विद्यालयों की बढ़ती हुई समस्याओं का सरल, प्रभावशाली एवं कल्पनाशील हल प्राप्त करने की दिशा में अत्यन्त लाभप्रद युक्ति है। इसके अतिरिक्त विद्यालय की कार्य-प्रणाली में अपेक्षित विकास तथा सुधार लाने के प्रति भी यह सहायक होगा।
प्रश्न c (ii) कक्षा-कक्षों में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता।
उत्तर- कक्षा-कक्षों में सुधार के दृष्टिकोण से क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। कक्षा-कक्षों में सुधार लाने के लिए विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धकों को अपनी क्रियाओं का स्वयं अवलोकन करना चाहिए तथा उनमें अपेक्षित सुधार लाने की चेष्टा अपने स्तर पर करनी चाहिए। जिस विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण नहीं होता है वहाँ प्रजातन्त्र का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा कक्षा-कक्षों में शिक्षक को अपनी कार्यपद्धति में सुधार लाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वह अपनी क्रियाओं का विकास कर सकता है तथा उनमें सुधार लाने का उसे अधिकार प्राप्त होता है। इसके द्वारा कार्य प्रणाली में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है।
प्रश्न c (iii) कक्षा-कक्ष में सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान ।
उत्तर-क्रियात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित पदों का अनुसरण किया जाना चाहिए- (i) समस्या की पहचान, मूल्यांकन एवं निरूपण, (ii) समस्या में रुचि रखने वाले दलों के बीच प्रारंभिक विवेचन एवं वार्ता जो कि प्रस्तावित मसौदे के रूप में समाप्त हो, (iii) सम्बन्धित अनुसंधान साहित्य का पुनर्विलोकन (iv) प्रथम स्तर पर बनाए हुए पहले कथन का रूपांतर करना तथा पुनः परिभाषित करना, (v) अनुसंधान कार्यविधि का चयन, (vi) मूल्यांकन प्रविधियों का निर्धारण, (vii) योजना का कार्यान्वित होना, (viii) परिणामों की व्याख्या करना, (ix) उन पर विवेचन करना तथा निष्कर्ष निकलना, (x) सामान्य संक्षिप्त विवरण।
1. प्रश्न d (i) मौलिक शोध के उदाहरण |
उत्तर – शैक्षिक प्रसंगों में मौलिक शोध के कतिपय उल्लेखनीय उदाहरण हैं-जीन पियाजे द्वारा बालक के यथार्थ जगत् एवं कार्य-कारण सम्बन्ध की अवधारणा के बारे में किये गये अध्ययन, प्रोफेसर बी. एफ. स्किनर द्वारा अभिक्रमित अनुदेशन की पद्धति एवं शिक्षण यन्त्रों से सम्बन्धित प्रयोग, मैक्लीलैण्ड एवं एटकिन्सन के शोधों के माध्यम से अन्वेषित ‘निष्पत्ति अभिप्रेरण (एचीवमेण्ट मोटिवेशन) का नवीन सम्प्रत्यय, नेड फ्लैण्डर्स के नेतृत्व में कक्षा-शिक्षण की परिस्थिति में शिक्षण-व्यवहार को दृष्टिगत रखकर निरूपित 2/3 का नियम, हमारे यहाँ महात्मा गाँधी के क्रान्तिक विचारों को आधार बनाकर बुनियादी तालीम के तहत ‘तकली- केन्द्रित’ शिक्षा की व्यवस्था तथा अरबिन्द की आश्रम प्रणाली- ये सभी शिक्षा के क्षेत्र में ‘मौलिक अनुसंधान’ के उदाहरण कहे जा सकते हैं क्योंकि इन अवधारणाओं एवं व्यवस्थाओं ने शिक्षा एवं शिक्षण की दिशा में एक नवीन पद चिह्न सृजित किये हैं तथा शिक्षण के बारे में चली आ रही धारणाओं को चुनौती देकर नये मानक कायम करने में सहायक रहे हैं। यहाँ ध्यान देना होगा कि पूर्वोल्लिखित उदाहरण शिक्षा के क्षेत्र में ‘मौलिक अनुसंधान’ माने जा सकते हैं, किन्तु इनका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा है। इनके अतिरिक्त अन्य कई दृष्टान्त चुने जा सकते हैं जो शिक्षा के औपचारिक एवं निरौपचारिक सन्दर्भों से सम्बद्ध अवधारणाओं को विकसित एवं परिष्कृत करने में महत्त्वपूर्ण रहे हैं।
प्रश्न d (ii) मौलिक अनुसंधान एवं शिक्षण-अधिगम सीमाएँ ।
उत्तर- ये निम्नलिखित हैं-
(1) समाज विज्ञान तथा व्यवहारवादी, विज्ञान के अनेक अनुक्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान के प्रयोग किये जाने की सम्भावना प्रायः नहीं के बराबर है।
(2) मौलिक अनुसंधानों में कठोरता एवं नियन्त्रण जैसे मुद्दे इसको पूरा करने में अत्यन्त आवश्यक माने जाते हैं।
(3) शैक्षिक गोचरों तथा शैक्षिक प्रक्रियाओं को निरूपित सिद्धान्तों एवं परिष्कृत अवधारणाओं के जरिए स्पष्ट करने में प्रायः कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इनका स्वरूप आत्मनिष्ठ तथा विवादास्पद होता है, यही कारण है कि शैक्षिक शोधों में सम्पन्न इस प्रकार के शोध परिमाणात्मक दृष्टि से अत्यन्त स्वल्प हैं।
(4) इसमें नवीन ज्ञान, सत्य या सिद्धान्त तक पहुँचने के लिए सामान्यीकरण का अवलम्ब ग्रहण करना परमावश्यक होता है।
प्रश्न d (iii) व्यवहृत अनुसंधान के उदाहरण ।
उत्तर- शैक्षिक अनुसंधान के तहत इस प्रकार के शोधों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी, अभिक्रमित अधिगम, कक्षा-शिक्षण में अन्तःक्रिया, मापन एवं मूल्यांकन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण विद्यालय-वातावण, शैक्षिक प्रबन्ध तथा शैक्षिक परिस्थितियों में नेतृत्व, आदि से जुड़े शोध अधिकतर व्यवहृत अनुसंधान की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी में जो शोध
हुए हैं वे प्रायः विभिन्न शैक्षिक व्यवस्थाओं में मृदु उपागम एवं कठोर उपागम की अनेकानेक युक्तियों के अनुप्रयोग की सम्भाविता तथा उनकी प्रभाविता के आकलन से सम्बन्धित हैं। अभिक्रमित अधिगम के क्षेत्र में परिणामों की तात्कालिक एवं विलम्बित जानकारी के रूप में प्रतिपुष्टि, पदों के आकार एवं अनुक्रिया-माध्यम तथा व्यक्तिगत एवं सभी द्वारा निर्दिष्ट गति के आधार पर अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रस्तुतीकरण, आदि से सम्बद्ध अध्ययन स्पष्ट व्यवहृत अनुसंधान के नमूने हैं। पूर्व सन्दर्भित अन्य क्षेत्रों में भी अनेक ऐसे शोधों का उल्लेख किया जा सकता है जो इसी प्रकार के अनुसंधान की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। व्यवहृत पद का प्रयोग विशेष अर्थ परिसूचक होता है। इस प्रकार के शोध को प्रयोगशाला अथवा शैक्षिक परिस्थितियों में सम्पन्न किया जा सकता है।
प्रश्न d (iv) व्यवहृत अनुसंधान एवं शिक्षण अधिगम सीमाएँ।
उत्तर- ये निम्नलिखित हैं-
(1) यह सर्वविदित है कि हमारी व्यवहारिक परिस्थितियाँ जिनमें पूर्व अन्वेषित सत्यों, सिद्धान्तों एवं सामान्यीकरण को लागू करना होता है अत्यन्त गतिशील, अस्पष्ट एवं जटिल होती हैं। उन पर कठोर नियम तथा एक ठोस संरचनात्मक स्वरूप आरोपित कर सकना सम्भव नहीं है।
(2) व्यवहृत अनुसंधान के परिणामों को अन्य परिस्थितियों में सामान्यीकरण की सम्भावना सी रहती है तथा पूरा शोध उपक्रम समय एवं धन की दृष्टि से अपेक्षाकृत खर्चीला बन जाता है। ऐसे शोधों में निष्कर्ष विश्वसनीयता तथा वैधता दोनों ही पैमानों पर प्रायः विवाद के घेरे में सरलता से आ जाते हैं।
(3) व्यवहृत अनुसंधानों का लक्ष्य ज्ञान की परिधि में विस्तार करने या किसी सिद्धान्त में विकास के प्रति उन्मुख नहीं होते हैं, बल्कि निरूपित सिद्धान्त या पूर्व अन्वेषित ज्ञान को कहाँ, कब और कैसे प्रयोग में लाया जाए जिससे जीवन की परिस्थितियों में उनका उपयोग हो यह पता लगाने तक सीमित होता है।
प्रश्न e (i) क्रियात्मक अनुसंधान का उदाहरण ।
उत्तर-शिक्षा के औपचारिक तथा निरौपचारिक सन्दर्भों में विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय किसी भी स्तर पर क्रियात्मक अनुसंधान की विधि अपनाए जाने के अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जा सकते हैं। ऐसे शोधों में शिक्षक, प्रधानाचार्य या शैक्षिक प्रशासक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में एक टीम की भाँति अनुसंधानकर्ता की भूमिका अदा कर सकते हैं। कोहेन तथा मैनियन द्वारा इंगित आगे दिये गये उदाहरण क्रियात्मक अनुसंधान के सन्दर्भों को उजागर तो करते हैं, किन्तु इन्हें ऐसे दृष्टान्तों की पूर्ण सूची के रूप में सर्वथा नहीं लेना चाहिए।
क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रकार का हस्तक्षेप है जो-
(1) कार्य की प्रेरक-शक्ति के रूप में कार्यशील होता है। इसका उद्देश्य अन्य विकल्पों की तुलना में किसी कार्य को अत्यधिक कुशलता एवं शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराना है।
(2) व्यक्तिगत कार्यशीलता, मानवीय सम्बन्धों एवं नैतिकता की ओर प्रवृत्त होता है तथा इस प्रकार कार्यकर्ताओं की कार्य-कुशलता, उनकी अभिप्रेरणाओं, सम्बन्धों तथा कल्याण से सम्बन्धित होता है।
(3) कार्य-विश्लेषण पर बल देता है तथा इसका उद्देश्य व्यावसायिक प्रकार्यता तथा कार्य- कुशलता में सुधार लाना है।
(4) यह संगठनात्मक परिवर्तनों से सम्बन्धित होता है जहाँ तक कि इसके द्वारा व्यापार एवं उद्योग में उन्नत प्रकार्यता प्राप्त होती है।
(5) सामान्यतः सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में यह नियोजन तथा नीति-निर्धारण से सम्बन्धित
(6) नव-प्रवर्तन एवं परिवर्तन तथा चल रही व्यवस्था में इन्हें कैसे लागू किया जा सकता है ? से सम्बद्ध है।
(7) किसी भी सन्दर्भ में जहाँ किसी समस्या-विशेष के समाधान की आवश्यकता हो, समस्या के हल प्राप्त करने पर बल देता है।
(8) सैद्धान्तिक ज्ञान के विकास हेतु अवसर प्रदान करता है। यह विधि के शोध-अंश पर अधिक जोर होता है।
प्रश्न e (ii) एक विद्यालय के संगठनात्मक वातावरण एवं सहविद्यालीय क्षेत्रों में शिक्षण अधिगम की प्रासंगिकता ।
उत्तर-क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सिद्धान्त निरूपण या सिद्धान्त परीक्षण न होकर किसी परिस्थिति विशेष में पाई जाने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है अर्थात् परिस्थिति में सुधार करना है न कि सामान्यीकरण करना।
कोहेन तथा मैनियन ने शिक्षण अधिगम के सन्दर्भ में क्रियात्मक अनुसंधान के पाँच लक्ष्यों का उल्लेख किया है जिससे विद्यालयों में संगठनात्मक वातावरण सकारात्मक बना रहे। ये लक्ष्य भारतीय सन्दर्भ में भी अपनी प्रासंगिकता रखते हैं-
(1) यह खास परिस्थितियों में पहचानी गई समस्याओं या दी हुई परिस्थितियों को कुछ खास रूप में सुधारने का तरीका है।
(2) यह सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का तरीका है जिसमें शिक्षक को नई विधियों एवं कुशलताओं में दीक्षित किया जाता है, उसकी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को तीव्र बनाया जाता है तथा आत्म- अभिज्ञता के स्तर को समुन्नत किया जाता है
(3) यह प्रचलित परम्परागत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत शिक्षण एवं अधिगम की परिस्थितियों में अतिरिक्त या नव-प्रवर्तनात्मक उपागमों का सन्निवेश करने का तरीका है, क्योंकि ये व्यवस्थाएँ प्रायः परिवर्तन तथा नवप्रवर्तन के प्रति प्रतिरोध खड़ा करती हैं।
(4) यह अभ्यासकर्ता शिक्षक एवं शैक्षणिक शोधकर्ता के मध्य आमतौर से पाई जाने वाली स्वल्प सम्प्रेषण तथा परम्परागत अनुसंधान द्वारा स्पष्ट विहितीकरण या निर्देश न दे पाने की स्थिति को सुधारने का तरीका है।
(5) इसके तहत वास्तविक रूप में वैज्ञानिक शोध की कठोरता का अभाव होते हुए भी आत्मनिष्ठ एवं प्रभाववादी उपागम द्वारा कक्षा शिक्षण की समस्या का समाधान प्राप्त करने की तुलना में अपेक्षाकृत वरीय (अधिमान्य) विकल्प प्रदान करने का तरीका कहा जा सकता है।
प्रश्न e (iii) क्रियात्मक अनुसंधान एवं शिक्षण अधिगम सीमाएँ ।
उत्तर- क्रियात्मक अनुसंधान एवं शिक्षण अधिगम सीमाएँ निम्नलिखित हैं-
(1) क्रियात्मक अनुसंधान के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि इसके द्वारा तथा सामान्य बुद्धि प्रयोग द्वारा समस्या समाधान ढूँढ़ निकालने की पद्धति में कोई अन्तर नहीं है।
(2) क्रियात्मक अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य तथा सन्दर्भ की भी आलोचना की जाती है। क्योंकि इसमें स्पष्टता तथा वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है जिससे वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करना कठिन हो जाता है।
(3) इसके तहत सामान्यीकरण का निर्माण करना सम्भव एवं वांछनीय उद्देश्य नहीं माना जाता है जो वैज्ञानिक ज्ञान के समर्थन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।
कोरी ने भी इस ओर संकेत किया है कि क्रियात्मक अनुसंधान को एक सहयोगात्मक प्रयास का रूप देना इसे उतना ही पेचीदा बना देता है जो सामूहिक कार्य के सम्पादन में प्रायः देखने को मिलता है।
अतः क्रियात्मक अनुसंधान का परिस्थितिगत परिप्रेक्ष्य एवं इसका नमनीय स्वरूप जहाँ इसे लोकप्रिय बनाने में सफल रहा है, वहीं वैज्ञानिक विधि के अनुप्रयोग की दृष्टि से भी इसकी सीमा है।
प्रश्न e (iv) क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं का चयन।
उत्तर-शैक्षिक प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान हेतु विभिन्न सम्भावनाएँ निहित हैं। विशेषकर विद्यालय की कार्य-प्रणाली में सुधार तथा प्रगति लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान आज आवश्यक माना जाने लगा है। प्रत्येक अनुसंधान कार्य का प्रारम्भ किसी समस्या विशेष से होता है। जब तक अनुसंधानकर्ता समस्या का प्रत्यक्षीकरण भली प्रकार नहीं करता, अनुसंधान की भूमिका प्रस्तुत नहीं हो सकती। हमारे विद्यालयों में क्रियात्मक अनुसंधान की दृष्टि से अनेक समस्याएँ अध्ययन का विषय बन सकती हैं और उनके समाधान द्वारा विद्यालय की कार्य-पद्धति में सुधार एवं विकास हेतु मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय के उर्वर- प्रांगण में क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा अनेकानेक सुधार योजनाओं का श्रीगणेश सम्भव है, जिनके बीज शीघ्र अंकुरित हो सकेंगे और निकट भविष्य में एक सुन्दर विकास-वृक्ष का रूप धारण कर लेंगे।
क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं का चयन विद्यालय तथा उसके कार्यकर्ताओं की कार्य- प्रणाली को अशोधित एवं संवर्द्धित करने की दृष्टि से करना चाहिए। यदि अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य अपने विद्यालय की समस्याओं को जानना समझना प्रारम्भ करें तो उन्हें प्रत्येक पग पर समस्याओं के दर्शन होंगे। सम्पूर्ण विद्यालय की परिस्थिति समस्याओं का एक अद्भुत कोष प्रतीत होगी। समस्याओं को देखने के लिए एक विशेष दृष्टि अपनानी पड़ती है। इस दृष्टि को हम वैज्ञानिक अथवा वस्तुनिष्ठ दृष्टि की संज्ञा दे सकते हैं। जब तक हम तटस्थ भाव से अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन करना नहीं सीखते, तब तक हमें परिस्थितियों के बाधक तत्त्वों का पता नहीं लग पाता है। इसके अतिरिक्त हमें परिस्थितियों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए तभी हम समस्याओं की पहचान कर सकते हैं।
समस्याओं को पहचानने में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धान्त काम करता है। एक ही परिस्थिति में कुछ व्यक्तियों को समस्या दिखाई पड़ती है तो कुछ को नहीं। जिसे हम समस्या के रूप में देखते हैं, उसे दूसरा व्यक्ति देख भी नहीं पाता। सभी अध्यापक विद्यालय के पुस्तकालय में नित्य जाते हैं परन्तु उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो पुस्तकालय का उचित उपयोग न होने से व्यग्रता का अनुभव करते हैं। कहने का आशय यह है कि समस्या के प्रति संवेदनशीलता किसी में कम होती है और किसी में अधिक होती है। अतः क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का चयन अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, निरीक्षकों एवं प्रबन्धकों की व्यक्तिगत संवेदनशीलता पर निर्भर होता है।
प्रश्न f (i) क्रियात्मक अनुसंधान एवं समस्याओं के स्रोत ।
अथवा
क्रियात्मक शोध समस्या के स्रोत ।
उत्तर- क्रियात्मक अनुसंधान की सभी समस्याएँ विद्यालय की कार्य-पद्धति से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होती हैं। प्रत्येक समस्या का उद्गम विद्यालय की कार्यप्रणाली में ढूँढ़ा जा सकता है। विद्यालय की समस्याओं का स्रोत विद्यालय की कार्य-प्रणाली को ही मानना समीचीन है। परन्तु स्पष्टता के लिए मूल स्रोत को चित्र में व्यक्त किया गया है जिसमें समस्याओं को चार वर्गों में विवेचित किया जा सकता है-
1. शिक्षण से सम्बन्धित समस्याएँ,
2. परीक्षण से सम्बन्धित समस्याएँ,
3. पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के आयोजन से सम्बन्धित समस्याएँ, तथा
4. विद्यालय के संगठन तथा प्रबन्धन की गुणवत्ता से सम्बन्धित समस्याएँ ।
प्रश्न f (ii) शिक्षण से सम्बन्धित समस्याएँ ।
17 |
–
उत्तर – शिक्षण से सम्बन्धित समस्याएँ-शिक्षण-क्रिया का अन्तिम लक्ष्य, बालक के व्यवहारों में परिवर्तन लाना होता है। वह व्यवहार-परिवर्तन बालक के आन्तरिक तथा बाह्य दोनों पक्षों में होते हैं। विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों द्वारा इस प्रकार के व्यवहार परिवर्तन लाए जाते हैं। शिक्षक अपनी शिक्षण-विधि, सहायक सामग्री तथा अन्य उपयोगी साधनों का प्रयोग इसलिए करता है ताकि बालक के व्यवहारों में अभीष्ट परिवर्तन आ सके। इस प्रकार शिक्षण- प्रक्रिया से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ जुड़ी हुई हैं। ये समस्याएँ शिक्षक तथा शिक्षार्थी— दोनों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। इन समस्याओं को मुख्यतः निम्नांकित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है-
(i) पाठ्य-वस्तु को समझने की समस्या ।
(ii) उपयुक्त शिक्षण-विधि की समस्या ।
(iii) शिक्षक-शिक्षार्थी सम्बन्ध विषयक समस्याएँ ।
(iv) कक्षा में शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करने की समस्या ।
(v) छात्रों में परस्पर सामंजस्य एवं सम्प्रेषणीयता की समस्या ।
(vi) गृह-कार्य तथा लिखित कार्य की समस्या ।
(vii) सस्वर तथा मौन वाचन की समस्या ।
(viii) वर्तनी की समस्या ।
(ix) प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति (लिखित तथा मौखिक) की समस्या ।
(x) शुद्ध उच्चारण की समस्या ।
(xi) अध्येय विषय में छात्रों की रुचि न लेने तथा अनवधान विषयक समस्याएँ ।
(xii) कक्षा में विलम्ब से आने की समस्या ।
अनुभवी शिक्षक अपनी समस्याओं का वर्गीकरण पूर्व वर्णित किसी-न-किसी श्रेणी में अवश्य
प्राप्त कर लेगा। इन समस्याओं को अच्छी प्रकार परिभाषित एवं सीमांकित करने के बाद ही अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया जा सकता है।
प्रश्न f (iii) परीक्षण से सम्बन्धित समस्याएँ।
उत्तर – शिक्षण तथा परीक्षण दोनों विद्यालय की महत्त्वपूर्ण क्रियाएँ हैं। छात्रों की उपलब्धियों का मापन नितान्त आवश्यक है। इसके द्वारा छात्रों की प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। विद्यालयों में परीक्षण से सम्बन्धित समस्याओं को समझने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक तथा प्रधानाचार्य शिक्षा के उद्देश्यों को न भूलें। वे परीक्षण को एक महत्त्वपूर्ण क्रिया के रूप में समझें ।
आजकल शिक्षा में मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जा रहा है। मूल्यांकन के अन्तर्गत विद्यार्थी को ही केन्द्र मानकर परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। अध्यापक को अपने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक मूल्यांकन की विधियों में पर्याप्त सुधार लाना चाहिए। परीक्षण से सम्बन्धित समस्याओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है-
(i) परीक्षण विधि की विश्वसनीयता एवं वैधता की समस्या ।
(ii) परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले परखों के निर्माण की समस्याएँ ।
(iii) विविध परखों के प्रयोग की समस्याएँ ।
(iv) परीक्षाओं द्वारा छात्रों की उपलब्धियों को बढ़ाने की समस्या ।
(v) परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों में छात्रों को अधिक विकल्प देने की समस्या ।
(vi) प्रश्न-पत्रों में निबन्धात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परखों के समन्वय की समस्या ।
(vii) निदानात्मक परखों का निर्माण एवं उनका प्रयोग कब तथा किस उद्देश्य से किया जाए, इससे सम्बन्धित समस्याएँ ।
(viii) परीक्षण तथा शिक्षण में समन्वय लाने की समस्या ।
परीक्षण से सम्बन्धित इन समस्याओं पर क्रियात्मक अनुसंधान की योजना अध्यापक एवं प्रधानाचार्य – दोनों के सहयोग होने पर ही कार्यान्वित हो सकती है। इनमें से कुछ समस्याओं का अध्ययन स्वयं करेगा किन्तु प्रधानाचार्य की सम्मति अथवा सहयोग के बिना यह कदापि सम्भव नहीं हो सकता। अनुसंधान प्रारम्भ करने से पूर्व इन समस्याओं के स्वरूप को और विश्लेषित करना होगा।
प्रश्न f (iv) पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के आयोजन से सम्बन्धित समस्याएँ ।
उत्तर- प्रत्येक विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। इन क्रियाओं द्वारा बालकों का सामाजिक, सांवेगिक एवं चारित्रिक विकास करना परम उद्देश्य है। बालकों में प्रजातान्त्रिक गुणों, यथा- परस्पर सहयोग, सहिष्णुता एवं मैत्री भाव से किसी कार्य को करना, नेतृत्व ग्रहण की क्षमता, आदि का संचार किया जाता है तथा उन्हें भावात्मक एकता की ओर आकर्षित किया जाता है। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस प्रकार के सामाजिक सदस्य चाहिए, उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी विद्यालयों तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं पर होती है। इसी दृष्टि से विद्यालय के अन्तर्गत विविध क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ विद्यालय में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन क्रियाओं के आयोजन में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के सम्यक् संचालन पर ही विशेष रूप से निर्भर करता है। विद्यालय समाज की क्रियाओं का लघु रूप में प्रतिनिधित्व करता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ समाज में बड़े पैमाने पर सम्पादित होने वाली क्रियाओं का उत्तरदायित्व ग्रहण करने में छात्रों को सक्षम बनाती हैं तथा इनके द्वारा विद्यालय में एक ‘सामूहिक रूप में जीवनयापन’ के संस्कार विकसित होते हैं
क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। इन क्रियाओं से विद्यालय की गतिविधियों में सामाजिक चेतना का प्राण फूँका जा सकता है। उन्हें विद्यालय तथा उसमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए सर्वथा लाभदायक बनाया जा सकता है। इन क्रियाओं की व्यवस्था करते समय अध्यापक तथा प्रधानाचार्य कतिपय समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ये समस्याएँ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को सार्थक बनाने में बाधक होती हैं। इस प्रकार की समस्याओं को निम्नांकित रूप में विभाजित किया जा सकता है-
(i) पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में छात्रों द्वारा स्वयं रुचि न लेना ।
(ii) इन क्रियाओं के संगठन में उद्देश्य विहीनता की समस्या ।
(iii) विविध पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं; यथा वाद-विवाद प्रतियोगिता, अन्त्याक्षरी, प्रहसन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदि का विद्यालय की परम्परा तथा औपचारिक कार्यवाही या रस्म अदायगी के रूप में आयोजन।
(iv) अध्यापकों द्वारा इन क्रियाओं में यथेष्ट रुचि एवं उत्साह का प्रदर्शन न किये जाने की समस्या ।
(v) विविध पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का विधिवत् आयोजन न होना।
(vi) पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को विद्यालय का आडम्बर मात्र समझने की समस्या।
(vii) पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संगठन हेतु अपेक्षित साधनों का अभाव। (viii) पाठ्यक्रम में निर्धारित संज्ञानात्मक संज्ञानेत्तर क्रियाओं में परस्पर समन्वय लाने की समस्या ।
इन समस्याओं का क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से हल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक एवं प्रधानाचार्य दोनों ही प्रयत्नशील हों। विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन कर लेना सर्वथा उपयुक्त होगा।
प्रश्न g (i) विद्यालय के संगठन एवं प्रावधान की गुणवत्ता से सम्बन्धित समस्याएँ ।
उत्तर-प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में विद्यालयों को एक गम्भीर उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। विद्यालय का प्रबन्धन इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि अध्यापक वर्ग तथा छात्रों में अपने राष्ट्र की जरूरतों, अपेक्षाओं एवं मूल्यों के प्रति चेतना उत्पन्न हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय के संगठन एवं प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान प्रजातान्त्रिक तरीके से किया जाय। क्रियात्मक अनुसंधान इस प्रकार की समस्याओं के लिए सर्वोत्तम युक्ति है। इस क्षेत्र में अधोलिखित प्रकार की समस्याओं का उल्लेख किया जा सकता है-
(i) विद्यालय में विविध क्रियाओं (जैसे-शिक्षण, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ, परीक्षण आदि) में समन्वय लाने की समस्या ।
(ii) विद्यालय में शैक्षिक वातावरण निर्मित करने की समस्या ।
(iii) अध्यापकों में परस्पर सहयोग एवं संगठन के साथ कार्य करने के प्रति प्रेरणा प्रदान करना ।
(iv) विद्यालय के अन्तर्गत अध्यापक संघ तथा छात्र संघ के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण ।
(v) विद्यालय में अनुशासन की समस्या ।
(vi) विद्यालय के पुस्तकालय तथा वाचनालय में पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने की समस्या ।
(vii) कक्षा-गृहों को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाये रखने की समस्या ।
(viii) विविध विषयों (यथा-विज्ञान, भूगोल, इतिहास, आदि) के कक्षा-गृहों में पर्याप्त साज-सामान का प्रबन्ध करना।
(ix) अध्यापकों तथा छात्रों में अन्तर्मानवीय सम्बन्धों की समस्याएँ ।
(x) विद्यालयों में भावात्मक एकता की समस्या ।
(xi) विद्यालय के स्तर को ऊँचा उठाने की समस्या।
(xii) विद्यालय में सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्ध के तरीकों एवं रणनीतियों को अपनाने की समस्या । विद्यालय के संगठन तथा प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान शिक्षा की दृष्टि से बड़ा ही मूल्यवान होता है। विद्यालयों में समुचित वातावरण का सृजन आज की एक विशेष
आवश्यकता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा इस प्रकार का वातावरण सहज ही निर्मित किया ज सकता है। अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को चाहिए कि विद्यालय के संगठन तथा प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्याओं का चुनाव परस्पर विचार-विमर्श के आधार पर करें।
प्रश्न g (ii) क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं का चयन।
उत्तर – समस्याओं का चयन सरल कार्य नहीं है। जिस परिस्थिति में हम कार्य करते हैं, उसे आलोचनात्मक एवं तटस्थ दृष्टि से देखने पर ही समस्याओं का पता लग सकता है। हम लोगों में से कितने ही व्यक्ति समस्याओं को देखने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों को अनुसंधान की भाषा में समस्यान्ध की संज्ञा दी जा सकती है। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्याओं का चुनाव करने के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उन कठिनाइयों के बारे में संवेदनशील बनें जो उन्हें अपने कार्यों में बाधा पहुँचाती हैं। तत्पश्चात् कतिपय कठिनाइयों की एक सूची स्वयं निर्मित करनी चाहिए। इन कठिनाइयों के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए उन्हें अनुसंधान के लिए उपयुक्त ‘समस्या’ मिल जायेगी।
क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का चयन करते समय निम्नांकित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए-
(1) समस्या का सम्बन्ध विद्यालय से हो। विद्यालय की कार्य-प्रणाली में उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए ।
(2) समस्या का अध्ययन विद्यालय के अन्दर सम्भव हो क्योंकि इस प्रकार के अनुसंधान विद्यालय के व्यक्ति ही समस्या का अध्ययन करते हैं।
(3) समस्या का अस्तित्व वास्तविक रूप में हो अर्थात् समस्या काल्पनिक न हो।
(4) समस्या अनुसंधानकर्ता के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो अर्थात् समस्या का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उस व्यक्ति से होना चाहिए, जो उसे अनुसंधान का विषय बना रहा है
(5) समस्या के समाधान की वास्तविक आवश्यकता हो ।
(6) समस्या का क्षेत्र न तो अत्यन्त व्यापक हो और न अत्यन्त संकुचित हो ।
(7) समस्या का अपेक्षित स्तर तक ‘वस्तुनिष्ठ विश्लेषण’ सम्भव हो ।
(8) समस्या का जिस परिस्थिति से सम्बन्ध हो, उसका निश्चित पता हो।
(१) समस्या का सम्बन्ध जिस व्यक्ति से हो, वह स्वयं उसका प्रत्यक्षीकरण करे।
प्रश्न g (iii) क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या के चयन में महत्वपूर्ण तत्व ।
उत्तर-क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का चयन कुछ विशेष तत्त्वों पर आधारित होता है। इन तत्त्वों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं-
1. अनुभूति आवश्यकता – सामान्य परिस्थिति में जब तक हमें परिवर्तन एवं सुधार आवश्यकता का अनुभव नहीं होता, समस्याओं को पहचानना कठिन होता है। अनुसंधान के लिए की
हैं। व्यक्ति किसी समस्या का चुनाव तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह अभिप्रेरित न हो। समस्याओं का चुनाव करने के निमित्त यह एक आधारभूत तत्त्व है। इसे हम प्रेरणा भी कह सकते। यह तथ्य प्रत्येक कार्य के लिए महत्त्वपूर्ण होता है।
2. परिस्थितियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण-जिस परिस्थिति में हम कार्य करते हैं, उसका तटस्थ रूप में विश्लेषण किये बिना अनुसंधान हेतु समस्याओं का चयन नहीं किया जा सकता। जब हम किसी कार्य को करते समय व्यक्तिगत रूप से लिप्त होते हैं तो उपयुक्त समस्याओं की पहचान नहीं हो पाती है, किन्तु वस्तुनिष्ठ ढंग से उस कार्य-पद्धति का विश्लेषण करने पर अनेक समस्याएँ दृष्टिगोचर होने लगती हैं।
3. परिस्थितियों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि- परिस्थितियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि उनके प्रति आलोचनात्मक दृष्टि रखी जाय। बहुधा स्वस्थ आलोचनाएँ अनुसंधान के निमित्त कई समस्याओं को जन्म देती हैं।
4. गोष्ठियाँ एवं विचार-विमर्श – अनुसंधान के लिए समस्याओं का चयन करने के निमित्त गोष्ठियों की सहायता ली जा सकती है। अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए विचार-विमर्श पद्धति अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध होती है। इस प्रकार अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबन्धक एवं निरीक्षक शैक्षणिक गोष्ठियों एवं विचार-विमर्श सभाओं के माध्यम से क्रियात्मक अनुसंधान के लिए अनेक उपयुक्त समस्याओं का चुनाव सरलतापूर्वक कर सकते हैं। जब विद्यालय की परिस्थितियों के बारे में कई प्रबुद्ध मस्तिष्क एक साथ विचार करेंगे तो निश्चय ही उत्तम फल प्राप्त होंगे। विद्यालय की समस्याओं को पहचानने का सबसे सुगम ढंग विचार-विमर्श है। समूह में विचार करने से हमें एक-दूसरे के चिन्तन का ज्ञान होता है। हम दूसरों के विचारों से अवगत होते हैं। हमें अपनी कूपमण्डूकता से ऊपर उठने का संकेत प्राप्त होता है। सामूहिक चिन्तन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें किसी परिस्थिति अथवा विषय-विशेष पर एक साथ कई दृष्टिकोण उपलब्ध हो जाते हैं। अनुसंधान के निमित्त समस्याओं का चुनाव गोष्ठियों तथा विचार-विमर्श सभाओं के माध्यम से करना अधिक विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक भी है।
5. विद्यालय की प्रक्रियाओं में अन्तर्दृष्टि-समस्या का चुनाव इस बात पर भी निर्भर होता है कि कार्यकर्ताओं (यथा-अध्यापक, प्रधानाचार्य अथवा निरीक्षक) में विद्यालय की प्रक्रियाओं के समझने की दृष्टि से किस प्रकार की सूझ अथवा अन्तर्दृष्टि विद्यमान है। सूझ का सम्बन्ध प्रायः हमारे अनुभवों से होता है। अनुभवों की दृष्टि से हम जितना समृद्ध बन जाते हैं, हमारी अन्तर्दृष्टि भी उतनी ही पैनी होती रहती है। इसीलिए सही अर्थ में अनुभवी व्यक्ति नौसिखियों की तुलना में समस्याओं को शीघ्रतापूर्वक इंगित कर देते हैं।
प्रश्न g (iv) क्रियात्मक परिकल्पना का अर्थ एवं महत्व।
उत्तर-परिकल्पनाएँ अनुसंधान को दिशा प्रदान करती हैं। इनके द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त करने का संकेत मिलता है। प्रत्येक अनुसंधान में परिकल्पनाओं का विशेष महत्त्व है। क्रियात्मक अनुसंधान में परिकल्पनाओं को विशेष नाम से पुकारा जाता है। इन्हें क्रियात्मक परिकल्पना कहा जाता है क्योंकि इनके अन्तर्गत ‘क्रिया’ के प्रति स्पष्ट उल्लेख रहता है।
अनुसंधान में परिकल्पना शब्द का प्रयोग एक ऐसे कथन के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा किसी समस्या के सम्भव समाधानों का बोध होता है। परिकल्पना में सदैव ज्ञात से अज्ञात की ओर के पक्षों का अनुमान किया जाता है। इसका स्वरूप अस्थायी अथवा आजमायशी होता है। इसी के आधार पर नए सिद्धान्तों का निर्माण किया जाता है, किन्तु परिकल्पना को सिद्धान्त का रूप धारण करने में बहुत समय लगता है। कई प्रयोगों द्वारा परिकल्पना का सत्यापन करने पर ही उसे सिद्धान्त का रूप दिया जा सकता है।
परिकल्पना के महत्त्व को बताते हुए हिलड्रेथ होक मैकाशन ने कहा है कि “शोध में परिकल्पना की भूमिका को अत्यधिक रूप में रेखांकित करना सम्भव नहीं है। यह पूरे अध्ययन का केन्द्रवर्ती बिन्दु होती है जिससे संकलित किये जाने वाले प्रदत्तों के चयन में निर्देश प्राप्त होता है। प्रयोगात्मक अभिकल्प निश्चित होता है, सांख्यिकी विश्लेषण के तरीके तय होते हैं तथा पूरी अध्ययन की प्रणाली के बारे में संकेत मिलता है।”
क्रियात्मक परिकल्पना विद्यालयों की कार्य-प्रणाली में सुधार और प्रगति लाने के लिए बनायी जाती है। इनके द्वारा समस्याओं का समाधान प्राप्त होने का संकेत मिलता है। इसकी सत्यता का पता कम समय में लगाया जा सका है। इन परिकल्पनाओं का स्वरूप परिस्थितियों के परिवर्तित होता है।
क्रियात्मक परिकल्पना का महत्त्व
क्रियात्मक परिकल्पना का महत्व निम्न प्रकार है-
अनुसार
(1) क्रियात्मक परिकल्पनाएँ अनुसंधान को एक दिशा प्रदान करती हैं। इनके बिना क्रियात्मक अनुसंधान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
(2) क्रियात्मक परिकल्पना के निर्माण से अनुसंधानकर्ता को यह बोध होता है कि उसे किस ओर चलना है। वह अपनी विचार प्रक्रियो को क्रियात्मक परिकल्पना में केन्द्रित कर देता है जिससे उसके अनुसंधान विषयक विचारों में तर्कसंगतता का समावेश होता है।
(3) क्रियात्मक परिकल्पना को क्रियात्मक अनुसंधान की धुरी समझना चाहिए। इसका निर्धारण हो जाने पर अनुसंधान का गन्तव्य निश्चित हो जाता है जिससे अनुसंधान कार्य में पर्याप्त स्पष्टता एवं शुद्धता आती है।
(4) क्रियात्मक परिकल्पना अनुसंधानकर्ता में एक अदम्य विश्वास उत्पन्न कर देता है। इसकी रचना न होने तक अनुसंधानकर्ता विभिन्न तर्क-वितर्क में उलझा रहता है।
(5) इसके द्वारा अनुसंधान की विधि तथा उसके परिणामों का स्पष्ट निर्देश मिलता है।
प्रश्न h (i) सामान्य परिकल्पना तथा क्रियात्मक परिकल्पनाओं में भेद ।
उत्तर-सामान्य परिकल्पनाएँ प्रायः मौलिक अनुसंधानों के तहत निर्मित की जाती हैं। इनके द्वारा समस्या-विशेष के सम्बन्ध में सर्वाधिक सम्भव प्रभावी समाधान की कल्पना की जाती है। अनुसंधानकर्ता अपनी परिकल्पना का निर्माण अनेक सम्भव अनुमानों के आधार पर करता है। इसीलिए परिकल्पनाओं को एक कुशल अटकल भी कहा जाता है। क्रियात्मक परिकल्पनाओं में भी एक प्रकार का अनुमान ही कार्यशील होता है। किन्तु इस तरह की परिकल्पनाओं में क्रिया- पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ अनुमान का उल्लेख क्रियात्मक पहलू को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। सामान्य परिकल्पनाओं में क्रिया-पक्ष का उल्लेख आवश्यक नहीं है।
क्रियात्मक परिकल्पना की सत्यता का पता अल्प अवधि में लगाया जा सकता है, किन्तु सामान्य परिकल्पनाओं की सत्यता एक निश्चित अवधि के बाद स्थापित हो जाती है। क्रियात्मक परिकल्पनाओं का स्वरूप परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होता है। एक अनुसंधान के अन्तर्गत अनेक क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। सामान्य परिकल्पनाओं का स्वरूप अपेक्षाकृत कम परिवर्तनशील होता है। उनमें परिवर्तन अनुसंधान की रूपरेखा को संशोधित किये बिना नहीं लाया जा सकता।
दोनों प्रकार की परिकल्पनाओं में अनुमान का स्थान महत्त्वपूर्ण है। बिना अनुमान के इनका निर्माण असम्भव है। दोनों की सत्यता परीक्षणों के बाद मालूम होती है। दोनों द्वारा समस्या के सम्भव समाधानों की परीक्षा होती है तथा किसी-न-किसी प्रकार के परिणाम तक पहुँचा जाता है। इस परिणाम के आधार पर परिकल्पना को मान्य, अमान्य या अशोधनीय घोषित किया जाता है।
प्रश्न h (ii) क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण।
उत्तर-समस्या का विशद विश्लेषण करने पर ही क्रियात्मक परिकल्पना के प्रति संकेत प्राप्त. होते हैं। समस्या के कारणभूत तत्त्वों से इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इसका तात्पर्य यह है कि क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करने से पूर्व समस्या के कारणों का विश्लेषण भली प्रकार कर लेना चाहिए। समस्या से सम्बन्धित वे कारण जिनका विश्लेषण अनुसंधानकर्ता सरलतापूर्वक कर सकता है, क्रियात्मक परिकल्पना के मुख्य स्रोत बन सकते हैं।
क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण निम्नांकित बातों पर ध्यान रखते हुए करना चाहिए-
(1) समस्या का सांगोपांग विश्लेषण करना चाहिए।
(2) समस्या के स्वरूप का परिभाषीकरण एवं सीमांकन स्पष्ट रूप में होना चाहिए।
(3) समस्या के कारणभूत तत्त्वों की विवेचना विस्तारपूर्वक हो ।
(4) समस्या के सभी पक्षों का समर्थन उपयुक्त साक्षियों द्वारा सम्भव हो ।
(5) समस्या के सभी सम्भव समाधानों का अनुमान लगाना चाहिए।
(6) केवल उन्हीं सम्भव समाधानों पर अधिक विचार करना चाहिए जो अनुसंधानकर्ता की, सामर्थ्य के भीतर हों।
(7) सम्भव समाधानों को प्राप्त करने के ढंगों पर विशेष रूप से सोचना चाहिए।
(8) क्रियात्मक परिकल्पना का अन्तिम रूप निर्धारित करते समय उसको अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
प्रश्न h (iii) क्रियात्मक परिकल्पना की विशेषताएँ ।
उत्तर- क्रियात्मक परिकल्पना की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-
1. सत्यापनशीलता-एक अच्छी क्रियात्मक परिकल्पना की यह पहचान है कि उसकी सत्यता अथवा असत्यता के बारे में परीक्षण सम्भव होता है। उसे विद्यालय की परिस्थितियों में ही परीक्षित किया जा सकता है। क्रियात्मक परिकल्पना की सत्यापनशीलता का पता उसके पूर्वार्द्ध (क्रिया पक्ष) को विश्लेषित करके लगाया जा सकता है। यदि उसका क्रिया पक्ष व्यावहारिक दृष्टि से है तो उसका परीक्षण सरलतापूर्वक किया जा सकता है
2. प्रभाव गाम्भीर्य-क्रियात्मक परिकल्पना की क्रियान्विति के बाद परिस्थिति पर प्रभाव किस रूप में पड़ेगा तथा यह प्रभाव कितना महत्त्वपूर्ण होगा? आदि प्रश्नों द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि अमुक क्रियात्मक परिकल्पना कितनी उपयोगी है ? क्रियात्मक परिकल्पना के प्रति इस प्रकार के प्रश्न विद्यालय के सन्दर्भ में पूछे जाने चाहिए। अनुसंधानकर्ता यह पूछ सकता है कि अमुक क्रियात्मक परिकल्पना का प्रभाव विद्यालय में कितने लोगों पर पड़ेगा? इसके कार्यान्वयन से छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा अथवा अध्यापकों पर? कितने छात्र अथवा अध्यापक इससे प्रभावित होंगे?
3. स्पष्टता- क्रियात्मक परिकल्पना को स्पष्ट शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इससे तात्पर्य यह है कि क्रियात्मक परिकल्पना का स्पष्टीकरण जिन शब्दों अथवा पदों की सहायता से किया जाता है, उनके अर्थ निश्चित कर दिये जाते हैं ताकि सभी लोग उसका एक ही अर्थ समझें । अधोलिखित क्रियात्मक परिकल्पना में चिह्नित शब्दों के कई अर्थ प्रतिध्वनित होते हैं, अतः उनका अर्थ निश्चित कर दिया गया है।
“यदि विद्यालय में विज्ञान तथा अंग्रेजी के अध्यापकों द्वारा पढ़ाई में कमजोर छात्रों की अतिरिक्त कक्षाएँ लगाने की व्यवस्था की जाये तथा इसके लिए उन्हें प्रतिफल दिया जाये तो वे प्राइवेट ट्यूशन अधिक नहीं करेंगे और विद्यालय के कार्यों में ढील नहीं आने देंगे।”
चिह्नित शब्दों के अतिरिक्त इस परिकल्पना में कुछ अन्य शब्द भी हैं जिन्हें स्पष्ट करना होगा; यथा- पढ़ाई में कमजोर छात्र, प्रतिफल आदि। पढ़ाई में कमजोर छात्र किसे कहा जायेगा ? प्रतिफल किस रूप में तथा कितनी मात्रा में दिया जायेगा ? आदि प्रश्नों के उत्तर निश्चित होने चाहिए।
4. सोद्देश्यता – अनुसंधानकर्ता को क्रियात्मक परिकल्पना का उद्देश्य मालूम होना चाहिए। जैसे अभी दिये हुए उदाहरण में क्रियात्मक परिकल्पना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा अध्यापकों में विद्यालय के कार्यों को ईमानदारी के साथ करने की प्रेरणा प्राप्त हो । क्रियात्मक परिकल्पना का यह उद्देश्य अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य से सम्बन्धित होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करते समय अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के उद्देश्यों को सामने रखे।
5. समस्या से सम्बद्धता – प्रत्येक क्रियात्मक परिकल्पना का सम्बन्ध उस समस्या से होना चाहिए जिसके लिए उसे निर्मित किया गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि क्रियात्मक परिकल्पना की जड़ें ‘समस्या’ के समाधान से अवश्य जुड़ी होनी चाहिए तभी उसे समस्या के प्रति प्रासंगिक माना जा सकता है। एक अच्छी क्रियात्मक परिकल्पना समस्या – विशेष से जुड़ी होती है।
प्रश्न h (iv) क्रियात्मक परिकल्पना के स्त्रोत ।
उत्तर- क्रियात्मक परिकल्पना के मुख्य स्रोतों को इस प्रकार इंगित किया जा सकता है-
1. सृजनात्मक कल्पनाएँ-
क्रियात्मक परिकल्पना के लिए उच्चकोटि की सर्जनशीलता की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार कलाकार अपनी समस्त कलाकृति को सर्जनात्मक कल्पना के आधार पर ढालता है और उसका रूप निर्धारित करता है, उसी प्रकार एक अनुसंधानकर्ता अपने शोध- कार्य की रूपरेखा निर्मित करते समय अपनी सर्जनात्मक कल्पना का प्रयोग करता है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक परिकल्पनाओं की उत्पत्ति सर्जनात्मक कल्पना के अभाव में असम्भव है।
2. अन्तर्दृष्टि-
अनुसंधान कार्यों में अन्तर्दृष्टि अथवा सूझबूझ के बिना एक पग भी आगे बढ़ना कठिन है। यहाँ अन्तर्दृष्टि से तात्पर्य है-एक ऐसी विशेष दृष्टि, जिसके द्वारा परिस्थितियों की सतह मात्र को ही दर्शन नहीं होता, अपितु उनके भीतरी अंशों का भी बोध होता है। अन्तर्दृष्टि द्वारा व्यक्ति किसी विषय की गहराई में प्रवेश कर सकता है। क्रियात्मक परिकल्पनाओं के निर्माण में अन्तर्दृष्टि का विशेष महत्त्व है। इस प्रकार की दृष्टि के बिना हम उत्तम कोटि की क्रियात्मक परिकल्पनाओं का सृजन नहीं कर सकते। विद्यालय की परिस्थितियों के बारे में हमारी सूझबूझ जितनी ही गहरी होगी, हम क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण उतना ही कुशलतापूर्वक कर सकेंगे।
3.अनुभव – अन्तर्दृष्टि अथवा अनुभव में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जैसे-जैसे हमारे अनुभवों का भण्डार बढ़ता है, हमारी सूझबूझ भी पैनी होती जाती है। अनुभवी व्यक्तियों में क्रियात्मक परिकल्पनाओं के निर्माण की क्षमता अधिक होती है। हमें अपने अनुभवों से जो कुछ प्राप्त होता है, उसका सदुपयोग हम क्रियात्मक परिकल्पनाओं के निर्माण में कर सकते हैं। अनुभवों की आँच में तपाई हुई क्रियात्मक परिकल्पना अत्यन्त प्रभावकारी होती है।
4. समस्या के कारणों का विश्लेषण-समस्या के कारणों का सूक्ष्म विश्लेषण किये बिना क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण न्यायसंगत नहीं है। ऐसा न करने से यह सम्भव है कि क्रियात्मक परिकल्पना का समस्या विशेष से सम्बन्ध विच्छेद हो जाये। अतः प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करने से पूर्व वे समस्या – विशेष के कारणों का सांगोपांग विश्लेषण कर लें।
5. विचार-विमर्श – अनुसंधान के अन्तर्गत विचार-विमर्श पद्धति का प्रयोग कई स्थानों पर किया जा सकता है। क्रियात्मक परिकल्पनाओं की रचना हेतु परस्पर विचार-विमर्श द्वारा अनेक लाभ होते हैं। सामूहिक चिन्तन द्वारा क्रियात्मक परिकल्पनाओं के क्रिया-पक्षों की व्यावहारिकता के सम्बन्ध में कई व्यक्तियों की स्पष्ट राय मिल जाती है। इसके अतिरिक्त कई नवीन क्रियात्मक परिकल्पनाएँ विचार-विमर्श के माध्यम से निर्मित की जा सकती हैं। बहुधा हम अकेले क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण सरलतापूर्वक नहीं कर पाते। किन्तु जब हम किसी समूह में विचार-विमर्श करते हैं तो अपने ही विचार क्रियात्मक परिकल्पना के निर्माण हेतु प्रभावकारी संकेत देते हैं।
प्रश्न (i) क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण हेतु रूपरेखा ।
उत्तर-क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण हेतु जो रूपरेखा इस प्रकार निर्मित की जाती है, उसके निम्नांकित घटक होते हैं-
1. क्रियाओं का विवरण- इसके अन्तर्गत जिन क्रियाओं को प्रारंभ किया जाना है, उनका उल्लेख स्पष्टतापूर्वक कर दिया जाता है।
2. विधि-जिन क्रियाओं का उल्लेख किया जाता है उनकी सम्पादन विधि के बारे में विवरण प्रस्तुत किया जाता है।
3. अपेक्षित साधन-इससे तात्पर्य यह है कि अनुसंधानकर्ता यह स्पष्ट करे कि अमुक क्रिया के सम्पादन हेतु किन साधनों की आवश्यकता होगी।
4. समय- इसके अन्तर्गत क्रियाओं के सम्पादन में अनुमानित समय का ब्यौरा देना अभीष्ट होता है।
प्रश्न (ii) क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों के मूल्यांकन की प्रेक्षण विधि।
उत्तर-क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का मूल्यांकन इस विधि द्वारा प्रचुरता के साथ किया जाता है। इसके अन्तर्गत अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य नियमित रूप से जाँच-पड़ताल करता है तथा अपने प्रेक्षण को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास करता है।
प्रेक्षण तीन प्रकार के होते हैं-
(क) पूर्ण-व्यवस्थित प्रेक्षण,
(ख) अर्द्ध-व्यवस्थित प्रेक्षण,
(ग) स्वतन्त्र प्रेक्षण।
अनुसंधान के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए पूर्ण व्यवस्थित प्रेक्षण की पद्धति को ही अपनाना न्यायसंगत होगा। इससे प्रेक्षण की वस्तुनिष्ठता बढ़ जाती है। इसके लिए एक खाका निश्चित कर लिया जाता है, जिसमें उन बातों का उल्लेख होता है जिनके प्रति प्रेक्षण करना है।
अर्द्ध-व्यवस्थित प्रेक्षण में खाका का प्रयोग नितान्त आवश्यक नहीं होता है। स्वतन्त्र प्रेक्षण
में परिस्थितियों को नियन्त्रित किये बिना अवलोकन किया जाता है। इन दोनों प्रकार के प्रेक्षणों का प्रयोग क्रियात्मक अनुसंधान में अधिक बहुलतापूर्वक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मगत पक्षों का समावेश होने की सम्भावना बनी रहती है।
पूर्ण व्यवस्थित प्रेक्षण के लिए अनुसंधानकर्ता कुछ विशेष व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें एक व्यवस्थित रूप में प्रेक्षण करने के लिए कहेगा। यह कार्य वह स्वयं भी कर सकता है। परिस्थितियों के अनुसार इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लेना चाहिए।
जिन बातों का परीक्षण करना हो, उन्हें सूचीबद्ध कर देने से प्रेक्षण में वस्तुनिष्ठता आती है। प्रेक्षणकर्ता को प्रेक्षण की अवधि में केवल उन्हीं तथ्यों को अंकित करना चाहिए जो वस्तुनिष्ठ रूप में विद्यमान हों। तथ्यों अथवा घटनाओं के अर्थों व व्याख्याओं का लेशमात्र भी उल्लेख नहीं करना चाहिए।
प्रश्न i (iii) क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों के मूल्यांकन का अभिमत संग्रह।
उत्तर-क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का मूल्यांकन अभिमत-संग्रह द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लिए अनुसंधानकर्ता विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापकों तथा छात्रों की सम्मति लेगा, किन्तु स्मरण रहे कि दूसरों के मतों पर सर्वथा निर्भर करना अनुसंधान की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। सम्भव है कि मतों को अभिव्यक्त करते समय विद्यालय के सभी लोग (जिनका मत-संग्रह किया जा रहा हो) किसी विशेष पक्षपात के शिकार बन जायें। ऐसी स्थिति का निराकरण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के मतों को अलग-अलग एकत्र करना चाहिए ।
अभिमतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे विषयों की सूची देनी चाहिए जिन पर विचार व्यक्त करना हो। इससे सम्मतियों का आधार निश्चित हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति एक ही बात पर अपनी सम्मति प्रकट करता है। इस प्रकार के अभिमत-संग्रह द्वारा अनुसंधान के परिणामों के बारे में अन्य व्यक्तियों के विचार मालूम हो जाते हैं।
प्रश्न i (iv) नियंत्रित व अनियंत्रित प्रश्नावली ।
उत्तर- नियन्त्रित प्रश्नावली- इस प्रकार की प्रश्नावली वह प्रश्नावली होती है जिनके प्रश्नों के उत्तर पहले से विकल्प उत्तरों के रूप में दिये होते हैं। इन विकल्प उत्तरों में उत्तरदाता कोई एक उत्तर चुनकर देता है। दूसरे शब्दों में, एक प्रश्न के लिए तीन, चार या अधिक उत्तर होते हैं। इन प्रश्नों में से उत्तरदाता को जो उत्तर पसन्द होता है वह उत्तर उत्तरदाता द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार की प्रश्नावली प्रतिबन्धित प्रश्नावली या नियन्त्रित प्रश्नावली इसलिए कहलाती है क्योंकि उत्तरदाता को प्रतिबन्धित उत्तरों में से ही कोई एक उत्तर देना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली में कुछ नियन्त्रण होता है।
नियन्त्रित रूप प्रश्नावली के अन्तर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सम्भावित उत्तर साथ ही दिये रहते हैं और उत्तरदाता को उन्हीं सम्भव उत्तरों में से किसी एक को चिह्नित करना पड़ता है।
अनियन्त्रित या खुली प्रश्नावली-इस प्रकार की प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर देने में उत्तरदाता पर कोई नियन्त्रण अथवा प्रतिबन्ध नहीं होता है। उत्तरदाता उत्तर देने के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र होता है। प्रश्नावली में अप्रतिबन्धित प्रश्न तब बनाये जाते हैं जब कोई शोधकर्ता किसी अध्ययन समस्या के सम्बन्ध में गुणात्मक अथवा विवरणात्मक या विस्तृत जानकारी अर्जित करना चाहता है।
अनियन्त्रित रूप प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जाते। उत्तरदाता स्वयं सोचकर उत्तर लिखता है। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। उदाहरणार्थ-
1. विद्यालय में छात्रों के भाग जाने की प्रवृत्ति अब क्यों कम हो रही है ?
2. विद्यालय में छात्र अवकाश के घण्टों के बाद पढ़ने में रुचि क्यों नहीं दिखाते ?
3. वर्तमान शिक्षा पद्धति के क्या-क्या दोष हैं?
4. परिवार नियोजन अपनाने के क्या-क्या कारण हैं ?
5. सरकारी भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आपके सुझाव क्या हैं ?
क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए नियन्त्रित रूप प्रश्नावली का प्रयोग करना अधिक समीचीन है। इससे मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का समावेश होता है।
यहाँ ज्ञातव्य है कि प्रश्नों का चुनाव अत्यन्त सतर्कतापूर्वक करना चाहिए। उनके उत्तरों को विचार-विमर्श द्वारा निर्धारित करने के पश्चात् ही प्रश्नों के साथ विकल्प के लिए रखना चाहिए। अध्यापकों तथा छात्रों द्वारा मूल्यांकन कराने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग करना चाहिए।
प्रश्न i (v) अनुसंधान की साक्षात्कार विधि ।
उत्तर-साक्षात्कार एक अध्ययन विधि भी है और एक अध्ययन यन्त्र भी है जिसकी सहायता ने से महत्त्वपूर्ण आँकड़े एकत्र किये जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में भी साक्षात्कार विधि से आँकड़े एकत्र किये जा सकते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अध्ययन इकाइयों के उन अनुभवों तथा विचारों, आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिसके सम्बन्ध में हमको प्रत्यक्ष रूप से भी दिखाई
नहीं पड़ रहा है। इसके महत्त्व के सम्बन्ध में ऑलपोर्ट का मत है कि “यदि हम जानना चाहते हैं कि लोग किस प्रकार अनुभव करते हैं? क्या याद रखते हैं? उनके संवेग और अभिप्रेरणाएँ किस प्रकार की हैं? उनके कार्य करने के कारण क्या हैं? तो उनसे हम पूछ ही क्यों न लें। ”
साक्षात्कार जितना उपयोगी और महत्त्वपूर्ण अनुसंधान यन्त्र के रूप में है उतना ही उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण साक्षात्कार विधि के रूप में भी है। यह कार्य क्षेत्र की एक विशेष प्रविधि है जिसका के उपयोग किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के व्यवहार के देखने, उनके कथनों को लिखने तथा सामाजिक या समूह अन्तः क्रिया के स्पष्ट परिणामों या समूह अन्तःक्रिया के स्पष्ट परिणामों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है।
साक्षात्कार का उपयोग बहुधा किसी अनुसंधान समस्या का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रारम्भिक ज्ञान में समस्या में निहित चरों के सम्बन्ध का अध्ययन किया जाता है। बहुधा साक्षात्कार विधि द्वारा इस प्रकार के किये गये अध्ययनों और उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर चर अनुसंधान परिकल्पना या परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। साक्षात्कार का उपयोग किसी अनुसंधान समस्या के अध्ययन में भी किया जा सकता है। इस विधि द्वारा एक विशेष प्रकार के तथ्य समस्या के सम्बन्ध में प्राप्त होते हैं ।
क्रियात्मक अनुसंधान में साक्षात्कार विधि का प्रयोग सबसे सरल है। इसके द्वारा विद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों का साक्षात्कार किया जा सकता है और उनके विचारों को जानकर अनुसंधान के परिणामों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। वस्तुतः साक्षात्कार तथा प्रश्नावली दोनों ही ‘अभिमत संग्रह’ के दो ढंग हैं। इनके द्वारा व्यक्तियों की सम्मतियाँ अधिक वस्तुनिष्ठ रूप में संकलित हो जाती हैं। साक्षात्कार के समय प्रेक्षण का भी अनुप्रयोग सम्भव है।
प्रश्न j (i) ‘चेक लिस्ट’ क्या है?
उत्तर-क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों को वस्तुनिष्ठ रूप में रखने के लिए यह एक सुगम तरीका है। इसके अन्तर्गत कुछ बिन्दुओं पर केन्द्रित सूची प्रस्तुत की जाती है, जिन्हें चैक करने के लिए कहा जाता है। व्यक्तिगत एवं सामान्य समस्याओं का पता लगाने के लिए भी यह एक मितव्ययी साधन है। समस्याओं की सूची प्रस्तुत करके व्यक्तियों से उन उपयुक्त समस्याओं को चिह्नित करने के लिए कहा जाता है, जो उन पर लागू हैं। इस प्रकार की सूची ‘समस्या चेक- लिस्ट’ के नाम से पुकारी जाती है।
क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए इसका प्रयोग सावधानी के साथ करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि चेक-लिस्ट के अन्तर्गत उन्हीं बातों का उल्लेख हो, जिनका सम्बन्ध क्रियात्मक परिकल्पना के अभीष्ट प्रभावों से हो। इसके बिना चेक लिस्ट की “वैधता कम हो जाती है। अतः प्रत्येक चेक लिस्ट के अन्तर्गत केवल संगत तथ्यों का ही समावेश होना चाहिए।
प्रश्न j (ii) अनुसंधान की सांख्यिकीय विधियाँ ।
उत्तर- क्रियात्मक अनुसंधान में सांख्यिकी के लिए विशेष स्थान नहीं है, तथापि कुछ स्थलों पर सांख्यिकी की सरल विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इन विधियों के प्रयोग से अनुसंधानकर्ता अपने परिणामों को वस्तुनिष्ठ ढंग से प्रकट कर सकता है।
इन मूल्यांकन विधियों के अतिरिक्त अन्य विधियाँ भी हैं, जिनका प्रयोग क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का मूल्यांकन करने के निमित्त किया जा सकता है। अनुसंधानकर्ता को अपनी आवश्यकतानुसार ही मूल्यांकन विधियों का चुनाव करना चाहिए। इनके चुनाव में यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल्यांकन विधि उपयुक्त एवं सुलभ हो। कुछ अन्य बातों पर भी विचार करना आवश्यक होता है। वे इस प्रकार हैं-
1. मूल्यांकन अधिक-से-अधिक विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ हो ।
2. मूल्यांकन की वैधता पर कोई संशय न उठाया जा सके।
3. व्यावहारिक दृष्टि से मूल्यांकन सुगम हो ।
4. मूल्यांकन के लिए वास्तविक साक्षियाँ उपलब्ध हों।
5. मूल्यांकन में व्यक्तिगत पक्षपातों तथा पूर्वाग्रहों पर पूर्ण प्रतिबन्ध हो ।
6. मूल्यांकन की उपयुक्तता एवं पर्याप्तता स्पष्ट रूप में निर्धारित की गई हो।
7. मूल्यांकन का प्रयोग अनुसंधानकर्ता स्वयं करे या किसी विश्वसनीय सूत्र से प्राप्त करे ।
प्रश्न (j) (iii) क्रियात्मक परियोजनाओं में सुधार के लिए सुझाव ।
उत्तर-
1. क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या शिक्षक की कक्षागत समस्या हो किसी अन्य शिक्षक की समस्या न हो, क्योंकि अनुसंधान शिक्षक का, शिक्षक द्वारा, शिक्षक के लिए होता है।
2. समस्या वास्तविक हो, सैद्धान्तिक अथवा सुनी हुई, पुस्तकीय अथवा कल्पनात्मक न हो।
3. क्रियात्मक अनुसंधान से विद्यालय के कार्य में व्यवधान न हो। इसे शिक्षक कक्षा शिक्षण कार्य में संलग्न रहते हुए ही करता है।
4. क्रियात्मक अनुसंधान से विद्यालय को लाभ होना चाहिए। इससे उसकी प्रसिद्धि में बढ़ोतरी हो ।
5. अनुमानित कारणों के विश्लेषण स्तर पर साक्षियाँ विश्वसनीय तथा वैध हों। साक्षियाँ ऐसी हों जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करे ।
6. समस्या समाधान के लिए जो भी क्रियाएँ करनी हों वे शिक्षक के हाथ में हों। यदि प्राचार्य अथवा अभिभावकों के सहयोग की अपेक्षा हो तो उन्हें पहले से ही विश्वास में लेना अत्यन्त आवश्यक है। क्रियात्मक अनुसंधान का यह सामाजिक दायित्व भी माना जाता है
7. क्रियात्मक अनुसंधान में मितव्ययिता से कार्य करना चाहिए। सामान्यतया इसके लिए धन की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। यदि कुछ धन की आवश्यकता हो भी तो प्राचार्य को विश्वास में लेकर व्यवस्था करायी जा सकती है कि इससे विद्यालय का ही अन्ततः हित होगा।
8. समस्या के चयन में वस्तुनिष्ठता का दृष्टिकोण होना अत्यन्त आवश्यक है। इस सन्दर्भ में अनुसंधानकर्ता को पक्षपाती नहीं होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से वैज्ञानिकता तिरोहित हो जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनिवार्य है।
प्रश्न j (iv) क्रियात्मक अनुसंधान निर्माण में सावधानियाँ ।
उत्तर-
1. क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का चुनाव उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पर करना चाहिए।
2. क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएँ विद्यालय की परिस्थितियों से आबद्ध होनी चाहिए।
3. क्रियात्मक अनुसंधान के लिए समस्याओं का परिभाषीकरण तथा सीमांकन अवश्य करना चाहिए।
4. क्रियात्मक अनुसंधान में परिकल्पनाओं का निर्माण करते समय यह सावधानी रखनी चाहिए कि उनमें लक्ष्य तथा प्रस्तावित कार्य-प्रणाली के प्रति स्पष्ट संकेत हो। उसी कार्य-प्रणाली का उल्लेख करना चाहिए जो अनुसंधानकर्ता की सामर्थ्य एवं अधिकार के भीतर हो ।
5. क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करने से पूर्व समस्या के कारणों का विश्लेषण भली-भाँति कर लेना चाहिए।
6. अनुसंधानकर्ता को क्रियात्मक परिकल्पना के क्रियान्वयन की विधि को कुछ विस्तार के साथ अंकित कर लेना चाहिए।
7. क्रियात्मक परिकल्पना के क्रियान्वयन से प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति में आत्मगत पक्षों पर पूर्ण प्रतिबन्ध रखना चाहिए।
8. क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का मूल्यांकन बहुत वस्तुनिष्ठता के साथ करना चाहिए।
|
9. मूल्यांकन विधियों का प्रयोग करते समय इनकी उपयुक्तता तथा पर्याप्तता के बारे में विचार कर लेना चाहिए।
10. क्रियात्मक अनुसंधान में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग बहुत सीमित रूप में किया जाना उपयुक्त रहता है। इस सम्बन्ध में अनुसंधानकर्ता को विशेषज्ञों की राय ले लेनी चाहिए।
प्रश्न j (v) क्रियात्मक अनुसंधान से भावी अनुसंधानकर्ताओं को लाभ।
उत्तर-
क्रियात्मक अनुसंधान करने से भावी अनुसंधानकर्ता को क्या लाभ होगा इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक होता है जिससे भावी अनुसंधानकर्ता पूर्व शोधों के निष्कर्षों का लाभ उठा सके तथा अनुसंधान को आगे ले जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण-अधिगम, अभिप्रेरणात्मक युक्तियों, परीक्षण, मूल्यांकन, संस्थागत क्षमता विकास, प्रबन्धन तथा शैक्षिक व्यवस्थाओं की मॉनीटरिंग से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों के उत्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से शैक्षिक अनुसंधान की विधि को आधुनिक प्रविष्टि माना जा सकता है।
विगत कई दशकों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अध्ययन तथा शोध निरन्तर सम्पन्न हो रहे हैं और हुए भी हैं। नई सहस्राब्दी में इन शोधों / अध्ययनों के माध्यम से प्राप्त जानकारियों, निष्कर्षों एवं सामान्यीकरणों के मन्थन को आधार बनाकर भावी अनुसंधानकर्ता बहुत कुछ सीख सकते हैं तथा उनसे लाभान्वित भी हो सकते है।
अतः क्रियात्मक अनुसंधान से भावी अनुसंधानकर्ताओं को सन्देश अवश्य देना चाहिए जिससे वे कार्यान्वयन युक्तियों में अपेक्षित सुधारों/परिवर्तन करके विशेष रूप से क्रियात्मक शोध को अधिक उपयोगी बना सकें। शैक्षिक अनुसंधान का सीधा प्रयोजन होता है- शैक्षिक समस्याओं का व्यवस्थित या वैज्ञानिक ढंग से हल प्राप्त करना । शोध के साक्ष्यों को अपनी कार्य परिस्थिति में सूझ-बूझ तथा समझ की गहराई को बढ़ाने में सहायक बनाना।
भावी अनुसंधानकर्ताओं की व्यावसायिक निपुणता तथा कार्य कुशलता को प्रगाढ़ बनाने की दृष्टि से शैक्षिक शोध के तहत कतिपय अत्यन्त युक्तियों तथा रचना – कौशलों का विवरण देना चाहिए। महत्त्वपूर्ण अनुक्षेत्रों में सम्पन्न शोधों के परिणामों तथा निष्कर्षों का निहितार्थ एवं उनका सन्देश विद्यालय स्तर पर प्रदान करना चाहिए। अनुसंधानकर्ताओं को शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। कोई भी अनुदेशात्मक व्यवस्था बनाने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को उसके उद्देश्यों को व्यवहारपरक रूप में निश्चित कर लेना चाहिए ।
आगामी शोध के अनुक्षेत्रों के बारे में भी भावी शिक्षकों अथवा अनुसंधानकर्ताओं को जानकारी देने से उन्हें लाभ होता है और उनके समक्ष लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर क्रियात्मक अनुसंधान होने पर वह आगामी अनुसंधानकर्ताओं को लाभ पहुँचा सकते हैं। भावी अनुसंधानकर्ताओं से यह उम्मीद की जाती है कि वे पूर्व वर्णित कुछ अनुक्षेत्रों को चुनकर उनमें सम्पन्न शोधों के परिणामों एवं निष्कर्षों को थोड़ी और विशदता तथा गहराई से जानने-समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार पूर्व अनुसंधान को अधिक उपयुक्त तथा व्यापक बनाने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न j (vi) व्यवहृत शोध की प्रकृति ।
उत्तर-
वस्तुतः व्यावहारिक शोध व्यावहारिक होता है और इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगितावादी होता है जो सामान्यतः व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करता है। मौलिक शोध द्वारा जहाँ सिद्धान्त और सूत्र खोजे जाते हैं वही व्यावहारिक शोध उन सूत्रों और सिद्धान्तों की सहायता से विशेष समस्या के समाधान से सम्बन्धित होते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में व्यावहारिक शोध के द्वारा नवीन यंत्र, नई तकनीक की खोज की जाती है जिससे देश तथा राष्ट्र विकास की गति बना रहे हैं। समाज की शैक्षणिक, आवासीय, तकनीकी, आर्थिक समस्याओं के समाधान में व्यावहारिक शोध उपयोगी सिद्ध हुआ है।
प्रश्न j (vii) वैज्ञानिक विधि की प्रक्रिया।
उत्तर-
वैज्ञानिक विधि की प्रक्रिया इस प्रकार है—
(i) सर्वप्रथम समस्या बतायी जाती है।
(ii) समस्या से सम्बन्धित सामग्री का संकलन किया जाता है,
(iii) कल्पित सिद्धान्त का निर्माण किया जाता है।
(iv) कल्पित समाधान के आधार पर अन्य निरीक्षणीय वस्तुओं के बारे में भी पूर्व कथन किया जाता है।
(v) पूर्वकथन के अनुसार परिणाम निकले अथवा नहीं, इसकी जाँच की जाती है।
(vi) फिर उसी आधार पर उस कल्पित समाधान को स्वीकार किया जाता है अथवा रद्द किया जाता है या नए प्रमाणों के प्रकाश में उसमें संशोधन किया जाता है। अवलोकन, अवलोकन को लिखना, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, परीक्षण, मापन, प्रयोग करना, संख्या का उपयोग, दूरी व समय में सम्बन्ध आदि के आधार पर समस्या का अध्ययन वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत किया जाता है।
प्रश्न j (viii) क्रियात्मक शोधकर्ता के गुण ।
उत्तर-
(i) क्रियात्मक शोधकर्ता द्वारा स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन किया जाता है क्योंकि स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का इतनी जल्दी अध्ययन किसी अन्य अनुसंधान पद्धति द्वारा नहीं हो सकता है।
(ii) शोधकर्ता क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर अध्ययन समस्या का मूल्यांकन उचित ढंग से करता है क्योंकि समस्या का अध्ययन वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है तथा कई बार अनुसंधानकर्ता उस समूह का सहभागी निरीक्षणकर्ता होता है।
(iii) जब कोई क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की तात्कालिक समस्या के सम्बन्ध में जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर नीति निर्माण का कार्य कर सकता है।
प्रश्न j (ix) क्रियात्मक शोध आधारित प्रतिवेदन की आवश्यकता ।
उत्तर-
क्रियात्मक शोध आधारित प्रतिवेदन (रिर्पोट) का एक लक्ष्य चलन पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। क्रियात्मक अनुसंधान में इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है। लेकिन कार्यशाला के साथ कठिनाई यह होती है कि इसमें लोग प्रपत्र प्रस्तुत करने लगते हैं बजाय शोध के विषय में पहल करने की अपेक्षा। कार्यशाला में आपको लोगों के क्रियात्मक शोध प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में आश्वस्त करने का अवसर प्राप्त होती है। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रसार के लिए अपनी संस्था से बाहर कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र पढ़कर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शोध पत्रिकाओं के शोध-पत्र प्रकाशित कर अपने परिणामों का विस्तार कर आपके द्वारा किए गए क्रियात्मक शोध का महत्व और उपयोगिता बढ़ा सकते हैं।
(3) शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान पिछले साल के प्रश्न
शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान | MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH, VARANASI
| विषय | शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान प्रश्न
Shiksha mein kriyaatmak anusandhaan Question Paper |
| SUBJECT | Action Reseacher In Education Question |
| पेपर कोड | १04 |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय |
| कोर्स | बी.एड |
| सेमेस्टर | प्रथम |
| FULL MARKS | 50 |
| lnfo | यहाँ महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के पेपर -१04 शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान प्रश्न दिया गया है | |