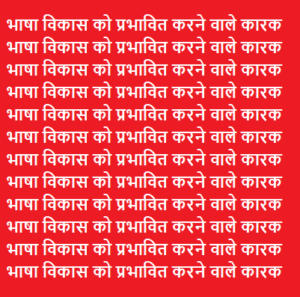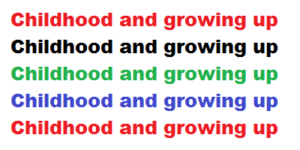शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ वस्तुतः दार्शनिक ही होती हैं।” इस कथन पर प्रकाश डालिए।
| प्रश्न | शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ वस्तुतः दार्शनिक ही होती हैं।” इस कथन पर प्रकाश डालिए |
| विश्वविद्यालय नाम | महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय , और अन्य |
| सेमेस्टर | प्रथम -01 |
| संछिप्त जानकारी | इस पेज में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड के प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य के शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ वस्तुतः दार्शनिक ही होती हैं।” इस कथन पर प्रकाश डालिए। उतर दिया गया है | |
| VVI NOTES.IN के इस पेज में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड के प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य सिलेबस , शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य प्रश्न – शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ वस्तुतः दार्शनिक ही होती हैं।” इस कथन पर प्रकाश डालिए । शामील किया गया है | | |
प्रश्न 2 (i) “शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ वस्तुतः दार्शनिक ही होती हैं।” इस कथन पर प्रकाश डालिए।
उत्तर –
शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ
(1) निरक्षरता की समस्या-
समाज या प्रौढ शिक्षा की सबसे प्रथम समस्या है भारत में निरक्षर वयस्कों की संख्या अधिक होना। सन् 2011 ई. की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है जिसमें से 74 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं और बाकी 26 प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षा एवं अज्ञानता से ग्रसित हैं। इन अशिक्षित एवं अज्ञानी व्यक्तियों को शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त कराना बहुत ही जटिल समस्या है जिसका समाधान करना अत्यधिक कठिन है। इस समस्या पर प्रकाश डालते हुए पी. एन. चटर्जी ने लिखा है, “विश्व के निरक्षर वयस्कों की सम्पूर्ण संख्या में आधे से अधिक भारत में निवास करते हैं। उनको ज्ञान के अल्प-प्रकाश में लाने का कार्य अति विशाल है।”
(2) धनाभाव की समस्या-
समाज शिक्षा की दूसरी समस्या है भारत के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए धन की कमी का होना। सन् 1951 ई. की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 12 वर्ष से अधिक आयु के प्रौढ़ों की संख्या 21.6 करोड़ है। इन वयस्कों को यदि । वर्ष में साक्षर बनाना हो तो 35 लाख से अधिक अध्यापकों एवं प्रौढ़-विद्यालयों की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए कि प्रौढ़ विद्यालय में न्यूनतम व्यय 250 रुपया वार्षिक हो तो 35 लाख प्रौढ़-विद्यालयों का संचालन करने के लिए 8.75 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। भला इतनी बड़ी धनराशि प्रौढ़ों को साक्षर बनाने में कैसे खर्च की जा सकती है, जबकि भारत की राष्ट्रीय आय केवल इस धनराशि से दुगुनी ही है। इस प्रकार समाज शिक्षा के प्रसार के लिए धन की जटिल समस्या है।
(3) अध्यापकों के अभाव की समस्या-
समाज शिक्षा की तीसरी समस्या है इसके लिए उपयुक्त अध्यापकों का अभाव होना। जिन अध्यापकों को प्रौढ़-विद्यालयों में नियुक्त किया जाता है, वे प्रायः प्राथमिक विद्यालयों के हुआ करते हैं, जिनमें प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करने की योग्यता का सर्वथा अभाव होता है। न तो उन्हें प्रौढ़ मनोविज्ञान का ज्ञान होता है और न ही वे उनके लिए उपयुक्त शिक्षण-विधियों और उनके प्रयोग करने की योग्यता रखते हैं। ऐसी स्थिति में भला इन शिक्षकों से प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की कैसे आशा की जा सकती है। उपयुक्त शिक्षकों के अभाव की समस्या की अपेक्षा अध्यापकों का कम संख्या में उपलब्ध होना अधिक जटिल समस्या है। ग्रामों में जहाँ प्रौढ़- निरक्षरों का भण्डार है, जीवन के लिए आवश्यक सुविधाओं के अभाव में ग्रामों में स्थित प्रौढ़ विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तैयार नहीं होते हैं। इन विद्यालयों में अध्यापिकाओं का तो और भी अभाव रहता है। इस प्रकार अध्यापकों के अभाव में समाज शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होना असम्भव हो गया है।
(4) समाज के उत्तरदायित्व की समस्या-
समाज शिक्षा की चतुर्थ समस्या है-समाज शिक्षा का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, शिक्षा विभागों, जिला परिषदों और सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं में से किस पर हो ? केन्द्रीय सरकार ने यह उत्तरदायित्व राज्य सरकार को दिया है और स्वयं को इस महत्वपूर्ण कार्य के भार से मुक्त करने का प्रयास किया है। किन्तु सरकारें धनाभाव एवं अन्य समस्याओं के कारण इस भार को ठीक से वहन नहीं कर पा रही हैं। अतः समाज शिक्षा का प्रसार खटाई में पड़ गया है। यदि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार समाज शिक्षा की उपेक्षा करती रही तो समाज शिक्षा की कल्पना को साकार रूप देना सम्भव नहीं है।
(5) पाठ्यक्रम निर्धारण की समस्या-
समाज शिक्षा की पाँचवीं समस्या है-पाठ्यक्रम के निर्धारण में कठिनाइयों का होना । प्रमुख कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं-
(अ) बहुत दिनों से समाज-
शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है किन्तु अब तक इस बात पर मतैक्य नहीं हो सका है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम सबसे उपयोगी होगा? वयस्कों की अभिरुचियाँ आवश्यकताएँ एवं दृष्टिकोण बालकों से भिन्न होने के कारण उनके लिए बालकों के लिए प्रयुक्त पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ों में शिक्षा सम्बन्धी व्यक्तिगत विभिन्नता की समस्या है। कुछ प्रौढ़ निरक्षर हैं, कुछ अशिक्षित हैं और नवसाक्षर हैं। इन सभी के लिए पृथक्-पृथक् पाठ्यक्रम की आवश्यकता है।
(ब) पाठ्यक्रम निर्धारण सम्बन्धी दूसरी कठिनाई यह है कि यदि हम वास्तव में प्रौढ़ों के रहन- सहन का स्तर ऊँचा करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जो उन्हें बौद्धिक ज्ञान के साथ-साथ किसी न किसी कला या कौशल में प्रशिक्षित या दक्ष बना सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी तीसरी कठिनाई यह है कि प्रौढ़ों में सभी आयु के पुरुष एवं स्त्रियाँ हैं। मोटे रूप में इन्हें तीन आयु श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-
(i) 12 से 17 वर्ष के प्रौढ़, (ii) 19 से 35 वर्ष तक के प्रौढ़ एवं (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु के प्रौढ़। इन तीनों श्रेणियों की अभिरुचियों, आवश्यकताओं, बौद्धिक स्तरों एवं दृष्टिकोणों में अन्तर होता है। अतः सबके लिए समान पाठ्यक्रम निर्धारित करना एक जटिल समस्या है।
(6) शिक्षण-पद्धति के निर्धारण की समस्या-समाज शिक्षा की छठी समस्या है-
प्रौढ़ों के लिए उपयुक्त शिक्षण-पद्धति का निर्धारण करने में कठिनाइयों का होना। हम देखते हैं कि बच्चों में जीवन एवं संसार के प्रति किसी विशिष्ट दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण सभी बच्चों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु प्रौढ़ों का जीवन एवं संसार के प्रति दृष्टिकोण एक समान नहीं होता है। उन्हें अधिक सामाजिक स्वतन्त्रता के उपयोग का अवसर मिलने के कारण उनमें अहम् की भावना का पर्याप्त रूप से विकास हो जाता है। उनमें कुछ ऐसी आदतों, नियमों एवं सिद्धान्तों का विकास हो जाता है, जिनके विरुद्ध वे न तो स्वयं कार्य करना चाहते हैं और न दूसरों को ऐसा कोई कार्य करने का अवसर देना चाहते हैं। इन सभी परिस्थितियों के कारण प्रौढ़ों के लिए उपयोगी एवं प्रभावशाली शिक्षण पद्धति, निर्धारित करना अति दुष्कर है। यदि सभी प्रौढ़ों के लिए एक पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो यह निश्चय है कि उन्हें वह अरुचिकर प्रतीत होगी और उसकी अहम् की भावना स्वतन्त्रता, आदतों, नियमों एवं सिद्धान्तों को ठेस पहुँचेगी, जिसके परिणामस्वरूप उसका असफल हो जाना अवश्यम्भावी है। इन्हीं कठिनाइयों के कारण सामाजिक शिक्षा के लिए अभी तक किसी एक पद्धति को निश्चित नहीं किया जा सकता।
(7) उपयुक्त साहित्य की समस्या-
समाज शिक्षा की सातवीं समस्या है इसके लिए उपयुक्त साहित्य के तैयार करने एवं जुटाने की आवश्यकता । प्रौढ़ विद्यालयों में मुख्यतः प्रौढ़ों को लिखना- पढ़ना एवं गणित की शिक्षा प्रदान की जाती है जो उन्हें भविष्य में शिक्षित बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि प्रौढ़ विद्यालय की शिक्षा के उपरान्त नवसाक्षर शिक्षा ग्रहण करने का कार्य समाप्त कर देते हैं जिसके परिणामस्वरूप वे पुनः निरक्षर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नवसाक्षरों के लिए प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो उनमें सामाजिक भावना, आलोचनात्मक शक्ति एवं वस्तुओं को परखने की क्षमता के विकास में योग दे ताकि, “वे कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं निकृष्ट के बीच, ज्ञान के क्षेत्र में सच एवं झूठ के बीच एवं आचरण के क्षेत्र में भले और बुरे के बीच में अन्तर ला सकें।”
(8) शिक्षा के साधनों की समस्या-
समाज शिक्षा की आठवीं समस्या है-इसके लिए साधनों के चयन में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता। “समाज शिक्षा के साधनों का अभिप्राय है-वे समूह या संस्थाएँ जो समाज शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क रखती हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान करती हैं एवं उनकी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करती हैं।” इन साधनों के चयन में इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि प्रौढ़ को ज्ञान प्राप्त करने के प्रति आकर्षित करें। किन्तु ऐसे साधनों का चुनाव करने के लिए अत्यधिक विवेक और अनुभव की आवश्यकता है। यह कार्य केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा हो सकता है जो प्रौढ़ मनोविज्ञान में दक्ष हो ।