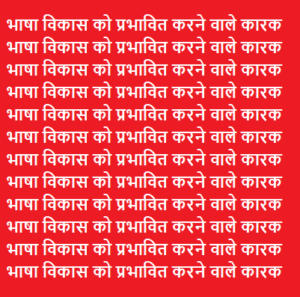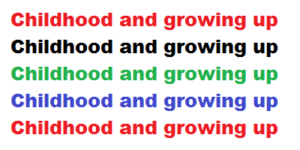शिक्षा दर्शन के विभिन्न अंगों की विवेचना कीजिए
| प्रश्न | शिक्षा दर्शन के विभिन्न अंगों की विवेचना कीजिए |
| विश्वविद्यालय नाम | महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय |
| सेमेस्टर | प्रथम -01 |
| संछिप्त जानकारी | इस पेज में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड के प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य के शिक्षा दर्शन के विभिन्न अंगों की विवेचना कीजिए उतर दिया गया है | |
| VVI NOTES.IN के इस पेज में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड के प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य सिलेबस , शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य प्रश्न – शिक्षा दर्शन के विभिन्न अंगों की विवेचना कीजिए। अथवा दर्शन को परिभाषित कीजिए। इसके प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए।अथवा शैक्षिक दर्शन को परिभाषित कीजिए। ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा के शैक्षिक महत्त्व को प्रतिपादित कीजिए। अथवा शिक्षा में तत्वमीमांसा की भूमिका का वर्णन करें। को शामील किया गया है | | |
प्रश्न – शिक्षा दर्शन के विभिन्न अंगों की विवेचना कीजिए।
अथवा
दर्शन को परिभाषित कीजिए। इसके प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए।
अथवा
शैक्षिक दर्शन को परिभाषित कीजिए। ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा के शैक्षिक महत्त्व को प्रतिपादित कीजिए।
अथवा
शिक्षा में तत्वमीमांसा की भूमिका का वर्णन करें।
उत्तर—
दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा
दर्शन और अंग्रेजी भाषा की फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है- ‘फिलॉस’ तथा ‘सोफिया’। फिलॉस का प्रेम तथा सोफिया का अर्थ है – ज्ञान। अन्तः दर्शन शब्द का अर्थ हुआ |’ज्ञान से प्रेम’ ।
दर्शन की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए सेलर्स ने लिखा है-
“दर्शन एक ऐसा अनवरत प्रयास है जिसके द्वारा मनुष्य संसार तथा अपनी प्रकृति के सम्बन्ध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करता है।”
राधाकृष्णन के अनुसार, “दर्शन वास्तविकता की प्रकृति का तार्किक अध्ययन है।”
प्लेटो के अनुसार दार्शनिक की परिभाषा इस प्रकार है-“वह जिसे प्रत्येक करार के ज्ञान में रुचि है और जो सीखने के लिए जिज्ञासु है और ज्ञान से कभी भी संतुष्ट नहीं होता, वास्तव में दार्शनिक कहा जा सकता है।”
दर्शन के प्रमुख विभाग
दर्शन के प्रमुख रूप से तीन भाग हैं जो निम्न प्रकार हैं-
(1) तत्त्व मीमांसा- तत्त्व मीमांसा के तीन विभाग हैं-
(i) प्रकृति-दर्शन,
(ii) आत्म-दर्शन तथा
(iii) ईश्वर दर्शन।
(2) ज्ञान मीमांसा – ज्ञान मीमांसा में ज्ञान सम्बन्धी अध्ययन किया जाता है।
(3) मूल्य मीमांसा- मूल्य मीमांसा में व्यक्ति के धार्मिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है।
तत्त्व मीमांसा तथा शिक्षा दर्शन
सृष्टि क्या हैं? इस सम्बन्ध में व्यक्ति की जानने की ललक होती है या सत्य क्या है? इसको व्यक्ति जानना चाहता है यह समाधान तत्त्व मीमांसा में होते हैं। ऐसे प्रश्नों के समाधान एवं सर्वसम्मत भी नहीं है और न उनको प्रमाणित ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यथार्थ का अनुभव कराने में जो उसका प्रमुख और व्यावहारिक पक्ष है शिक्षा अपने को असमर्थ-सा पाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के सामने अनेक विकल्प उठ खड़े होते हैं-
(i) तत्त्व मीमांसा के क्षेत्र में उत्पन्न विवादों के चक्कर में छूटने का एक विकल्प यह है कि शिक्षाविद मिलकर एक सर्वसम्मत शैक्षिक तत्त्व ज्ञान को निश्चित करें। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार प्रधान है। अतः मनुष्य, उसकी प्रकृति, उसकी आवश्यकताओं, उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन पर देश और काल के सन्दर्भ में तात्त्विक विचार करके शिक्षा का स्वतन्त्र तत्त्व ज्ञान स्थिर करने की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षाविद् को विभिन्न शाखाओं से मदद लेनी होगी, विशेष रूप से विज्ञान और मनोविज्ञान से ।
शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष को ही लें तो मतैक्य नहीं मिलेगा। अब से ढाई हजार साल पहले अरस्तू ने यह कहा था कि क्या पढ़ना चाहिए-सद्गुण या उत्तम जीवन-इस बारे में एकमत नहीं रहा। यह भी स्पष्ट नहीं कि शिक्षा का क्षेत्र ज्ञान है अथवा नैतिक गुण। वर्तमान शिक्षा प्रणाली भ्रांतिपूर्ण है। कोई नहीं कह सकता है कि ठीक सिद्धान्त क्या है, जिस पर शिक्षा को चलना चाहिए। क्या जीवनोपयोगी ज्ञान या सद्गुण या उच्चज्ञान शिक्षा का उद्देश्य हो ? इन तीनों उद्देश्यों के समर्थक पाये जाते हैं। शिक्षा के साधनों के बारे में एकमत नहीं है। अरस्तू के समय से लेकर अब तक यही स्थिति बनी हुई है। एक कठिनाई और आ खड़ी हुई है। प्रजातन्त्र के उदय से विचार भिन्नता को ज्यादा महत्त्व मिला है। साथ ही राजनीति और अर्थशास्त्र को मानव जीवन में अधिक महत्त्व प्राप्त हो गया है और अध्यात्मवाद का पक्ष कमजोर पड़ता जा रहा है। इसलिए शिक्षा का काम अधिक कठिन होता जा रहा है और उसके तात्त्विक पक्ष पर गम्भीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता से स्वतन्त्र शिक्षा-दर्शन का विकास हो रहा है। पाश्चात्य शिक्षा जगत में तो ऐसा हो ही रहा है। भारत में अति प्राचीन काल से शिक्षा तत्त्व मीमांसा से जुड़ी रही है। अब आवश्यकता इस बात की है कि नयी परिस्थितियों में भारतीय शिक्षा-दर्शन का विकास किया जाए। यह शिक्षा-दर्शन न केवल उद्देश्यों का वरन् पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियों और शिक्षा व्यवस्था तथा मूल रूप से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाए।
(ii) उपर्युक्त विवरण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि तात्त्विक मीमांसा के धरातल को छोड़ना शिक्षा के लिए न तो सम्भव ही है और न खतरों से खाली। साथ ही संसार की यथार्थता और ‘संसार की असारता’ के दो परस्पर विरोधी मतों से बने दो अलग-अलग खेमों में से किसी एक खेमे में जाकर बैठना भी शिक्षक के लिए तर्कसंगत नहीं है। उदाहरण के लिए शिक्षा (मान लें) संसार की असारता पर विश्वास करने वालों के मत को स्वीकार करके एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लग जायें जिसमें सभी छात्र दार्शनिक वैरागी शासक बन जायें तो संसार की बड़ी दुर्गति होगी। सारे के सारे छात्र इस संसार को माया और भ्रमजाल मानकर जीवन की यथार्थता से मुँह मोड़ कर जंग में जा बैठें तथा कर्महीन बनकर समाधिस्थ हो जायें तो देश का क्या होगा ? समाज कैसे चलेगा? कृषि, उद्योग-धंधे, व्यापार और दुनियादारी ठप्प हो जाएगी। हमारे देश में इस प्रकार की विचारधारा से जहाँ दर्शन, धर्म कला और साहित्य की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो गईं। वहीं संसार के प्रति वैराग्य होने से देश को आक्रमणकारियों का शिकार होकर महान कष्ट भोगना पड़ा। दूसरी ओर संसार में सार है, यही यथार्थ है-इस मत को सभी स्वीकार करें अपनी व्यवस्था बना लें तो दूसरे प्रकार के छात्र बनेंगे। उनमें हर प्रकार की वासना और योगेच्छा पैदा होगी। दुराचार और आसुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी क्योंकि सांसारिक ऐश्वर्य की वृद्धि से मदांध होकर वे विवेक खो बैठेंगे। यह सब कुछ हम भारत को वर्तमान शिक्षा पद्धति के परिणामों के रूप में देख रहे हैं तब क्या किया जाए?
वास्तव में शिक्षा के लिए किसी एक तात्त्विक विचारधारा से सम्पूर्ण रूप से जुड़ जाना उपयुक्त न होगा। शिक्षा तत्त्व मीमांसा से एक दूसरे प्रकार से लाभ उठा सकती है। इससे दूसरा विकल्प बनता है। वह यह है कि शिक्षाशास्त्री तत्त्व मीमांसा के क्षेत्र में उत्पन्न सभी मतों और वाद-बिन्दुओं का बारीकी से अध्ययन करें। फिर यह देखें कि उनमें कहाँ तक संगति और कहाँ तक असंगति है। यह वर्णनात्मक एवं मूल्यांकन प्रधान ढंग है जो शिक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं उनकी व्यावसायिक तैयारी करने के कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार की दार्शनिक एवं तात्त्विक विचारधाराओं के अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक इन सबका मूल्यांकन करके विभिन्न तात्त्विक मतों से वे बिन्दु छाँटकर निकल सकें, जो देश-काल और व्यक्ति के सन्दर्भ में सार्थक हो। ऐसा करने से अधिकांश अध्यापक – शिक्षक न तो अवगत हैं और न ही वे जानकार भी इस तरफ ध्यान देते हैं।
(iii) शिक्षा का प्रमुख दायित्व यह है कि वह छात्रों को इस संसार में सफलतापूर्वक और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करे। परन्तु इस दायित्व को पूरा करना तभी सम्भव होगा जब वह पहले निश्चय हो कि संसार की वास्तविकता, उसका यथार्थ क्या है। इस बिन्दु पर आते ही मतभेद उठ खड़े होते हैं। एक तत्त्वज्ञानी यह कहता है कि संसार अनुसार है, माया और भ्रम है, तो दूसरा कहता है यह संसार वास्तविक है, क्योंकि यह अनुभवगत है तो पहले मत को मान लें, तो शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप एक प्रकार का होगा और दूसरे का मान लें तो उसका प्रारूप पहले से सर्वथा भिन्न होगा। ऐसी दशा में शिक्षाकर्मी किंकर्त्तव्यविमूढ़ होकर उस नाव के समान बनकर रह जायेगा जो लहरों के थपेड़ों में दिशाहीन होकर चक्कर काटती रहती है तब तो क्या यह विकल्प चुनना उपयुक्त न होगा कि शिक्षा तत्त्व मीमांसा के चक्कर से छुटकारा पा ले। अच्छा यही होगा कि वह तत्त्व मीमांसा को नकारे परन्तु इस विकल्प को चुनना आसान नहीं है क्योंकि तत्त्व मीमांसा को नकारने की बात करना एक अन्य प्रकार के तात्त्विक विवाद को जन्म देना है।
ज्ञान मीमांसा तथा शिक्षा दर्शन
ज्ञान मीमांसा और शिक्षा के तत्त्व निम्न प्रकार हैं-
(i) ज्ञान और छात्र प्रकृति-
शिक्षण प्रक्रिया में छात्र ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। अतः शिक्षा का केन्द्रीय बिन्दु छात्र है। छात्र एक मनुष्य और सजीव प्राणी है। अतः उसकी प्रकृति की जानकारी प्राप्त करना शिक्षक के लिए आवश्यक है। मानव प्रकृति की जानकारी एक ओर तत्त्व मीमांसा से और दूसरी ओर आधुनिक मनोविज्ञान से प्राप्त होती है।
तत्त्व मीमांसा के अन्तर्गत सत्य के विषय में कहा गया है कि कुछ लोग सत्य को चेतन मानते हैं और विश्वास करते हैं कि वह चेतन एक पारलौकिक तत्त्व है और समस्त जगत्-जीव उसी से उत्पन्न मनुष्य अन्दर भी उसी तत्त्व का एक अंश विद्यमान है। इसे ‘आत्मा’ कहा गया है। ज्ञान का अधिकारी यही आत्मा है। ज्ञान प्राप्ति में शरीर का कोई महत्त्व नहीं है। शिक्षा की दृष्टि से इस विचार का महत्त्व यह है कि छात्र के भीतर वर्तमान आत्मतत्त्व को जानने और पहचानने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि आत्मतत्त्व ही अनुभवकर्त्ता है, वही ग्रहण करता है। शरीर की ज्ञानेन्द्रियों से जो अनुभव प्राप्त होते हैं, उन्हें भोगने वाला वही है। सोते समय मनुष्य स्वप्न देखता है। उस समय ज्ञानेन्द्रियाँ निष्क्रिय रहती हैं, परन्तु उस समय देखने वाला, गंध लेने वाला और सुनने वाला यही आत्मा है। इसका अर्थ है कि छात्र के भीतर वर्तमान आत्मा का विकास करना, उसको विकारों से मुक्त करना शिक्षा का मूल दायित्व है। इसमें संदेह नहीं कि यह आत्मतत्त्व शिक्षा से प्रभावित होता है। इसीलिए प्राचीन धार्मिक शिक्षा में छात्रों को एक विशेष प्रकार के अनुशासन में रहना पड़ता था।
मानव प्रकृति का एक अन्य पहलू सामाजिकता है। कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है। वह जंगली पशुओं से भिन्न इसलिए है कि वह अपने समान अन्य पशुओं के बीच रहना पसन्द करता है। सच तो यह है कि समाज में रहने से ही उसमें मानवीय गुण जैसे-त्याग, सेवा, सहयोग और भाईचारा आदि उत्पन्न हुए। उसकी अनेक खोजें और आविष्कार समाज के कारण सम्भव हुए। भेड़ियों की माँद में पले मानव बालक यह सिद्ध करते हैं कि समाज से अलग रहने के कारण वे पशु बन गये। समाज में रहने के कारण मनुष्य को भाषा, साहित्य, संस्कृति और सभ्यता का वरदान मिला।
मनोवैज्ञानिकों का एक वर्ग बताता है कि सामाजिकता मनुष्य की आदि प्रवृत्ति है, बच्चा पैदा होते ही सामाजिक बन जाता है। वास्तव में स्नेह और सुरक्षा पाने के लिए उसका सामाजिक होना अनिवार्य है। मनुष्य के भीतर वर्तमान प्रकृति प्रदत्त संवेग या भावनाएँ जैसे-स्नेह, भय, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष सामाजिकता के आधार हैं, उसकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएँ जैसे-शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आदि तभी पूरी होती हैं, जब वह समाज का सहारा ले । अस्तु, मनुष्य की सामाजिकता की उपेक्षा शिक्षा नहीं कर सकती। प्राचीनकाल की शिक्षा का भी एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य यह था कि मनुष्य दूसरों के लिए जीना मरना सीखे और वर्तमान शिक्षा भी छात्रों के समाजीकरण पर बल देती है। जब हम राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता की बात करते हैं अथवा छात्रों में विश्वबंधुत्व की भावना पैदा करने की बात करते हैं, तो हमें छात्रों की सामाजिक वृत्ति के विकास की सुदृढ़ बनानी होगी। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय जैसे-नागरिकशास्त्र, सामाजिक ज्ञान, भारतीय संस्कृति का परिचय, राष्ट्रीय सेवा आदि शामिल करना होगा ताकि छात्र अतिव्यक्तिवादी न बन जाये। व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अलग महत्त्व है। छात्रों के व्यक्तित्व को दबाया नहीं जाना चाहिए परन्तु यह ध्यान रखना होगा कि वे निपट विद्रोही और उच्छृंखल न बन जायें। उनके भीतर वर्तमान प्रतिभा समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो। छात्र अपनी क्षमताओं का विकास अपने लिए नहीं प्रत्युत् अपने चारों ओर वर्तमान समाज के लिए करें।
(ii) ज्ञान और अध्यापक-कुछ ज्ञान-
मीमांसकों का मत है कि ज्ञान मनुष्य के मन में वर्तमान है, यह केवल सुषुप्तावस्था में पड़ा रहता है। ईश्वरीय प्रेरणा से वह स्फुरित होता है। इस दृष्टि से ईश्वर ही ज्ञानदाता है। यदि ऐसा न होता, तो हर व्यक्ति अपने प्रयासमात्र से ज्ञानी बन जाता। बहुत से ऐसे साधु-सन्त, विचारक और ज्ञानी हो गये हैं जिनके मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ और इसके लिए वे ईश्वर की कृपा को साधन मानते हैं। यदि ऐसा विचार सत्य है, तो शिक्षा और शिक्षक का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। परन्तु व्यावहारिक दुनिया में तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अदृष्ट शक्ति के भरोसे बैठे रहना एक मूर्खता ही होगी। साधारणजन तो अज्ञान के अन्धकार में डूबे रहेंगे क्योंकि भगवान की कृपा तो कुछ ही लोगों पर होगी।
कुछ ज्ञान-मीमांसक यह मानते हैं कि ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से वर्तमान है परन्तु उसे सक्रिय बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु मनुष्य ही है परन्तु उसे लोग ब्रह्म या ईश्वर की प्रतिकृति मानते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा चाहिए। वे कहते हैं कि बिना ‘गुरु’ के ज्ञान सम्भव नहीं। इस मत के अनुसार शिक्षा और शिक्षक का बड़ा महत्त्व है परन्तु आधुनिक शिक्षक ‘गुरु’ नहीं है। गुरु को विशेष प्रकार से परिभाषित किया गया है। सरल अर्थों में गुरु को तत्त्वज्ञानी होना चाहिए जिसने अपने तप (कष्ट सहन) से सत्य का दर्शन किया हो और जो दयावान हो, परोपकारी हो । ऐसा गुरु दुर्लभ होता है। प्राचीन धार्मिक शिक्षा में ऐसे ही गुरु का महत्त्व था। शिक्षा केवल कुछ लोगों • को दी जाती थी या कुछ लोग जो साधनसम्पन्न होते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। इनके लिए ‘गुरु’ तलाश करके सुलभ कराये जाते थे। आज स्थिति बदल चुकी है। प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा देने और वह भी अनिवार्य और मुफ्त देने का प्रावधान है। ऐसी दशा में इतनी संख्या में ‘गुरु’ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। अब गुरु का स्थान ‘शिक्षक’ या ‘अध्यापक’ ने लिया है और ‘शिक्षा’ ‘ब्रह्म ज्ञान’ से भिन्न है जिसे पाने के लिए नचिकेता और सत्यकाम भटकते रहे थे।
ज्ञान मीमांसकों का एक वर्ग यह भी कहता है कि छात्र स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है। जो ज्ञान वह अपने निजी प्रयास से अर्जित करता है, वही सच्चा ज्ञान है। इस विचार ने शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला है। बाल केन्द्रित शिक्षा के आन्दोलन का जन्म इसी विचार से हुआ। अध्यापक एक ऐसे सूत्रधार के समान है जो नाटक के मंच की व्यवस्था करता है और अभिनेताओं को निर्देशन देता है, परन्तु स्वयं पर्दे के पीछे रहता है। इसका उद्देश्य छात्रों को स्वयं सीखने में सहायता देना है। इस स्थिति में अध्यापक केवल सीखने की प्रक्रिया में निर्देश देता है। यहाँ भी स्पष्ट है कि छात्रों को ज्ञान देने में अध्यापक का महत्त्व किसी न किसी रूप में बना हुआ है। मनोविज्ञान की खोजों से और विज्ञान के आविष्कारों से अध्यापकों के महत्त्व में अत्यधिक बदलाव आने की आशंका उत्पन्न हो गयी है। इसका एक उदाहरण अभिक्रमित शिक्षण और शिक्षण-यन्त्र है जिनके द्वारा छात्र अध्यापक से नहीं, पहले से बनाये गये कार्यक्रम और यन्त्रों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी जमाने में शिक्षा की कल्पना अध्यापक के अभाव में की ही नहीं जा सकती थी। आज तो अध्यापक निरर्थक बना जा रहा है। एजूकेशनल टेक्नालॉजी का यह परिणाम है। दूरस्थ शिक्षा और आकाशीय विश्वविद्यालय इस दिशा में शिक्षा को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके परिणाम जिनके कारण ‘अध्यापक’ का पद ही समाप्त हो जाये, अभी देखना बाकी है। अध्यापक के ‘व्यक्तित्व’ को क्या मशीनें प्राप्त कर लेंगी? इसका निर्णय भविष्य करेगा। इतना तो सच है कि कागज पर बने शिक्षण कार्यक्रम और मशीनें छात्र के साथ रागात्मक सम्बन्ध और अंतःक्रिया नहीं पैदा कर सकते। ‘कम्प्यूटर’ एक मानवीय भावों से सम्पन्न अध्यापक का स्थान नहीं ले सकता।
मूल्य मीमांसा और शिक्षा
अन्तर्वर्ती मूल्य या परवर्ती मूल्य-मूल्यों के दो प्रकार हैं-अन्तर्वर्ती (इन्ट्रिन्जिक) और परवर्ती (एक्सट्रिन्जिक)। कुछ लोगों ने प्रथम को स्वतः मान मूल्य और दूसरे को उपकरणीय मूल्य कहा है। प्रथम प्रकार के मूल्य वे हैं जिनका अपने आप में महत्त्व है (जिन्हें हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन नहीं बनाते वरन् जिन्हें प्राप्त करना ही मानव-जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार के मूल्यों की श्रेणी में सत्य, शिव, सुन्दर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे मूल्य रखे जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के मूल्य, परवर्ती या उपकरणीय मूल्य वे हैं, जिनको हम किसी महान् उद्देश्य की प्राप्ति के साधन या निमित्त रूप में अपनाते हैं, जैसे-श्रम, ईमानदारी, निष्ठा आदि)।
शिक्षा का मुख्य सरोकार अन्तर्वर्ती मूल्यों से है क्योंकि उनकी प्राप्ति मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। यदि शिक्षा का उद्देश्य जीवन की तैयारी है, तो वह अन्तर्वर्ती या स्वतः मान मूल्य शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं या शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायक हैं। शिक्षा के उद्देश्य जैसे- ‘ज्ञानार्जन’, ‘सर्वांगीण जीवन’ (स्पेंसर), ‘सत्य की खोज’ (प्लेटो) आदि स्वतः मान मूल्यों की आधार- शिला पर खड़े किये गये हैं। यह मूल्य सूक्ष्म से अधिक सम्बन्ध रखते हैं। अस्तु, शिक्षक का ध्यान भौतिक वस्तुओं की ओर कम रहेगा। वह चाहेगा कि उसके छात्र सूक्ष्म विचारों की समस्या और मूल तत्त्व को ग्रहण करें। उनके अध्ययन की सामग्री बौद्धिक विषय ही होंगे। जैसे-गणित, भाषा, साहित्य, धर्म और दर्शन। सम्भवतः प्राचीन काल से लेकर अब तक इन विषयों का प्राधान्य इसलिए रहा है कि इनके द्वारा सूक्ष्म तत्त्व को ग्रहण करने में सहायता मिलती है। स्वतः मान मूल्यों की शिक्षण विधियों में चिन्तन और तर्क को ज्यादा महत्त्व मिला है।
अब प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसे उपाय भी अपनाये जा सकते हैं जिनसे छात्रों को इन स्वतः मान अन्तर्वर्ती मूल्यों को व्यवहार में लाकर अनुभव कराया जा सके। केवलं व्याख्या या सिद्धान्त की शिक्षा कारगर नहीं हो सकती। मूल्यों को पहले अध्यापक के और बाद में छात्र के व्यवहार में उतर कर अनुभवजन्य बनना चाहिए। उदाहरण के लिए ‘सत्य’ क्या है? इसे समझाने के बजाय उन्हें सत्य की शोध और खोज करने का व्यवहार सिखाया जाये, ‘सुन्दरं’ का अनुभव छात्रों को उत्तम मनोभावों, जैसे-स्नेह, सहानुभूति और करुणा के माध्यम से कराया जा सकता है, ‘शिवं’ का अनुभव एक ऐसी जीवन-शैली के द्वारा कराया जा सकता है, जिसमें परस्पर सहयोग, परहित चिंतन और सेवा प्रधान हो। ऐसे सूक्ष्म मूल्यों की जड़ें मन में जमाने के लिए यह आवश्यक होगा कि विद्यालय का सम्पूर्ण वातावरण सुनियोजित ढंग से तैयार किया जाये।