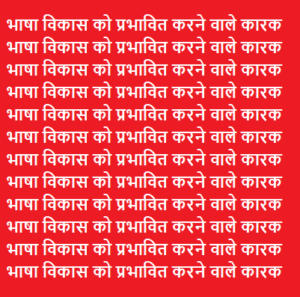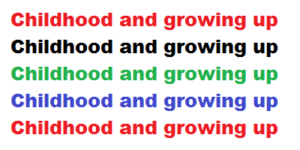शिक्षा और दर्शन के परस्पर सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए
| प्रश्न | शिक्षा और दर्शन के परस्पर सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए |
| विश्वविद्यालय नाम | महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय , और अन्य |
| सेमेस्टर | प्रथम -01 |
| संछिप्त जानकारी | इस पेज में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड के प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य के शिक्षा और दर्शन के परस्पर सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए उतर दिया गया है | |
| VVI NOTES.IN के इस पेज में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड के प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य सिलेबस , शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य प्रश्न – शिक्षा तथा दर्शन में परस्पर सम्बन्ध है, एक का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में भी कैसे परिवर्तन हो जाता है? अथवा शिक्षा और दर्शन के परस्पर सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए। अथवा शिक्षा और दर्शन की अन्योन्याश्रितता स्पष्ट कीजिए। अथवा शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है।” इस उक्ति की सतर्कतापूर्वक व्याख्या कीजिए। शामील किया गया है | | |
प्रश्न 2 (iii) शिक्षा तथा दर्शन में परस्पर सम्बन्ध है, एक का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में भी कैसे परिवर्तन हो जाता है?
अथवा
शिक्षा और दर्शन के परस्पर सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए।
अथवा
शिक्षा और दर्शन की अन्योन्याश्रितता स्पष्ट कीजिए।
अथवा
शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है।” इस उक्ति की सतर्कतापूर्वक व्याख्या कीजिए।
उत्तर –
शिक्षा और दर्शन का सम्बन्ध
डॉ0 राधाकृष्णन का कथन है, “दर्शन यथार्थता के स्वरूप का तार्किक ज्ञान है।” इसी कारण कहा जाता है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने जीवन में पूर्ण बनाने का प्रयास करती है। व्यक्ति को पूर्ण बनाने तथा उसके विकास के लिए अनुभव आवश्यक होता है। दर्शन अनुभव प्राप्त करने में विशेष रूप से सहायता प्रदान करता है। स्पष्ट है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। बिना दर्शन की सहायता शिक्षा को पूर्णतः नहीं मिल सकती।
‘शिक्षा दर्शन’ दर्शन की एक शाखा है। शिक्षा दर्शन ऐसे प्रश्नों से सम्बन्धित है-जैसे शिक्षक क्या है ? शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? आदि। शिक्षा दर्शन से सम्बन्धित अनेक समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करता है और उनका समाधान भी करता है। शिक्षा दर्शन के उद्देश्य के विषय में कनिंघम ने इस प्रकार लिखा है- “शिक्षा दर्शन अनेक दार्शनिक विचारधाराओं द्वारा निकाले गये सिद्धान्तों के प्रयोग के रूप में इन विचारधाराओं से भिन्न समस्याओं की खोज के लिए निर्देशन लेता है-” निम्नलिखित पंक्तियों में हम यह स्पष्ट करेंगे कि दर्शन किस प्रकार शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा किस प्रकार दर्शन को प्रभावित करती है-
1. दर्शन शिक्षा का पूरक है-दर्शन शिक्षा का पूरक है। इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षण कला दर्शन के अभाव में पूर्णता प्राप्त करने में असमर्थ रहती है। जर्मन दार्शनिक फिक्टे के अनुसार, “दर्शन के अभाव में शिक्षा की कलापूर्ण स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकती।”
2. दर्शन शिक्षा का आधार है-शिक्षा का आधार दर्शन है। जेण्टाइल के अनुसार, “बिना दर्शन की सहायता से शिक्षा प्रक्रिया सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती।”
3. दर्शन शिक्षा की अमूल्य सहायता करता है-दर्शन शिक्षा की अमूल्य सहायता करता है। बटलर के शब्दों में- “दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ-प्रदर्शक है, शिक्षा अनुसन्धान के क्षेत्र के रूप में दार्शनिक निर्णय हेतु निश्चित सामग्री को आधार के रूप में प्रदान करती है।”
4. दर्शन शिक्षा का सिद्धान्त है-दर्शन शिक्षा का सिद्धान्त है। ड्यूवी के अनुसार, “अपने सामान्यतम रूप में दर्शन शिक्षा सिद्धान्त है।”
5. दर्शन विश्व की प्राचीनतम विद्या है-ई० वी० शर्क के अनुसार, “दर्शन विश्व की प्राचीनतम विद्या है। इसका वास्तविक अर्थ है-विज्ञान अथवा व्यवस्थित प्रयत्न जो सैकड़ों वर्षों के एकत्रित साक्ष्यों पर आधारित है।”
6. शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है-दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करता है जबकि शिक्षा उन्हें प्राप्त करने के साधनों को निश्चित करती है। शिक्षा के अभाव में कोई सिद्धान्त व्यावहारिक रूप नहीं ले सकता है। व्यक्ति के विकास के लिए अनुभव आवश्यक होता है। दर्शन अनुभव प्राप्त करने में विशेष सहायक होता है। इस तथ्य को सर जॉन एडम्स ने अपने शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट किया है- “शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। यह दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पक्ष जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का व्यावहारिक साधन है।”
हरबर्ट ने दर्शन और शिक्षा का सम्बन्ध बताते हुए लिखा है, “शिक्षा को छुट्टी मनाने का अवसर ही कहाँ है, जब तक कि दर्शन की गुत्थियाँ सदैव के लिए न सुलझ जायँ ।’
उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि दर्शन और शिक्षा आपस में घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार दार्शनिक विचारधाराएँ उत्पन्न होती हैं और उसी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य तथा प्रणाली निश्चित की जाती है।
रॉस ने दर्शन और शिक्षा का सम्बन्ध बताते हुए लिखा है, “दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं। एक में दूसरा निहित है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष।” शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों तथा आदर्शों का बालकों में प्रसार करता है। इसी कारण वह शिक्षा के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है। शिक्षक अपनी दार्शनिक विचारधारा के अनुकूल अपना आदर्श प्रस्तुत करता है। आदर्शों एवं उद्देश्यों को निश्चित करने के लिए दार्शनिक विचारधारा अनिवार्य है। इसी कारण अध्यापकों को दार्शनिक विचारधाराओं से बालकों को प्रेरित तथा प्रभावित कर आगे बढ़ाना होता है। यदि आदर्शों को शिक्षा से पृथक् कर दिया जाय तो शिक्षा अर्थहीन हो जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के पद का मापदण्ड भी दार्शनिक विचारधाराओं से बनता है।
अतः शिक्षा और दर्शन का एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षा और दर्शन एक-दूसरे पर निर्भर है। यहाँ पर हम दर्शन और शिक्षा की पारम्परिक निर्भरता की पुष्टि में कुछ शिक्षाविदों के कथन प्रस्तुत करेंगे-
ड्यूवी- “दर्शन अपने सामान्यतया रूप में शिक्षा सिद्धान्त है। “
जेण्टाइल – “दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती।” फिक्टे- “शिक्षा का कार्य दर्शनशास्त्र की सहायता के बिना पूर्णतया तथा स्पष्टता को प्राप्त नहीं “कर सकता।”
स्पेन्सर- “वास्तविक शिक्षा का संचालन एक वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है।”
हम रॉस के कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि “शिक्षा सम्बन्धी समस्त प्रश्न अन्ततः दर्शन से सम्बन्धित हैं।” इस सम्बन्ध में हम शिक्षा और दर्शन का सम्बन्ध स्पष्ट कर चुके हैं। वास्तव में शिक्षा का आधार दर्शन है। दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती ।
जो विद्वान् यह कहते हैं कि ‘शिक्षा को दार्शनिक विचारों से मुक्त कर देना चाहिए’ उनके विचार अत्यन्त संकीर्ण हैं। जेण्टाइल ने इन विचारों का खण्डन किया है। वह कहता है कि “जो व्यक्ति इस बात में विश्वास रखते हैं कि दर्शनविहीन होने पर भी शिक्षण प्रक्रिया उत्तम रीति से चल रही है वे शिक्षा के अर्थों को पूर्णरूपेण समझने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं।”
हम इस कथन से सहमत हैं कि “सभी शैक्षिक समस्याएँ अन्य में दर्शन की ही समस्याएँ होती हैं।” इस कथन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के सभी अंगों-शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का प्रभाव पड़ता है। दार्शनिक विचारधाराओं के परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठ्यविधि आदि में भी परिवर्तन होता रहता है।
इस प्रश्न के उत्तर में इस तथ्य की व्याख्या से कि दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिए एक शिक्षा दर्शन की क्यों आवश्यकता होती है। प्लेटो, स्पेन्सर, लॉक, डीवी, महात्मा गाँधी, टैगोर, विवेकानन्द और राधाकृष्णन महान् दार्शनिक होने के साथ-साथ महान् शिक्षाशास्त्री भी थे। स्पेन्सर का कथन है-“वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है।” प्रत्येक अध्यापक को दर्शन का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि शिक्षा और दर्शन में अटूट सम्बन्ध है। फिक्टे के अनुसार, “दर्शन के अभाव में शिक्षा की कला पूर्ण स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती है,” ड्यूवी अध्यापक के लिए दर्शन का ज्ञान अनिवार्य समझता है। उसके अनुसार, “दर्शन अपने सामान्य रूप से शिक्षा सिद्धान्त ही है।’