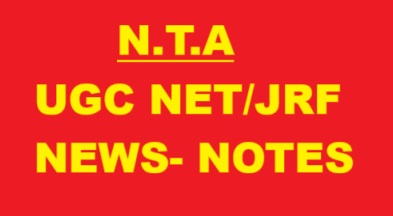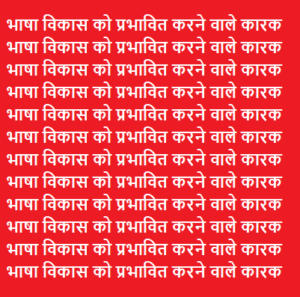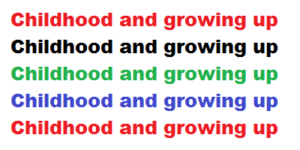NTA UGC NET PAPER-2 EDUCATION NOTES
| TOPIC | NTA UGC NET PAPER-2 EDUCATION SYLLABUS |
| SUBJECT CODE | 09 (EDUCATION) |
| SHORT INFO | VVI NOTES.IN के इस पेज में NTA UGC NET PAPER -02 EDUCATION में TEN (10) यूनिट है जिसका नाम निचे दिया गया है | 10 यूनिट के सभी टॉपिक के नोट्स भी दिया जा रहा है | जिसे आप अध्ययन कर NTA UGC NET EDUCATIONका परीक्षा पास कर सकते है | |
UGC NET PAPER-2 EDUCATION EXAM PAITURN
NTA UGC NET शिक्षा (EDUCATION) के परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे| यह परीक्षा 300 अंकों की होगी , जो 3 घंटे में हल किए जाएंगे। इस परीक्षा में 2 पेपर होंगे जिनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
| यूजीसी नेट पेपर -२ शिक्षा परीक्षा पैटर्न | |
| FULL MARKS | PAPER-1=100
PAPER-2=200 |
| प्रश्नों के प्रकार | OBJECTIVE |
| पत्रों की संख्या | यूजीसी नेट पेपर I – सामान्य
पेपर-II – विषय संबंधित शिक्षा |
| Num OF QUESTION | PAPER-1=50
PAPER-2=100 |
| TIME | 3 HOURS |
| NIGATIVE | NO |
UGC NET PAPER -2 EDUCATION ALL UNIT NAME
| UGC NET PAPER -02 EDUCATION में दस यूनिट है | जिसका नाम निचे लिखा गया है | ये दस यूनिट के सिलेबस के अनुसार इसका उतर भी दिया जायेगा | |
- ईकाई 1 शैक्षिक अध्ययन
- इकाई 2 शिक्षा का इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र
- ईकाई 3 शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया
- ईकाई 4 अध्यापक शिक्षा
- ईकाई 5 पाठ्यचर्या अध्ययन
- ईकाई 6 शिक्षा में शोध
- ईकाई 7 शिक्षणशास्त्र, प्रौढशिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन
- ईकाई 8 शिक्षा में/के लिए प्रौद्योगिकी
- ईकाई 9 शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व
- ईकाई 10 समोवशी शिक्षा
| NTA UGC NET/JRF सम्बन्धी न्यूज नोट्स pdf के लिए ग्रुप को ज्वाइन करे | |
| व्हाट एप ग्रुप |  |
| टेलीग्राम लिंक |  |
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 1 NOTES IN HINDI
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 1 NOTES IN HINDI PDF
ईकाई 1 शैक्षिक अध्ययन नोट्स
| इस यूनिट से सम्बन्धित शेष नोट्स जल्द हो जोड़ा जायेगा | |
शिक्षा (Education)
शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है, जो निरन्तर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है। “किसी भी दर्शन के निर्धारण तथा विकास के लिए पर्याप्त सूक्ष्म निरीक्षण, मनन तथा चिन्तन की आवश्यकता होती है। दार्शनिक सिद्धान्तों को मूर्त रूप शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से ही दिया जाता है। दर्शन से सम्बन्ध बनाए बिना शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम रीति से नहीं चल सकती है।”
शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार, शिक्षा एक विकास सम्बन्धी प्रक्रिया है अर्थात् शिक्षा मानव जीवन में निरन्तर प्रवाहमान प्रक्रिया है। इस विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना परम आवश्यक है। शिक्षा को आंग्ल भाषा में ‘एजुकेशन’ (Education) कहते हैं। ‘एजुकेशन’ शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित शब्दों से हुई है |
शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के ‘एडूकेटम’ (Educatum) शब्द का अर्थ है- शिक्षित करना। “प्रत्येक बालक के अन्दर जन्म से ही कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। जैसे-जैसे बालक वातावरण के सम्पर्क में आता जाता है, वैसे-वैसे उसकी शक्तियों को अन्दर से बाहर की ओर विकसित करना ही शिक्षा है।” इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। अतः व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य मानव जीवन के उन समस्त पक्षों से जो उसे परिष्कृत रूप में ढालते हैं तथा सभ्य बनाते हैं। शिक्षा का संकुचित रूप से तात्पर्य विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा से है। वास्तविक रूप में शिक्षा का प्रथम स्रोत राज्य होता है। शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं –
● जे एस मिल के अनुसार, “शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं, ताकि वे उसका संरक्षण कर सकें और यदि सम्भव हो तो उसमें उन्नति भी कर सकें।’
● टैगोर के अनुसार, “शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके।’
● फ्रोबेल के अनुसार, “शिक्षा वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर निकलती हैं।”
● विवेकानन्द के अनुसार, “शिक्षा मनुष्य के अन्दर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। “
● काण्ट के अनुसार, “शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है, जिसकी उसमें क्षमता है।”
● सुकरात के अनुसार, “शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना।”
●जे. कृष्णामूर्ति के अनुसार, “शिक्षा संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। “
● पाल फ्रेरे के अनुसार, “शिक्षा का अर्थ सम्प्रेषण एवं संवाद है न कि ज्ञान का हस्तान्तरण।”
●मैकेंजी के अनुसार, “शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य बच्चों द्वारा उनकी शक्तियों के विकास के लिए चेतनापूर्ण प्रयास से है। “
दर्शन ( Philosophy)
दर्शन अंग्रेजी भाषा के ‘फिलॉसफी’ (Philosophy) शब्द का रूपान्तर है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों ‘फिलोस’ (Philos) तथा ‘सोफिया’ (Sophia) से हुई है। ‘फिलोस’ का अर्थ है- प्रेम अथवा अनुराग और ‘सोफिया’ का अर्थ है-ज्ञान अर्थात् फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ ज्ञान के प्रति अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम है। विशिष्ट तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का अर्थ अमूर्त चिन्तन करने के उस प्रयास से है, जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा सम्पूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटन किया जाता है। वास्तव में सत्य की खोज करना ही दर्शन है।
भारतीय परिवेश में दर्शन का अर्थ
‘दर्शन’ पद की व्युत्पत्ति के दो अर्थ हैं। पहले, दुश्यते अनेन इति दर्शनम्। इस व्युत्पत्ति के अनुसार, संस्कृत में दर्शन का अर्थ होता है-जिसके द्वारा देखा जाए। दूसरे, ‘दर्शन’ शब्द से वे सभी पद्धतियाँ अपेक्षित हैं, जिनके द्वारा परमार्थ का ज्ञान होता है। ‘देखा जाए’ इस पद का अर्थ यों तो ‘ज्ञान प्राप्त किया जाए’ यह भी हो सकता है, फिर भी इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना उचित है कि ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन है; जैसे- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द आदि, किन्तु इन सभी में सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख साधन ‘प्रत्यक्ष’ है।
दर्शन के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं —
● प्लेटो के अनुसार, “जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई-नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी सन्तुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा जाता है।”
● हैण्डरसन के अनुसार, “दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है, जिनका मानव ने कभी अनुभव किया हो। ”
● शोपेनहावर के अनुसार, “संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है।” बर्ट्रेण्ड रसेल के अनुसार, “अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है।’
● कौटिल्य के अनुसार, “आन्वीक्षिकी विद्या ही दर्शन है।”
● डॉ. बलदेव उपाध्याय के अनुसार, “दर्शन एक ठोस सिद्धान्त है, न कि अनुमान या कल्पना, इसे व्यवहार में लाकर व्यक्ति निर्धारित लक्ष्य या मार्ग प्रशस्त कर लेता है। ”
● डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार, “यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन की दर्शन है। ”
● महात्मा गाँधी के अनुसार, “दर्शन एक प्रयोग है जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय-वस्तु होती है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं।”
अतः दर्शनशास्त्र को एक ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा मानव-अनुभूतियों के सम्बन्ध में समग्र रूप में सत्यता से विचार किया जाता है अथवा जो सम्पूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता है।
दर्शन के प्रकार एवं प्रकार्य
दर्शन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं
● आदर्शवादी या विचारवादी
● बहुवादी या अनेकेश्वरवादी
● भौतिक या प्रकृतिवादी
दर्शन के प्रमुख प्रकार्य निम्नलिखित हैं
● विश्लेषणात्मक प्रकार्य
● मानकी प्रकार्य
● बौद्धिक प्रकार्य
दर्शन के तत्त्व
दर्शन के तत्त्व शिक्षा की प्रक्रिया, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षक की भूमिका, शिक्षा की व्यवस्था आदि का स्वरूप विकसित करते हैं। दर्शन को शिक्षा सिद्धान्त माना जाता है। इसलिए दार्शनिकों ने शिक्षण संस्थाओं तथा आश्रमों की स्थापना की, जिससे दार्शनिक विचारों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सके। दर्शन केवल मीमांसा का ही विषय नहीं, अपितु इसका जीवन से सीधा सम्बन्ध होता है। शिक्षा व दर्शन के सम्बन्ध को निम्न चार्ट से समझा जा सकता है
दर्शन के तत्त्व
दर्शन एवं शिक्षा
1. तत्त्वमीमांसा (सत्य का प्रकाश)
2. ज्ञानमीमांसा (ज्ञान स्वरूप)
3. मूल्यमीमांसा (ज्ञान के चयन के मानक)
4. तर्कमीमांसा (ज्ञान प्राप्त करने के साधन)
दर्शन एवं शिक्षा
शिक्षा के घटक
1. शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य
2. शिक्षा की प्रक्रिया
3. पाठ्यक्रम का स्वरूप
4. शिक्षण की विधियाँ
5. शिक्षण की प्रविधियाँ
6. शिक्षक की भूमिका
7. विद्यालय प्रबन्धन
8. परीक्षा प्रणाली
दर्शन के तत्त्वों का सम्बन्ध सत्य के प्रत्यय से होता है, जिसे तत्त्वमीमांसा कहा जाता है। ज्ञान के प्रत्यय का सम्बन्ध ज्ञानमीमांसा से होता है। ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया तार्किक चिन्तन पर आधारित होती है, जिसमें आगमन व निगमन चिन्तन को प्राथमिकता दी जाती है। ज्ञान के चयन के लिए जो मानक प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें मूल्य कहा जाता है। इसका विवेचन मूल्यमीमांसा के अन्तर्गत होता है। मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता संवेदनशीलता तथा आचरण की आवश्यकता होती है। दर्शन के ये सभी तत्त्व शिक्षा के घटकों के स्वरूप को आधार प्रदान करते हैं।
दर्शन के कार्य
दर्शन के कार्य निम्नलिखित हैं
• दर्शन व्यक्ति की जिज्ञासा की तृप्ति करके ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।
• यह शब्दों और अर्थों का विश्लेषण करके कार्य की सही दिशा निश्चित करता है।
• यह वास्तविक सत्य की खोज करने का प्रयास करता है तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा प्राप्त सत्यों में अन्तर्विरोधों को यह दूर करता है।
• यह ध्यान को केन्द्रित करने में व्यक्ति की सहायता करता है। सांसारिक इच्छाएँ एवं इन्द्रियजनित कामनाएँ संयम प्राणायाम, धारणा द्वारा चित्तवृत्तियों का विरोध करना सम्भव है तथा इस कार्य में दर्शन सहायता करता है।
• यह जीव, जगत्, सत्, चित्, आनन्द, आत्मन्, परमात्मन्, मनस् आदि से सम्बन्धित प्रश्नों का समाधान ढूँढने का प्रयास करता है।
• यह मानव-जीवन के आदि अन्त पर विचार करके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है।
• यह जीवन की विभिन्नताओं और विसंगतियों को सामंजस्य में लाने का प्रयास करता है।
• यह तथ्यों का मात्र संग्रह न करके उनमें व्याप्त सम्बन्धों को देखता तथा प्रत्येक अनुभवगम्य वस्तु की आत्मा को देखने का प्रयास करता है।
भारतीय दर्शन (Indian Philosophy)
इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के प्राचीनतम ग्रन्थ ‘वेद’ ही हैं, भारतीय दर्शन का स्रोत वेद है। वेद कोई दार्शनिक ग्रन्थ नहीं है, वरन् दर्शनों के आधारभूत ग्रन्थ हैं। वेदों ने बाद के भारतीय दर्शनों पर अत्यधिक प्रभाव डाला, जिन्हें आज हम षड्दर्शन कहते हैं। वे सभी वेदों को मानने वाले हैं।
यद्यपि कुछ दर्शन वेदों को नहीं मानते, इनमें चार्वाक, बौद्ध तथा जैन शामिल हैं। इस दृष्टि से भी वेदों का महत्त्व है, क्योंकि भारत में जो चिन्तन हुआ, वह या तो वेदों के समर्थन के लिए या खण्डन के लिए। उल्लेखनीय है कि पहले ‘नास्तिक’ शब्द वेदनिन्दक के लिए प्रयुक्त होता था, किन्तु बाद में इसका अर्थ ‘अनीश्वरवादी’ हो गया।
© महत्त्वपूर्ण तथ्य
● श्रीमद्भागवद्गीता नीतिशास्त्र का विश्वविख्यात ग्रन्थ है गीता का मुख्य सन्देश ‘निष्काम कर्म’ है अर्थात् बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करना चाहिए। गीता में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म-तीन मार्गों की महिमा बताई गई है।
● चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है। इसके अनुसार जड़-जगत सत्य है और यह वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी-इन चार भौतिक तत्त्वों से बना है। चेतना की उत्पत्ति भौतिक तत्त्व से ही है।
● जैन दर्शन के अनुसार, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान एवं शब्द भी प्रमाण है। इस दर्शन के अनुसार जितना सजीव शरीर है, उतना ही चैतन्य जीव है। संसारिक बन्धन से छुटकारा पाने हेतु सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र, तीन उपाय बताए गए हैं।
● बौद्ध दर्शन के अनुसार, जगत के सभी जीवों में एवं सभी दशाओं में दुःख वर्तमान है और इस दुःख का कारण है- क्योंकि कोई भी भौतिक-आध्यात्मिक वस्तु अकारण नहीं है। संसार की सभी वस्तुएँ परिवर्तनशील हैं। मरण का कारण जन्म है। जन्म का कारण तृष्णा है और तृष्णा का कारण अज्ञान है। दुःखों के कारण यदि नष्ट हो जाए तो दुःख का अन्त भी हो जाएगा। चौथा सत्य ‘दुःख-निवृत्ति’ के उपाय के रूप हैं।
शिक्षा दर्शन का अर्थ
प्राचीनकाल में किसी भी प्रकार को दर्शन कहा जाता था, परन्तु जैसे-जैसे ज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ, वैसे-वैसे हमने उसे अलग-अलग अनुशासनों (विषयों) में विभाजित करना प्रारम्भ किया। यथा-मानव शास्त्र, धर्मशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि । ज्ञान की उस शाखा को जिसमें अन्तिम सत्य (Ultimate Reality) की खोज की जाती है, उसे दर्शन कहा जाता है।
सर जॉन एडम्स (Sir John Adams) के अनुसार, “शिक्षा, दर्शन का क्रियात्मक पहलू है। यह दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पहलू तथा जीवन के आदर्शों को वास्तविक रूप देने का क्रियात्मक साधन है।” सामान्यतः शिक्षा वह प्रभाव है, जो किसी प्रबल विश्वास से युक्त व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर इस उद्देश्य से डाला जाता है कि दूसरा व्यक्ति भी उसी विश्वास को ग्रहण कर ले।
एडम्स ने शिक्षा-विषयक के अनेक विश्लेषण में निम्नलिखित बातें रखी हैं
यह प्रक्रिया केवल चेतनशील (Conscious) ही नहीं, वरन् आयोजित (Deliberate) भी है। शिक्षक या गुरु के मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से यह आशय होता है कि वह शिष्य के विकास को सुधारे।
शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व के विकास में सुधार करने के लिए उस पर प्रभाव डालता है।
शिक्षा के विकास को सुधारने के दो साधन हैं
(i) शिक्षक के व्यक्तित्व का शिष्य के व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव डालना
(ii) ज्ञान के विभिन्न रूपों का प्रयोग।
हेण्डरसन के मतानुसार, “शिक्षा-दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन में प्रयोग है।”
शिक्षा दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कनिंघम (Cunningham) ने लिखा है-प्रथम, दर्शन सभी वस्तुओं का विज्ञान है, इस प्रकार शिक्षा-दर्शन, शिक्षा की समस्याओं को अपने सभी मुख्य पक्षों में देखता है।
द्वितीय, दर्शन सभी वस्तुओं को अन्तिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। इसलिए भी शिक्षा-दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतम समस्याओं का समग्र रूप में अध्ययन करता है और शिक्षा विज्ञान की उन समस्याओं को अध्ययन के लिए छोड़ देता है, जो तात्कालिक हैं तथा जिनका वैज्ञानिक विधि से सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है, उदाहरणस्वरूप-“छात्र- योग्यता के मापन की समस्या।”
शिक्षा एवं दर्शन का सम्बन्ध
शिक्षा तथा दर्शन के बीच केवल घनिष्ठ सम्बन्ध ही नहीं, अपितु दोनों एक-दूसरे पर आश्रित भी हैं। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है, जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन भी है। शिक्षाशास्त्री समय-समय पर दार्शनिकों के सम्मुख प्रायः ऐसी नई-नई तथा कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं, जो उन्हें अध्यापन कार्य के समय कठिनाई देती हैं।
इस प्रकार शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि महान् दार्शनिक महान् शिक्षाशास्त्री भी हुए हैं। सभी दार्शनिकों ने अपने-अपने दर्शन को क्रियात्मक अथवा व्यावहारिक रूप देने के लिए अन्त में शिक्षा का ही आश्रय लिया है। शिक्षा तथा दर्शन के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं
● स्पेन्सर के अनुसार, “वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है।”
● एडम्स के अनुसार, “शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है। यही दार्शनिक पक्ष हा पहा चिन्तन का सक्रिय पहलू है।”
● जे एस रॉस के अनुसार, “दर्शन तथा शिक्षा किसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और वे एक-दूसरे में अन्तर्निहित हैं। ”
● हरबर्ट के अनुसार, “जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यावहारिक रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक शिक्षा को चैन नहीं आ सकता । ”
● रॉस ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया है कि “शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन सैद्धान्तिक पहलू है, जबकि शिक्षा गतिशील तथा व्यावहारिक पहलू है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। दर्शन तब तक अधूरा रहता है जब तक उसकी व्यावहारिकता न हो और शिक्षा का स्वरूप बिना दर्शन के विकसित नहीं किया जा सकता। ”
शिक्षा से सम्बन्धित मूल प्रश्नों का उत्तर दर्शन ही देता है; जैसे
● शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए?
● गणित क्यों पढ़ाया जाना चाहिए?
● शिक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या हो?
● शिक्षा की प्रक्रिया क्या हो?
● शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए?
शिक्षा दर्शन के सरोकार व क्षेत्र
सरोकार (Concerns) शिक्षा- दर्शन शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करता है। इसके अन्तर्गत शिक्षा का उद्देश्य क्या हो? उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या पाठ्यक्रम बनाया जाए तथा अन्त में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ाने या शिक्षा देने की विधि क्या हो इत्यादि सभी पक्षों पर विचार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ में ज्ञान को विभिन्न शाखाओं में विभाजित नहीं किया गया था। उस समय ज्ञान की सभी शाखाएँ दर्शन ही थीं। थेल्स को पश्चिमी-दर्शन का जन्मदाता माना है, किन्तु उसने वैज्ञानिक पद्धति अपनाई थी। अरस्तू उच्चकोटि का दार्शनिक था, किन्तु इसे विज्ञान का जन्म दाता माना जाता है।
क्षेत्र (Scope) शिक्षण-
विधियों के क्षेत्र में विज्ञान तो योगदान देता ही है, शिक्षा-दर्शन का योगदान भी कम नहीं है। आज शिक्षा-दर्शन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया है। इसके अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी समस्त तत्त्वों एवं समस्याओं और अनुशासन आदि का अध्ययन करते हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा दर्शन की भूमिका यथा – शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक, शिक्षालय संगठन
का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है
● उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षा की प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो बात हमारे सामने आती है, वह है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना। अतः शिक्षा दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
● पाठ्यक्रम केवल पाठ्यक्रम को बना लेने से ही उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती, बल्कि पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन करना उसे सफल बनाना भी आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम को संचालित करने वाला शिक्षक होता है और इसकी सफलता शिक्षण-विधियों पर ध्यान देकर उपयोगी शिक्षण-विधि के प्रयोग में सहायता देता है।
● सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र शिक्षा-दर्शन सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक उपलब्धियों आदि के क्षेत्र में भी गहन अध्ययन और विचार करता है और उसी के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियाँ
आदि निर्धारित करती है।
● शिक्षालय संगठन और अनुशासन शिक्षा-दर्शन का एक विशेष महत्त्वपूर्ण क्षेत्र विद्यालय संगठन एवं अनुशासन आदि की समस्या का अध्ययन करना है। विद्यालय में अनुशासन का स्वरूप क्या हो अथवा अनुशासनहीनता को किस प्रकार दूर किया जाए आदि विषयों का अध्ययन दिशा-दर्शन में ही किया जाता है।
शिक्षक के लिए शिक्षा-दर्शन की उपादेयता
शिक्षक के लिए शिक्षा-दर्शन की उपादेयता के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख विद्वानों अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है
जॉन डीवी के अनुसार, “शिक्षा-दर्शन बने बनाए विचारों को व्यवहार की एक व्यवस्था पर लागू करना नहीं है, जिसमें पूर्णतया भिन्न उद्गम और प्रयोजन होते हैं। वह तो समकालीन सामाजिक जीवन की समस्याओं के विषय में सही मानसिक और नैतिक अभिवृत्तियों के निर्माण की समस्याओं से सम्बन्धित है अर्थात् शिक्षक शिक्षा-दर्शन से शिक्षण सिद्धान्त प्राप्त करता है। ”
स्पेंसर के अनुसार, “केवल एक सच्चा दार्शनिक ही शिक्षा को व्यावहारिक रूप दे सकता है। वह विद्यार्थियों से कैसे व्यवहार करता है और उन्हें अपनी बात कैसे समझाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षार्थी उसके लिए क्या हैं।”
बर्ट्रेण्ड रसेल के अनुसार, “दर्शन शास्त्र का अध्ययन प्रश्नों के सुनिश्चित उत्तर प्राप्त करने हेतु नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि स्वयं प्रश्नों के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न सम्भावनाओं की हमारी अवधारणा को व्यापक बनाते हैं। हमारी बौद्धिक कल्पना को समृद्ध करते हैं और हठवादी सुनिश्चितता को कम करते हैं, जोकि कल्पना के विरुद्ध मस्तिष्क को बन्द कर देती है, बल्कि सर्वोपरि क्योंकि विश्व की महानता जिस पर दर्शन विचार करता है मस्तिष्क को भी महान् और विश्व से एकीकरण के योग्य बना देती है, जोकि उसके सर्वोच्च शुभ का निर्माण करता है।”
नोट शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन का सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के लक्ष्यों और आदर्शों को लेकर है।
आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा दर्शन का महत्त्व शिक्षा
दर्शन में ‘शिक्षा’ और ‘दर्शन’ दो शब्द मिले हुए हैं तथा ये दोनों शब्द मानव के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। ये दोनों अंग एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक (सैद्धान्तिक पक्ष है, जबकि शिक्षा क्रियात्मक (व्यावहारिक) पक्ष है।
शिक्षा-दर्शन का महत्त्व शिक्षक के लिए निम्नलिखित कारणों से है
● शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का हल
● शिक्षा का पथ-प्रदर्शन
● शिक्षा प्रक्रिया की स्पष्टता
● शैक्षणिक प्रश्न जीवन दर्शन से सम्बन्धित शिक्षा में प्रयोग के लिए अवसर
● शिक्षा और दर्शन अन्योन्याश्रित
● शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण
● शिक्षा के सिद्धान्त, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, छात्र प्रकाशक आदि की सम्यक् जानकारी
● शिक्षण विधियों का निर्माण
● अनुशासन की स्थापना हेतु
शिक्षा के दार्शनिक आधार
दर्शन और शिक्षा में अटूट सम्बन्ध पाया जाता है और ये एक-दूसरे पर आश्रित होते हैं। दर्शन ब्रह्माण्ड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है। इसमें मनुष्य जीवन के अन्तिम उद्देश्य और उस उद्देश्य की प्राप्ति के साधन मार्गों पर भी विचार किया जाता है। अब ये उद्देश्य कैसे प्राप्त हों, इसमें शिक्षा हमारी सहायता करती है। शिक्षा हमारे आचार-विचार में परिवर्तन करती है और हमें नए ज्ञान की खोज करने के लिए अवलोकन, परीक्षण, चिन्तन और मनन शक्तियों का विकास करती है।
।
इस ज्ञान एवं कौशल के आधार पर हम दर्शन का पुनर्निर्माण करते हैं। नया दर्शन नई शिक्षा को जन्म देता है और नई शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है और यह चक्र सदैव चलता रहता है। दर्शन और शिक्षा की इस अन्योन्याश्रितता को समझने के लिए दर्शन के शिक्षा पर प्रभाव और शिक्षा के दर्शन पर प्रभाव को अलग-अलग समझना होगा।
दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव
दर्शन का शिक्षा पर पड़ने वाला प्रभाव निम्नलिखित है
● दर्शन और शिक्षा का सम्प्रत्यय दर्शन शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है। इस व्याख्या से हमें शिक्षा के सही सम्प्रत्यय का ज्ञान होता है।
● दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य दर्शन का सर्वप्रथम भाग तत्त्वमीमांसा होता है। इसमें सृष्टि-सृष्टा, आत्मा-परमात्मा, जीव-जगत और जन्म-मरण आदि की व्याख्या होती है और उसके आधार पर मानव जीवन के उद्देश्य दिए जाते हैं। शिक्षा द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।
● दर्शन और शिक्षा की पाठ्यचर्या पाठ्यचर्या तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। अतः यदि शिक्षा के उद्देश्य दर्शन से प्रभावित होते हैं, तो उसकी पाठ्यचर्या भी उससे प्रभावित होनी चाहिए।
● दर्शन और शिक्षण विधियाँ दर्शन की ज्ञानमीमांसा से मानव बुद्धि, ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की विधियों की व्याख्या होती है। इसी के आधार पर दार्शनिक शिक्षण विधियों का विधान करते हैं।
दर्शन और अनुशासन दर्शन का तीसरा मुख्य भाग आचारमीमांसा होता है। इसमें मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए और क्या नहीं, इसकी विशद् व्याख्या होती है। इस ज्ञान के आधार पर ही अनुशासन का सम्प्रत्यय नि
श्चित किया जाता है।
दर्शन शिक्षक तथा शिक्षार्थी दर्शन की तत्त्वमीमांसा में मनुष्य के स्वरूप और आचारमीमांसा में उसके करणीय तथा अकरणीय कर्मों की विशद व्याख्या की जाती है। दर्शन की इस व्याख्या के अनुसार ही शिक्षक और शिक्षार्थी का स्वरूप एवं उनके कर्त्तव्य निश्चित होते हैं।
दर्शन और विद्यालय प्रायः सभी दार्शनिक मनुष्य के लिए आचार संहिता तैयार करते हैं और इसके लिए शिक्षा का विधान करते हैं। अब यह शिक्षा कहाँ दी जाए और कैसे दी जाए, इस पर भी वे प्रकाश डालते हैं।
शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव
शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव निम्नलिखित है
● शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है शिक्षा के द्वारा ही हम भाषा सीखते हैं और उसी के द्वारा हम विचार करना सीखते हैं। अशिक्षित व्यक्ति से दर्शन जैसे विषय के विकास की आशा नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से शिक्षा दर्शन के विकास की आधारशिला होती है।
● शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है कोई भी समाज अपने पूर्वजों द्वारा निश्चित इन सिद्धान्तों का ज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त करता है। शिक्षा के अभाव में हम दार्शनिक सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार शिक्षा दर्शन के ज्ञान को सुरक्षित रखती है।
● शिक्षा दार्शनिक सिद्धान्तों को मूर्त रूप देती है दर्शन इस ब्रह्माण्ड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है, मनुष्य जीवन की व्याख्या करता है। मनुष्य जीवन के उद्देश्य निश्चित करता है और यह स्पष्ट करता है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। शिक्षा वह प्रकिया है, जिसके द्वारा हम दर्शन के निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। अंग्रेज विद्वान् जॉन एडम्स महोदय इस सत्य को स्वीकार करते हुए कहा करते थे कि “शिक्षा दर्शन का एक गतिशील पहलू है।” अमेरिकी विद्वान् जॉन डीवी ने इसी सत्य को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है “दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धान्त ही है। ”
● शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है मनुष्य एक गतिशील और प्रगतिशील प्राणी है। विकास के इस पथ में उसके सामने नित्य नई समस्याएँ आती रहती हैं। शिक्षा हमें इन समस्याओं से परिचित कराती हैं और यदि हम में दार्शनिक की तीक्ष्ण बुद्धि होती है, तो हम उन समस्याओं पर विचार करने लगते हैं जिससे दर्शन का विकास होता है।
इस प्रकार जनशिक्षा, स्त्री-शिक्षा और शिक्षा में राज्य के हस्तक्षेप आदि पर भी विचार करता है, इतना ही नहीं अपितु शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी और किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हम दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रयोग करते हैं।
शिक्षा में भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का योगदान
भारतीय सन्दर्भ में दर्शन का अर्थ परम तत्त्व का साक्षात्कार करना है। भारतीय दर्शन का लक्ष्य आध्यात्मिक, अधिभौतिक तथा अधिदैविक तीनों प्रकार के दुःख का विनाश एवं अखण्ड आनन्द की प्राप्ति है। वैदिक दर्शनों में षड्दर्शन अत्यधिक प्राचीन एवं प्रसिद्ध है। ये सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदान्त के नाम से विदित हैं।
शिक्षा और दर्शन दोनों ही एक-दूसरे पर निर्भर हैं, दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा दार्शनिक दृष्टिकोणों पर नियन्त्रण रखती है तथा उसकी कमियों को दूर
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 2 NOTES IN HINDI
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 2 NOTES IN HINDI PDF
ईकाई 2 शिक्षा का इतिहास राजनीति और अर्थशास्त्र नोट्स
| इस यूनिट से सम्बन्धित नोट्स जल्द हो जोड़ा जायेगा | |
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 3 NOTES IN HINDI
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 3 NOTES IN HINDI PDF
ईकाई 3 शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया नोट्स
| इस यूनिट से सम्बन्धित नोट्स जल्द हो जोड़ा जायेगा | |
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 4 NOTES IN HINDI
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 4 NOTES IN HINDI PDF
ईकाई 4 अध्यापक शिक्षा नोट्स
| इस यूनिट से सम्बन्धित नोट्स जल्द हो जोड़ा जायेगा | |
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 5 NOTES IN HINDI
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 5 NOTES IN HINDI PDF
ईकाई 5 पाठ्यचर्या अध्ययन नोट्स
| इस यूनिट से सम्बन्धित नोट्स जल्द हो जोड़ा जायेगा | |
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 6 NOTES IN HINDI
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 6 NOTES IN HINDI PDF
ईकाई 6 शिक्षा में शोध नोट्स
| इस यूनिट से सम्बन्धित नोट्स जल्द हो जोड़ा जायेगा | |
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 7 NOTES IN HINDI
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 7 NOTES IN HINDI PDF
ईकाई 7 शिक्षणशास्त्र, प्रौढशिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन नोट्स
| इस यूनिट से सम्बन्धित नोट्स जल्द हो जोड़ा जायेगा | |
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 8 NOTES IN HINDI
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 8 NOTES IN HINDI PDF
ईकाई 8 शिक्षा में/के लिए प्रौद्योगिकी नोट्स
| इस यूनिट से सम्बन्धित नोट्स जल्द हो जोड़ा जायेगा | |
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 9 NOTES IN HINDI
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 9 NOTES IN HINDI PDF
ईकाई 9 शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व नोट्स
| इस यूनिट से सम्बन्धित नोट्स जल्द हो जोड़ा जायेगा | |
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 10 NOTES IN HINDI
UGC NET PAPER 2 UDUCATION UNIT 10 NOTES IN HINDI PDF
ईकाई 10 समोवशी शिक्षा नोट्स
| इस यूनिट से सम्बन्धित नोट्स जल्द हो जोड़ा जायेगा | |