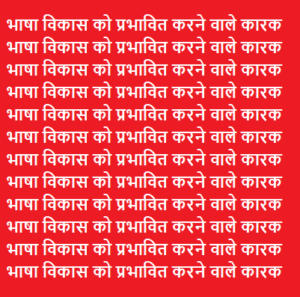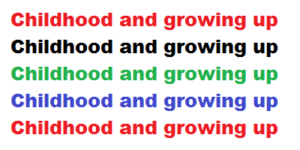लिंग विद्यालय एवं समाज
Ling vidyaalay evan Samaaj
| विषय | लिंग विद्यालय एवं समाज |
| SUBJECT | Ling vidyaalay evan Samaaj |
| SUBJECT | Gender, School and Society |
| UNIVERSITY | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय |
| COURSE | बी.एड प्रथम सेमेस्टर |
| PAPER | २ |
| CODE | 103 |
| lnfo | इस पेज में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के लिंग विद्यालय एवं समाज सिलेबस , नोट्स एवं क्वेश्चन पेपर को शामिल किया गया है | |
VVI NOTES के इस पेज में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के लिंग विद्यालय एवं समाज सिलेबस , लिंग विद्यालय एवं समाज नोट्स , लिंग विद्यालय एवं समाज क्वेश्चन पेपर , लिंग विद्यालय एवं समाज सीरिज , लिंग विद्यालय एवं समाज प्रश्न उत्तर ,लिंग विद्यालय एवं समाज गेस पेपर , लिंग विद्यालय एवं समाज गाइड ,लिंग विद्यालय एवं समाज बुक ,लिंग विद्यालय एवं समाज प्रश्न ,लिंग विद्यालय एवं समाज क्वेश्चन पेपर इत्यादी को सामिल किया गया है |
लिंग विद्यालय एवं समाज सिलेबस
LING VIDYALALAY EVAN SAMAAJ SYLLABUS
| विषय | लिंग विद्यालय एवं समाज
Ling vidyaalay evan Samaaj Syllabus |
| SUBJECT | Gender, School and Society Syllabus |
| पेपर कोड | 103 |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय |
| कोर्स | बी.एड |
| सेमेस्टर | प्रथम सेमेस्टर |
| F.M | 100 (FULL MARKS) |
| lnfo | यहाँ महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के पेपर कोड 103 लिंग विद्यालय एवं समाज के सिलेबस दिया गया है | यह विषय सभी स्टूडेंट्स का समान होता है | |
Unit-1
A. Meaning of Gender and sex, Difference between Sex and Gender. Concept of
Masculinity and Feminity Specific roles.
B. Nature and characteristics of Indian society, Agency of Socialization: School
family, community activity centers and hobbyclub.
Unit-2
A. Emergence of Gender roles, Agencies of education with reference to gender:
Family, community, school and mass media.
B. Gender Inequalities in Society: Causeds and probable solutions, Concept of gender equality and equity. Influence of gender equality and empowerment of women.
Unit-3
A. Co-education Schools: Their strengths and weaknesses in the Indian Con- text. Gender inequality in the classroom: Co-education and single ‘sex school- ing. The girl child in the Indian Society.
B. Curriculum and Teaching Transactions: vulnerable areas for gender dis- crimination. Measures to provide discrimination free school system. Incentives for the education of girls. Creation gender inclusive class- room, teaching learning material and classroom transaction.
Unit-4
A. The role of teachers in formulating positive notions about every gender among students. gender studies- shift from women studies to gender studies.
B. Incentives of government to promote gender equality with special refer- ence to women and transgender. Transgender-Concept, legal provisions and strategies for empowerment. Supreme court verdict about transgender.
(2) लिंग विद्यालय एवं समाज नोट्स
LING VIDYALALAY EVAN SAMAAJ NOTES
| विषय | लिंग विद्यालय एवं समाज नोट्स
Ling vidyaalay evan Samaaj Notes |
| SUBJECT | Gender, School and Society Question- Answer |
| पेपर कोड | 103 |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय |
| कोर्स | बी.एड |
| सेमेस्टर | प्रथम |
| FULL MARKS | |
| lnfo | यहाँ महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के पेपर -103 समावेशी शिक्षा के नोट्स दिया गया है | |
लघु उत्तरीय प्रश्न
(Short Answer Type Questions)
निर्देश : इस खण्ड में प्रश्न संख्या 1 (a से j) लघु उत्तरीय प्रश्न है। परीक्षार्थियों को सभी दस (a से j) प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। (10 × 4 = 40 अंक)
प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए-
प्रश्न : (i) लिंग और जेण्डर में अंतर बताइए।
उत्तर-
लिंग पुरुष और महिला शरीर के बीच जैविक अंतरों को संदर्भित करता है, जबकि जेंडर अन्य सभी चीजों को संदर्भित करता है जो हमें “पुरुष” और “महिला” बनाती है। जहाँ हमारा जैविक जन्म हमें एक पुरुष या महिला के रूप में परिभाषित करता है, वहीं समाज ने लिंग के आधार पर भूमिकाओं में अंतर किया है। इन दोनों में निम्न अंतर पाए जाते हैं-
(1) लिंग स्थिर होता है तथा प्रकृति पर आधारित होता है, जबकि जेण्डर अस्थिर होता है तथा संस्कृति पर आधारित होता है। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि लिंग एक जैविक तथ्य है, जबकि जेण्डर सीखा हुआ व्यवहार है, जो समय के साथ बदलता रहता है तथा विभिन्न संस्कृतियों में भी इसके स्वरूप में अन्तर हो सकता है।
(2) ‘जेण्डर’ शब्द सम्बन्धमूलक है क्योंकि यह केवल स्त्री या पुरुष का द्योतक नहीं है, अपितु उनमें पाए जाने वाले सम्बन्धों को भी स्पष्ट करता है, जबकि लिंग में ऐसा नहीं है क्योंकि यह केवल मात्र स्त्री या पुरुष का द्योतक है। किसी विशिष्ट समय में जेण्डर से अभिप्राय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों एवं अवसरों से है, जो पुरुष या स्त्री के साथ जुड़े होते हैं। अनेक समाजों में ” परम्परागत जेण्डर आधारित लक्षणों में भी भेद किया जाता है। उदाहरणार्थ, विनम्र होना स्त्रियोचित गुण
है, जबकि प्रबल होना पुरुषोचित गुण है। इसी प्रकार, भावुक होना, ग्रहणशील होना, संकोची होना, निष्क्रिय होना अथवा कोमल हृदय होना स्त्रियोचित गुण माने जाते हैं, जबकि तार्किक होना, आग्रही होना, विश्लेषणपरक होना, बहादुर होना, सक्रिय होना तथा कठोर हृदय होना पुरुषोचित गुण माने जाते हैं, जिनको जेण्डर से जोड़ा जाता है।
प्रश्न a (ii) लिंग तथा लैंगिकता का अर्थ ।
उत्तर-
लिंग तथा लैंगिकता हेतु आंग्ल भाषा में Gender तथा Sex शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लिंग (Gender) का प्रयोग हम व्यक्तियों तथा आस-पास की वस्तुओं के नामों में भी प्रयुक्त करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य के दो रूप सृष्टि के समुचित परिचालन हेतु बनाये, जिसमें एक है स्त्री और दूसरा है पुरुष । स्त्री तथा पुरुष ही अपनी प्रारम्भ अवस्था में बालिका और बालक से सम्बोधित किये जाते हैं। हमारे आस-पास के पर्यावरण में हम जो कुछ भी देखते हैं उसे किसी-न-किसी नाम से जानते हैं और इन नामों में ही उनका लिंग छुपा होता है।
व्याकरणिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाये तो संस्कृत में तीन लिंग हैं-
(1) स्त्रीलिंग – स्त्रीबोधक
(2) पुल्लिंग – पुरुषबोधक
(3) नपुंसकलिंग – स्त्री तथा पुरुष से अतिरिक्त हेतु ।
हिन्दी व्याकरण में तीन लिंग तथा अंग्रेजी ग्रामर में भी तीन लिंग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार व्याकरण की शब्दावली में जिससे किसी के स्त्री-पुरुष या उससे अतिरिक्त होने का बोध हो, वह लिंग कहलाता है।
लिंग का सामान्य जीवन में प्रयोग स्त्री-पुरुष के सन्दर्भ में होता है, परन्तु यहाँ लिंग की अवधारणा और उससे जुड़े विषयों में व्यापक अर्थ है।
लिंग से ही मिलता-जुलता शब्द है लैंगिकता अथवा कामुकता। सृष्टि की प्रक्रिया के सुचारु रूप से चलने हेतु काम की भावना ईश्वर ने प्रत्येक जीव को प्रदान की जो विपरीत लिंग के संसर्ग से पूर्ण होकर अपनी भाँति के किसी नये जीव का विकास करती है। इस प्रकार अपने व्यापक अर्थों में लैंगिकता से तात्पर्य लिंग के प्रति आकर्षण, अवबोध, भेदभाव, सम्पर्क, सहयोग इत्यादि से है।
प्रश्न a (iii) लिंग तथा लैंगिकता का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य ।
उत्तर-
लिंग तथा लैंगिकता की व्यक्ति के अपने मनोविज्ञान तथा समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यावश्यक हो जाता है। आज बालक हो या बालिका, दोनों ही एक-दूसरे से अलग-थलग होकर न तो अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और न ही समाज का सर्वांगीण विकास। अतः लिंग और लैंगिकता के भीतर निहित मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्यों से अवगत होना अत्यावश्यक हो जाता है।
लिंग तथा लैंगिकता के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यों से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि मनोविज्ञान क्या है? इसकी क्या परिभाषा है? यह जानने के लिए निम्नांकित वर्णन दृष्टव्य है-
1. मनोविज्ञान को गैरिट ने आत्मा का विज्ञान माना है जिसमें ‘साइकोलॉजी’ (Psychology) शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों- ‘साइकी’ (Psychi), जिसका अर्थ है- ‘आत्मा’ (Soul) तथा ‘लोगस’ (Logos), जिसका अर्थ है- ‘अध्ययन’ (Study) से हुई है। इस प्रकार मनोविज्ञान का अर्थ है – ‘Study of the Soul’ अर्थात् ‘आत्मा का अध्ययन’। प्लेटो, अरस्तू, डेकार्टे इत्यादि ने भी इसे ‘आत्मा का विज्ञान’ माना है।
2. मध्य युग के दार्शनिकों, जिनमें इटली के दार्शनिक पोम्पोनाजी का नाम उल्लेखनीय है, ने मनोविज्ञान को ‘मस्तिष्क का विज्ञान’ बताया।
3. 16वीं शताब्दी में वाइत्स, विलियम जेम्स, विलियम वुण्ट, जेम्ससन इत्यादि विद्वानों ने मनोविज्ञान को ‘चेतना का विज्ञान’ बताया।
4. 20वीं शताब्दी के आरम्भ में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ बताये गये, जिसमें सर्वाधिक मान्यता ‘व्यवहार के विज्ञान’ को दी गयी।
प्रश्न a (iv) भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-
(i) प्राचीनता के साथ स्थायित्व,.
(ii) क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता,
(iii) आध्यात्मवाद की अवधारणा के महत्त्व,
(iv) भाषायी विविधता,
(v) धर्म की प्रमुखता,
(vi) सहिष्णुता,
(vii) प्रजातीय विविधता,
(viii) धार्मिक विविधता,
(xi) जातिगत विविधता,
(x) सांस्कृतिक विविधता,
(xi) जनांकिकीय विविधता,
(xii) समन्वय,
(xiii) अनुकूलनशीलता,
(xiv) सर्वांगीणता,
(xv) कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास,
(xvi) विविधता में एकता,
(xvii) जाति व्यवस्था आदि।
प्रश्न a (v) समाजीकरण के अभिकरण में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
परिवार ही व्यक्ति का समाजीकरण करता है। वह समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक नियमों के अनुकूल बनाता है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को सामाजिक आदर्शों, संस्कृति, परंपराओं, रुढ़ियों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है तथा वह आगे चलकर जीवन में इन सीखी हुई बातों को प्रयोग में लाता है। बालक जन्म के समय कोरा पशु के समान होता है। जैसे-जैसे वह परिवार के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है वैसे-वैसे वह अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हुए सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों को सीखता रहता है। इसी लिए परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहते हैं परिवार के बाद बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है और समाजीकृत होता है।
प्रश्न a (vi) लिंग तथा लैंगिकता का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का महत्व बताइए।
उत्तर—
लिंग तथा लैंगिकता का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का महत्व निम्न कारणों से है-
1. मूल- प्रवृत्तियों तथा सहज क्रियाओं हेतु,
2. स्वस्थ लैंगिक विकास हेतु,
3. अभिवृद्धि तथा विकास हेतु,
4. चारित्रिक विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण हेतु,
5. मानवता के विकास हेतु,
6. अधिगम हेतु,
7. रुचि तथा व्यक्तिगत विभिन्नता हेतु,
8. आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण हेतु,
9. निर्देशन एवं परामर्श हेतु,
10. मानव व्यवहारों के ज्ञान हेतु ।
प्रश्न a (vii) मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएँ ।
उत्तर –
मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं-
(1) मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात तथा आन्तरिक होती हैं।
(2) मूल-प्रवृत्तियाँ किसी-न-किसी रूप में संसार के सभी प्राणियों में पायी जाती हैं, अतः ये सार्वभौम विशेषता-सम्पन्न हैं।
(3) मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति हेतु किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती।
(4) प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित होती है।
(5) मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का ज्ञान पहले से नहीं होता है।
(6) मूल-प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार से पृथक् नहीं किया जा सकता।
प्रश्न a (viii) लिंग तथा लैंगिकता के संशोधित होने के कारण बताइए।
उत्तर—
(1) बालक तथा बालिकाओं के पालन-पोषण में अन्तर होता है। इस कारण उनकी मूल-प्रवृत्तियों का प्रकाशन भिन्न-भिन्न होता है, जैसे- बालिकाओं को प्रारम्भ से ही मूल प्रवृत्तियों को दबाना और सीमित रखना सिखाया जाता है जबकि बालकों में यह प्रवृत्ति खुली हुई होती है।
(2) मूल-प्रवृत्तियाँ बालक तथा बालिकाओं में न्यूनाधिक्य रूप से पायी जाती है। उदाहरणस्वरूप बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा शिशु रक्षा, संवेदना, संचय की प्रवृत्ति तो वहीं बालकों में क्रोध, कामुकता, श्रेष्ठता, अधिकार की भावना इत्यादि संवेग ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि उन्हें इसे दबाने की शिक्षा बालिकाओं की अपेक्षा कम मिलती है और बालिकाओं को प्रारम्भ से ही अपने संवेगों को नियंत्रित करना सिखाया जाता है।
(3) सहज क्रिया अर्थात् जिनको हम यन्त्रवत् और बिना विचारे करते हैं, कहलाती है। इस पर भी लिंग तथा लैंगिकता का प्रभाव देखने को मिलता है। लिंग के आधार पर इन सहज प्रवृत्तियों में बालक तथा बालिकाओं में सहज क्रियाओं को देखा जा सकता है, जैसे-बालिकाएँ प्रारम्भ से ही घरेलू क्रियाकलापों में तथा बालक प्रारम्भ से ही बाह्य क्रियाकलापों में सहज रूप से रुचि लेने लगते हैं।
प्रश्न a (ix) लिंग तथा लैंगिकता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का महत्त्व।
उत्तर—
लिंग तथा लैंगिकता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का महत्त्व इस प्रकार है-
1. पालन-
पोषण-बालक तथा बालिकाओं के पालन-पोषण पर समाज का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। मनुष्य शिशु जन्म के कुछ समय तक अपने परिवार तथा समाज पर निर्भर रहता है और जब तक वह जीवित भी रहता है तब तक समाज पर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर रहता है। समाज का स्वरूप यदि बन्द समाज का होगा तो लिंग के आधार पर बालक तथा बालिकाओं के पालन-पोषण में अन्तर होगा और यदि खुला तथा प्रगति उन्मुख समाज होगा तो उस समाज में लिंग तथा लैंगिकता विषयी दृष्टिकोण में व्यापकता और खुलापन होगा।
2. वातावरण सृजन —
समाज बालक तथा बालिकाओं के लिए जैसा वातावरण सृजित करेगा, उनका विकास उसी प्रकार का होगा। समाज में यदि लिंग तथा लैंगिकता के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं है तो ऐसे वातावरण में भेदभाव और भावना ग्रन्थियों के पनपने की आशंका अधिक होती है और ऐसा समाज लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाकर स्वस्थ वातावरण सृजित किया जा रहा हो वहाँ पर एक परस्पर अन्तर्क्रिया तथा वैचारिक आदान-प्रदान का वातावरण सृजित होता है।
3. सुरक्षात्मक कार्य-
समाज बालक तथा बालिकाओं को शारीरिक, सांवेगिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य सम्पन्न करता है जिससे सुरक्षात्मक अनुभूति आती है । सभ्य समाज बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की सुरक्षा हेतु अधिक सचेष्ट होते हैं और बालकों में प्रारम्भ से ही बालिकाओं के प्रति आदर-सम्मान की भावना भरते हैं।
4. सर्वांगीण विकास-
समाज अपने सभी सदस्यों के सर्वांगीण विकास का कार्य सम्पन्न करता है। इस हेतु समाज तरह-तरह के सामाजिक आयोजन करता है और अपने सदस्यों को उनमें भाग लेने हेतु अवसर प्रदान करता है। बालक और बालिकाओं में लिंगाधारित भेदभाव न करके समाज को समान रूप से उनके सर्वांगीण विकास हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए।
5. नैतिक तथा चारित्रिक विकास-
समाज बालक तथा बालिकाओं को समाजोपयोगी तथा आदर्श नागरिक बनाने हेतु उनके नैतिक तथा चारित्रिक विकास पर बल देता है। नैतिक तथा चारित्रिक गुण बालक तथा बालिकाओं में कुछ सामान्य रूप से तथा कुछ विशिष्ट रूप से पाये जाते हैं बालिकाओं में जिन नैतिक तथा चारित्रिक गुणों की अनिवार्यता होती है वे आवश्यक नहीं कि बालकों में भी हों और बालकों में पाये जाने वाले नैतिक तथा चारित्रिक गुण आवश्यक नहीं कि वे बालिकाओं में भी पाये जाये। इस प्रकार नैतिक तथा चारित्रिक विकास का महत्वपूर्ण कार्य समाज लिंग तथा लैगिंकता को दृष्टिगत रखते हुए करता है।
प्रश्न (a) (x) भारत में लैंगिक असमता (असमानता) किस रूप में पायी जाती है?
उत्तर-
भारत पुरुष प्रधान एवं पितृसत्तात्मक समाज है। इसमें अन्य सभी समाजों की तरह जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों एवं स्त्रियों में लैंगिक असमता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारत में स्त्रियों एवं पुरुषों में लैंगिक असमता निम्न रूपों में देखी जा सकती है-
लिंग-भेदभाव : सामाजिक फन्दे का अत्याचार (Sex Discrimination : The Tyranny of Social Trap)-
प्रत्येक पितृसत्तात्मक परिवार का यह सामान्य लक्षण है कि वहाँ पुरुष की प्रधानता होती है और स्त्री का अवमूल्यन होता है। भारतीय समाज में इसका रूप अत्यन्त कठोर है। लड़की का जन्म ही अपने में अभिशाप है। पुत्र मुक्तिदाता, बुढ़ापे का सहारा और घर की पूँजी है, जबकि पुत्री का जन्म एक दायित्व और कर्ज है। इसलिए जन्म से ही लिंग-भेदभाव शुरू हो जाता है। इनके लालन- पालन के तौर-तरीके बिल्कुल अलग-अलग हैं। के.एम. पणिक्कर (K.M. Panikkar) ने स्पष्ट लिखा है कि “हिन्दू सामाजिक जीवन की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक हिन्दू संयुक्त परिवार में स्त्री को प्रदान की जाने वाली प्रस्थिति है। आधारभूत रूप से हिन्दू सामाजिक व्यवस्था यह मानकर चलती है कि पुत्री परिवार का भाग नहीं है। वह तो एक ऐसा आभूषण है जो गिरवी रखा है और जब उसका कानूनी मालिक आयेगा और उसकी मांग करेगा, तो उसे दे दिया जायेगा।”
प्रश्न (a) (xi) भारत में लैंगिक असमता को कम करने हेतु सुझाव दीजिए।
उत्तर-
लैंगिक असमता एवं स्त्री सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए हम निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं-
1. वैधानिक सुधार-स्त्री-
संगठनों की सहभागिता व सलाह से स्त्री सम्बन्धी एक भारतीय स्त्री अधिनियम पारित हो जो विवाह, उत्तराधिकार, सम्पत्ति, यौन, सन्तानोत्पत्ति आदि विषयों पर स्पष्ट आदेश प्रदान करे। भारत की प्रत्येक वयस्क स्त्री को यह अधिकार दिया जाए कि वह बिना धर्म, जाति, समुदाय के भेदभाव के अपने लिए इस अधिनियम को ग्रहण कर सकती है, इसका लाभ उठा सकती है।
2. स्त्री-शिक्षा का प्रसार-
स्त्री-शिक्षा न केवल अनिवार्य की जाए वरन निर्धन परिवारों की कन्याओं को छात्रवृत्तियाँ भी दी जाएँ। स्त्री छात्रावासों की व्यवस्था की जाए। इस शिक्षा का आधुनिक अर्थों में व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए। स्कूलों के साथ ही एक उत्पादन केन्द्र भी हो तो और भी अच्छा है। स्त्री-शिक्षा का उद्देश्य स्त्री को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाना होना चाहिए।
3. रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन-
स्त्रियों में अधिक-से-अधिक रोजगार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को आरक्षण व सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति अपनानी चाहिए। स्त्रियों को वे सब सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों व जनजातियों को मिल रही हैं।
प्रश्न (b)(i)’लिंग’ (जेण्डर) से आप क्या समझते हैं?
उत्तर-
लिंग शब्द व्याकरण की दृष्टि से तीन लिंगों का द्योतक है-
1. स्त्रीलिंग – स्त्री का बोधक है
2. पुल्लिंग -पुरुष का बोधक है।
3. नपुंसकलिंग – स्त्री तथा पुरुष के अतिरिक्त का बोधक है।
सामान्य व्यवहार में हम लिंग से तात्पर्य स्त्री और पुरुष होने से लगाते हैं। मनुष्यों में स्त्री तथा पुरुष आते हैं, परन्तु मनुष्य स्वयं इस संतुलन को बिगाड़कर मात्र पुरुषों का ही वर्चस्व रखना चाहता है, क्योंकि लिंगीय भेदभाव अपने चरम पर है। लिंग के निर्धारण में कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से योगदान पर से नहीं दे सकता। इस प्रकार यह ऐच्छिक क्रिया न होकर अनैच्छिक क्रिया है।
इस प्रकार जैविक रूप से लिंग को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब पुरुष का X और स्त्री का X गुणसूत्र मिलता है तो बालिका और जब पुरुष की ओर से Y तथा स्त्री जिसके पास XX ही गुणसूत्र है, इसमें से X मिलता है तब बालक का निर्माण होता है। स्पष्ट है कि लिंग निर्धारण में स्त्री या पुरुष किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह कार्य अनैच्छिक है, परन्तु हमारे समाज पुत्र न होने पर स्त्री को प्रताड़ित किया जाता है।
प्रश्न (b) (ii) लैंगिक असमानता के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर
प्रत्येक समाज में लैंगिक असमता अनेक रूपों में विद्यमान रहती है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन (Amartya Sen) के अनुसार, “लैंगिक असमता विश्व के सभी देशों- जापान से जाम्बिया तथा यूक्रेन से संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, परन्तु पुरुषों एवं स्त्रियों में असमता अनेक रूपों में होती है।” यह एक सजातीय प्रघटना न होकर अनेक अन्तर्सम्बन्धित समस्याओं से जुड़ी प्रघटना है। इनके अनुसार लैंगिक असमता को सामान्यतः निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-
1. मर्त्यता असमता-
विश्व के अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों एवं पुरुषों में असमता का एक बर्बर प्रकार सामान्यतया स्त्रियों की उच्च मर्त्यता दर में परिलक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है। मर्त्यता असमता अत्यधिक मात्रा में उत्तरी अफ्रीका तथा एशिया (चीन एवं दक्षिण एशिया सहित) में देखी जा सकती है।
2. विशेष अवसर असमता-
यूरोप तथा अमेरिका जैसे अत्यधिक विकसित एवं अमीर देशों के साथ-साथ अधिकांश अन्य देशों में उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण में लैंगिक पक्षपात स्पष्टतया देखा जा सकता है।
3. व्यावसायिक असमता-
व्यावसायिक असमता भी लगभग सभी समाजों में पायी जाती है। जापान जैसे देश में, जहाँ जनसंख्या को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं अन्य सभी प्रकार की मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ पर भी रोजगार एवं व्यवसाय प्राप्त करना स्त्रियों के लिए पुरुषों की में काफी कठिन कार्य माना जाता है। ।
प्रश्न (b) (iii) लैंगिक असमता का अर्थ बताइए ।
उत्तर –
पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग एक जैविकीय तथ्य हैं। यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड़ दी जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य बन जाता है जिसे लैंगिक असमता कहा जाता है। ‘लिंग’ शब्द का प्रयोग पुरुषों तथा स्त्रियों के गुणों के कुलक तथा उनके समाज द्वारा उनसे अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान इन्हीं अपेक्षाओं से होती है। ये अपेक्षाएँ इस विचार पर आधारित हैं कि कुछ गुण, व्यवहार, लक्षण, आवश्यकताएँ तथा भूमिकाएँ पुरुषों के लिए ‘प्राकृतिक’ हैं, जबकि कुछ अन्य गुण एवं भूमिकाएँ स्त्रियों के लिए प्राकृतिक हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि लिंग केवल जैवकीय नहीं है क्योंकि लड़का या लड़की जन्म के समय यह नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, क्या सोचना है अथवा किस प्रकार से प्रतिक्रिया करनी है। प्रत्येक समाज में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के रूप में उनकी लैंगिक पहचान तथा सामाजिक भूमिकाएँ समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से निश्चित की जाती हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा उन्हें उन सांस्कृतिक अपेक्षाओं का ज्ञान दिया जाता है जिनके अनुसार उन्हें व्यवहार करना है। ये सामाजिक भूमिकाएँ एवं अपेक्षाएँ एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में अथवा एक ही समाज के भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न होती हैं।
प्रश्न (b) (iv) विद्यालय का समुदाय पर प्रभाव का वर्णन कीजिए।
उत्तर –
समुदाय पर विद्यालय के प्रभाव का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जाता है-
(1) समुदाय की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण- प्रत्येक समुदाय के अपने रीति- रिवाज, परम्पराएँ, विश्वास, नैतिकता, नियम, साहित्य आदि होते हैं जिनको उस समुदाय ने प्राचीन समय से लेकर आज तक अर्जित किया है। शिक्षा, समुदाय की इस सांस्कृतिक विरासत को बनाये रखने तथा विकसित करने की प्रक्रिया है। विद्यालय इस सांस्कृतिक विरासत को आने वाली सन्तति को प्रदान करके उसको बनाये रखते हैं। साथ ही वे आने वाली सन्तति को इस योग्य भी बनाते हैं कि वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार उस विरासत को अपना योगदान कर सकें। विद्यालयों के अभाव में इस जटिल एवं विस्तृत तथा विशाल विरासत को थोड़े-से जीवनकाल में सीखना सम्भव नहीं है |
(2) समुदाय की आवश्यकताओं व माँगों की पूर्ति-प्रत्येक समुदाय की अलग-अलग आवश्यकताएँ एवं माँगें होती हैं। विद्यालय अपनी योजना तथा कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके समुदाय की माँगों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
प्रश्न (b)(v) “विद्यालय समाज का लघु रूप है।” स्पष्ट कीजिए।
अथवा
“विद्यालय समाज का प्रतिनिधि है।” व्याख्या कीजिए।
अथवा
“विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है।” इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं?
उत्तर-
विद्यालय का स्थान समाज के बीच शरीर में हृदय की स्थिति के समान है अर्थात् समाज और विद्यालय एक-दूसरे के पूरक हैं। इसके पारस्परिक सम्बन्धों के कारण ही विद्यालय को समाज का आदर्श स्वरूप कहा गया है। इस समबन्ध में क्लाइड एम. कैम्पवेल का मत है कि-
(i) विधान के पाठ्यक्रम का निर्धारण समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है।
(ii) विद्यालय अपने कार्यों को पूरा करने के लिए समाज के समस्त साधनों का उपयोग करता है और समाज इसमें सहयोग प्रदान करता है। विद्यालय अच्छे हैं या बुरे इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बालक का निश्चित दिशा में विकास करते हुए उसका समाजीकरण किया है या नहीं ?
प्रश्न (b) (vi) समाज में विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्त्व की व्याख्या कीजिए।
उत्तर-
समाज में विद्यालय के स्थान, महत्त्व और आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए एस. बालकृष्ण जोशी (S. Balkrishan Joshi ) ने लिखा है – “किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन् विद्यालयों में होता है।” विद्यालय को यह महत्त्वपूर्ण स्थान कुछ कारणों से दिया जाता है। हम उनका उल्लेख नीचे कर रहे हैं-
(1) जीवन की जटिलता –
आज का जीवन प्राचीन काल के जीवन के समान सरल और सुखमय नहीं है। उस समय मनुष्य के पास अपनी सब आवश्यकताओं के स्वयं पूर्ण करने और अपने बच्चों की शिक्षा की स्वयं देखभाल करने के लिए समय था। आज जनसंख्या की वृद्धि, आवश्यकताओं की अधिकता और वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य के कारण जीवन बहुत कठिन हो गया है। मनुष्य को अपने कार्यों से इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा की देखभाल कर सके। इसलिए उसने यह कार्य विद्यालय को सौंप दिया है
(2) विशाल सांस्कृतिक विरासत –
आज की सांस्कृतिक विरासत बहुत विशाल हो गई है। इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान, कुशलताओं और कार्य करने की विधियों का समावेश हो गया है। ऐसी विरासत की शिक्षा देने में व्यक्ति अपने को असमर्थ पाते हैं। अतः उन्होंने यह कार्य विद्यालय को सौंप दिया।
(3) समाज की निरन्तरता व विकास –
‘विद्यालय’ एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक होने के कारण विद्यालय सामुदायिक जीवन का वह स्वरूप है, जिसमें समाज की, निरन्तरता और विकास के लिए सभी प्रभावपूर्ण साधन केन्द्रित होते हैं। विद्यालय के इसी महत्त्व के कारण टी.पी.नन (T.P.Nunn) ने लिखा है- “विद्यालय को समस्त और संसार का नहीं, वरन् समस्त मानव-समाज का आदर्श लघु रूप होना चाहिए।”
प्रश्न (c) (i) विद्यालय एवं समुदाय में संबंध बताइए ।
उत्तर-
विद्यालय तथा समुदाय के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये दोनों अपनी-अपनी उन्नति एवं स्थायित्व के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना करता है जिनके द्वारा समाज के विचारों, मान्यताओं, आदर्शों, क्रिया-कलापों, मानदण्डों तथा परम्पराओं को आने वाली पीढ़ी को प्रदान किया जा सके। इस तथ्य की पुष्टि हम फ्रैंकलिन (Franklin) के शब्दों से कर सकते हैं- “समाज, शिक्षा-संस्थाओं को अपने सदस्यों में ऐसे ज्ञान, कौशलों, आदतों तथा आदर्शों का प्रसार करने एवं सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है जो उसके स्वयं के स्थायित्व एवं निरन्तर विकास के लिए परमावश्यक है।”
प्रश्न (c) (ii) समुदाय का विद्यालय पर क्या प्रभाव है? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
सामान्यतः लोग ‘समुदाय’ (Community) तथा ‘समाज’ (Society) का एक ही अर्थ लगाते हैं, परन्तु इनके अर्थ में विभिन्नता है। इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए आर.जी कॉलिंगवुड (R.G. Collingwood) ने लिखा है- “समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति, प्रौढ़ एवं बच्चे, सामाजिक तथा असामाजिक व्यक्ति सभी आते हैं जो एक निश्चित भू-भाग पर रहकर सामान्य जीवन में भाग लेते हैं, परन्तु वे सभी उसके संगठन या अभिप्राय के प्रति सचेत या जागरूक नहीं रहते हैं। समाज एक प्रकार का समुदाय या समुदाय का अंश है, जिसके सदस्य सामाजिक रूप से सचेत होकर उसके सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं और वे समान उद्देश्यों तथा मान्यताओं के फलस्वरूप एकता में बँधे रहते हैं।”
प्रश्न (c) (iii) विद्यालय की परिभाषा एवं इसकी विशेषताएँ बताइए ।
उत्तर-
विद्यालय की परिभाषा निम्नलिखित है-
विलर्ड वालर — “विद्यालय सामाजिक अन्तर्क्रिया का एक बन्द संगठन है।”
अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-दल की रिपोर्ट- “विद्यालय को प्रयोगशालाएँ होना चाहिए जिसमें आदर्श के रूप में कल्पित सामाजिक जीवन, पुनर्संगठन और अभिनीत होता है।”
टी.पी. नन– “किसी राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग होते हैं।”
विद्यालय के लक्षण या विशेषताएँ
आधुनिक समय में विद्यालय (प्राथमिक, माध्यमिक सभी) समाज के अंगस्वरूप माने जाते हैं, अतः उसमें समाज के लक्षण पाये जाते हैं। विद्यालय की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं-
1. विद्यालय की एक निश्चित जनता होती है। उसमें विद्यार्थी और अध्यापक ही होते हैं।
2. विद्यालय का एक निश्चित ढाँचा होता है। राजनीति की क्रियाओं का प्रभाव विद्यालय की क्रियाओं पर पड़ता है
3. विद्यालय सामाजिक तन्तुओं का समवाय होता है। विद्यालय में समाज के विभिन्न अंग एक समवाय के रूप में पाये जाते हैं ।
4. विद्यालय में हम-भाव व्याप्त होता है। विद्यालय किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी का होता है इसीलिए उसमें हम-भाव पाया जाता है न कि अहंभाव ।
5. विद्यालय की अपनी एक निश्चित संस्कृति होती है। विद्यालय के अपने ही आदर्श होते हैं जिसके अनुसार विद्यार्थी और अध्यापक व्यवहार करते हैं, ज्ञान-विज्ञान के साहित्य पढ़ाते- लिखते हैं, ज्ञान की परीक्षाएँ होती हैं, कक्षा, वर्ग आदि का संगठन होता है। इन लक्षणों के अलावा * और भी विशेषताएँ विद्यालय में पायी जाती हैं, जो आधुनिक समय में द्रष्टव्य हैं।
6. विद्यालय का एक स्वतन्त्र वातावरण होता है। विद्यालय बालक की स्वतन्त्रता को अधिक महत्त्व देता है जिसमें उसकी जन्मजात शक्तियाँ और योग्यताएँ पूर्णतया स्वतंत्र ढंग से विकसित होती हैं।
7. विद्यालय बाल केन्द्रित होता है। आधुनिक विद्यालय में शिक्षा की क्रिया बालक को केन्द्र बनाकर की जाती है जिससे कि बालक की शक्तियों का ख्याल रखा जाता है और अध्यापक उस पर पूरी दृष्टि डालता है। इस सम्बन्ध में रूसो ने कहा है, “बालक वह पुस्तक है जिसे अध्यापक को से अन्त तक पढ़ना चाहिए।”
प्रश्न (c) (iv) शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए।
अथवा
“परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है” स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार की निम्नलिखित भूमिका है-
(1) सीखने का प्रथम स्थान-घर या परिवार प्रथम स्थान है, जहाँ बालक बहुत-सी बातें सीखता है। रेमॉण्ट (Raymont) के शब्दों में, “सामान्य रूप से घर ही वह स्थान है, जहाँ बालक अपनी माँ से चलना, बोलना, मैं और तुम में अन्तर करना और अपने चारों ओर की वस्तुओं के सभी गुणों को सीखता है।”
(2) नैतिक व सामाजिक प्रशिक्षण-परिवार नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण का सबसे मुख्य स्थान है। पहले बच्चा भाषा सीखता है फिर वह भाषा के माध्यम से नैतिक और सामाजिक
नियमों को सीखता है। वह परिवार के ढंगों, व्यवहारों और परम्पराओं को अपनाता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे-वैसे वह अधिक उत्तम, नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है।
(3) दूसरों से अनुकूलन—बालक घर में ही दूसरों से अनुकूलन करने का पहला पाठ सीखता है। वह परिवार के विभिन्न सदस्यों को एक-दूसरे से मेल रखते हुए देखता है। इसका उस पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और वह भी वैसा ही करने का प्रयत्न करता है।
(4) सामाजिक व्यवहार का आधार -बालक परिवार के सामाजिक जीवन में जो अनुभव प्राप्त करता है, वही भविष्य में उसके सामाजिक व्यवहार का आधार होता है।
परिवार बालक की प्रथम पाठशाला
इस सम्बन्ध में पेस्तालोजी ने कहा है कि “घर बच्चों की प्रथम पाठशाला है। घर बालक की शिक्षा का सर्वोत्तम एवं प्रथम स्थान विद्यालय है।”
फ्रोबेल के अनुसार, “माताएँ आदर्श अध्यापिकाएँ हैं एवं घर द्वारा ही दी गयी अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली एवं स्वाभाविक है। ”
प्रश्न (c) (v) महिला सशक्तीकरण में मीडिया ने प्रभावी भूमिका नहीं निभाई है? कारण स्पष्ट करें।
उत्तर—
महिला सशक्तीकरण में मीडिया की भूमिका–
जो ब्रांट (Jo Bryant) के अनुसार, मीडिया, स्त्रियों की स्थिति एवं छवि के प्रस्तुतीकरण में सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही भूमिकायें अदा कर सकता है। मीडिया शिक्षा तथा समाजीकरण का एक सशक्त उपकरण है। एक ओर मीडिया ने जहाँ महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है वहीं दूसरी ओर इसने एक नकारात्मक स्त्री छवि की प्रस्तुति की है जिसका उदाहरण हम महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा। जिसमें पोर्नोग्राफी तथा स्त्री शरीर का अश्लील प्रदर्शन शामिल है, के रूप में देखते हैं। विस्तृत रूप से देखने पर स्पष्ट होता है कि स्त्रियों के प्रति मीडिया का व्यवहार संकीर्ण रहा है तथा उनके प्रस्तुतीकरण का तरीका ऐसा रहा है जिनसे उनकी स्टीरियोटाइप जेन्डर भूमिकाओं की पुष्टि होती रही जिसमें महिलाओं को पत्नी, माँ या पुरूष की सेवक के रूप में दिखाया जाता रहा है। विशेषकर विज्ञापनों में। उदाहरणार्थ – एक विज्ञापन में महिला दफ्तर में काम करती हुई भी घर में क्या खाना बनाएगी इसकी चिन्ता करती दिखाई जाती है।
महिलाओं पर विभिन्न मीडिया किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, उनको सही या गलत किस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका संक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार है-
1.फिल्मों/सिनेमा में महिलायें –
सभी सांस्कृतिक माध्यम चाहे वे थियेटर, आर्ट या आर्किटेक्चर हों, समाज के नैतिक तथा स्वीकृत ढाँचे की ही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से मीडिया जहाँ एक तरफ सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होता है वहीं दूसरी तरफ वह सामाजिक मूल्यों को चुनौती देने तथा नयी छवि गढ़ने का भी कार्य करता है। इस प्रकार यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिससे समाज तथा व्यक्ति दोनों ही प्रभावित होते हैं। दर्शकों पर सिनेमा तथा फिल्म का गहरा प्रभाव पड़ता है। मुम्बई फिल्म इन्डस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है तथा प्रत्येक वर्ष हजारों फिल्में बनती हैं स्त्रियों का फिल्मों में चित्रण स्टीरियोटाइप रहा है जिसमें उन्हें आदर्श पारम्परिक, पवित्र सहनशीलता तथा निस्वार्थ भाव की देवी जैसी छवि में चित्रित किया जाता रहा है। उसे दूसरों के सुख के लिये सब कुछ त्याग करने को तत्पर दिखाया जाता है जिसमें समाज भी उससे अपनी इच्छाओं व अधिकारों को छोड़ देने की अपेक्षा रखता है। फिल्मों में इस त्याग के बदले उसे कोई इनाम नहीं मिलता बल्कि उसे और ज्यादा त्यागमयी व दुखी दिखाया जाता है। फिल्मों में कुछ ही फिल्मों में उसे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की तरह दिखाया जाता है, अधिकतर तो उन्हें पत्नी, माँ व बहन के स्टीरियोटाइप के पारम्परिक ढाँचे में ही चित्रित किया जाता है।
2. महिलाओं का टेलिविजन में प्रस्तुतीकरण –
टेलिविजन पर दिखाये जाने वाले धारावाहिक या सीरियल यद्यपि स्त्री-आधारित होते हैं परन्तु वे भी सामाजिक रूढ़ियों पर ही चलते दिखाई देते हैं जिसमें अधिकतर महिलायें घरेलू पत्नियाँ होती हैं तथा वे संयुक्त परिवार के सास-बहू झगड़े सुलझाती नजर आती हैं। इसमें एकता कपूर निर्देशित पारिवारिक सीरियल उल्लेखनीय हैं। इन सभी सीरियल में त्यागी, सहनशील महिलायें दिखाई जाती हैं जो परिवार तथा सामाजिक मूल्यों की रक्षा की खातिर किसी भी हद तक जा सकती हैं। कुछ खलनायिकायें भी होती हैं जिनके जीवन का उद्देश्य अपने परिवार को बर्बाद करना होता है जिनके साथ परिवार द्वारा कभी बुरा व्यवहार किया जा चुका होता है।
3. विज्ञापन में महिलाओं का प्रस्तुतीकरण-फिल्मों तथा टेलिविजन के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले विज्ञापन ही होते हैं जहाँ महिलाओं को काफी प्रचार मिलता है। अधिकतर विज्ञापनों का केन्द्र महिलायें तथा बच्चे ही होते हैं जो मुख्य उपभोक्ता वर्ग होते हैं। सभी प्रकार के उत्पादों चाहे वे पुरुषों द्वारा इस्तेमाल लाई जाने वाली वस्तुयें हों या ट्रक टायर ऑटों के ही विज्ञापन क्यों न हों स्त्री माडल्स का भरपूर उपयोग किया जाता है। कई तरह के जेन्डर विभेदनकारी विज्ञापन जिनमें फेयरनेस क्रीम या किसी खास पुरुष इत्र से खिंची चली आ रही लड़कियाँ हों, सतत रूप से प्रदर्शित किये जाते हैं। ऐसे विज्ञापन होते हैं जिसमें चिंतित माँ होती है जिसमें बताया जाता है कि कैसे अपने बच्चों की देखभाल करें या फिर आकर्षक युवा लड़कियाँ जिन्हें पुरुषों को काबू में रखने के नुस्खे बताये जाते हैं। इसमें लड़कियों को ऐसे पुरुषों को रिझाने के प्रयास करते दिखाया जाता है जो खास सूटिंग्स पहनते हैं, जूते व टाई तथा खास प्रकार की गाड़ी या स्कूटर चलाते हैं तथा विशेष प्रकार की सिगरेट। इसके पीछे आकर्षक लड़कियाँ दिखाकर पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है चाहे बेचे जा रहे प्रोडक्ट का किसी महिला से सम्बन्ध हो अथवा नहीं। महिला की लैंगिक पहचान पर ही जोर दिया जाता है जिससे समाज में उसकी छवि, भूमिका तथा स्तर छिन्न-भिन्न होता है।
4. समाचार-पत्रों तथा मैगजीन में महिलाओं का प्रस्तुतीकरण- वर्तमान में महिलाओं से जुड़े मुद्दे तथा समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किये जाते हैं परन्तु शुरू में ऐसा नहीं था। किसी सनसनीखेज वारदात, मर्डर या दहेज हत्या को ही मुखपृष्ठ पर जगह मिल पाती थी। कुछ समाचार-पत्र ‘महिला पृष्ठ’ छापते हैं जिनमें सौन्दर्य सुझाव, व्यंजन तथा फैशन होता है कभी-कभी ही कुछ गम्भीर विषयवस्तु छपती है। महिलाओं की पत्रिकायें भी अधिकतर एलीटिस्ट होती हैं तथा सामान्यतः वे ऐसे मूल्यों को बढ़ावा देती हैं जिनमें महिलाओं को पुरुषों की सेवा करने के उपभोग की वस्तु के रूप में पेश किया जाता है जिसमें या तो वे किचन में खाना बनाती होती हैं या बाल्टी भर कपड़े धोते, घायलों को मरहम लगाते या पति व बच्चों को खाना खिलाते दिखती हैं। जिसमें महिलाओं की पति पर आश्रित छवि ही सामने आती है न कि ऐसी महिला की जो कि ज्ञानी या धनोपार्जन करने वाली है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन स्त्री विरोधी की तरह कार्य करते हैं व उन्हें केवल ‘सेक्स सिम्बल’ (sex symbol) की तरह प्रस्तुत करते हैं।
हालाँकि आजकल विज्ञापन में ‘कैरियर वुमन’ तथा ‘आत्मनिर्भर महिला’ को दिखाया जाता है तथा है पुरुषों को भी घरेलू जिम्मेदारियों में भागीदारी करते तथा बच्चों की जिम्मेदारी उठाते दिखाया जाता है।
प्रश्न (c) (vi) पाठ्यक्रम किस प्रकार से जेण्डर संवेदनशील बनाने में सहायक है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
उत्तर—
पाठ्यक्रम सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का मूलाधार है। बिना पाठ्यक्रम के हम किसी भी शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी उद्देश्यों एवं शैक्षिक सेवाओं के वितरण के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य, विषय- वस्तु, पाठ प्रदर्शन की अवधि एवं तरीकों तथा शिक्षाशास्त्रियों को कैसे विषय-वस्तु पढ़ानी है एवं कैसे शैक्षिक परिणामों का मूल्यांकन करना है आदि को निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रदान करता है। राष्ट्रीय
प्रश्न (c) (vi) पाठ्यक्रम किस प्रकार से जेण्डर संवेदनशील बनाने में सहायक है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
उत्तर —
पाठ्यक्रम सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का मूलाधार है। बिना पाठ्यक्रम के हम किसी भी शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी उद्देश्यों एवं शैक्षिक सेवाओं के वितरण के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य, विषय- वस्तु, पाठ प्रदर्शन की अवधि एवं तरीकों तथा शिक्षाशास्त्रियों को कैसे विषय-वस्तु पढ़ानी है एवं कैसे शैक्षिक परिणामों का मूल्यांकन करना है आदि को निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रदान करता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रचलित सामाजित एवं लैंगिक विभिन्नताओं को एवं परम्परागत लैंगिक रूढ़िवादों को अव्यक्त रूप से परिपुष्ट कर अधिगम विभिन्नताओं सम्बन्धी आवश्यकताओं की उपेक्षा कर और साथ ही साथ पूरे देश में लड़कियों एवं लड़कों पर आधारित अधिगम शैली को प्रोत्साहित करता है। वैकल्पिक रूप से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम महिलाओं एवं पुरुषों के मध्य समानता के बारे में सकारात्मक संदेश को विकसित करने का एक वाहक हो सकता है।
शिक्षाशास्त्रियों के लिए पाठ्यक्रम विसंयोजन एक प्रमुख मुद्दा है। विश्वभर में लड़के एवं लड़कियाँ अलग-अलग अध्ययन आधारित विषय चुन रहे हैं। जैसे कि लड़के इंजीनियरिंग, विज्ञान एवं कृषि आधारित विषयों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि लड़कियों का स्वास्थ्य एवं शिक्षा अध्ययन सम्बन्धी विषयों की तरफ ध्यान केन्द्रित है। ये पाठ्यक्रम आधारित लैंगिक विभिन्नताएँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये भावी रोजगार एवं आय आधारित सार्थक परिणाम व्यक्त करती हैं। कुछ मामलों में अनिवार्य पाठ्यक्रम ‘सेक्स’ के आधार पर भिन्न होता है, जैसेकि गृहविज्ञान तथा अर्थशास्त्र लड़कियों के लिए एवं कृषि तकनीकी लड़कों के लिए तथा इसी प्रकार साधारणतया लिंग आधारित संवेदनशीलता और प्रासंगिक विषय-सामग्री एवं अध्ययन की विधियाँ, अध्यापकों की अपेक्षाएँ आर्थिक विषय एवं सामाजिक मूल्य आदि सभी विद्यार्थियों के चुनाव को प्रभावित करते हैं।
पाठ्यक्रम दो मुख्य लैंगिकता सम्बन्धी आधारों पर संरचित किया जाता है—
1. विभिन्न विषय पुरुषत्व एवं नारीत्व से सम्बन्धित होते हैं
2. अध्यापक, लड़का या लड़की होने सम्बन्धी आधार पर अलग-अलग विषय एवं अलग- अलग व्यवहार तरीकों से अध्ययन करवाते हैं।
अधिकांश पाठ्यक्रम क्षेत्र, एक लिंग या दूसरे लिंग क्षेत्रों से सम्बन्धित होता है। उदाहरण के लिए बहुत-से पश्चिमी देशों से गणित एवं विज्ञान के साथ-साथ तकनीकी पुरुषत्व आधारित विषय के रूप में देखे जाते हैं। मानविकी एवं भाषाएँ (राष्ट्रीय भाषाएँ तथा आधुनिक विदेशी भाषाएँ) नारीत्व आधारित विषय स्वीकार किए जाते हैं। यह पाठ्यक्रम आधारित विशिष्टता उपलब्धि से सम्बन्धित नहीं होती। उदाहरण के लिए लड़कों एवं लड़कियों में गणित आधारित उपलब्धि लगभग समान है। जबकि गणित दृढ़ता से पुरुषत्व के रूप में चिह्नित किया जाता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी विशेषतः दृढ़तापूर्वक लैंगिकता आधारित है। इसका परिणाम यह है कि जहाँ पर विद्यार्थी व्यावसायिक विषयों की चुनाव करते हैं, वहाँ पर उनको एक या एक से अधिक एकल सेक्स आधारित कक्षाओं तक पहुँचने में शिक्षित किया जा रहा है।
यहाँ पर यह समझना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि यह लैंगिक अंकन अपरिवर्तनीय नहीं है जिसको समाज के द्वारा मध्यस्थता प्रदान की जाती है। इस प्रकार यह पाठ्यक्रम उच्च स्तर आधारित विषय पुरुषत्व से सम्बन्धित एवं निम्न स्तर आधारित विषय नारीत्व से सम्बन्धित प्रदर्शित करता है।
इस लैंगिक आधारित पाठ्यक्रम का यह परिणाम हुआ कि यदि युवा लोग अन्य लिंग नामांकित विषयों में सफलता प्राप्त कर लेते थे तो वे असहज महसूस करते थे। इसका कारण उनकी उपलब्धि बाधित हुई एवं इसके साथ ही वे विद्यार्थी इन विषयों के अतिरिक्त जल्द से जल्द जो विषय उनके लिए थे उनका चुनाव करने हेतु निर्देशित हुए। इससे सबसे बड़ी समस्या यह पैदा हुई कि लड़कियाँ एवं युवा महिलाएँ गणित, विज्ञान एवं तकनीकी आधारित विषयों की तरफ कम प्रवृत्त हुईं, परिणामस्वरूप उनके लिए उच्च स्तर एवं बाद में बेहतर कैरियर के रास्ते बन्द हो गए। इसी प्रकार से लड़के मानविकी एवं आधुनिक विदेशी भाषाओं के अतिरिक्त विषय चुनाव की तरफ प्रवृत्त हुए, जिससे उनके लिए इस विषय सम्बन्धी विकल्प समाप्त हो गए।
प्रश्न (c) (vii) पुरुषत्त्व से क्या तात्पर्य है?
उत्तर—
पुरुषत्त्व (मर्दानगी) पुरुषों और लड़कों से जुड़ी विशेषताओं, व्यवहारों और भूमिकाओं का एक समूह है। पुरुषत्त्व को सामाजिक रूप से निर्मित के रूप में समझा जा सकता है। इस बात के भी प्रमाण हैं कि पुरुष माने जाने वाले कुछ व्यवहार सांस्कृतिक कारकों और जैविक कारकों दोनों से प्रभावित होते हैं।
पुरुषत्त्व के प्रमुख गुण है—
(i) पुरुषों में पायी जाने वाली गंभीरता का आ जाना,
(ii) श्रेष्ठता का भाव आना,
(iii) पारिवारिक दायित्वों का बोध,
(iv) शारीरिक परिवर्तन,
(v) आवाज में गंभीरता का आना
(vi) पुरुषों में पाई जाने वाली रुचियों का विकास,
(vii) सांवेगिक कठोरता तथा दृढ़ता,
(viii) निर्णय शक्ति का विकास
(xi) पारिवारिक विषयों में हस्तक्षेप,
(x) विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण तथा उनकी सुरक्षात्मक जिम्मेदारी की भावना ।
प्रश्न (c) (viii) पाठ्यचर्या की विशेषताएं।
उत्तर—
(i) पाठ्यचर्या सैद्धान्तिक के साथ-साथ व्यावहारिक भी होना चाहिए जिससे छात्रों को व्यावहारिक बनाया जा सके और छात्र स्वक्रिया द्वारा सीख सके।
(ii) पाठ्यचर्या सम्पूर्ण एवं व्यापक होता है।
(iii) पाठ्यचर्या छात्रों में मूल्यों की स्थापना करने में सहायक होती है।
(iv) पाठ्यचर्या में विद्यालय में होने वाली समस्त योजनाबद्ध क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है।
(v) पाठ्यचर्या विषयवस्तु के ज्ञान के साथ-साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा अन्य प्रवृत्तियों के आयोजन से बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है।
(vi) पाठ्यक्रम को क्रिया व अनुभव के रूप में समझा जा सकता है।
(vii) पाठ्यचर्या से छात्र समय का उपयोग करना सीखते हैं।
(viii) पाठ्यक्रम कल्पनात्मक न होकर वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होता है।
प्रश्न (c) (ix) शिक्षा में समानता को कैसे प्राप्त किया जाय? तर्क दीजिए।
उत्तर—
शिक्षा में समानता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सुझाव होने चाहिए-
1. सभी लड़कियों के लिए शिक्षा की पहुँच – सरकार को शिक्षा पर अधिक खर्च करने का दबाव बनाया जाना चाहिए। मुफ्त तथा सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा देश के प्रत्येक क्षेत्र में लड़कियों के लिए स्कूलों की पहुँच को सुनिश्चित करना चाहिए।
2. लड़कियों की शिक्षा में गुणवत्ता तथा धारण क्षमता-सरकारी स्कूल वंचित वर्गों विशेषकर लड़कियों के लिए खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के केन्द्र बनते जा रहे हैं जिससे लड़कियों की ड्रॉपआउट दर भी बढ़ रही है। अतः सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं तथा शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारा जाना चाहिए।
3. धार्मिक पहचान वाले स्कूलों पर राष्ट्रस्तरीय विचार विमर्श – बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों के धार्मिक पहचान वाले स्कूलों के स्तर तथा संख्या के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि इन स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा मुश्किल से ही साम्प्रदायिकता या जेन्डर समानता पर कुछ विचार रखती है। धार्मिक स्कूलों की अनियन्त्रित स्थिति तथा जिस प्रकृति की वे शिक्षा प्रदान करते हैं उनका जेन्डर समानता में बड़े महत्त्वपूर्ण निहितार्थ हैं, क्योंकि इन स्कूलों का एक निश्चित लक्ष्य होता है जो लड़कियों की अधीनता को पुनर्बलित करते हैं तथा उनकी पहचान को पूर्णतः धार्मिक पहचान के रूप में ही सुनिश्चित करते हैं।
4. जेन्डर को रूपान्तरण तथा संगठनकारी सिद्धान्त को चिह्नित करने के रूप में स्थापित करना-जेन्डर केवल एक ‘जोड़े गए’ (add on) विषय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए; यह एक बीच में से होकर जाने वाला मुद्दा है जिसे पुनः सम्प्रत्यीकरण के सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया जाना चाहिए तथा समाहित करना चाहिए। जेन्डर को एक अतिरिक्त विषय के रूप में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इससे जेन्डर मुद्दे न केवल हाशिये पर जाएँगे बल्कि अधिगमकर्त्ता पर भारी पाठ्यक्रम का बोझ भी बढ़ेगा। इसके बजाय इसे शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर तथा पहलुओं में बताया जाना चाहिए। जेन्डर को रूपान्तरण के लिए एक महत्त्वपूर्ण चिह्न या निशान (critical marker) के रूप में पहचाना जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के लिए महत्त्वपूर्ण संगठनकारी सिद्धान्त के रूप में कार्य करना चाहिए।
5. जेन्डर : महिलाओं के लिए मुद्दा- यह जन सामान्य का मुद्दा है क्योंकि पितृसत्तात्मकता बनी रहती है। पुरुष व स्त्रियाँ दोनों इसे सहारा देते हैं। चूँकि पुरुष इस समस्या के एक अंग हैं— अतः पुरुषों को शिक्षा द्वारा इसके हल करने हेतु प्रशिक्षण देना चाहिए। लड़कों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह स्वयं का सामना कर सकें तथा यह समझने का प्रयास कर सकें कि वह कैसे पितृसत्तात्मकता से लाभ उठा रहा है, कैसे वे इससे सत्ता तथा फायदे प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से तन्त्र में बदलाव न लाकर वे जेन्डर असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हें यह समझाया जाना चाहिए कि अन्ततः जेन्डर असमानता से किसी को लाभ नहीं पहुँचता – इससे केवल अविश्वास असुरक्षा तथा असामंजस्यता ही फैलती है। शिक्षा द्वारा लड़कों को इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वे पुरुषत्व के अन्तर्गत हुए अपने समाजीकरण पर प्रश्न उठा सकें तथा अपने निजी जीवन सम्बन्धों, घरेलू जिन्दगी तथा लैंगिकता में एक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकें।
6. लड़कियों की समानता एवं सशक्तीकरण के लिए सूक्ष्म एवं सक्रिय उपागम-
लड़कियों की समानता तथा सशक्तीकरण लम्बे समय से शिक्षा नीतियों के मुख्य उद्देश्य रहे हैं, परन्तु इसे क्रियान्वयन में सूक्ष्म धार (critical edge) का अभाव रहा है। इसलिए इन उद्देश्यों को समझने के लिए एक सूक्ष्म परिवर्तन तथा अधिकतम विशिष्टता चाहिए, शिक्षा के प्रत्येक स्तर तथा क्षेत्रों में समानता का दृष्टिकोण ऐसा हो कि
(i) जो कि स्वतन्त्र समान ‘परिणाम’ का उद्देश्य रखे न कि औपचारिक, समान या एक जैसे व्यवहार का ।
(ii) जेन्डरीकृत पदानुक्रम के विशिष्ट हानियों को पहचाने तथा विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म तथा ग्रामीण शहरी विभाजन के द्वारा अधीनता को पहचाने परन्तु उसे स्वीकार न करें, बल्कि जेन्डर की हानियों को ‘दूर’ (dismantle) करने का प्रयास करें।
(iii) जो अधिगमकर्त्ता की मदद करे कि वह इन हानियों पर विजय प्राप्त करें तथा अपनी क्षमताओं को इतना विकसित करें जिससे सार्थक समानता प्राप्त की जा सके।
प्रश्न (c) (x) महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित किसी एक सरकारी योजना का वर्णन कीजिए।
उत्तर—
सुकन्या समृद्धि योजना- शादी व उच्च शिक्षा-प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने नवजात बच्चियों के लिए एक छोटी जमा योजना शुरू की है, ‘सुकन्या समृद्धि’ के नाम से शुरू इस योजना के अन्तर्गत बच्ची के माता-पिता अथवा उसके कानूनी अभिभावक डाकखाने में बच्ची के नाम से जमा खाता खोल सकते हैं
इस योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं-
(1) बच्ची के नाम से खाता उसके जन्म से 10 वर्ष की अवधि के बीच में खोला जा सकता है
(2) इस योजना के लागू होने के एक वर्ष पूर्व जिन बच्चियों की आयु 10 वर्ष की हो चुकी है, वे भी नई योजना के तहत खाता खोल सकेंगी।
(3) न्यूनतम जमा राशि ₹1,000 वार्षिक है। जमा राशि ₹100 के गुणक में होनी चाहिए यदि न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाती है, तो प्रतिवर्ष के हिसाब से ₹50 जुर्माना देय होगा।
(4) एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा किए जा सकते हैं।
(5) खाता खुलने की तारीख से 14 वर्ष की अवधि तक राशि जमा करनी है।
(6) माता-पिता व कानूनी अभिभावक खाते को संचालित कर सकते हैं।
(7) 10 वर्ष की होने के बाद बच्ची खुद भी खाते का संचालन कर सकती है, जबकि धन अभिभावक जमा करेंगे।
(8) जमा राशि खाता के खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि में मैच्योर (पूर्ण) होगी। हालाँकि कुल जमा राशि का आधा (वित्त वर्ष के अंत में) लड़की की शादी व उच्च शिक्षा के लिए निकाला जा सकता है। लेकिन यह तभी सम्भव है जब लड़की की उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो।
(9) यदि लड़की की शादी जमा-अवधि पूर्ण होने के पहले ही हो जाती है, तो खाता बंद कर दिया जाएगा। एक लड़की एक ही खाता खोल सकती है और माता-पिता इस तरह के खाते अपनी अधिकतम दो बच्चियों के लिए ही खोल सकते हैं।
प्रश्न (c) (xi) चुनौतीपूर्ण लिंग असमानता से आशय ।
अथवा
लैंगिक असमानता के कारणों को स्पष्ट करें।
अथवा
लैंगिक असमानता के क्या कारण हैं?
उत्तर-
चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता से क्या तात्पर्य है, इसके पूर्व चुनौतीपूर्ण लिंग तथा असमानता, इन शब्दों का पृथक्-पृथक् अर्थ एवं समन्वित अर्थ के द्वारा स्पष्टीकरण किया जा रहा है।
चुनौतीपूर्ण हेतु अंग्रेजी में ‘Challenging’ शब्द प्रयुक्त किया जाता है। चुनौती शब्द का प्रयोग शिक्षा, अध्ययन, कार्यक्षेत्र, व्यापार, समाज इत्यादि क्षेत्रों के लिए किया जाता है। यह शब्द यह दर्शाता हैं कि जिस क्षेत्र विशेष के साथ यह प्रयुक्त किया जा रहा है, उसका मार्ग सीधा-सपाट न होकर तमाम बाधाओं और परेशानियों से परिपूर्ण है।
वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र की अपनी-अपनी चुनौतियाँ हैं, परन्तु यहाँ हम लिंग आधारित चुनौतियों का निरूपण कर रहे हैं। लिंग के आधार पर भेदभावों का इतिहास पुराना है और हमारे समाज में पुरुष प्रधानता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि लिंगीय असमानता खान-पान से लेकर शिक्षा आदि प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। चुनौतीपूर्ण लिंग से तात्पर्य स्त्रियों से है, क्योंकि अभी तक पुरुष-प्रधान समाज में ये हाशिये पर रही हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् तमाम संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों के पश्चात् भी इनकी चुनौतियाँ कम नहीं हुई हैं।
लिंग से तात्पर्य बालक या बालिका अथवा स्त्री या पुरुष होने का निर्दिष्टीकरण है। लिंग के आधार पर वैयाकरणों द्वारा भी समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थलों को तीन लिंगों— स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग में विभक्त किया गया है। स्त्रीलिंग स्त्रीसूचक, पुल्लिंग पुरुषसूचक तथा इन दोनों के अतिरिक्त का बोध नपुंसकलिंग के द्वारा होता है।
यहाँ पर असमानता से तात्पर्य ऐसी असमानता से है जो विशिष्टीकृत न होकर सामान्यीकृत है अर्थात् असमानता की एक सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया गया, जैसे- तीव्र बुद्धि तथा मन्द बुद्धि में असमानता, भाषा की विविधता की असमानता, शारीरिक बनावट, रंग-रूप की असमानता, सामाजिक स्तर की असमानता, आर्थिक स्तर की असमानता, निवास स्थान तथा भौगोलिक वातावरण की असमानता, सांवेगिक असमानता तथा लिंगीय असमानता इत्यादि ।
प्रश्न (d) (i) लिंगीय असमानतापूर्ण व्यवहार की पहचान के क्षेत्र।
उत्तर-
1. खान-पान- लिंगीय असमानता बालक तथा बालिकाओं के खान-पान में भी परिलक्षित होती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के खान-पान तथा पोषण और शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा की जाती है। प्राथमिकता पर बालकों को रखा जाता है। यह असमानता परिवार में परिवार के सदस्यों तथा माता-पिता द्वारा की जाती है।
2. रहन-सहन- लिंगीय असमानता बालक और बालिकाओं के रहन-सहन के स्तर में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। बालिकाओं हेतु समुचित वस्त्र, कक्षादि की व्यवस्था न की जाकर सारी व्यवस्था और सुख-सुविधाओं के केन्द्र में बालकों को ही रखा जाता है।
3. शिक्षा—- बालिकाओं की पिछड़ी स्थिति का एक प्रमुख कारण है उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होना। लड़की को परिवार वाले पराया धन समझते हैं और उसकी शिक्षा पर व्यय नहीं करना चाहते जिससे शैक्षिक दृष्टि से वे बालकों की अपेक्षा पिछड़ जाती हैं।
4. सामाजिक कार्यों में सहभागिता— बालिकाओं के साथ होने वाला असमानतापूर्ण व्यवहार सामाजिक कार्यों में सहभागिता के अवसरों पर देखा जा सकता है। बालकों को सामाजिक कार्यों में अधिक प्राथमिकता दी जाती है वहीं बालिकाओं को इन क्रियाकलापों से दूर रखा जाता है, क्योंकि स्त्रियों को घरेलू कार्यों के ही योग्य समझा जाता है।
5. निर्णय लेने विषयी बालिकाओं को बालकों की अपेक्षा निर्णय लेने की छूट परिवार तथा समाज में नहीं प्रदान की जाती है। बालिकायें पिता, पति तथा पुत्र के सान्निध्य में ही जीवन व्यतीत करती हैं और आजीवन इन्हीं पर आधारित रहती हैं। अतः निर्णय लेने विषयी विषयों पर भी लैंगिक असमानता दिखाई देती है।
6. जिम्मेदारियों के वितरण में बाह्य और महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ प्रदान
बालिकायें चाहे जितनी भी योग्य क्यों न हों, परन्तु उन्हें नहीं की जाती हैं, क्योंकि यह धारणा है कि पुरुष ही जिम्मेदारीपूर्ण विशेषतः घर से बाहर का अच्छी प्रकार निर्वहन कर सकते हैं। इस प्रकार जिम्मेदारियों के वितरण में भी हमें लिंगीय असमानता दिखती है।
प्रश्न (d) (ii) चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता के कारण।
अथवा
लैंगिक असमानता के कारणों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
1. गरीबी— भारतीय जनता अभी भी दो वक्त के भोजन का प्रबन्ध करने और सिर पर छत के आयोजन में अपनी पूरी उम्र व्यतीत कर देती है। गरीबी के कारण बालिकाओं को अभिशाप माना जाता है। कहावत है कि गरीबी में आटा गीला, ठीक इसी प्रकार गरीब घर में यदि बालिका का जन्म हो जाये तो उसके पालन-पोषण के साथ-साथ दहेज में दी जाने वाली मोटी रकम के विषय में सोचकर ही व्यक्ति चिन्तित हो जाता है। इस प्रकार चुनौतीपूर्ण लिंग के प्रति असमानता का एक कारण गरीबी है।
2. अशिक्षा- शिक्षा के प्रसार हेतु किये जाने वाले अथक् प्रयासों के पश्चात् भी अभी अशिक्षित लोगों की भरमार है जो वही पुराने ढर्रे पर चलते हैं कि लड़की पढ़-लिखकर क्या करेगी, उसका काम चूल्हा-चौका सँभालना है। इस प्रकार अशिक्षित परिवारों में बालिकाओं की शिक्षा पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, जिस कारण से स्त्रियाँ असमानतापूर्ण व्यवहार आजीवन सहने के लिए विवश हो जाती हैं।
3. सामाजिक कारण- लिंगीय असमानता के मूल में सामाजिक कारणों की भूमिका भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। लिंगीय असमानता के सामाजिक कारण हैं, जैसे- दहेज, बाल-विवाह, विधवा विवाह को समाज में अच्छी दृष्टि से न देखना इत्यादि। माता-पिता अपने सपने और जीवन-भर की जमा पूँजी बच्चों के पालन-पोषण में व्यय कर देते हैं, फिर भी दहेज के लोभी थोड़े-से पैसों के लिए लड़कियों को जला देते हैं। बाल-विवाह के कारण बालिकाओं को कलम-कॉपी की जगह पारिवारिक जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाती हैं और विधवा होने पर स्त्री को ताने सुनकर ही अत्यन्त दयनीय अवस्था में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इन सामाजिक कारणों से चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता बढ़ती ही जाती है।
4. आर्थिक कारण- स्त्रियों को पुरुषों की भाँति समाज के सम्पर्क में आने और समाजीकरण की छूट नहीं होती है, जिस कारण वे बाहर के कार्यों से सर्वथा अनभिज्ञ और स्वयं को इन कार्यों के लिए अयोग्य मानने के मनोविज्ञान से ग्रसित हो जाती हैं। यदि पुत्र होता है तो वह कहीं भी जाकर चार पैसे कमाकर अपने परिवार का पेट पाल सकता है, पारिवारिक व्यापार तथा उद्योग को सँभाल सकता है, परन्तु इन आर्थिक क्रियाकलापों के लिए बालिकाओं को सर्वथा अनुपयुक्त समझा जाता है। इस प्रकार आर्थिक कारणों से चुनौतीपूर्ण लिंग की चुनौती बनी ही रह जाती है।
5. धार्मिक कारण- हमारे धर्मग्रन्थों में लिखी बातों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने तथा देश, काल और परिस्थिति समझे बिना तब कही गयी बातों को जस का तस अपनाने की प्रवृत्ति से लिंगीय असमानता में वृद्धि हो रही है।
प्रश्न (d) (iii) चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्त्व ।
उत्तर-
1. सर्वांगीण विकास चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास बिना शिक्षा के सम्भव नहीं हो सकता है। अतः शिक्षा के द्वारा ही स्त्रियों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। स्त्रियों के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए उनकी शिक्षा की आवश्यकता अत्यधिक है। सर्वांगीण विकास के अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, आर्थिक इत्यादि विकास आते हैं और इनकी सुनिश्चितता शिक्षा के द्वारा ही की जा सकती है।
2. आत्मनिर्भरता— शिक्षा के बिना स्त्रियों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा औपचारिक रूप से रुचियों को दृष्टिगत रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास क्वा कार्य सम्पन्न किया जाता है। आत्मनिर्भरता की आवश्यकता स्त्रियों के आर्थिक स्वावलम्बन के लिए तो है ही, साथ ही साथ इसकी आवश्यकता परिवार तथा समाज की आत्मनिर्भरता के लिए भी अत्यधिक है।
3. सामाजिक विकास समाज की अभिन्न अंग स्त्रियाँ होती हैं। स्त्री-विहीन समाज की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। समाज तभी सभ्य बनेगा जब वहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था होगी। सामाजिक परिवर्तन में स्त्रियों की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है जिससे सामाजिक गतिशीलता आती है और कुप्रथाओं का अन्त होता है।
4. सांस्कृतिक विकास- सांस्कृतिक विकास हेतु चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्त्व अत्यधिक है। सांस्कृतिक शिक्षा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही रूप से प्रदान की जाती है, परन्तु औपचारिक शिक्षा सोद्देश्य होने के कारण अधिक प्रभावी होती है। सांस्कृतिक विकास का अभिन्न अंग स्त्रियाँ होती हैं। अतः सांस्कृतिक विकास, संरक्षण तथा हस्तान्तरण हेतु इनकी शिक्षा की आवश्यकता अत्यधिक है।
5. कुरीतियों पर विजय पाने हेतु समाज में अनेक कुरीतियाँ व्याप्त हैं और इन कुरीतियों के केन्द्र में प्रायः स्त्रियाँ ही होती हैं। स्त्रियों के द्वारा अज्ञानता के कारण अन्धविश्वासों और कुरीतियों का प्रसार किया गया है तथा स्त्रियों का शोषण होता है। जब ये चुनौतीपूर्ण लिंग शिक्षित होंगे तो सामाजिक कुरीतियों पर विजय प्राप्त होगी।
प्रश्न (d) (iv) चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में परिवार की भूमिका ।
उत्तर
बालक में अनुकरण की सहज प्रवृत्ति पायी जाती है जिसके कारण वह अपने से बड़ों का अनुकरण करता है। यदि पारिवारिक वातावरण में बालक-बालिकाओं के मध्य भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है तो बालक भी ऐसा ही करना सीखता है। परिवार में चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता हेतु कुछ कारक उत्तरदायी हैं
1. पारिवारिक पृष्ठभूमि–
परिवार में चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता हेतु उत्तरदायी तत्त्व पारिवारिक पृष्ठभूमि है। पिछड़ी तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले परिवारों में लिंगीय असमानता अधिक देखने को मिलती है।
2. अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव- चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता हेतु परिवार के सदस्यों तथा माता-पिता का अशिक्षित और जागरूक न होना प्रमुख उत्तरदायी कारक है।
3. रूढ़िवादिता – रूढ़िवादी परिवारों में लिंगीय असमानता अधिक पायी जाती है। इस प्रकार के परिवार स्त्री-शिक्षा के महत्त्व और नवीन प्रतिमानों को रूढ़िवादी विचारों के कारण नहीं अपनाते हैं जिससे उनकी असमानता में वृद्धि होती है।
4. पिछड़ापन एवं गरीबी — पिछड़ेपन एवं गरीबी के कारण परिवार चुनौतीपूर्ण लिंगों की समानता में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाते। गरीबी तथा पिछड़ेपन के कारण खान-पान रहन-सहन और शिक्षा पर प्रथम अधिकार लड़कों का समझा जाता है जिस कारण लड़कियाँ पीछे रह जाती हैं।
5. सन्तानों की अधिकता- लोगों की मानसिकता है कि सन्तान ईश्वर की देन है। अतः वे सन्तानोत्पत्ति करते जाते हैं और किसी भी प्रकार के परिवार नियोजन के साधनों को नहीं अपनाते हैं, परन्तु अधिक सन्तान हो जाने के कारण उनके वस्त्र और भोजन की सुविधा जुटाने की ही चुनौती रहती है। ऐसे में उनकी शिक्षा या समानता की बात करना भी बेमानी हो जाता है।
6. सामाजिक स्थिति— सामाजिक रूप से स्तरीकरण में निम्न पायदान पर स्थित जातियों की स्थिति चिन्तनीय है और इनमें भी स्त्रियों की स्थिति तो और भी दीनतापूर्ण है। इस कारण से चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है।
प्रश्न (d) (v) परिजनों के सहयोग से चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा हेतु किये जाने वाले प्रयास।
उत्तर—
1. परिवार को गर्भावस्था में कभी भी भ्रूण का लिंग जानने या गर्भवती पर पुत्र जन्म को लेकर दबाव नहीं बनाना चाहिए।
2. कुछ परिवार सिर्फ परम्परा और मान्यताओं का रोना रोते हुए पुत्र जन्म की आस रखते हैं, जिससे भी लड़कियाँ उपेक्षित और असमान व्यवहार की शिकार हो जाती हैं।
3. परिवार में लड़का हो या लड़की, दोनों को समान अधिकार तथा सभी प्रकार के उत्तरदायित्व प्रदान किये जाने चाहिए।
4. परिवार में लिंगीय अपमानसूचक शब्दावली तथा व्यवहार का प्रयोग नहीं होना चाहिए अन्यथा बच्चे भी अनुकरण करेंगे।
5. परिवार को चाहिए कि वह उपलब्ध संसाधनों में बिना किसी भेदभाव के लड़कियों और लड़कों के पोषण, खान-पान, रहन-सहन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय करे।
6. पारिवारिक कार्यक्रमों में बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर परिवार रूढ़िवादी लिंगीय धारणा को तोड़ने में सहायता प्रदान कर समाज के सामने आदर्श स्थापित कर सकते हैं।
7. परिवार को चाहिए कि वह बालिकाओं के विद्यालयीकरण तथा समाजीकरण को प्रोत्साहित करे। 8. परिवार को चाहिए कि वह सामाजिक कुरीतियों, जैसे—पर्दा प्रथा, बाल-विवाह, दहेज प्रथा, विधवाओं के पुनर्विवाह का निषेध, पैतृक सम्पत्ति पर स्त्री का अधिकार न होना, पितृ कर्मों में बालिकाओं के सम्मिलित होने का निषेध, मुखाग्नि देने का निषेध इत्यादि का बहिष्कार करे। इस प्रकार यदि प्रत्येक परिवार ‘हम बदलेंगे जग बदलेगा’ की नीति का पालन करे तो चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता में कमी आ सकती है।
9. प्रौढ़ शिक्षा में परिवार के लोगों को सहयोग प्रदान करना चाहिए और आगे बढ़कर इसे ग्रहण करना चाहिए जिससे वे जागरूक हो सकें।
10. परिवार को आपसी सहयोग के भाव का विकास करना चाहिए, इससे स्त्रियों की असमानता कम होगी।
प्रश्न (d) (vi) चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में परिवार की प्रभाविता हेतु सुझाव।
उत्तर—
1. परिवार के पास संसाधन भले ही न्यून हों, परन्तु अपने आन्तरिक विषयों में इस संस्था पर राज्य भी किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता है। अतः परिवार को लिंगीय ही नहीं, ऐसे विभेदक विषयों जिससे परिवार, समाज, राज्य तथा राष्ट्र कमजोर और विखण्डित होते हैं, उनका बहिष्कार करना चाहिए।
2. परिवार ही वह संस्था है जो प्रेम, सहानुभूति, त्याग, करुणा, परोपकार इत्यादि माननीय मूल्यों के साथ-साथ बालकों में विचार और व्यापकता भरता है। कोई भी बच्चा सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों से सीखता है, उनका अनुकरण करता है और आदर्श मानता है। ऐसे में परिवार को प्रशिक्षण अपने इस महनीय दायित्व का बोध होना चाहिए।
3. परिवार को चाहिए कि वह सामाजिक कुरीतियों का निर्भय होकर विरोध करे।
4. परिवार और पारिवारिक सदस्यों को घर ही नहीं, बाहर भी बालिकाओं और स्त्रियों के लिए आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए।
5. परिवार का कार्य केवल भरण-पोषण मात्र ही नहीं है, अपितु स्वस्थ तथा सकारात्मक विचारों के लिए परिवार को मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए।
6. परिवार में बालक-बालिकाएँ सभी को आत्म-प्रकाशन के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने चाहिए, इससे लिंगीय समानता आती है।
7. परिवार को सामाजिक क्रियाओं, मेलों, प्रदर्शनियों इत्यादि में बालिकाओं को प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
8. परिवार की बालिकाओं के स्वतन्त्र अस्तित्व और निर्णयन का सम्मान करना चाहिए।
9. परिवार को चाहिए किं वह बालिकाओं की विशिष्ट रुचियों के अनुरूप ही उनकी शिक्षा की व्यवस्था करे।
10. परिवार को चाहिए कि वे बालिकाओं की व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था करे।
प्रश्न (d) (vii) पाठ्य-पुस्तकों में ‘लिंगभेद’ पर टिप्पणी लिखें।
उत्तर- लिंगीय असमानता में पाठ्यक्रम की भूमिका इस प्रकार है—
(i) इसके अंतर्गत लिंगीय भेदभाव/असमानता दूर करने का उद्देश्य भी निहित होता है।
(ii) पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा बालक-बालिकाओं में अन्तःक्रिया होती है, सहयोग तथा आपसी समझ का विकास होता है जिससे लिंगीय समानता में सहयोग प्राप्त होता है।
(iii) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत लिंगीय समानता हेतु पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया जाता है।
(iv) पाठ्यक्रम के द्वारा लिंगीय समानता और उसकी सशक्त भूमिका प्रस्तुतीकरण सर्वांगीण विकास के अन्तर्गत किया जा रहा है।
(v) पाठ्यक्रम का निर्माण बिना किसी लिंगीय भेदभाव के किया जाता है।
(vi) पाठ्यक्रम के निर्माण में लिंगीय रुचियों तथा आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है जिससे लिंगीय शिक्षा और समानता में वृद्धि हुई है।
|
(vii) पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिंगीय समानता हेतु आपस में मिलकर रहने तथा अन्तःप्रक्रिया करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं।
(viii) पाठ्यक्रम निर्माण का आधार मनोवैज्ञानिक होता है जिसमें बालिकाओं के मनोवैज्ञानिक
का भी ध्यान रखा जाता है।
प्रश्न (d) (viii) राज्य तथा कानून की चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता हेतु शिक्षा में भूमिका ।
उत्तर—
1. राज्य के द्वारा चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क कर दिया गया है।
2. पृथक् विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना का कार्य ।
3. महिला शिक्षिकाओं तथा निरीक्षिकाओं की नियुक्ति ।
4. छात्रावासों की व्यवस्था द्वारा ।
5. छात्रवृत्तियाँ प्रदान कर।
6. चुनौतीपूर्ण लिंग के नामांकन दर में वृद्धि हेतु राज्य निरन्तर प्रयासरत हैं
7. राज्य द्वारा अपव्यय तथा अवरोधन में कमी लाने के लिए यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। 8. राज्य चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा हेतु जनसंचार के साधनों की मदद से जागरूकता फैला रहा है।
9. पाठ्यक्रम में इनकी रुचि तथा आवश्यकतानुरूप विषयों का समावेश ।
10. धारा 45 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
11. महाविद्यलयों में प्रवेश तथा नौकरी में आरक्षण प्रदान कर राज्य इनकी शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
12. राज्य स्त्री-शिक्षा की दिशा में कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को प्रोत्साहित करते हैं और मानकों में भी कुछ ढील देते हैं।
13. राज्य सरकारें चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता हेतु शिक्षा के लिए सस्ते ऋणों को उपलब्ध कराती हैं जिससे आर्थिक तंगी आड़े न आये।
14. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय, महिला समाख्या, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, मध्याह्न भोजन योजना, सर्वशिक्षा अभियान, साइकिल एवं लैपटॉप वितरण तथा एकमुश्त राशि इत्यादि योजनाओं के द्वारा राज्य सरकारें चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा की दिशा में कार्य कर रही हैं।
15. आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना ।
16. प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार ।
प्रश्न (d) (ix) राज्य और कानून की चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता में प्रभाविता हेतु सुझाव ।
उत्तर—
1. राज्य को चाहिए कि वह जनशिक्षा के प्रसार हेतु व्यापक कार्यक्रम तैयार करे जिसके अन्तर्गत उपयोगी पाठ्यक्रम, लचीला समय तथा व्यावहारिक और जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान कराया जाये जिससे चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा की दिशा में गति आयेगी।
2. कानून सर्वोपरि है, परन्तु व्यवहार में प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि कानून भी व्यक्ति विशेष के ‘आगे नतमस्तक हो जाता है। बड़ी-बड़ी पहुँच वाले इसका लाभ उठाकर स्त्रियों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर उनका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति भाषणों में या सैद्धान्तिक रूप में चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता और शिक्षा का पक्ष लेते हैं, परन्तु व्यवहार में कुछ और ही करते हैं, जिसका सन्देश आम जनता के मध्य नकारात्मक जाता है। अतः कानून और राज्य को चाहिए कि वह खिलवाड़ करने वालों की न सुने तथा उनके लिए कठोरतम दण्ड का प्रावधान भी करे।
3. राज्य को चाहिए कि जो कानून है उसका पालन सख्ती के साथ कराये। कानून का सख्ती के साथ पालन यदि कराया जायेगा तो चुनौतीपूर्ण की समानता और शिक्षा के लिए जो प्रावधान किये गये हैं, वे वास्तविकता के धरातल पर आ जायेंगे।
4. राज्य तथा कानून को भाई-भतीजावाद की बुराई से दूर रहना चाहिए। बड़े-बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्तियों को ही अपने चारों ओर नियुक्त कर देते हैं, जिसके कारण वे मनमाना उपयोग अपने पद का करते हैं। ऐसी मानसिकता के व्यक्ति जब तक राज्य और उच्च पदों पर आसीन रहेंगे तब तक चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता हेतु शिक्षा की सुनिश्चितता सन्देहास्पद रहेगी। अतः इस प्रवृत्ति की रोकथाम तत्काल की जानी चाहिए।
कानून के
5. भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने नेता को चयनित करती है, परन्तु अशिक्षा के कारण दागी नेताओं, जो बलात्कार, अपहरण तथा फिरौती जैसे गम्भीर अपराधों में संलग्न हैं, उन्हें भी चुन लिया जाता है और ऐसे नेता जब तक देश का नेतृत्व करेंगे तब तक चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता हेतु शिक्षा का स्वप्न पूर्ण नहीं हो सकेगा, अतः ऐसे नेताओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए।
प्रश्न (d) (x) सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका ।
उत्तर-
1. लिंग भारतीय समाज की संरचना का आधार तत्त्व है।
2. लिंग के आधार पर ही सामाजिक रचना में पुरुषों की प्रधानता रही है।
3. लिंग के आधार पर ही भारतीय समाज पुरुष-प्रधान तथा पितृसत्तात्मक रहा है।
4. लिंग के आधार पर ही समाज के सभी कार्यों, जैसे— सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आदि का सम्पादन किया जाता है।
5. लिंग के आधार पर ही समाज के दायित्वों तथा पारिवारिक कर्त्तव्यों का विभाजन किया गया है।
6. लिंग सामाजिक संरचना में कार्यों, उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों को प्रभावित करता है।
7. लिंग सामाजिक संरचना की गतिशीलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
8. लिंग के आधार पर ही आर्थिक उत्तरदायित्वों तथा संसाधनों का वितरण सामाजिक संगठन में किया जाता है।
9. लिंग के आधार पर ही सामाजिक संरचना में आधुनिकीकरण, उदारीकरण इत्यादि प्रवृत्तियाँ आती हैं।
प्रश्न (e) (i) समाजीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
अथवा
समाजीकरण क्या है?
उत्तर-
बालक जब जन्म लेता है तब यह पाशविक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। ज्यों-ज्यों वह बढ़ता है, उसमें समाज की आकांक्षाओं, मान्यताओं एवं आदर्शों के अनुसार परिवर्तन आने लगते हैं। प्रौढ़ व्यक्ति समाज के आदर्शों से ही प्रेरित होते हैं। हम भाषा का व्यवहार करते हैं। समाज में भाषा का बड़ा महत्त्व है। व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति हमारी कुछ अभिवृत्तियाँ होती हैं। बालक को इन सब सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखना है तभी वह अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकेगा। ड्रेवर महोदय के अनुसार, “समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के प्रति अपना अनुकूलन करता है और इस सामाजिक वातावरण का वह मान्य, सहयोगी एवं कुशल सदस्य बन जाता है।”
समाजीकरण सामाजिक अन्तःक्रिया से होता है। इसमें बालक एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। यह सामाजिक अन्तःक्रिया दो स्तरों पर होती है। प्रारम्भिक अन्तःक्रिया व्यक्तियों के मध्य होती है और गौण अन्तःक्रिया व्यक्ति के मध्य होती है।
सामाजिक अन्तःक्रिया कई रूपों में प्रकट होती है। प्रथमतः, प्रतिद्वन्द्विता का रूप है जिसमें अविभाज्य लक्षण को दो या दो से अधिक व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं। दूसरा रूप सहयोग का है। इसमें सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न होता है। व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए प्रतिद्वन्द्विता एवं सामूहिक उपलब्धि के लिए सहयोग अत्यावश्यक सामाजिक अन्तःक्रिया है। सामाजिक अन्तःक्रिया का तीसरा रूप संघर्ष है। संघर्ष में पारस्परिक विरोध होता है। समंजन चौथा रूप है। समंजन में पारस्परिक अनुकूलन निहित है। सामाजिक अन्तःक्रिया का परिणाम हम दूसरों की रुचियों के साथ तादात्म्य के रूप में देखते हैं। संकेत एवं अनुकरण भी प्रभावशाली अन्तः क्रियाएँ हैं। इन अन्तःक्रियाओं से बालक का समाजीकरण होता है।
प्रश्न (e) (ii) बालक का समाजीकरण करने वाले तत्त्व।
उत्तर—
बालक का समाजीकरण विद्यालय, परिवार, समुदाय सभी जगह होता रहता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया में कई तत्त्व कार्य करते हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख तत्त्वों पर संक्षेप में विचार करेंगे_
1. परिवार — परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। बालक परिवार में जन्म लेता है और यहीं पर उसका विकास प्रारम्भ होता है। वह माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची, दादा-दादी आदि के सम्पर्क में आता है। ये सभी सम्बन्धी बालक को परिवार के आदर्शों को प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार बालक पारिवारिक प्रथाओं को जान लेता है। समाजीकरण का यह प्रारम्भिक प्रयास होता है। बालक परिवार में रहकर सहयोग, त्याग आदि सामाजिक गुणों को सीखने का प्रयास करता है
युद्ध
2. उत्सव- भारत में अनेक प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक उत्सव मनाये जाते हैं। होली के दिनों में लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाते हैं। दशहरा के समय लोग राम-रावण के
को देखने के लिए हजारों की संख्या में एक स्थान पर एकत्र होते हैं। दीपावली के समय गणेश- लक्ष्मी का पूजन करके अपने घर को लोग प्रकाशित करते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा 2 अक्टूबर को सभाओं का आयोजन, चर्खा तथा तकली प्रतियोगिता तथा भजन-कीर्तन का आयोजन करके लोग खुशी मनाते हैं। बालक इन सब उत्सवों में भाग लेकर सहयोग, प्रतिद्वन्द्विता आदि गुण सीखता है। वह सामूहिक रूप से खुशी मनाना सीखता है |
3. विद्यालय — समाजीकरण करने में विद्यालय बहुत महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। विद्यालय इस प्रक्रिया का औपचारिक अभिकरण है। अतः विद्यालय इस स्थिति में होता है कि वह बालकों का सामाजिक संस्कृति से परिचय कराये और सामाजिक प्रथाओं का मूल्यांकन करके नये समाज की रचना की प्रेरणा दे। विद्यालय भी एक प्रकार का समाज ही है। यहाँ पर छात्रों के बीच में, छात्रों एवं अध्यापकों के बीच में, अध्यापकों के ही बीच में, छात्रों एवं प्रधानाचार्य के मध्य तथा शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य के मध्य सामाजिक अन्तःक्रिया होती रहती है
4. खेल – खेल – कूद भी बालक का समाजीकरण करते हैं। खेल में सामाजिक अन्तःक्रिया का स्वाभाविक प्रदर्शन होता है। स्वस्थ संघर्ष एवं स्वस्थ प्रतियोगिता का यहाँ दर्शन होता है। हार-जीत के आधार पर मनोविकार न उत्पन्न हो, यह भावना खेल ही प्रदान करता है। सहयोग की भावना का भी स्वाभाविक विकास होता है। खेल में भाग लेने वालों में जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होता। खिलाड़ियों में अन्य भेदभाव भी नहीं होते।
प्रश्न (e) (iii) समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका ।
अथवा
समाजीकरण में विद्यालय का क्या महत्त्व है?
उत्तर-
1. अध्यापकों में आपस में आदर्शों पर मतभेद न होना चाहिए। इसमें छात्रों के मन में संस्कृति के प्रति सन्देह उत्पन्न नहीं होगा।
2. कभी-कभी छात्रों के माता-पिता के आदर्श अध्यापकों के आदर्शों से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। इस प्रकार की स्थिति का विश्लेषण करके अध्यापकों को अपने एवं छात्रों के माता-पिता के आदर्शों में समन्वय स्थापित करना चाहिए।
3. विद्यालय में मानवीय सम्बन्ध उचित हों। छात्रों का शिक्षकों से एवं शिक्षकों का प्रधानाचार्य से स्वस्थ सम्बन्ध होना चाहिए।
4. अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना के साथ-साथ समालोचनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होना चाहिए।
5. छात्रों में सामाजिक मूल्यों के प्रति सृजनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए जिससे संस्कृति का विकास हो सके।
6. सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए।
7. विद्यालय में स्वस्थ परम्पराओं का विकास करना चाहिए जिससे सामाजिक परम्परा से प्रेरित होकर छात्र अनुशासित जीवन बितायें।
8. छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए।
9. अन्तरसामूहिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे एक समूह के छात्र अन्य समूहों की संस्कृति का आदर कर सकें।
10. विद्यालय को सामुदायिक केन्द्र के रूप में परिवर्तित करना चाहिए जिससे स्थानीय समुदाय की मान्यताओं का छात्र दर्शन कर सकें।
11. छात्रों में यह भावना भरना कि वे माता-पिता एवं परिवार के विरुद्ध न चलें। यदि कहीं पर उन्हें त्रुटि दिखाई पड़े तो उसमें संशोधन करके उसे स्वीकार करें।
12. जब अध्यापक के आदर्श से छात्र के माता-पिता के आदर्श मेल नहीं खाते तो कभी- केभी छात्र अपने अध्यापक के विरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का अवसर ही न आने देना चाहिए।
13. अध्यापक को सामाजिक आचरण का मानदण्ड स्थिर करना चाहिए। उसे भी उसी के अनुसार चलना चाहिए ताकि छात्र कक्षा में या कक्षा से बाहर अध्यापक के आचरण का अनुसरण कर सकें।
प्रश्न (e) (iv) लैंगिकता हेतु समाजीकरण में आवश्यक जनसंचार के साधन । अथवा जनसंचार माध्यमों का वर्गीकरण करें।
उत्तर—
1. समाचार पत्र-
समाचार पत्रों से देश-विदेश के प्रतिदिन के समाचार ज्ञात होते हैं। समाचार पत्रों से विदेश की आर्थिक, राजनैतिक तथा व्यावसायिक प्रगति का पता लगता है। इसमें कहानियाँ, लेख, साहित्यिक समीक्षायें, साक्षात्कार, खेल जगत् की घटनायें छपती हैं, जिनसे बालक को ज्ञान तथा जागरूकता की प्राप्ति होती है। शिक्षा से सम्बन्धित कई जानकारियों से बालक अवगत होता है।
2. चलचित्र —
बालकों को शिक्षाप्रद चलचित्र दिखाना चाहिए। आजकल विभिन्न ज्ञानवर्द्धक विषयों पर ‘डॉक्युमेण्ट्री फिल्म’ का निर्माण कर बालकों को दिखाया जाता है। चलचित्र का प्रभाव बालक पर शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक पड़ता है।
3. दूरदर्शन –
दूरदर्शन भारत में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने का कार्य अपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से कर रहा है। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के हेतु तरह-तरह के ज्ञानवर्द्धक मनोरंजनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। इस समय दूरदर्शन 23 चैनलों का संचालन कर रहा है। यह सैटेलाइट के माध्यम से DD Sports, DD India, DD Gyan Darshan तथा 12 अन्य क्षेत्रीय चैनलों को चला रहा है।
4. रेडियो-
रेडियो की पहुँच भारत के दूरदराज इलाकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक भी है रेडियो पर अनेक शिक्षाप्रद कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देश-विदेश के समाचार तथा छात्रों हेतु विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। यह कार्यक्रम अंग्रेजी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल तथा क्षेत्रीय भाषाओं से सम्बन्धित होते हैं। इस प्रकार रेडियो के द्वारा व्यापक रूप से शिक्षा तथा नई-नई जानकारियों को विभिन्न आयु वर्ग, लिंग तक मनोरंजनात्मक ढंग से किया जा रहा है।
5.पुस्तकालय तथा वाचनालय –
पुस्तकालय तो ज्ञान की राशि है। यहाँ पर मुद्रित रूप में ज्ञान का अनुपम भण्डार होता है। पुस्तकालय की विभिन्न पुस्तकों का ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। वाचनालयों में व्यक्ति परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं जो शैक्षिक पुनरुत्थान तथा विकास की दृष्टि से अत्यावश्यक है।
प्रश्न (e) (v) लैंगिकता हेतु समाजीकरण में जनसंचार के साधनों की भूमिका ।
उत्तर—
1. मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के साथ-साथ लैंगिक तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता प्रदान की जाती है।
2. बालिकाओं की शिक्षा तथा स्त्री सुरक्षा आदि विषयी प्रावधानों से अवगत कराते हैं।
3. समय-समय पर आँकड़ों के प्रदर्शन द्वारा लैंगिक भेदभावों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
4. जनसंचार के साधनों की कार्य-प्रणाली में महिलाओं की सहभागिता पुरुषों के समान ही है चाहे वह न्यूज प्रस्रोती हों, कार्यक्रम निर्देशक हों या कार्यक्रम संचालक ।
5. नाटक तथा डॉक्यूमेण्ट्री फिल्म, लघु फिल्मों के द्वारा लैंगिक भेदभावों को दर्शाया जाता है जिससे लोगों में इस प्रकार के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में सहायता मिलती है।
6. महिलाओं की सशक्त छवि का प्रस्तुतीकरण ।
7. जनसंचार के साधनों में महिलाओं की समस्याओं, उनकी रुचि इत्यादि के विषय में अलग से स्तम्भ होते हैं।
8. प्रिण्ट मीडिया द्वारा स्त्रियों पर किताब, कवितायें तथा लेखों के द्वारा लैंगिक भेदभावों पर संवेदना जाग्रत की जाती है।
9. जनसंचार के साधन अपने प्रयासों द्वारा समाज में हो रहे लैंगिक भेदभावों की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और यह भी बताते हैं कि यदि ऐसा ही होता रहा तो भविष्य कैसा होगा, इस प्रकार जनसंचार के साधनों का महत्त्व अत्यधिक है।
10. जनसंचार के माध्यमों द्वारा ही देश के किसी भी कोने में हो रहे शोषण, अपराध और लैंगिक भेदभाव की खबरें सभी तक पहुँच जाती हैं जिससे आरोपी का बच निकलना मुश्किल हो जाता है। तमाम ऐसे दुर्व्यवहार जिसमें आरोपी को पकड़ने और सजा दिलाने में जनसंचार के साधनों द्वारा आवाज उठायी गयी।
11. ये साधन प्रशासन तथा कानून पर दबाव भी बनाते हैं जिससे पीड़िता को समुचित न्याय मिलता है।
प्रश्न (e) (vi) समुदाय की परिभाषाएँ दीजिए।
अथवा
समुदाय को परिभाषित कीजिए।
उत्तर- समुदाय के अर्थ के और अधिक स्पष्टीकरण के लिए कुछ परिभाषायें निम्न प्रकार दृष्टव्य हैं
1. के. डेविस के अनुसार- “समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है, जिसके अन्तर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं।”
2. ऑगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार –
“किसी सीमित क्षेत्र के अन्तर्गत सामाजिक जीवन । के सम्पूर्ण संगठन को समुदाय समझा जा सकता है।”
3. जिन्सबर्ग के अनुसार “समुदाय सामाजिक प्राणियों का एक ऐसा समूह समझा जाता है जो सामान्य जीवन व्यतीत करता हो, जिसमें सब प्रकार के असीमित विभिन्न तथा जटिल सम्बन्ध होते हैं एवं जो उस सामान्य जीवन के परिणामस्वरूप होते हैं जो उसका निर्माण करते हैं।”
4. कुक के अनुसार- “एक भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत मानवीय सम्बन्धों का एक निश्चित रूप अर्थात् व्यक्ति, संस्कृति एवं भूमि का समन्वित रूप समुदाय है।”
5. मैकाइवर के अनुसार-
“जब कभी किसी लघु या वृहत् समूह के सदस्य इस प्रकार रहते हैं कि वे एक या दूसरे उद्देश्य से भाग न लेकर जीवन की समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं, तब हम ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं।”
प्रश्न (e) (vii) समुदाय का महत्त्व एवं कार्य बताइए।
उत्तर-
1. नैतिक एवं चारित्रिक विकास का कार्य एवं महत्त्व –
समुदाय अपने शुद्ध वातावरण, अनुशासन, नैतिक तथा चारित्रिक महत्त्व की प्रधानता के कारण अपने सदस्यों का भी इसी दिशा में नैतिक तथा चारित्रिक विकास का कार्य सम्पन्न करता है। समुदाय के इस कार्य का प्रभाव हम विद्यालयी उद्देश्यों पर भी देख सकते हैं जहाँ नैतिक तथा चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता है। इस प्रकार समुदाय का यह कार्य महत्त्वपूर्ण है।
2. व्यवहारों तथा गतिविधियों पर नियन्त्रण-
बालक जैसे-जैसे बड़ा और सक्रिय होता है वैसे-वैसे वह समुदाय का सक्रिय सदस्य बन जाता है। समुदाय बालक के व्यवहारों तथा गतिविधियों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो समुदाय उसे दण्डित भी करता है। समुदाय इस प्रकार व्यक्ति के व्यवहारों तथा गतिविधियों पर नियन्त्रण करने के साथ-साथ सामाजिक नियन्त्रण का कार्य सम्पन्न करता है। समुदाय की प्रभाविता के कारण अशोभनीय व्यवहार तथा अराजक गतिविधियाँ न करने के प्रति भय बना रहता है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यवहारों और गतिविधियों के नियंत्रण का समुदाय का कार्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इससे स्त्रियों की सुरक्षा, वृद्धों की सेवा तथा देश व समाज-विरोधी गतिविधियों को करने के प्रति भय व्याप्त रहता है। इस दृष्टि से समुदाय महत्त्वपूर्ण अभिकरण है।
3. आदतों तथा विचारधाराओं का निर्माण-
प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों को जीवन निर्वहन करने तथा उनकी विचारधाराओं के निर्माण हेतु नियम तथा आदर्शों को प्रस्तुत करता है जिससे व्यक्ति की आदतों तथा विचारधाराओं का निर्माण होता है। यदि समुदाय संकीर्ण विचारों युक्त है तो उसके सदस्यों के विचार तथा आदतें संकीर्णतायुक्त तथा अगतिशील होंगी। इस प्रकार आदतों और विचारधाराओं के निर्माण में समुदाय की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।
4. रीति-रिवाजों, मान्यताओं तथा संस्कृति का निर्माण-
प्रत्येक समुदाय की अपनी विशिष्ट मान्यतायें, रीति-रिवाज तथा संस्कृति होती है जिसका अनुकरण उसकी भावी पीढ़ी करती है। ग्रामीण तथा शहरी समुदायों के रीति-रिवाजों, मान्यताओं तथा संस्कृतियों में अन्तर होता है जिसके परिणामस्वरूप दोनों परिवेश में रहने वाले व्यक्तियों पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कुछ समुदायों में अपने से बड़ों और वृद्धों की सेवा तथा सम्मान की संस्कृति है तो प्रभावस्वरूप भावी पीढ़ियाँ भी वैसा ही करती हैं।
प्रश्न (e) (viii) भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं की समानता के अधिकार ।
उत्तर—
पुरुषों के समान महिलाओं को भारतीय संविधान द्वारा दिये गये प्रमुख अधिकार निम्न हैं-
(1) समानता का अधिकार से तात्पर्य है अवसरों की समानता, कानून के समक्ष समानता, नौकरियों के आधार पर रंग, जन्म स्थान, विश्वास एवं लिंग की भिन्नता के आधार पर भेदभाव न समझा जाय।
(2) स्वतन्त्रता का अधिकार के अन्तर्गत भाषण की स्वतन्त्रता, निवास की स्वतन्त्रता एवं व्यवसाय तथा आवागमन की स्वतन्त्रता है।
(3) शोषण के विरुद्ध स्वतन्त्रता अर्थात् ‘बेगार’ के कार्य नहीं कराये जा सकेंगे।
(4) धर्म की स्वतन्त्रता अर्थात् अपने विश्वास के अनुसार कोई भी धर्म अपनाया जा सकता है। (5) सम्पत्ति का अधिकार अर्थात् सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने, खरीदने एवं बेचने का अधिकार होगा।
(6) सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार-स्व की संस्कृति के अनुसार आचरण एवं संरक्षण के अलावा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार है।
(7) संवैधानिक उपचार का अधिकार से तात्पर्य है मौलिक अधिकारों के अनुपालन न होने पर विरोधस्वरूप न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार।
दुःख की बात यह है कि अनेकों भारतीय महिलाएँ प्रदत्त अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। उन्हें इनकी जानकारी दी जानी चाहिए।
प्रश्न (e) (ix) लिंग असमानता की चुनौतियों में विद्यालय की भूमिका।
उत्तर-
शिक्षा आयोग (1964-66) ने भी बालिकाओं की शिक्षा पर बल देते हुए कहा है कि हमारे मानवीय साधनों ने पूर्ण विकास, घरों के सुधार और शैशव के सर्वाधिक संस्कारग्राही वर्गों में बच्चों के चरित्र के निर्माण हेतु स्त्रियों की शिक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। महिला शिक्षा प्रवसन दर घटाने में भी सहायक हो सकती है। आधुनिक समय में स्त्रियों का कार्य घर एवं सन्तान पालन से कहीं आगे है। वह अब अपने निजी व्यवसाय अपना रही है और समान विकास के समस्त पहलुओं के दायित्वों में पुरुष का हाथ बँटा रही है। स्वतन्त्रता संघर्ष में नारियाँ भी पुरुषों के साथ लड़ी हैं, परन्तु स्वतन्त्रता मिलने के बाद किये गये प्रयासों के बावजूद शिक्षा प्रणाली महिलाओं की समानता के प्रति पर्याप्त योगदान नहीं कर सकी। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 64.6% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। ऐसे देश में जहाँ पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ अधिक निरक्षर हैं। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1993-94 की अवधि में कुल नामांकन के अनुपात में विद्यालयों में लड़कियों का नामांकन प्राथमिक स्तर पर 43%, मिडिल स्तर पर 39%, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 34% तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर 33% है। संशोधित कार्य योजना सन् 1992 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 100 बालिकाओं के कक्षा I में प्रवेश लेने पर कक्षा पाँच में उनकी संख्या घटकर 40, कक्षा VIII में 18, कक्षा IX में और कक्षा XII में केवल एक रह जाती है- शहरी क्षेत्रों के लिए संगत आँकड़े क्रमशः 82, 62, 32, 14 हैं। यदि तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश हेतु 10 एवं 12 वर्ष की न्यूनतम सामान्य शिक्षा अवधि निर्धारित हो तो ग्रामीण बालिकाएँ प्रवेश नहीं पा सकती हैं। व्यावसायिक उच्च और तकनीकी शैक्षणिक सुविधाओं का बड़ा भाग शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित है। इस सेक्टर में बालिकाओं की सहभागिता अत्यन्त कम है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग और कृषि आधारित पाठ्यक्रमों में भी महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता काफी कम है। ऐसे पाठ्यक्रमों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकार को बालिकाओं की व्यावसायिक शिक्षा निःशुल्क कर देनी चाहिए जिससे वे उच्च तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सकें। बालिकाओं को महँगी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके अभिभावक उनकी शिक्षा पर धन व्यय करना धन की बरबादी समझते हैं। अतः बालिकाओं का व्यावसायिक क्षेत्र में तभी नामांकन बढ़ सकता है जब उनके लिए यह शिक्षा निःशुल्क हो जाए।
प्रश्न (f) (i) लिंग असमानता की चुनौतियों में शिक्षक की भूमिका ।
उत्तर- लिंग असमानता की चुनौतियों में शिक्षक की भूमिका
लिंग असमानता की चुनौतियों में शिक्षक की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक समाज का एक अभिन्न अंग होते हैं लेकिन कभी-कभी शिक्षक लिंग असमानता को बढ़ावा देने का कार्य भी करने लगते हैं। उनमें लिंग के आधार पर समाज के अन्य तबकों की ही भाँति रूढ़िवादिता तथा पूर्वाग्रह उत्पन्न हो जाते हैं। इन पूर्वाग्रहों से अभिप्रेरित होकर शिक्षक लिंग असमानता को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने लगता है। शिक्षक को सदैव कक्षा में लिंग समानता का व्यवहार करना चाहिए। शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि शिक्षकों में संवेदनशीलता उत्पन्न की जा सके जिससे वे जेण्डर भेद के पूर्वाग्रह से बाहर निकलकर संविधानसम्मत व्यवहार अपना सकें। शिक्षक का अपने छात्र एवं छात्राओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। छात्र भी अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सलाह को विशेष महत्त्व देते हैं। अतः शिक्षकों को इस बात के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक है कि वह अपने व्यक्तित्व के द्वारा छात्रों को प्रभावित करें और उनसे अन्तःक्रिया बढ़ाएँ।
शिक्षक को भी लिंग पूर्वाग्रहों से बाहर निकलकर लिंग समानतापूर्ण व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। उसे प्रतिभा के आधार पर छात्रों का चुनाव करना चाहिए तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों की योग्यता एवं प्रतिभा को महत्त्व देना चाहिए। अधिकांशतः यह देखा गया है कि कुछ शिक्षक छात्रों को अधिक महत्त्व देते हैं और छात्राओं को कम। कभी-कभी इसके विपरीत स्थिति भी आ जाती है, शिक्षक छात्राओं को अधिक महत्त्व देते हैं और छात्रों को कम। इन सभी स्थितियों में शिक्षक का व्यवहार भेदभावपूर्ण हो जाता है तथा न्याय एवं समानता पर आधारित नहीं रहता है। शिक्षकों को हमेशा छात्र एवं छात्राओं की प्रतिभा तथा योग्यता को महत्त्व देना चाहिए न कि उनके लिंग को । शिक्षक की दृष्टि में सभी छात्र एकसमान होने चाहिए और उन्हें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक को सदैव गुरु की मर्यादा में रहना चाहिए और छात्रों से, चाहे वे किसी भी लिंग के हों, उनसे अपने बच्चों की भाँति व्यवहार करना चाहिए जिसमें पक्षपात की कतई गुंजाइश न हो।
प्रश्न (f) (ii) लिंग असमानता की चुनौतियों में पाठ्य-पुस्तकों की भूमिका बताइए।
उत्तर—
लिंग असमानता को बढ़ाने में पाठ्य-पुस्तकों की भी भूमिका होती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान परिषद् में यह सिफारिश की गई है कि महिलाओं से सम्बन्धित कोर पाठ्यक्रम के घटक तैयार कराए जाएँ और इसका दायित्व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् के महिला सेल को दिया जाए। कार्य योजना में यह भी उल्लेख है कि सेल को स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों में से लिंग सम्बन्धी भेदभाव के अंशों को हटाने के कार्य में तेजी लायी जाए। समिति का विचार है कि शिक्षा की पाठ्य-पुस्तकों में से लिंग सम्बन्धी भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा की पाठ्यवस्तु में लिंग सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य का अर्थ पाठ्य-पुस्तकों में से लिंग सम्बन्धी भेदभाव को हटाना मात्र नहीं है। समीक्षा समिति द्वारा कराये गये NCERT की पुस्तकों के अध्ययन से यह पता चलता है कि उनमें स्पष्ट लिंग सम्बन्धी पूर्वाग्रह है। इसमें महिला की अपेक्षा पुरुष पात्रों की प्रधानता है। इसमें महिला पात्रों को निष्क्रिय या उदासीन और घरेलू वातावरण में प्रदर्शित किया गया है जबकि पुरुषों को अधिकार/ शक्ति और प्रतिष्ठा की स्थिति में दिखाया गया है।
लिंग असमानता की चुनौतियों से लड़ने के लिए पाठ्यक्रम में महिला लिंग को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उनके स्वतन्त्रता संग्राम में किये गये योगदानों की चर्चा होनी चाहिए। उन्हें सम्माननीय स्थिति में प्रस्तुत करना चाहिए न कि निष्क्रिय अवस्था में। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से जिन महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हुए हैं उन्होंने अपने आपको प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित किया है तथा उन्होंने एक अच्छी राजनीतिज्ञ, ईमानदार अफसर एवं कर्मठ कर्मचारी के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पहचान बनायी है। यह सत्य है कि पुरुष लिंग को एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में घर तथा समाज सदैव तत्पर रहता है और उन्हें आगे बढ़ने के भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। महिला को सदैव पुरुष से कमतर घर एवं समाज में समझा जाता है और उसके जीवन से सम्बन्धित निर्णय भी परिवार के लोग ही करते हैं, उसे सदैव एक आर्थिक बोझ ही माना जाता है और उसको कभी भी आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास नहीं किया जाता है, उसे आगे बढ़ने के भी बहुत कम अवसर प्राप्त होते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ तथा परिवार के सदस्यों की सेवा सुश्रूषा की जिम्मेदारी डालकर आर्थिक क्षेत्र में उसके बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया जाता है। पाठ्य-पुस्तकों को महिला लिंग की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करनी चाहिए।
प्रश्न (f) (iii) पाठ्यक्रम के विचार एवं महिला लिंग के शैक्षिक अवसर।
उत्तर-
पाठ्यक्रम में यह स्पष्ट किया गया है कि सर्वविदित है कि विविध क्षेत्रों में महिलाओं को दोयम दर्जे की स्थिति प्राप्त है, परन्तु सरकार शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराने के लिए स्वतन्त्रता के बाद से ही कटिबद्ध है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत में वर्ष 2001 में 102 करोड़ 70 लाख 15 हजार 257 व्यक्ति थे, उनमें से 49.57 करोड़ स्त्रियाँ ही थीं। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर 54.1% है जबकि पुरुषों में साक्षरता दर 75.9% है। मुस्लिम एवं घुमन्तू समुदायों की साक्षरता दर बहुत कम है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्त्रियों में साक्षरता दर बहुत कम है। 1996 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित National Policy on Education 1986 : Programme of Action में यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा व्यवस्था स्त्रियों की समानता की दिशा में बहुत योगदान नहीं कर पायी है। अतः सरकार ने इस दिशा में निम्नलिखित कार्य करने की नीति बनायी है-
1. लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा की योजना बनायी जाए।
2. स्त्रियों के लिए (आयु वर्ग 15-35 जिनकी संख्या 1995 तक 6.8 करोड़ थी) उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए।
3. लड़कियों/स्त्रियों को व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा दिलायी जाए।
4. स्त्रियों की शैक्षिक समानता के लिए विविध प्रकार की क्रियाएँ की जाएँ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय स्त्रियों की दशा में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को हस्तक्षेप करना होगा। यह निश्चित किया गया था कि-
1. शिक्षा को हस्तक्षेप करने की भूमिका निभानी होगी।
2. पाठ्यक्रमों और पाठ्य-पुस्तकों की पुनः रचना करनी होगी जिससे नये मूल्यों का विकास हो सके ।
3. व्यावसायिक, तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा में महिलाओं के प्रवेश का विस्तार किया जाएगा।
4. स्त्रियों को शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त हो सके, इसके लिए गतिशील प्रबन्ध ढाँचा सृजित करना होगा।
प्रश्न (f) (iv) लिंग असमानता की चुनौती एवं परिवार की भूमिका ।
उत्तर—
लिंग असमानता सर्वप्रथम परिवार से ही प्रारम्भ होती है। माता-पिता की दृष्टि से सभी बच्चे बराबर होते हैं परन्तु सर्वप्रथम परिवार में बेटी की कामना न करके बेटे की कामना की जाती है। यहीं से लिंग असमानता परिवारों में प्रारम्भ हो जाती है। यदि पुत्र कामना के बाद भी पुत्री का जन्म होता है तो परिवार में न कोई धूमधाम से समारोह किया जाता है और न ही नये (कन्या) शिशु का स्वागत किया जाता है। परिवार से लेकर रिश्तेदारों तथा समाज सभी की इस सन्दर्भ में प्रतिक्रिया ठण्डी हो जाती है जैसे बहुत बड़ी विपत्ति उनके ऊपर आ गयी हो। इसके पश्चात् पोषण की दृष्टि से भी उनमें असमानता रखी जाती है। शैशवावस्था से ही उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाता है और न ही उनके स्वास्थ्य को खराब न होने देने के लिए टीकाकरण आदि की प्रवृत्ति ठीक प्रकार से निभायी जाती है। माता की दृष्टि से यद्यपि उसके सभी बच्चे बराबर होते हैं परन्तु फिर भी वह अपने बेटे के पोषण पर बेटी की अपेक्षा अधिक ध्यान देती है और यही व्यवहार परिवार के अन्य सदस्य करते हैं। बीमार हो जाने पर पुरुष लिंग के शिशु को तत्काल चिकित्सक को दिखाया जाता है परन्तु महिला लिंग के शिशु पर ध्यान तक नहीं दिया जाता है जब तक उसकी स्थिति अधिक बिगड़ने न लगे। शिक्षा की दृष्टि से भी असमानता व्यक्त की जाती है। निःशुल्क शिक्षा बालिकाओं को अधिक दिलायी जाती है तथा उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पुत्रों को दिलायी जाती है। बालिकाओं को घरेलू शिक्षा सिलाई, कढ़ाई तथा खाना बनाने की शिक्षा घर पर ही दी जाती है। यदि विद्यालय निकट क्षेत्र में नहीं होते हैं तो बालकों को दूरदराज शहरों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है और उन्हें छात्रावास में रखा जाता है और बालिकाओं को घर पर बिठा लिया जाता है और घर के दायित्वों को सँभालने में उनकी सहायता ली जाती है तथा उनके विवाह सम्बन्ध तय कर दिये जाते हैं। यद्यपि सरकार ने बालिकाओं एवं बालकों के विवाह सम्बन्ध की आयु निर्धारित कर रखी है। अठारह वर्ष से पूर्व बालिकाओं का विवाह और इक्कीस वर्ष से पूर्व बालकों का विवाह वैध नहीं माना जाता है परन्तु आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दस वर्ष से कम की बालिकाओं के वैवाहिक सम्बन्ध भी धड़ल्ले से किये जा रहे हैं। वैवाहिक सम्बन्ध हो जाने के बाद बालिकाओं के विकास, शिक्षा, व्यवसाय आदि की सम्भावनाएँ स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं क्योंकि वैवाहिक सम्बन्ध होने के पश्चात् वे शीघ्र माताएँ बन जाती हैं। कच्ची उम्र में विवाह होने के कारण उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगता है और घर तथा बच्चों को जिम्मेदारी बढ़ती जाती है जिसमें बालिका उलझ कर रह जाती है। वह पूर्ण रूप से अपने श्रति पर निर्भर हो जाती है और यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो अपने पिता अथवा भाइयों के पास पहँचा दी जाती है जिससे पति की सम्पत्ति में उसको हिस्सा न देना पड़े और वह पिता तथा भाइयों पर निर्भर होकर रह जाती है।
प्रश्न (f) (v) महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा ।
अथवा
महिला सशक्तिकरण की अवधारणा स्पष्ट करें।
उत्तर-
“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता । ” ।
कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। धार्मिक तथा सामाजिक कुप्रथाओं व रीति-रिवाजों के कारण पुरुष तथा महिलाओं में भेद किया जाता था। संसार को आगे बढ़ाने वाली स्त्री पर अनेक अत्याचार किए जाते थे। महिलाओं को पुरुष के समान शिक्षा प्राप्त नहीं करने दी जाती थी। महिलाओं को घर की चहारदीवारी में घर- गृहस्थी सँभालने, सन्तान के लालन-पालन तथा परिवार के सदस्यों की सेवा करने तक सीमित किया जाने लगा था। पुरुष को स्वामी माना जाता था। महिलाओं को किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं थी। पर्दा प्रथा प्रचलित थी। महिलाओं को अर्थोपार्जन से दूर रखा जाता था। परन्तु 21वीं सदी के भारत में ऐसा नहीं है। आज शिक्षा के प्रभाव के कारण महिलाओं के साथ इस प्रकार का अन्याय सहन नहीं किया जाता है। अब स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है।
आधुनिक वैश्विक समाज में पुरुष तथा महिला को एक गाड़ी के दाएँ व बाएँ वाले दो पहियों के समान माना जाता है। इनमें से एक भी पहिए के खराब होने से इस सांसारिक गाड़ी को सर्वोत्तम तरीके से आगे बढ़ाना कदापि सम्भव नहीं हो सकता है। आज महिलाएँ पुरुषों के कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही हैं। वर्तमान समय में हर क्षेत्र में महिलाएँ कार्य कर रही हैं। आज ये अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में जहाँ लिंगभेद के आधार पर पुरुषों व महिलाओं में विभेद करने को प्रतिबन्धित किया गया है वहीं महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयत्न करने की बात कही गई है। आज सम्पूर्ण विश्व की महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति अलख जगा दी है। वे अपनी बौद्धिक योग्यता, तकनीकी, सामर्थ्य एवं तार्किक विवेक से पुरुषों को चमत्कृत कर रही हैं। पुत्री, पत्नी, माता के रूप में अपने पारिवारिक दायित्वों के सम्यक् निर्वहन के साथ-साथ वे मानव कल्याण की दिशा में अपना योगदान करने के लिए कृत संकल्पित प्रतीत होती हैं। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था में तो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। महिलाओं के सामर्थ्यवान न होने पर समाज के विकास का कार्य विकृत हो सकता है, जबकि सामर्थ्यवान होने पर समाज दुगुनी प्रगति कर सकता है। आज महिलाएँ सशक्त हो गई हैं।
प्रश्न (f) (vi) महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका ।
अथवा
महिला सशक्तिकरण के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
उत्तर-
महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता व इसके मार्ग की बाधाओं को दूर करने में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। बालक-बालिकाओं के प्रारम्भिक विकास में माताओं के अतुलनीय योगदान को देखते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षित समाज विकासोन्मुख राष्ट्र के निर्माण हेतु महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है । उपप्रधानमन्त्री जगजीवन राम ने एक अखिल भारतीय गोष्ठी में कहा है— “एक कन्या को पढ़ा देने से आगे आने वाली पीढ़ी सुशिक्षित होगी क्योंकि बालक की प्रारम्भिक पाठशाला घर है। माता ही उसकी प्रथम शिक्षिका है।”
स्त्री समाज का आधार है, उसे शिक्षित करना सम्पूर्ण समाज को शिक्षित करना है। नेपोलियन ने कहा था— “मुझे सुशिक्षित माताएँ दो, मैं एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूँगा।”
अंग्रेजी में एक कहावत है स्त्री के विषय में— “जो हाथ पालने को झुलाता है, वह संसार का शासन भी करता है।”
शिक्षित महिलाएँ ही अपने अधिकारों को जान व समझ कर उनका लाभ उठा सकती हैं एवं अपने विविध कर्त्तव्यों का सम्यक तरीके से निर्वहन कर सकती हैं। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएँ प्रायः अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहती हैं। यदि उन्हें इसकी जानकारी मिल भी जाती है. तो सरकारी मशीनरी के असहयोग तथा समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण उनका व्यावहारिक रूप से उपभोग नहीं कर पाती हैं। इस दृष्टि से महिला सशक्तीकरण के जन-आन्दोलन को यथार्थ रूप देने के कार्य में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु महिला साक्षरता में वृद्धि, लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, लड़कियों के शाला त्याग पर अंकुश तथा कन्या शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करने की आवश्यकता है। इनके माध्यम से महिलाओं के विकास में वृद्धि होगी तथा वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपने पर हो रहे अत्याचारों का विरोध कर सकेंगी।
प्रश्न (g) (i) महिला सशक्तिकरण के आयाम।
अथवा
महिला सशक्तिकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए।
उत्तर—
महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं-
(1) पारिवारिक सशक्तिकरण—
पारिवारिक सशक्तिकरण से तात्पर्य है परिवार के अन्दर सभी महिला सदस्यों को उनके नैसर्गिक अधिकार, प्रतिष्ठापरक प्रस्थिति, आर्थिक स्वायत्तता तथा समतापरक निर्णयन प्रतिभागिता को न सिर्फ शुरू करना वरन् उसे निरन्तर जारी रखना व संरक्षित करना भी सुनिश्चित करना। इस हेतु परिवार में पोषण, स्नेह, शिक्षा, सुरक्षा, अधिकार आदि किसी भी दृष्टि से बालक व बालिकाओं के मध्य विभेद समाप्त करके बालक तथा बालिकाओं को समान मानना होगा। परिवार में महिलाओं को समान मानना होगा। परिवार में माता, बहन, पत्नी के रूप में महिलाओं को सम्मान देना होगा। तभी महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
(2) सामाजिक सशक्तिकरण महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में महिलाओं को समाज में व्याप्त पुरुषवादी मानसिकता से स्वतन्त्रता दिलाकर उन्हें सम्मानजनक व समतायुक्त स्थान देना होगा। सामाजिक प्रौद्योगिकी के द्वारा महिलाओं के प्रति परम्परागत अन्धविश्वास, शोषण अभिवृत्ति आर्थिक पर निर्भर रोजगार, यौन भेदभाव, नकारात्मक तथा अशिक्षा प्रवृत्ति आदि का निराकरण करना होगा। महिलाओं के प्रति स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण को विकसित करना होगा।
(3) आर्थिक सशक्तिकरण— महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं की वैयक्तिक आर्थिक स्थिति का उन्नयन करने, उन्हें धनार्जन के पर्याप्त अवसर देने तथा आर्थिक मुद्दों पर अपनी सलाह देने व निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
(4) शैक्षिक सशक्तिकरण- शैक्षिक सशक्तिकरण को महिला सशक्तिकरण के सभी आयामों का आधार कहा जा सकता है जिसके द्वारा महिलाओं को शिक्षित करके विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें क्रियाशील, विवेकशील तथा प्रभावशील बनाना सम्भव हो सकता है।
(5) राजनैतिक सशक्तिकरण— इसका अर्थ है कि न केवल राजनीति में महिलाओं के प्रतिभाग को पुरुषों के समकक्ष लाना है वरन् राजनैतिक शासन व्यवस्था के स्तर पर बनाए गए नीतियों व सरकारी अधिनियमों, परिनियमों व अध्यादेशों व निर्णयों आदि के माध्यम से महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार लाना है।
प्रश्न (g) (ii) महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण।
उत्तर-
आधुनिक भारत, जिसकी नींव ही संविधान निर्माताओं ने समानता, न्याय, भ्रातृत्व इत्यादि के आधार पर रखी, उसमें महिलाओं की शिक्षा, समानता तथा सशक्तिकरण के कार्य को गम्भीरतापूर्वक लिया गया। महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण हेतु स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। महिलाओं की शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष रूप से योजनायें चलायी जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण के कार्य हेतु महिलाओं की शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास, जैसे— महिला विद्यालयों की स्थापना, महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति, छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, नगद धनराशि, साइकिल, गणवेश, पुस्तक आदि का वितरण किया जा रहा है। महिलाओं को शिक्षा तथा सशक्तिकरण प्रदान करने हेतु उनकी रुचियों का ध्यान रखते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा प्रौढ़ शिक्षा विषयी प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप निश्चित ही बालिका शिक्षा में गति आयी है। जैसे-जैसे बालिकाएँ शिक्षा की सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही हैं वैसे-वैसे महिला सशक्तिकरण के कार्य में तीव्रता आती जा रही है। स्वतन्त्रता के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा गठित आयोगों, जैसे— राधाकृष्णन् आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों (1969, 1976, 1986), आचार्य राममूर्ति समिति, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचनाओं के द्वारा महिला शिक्षा के प्रसार हेतु पाठ्यक्रम, शिक्षिकाओं की नियुक्ति, मूलभूत ढाँचे में सुधार इत्यादि के सुझाव दिये गये हैं जिससे महिलाएँ स्वावलम्बी और सशक्त बन रही हैं।
इस प्रकार महिला शिक्षा का आज हम जो स्वरूप देख रहे हैं, वह कई वर्षों के परिश्रम का परिणाम है और इस कार्य के लिए अनेक लोगों ने आवाज उठायी है। आज महिला शिक्षा को बुद्धिजीवी वर्ग, पुरुषों की शिक्षा से भी अधिक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण मानता है। धीरे-धीरे महिला शिक्षा की स्वीकार्यता जनसामान्य में भी बढ़ी है। महिला शिक्षा से इस प्रकार तात्पर्य है महिलाओं की शिक्षा, परन्तु ‘शिक्षा’ शब्द का अर्थ आज अति व्यापक हो गया है। अतः महिलाओं की शिक्षा का सम्प्रत्यय भी व्यापक हो गया है।
प्रश्न (g) (iii) महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण के मध्य सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के मध्य व्याप्त सम्बन्ध निम्नवत् है-
1. महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के मध्य सम्बन्ध इसलिए भी है कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बल देती है।
2. महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण दोनों ही किसी एक क्षेत्र में महिलाओं के विकास को प्रमुखता न देकर सभी क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं।
3. महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं का प्रजातान्त्रिक प्रणाली में योगदान बढ़ता है।
4. अशिक्षित महिला का सशक्तिकरण मुश्किल होता है क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा सशक्तिकरण के लिए आन्तरिक गुणों को बाहर निकाला जाता है।
5. आज की महिला सशक्त कही जा सकती है जो शिक्षित है क्योंकि शिक्षा महिलाओं में कुशलता लाती है जिससे नये-नये अवसरों के मार्ग खुलते हैं।
6. महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के द्वारा ही महिलाएँ देश तथा विदेश में महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन हो रही हैं।
7. महिला शिक्षा के द्वारा ही महिलाएँ सशक्त होंगी क्योंकि वे अपने अधिकारों, अस्तित्व की रक्षा तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपनी भूमिका के महत्त्व से अवगत होंगी।
8. महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के मध्य इसलिए भी सम्बन्ध हैं क्योंकि शिक्षा के द्वारा महिलाओं में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है जिससे वे सशक्तिकरण की ओर अग्रसर होती हैं।
9. महिला शिक्षा के द्वारा स्त्रियाँ अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भली प्रकार करती हैं जिससे परिवार तथा समाज में वे सशक्त बनती हैं।
10. शिक्षा के द्वारा ही आज विविध क्षेत्रों में महिलाएँ अपनी कार्य-क्षमता, नेतृत्व शक्ति तथा प्रबन्धन गुण
के कारण सशक्त बन रही हैं।
प्रश्न (g) (iv) सहशिक्षा की परिभाषा दीजिए।
उत्तर-
सहशिक्षा के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं, जिन्हें निम्न परिभाषाओं के माध्यम से समझा जा सकता है-
ब्रिटेनिका विश्वकोश के अनुसार सहशिक्षा का अर्थ है- “लड़के तथा लड़कियों को एक ही समय, एक ही स्थान पर, एक ही अधिकारी द्वारा, एक ही शासन के अधीन, एक ही तरीके से, एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए।”
माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) के शब्दों में, “समता के आधार पर एक ही संस्था में लड़के एवं लड़कियों को शिक्षा देना सहशिक्षा कहलाता है।” इस प्रकार कहा जा सकता है कि सहशिक्षा संस्थाओं में लड़के एवं लड़कियाँ साथ-साथ पाठ्यचर्या को पूर्ण करते हैं।
माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) का विचार है- “ऐसा जान पड़ता है कि सहशिक्षा के सम्बन्ध में हमारे स्कूलों की शिक्षा प्रणाली उस समुदाय की सामाजिक पद्धति से आगे नहीं बढ़ सकती है जिसमें कि स्कूल स्थापित किये जाने चाहिए। हमारा विचार है कि जिन स्थानों पर सम्भव हो वहाँ लड़कियों के पृथक् स्कूल हों क्योंकि ये मिश्रित स्कूलों की अपेक्षा उनकी शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विशेषताओं के विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान करेंगे और सभी राज्यों को ऐसे स्कूल पर्याप्त संख्या में खोलने चाहिए। परन्तु ये उन लड़कियों के लिए खाले जाने चाहिए जिनके अभिभावकों को मिश्रित सकूलों की सुविधाओं से लाभ उठाने में आपत्ति हो ।” इसी प्रकार शिक्षा आयोग (1946-66) ने सहशिक्षा के सम्बन्ध में अपने सुझाव देते हुए कहा है कि “कॉलेज के स्तर पर स्थानीय ऐतिहासिक परम्पराएँ और सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि यह निर्धारित करती हैं कि वहाँ महिलाओं के लिए पृथक् कॉलेज हों या मिश्रित कॉलेज हों। शिक्षा के स्तर के लिए सहशिक्षा की समरूपी नीति आवश्यक नहीं है, परिस्थिति प्रत्येक राज्य में भिन्न है।…. अतएव इस स्तर पर सहशिक्षा सम्बन्धी नीति का निर्णय प्रत्येक राज्य की सरकार को करना होगा।” पूर्व स्नातक स्तर पर यदि स्थानीय माँग हो तो महिलाओं के लिए पृथक् कॉलेज स्थापित किये जा सकते हैं। शिक्षा आयोग के विचार में स्नातकोत्तर स्तर पर महिलाओं के लिए पृथक् शिक्षा संस्थाओं का कोई औचित्य नहीं है।
प्रश्न (h) (i) कामकाजी स्त्री की शिक्षा।
उत्तर
निरक्षरता से उत्पन्न होने वाली गरीबी, जो सदियों से चली आ रही है, ने कामकाज करने वाले बालक/बालिकाओं में बढ़ोतरी करने के अलावा धनार्जन की मजबूरी एवं लालच से कामकाज करने वाले कानूनी, गौर-कानूनी शोषण को भी प्रोत्साहित किया है। काम-काज करने वाले बालक- बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना शिक्षा के उद्देश्य की अपेक्षित शर्त है। वर्तमान समय में हमारे देश में लगभग 9 करोड़ बच्चे काम करने वाले हैं। शिक्षा के कार्यक्रम में अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा प्रणालियों में साधारण रूप से सुधरी हुई शिक्षा को काम करने वाले बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया गया है। इसके साथ ही फर्म के मालिकों एवं प्रबन्धकों के लिए यह आवश्यक कर दिया जाए कि वे कामकाजी बालक/बालिकाओं को शिक्षा से सम्बद्ध क्रिया-कलापों में सम्मिलित होने तथा उन्हें शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने को प्रोत्साहित करें। मुक्त शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करके कामकाजी बालक/बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
प्रश्न (h) (ii) स्त्री-शिक्षा के संगठन।
उत्तर-भारतवर्ष में स्त्री-शिक्षा की व्यवस्था प्राचीन काल से ही दो प्रमुख रूपों में मिलती है। एक छात्रों तो एकमात्र स्त्री-शिक्षालयों में दी जाती हैं तथा दूसरी व्यवस्था के अन्तर्गत स्त्री-शिक्षा अन्य पुरुष के साथ सह-शिक्षा विद्यालयों में दी जाती है।
वैदिक काल में स्त्री-शिक्षा व्यवस्था ‘तपोवनों’ में संचालित होती थी। इन तपोवनों में महिलाओं तथा पुरुषों के लिए शिक्षा-व्यवस्था न होकर कुमारियों और कुमारों जिन्हें ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी कहकर पुकारा जाता था, के लिए होती थी। कुमार आश्रम बहुत दूरी पर पृथक्-पृथक् हुआ करते थे जिनकी व्यवस्थाएँ पुरुष व्यवस्थापकों (ऋषियों) तथा स्त्री व्यवस्थापिकाओं (विदुषियों) के हाथों में होती थी। परन्तु गुरु-आश्रमों में यदि गुरु कोई कन्या रखता था तो वह कुमार-विद्यार्थियों के साथ अध्ययन कर लेती थी। गुरु के आश्रम में कुमार ओर कुमारी छात्राएँ भाई-बहिन के सम्बन्ध स्थापित करके अध्ययनशील रहते थे। पुराने काल में कुमार और कुमारी को जीवन के लिए तैयार किया जाता था अतः इनका ब्रह्मचर्य-काल शक्ति-संचय का काल होता था। इस शक्ति को संचित करके वे कठोर जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्याश्रम पूर्ण करते थे और बाद में गृहस्थाश्रम का उपभोग करके योग्य सन्तान उत्पन्न करते थे। इसलिए आधुनिक गुरुकुल प्रणाली जिसे युग प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्थापित किया था, इसी धारणा से चलायी थी कि कुमार और कुमारी पृथक्-पृथक् रहकर शिक्षार्जन काल में ब्रह्मचर्यपूर्वक रह सकें और शक्ति संचित करके अपने भावी जीवन में आने वाले प्रत्येक संघर्ष को झेलकर सफलता प्राप्त कर सकें।
प्रश्न (h) (iii) स्त्री-शिक्षा का प्रशासन एवं नियंत्रण।
उत्तर-
शिक्षा राज्यों के उत्तरदायित्व का विषय है जिसका विकास राज्यों को ही करना होता है,
परन्तु केन्द्रीय सरकार राज्यों को विकासात्मक अनुदान प्रतिवर्ष दिया करती है। इस प्रकार स्त्री-शिक्षा के सभी विद्यालय प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक चार प्रशासकों के नियन्त्रण में हैं-
(1) केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में,
(2) राज्य सरकार के प्रशासन में,
(3) स्थानीय परिषदों के प्रशासन में, तथा
(4) व्यक्तिगत अथवा सामाजिक प्रशासन में ।
केन्द्रीय सरकार स्त्री-शिक्षा की कोई पृथक् व्यवस्था नहीं करती, वह इस शिक्षा को भी शिक्षा मन्त्रालय में माध्यम से सामान्य शिक्षा की भाँति व्यवस्थित करती है। परन्तु ‘राष्ट्रीय महिला शिक्षा- परिषद्’ की संस्तुति पर वह विशिष्ट आयोग या समिति नियुक्त करके उसकी स्थिति का सर्वेक्षण करा लेती है और स्त्री-शिक्षा के विकास की संस्तुतियाँ स्वीकार करके एक राष्ट्रव्यापी नीति बना लेती है जिसकी सूचना राज्य सरकारों को दे दी जाती है। राज्य सरकारें उस नीति का पालन करके स्त्री-शिक्षा की व्यवस्था करती हैं।
राज्य सरकारें और प्रदेश में शिक्षा विभाग की सहायता से सभी स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था, प्रशासन और नियन्त्रण करती हैं। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा का संचालन शिक्षा विभाग (प्रान्तीय) करता है। स्त्री-शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रदेश के शिक्षा विभाग में महिला शिक्षा निदेशक ही उत्तरदायी होती है। निर्धारित महिलाएँ शिक्षा निर्देशक अपनी सहायतार्थ मण्डलों की सीमा निर्धारित करके ‘विद्यालयों की मण्डलीय निरीक्षिका’ की नियुक्ति कराती हैं। एक मण्डल के सभी कन्या विद्यालयों की शिक्षा-व्यवस्था का प्रशासनिक तथा आर्थिक उत्तरदायित्व उपर्युक्त निरीक्षक के माध्यम से सम्पन्न होता है। इस प्रकार स्त्री-शिक्षा माध्यमिक स्तर तक दोहरे शासन में रहती है।
प्रश्न (h) (iv) सह-शिक्षा के संदर्भ में स्त्री-शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
प्रत्येक शिक्षा आयोग ने अपनी संस्तुतियों में यही कहा है कि स्त्रियों के लिए पुरुषों के समान सामान्य पाठ्यक्रम तथा एक-एक पृथक् विशिष्ट पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। इस विशिष्ट पाठ्यक्रम में गृह-विज्ञान, गृह-अर्थशास्त्र और गृह प्रबन्ध जैसे विषय, ललित कलाएँ (संगीत, चित्रकला और नृत्यकला) रखी जानी चाहिए।
वास्तव में स्त्री-शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य स्त्रियों को योग्य गृहिणी, योग्य माता और योग्य पत्नी बनाना है। इसके अतिरिक्त वे भारत के सामान्य नागरिकों की भाँति पुरुषों के समान कर्त्तव्यों और अधिकारों का निर्वाह कर सकती हैं। भारतीय संविधान में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हैं।
कोठारी आयोग ने सुझाव दिया है कि स्त्रियों को स्त्रियोचित पाठ्यक्रम तो अवश्य मिलना चाहिए; परन्तु वह इस बात में स्वतन्त्र होनी चाहिए कि वह किसी पाठ्क्रम का चयन कर सकती है। उस पर गृह विज्ञान, गृह-प्रबन्ध और गृह- अर्थशास्त्र लादा नहीं जाना चाहिए। परन्तु हाईस्कूल स्तर तक उपर्युक्त गृह-विज्ञान सम्बन्धी विषयों के माध्यम से गृह-व्यवथा का जानना आवश्यक है। अतः इस स्तर तक इन विषयों को अनिवार्य बनाया जा सकता है।
उच्च माध्यमिक स्तर तथा उच्च शिक्षा-स्तर पर उन महिलाओं के लिए जो नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकतीं, घर पर ही पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए ‘पत्राचार शिक्षण व्यवस्था’ तथा ‘सेवा-कालीन’ शिक्षा-व्यवस्था उपयुक्त रहेंगी। महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से परीक्षाओं में बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि महिलाएँ भी पुरुषों के पाठ्यक्रम ग्रहण करके कुशल शिक्षक, कुशल चिकित्सक, योग्य अभियन्ता, नेता और समाज सुधारक बन सकती हैं। अतः उन्हें विषय चयन की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।
प्रश्न (h) (v)सह-शिक्षा के गुणों का वर्णन कीजिए।
अथवा
भारतीय परिप्रेक्ष्य में सह-शिक्षा की ताकत का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
सहशिक्षा के समर्थन में तर्क दिया जाय तो तीन तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रथम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की कम जनसंख्या होने के कारण अलग स्कूल या कॉलेज खोलना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है। विशेषकर यह परिस्थिति ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में बहुत ही गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न कर देती है। वही भवन, वही साधन-सामग्री, पुस्तकालय तथा अन्य सुविधाएँ लड़कियों के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती हैं। अतः अतिरिक्त वित्तीय भार और अनावश्यक वृद्धि अपव्ययपूर्ण होगी। द्वितीय दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक है, जिसमें नारी-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति का कथन है—“पारस्परिक सम्पर्क जिज्ञासा की उस भावना का अन्त कर देता है, अजनबीपन के कारण उत्पन्न हो जाती है जो लिंगों के अलगाव और पृथकता की विशेषता है।” ऐसा समझा जाता है कि केवल साथ रहने में ही प्राकृतिक भावनाओं की समझ व आत्मविश्वास की भावना आ सकती है । एक विद्वान् लेखक का मत है-“भावी माताओं को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे आँसू भरकर कहें कि वे पुरुषों को समझती ही नहीं।” ऐसा माना जाता है कि सहशिक्षा के द्वारा यौन प्रवृत्ति को उचित मार्ग दिया जा सकता है। तृतीय कारक के रूप में भावनात्मक सन्तुलन को प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा समझा जाता है कि पुरुष एक हिंसक पशु है और वह नारी के कारण सीमाओं को ध्वस्त नहीं कर पाता है। लड़के-लड़कियाँ परस्पर गुण ग्रहण कर सकते हैं-लड़के, लड़कियों से धैर्य और लड़कियाँ, लड़कों से आत्मनिर्भरता। इस प्रकार लड़के अधिक सुधरे बनते हैं तथा लड़कियाँ कम लज्जावती और नाजुक बनती हैं।
प्रश्न (i) (i) सहशिक्षा के दोष / अवगुण बताइए ।
उत्तर-
सहशिक्षा के दोष निम्न हैं-
1. बालक के व्यक्तित्व पर वातावरण और समूह-सम्पर्क का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब दो विरोधी यौन-भावनाओं के व्यक्ति पारस्परिक सम्पर्क में आते हैं तो उनका ध्यान शिक्षा में नहीं रहता। उनका अवधान यौन आकर्षण के कारण पढ़ाई से हट जाता है। शिक्षा ग्रहण करना पर्याप्त संयम, तपस्या और श्रम का कार्य है। इसे यूँ ही ग्रहण नहीं किया जाता। सह-शिक्षा विद्यालयों में अधिकांश छात्रों के परीक्षा परिणाम आशा के विपरीत जाते हैं। इसका कारण विरोधी यौन आकर्षण है जिससे प्रभावित होकर बालक पथभ्रष्ट हो जाता है और अपना लक्ष्य भूल जाता है।
2. छात्र में छात्रा की अपेक्षा हीनभावना होती है। पुरुष, महिला के सम्पर्क में आते ही उसके सम्मुख आत्महीनता का शिकार हो जाता है। इस प्रकार पुरुष छात्र का व्यक्तित्व विकास की स्थिति में न रहकर हीनभावना से पूरित हो जाता है। यदि शारीरिक रचना में पुरुष की अपेक्षा महिला कम सुन्दर होती है तो उसके विपरीत महिला में ही हीनभावना जाग्रत हो जाती है और उसके व्यक्तित्व पर अवांछनीय प्रभाव पड़ने लगता है।
प्रश्न (i) (ii) भारतीय समाज में स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
प्रजातन्त्र में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से स्त्री-शिक्षा का बहुत अधिक महत्त्व है। स्त्री को पुरुष के समान कर्त्तव्य निर्वाह तथा अधिकारों का उपभोग करने के अवसरों तथा सुविधाओं की प्राप्ति हुई है। यदि स्त्री पुरुषों के समान योग्य और शिक्षित हो तो वह अपने मतदान का सदुपयोग कर सकती है और राष्ट्र की, समाज की, परिवार की और व्यक्तिगत समस्याओं पर चिन्तन करके उनके हल प्रस्तुत कर सकती है।
सामाजिक क्षेत्र में स्त्री-जाति सामाजिक सुधार का आधारशिला होती है। वह परिवार का सृजन और निर्माण करने वाली होती है। सबसे पहले नागरिकता की शिक्षा उसी के संरक्षण में मिलती है। यदि स्त्री शिक्षित नहीं होती तो वह परिवार में रहकर नागरिकता का प्रसार करने का उत्तरदायित्व न्यायपूर्वक नहीं निभा सकती। इसलिए स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता और महत्त्व अनुभव किया जाता है। स्त्री बालक की सबसे पहली और महत्त्वपूर्ण शिक्षक होती है। यदि वह अशिक्षित हुई तो बालक का शैक्षिक तथा सामाजिक विकास उपयुक्त रूप में नहीं होता। नारी समाज की शक्ति होती है। वह प्रेम, दया, त्याग की मूर्ति होती है। उसके इन गुणों के कारण वह समाज की प्रतिष्ठित शक्ति है। वह सच्चे अर्थों में सृजन की प्रेरणा है जिसको शिक्षित करके मानवीय गुणों की अनुभूति में सहयोग पाया जा सकता है।
स्त्री देश की संस्कृति, धर्म, साहित्य, कला एवं ज्ञान-विज्ञान का स्तम्भ होती है। उसे शिक्षित बनाकर उनकी सृजनात्मक क्रियाशीलताओं को प्रबुद्ध, शुद्ध और समुन्नत बनाया जा सकता है। यह सृजनात्मक क्रियाशीलता पुरुष का उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक और अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व और मार्गदर्शन तभी कर सकती है जब वह सुशिक्षित हो, साधन सम्पन्न हो। अतः राष्ट्र में स्त्रीत्व का विकास करने के लिए स्त्री-शिक्षा महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।
प्रश्न (i) (iii) महिला शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के सुझावों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह व्यवस्था है कि शिक्षा को महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन लाने के साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली-
1. महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका अदा करेगी।
2. नये सिरे से तैयार किये गये पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों के माध्यम से नये मूल्यों के विकास में योगदान देगी।
3. विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत महिलाओं सम्बन्धी अध्ययन को प्रोत्साहित करेगी। लक्ष्यों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं-
(i) महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका की योजना के लिए समूची शिक्षा प्रणाली को तैयार करना।
(ii) विभिन्न पाठ्यक्रमों के एक माँग के रूप में महिलाओं सम्बन्धी अध्ययनों को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहन देना।
प्रश्न (i) (iv) राष्ट्रीय कार्यक्रम द्वारा प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु सुझाव का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
सर्वशिक्षा अभियान की वर्तमान योजना के अन्तर्गत यह कार्यक्रम प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्ति से वंचित पिछड़ी बालिकाओं हेतु अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराना है। यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन विकास खण्डों में चलाया जा रहा है, जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है तथा लैंगिक भेदभाव भी राष्ट्रीय लैंगिक भेदभाव से अधिक है। यह कार्यक्रम ऐसे जिलों एवं विकास खण्डों में संचालित किया जा रहा है जहाँ न्यूनतम 5 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की है साथ ही जहाँ अनुसूचित जाति/जनजाति साक्षरता की दर वर्ष 1991 के आधार पर राष्ट्रीय औसत से 10% कम है।
समाधान हेतु सुझाव– कोठारी आयोग (1964-66) ने देश में नारी-शिक्षा के विकास हेत नीचे लिखे सुझाव दिए—
1. राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रस्तावित विशेष कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना।
2. स्त्री-शिक्षा के सम्पूर्ण नारी विकास के कार्यक्रमों को एक अंग के रूप में अपनाना।
3. लड़कों व लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता प्रदान की जाए।
4. स्त्री-शिक्षा के लिए प्राथमिकता के आधार पर धन दिया जाए।
5. स्त्री-शिक्षा के विकास में केन्द्र व राज्य दोनों ही रुचि लें।
प्रश्न (i) (v) स्त्री-शिक्षा हेतु कोठारी आयोग के सुझावों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
‘कोठारी कमीशन’ ने स्त्री-शिक्षा के समस्त पक्षों के विषयों में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं ज निम्नलिखित हैं-
(1) प्राथमिक शिक्षा- ‘कोठारी कमीशन’ ने बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अधोलिखित सुझाव दिये हैं-
1. भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएँ।
2. बालिकाओं को बालकों के प्राथमिक विद्यालयों में भेजने के लिए जनमत का निर्माण किया जाय।
(2) माध्यमिक शिक्षा- ‘कोठारी कमीशन’ ने बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा के विषय में उक्त विचार प्रकट किये हैं-
बालिकाओं के लिए पृथक् विद्यालयों की स्थापना की जाय। जहाँ यह सम्भव नहीं है, वहाँ के स विद्यालय में कुछ अध्यापिकाओं की अनिवार्य रूप से नियुक्ति की जाय।
(3) उच्च शिक्षा- ‘कोठारी कमीशन’ ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा के बारे में निम्नांकित सुझाव अक्षरबद्ध किये हैं-
1. छात्रवृत्तियों एवं मितव्ययी छात्रावासों की व्यवस्था करके, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
2. बालिकाओं के लिए पूर्व-स्नातक स्तर पर पृथक् कॉलेजों का निर्माण किया जाय।
3. बालिकाओं के कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानवशास्त्र आदि पाठ्य-विषयों में से चयन करने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाय।
प्रश्न (i) (vi) स्त्री-शिक्षा हेतु राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, 1958 के सुझाव का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
भारत सरकार ने सन् 1958 में स्त्री-शिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में ‘राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति’ की नियुक्ति की। इस समिति को ‘देशमुख समिति’ भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य — स्त्री-शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करना था। ‘समिति’ ने फरवरी, 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार समक्ष प्रस्तुत किया और उसमें निम्नांकित सुझाव दिए-
1. केन्द्रीय सरकार को कुछ समय के लिए स्त्री शिक्षा को एक विशिष्ट समस्या के रूप स्वीकार करना चाहिए और उसके प्रसार का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।
2. केन्द्रीय सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में स्त्री-शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना चाहिए।
3. केन्द्रीय सरकार को सब राज्यों के लिए स्त्री-शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारित करनी चाहिए और उनको इस नीति का अनुसरण करने के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए।
प्रश्न (j) (i) राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् (1959) के सुझावों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
‘देशमुख समिति’ की सिफारिश को स्वीकार करके, केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने सन् 1959 में ‘राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्’ का निर्माण किया। सन् 1964 में इसका पुनर्गठन किया गया।. इस समय इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 27 सदस्य हैं। इसके मुख्य कार्य अधोलिखित हैं-
1. विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना।
2. उक्त क्षेत्रों में बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिए लक्ष्यों, नीतियों, कार्यक्रम एवं प्राथमिकताओं के विषयों में सुझाव देना ।
3. उक्त क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिए उपायों का सुझाव देना ।
4. बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में जनमत का निर्माण करने के लिए उचित उपायों का सुझाव देना।
प्रश्न (j) (ii) महिला शिक्षा हेतु हंसा मेहता समिति (1962) के सुझावों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
‘राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्’ का एक मुख्य कार्य — विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करना है। इन समस्याओं में सर्वप्रमुख यह है— क्या विद्यालय-स्तर पर बालकों एवं बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में अन्तर होना चाहिए? ‘परिषद’ ने इस समस्या पर विचार करने के लिए श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की जिसे ‘हंसा मेहता समिति’ कहा जाता है। इस समिति के सदस्यों ने पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् दो सुझाव प्रस्तुत किये; यथा—
पहला सुझाव यह था कि विद्यालय-स्तर पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अन्तर नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए ‘समिति’ ने कहा- “हम भारत में जनतन्त्रीय एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे समाज में शिक्षा का समबन्ध व्यक्तिगत क्षमताओं, रुझानों एवं रुचियों से होना चाहिए, जिनका लिंग से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। अतः ऐसे समाज में लिंग के आधार पर पाठ्यक्रमों में अन्तर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ”
दूसरा सुझाव यह था कि भारत में अभी जनतन्त्रीय एवं समाजवादी समाज के निर्माण की प्रतिक्रिया चल रही है। अतः इस अन्तःकालीन अवधि में हमें पुरुषों एवं स्त्रियों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यों के भेदों के आधार पर बालकों एवं बालिकाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए। किन्तु पाठ्यक्रमों की विभिन्नता नये समाज के निर्माण में उपस्थित नहीं करनी चाहिए। अतः ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जो पुरुषों एवं स्त्रियों के वर्तमान अन्तर को स्थायी या अधिक उग्र बना दे।
प्रश्न (j) (iii)महिला समाख्या का स्त्री-शिक्षा हेतु सुझावों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
यह योजना (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा) केन्द्र सरकार द्वारा अप्रैल, 1989 में शुरू गई। इसे इण्डो-चाइना संयुक्त कार्यक्रम के रूप में नीदरलैण्ड सरकार से शत-प्रतिशत सहायता मिलती है। प्रारम्भ में इस योजना के अन्तर्गत कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्य थे। परन्तु अब इसका संचालन आन्ध्र-प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश तथा असोम के 53 जिलों के 9000 ग्रामों में हो रहा है। महिला समाख्या कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछडी महिला वर्गों की शिक्षा तथा उनको अधिकार सम्पन्न करने का ठोस कार्यक्रम है।
महिला समाख्या के उद्देश्य-इस कार्यक्रम के निम्नांकित उद्देश्य हैं|
(1) महिलाओं की आत्मछवि एवं आत्मविश्वास को बढ़ाना।
(2) ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाएँ वह ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सकें उन्हें समाज में रचनात्मक भूमिका निभाने में सहायता दे सकें।
(3) प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण तथा भागीदारी वाला तरीका स्थापित करना।
प्रश्न (i) (iv) स्त्री-शिक्षा हेतु राममूर्ति समिति (1990) के सुझावों का वर्णन कीजिए
उत्तर-
आचार्य राममूर्ति समिति ने महिला शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नांकित महत्त्वपूर्ण सिफारिश की हैं-
1. शिशु देखभाल तथा शिक्षा केन्द्र प्राथमिक विद्यालयों के समीप स्थापित किये जाने चाहिए। साथ ही इनकी समयावधि को विद्यालयों की समयावधि के साथ समायोजित किया जाय।
2. कक्षा 1 से 3 का पाठ्यक्रम शिशु शिक्षा केन्द्रों के अनुकूल बनाया जाय।
3.आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों तथा विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित किया जाय।
4. 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जायें।
5. 500 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक जूनियर हाईस्कूल स्थापित किया जाय।
6.विद्यालय की समयावधि को स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल निर्धारित किया जाय।
7. शाला त्यागी (Drop outs) बच्चों के लिए गैर-औपचारिक (Non-formal) विधियों को काम में लाया जाय।
8.योग्य छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायें।
9.योग्य छात्राओं को यूनीफार्म, पाठ्य-पुस्तकें आदि प्रदान की जायें।
प्रश्न (j) (v) सह शिक्षा से आशय ।
उत्तर-
सहशिक्षा का अर्थ-
सहशिक्षा का अर्थ है-साथ-साथ शिक्षा अर्थात् बालक- बालिकाओं की एक साथ शिक्षा। पाठ्यक्रम, शिक्षक एवं कक्षा की त्रिवेणी में छात्र-छात्राओं का शिक्षा पाने के लिए एकत्रित होना ‘सहशिक्षा’ है। वैदिक काल से ही सहशिक्षा का प्रचलन चला आ रहा है आश्रम व्यवस्था में भी सहशिक्षा प्रचलित थी। मध्यकाल में सहशिक्षा कम हो गई तथा पुरुषों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा जबकि नारी को तो केवल ‘भोग्या’ बना दिया गया। अंग्रेजी शासन में पुनः सहशिक्षा का प्रारम्भ हुआ। महिला वर्ग में जागृति आई तथा उन्होंने भी पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने का साहस किया। जैसे-जैसे आधुनिकता का विकास हुआ, शिक्षा का प्रसार बढ़ता गया तथा सहशिक्षा देने हेतु अनेक स्कूल-कॉलेज खोले गए। शनैः-शनैः सहशिक्षा की व्यवस्था प्रायः प्रत्येक स्कूल तथा कॉलेज में की जाने लगी है।
प्रश्न (j) (vi) सहशिक्षा के पक्ष में विचार दीजिए ।
उत्तर-
सहशिक्षा के पक्ष में विचार- सहशिक्षा का प्रचलन कण्व ऋषि तथा वाल्मीकि जैसे ऋषियों के समय से चला आ रहा है। उनके आश्रमों में सहशिक्षा दी जाती थी। सहशिक्षा के पक्षधर इसके अनेक गुण बताते हैं। सर्वप्रथम सहशिक्षा से धन का अपव्यय रोका जा सकता है। जिन विषयों में छात्र-छात्राओं की संख्या कम होती है, उनके लिए भी लड़कों व लड़कियों की पृथक्-पृथक् व्यवस्था करने में देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, जबकि सहशिक्षा के तहत एक ही विद्यालय से काम चल जाता है तथा बचा हुआ पैसा अन्य विकास के कार्यों में लगाया जा सकता है। विद्यार्थी काल विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इससे आगे जाकर उनमें आत्मविश्वास तथा मनोबल बढ़ता है। सहशिक्षा में लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे से अपने विचारों के आदान-प्रदान करत हैं, जिससे उनका मार्ग सुगम हो जाता है। सहशिक्षा के अभाव में छात्र-छात्राएँ दोनों ही संकोची रह जाते
हैं और जब आगे जाकर कार्यालयों या अन्य विभागों में उन्हें साथ-साथ काम करना पड़ता है तो संकोच बने रहने के कारण कुछ समय तक दोनों को, विशेषकर लड़कियों को तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सहशिक्षा से जहाँ एक ओर लड़कियों में नारी सुलभ लज्जा, झिझक, पर पुरुष से भय, अबलापन, बेहद कोमलता, हीन भावना जैसी भावनाएँ कुछ हद तक दूर हो जाती हैं। कहीं लड़के भी लड़कियों की उपस्थिति में उचित व सभ्य व्यवहार करना सीख जाते हैं। लड़कियाँ भी सड़कों की उपस्थिति में सौम्य तथा शान्त रहना सीख जाती हैं तथा उनमें व्यवहार कुशलता, वीरता तथा साहस आदि गुणों का विकास होता है। सहशिक्षा के अन्तर्गत लड़के-लड़कियों में प्रतिस्पर्द्धा की भावना पैदा होती है और वे एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ करते हैं। यही स्वच्छ प्रतिस्पर्द्धा उनके अध्ययन, चिन्तन तथा मनन को बलवती बनाती है।
प्रश्न (j) (vii) सहशिक्षा के विपक्ष में दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर—
जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, फूल के साथ काँटे भी होते हैं, सुख तथा दुःख साथ-साथ चलते हैं उसी प्रकार सहशिक्षा के विपक्ष में भी अनेक मत हैं। भारतीय शास्त्रों का विधान है कि लड़के तथा लड़कियों की पाठशालाओं में पर्याप्त अन्तर होना चाहिए तथा वे अलग- अलग दिशाओं में होने चाहिए। सहशिक्षा पूर्ण रूप से भारतीय वातावरण के प्रतिकूल है इसका भारतीय इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। सभी महापुरुषों ने इसका कठोर विरोध किया है। ‘मनुस्मृति’ के अनुसार लड़के-लड़कियों की शिक्षा अलग-अलग होनी चाहिए। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी ‘सत्यार्थ प्रकाश’ नामक ग्रन्थ में सहशिक्षा का विरोध किया है।
इसके विरोधी पक्ष वालों का मत है कि लड़के-लड़कियों का जीवन एकदम भिन्न होता है लड़कों को आगे जाकर आजीविका कमानी पड़ती है इसीलिए उनकी शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जबकि लड़कियों को तो विवाह के बाद घर-गृहस्थी की जिम्मेदारी निभानी होती है इसलिए उन्हें बस इतना ज्ञान आधुनिक वातावरण के सहपाठी भाई-बहिन या मित्र की भावना में न रहकर प्रेमी- प्रेमिका की भावना से ग्रस्त रहते हैं। आजकल तो स्कूली सहशिक्षा के समय में ही लड़के-लड़कियों में आकर्षण पैदा हो जाता है और ऐसा होने पर दोनों ही अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यह स्थिति न तो अध्ययन, न जीवन का विकास, अपितु चरित्र पतन, विनाश की ओर अग्रसर करती है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रसंग अश्लीलता के भी आ जाते हैं जो नैतिकता के विपरीत होते हैं। ऐसे प्रसंगों को शिक्षक भी ठीक प्रकार से नहीं समझा पाते हैं तथा उस विषय में छात्र-छात्राओं का ज्ञान अधूरा रह जाता है अर्थात् सहशिक्षा ज्ञानवर्द्धन में बाधक है। विरोधी पक्ष वाले व्यक्तियों को सहशिक्षा में केवल हानियाँ ही नजर आती हैं। उनके अनुसार सहशिक्षा चारित्रिक पतन का कारण है।
प्रश्न (j) (viii) सहशिक्षा का महत्त्व।
उत्तर—
सह-शिक्षा व्यक्तित्व, नेतृत्व विकास के साथ-साथ सम्प्रेषण क्षमता में सहायक है। वर्तमान युग में सह-शिक्षा आवश्यक है। सह-शिक्षा प्राप्त करने से विद्यार्थी अपने जीवन में अधिक सफल रहते हैं। उनका कहना है कि हम पुरुषों और महिलाओं को हर सम्भव तरीके से एक साथ काम कर रहे हैं। जहाँ एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, तो हम बहुत शुरुआत यानी बचपन से एक ही धारणा में इस माहौल को विकसित करने की जरूरत है। सहशिक्षा से हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। सहशिक्षा में लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग विद्यालयों की आवश्यकता नहीं होगी, इससे बचे हुए पैसे को दूसरे कामों में लगाया जा सकता है जो कि सह शिक्षा के महत्त्व को दर्शाता है।
प्रश्न (j) (ix) सहशिक्षा की विशेषताएँ ।
उत्तर-
विश्व रूपी जीवन में नर-नारी दोनों एक पात्र हैं। विश्व रूपी रंगमंच पर नर-नारी दो ऐसे पात्र हैं, जिनके बिना जीवन रूपी नाटक का मंचन नहीं हो सकता है। प्रकृति और
पुरुष के रूप में उससे सृष्टि विकास का क्रम के अनुसार दोनों आज भी निरंतर जीवन और गृहस्थ की गाड़ी के दोनों पहियों के समान एक-दूसरे के पूरक बन कर एक-दूसरे का साथ निभाते हैं। सहशिक्षा के प्रयोग ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण धीरे-धीरे सामान्य हो जाता है। उनके अनुसार किसी चीज का लगातार उपयोग करने से उसके प्रति उदासीनता आ जाती है। अतः उदासीनता के कारण छात्रगण अपने अध्ययन अथवा भविष्य के प्रति अपनी ऊर्जा को अधिक केंद्रित कर सकते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि सहशिक्षा आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी है। लड़कों तथा लड़कियों के अलग-अलग संस्थानों के बजाय यदि एक ही संस्थान हो तो खर्च काफी कम किया जा सकता है। विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहाँ आर्थिक स्थिति मजबूत न हो वहाँ सहशिक्षा बहुत अधिक उपयोगी है। कुछ अन्य लोगों की धारणा है कि छात्र-छात्राओं के एक ही संस्थान में अध्ययन से उनके बीच आपसी समझ बढ़ती है। यह आपसी समझ उनके गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है।
प्रश्न (j) (x) सहशिक्षा के लाभ।
उत्तर-
सहशिक्षा के अनेक लाभ हैं। सहशिक्षा से लड़कियों में नारी स्वभाव सुलभ लज्जा, झिझक, पर-पुरुष से भय, कोमलता, अबलापन, हीनभावना किसी सीमा तक दूर हो जाती है। दूसरी ओर, युवक नारी के गुणों को अपना लेता है। उसकी निर्लज्जता, अक्खड़पन, अनर्गलता पर अंकुश लग जाता है और उसमें मृदुभाषिता, संयमित सम्भाषण, शिष्ट आचरण तथा नारी-स्वभाव के गुण विकसित होते हैं। युवक-युवतियों में भावों का यह आदान-प्रदान भावी जीवन में सफलता के कारण बनेंगे। सहशिक्षा से छात्र-छात्राओं में परस्पर प्रतिस्पर्द्धा की भावना पैदा होगी और इससे उनका बौद्धिक विकास भी होगा। दोनों वर्ग एक-दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करेंगे। लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे से झिझकेंगें नहीं। इससे लड़कियों में व्यर्थ की लज्जा दूर होगी, जिससे पढ़ाई समाप्त होने पर वे नौकरी में लड़कों से बात करने पर शर्माएँगी नहीं और लड़के भी लड़कियों के समक्ष अधिक संयम में रहना सीखेंगे। उन्हें नारी का सम्मान करने की प्रेरणा मिलेगी जिससे आगे जाकर उनका वैवाहिक जीवन भी सफल होगा।
प्रश्न (j) (xi) शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या महत्त्व है?
उत्तर-
शिक्षण अधिगम सामग्री के महत्त्व को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है-
(i) प्रेरणादायी,
(ii) क्रियात्मक अवसर की सुलभता,
(iii) स्पष्टीकरण में सहायक,
(iv) अर्थयुक्त अनुभव की प्राप्ति,
(v) रटने की प्रवृत्ति को कम करना,
(vi) शब्दावली में वृद्धि,
(vii) शिक्षण में कुशलता,
(viii) प्रत्यक्ष अनुभव,
(ix) दृश्य-श्रव्य द्वारा संग्रहण क्षमता में वृद्धि,
(x) मूर्त व अमूर्त रूप में प्रस्तुतिकरण,
(xi) मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित,
(xii) वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास तथा
(xiii) सक्रियता।
प्रश्न (j) (xii) समाज का क्या अर्थ है?
उत्तर-
व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक सम्बन्धों के व्यवस्थित रूप को ‘समाज’ कहते हैं। समाज को सामाजिक सम्बन्धों का जाल भी कहा जाता है। समाज में मानव व्यवहार व सम्बन्धों के नियंत्रण की व्यवस्था होती है जो समाज में संगठन व उपेक्षित स्थिरता प्रदान करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व रखते हैं। पारसन्स के अनुसार, “समाज को उन मानवीय सम्बन्धों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन व साध्य के रूप में की गयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, चाहे वे यथार्थ हों या प्रतीकात्मक।”
प्रश्न (j) (xiii) ट्रांसजेण्डर्स से सम्बन्धित समस्याओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
भेदभाव-ट्रांसजेंडर आबादी सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समूहों में से एक है।
लैंगिकता या लैंगिक पहचान अक्सर ट्रांसजेंडर को समाज द्वारा कलंक और बहिष्कार का शिकार बना देती है।
बहिष्कार- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है और कभी- कभी, यहां तक कि उनके अपने परिवार भी उन्हें बोझ के रूप में देखते हैं और उन्हें बाहर कर देते हैं
शिक्षा-उत्पीड़न, भेदभाव और यहां तक कि हिंसा के कारण ट्रांसजेंडर लोग समान शैक्षिक अवसरों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। अधिकांश ट्रांसजेंडर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि भारतीय स्कूल वैकल्पिक यौन पहचान वाले बच्चों को संभालने के लिए अपर्याप्त हैं। स्वास्थ्य-स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करते समय ट्रांसजेंडरों को अक्सर भेदभाव का अनुभव होता है, अपमान और उत्पीड़न से लेकर हिंसा और सेवा से पूरी तरह इनकार तक। यह समुदाय एचआईवी एड्स जैसी यौन संचारित बीमारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। हाल ही में यूएन एड्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ट्रांसजेंडरों के बीच एचआईवी का प्रसार 3.1% (2017) है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति ओर हिंसा से संबंधित तनाव शामिल हैं।
रोजगार– ट्रांसजेंडर आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं और आजीविका के लिए वेश्यावृत्ति और भीख मांगने जैसे व्यवसायों को करने के लिए मजबूर हैं या शोषणकारी मनोरंजन उद्योग का सहारा ले रहे हैं।
सार्वजनिक स्थानों और आश्रय तक पहुँच– ट्रांसजेंडरों को घरों या अपार्टमेंटों तक पहुंचने में सीधे भेदभाव ओर इनकार का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, उन्हें लिंग तटस्थ / अलग ट्रांसजेंडर शौचालयों के प्रावधान की कमी और सार्वजनिक शौचालयों तक पहुँच में भेदभाव के कारण भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
नागरिक स्थिति– ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सटीक और सुसंगत पहचान दस्तावेज रखना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है।
लिंग आधारित हिंसा–ट्रांसजेंडरों को अक्सर यौन शोषण, बलात्कार और शोषण का शिकार होना पड़ता है।
************
*********
********
******
&&&&&&&&&
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
(Long Answer Type Questions)
निर्देश – प्रश्न संख्या 2 से 9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। परीक्षार्थियों को प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल चार प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक (4 × 15 = 60 अंक) निर्धारित हैं।
इकाई-1
प्रश्न 2 (i) लिंग तथा लैंगिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लिंग तथा लैंगिकता के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर —
लिंग तथा लैंगिकता हेतु आंग्ल भाषा में Gender तथा Sex शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लिंग (Gender) का प्रयोग हम व्यक्तियों तथा आस-पास की वस्तुओं के नामों में भी प्रयुक्त करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य के दो रूप सृष्टि के समुचित परिचालन हेतु बनाये, जिसमें एक है स्त्री और दूसरा है पुरुष। स्त्री तथा पुरुष ही अपनी प्रारम्भ अवस्था में बालिका और बालक से सम्बोधित किये जाते हैं हमारे आस-पास के पर्यावरण में हम जो कुछ भी देखते हैं उसे किसी-न-किसी नाम से जानते हैं और इन नामों में ही उनका लिंग छुपा होता है।
व्याकरणिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाये तो संस्कृत में तीन लिंग हैं-
(1) स्त्रीलिंग- स्त्रीबोधक
(2) पुल्लिंग— पुरुषबोधक
(3) नपुंसकलिंग— स्त्री तथा पुरुष से अतिरिक्त हेतु।
हिन्दी व्याकरण में भी तीन लिंग तथा अंग्रेजी ग्रामर में भी तीन लिंग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार व्याकरण की शब्दावली में जिससे किसी के स्त्री-पुरुष या उससे अतिरिक्त होने का बोध हो, वह लिंग कहलाता है।
लिंग का सामान्य जीवन में प्रयोग स्त्री-पुरुष के सन्दर्भ में होता है, परन्तु यहाँ लिंग की हुए अवधारणा और उससे जुड़े विषयों में व्यापक अर्थ है। जैविक रूप से लिंग को परिभाषित करते कहा जा सकता है कि जब स्त्री तथा पुरुष के XX गुणसूत्र परस्पर मिलते हैं तब बालिका और जब स्त्री के XX गुणसूत्रों के साथ पुरुष के XY गुणसूत्र मिलते हैं तो बालक का लिंग निर्मित होता है।
लिंग से ही मिलता-जुलता शब्द है लैंगिकता अथवा कामुकता । सृष्टि की प्रक्रिया के सुचारु रूप से चलते रहने हेतु काम की भावना ईश्वर ने प्रत्येक जीव को प्रदान की जो विपरीत लिंग के संसर्ग से पूर्ण होकर अपनी भाँति के किसी नये जीव का विकास करती है। इस प्रकार अपने व्यापक अर्थों में लैंगिकता से तात्पर्य किसी लिंग के प्रति आकर्षण, अवबोध, भेदभाव, सम्पर्क, सहयोग इत्यादि से है।
लिंग तथा लैंगिकता के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य —
लिंग तथा लैंगिकता की व्यक्ति के अपने मनोविज्ञान तथा समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यावश्यक हो जाता है। आज बालक हो या बालिका दोनों ही एक-दूसरे से अलग-थलग होकर अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। दोनों में लैंगिक सामंजस्य होना आवश्यक है। अतः लिंग और लैंगिकता के भीतर निहित मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य से अवगत होना अत्यावश्यक हो जाता है।
लिंग तथा लैंगिकता के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यों से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि मनोविज्ञान क्या है? इसकी क्या परिभाषा है? यह जानने के लिए निम्नांकित वर्णन दृष्टव्य है-
1. मनोविज्ञान को गैरिट ने आत्मा का विज्ञान माना है जिसमें ‘साइकोलॉजी’ (Psychology) शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों— ‘साइकी’ (Psychi) जिसका अर्थ है— ‘आत्मा’ (Soul) तथा ‘लोगस’ (Logos), जिसका अर्थ है ‘अध्ययन’ (Study) से हुई है। इस प्रकार मनोविज्ञान का अर्थ है— ‘Study of the soul’ अर्थात् ‘आत्मा का अध्ययन’। प्लेटो, अरस्तू, डेकार्ट इत्यादि ने भी इसे आत्मा का विज्ञान’ माना है।
2. मध्य युग के दार्शनिकों, जिनमें इटली के दार्शनिक पोम्पोनाजी का नाम उल्लेखनीय है, ने मनोविज्ञान को ‘मस्तिष्क का विज्ञान’ बताया।
3. 16वीं शताब्दी में वाइत्स, विलियन जेम्स, विलियम वुण्ट, जेम्ससन इत्यादि विद्वानों ने मनोविज्ञान को ‘चेतना का विज्ञान’ बताया।
4. 20वीं शताब्दी के आरम्भ में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ बताये गये. जिसमें सर्वाधिक मान्यता ‘व्यवहार के विज्ञान’ को दी गयी।
परिभाषाएँ —
मनोविज्ञान की परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं–
1. गैरिसन व अन्य के अनुसार, “मनोविज्ञान का सम्बन्ध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है।”
2. स्किनर के अनुसार, “मनोविज्ञान, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है।”
3. बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वेल्ड के अनुसार, “मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है।”
4. पिल्सबरी के अनुसार, “मनोविज्ञान की सबसे सन्तोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के रूप में की जा सकती है।”
5. क्रो तथा क्रो के अनुसार, “मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव सम्बन्धों का अध्ययन है।” 6. जेम्स के अनुसार, “मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है।”
7. एच. आर. भाटिया के अनुसार, “शैक्षणिक पर्यावरण में किसी विचार अथवा क्रिया के व्यवहार के अध्ययन को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं।”
8. कॉलेसनिक के अनुसार, “मनोविज्ञान के सिद्धान्तों तथा उपलब्धियों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है।”
9. डॉ. विनोद उपाध्याय के अनुसार, “शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय के वातावरण में प्राप्त की हुई बालक की क्रियाओं का अध्ययन है।”
10. मन के अनुसार, “आधुनिक मनोविज्ञान का सम्बन्ध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है।”
11. वुडवर्थ के अनुसार, “मनोविज्ञान वातावरण के सम्बन्ध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ”
इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान की अधोलिखित विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं-
1. शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान है जिसकी सार्थकता अध्ययन के पश्चात् व्यवहार के संशोधन में आँकी जाती है।
2. शिक्षा मनोविज्ञान जीवन के वास्तविक आदर्शों की प्राप्ति में सहायक होता है
3. शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धान्तों को अपनाकर शुद्ध विज्ञान का स्वरूप ग्रहण कर
4. शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों, अध्यापक एवं अभिभावकों के लिए आवश्यक रूप से ज्ञेय है।
5. शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहारों का व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही रूपों में अध्ययन करता है।
इस प्रकार लिंग तथा लैंगिकता में मनोविज्ञान का महत्त्व अत्यधिक है, क्योंकि मनोविज्ञान मानव के समस्त व्यवहारों का अध्ययन प्रस्तुत करता है चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक रूप से लिंग तथा लैंगिकता का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का महत्त्व निम्न कारणों से है—
1. मूल-प्रवृत्तियों तथा सहज क्रियाओं हेतु—
प्रत्येक लिंग के व्यक्ति की अपनी कुछ मूल-प्रवृत्तियाँ तथा सहज क्रियाएँ होती हैं जिनके आधार पर उसकी क्रियाओं का निर्धारण होता है। ‘मूल-प्रवृत्तियों के सिद्धान्त’ का प्रतिपादन करने वाले अंग्रेज मनोवैज्ञानिक विलियम मैक्डूगल हैं। उन्होंने सन् 1908 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक ‘An Introduction to Social Psychology’ मूल-प्रवृत्तियों का विस्तृत वर्णन किया तथा मूल-प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल-प्रवृत्तियाँ सब मानव क्रियाओं के प्रमुख चालक हैं। यदि इन मूल-प्रवृत्तियों और इनसे सम्बन्धित शक्तिशाली संवेगों को हटा दिया जाये तो जीवधारी किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हो जायेगा। वह उसी प्रकार निश्चित और गतिहीन हो जायेगा, जिस प्रकार एक बढ़िया घड़ी, जिसकी कमानी हटा दी गयी हो या एक स्टीम इंजन, जिसकी आग बुझा दी गयी हो।
मूल-प्रवृत्तियों के और अधिक स्पष्टीकरण हेतु कुछ परिभाषाएँ दृष्टव्य
मैक्डूगल के अनुसार, “मूल-प्रवृत्ति परम्परागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे सम्बन्धित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है।”
जेम्स के अनुसार, “मूल-प्रवृत्ति की परिभाषा साधारणतः इस प्रकार कार्य करने की शक्ति के रूप में की जाती है जिससे उद्देश्यों और कार्य करने की विधि को पहले से जाने बिना निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है।”
वुडवर्थ के अनुसार, “मूल-प्रवृत्ति कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है।”
मरसेल के अनुसार, “मूल-प्रवृत्ति व्यवहार का एक सुनिश्चित और सुव्यवस्थित प्रतिमान है, जिसका आदिकारण जन्मजात होता है और जिस पर सीखने का बहुत कम या बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है।”
मूल-प्रवृत्तियों की उपर्युक्त परिभाषा के पश्चात् इसकी विशेषताएँ निम्न प्रकार दृष्टिगत होती हैं—
(i) मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात तथा आन्तरिक होती हैं।
(ii) मूल प्रवृत्तियाँ किसी-न-किसी रूप में संसार के सभी प्राणियों में पायी जाती हैं, अतः ये सार्वभौम विशेषता सम्पन्न हैं।
(iii) मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति हेतु किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती ।
(iv) प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित होती है।
(v) मूल-प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का ज्ञान पहले से नहीं होता है।
(vi) मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार से पृथक् नहीं किया जा सकता।
विलियम मैक्डूगल के शब्दों में “मूल प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव की क्रियाओं की प्रमुख चालक हैं। यदि मूल प्रवृत्तियाँ तथा उनसे सम्बन्धित शक्तिशाली संवेगों को हटा दिया जाये तो प्राणी किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। वह उसी प्रकार गतिहीन तथा निश्चल हो ” जायेगा जिस प्रकार एक अच्छी घड़ी, जिसकी मुख्य कमानी हटा दी गयी हो या स्टीम इंजन, जिसकी
आग बुझा दी गयी हो। ”
वर्गीकरण— मूल-प्रवृत्तियों के वर्गीकरण में मैक्डूगल का वर्गीकरण सर्वमान्य है। शारीरिक क्रियाओं के आधार पर मैक्डूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची तथा प्रत्येक से सम्बन्धित संवेग निम्न प्रकार बताये हैं—
मूल- प्रवृत्तियाँ —– संवेग
(i) पलायन, भागना —– भय
(ii) निवृत्ति अप्रियता —– घृणा
(iii) शिशु रक्षा —– वात्सल्य
(iv) संवेदना, शरणागति —– कष्ट
(v) काम —– कामुकता
(vi) जिज्ञासा कुतूहल —– आश्चर्य
(vii) आत्महीनता —– अधीनता की भावना
(viii) आत्म-प्रदर्शन —– श्रेष्ठता की भावना
(ix) सामूहिकता —– एकाकीपन
(x) भोजनान्वेषण —– भूख
(xi) संचय, संग्रह —– अधिकार की भावना
(xii) रचना —– रचना का आनन्द
(xiii) ह्रास —– आमोद
ये मूल प्रवृत्तियाँ न्यूनाधिक मात्रा में सभी व्यक्तियों में पायी जाती हैं तथा लिंग के आधार पर भी मूल-प्रवृत्तियों की मात्रा की न्यूनता और अधिकता में अन्तर पाया जाता है। काम नामक मूल प्रवृत्ति की प्रत्येक व्यक्ति में उपस्थिति पायी जाती है। लिंग चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनमें उपर्युक्त 14 मूल-प्रवृत्तियाँ पायी ही जाती हैं, परन्तु मूल प्रवृत्तियाँ लिंग तथा लैंगिकता के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित, परमार्जित तथा संशोधित होती रहती हैं, जिसके कारण तथा प्रभाव निम्नवत् हैं-
(i) बालक तथा बालिकाओं के पालन-पोषण में अन्तर होता है। इस कारण उनकी मूल- प्रवृत्तियों का प्रकाशन भिन्न-भिन्न होता है, जैसे- बालिकाओं को प्रारम्भ से ही मूल प्रवृत्तियों को दबाना और सीमित रखना सिखाया जाता है जबकि बालकों में यह प्रवृत्ति खुली हुई होती है।
(ii) मूल-प्रवृत्तियाँ बालक तथा बालिकाओं में न्यूनाधिक्य रूप से पायी जाती हैं। उदाहरणस्वरूप बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा शिशु रक्षा, संवेदना, संचय की प्रवृत्ति तो वहीं बालकों में क्रोध, कामुकता, श्रेष्ठता, अधिकार की भावना इत्यादि संवेग ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि उन्हें इसे दबाने की शिक्षा बालिकाओं की अपेक्षा कम मिलती है और बालिकाओं को प्रारम्भ से ही अपने संवेगों को नियन्त्रित करना सिखाया जाता है।
(iii) सहज क्रिया अर्थात् जिनको हम यन्त्रवत् और बिना विचारे करते हैं, कहलाती है। इस पर भी लिंग तथा लैंगिकता का प्रभाव देखने को मिलता है। लिंग के आधार पर इन सहज प्रवृत्तियों में बालक तथा बालिकाओं में सहज क्रियाओं को देखा जा सकता है जैसे— बालिकाएँ प्रारम्भ से ही घरेलू क्रियाकलापों में तथा बालक प्रारम्भ से ही बाह्य क्रियाकलापों में सहज रूप से रुचि लेने लगते हैं।
2. स्वस्थ लैंगिक विकास हेतु-
लिंग तथा लैंगिकता के मनोविज्ञान में परिप्रेक्ष्य का महत्त्व तथा आवश्यकता बालक तथा बालिकाओं में स्वस्थ लैंगिक विकास के लिए भी है, क्योंकि मनोविज्ञान प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बालक हो या बालिका, उसको महत्त्व प्रदान करता है। इस प्रकार स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण और लैंगिकता की भावना का विकास होता है।
3. अभिवृद्धि तथा विकास हेतु —
लिंग तथा लैंगिकता का सम्पत्यय बालक तथा बालिकाओं की अभिवृद्धि तथा विकास की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है जिसका अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। अभिवृद्धि तथा विकास के विषय में संक्षेप में आगे जानना आवश्यक है—
अभिवृद्धि— कोशिकाओं में होने वाली गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, जैसे- ऊँचाई, भार, चौड़ाई, हाथ-पैर तथा बाल इत्यादि का बढ़ना ।
फ्रैंक के अनुसार, “कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है । ”
विकास— सम्पूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास है। विकास के कारण बालक की कार्य-क्षमता तथा कुशलता में वृद्धि होती है। उदाहरणस्वरूप, पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि अभिवृद्धि है।
हरलॉक के शब्दानुसार, विकास, अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नई-नई
विशेषताएँ और नई-नई योग्यताएँ प्रकट होती हैं। ”
टॉयलर के अनुसार, “विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है।’
अभिवृद्धि तथा विकास के मनोवैज्ञानिक पक्ष का लिंग तथा लैंगिकता के परिप्रेक्ष्य में महत्त्व तथा प्रभाव यह है कि अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया का बालक तथा बालिकाओं पर प्रभाव अलग- अलग पड़ता है, जैसे— बालिकाओं की शारीरिक अभिवृद्धि किशोर वय में बालकों की अपेक्षा तीव्रता से होती है और मानसिक विकास, व्यावहारिक विकास की दृष्टि से भी वे शीघ्र ही परिपक्व हो जाती हैं। लैंगिक भेद के कारण बालकों में अभिवृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया बालिकाओं से भिन्न पायी जाती है।
4. चारित्रिक विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण हेतु— मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व का सूक्ष्मता से अवलोकन करता है और चरित्र के विकास पर भी बल देता है। लिंग तथा लैंगिकता के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत हम पाते हैं कि लिंग तथा लैंगिकता के आधार पर बालक तथा बालिकाओं के व्यक्तित्व में अलग-अलग गुणों तथा चारित्रिक गुण भी पाये जाते हैं जिनका अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है।
5. मानवता के विकास हेतु मानवता के विकास पर लिंग तथा लैंगिकता का प्रभाव पड़ता है। बालक और बालिकाओं में पाये जाने वाले मानवीय गुण भिन्न होते हैं, क्योंकि दोनों के पालन-पोषण तथा पारिवारिक सीख में लिंग के आधार पर ज्ञान प्रदान किया जाता है।
6. अधिगम हेतु – लिंग तथा लैंगिकता का प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। अधिगम में व्यक्तिगत विभिन्नता पर महत्त्व दिया जाता है तथा बालक तथा बालिकाओं में अधिगम हेतु अलग- अलग अभिरुचियों तथा रुचियों इत्यादि पर मनोविज्ञान बल देता है। मनोविज्ञान सीखने के नियमों द्वारा अधिगम को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देता है।
7. रुचि तथा व्यक्तिगत विभिन्नता हेतु- बालक तथा बालकों की रुचि और प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता को मनोविज्ञान में महत्त्व प्रदान किया जाता है और लिंग तथा लैंगिकता के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बालक तथा बालिकाओं दोनों की रुचियों तथा व्यक्तिगत विभिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए उनका विकास किया जाये और बालक तथा बालिकाओं दोनों को ही विकास करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं।
8. आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण हेतु मनोविज्ञान लिंग के आधार पर व्यक्ति विशेष की मानसिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। बालक तथा बालिकाओं में कुछ आपराधिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, जिनका अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लिंग तथा लैंगिकता की समस्याओं का अध्ययन तथा उसके उचित समाधानों का प्रस्तुतीकरण किया जाता है।
9. निर्देशन एवं परामर्श हेतु शंकाओं और उनके समुचित निदान की निर्देशन एवं परामर्श पर बल देता है। मनोविज्ञानं महत्त्वपूर्ण है।
लिंग तथा लैंगिकता के कारण उपजने वाली समस्याओं, आवश्यकता अत्यधिक होती है। अतः इस हेतु मनोविज्ञान अतः इस प्रकार भी लिंग तथा लैंगिकता के परिप्रेक्ष्य में
10. मानव व्यवहारों के ज्ञान हेतु— मनोविज्ञान के द्वारा मानव व्यवहारों का सूक्ष्म अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। बालक तथा बालिकाओं की आयु तथा उस आयु विशेष में उनके व्यवहारों और उनमें होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों का अध्ययन भी प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लिंग तथा लैंगिकता की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं।
प्रश्न 2 (ii) लिंग एवं लैंगिकता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट कीजिए।
अथवा
समाज को परिभाषित करते हुए लैंगिकता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालिए।
ANSWER–
समाज की परिभाषाएँ —
समाज को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार से परिभाषित किया है-
1. “समाज रीतियों, कार्य-विधियों, अधिकार व पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके उपविभागों, मानव-व्यवहार के नियन्त्रणों और स्वतन्त्रताओं की व्यवस्था है।”
-मैकाइवर एवं पेज
2. “समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक सम्बन्धों का एक योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक-दूसरे के साथ सम्बद्ध हैं।”
– प्रो. गिडिंग्स
3. “समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों की व्यवस्था है।”
-राइट
4. “समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जो कुछ सम्बन्धों या व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है, जो इन सम्बन्धों में नहीं बँधे हैं या जो व्यवहार में उनसे भिन्न होते हैं।”
5. “एक समाज अपेक्षाकृत, सर्वाधिक स्थायी समूह है जिसमें स्वार्थ, भू-भाग, जीवन-शैली, पारस्परिक सहयोग, अपनत्व की भावना, रहन-सहन की समानतायें उसे अन्य बाह्य लोगों से अलग करती है।”
-गिलिन
6.’समाज एक अमूर्त संकल्पना है जो किसी समूह के सदस्यों के बीच व्याप्त सामाजिक सम्बन्धों की समग्रता का बोध कराती है।”
-यूटर
7. “समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है अपितु उसके अन्तर्सम्बन्धों की जटिल व्यवस्था है। — लेपियर
8. समाज जीवित, परम्पराओं, रीतियों एवं प्रक्रियाओं का जटिल प्रारूप है जो पारस्परिक अन्तर्क्रियायें करते हुये विकसित होता है। फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रारूप में एकरूपता उत्पन्न हो जाती है और उसके एक भाग की हलचल सभी भागों को प्रभावित करती है।” -कूले 9.
9.”समाज मानवों द्वारा साध्य या साधन के रूप में यथार्थ या प्रतीकात्मक ढंग से की गई क्रियाओं से उत्पन्न सम्बन्धों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।”
-पारसन्स
लिंग तथा लैंगिकता के परिप्रेक्ष्य में ताने-बाने की भूमिका अत्यावश्यक है, क्योंकि मनोविज्ञान श्री चाहे बालक हो या बालिका, उसके लिए आनुवंशिकता के साथ-ही-साथ वातावरण की आवश्यकता को भी स्वीकार करता है। लिंग तथा लैंगिकता को हमारे आस-पास का वातावरण अर्थात् समाज काफी प्रभावित करता है। समाज क्या है, इसकी विशेषतायें क्या हैं, पहले यह जान लेना आवश्यक है।
समाज का अर्थ –
समाज हेतु आंग्ल भाषा में ‘Society’ शब्द प्रयुक्त किया जाता है, जिसका सामान्य अर्थ मनुष्यों के समूह से होता है। व्यक्तियों के मध्य स्थापित सम्बन्धों में संगठित रूप को इस प्रकार समाज कहते हैं।
परिभाषाएँ
समाज के अर्थ के और अधिक स्पष्टीकरण हेतु कुछ परिभाषाएँ दृष्टव्य हैं—
मैकाइवर तथा पेज के अनुसार “समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है, जो सदैव बदलता रहता है।”
टालकॉट पार्सनल के अनुसार- “समाज मानवीय सम्बन्धों का वह पूर्ण ढाँचा है जो वास्तविक या प्रतीकात्मक साधनों या सम्बन्धों के द्वारा कार्य करता रहता है।”
गिडिंग्स के अनुसार — “समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संघ का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक-दूसरे के साथ रहते हुए या सम्बद्ध हैं।”
लैपियर के अनुसार — “समाज का सम्बन्ध केवल लोगों के समूह के साथ नहीं, बल्कि उनके बीच होने वाले अन्तःकार्यों के जटिल ढाँचे के साथ है।”
प्यूटर के अनुसार — “यह एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बाद पाये जाने वाले पारस्परिक सम्बन्धों की जटिलता का बोध कराती है।”
राइट के अनुसार- “समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं है। समूह में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध से है, उन सब सम्बन्धों के संगठित रूप को समाज कहते हैं।”
विशेषताएँ
समाज की उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निम्नांकित विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं-
1. समाज व्यक्तियों का समूह है।
2. समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है।
3. समाज संगठित रूप है।
4. समाज व्यक्तियों के मध्य होने वाले अन्तर्क्रिया को द्योतित करता है।
5. समाज स्वयं संगठन है।
6. सम्बन्धों का संगठित रूप ही समाज
7. समाज में व्यक्ति परस्पर जुड़े होते हैं।
समाज के कार्य
समाज कई प्रकार के होते हैं, जैसे— परम्परागत समाज, बन्द समाज, मुक्त समाज, आदिम समाज, सभ्य समाज, सरल समाज, जटिल समाज, पूँजीवादी समाज, समाजवादी समाज, प्राचीन समाज, आधुनिक समाज आदि। समाज विभिन्न प्रकार के कार्यों का सम्पादन करता है जिसके कारण ही व्यक्ति समाज से अलग रहकर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है।
1. सामाजिक कार्य- समाज का प्रमुख कार्य सामाजिक कार्य है। प्रत्येक समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ नियम, रीति-रिवाज तथा परम्पराओं का पालन करना अपने सदस्यों को सिखाते हैं। समाज में रहकर ही बालक तथा बालिकायें सामाजिक व्यवस्था का पालन कर समाज के सक्रिय सदस्य बनते हैं जिसे हम समाजीकरण की प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार समाज से पृथक् रहकर समाजीकरण नहीं हो सकता, अतः इस दृष्टि से समाज महत्त्वपूर्ण है।
2. सांस्कृतिक कार्य — प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है जिसके आधार पर वह अपने बालक तथा बालिकाओं को सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। लिंग तथा लैंगिकता पर समाज की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे— विवाह की रस्में तथा बालक-बालिकाओं के वस्त्र आदि ।
3. शैक्षिक कार्य समाज शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है। वह विद्यालय के साथ मिलकर तथा अन्य अभिकरणों की सहायता तथा पृथक् रूप से भी शिक्षा के प्रचार-प्रसार का कार्य करता है। समाज का शिक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान है, सुशिक्षित तथा जागरूक समाजों में शैक्षिक उन्नति अधिक होती है। सामान्य विद्यालयी शिक्षा में योगदान देने के साथ-साथ बालकों के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु वातावरण सृजित करता है। इस हेतु समाज द्वारा वित्त की व्यवस्था कर विद्यालयों, पार्कों इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। समाज के द्वारा सभी वर्गों की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा मन्दबुद्धि और विकलांग बालकों, जैसे— विशिष्ट बालकों की शिक्षा के आयोजन के प्रति सकारात्मक प्रयास किये जाते हैं।
4. आर्थिक कार्य- समाज का प्रमुख कार्य अपने सदस्यों की आर्थिक गतिविधियों का संचालन करना है। आर्थिक उन्नति तथा विकास के लिए समाज कुछ नियमों का संचालन करता है जिसके अनुरूप आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है और समाज अपने सदस्यों की आर्थिक गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने, उन्नति हेतु वातावरण का सृजन भी करता है।
5. नैतिक एवं चारित्रिक कार्य- समाज अपने सदस्यों की सर्वांगीण उन्नति का प्रयास करता है और इसी क्रम में वह अपने सदस्यों की नैतिक तथा चारित्रिक उन्नति का प्रयास भी करता है। इस हेतु समाज उच्च आदर्शों तथा जीवन-मूल्यों को प्रोत्साहित करता है तथा साथ-ही-साथ ऐसे आदर्शों का प्रस्तुतीकरण भी करता है।
6. राजनैतिक कार्य- समाज अपने राजनैतिक कार्यों के अन्तर्गत अपने सदस्यों को राजनैतिक रूप से जाग्रत करने का कार्य करता है, उनकी राजनैतिक विचारधारा के निर्माण का कार्य भी सम्पन्न करता है।
7. सुरक्षात्मक कार्य समाज की संरचना और संगठन का महत्त्व इससे भी अत्यधिक है क्योंकि वह अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा का कार्य सम्पन्न करता है। समाज में रहकर ही व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता है, चाहे वह शिशु हो या कोई प्रौढ़। इस प्रकार समाज सामाजिक सुरक्षा का कार्य सम्पन्न करता है।
सुरक्षा का कार्य
8. सांवेगिक कार्य- समाज अपने सदस्यों की मनोवैज्ञानिक तथा सांवेगिक सम्पन्न करता है। इसीलिए समाज में रहकर ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर पाता है।
लिंग तथा लैंगिकता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य और उसके महत्त्व का आकलन अग्रवत् किया जा रहा है-
1. पालन-पोषण – बालक तथा बालिकाओं के पालन-पोषण पर समाज का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। मनुष्य शिशु जन्म के कुछ समय तक अपने परिवार तथा समाज पर निर्भर रहता है और जब तक वह जीवित रहता है तब तक समाज पर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर रहता है। समाज का स्वरूप यदि बन्द समाज का होगा तो लिंग के आधार पर बालक तथा बालिकाओं के पालन-पोषण में अन्तर होगा और यदि खुला तथा प्रगति उन्मुख समाज होगा तो उस समाज में लिंग तथा लैंगिकता विषयी दृष्टिकोण में व्यापकता और खुलापन होगा।
2. वातावरण सृजन- समाज बालक तथा बालिकाओं के लिए जैसा वातावरण सृजित करेगा, उनका विकास उसी प्रकार का होगा। समाज में यदि लिंग तथा लैंगिकता के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं है तो ऐसे वातावरण में भेदभाव और भावना ग्रन्थियों के पनपने की आशंका अधिक होती है और ऐसा समाज लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाकर स्वस्थ वातावरण सृजित किया जा रहा हो वहाँ पर परस्पर अन्तर्क्रिया तथा वैयक्तिक आदान-प्रदान का वातावरण सृजित होता है।
3. सुरक्षात्मक कार्य- समाज बालक तथा बालिकाओं को शारीरिक, सांवेगिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य सम्पन्न करता है जिससे सुरक्षात्मक अनुभूति आती है। सभ्य समाज बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की सुरक्षा हेतु अधिक सचेष्ट होते हैं और बालकों में प्रारम्भ से ही बालिकाओं के प्रति आदर-सम्मान की भावना भरते हैं।
4. सर्वांगीण विकास – समाज अपने सभी सदस्यों के सर्वांगीण विकास का कार्य सम्पन्न करता है। इस हेतु समाज तरह-तरह के सामाजिक आयोजन करता है और अपने सदस्यों को उनमें भाग लेने हेतु अवसर प्रदान करता है। बालक और बालिकाओं में लिंगाधारित भेदभाव न करके समाज को समान रूप से उनके सर्वांगीण विकास हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए।
5. नैतिक तथा चारित्रिक विकास- समाज बालक तथा बालिकाओं को समाजोपयोगी तथा आदर्श नागरिक बनाने हेतु उनके नैतिक तथा चारित्रिक विकास पर बल देता है। नैतिक तथा चारित्रिक गुण बालक तथा बालिकाओं में कुछ सामान्य रूप से तथा कुछ विशिष्ट रूप से पाये जाते हैं। बालिकाओं में जिन नैतिक तथा चारित्रिक गुणों की अनिवार्यता होती है वे आवश्यक नहीं कि बालकों में भी हों और बालकों में पाये जाने वाले नैतिक तथा चारित्रिक गुण आवश्यक नहीं कि वे बालिकाओं में भी पाये जायें। इस प्रकार नैतिक तथा चारित्रिक विकास का महत्त्वपूर्ण कार्य समाज लिंग तथा लैंगिकता को दृष्टिगत रखते हुए करता है।
6. समाजीकरण- समाज में रहकर ही बालक या बालिका का समाजीकरण होता है। समाजीकरण समाज के साथ अनुकूलन कर अपना विकास करने, सामाजिक नियम-कानूनों को मानने की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के कारण बालक तथा बालिकायें समाज के उपयोगी सदस्य बन सकते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में खुले समाज में बालकों की ही भाँति बालिकाओं को भी समान अवसर प्रदान किये जाते हैं, जिससे उनके समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है और इसके विपरीत बन्द तथा रूढ़िवादी समाज में बालिकाओं को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने की स्वतन्त्रता नहीं होने के कारण उनका समाजीकरण कुन्द हो जाता है। इस प्रकार लिंग तथा लैंगिकता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत समाज महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
7. अनौपचारिक शिक्षा— समाज अपने सदस्यों की अनौपचारिक शिक्षा का सशक्त तथा प्रभावी साधन है। व्यवहार, ज्ञान, वाग्-व्यवहार, संस्कृति, धर्म इत्यादि की शिक्षा अनौपचारिक रूप से समाज द्वारा प्राप्त होती है। समाज बालक तथा बालिकाओं की अनौपचारिक शिक्षा के साथ-साथ उनकी औपचारिक शिक्षा की भी व्यवस्था करता है। वैसे भी शिक्षा तथा समाज के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध है जिसे शिक्षा समाजशात्र के द्वारा अध्ययन किया जाता है। जागरूक तथा शिक्षित समाज में लिंग तथा लैंगिकता के विषयों पर अभेदपूर्ण, वैज्ञानिक तथा स्पष्ट दृष्टिकोण रखा जाता है जिससे स्वस्थ और प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है वहीं परम्परागत रूढ़ समाजों में बालिकाओं की औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा की अवहेलना की जाती है।
8. आदतों तथा रुचियों का विकास समाज जैसा होगा, उसके आदर्श जिस प्रकार के होंगे, वह अपने व्यक्तियों में उसी प्रकार की आदतों तथा रुचियों को प्रोत्साहित करेगा। बालक तथा बालिकाओं की रुचियों और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर भी प्रत्येक व्यक्ति की आदत और रुचियों में भिन्नता पायी जाती है, जिसमें से अच्छी, सकारात्मक तथा समाजोपयोगी आदतों तथा रुचियों को समाज द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। ये लिंग तथा लैंगिकता के परिप्रेक्ष्य में भी दृष्टिगत होती हैं ।
प्रश्न 2 (iii) यौन शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए ।
भारतीय समाज में यौन विषयक बातें करना वर्जित माना जाता है। जीव-विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य में यौनगत क्षमता स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। परन्तु सांस्कृतिक मानदण्डों तथा विधिनिषेधों के द्वारा यौनगत आचरण की अभिव्यक्ति परिसीमित रहती हैं। पाश्चात्य देशों में यौन सम्बन्धों में स्वच्छन्दता सामान्य बात है। कुछ समय से भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा पाश्चात्य जगत में विद्यमान यौन आचरण के खुलेपन ने यौन-शिक्षा के विचार को जन्म दिया है। विगत एक-डेढ़ दशक में फैली एच.आई.वी. तथा एड्स जैसी लाइलाज बीमारी ने भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न कर दिया है।
‘यौन शिक्षा का अर्थ —
जीवन के चार पुरुषार्थों— धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम को एक पुरुषार्थ के रूप में अपनाया गया है। आचार्य वात्स्यायन का कामसूत्र तथा खजुराहो के मन्दिरों में उत्कीर्ण रतिक्रीड़ा में लिप्त मुद्रायें सम्भवतः यौन शिक्षा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वैदिक काल में कामशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य स्त्री-पुरुष का अनर्गल, अनियन्त्रित पाशविक प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करके उन दोनों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति में सहायता प्रदान करना है। मनुष्य और पशु में अन्तर इतना ही होता है कि पशु अपने भोजन अथवा यौन की भूख मिटाते समय बदहवास होकर मर्यादाओं का अतिक्रमण कर लेता है, जबकि मनुष्य सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है।
आधुनिक समय में फ्रायड ने दमित कामेच्छा के प्रभाव का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करके मनुष्य के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया था।
यौन शिक्षा से तात्पर्य केवल यौन-क्रीड़ाओं व सम्बन्धों का ज्ञान करने से नहीं है, न ही यौन शिक्षा विवाह पूर्व या विवाहेतर यौन सम्बन्ध, यौन स्वतन्त्रता, काम-कला, यौन तृप्ति, अप्राकृतिक यौन-क्रियाएँ अथवा उन्मुक्त यौन व्यवहार का पर्याय है वरन् यौन शिक्षा का सम्बन्ध यौन विकृतियों तथा यौन सम्बन्धी गलत, अपर्याप्त व भ्रामक जानकारी के निषेध से है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों तथा यौन रोगों के होने के कारणों को समझाना अत्यन्त आवश्यक है। यौन शिक्षा इसी शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति करती है। यौन शिक्षा का सम्बन्ध यौन क्रियाओं तथा उनके प्रभाव के से है । यौन सम्बन्धी आशंकाओं तथा जिज्ञासाओं को जानकर यौन सम्बन्धों को सुरक्षात्मक् बनाने के उपाय यौन शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं। परन्तु यौन शिक्षा को लैंगिक सम्बन्धों के बारे में समझाने तक सीमित न रखकर प्रेम व विवाह से जोड़ना होगा। तब ही इसका दृष्टिकोण विस्तृत हो सकेगा।
भारतीय समाज यौन शिक्षा के सम्बन्ध में दो वर्गों में विभाजित है–
यौन शिक्षा के पक्ष का वर्ग- यौन शिक्षा के पक्षधर एड्स जैसी बीमारी के बढ़ने के खतरे, लड़कियों व युवतियों के यौन शोषण, बढ़ती यौन बीमारी, अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि आदि कारणों से यौन सम्बन्धी जानकारी का नियोजित व विज्ञानसम्मत आदान-प्रदान करने हेतु यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल देते हैं।
यौन शिक्षा के विपक्ष का वर्ग-
यौन शिक्षा के विपक्ष में पारस्परिक नैतिकता के पक्षधर यौन सम्बन्धी विषयों पर बातचीत करना मर्यादा तथा आदर्श का उल्लंघन मानते हुए शिक्षा को समाज में यौन व्यभिचार बढ़ाने का कारण मानते हैं।
पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित भारतीय समाज में यौन शिक्षा दी जाये अथवा नहीं, यह एक बड़ी समस्या है। नैतिक मूल्यों की सुरक्षा के साथ-साथ बच्चों, किशोरों तथा युवाओं को उनकी यौन सम्बन्धी जिज्ञासाओं का सही व सन्तोषप्रद उत्तर तो मिलना ही चाहिए। इसलिए मर्यादित तरीके से यौन शिक्षा के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने से पहले पर्याप्त चिन्तन, मनन एवं शोध की आवश्यकता है। यहाँ डॉ. श्रीमती फुलरेनु गुहा की अध्यक्षता में गठित नारी स्थिति में मिडिल स्कूल स्तर से यौन शिक्षा प्रारम्भ करने तथा यौन शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा सामग्री तैयार करने की अनुशंसा की थी।
यौन शिक्षा कार्यक्रम —
पहले घर-परिवार व समाज में रहकर ही व्यक्ति यौन शिक्षा प्राप्त करता था। लेकिन अब यह माध्यम यथेष्ट नहीं है। बालकों को यौन शिक्षा का पहला पाठ तो उनके माता-पिता घर पर ही पढ़ा सकते हैं। परन्तु बाद में बच्चों को यौन शिक्षा की पर्याप्त जानकारी शिक्षा संस्थाओं में दिया जाना सम्भव हो सकेगा। शिक्षा संस्थाओं में औपचारिक ढंग से यौन शिक्षा कब से दी जाये तथा कैसे दी जाये इन प्रश्नों के सम्बन्ध में भी मतभेद हैं। कुछ लोग यौन शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर देने की बात करते हैं, जबकि कुछ इसे उच्च स्तर पर देने की सिफारिश करते हैं। भारत में बालक तथा बालिकाएँ यौन दृष्टि से शीघ्र ही परिपक्व हो जाते हैं। यौन शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर ही दिया जाना उपयुक्त स्वीकार किया जा सकता है। यौन शिक्षा का वैज्ञानिक ज्ञान विधिवत् दिये जाने की आवश्यकता है, जिससे गलत धारणाओं तथा भ्रान्तियों के कारण उत्पन्न विकृतियों का अंत किया जा सके। एड्स जैसी यौन-जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी शिक्षा के द्वारा यौन सम्बन्धी उचित ज्ञान प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक है। यौन शिक्षा को एक पूर्ण विषय के रूप में शामिल न करके एक अनिवार्य तथा सामान्य प्रकृति के प्रश्न पत्र के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना अधिक उपयुक्त हो सकता है
प्रश्न 2 (iv) समाजीकरण के प्रभावशाली अंगों को स्पष्ट कीजिए।
अथवा
समाजीकरण के अभिकरणों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।
ANSWER–
समाजीकरण के अभिकरण —
समाजीकरण के प्रभावशाली अभिकरण निम्नलिखित हैं-
1. परिवार और समाजीकरण
बालक के संस्कार माता-पिता और परिवार पर निर्भर करते हैं। बालक के संस्कार गर्भस्थ काल से ही निर्मित होने लगते हैं जिन्हें जन्म के पश्चात विकसित होने का अवसर मिलता है। परिवार अथवा कुटुम्ब व्यक्ति का अनिवार्य समाज है जिसके आधार व्यक्ति के माता-पिता हुआ करते हैं। माता-पिता बालक के पोषण और रक्षण का उत्तरदायित्व निर्वाह करने में अपना कर्त्तव्य पालन करते हैं।। पिता बालक की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति का भरसक प्रयास करते हैं। कभी-कभी माता- पिता का बालक के प्रति व्यवहार सन्तुलित नहीं रहता है। कभी दोनों ही बालक पर असीमित प्यार उड़ेलकर बालक के असामाजिक तत्त्वों पर ध्यान नहीं देते। कभी माता लाड़ में आकर बालक को अधिक प्यार करती है और पिता उतना प्यार नहीं कर पाता। कभी एक से अधिक बच्चे होने पर जिनमें लड़के-लड़कियाँ दोनों ही हो सकते हैं, विविध स्तर का प्यार पाते हैं। इस प्रकार माता-पिता केअसंतुलित प्यार के कारण बालक में सामजिक गुणों का असंतुलन उत्पन हो जाता है |इकलौते बालक में माता-पिता के अटूट प्यार के कारण सामाजिक गुणों का अभाव पाया जाता है।। स्वावलम्बी नहीं होता, थोड़े ही संघर्ष में घबरा जाता है। वह सदैव यही इच्छा करता है कि उसके माता- पिता के समान समाज भी उसे उसी प्रकार असीमित प्यार करे, उसे महत्त्व दे और उसके अवगुणों पर ध्यान न दे, परन्तु समाज ऐसा नहीं कर पाता। इस व्यवहार से वह कुण्ठित होकर सन्तुलन खो बैठता। है और उसका व्यक्तित्व भी असन्तुलित हो जाता है। माता-पिता का बालकों के प्रति अमनोवैज्ञानिक व्यवहार उनके समाजीकरण को बहुत प्रभावित करता है। अधिक प्यार में पला लड़का अथवा लड़की विषम व्यवहार से युक्त होते हैं। अधिक प्यार में पली लड़की सामाजिकता के अभाव के कारण सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं करती। इसीलिए यह कहना असंगत नहीं होगा कि बालक ‘समस्यात्मक नहीं होते, वरन् माता-पिता ‘समस्यात्मक’ होते हैं जिनका असन्तुलित व्यवहार बालकों के समाजीकरण में बाधक होता है। वास्तव में बालकों का असामाजिक व्यवहार एवं असन्तुलित व्यक्तित्व उनके माता- पिता की समस्याओं को प्रकट करते हैं।
2. माता-पिता का पारस्परिक सम्बन्ध और समाजीकरण —
यदि माता-पिता आपस में आदर्श सम्बन्ध रखते हैं तो उनके प्रत्येक व्यवहार में सन्तुलन रहता है और बालकों के व्यवहारों में भी सन्तुलन उत्पन्न हो जाता है। यदि माता-पिता का पारस्परिक व्यवहार सन्तुलित और आदर्श न हुआ तो बालक का व्यवहार भी असन्तुलित रहेगा और वह समाज की मान्यताओं से मेल नहीं खा सकेगा। माता-पिता के व्यवहारों के प्रमुख चार रूप देखने को मिल सकते हैं-
(1) माता-पिता एक-दूसरे को पर्याप्त और सन्तुलित प्रेम करते हों ।
(2) माता-पिता एक-दूसरे को बिल्कुल प्रेम न करते हों।
(3) माता पिता से अधिक प्रेम करती हो, परन्तु पिता न करता हो ।
(4) पिता माता से बहुत प्रेम करता हो, परन्तु माता न करती हो ।
उपर्युक्त परिस्थितियों में प्रथम परिस्थिति बालक के समाजीकरण के अनुकूल होती है क्योंकि पारिवारिक जीवन सुखी और सन्तुलित होता है, परन्तु अन्य तीनों परिस्थितियाँ परिवार का वातावरण कलहपूर्ण, असन्तोषजनक और असामाजिक बना देती हैं तथा बालक के विकास के लिए आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपलब्धियों, सहयोग और सन्तुलित व्यवहार का अभाव रहता है। ऐसी परिस्थिति में बालक सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध व्यवहार करेगा, संवेगात्मक दृष्टि से अपरिपक्व रहेगा और कुण्ठाओं का सामना करके मानसिक उलझन प्राप्त करेगा।
3. कुटुम्ब का परिवर्तन और समाजीकरण —
सामयिक परिस्थितियों के कारण कभी-कभी बालक को एक कुटुम्ब का त्याग करके दूसरे कुटुम्ब में जाना पड़ता है। सभी कुटुम्ब एक से नहीं होते। उनमें सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार बालक को दूसरे कुटुम्ब में जाते ही असन्तुलन का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः जब एक परिवार में कोई संरक्षक न रहे तो बालक अपने निकटवर्ती सम्बन्धी के घर रहने लगते हैं अथवा निःसन्तान दम्पत्ति किसी बालक को गोद ले लेते हैं अथवा पति के मरने पर कोई स्त्री अपने बालकों सहित किसी अन्य पुरुष के परिवार में जाकर रहने लगती है अथवा पुनर्विवाह कर लेती है तो बालक दूसरे परिवार में अपने आपको अनुकूलित करने में बाधा अनुभव करता है। शैशवावस्था में बालक अपने कुटुम्ब के वातावरण में धीरे-धीरे अनुकूलित हो जाता है, परन्तु बाल्यावस्था में उसे उस वातावरण में अनुकूलता प्राप्त करने में बाधा और कठिनाइयाँ आती हैं। बालक दूसरे परिवार में जाकर असन्तुलित व्यवहार पाता है। वह या तो अत्यधिक लाड़-प्यार पाता है या उपेक्षा। इस प्रकार दूसरा कुटुम्ब या असन्तुलित व्यवहार उस बालक के समाजीकरण में बाधक हो जाता है।
4. परिवार के सदस्यों का पारस्परिक सम्बन्ध और समाजीकरण —
जब बालक परिवार में आता है तो उसका सम्पर्क माता-पिता के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी होता है। बालक उनके व्यवहार से प्रभावित होकर अपना व्यवहार निश्चित करता है। परिवार के सदस्यों के मध्य रहकर ही सहयोग, प्रेम, स्नेह, स्पर्द्धा, त्याग, बन्धुत्व, दया, विनय, मैत्री जैसे सामाजिक गुण विकसित हुआ करते हैं। परिवार के बड़े-बूढ़े बालकों में आदर्श, सद्व्यवहार, सच्चरित्र, नैतिकता और धार्मिकता के भाव उत्पन्न करके उन्हें व्यवहार करने की प्रेरणा दिया करते हैं। यदि परिवार के सदस्य उत्तम स्वभाव और सदाचरण वाले नहीं होते तो बालकों पर उनके आचरण का बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है। इस प्रकार परिवार के सदस्यों का पारस्परिक सम्बन्ध बालकों के समाजीकरण की प्रक्रिया को भली प्रकार प्रभावित करता है।
5. पड़ोस, संगत और समाजीकरण —
परिवार और विद्यालय के अतिरिक्त बालक अपना समय पड़ौस और संगत में व्यतीत करता है। यदि बालक अच्छे पड़ौस और सुसंगत में रहता है तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसके समाजीकरण की प्रगति अच्छी दिशा में होती है, परन्तु बुरा पड़ौस और बुरी संगत मिलने पर बालक में असामाजिकता आने का भय बना रहेगा। वह बालक जो शराब पीने वालों, धूम्रपान करने वालों, जुआ खेलने वालों के पास उठता बैठता अथवा रहता है तो उसमें भी शराब पीने, धूम्रपान करने और जुआ खेलने की लत पड़ जाती है, परन्तु जो बालक धार्मिक संघों, सुसंगतों और अच्छे पड़ोस में रहता-खेलता है, उसका समाजीकरण अच्छा ही होता है।
6. सामाजिक उद्वेग और समाजीकरण —
बालक जैसे-जैसे बड़ा होता है, वह सामाजिक आदर्शों और मान्यताओं से परिचित होता जाता है। वह कोई ऐसा कार्य अथवा व्यवहार करना पसन्द नहीं करता जिसे करने में उसे निन्दा और अपमान का भागी बनना पड़े। यह भाव सामाजिक उद्वेग होता है जिसकी प्रेरणा से वह सदैव सामाजिक कार्य करने का ही प्रयास करता है। सामाजिक उद्वेग से प्रेरित व्यवहार की स्थिति सामान्यतः किशोरों में जिनकी आयु 12 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक होती है, पाई जाती है। किशोर किसी भी सामाजिक दण्ड जैसे शारीरिक दण्ड, निन्दा, आलोचना, डाँट-फटकार और सुविधाओं का छीना जाना आदि को प्राप्त नहीं करना चाहता। वह सदैव इसे अपमान ही समझता है। इसलिए किशोर सामाजिक उद्वेग से प्रेरित होकर वही कार्य करना अच्छा समझता है, जिससे उसे समाज में अपमानित न होना पड़े। इस प्रकार किशोरों के अनेक व्यवहार सामाजिक उद्वेग के कारण सामाजिक हो जाते हैं। किशोर को समाज भी शारीरिक दण्ड देने की अपेक्षा आलोचना, फटकार, सुविधाओं का अपहरण तथा निन्दा को महत्त्वपूर्ण समझता है। इन दण्ड व्यवस्थाओं से किशोर को मानसिक क्लेश होता है और वह असामाजिक कार्य करने से बचना चाहता है।
7. सामाजिक एवं आर्थिक स्तर और समाजीकरण —
समाज में व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक स्तरों में भिन्नता पाई जाती है। उच्च सामाजिक स्तर एवं उन्नत आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से सम्बन्धित होने वाले बालक आत्म-गौरव और प्रतिष्ठा के साथ जीवन व्यतीत करते हुए उच्च स्तर के लोगों के सम्पर्क में आते हैं। इस प्रकार के बालक उच्च स्तरीय सामाजिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। इन बालकों को स्वतः ही सामाजिक प्रतिष्ठा भी उपलब्ध हो जाती है, परन्तु वे बालक जिनके परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियाँ हीन होती हैं, समाज में आवश्यक प्रतिष्ठा का उपभोग नहीं करते। उनमें आत्महीनता का भाव आने से उनके समाजीकरण की गति बहुत ढीली हो जाती है। यद्यपि कुछ हीन आर्थिक स्तर एवं सामाजिक स्तर के बालक भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके हैं, परन्तु ऐसे उदाहरण अधिक नहीं हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना ही पड़ेगा कि सामाजिक एवं आर्थिक स्तर की भिन्नता के कारण बालक का समाजीकरण भी भिन्न-भिन्न गतियों से होता है।
8. धर्म एवं समाजीकरण
बालक समाज में रहते हुए किसी-न-किसी धर्म का अनुयायी अवश्य होता है और वह उसके अनुरूप धर्म-संघ से भी सम्बन्ध रखता है। धर्म-संघ बालक के समाजीकरण को प्रभावित करता है। धर्म व्यक्ति में विविध मान्यताओं, आदर्शों और परम्पराओं को निर्मित करता है जिनका करने पर ही व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक मान्यता मिलती है। हिन्दू परिवार में रहकर मांसाहार करना पाप है और नित्य स्नानादि करना आवश्यक है। यदि कोई हिन्दू बालक इन बातों पर ध्यान दिये बिना कोई आचरण करता है तो उसकी निन्दा होती है। यही बात अन्य धर्मावलम्बियों के बालकों के सम्बन्ध में कही जा सकती है जो अपने धर्मानुसार सामाजिक आचरण करने के लिए बाध्य होते हैं परिवार के बड़े-बूढ़े बालकों में धार्मिकता और नैतिकता लाने का प्रयास करते हैं जिससे बालक के समाजीकरण की प्रगति में सहयोग मिलता है।
9. संस्कृति और समाजीकरण —
संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत योग देती है। व्यक्तित्व का निर्माण समाजीकरण पर निर्भर होता है इसलिए संस्कृति को बालक के समाजीकरण का आधार माना जा सकता है। जिस “देश और जाति की जैसी संस्कृति होती है उस देश और जाति की वैसी ही परम्पराएँ, मान्यताएँ और
आदर्श होते हैं जिनका अनुपालन करने पर ही समाजीकरण होना सम्भव हो सकता है।
10. व्यक्तिगत सामर्थ्य और समाजीकरण —
एक ही संस्कृति, एक ही जाति, एक ही धर्म और समुदाय में रहते हुए और समान सुविधाओं का उपभोग करते हुए भी व्यक्तियों का समाजीकरण एक-सा नहीं होता। इसका कारण व्यक्ति की निजी योग्यताएँ, शक्तियाँ और संस्कार होते हैं। देखने में आता है कि एक ही माता-पिता के बालक जिनका विकास एक-ही से वातावरण में होता है, एक-ही सामाजिकता ग्रहण नहीं करते और न एक ही कक्षा तथा विद्यालय में समान शिक्षा-योग्यता प्राप्त करते हैं। इसका कारण उनकी व्यक्तिगत शक्तियों, योग्यताओं और संस्कारों की विभिन्नताएँ ही हैं। इसलिए सामर्थ्य और संस्कार समाजीकरण की गति में भेद उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत वैभिन्य को समाजीकरण का प्रभावकारी तत्त्व माना जा सकता है।
प्रश्न 2 (v) समाजीकरण की विधियों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर —
समाजीकरण में प्रयुक्त होने वाली चारों प्रक्रियाएँ सार रूप में विविध विधियों के अन्तर्गत न जाकर केवल ‘पुरस्कार विधि’ और ‘दण्ड विधि’ में ही समाविष्ट की जा सकती हैं।
समाजीकरण की पुरस्कार विधि —
व्यक्ति सामाजिक परम्पराओं, मान्यताओं और मूल्यों का अनुसरण करके समायोजित प्रतिक्रिया दिखाता है तो उसे आत्म-सन्तुष्टि होती है। यह आत्म-सन्तुष्टि ही व्यक्ति के विकास का स्रोत है। पुरस्कार चाहे वह भौतिक हो, सामाजिक हो अथवा आत्मिक, दण्ड से सर्वोत्तम होता है। भौतिक और सामाजिक पुरस्कार व्यक्ति को आध्यात्मिक पुरस्कार की ओर ले जाते हैं। भौतिक पुरस्कार में भौतिक पदार्थ जैसे रुपया-पैसा, उपयोगी वस्तु आदि आते हैं जिनके मोह में बालक सामाजिक आचरण करने लगता है। जब वह सामाजिक आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा होती है, उसे स्नेह मिलता है। यह प्रशंसा और स्नेह सामाजिक पुरस्कार होते हैं, परन्तु जब बालक किसी भी सामाजिक प्रतिक्रिया के दिखाने में आत्म-सन्तोष प्राप्त करने लगता है तो उसके लिए सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक पुरस्कार होता है। आध्यात्मिक पुरस्कार ही व्यक्ति में आत्मानुशासन उत्पन्न करता है। इसलिए पुरस्कार देते समय भौतिक पुरस्कार का न्यूनतम, सामाजिक पुरस्कार तथा आध्यात्मिक पुरस्कार का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। सभी श्रेष्ठ व्यक्ति आत्म-सन्तुष्टि के लिए ही समाज-कल्याण और परोपकार के कार्य करते हैं। यही भाव बालकों में उत्पन्न करना चाहिए। जब व्यक्ति भौतिक पदार्थ की कामना न करे, सामाजिक प्रशंसा की लालसा न रखे, वरन् एकमात्र आत्म-सन्तुष्टि के लिए ही सामाजिक हित के कार्य करे तो वह व्यक्ति के पूर्ण समाजीकरण की चरम स्थिति होगी। यह स्थिति प्राचीन भारत में सभी श्रेष्ठ पुरुष अपनाते थे
समाजीकरण की दण्ड विधि —
अनुशासन स्थापन और समाजीकरण में दण्ड-विधि बुरी होते हुए भी समयानुकूल व्यवहृत होती आई है। माता-पिता और गुरुजन समय-समय पर सीखने की भूल होने अथवा सामाजिक आचरण न करने पर कोई-न-कोई दण्ड अवश्य दे देते हैं। बालक में दण्ड का उद्देश्य बालक का आत्म-सुधार होना चाहिए और वह उसके अपराध के अनुरूप उसकी मात्रा, उसके प्रकार और अवसर को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए।
समाजीकरण के समय बालक समय-समय पर भूल कर बैठता है, परन्तु सभी भूलों के लिए दण्ड दिया जाए, यह उचित नहीं । वास्तव में दण्ड उन्हीं भूलों पर दिया जाना चाहिए जो बालक द्वारा अनजाने में न होकर जान-बूझकर की गई हों । दण्ड का तात्पर्य केवल शारीरिक दण्ड अथवा आर्थिक दण्ड से नहीं लगाना चाहिए। दण्ड भी सामाजिक और आध्यात्मिक होते हैं। इस प्रकार शारीरिक, भौतिक अथवा आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चार प्रकार के दण्डों में से आवश्यकता पड़ने पर केवल सामाजिक और आध्यात्मिक दण्डों की व्यवस्था की जानी चाहिए। शारीरिक और आर्थिक दण्ड – तो कदापि उपयोग में नहीं लाने चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े भी तो उन्हें कम-से-कम प्रयोग में लाया जाए। निन्दा, फटकार, आलोचना, झिड़कना, सुविधाओं का अपहरण जैसे सामाजिक दण्ड ठीक हैं जिन्हें सामाजिक अपराधों के लिए दिया जा सकता है।
यदि व्यक्ति किसी असामाजिक कार्य करने के बाद आत्म-ग्लानि अनुभव करके असामाजिक कृत्य
से घृणा करने लगे और पश्चाताप करने लगे तो यह दण्ड आध्यात्मिक होगा जिससे व्यक्ति में आत्म-सुधार और आत्मानुभूति होगी। वास्तव में दण्ड का विधान व्यक्ति को आत्मानुभूति का अवसर देकर आत्म-सुधार के लिए ही होना चाहिए। यदि अपराध के कारण और परिस्थिति का अध्ययन कर लिया जाए तो अपराधी की विवशता का ज्ञान हो सकता है जिससे अपराधी को आत्म-सुधार की ओर लाना सरल होगा।
पुरस्कार और दण्ड में सन्तुलन —
समाजीकरण में सजीवता और सार्थकता लाने के लिए केवल पुरस्कार का उपयोग करना अथवा केवल दण्ड को व्यवहार में लाना ठीक नहीं। इन दोनों विधियों में सामंजस्य लाया जाना आवश्यक है। अधिक पुरस्कार के कारण बालक लोभी और स्वाभाविक प्रेरणा से वंचित हो जाता है। इससे समाजीकरण की प्रक्रिया निर्जीव हो जाती है। इसी प्रकार अधिक दण्ड का उपयोग करने से उचित बात बताने पर भी बालक उसकी विपरीत प्रतिक्रिया करके विरोधी भावना ग्रहण कर लेता है। इसलिए परिवार के बड़े-बूढ़े, अध्यापक बालक के समाजीकरण में पुरस्कार और दण्ड का सन्तुलित प्रयोग करें। दोनों ही प्रकार से बालक का आत्म-सुधार करना है।
प्रश्न 2 (vi) लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
अथवा
समुदाय का अर्थ स्पष्ट करें। महिलाओं की अनौपचारिक शिक्षा में के कार्यों का उल्लेख करें।
अथवा
एक समुदाय की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जेण्डर के संदर्भ में समुदाय की भूमिका की विवेचना कीजिए।
ANSWER-
समुदाय का अर्थ —
जब किसी स्थान पर कुछ लोग स्थायी रूप से कुछ समय तक बने रहते हैं तो उनमें परस्पर सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, घनिष्ठता बढ़ जाती है, एकता की भावना आ जाती है और उनमें सहयोग और साहचर्य के भाव विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार के समूह को हम समुदाय का नाम दे सकते हैं और वह भावना जो उसके सदस्यों में पायी जाती है, सामुदायिक भावना कहलाती है। उदाहरणार्थ- किसी गाँव के सब लोगों से मिलकर एक समुदाय की रचना होती है।
|
वस्तुतः ‘समुदाय’ शब्द को अंग्रेजी में ‘Community’ कहते हैं। इस शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के दो शब्दों—’काम’ (Com) तथा ‘म्युनिस’ (Munis) से हुआ है। ‘Com’ का अर्थ है ‘एक साथ’ (Together) तथा ‘Muni’ का अर्थ है सेवा करना। इस प्रकार ‘समुदाय’ का शाब्दिक अर्थ एक साथ सेवा करना है। परन्तु समाजशास्त्र में इसका प्रयोग इस शाब्दिक अर्थ के रूप में नहीं किया जाता।
समाजशास्त्र में समुदाय का प्रयोग मुख्यतः दो अर्थों में किया जाता है— प्रथम भौगोलिक अर्थ में और द्वितीय सामाजिक-सांस्कृतिक अर्थ में। भौगोलिक अर्थ में यह निश्चित भू-भाग पर निवास करने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। सामाजिक-सांस्कृतिक अर्थ में यह एक ऐसा समूह है, जिसके सदस्यों में ‘सामुदायिक भावना’ पायी जाती है। इसी भावना के कारण समुदाय के सदस्य परस्पर सम्बन्धित ह्येते हैं और अपने समुदाय को अन्य समुदायों को अन्य समुदायों में पृथक् करते हैं।
समुदाय की परिभाषाएँ —
1. एच. सी. मैन्जर के अनुसार, “यह समाज जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, समुदाय कहलाता है।”
2. ई. एस. बोगार्ड्स के अनुसार, “समुदाय एक सामाजिक समूह होता है, जिसमें कुछ मात्रा में ‘हम भाव’ होता है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है।”
3. ग्रीन के अनुसार, “समुदाय संकुचित प्रादेशिक घेरे में रहने वाले लोगों का समूह सामान्य ढंग का जीवन जीते हैं।”
समुदाय शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण होने के कारण परिवार इत्यादि अनौपचारिक अभिकरणों की श्रेणी में भी आता है। समुदाय का प्रभाव उसके सदस्यों पर अत्यधिक प्रभावपूर्ण रहता है। समुदाय दण्डित करने, बहिष्कृत करने, सुधार करने की शक्तियाँ भी रखता है। । समुदाय की उन्नति उसके सदस्यों पर निर्भर करती है। अतः समुदाय बिना किसी भेदभाव के अपने सभी सदस्यों की उन्नति का प्रयास करता है। समुदाय लैंगिक मुद्दाँ, जिनमें स्त्री-पुरुष की समानता, स्त्री-शिक्षा, स्त्रियों की स्वतन्त्रता, अधिकार तथा सुरक्षा इत्यादि आते हैं, उस पर सजग रहकर इन बुराइयों को समाप्त कर सकता है। लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय की भूमिका का आकलन निम्नवत् है-
1. सामाजिक अनुशासन की स्थापना – लैंगिकता हेतु शिक्षा की प्रभाविता हेतु समुदाय
को सामाजिक अनुशासन की स्थापना करनी चाहिए, जिससे समुदाय के सभी सदस्य अनुशासन में रहते हुए समानता का व्यवहार करते हैं। सामाजिक अनुशासन के कारपा सामाजिक बुराइयों, दुर्व्यवहारी और असमानता का व्यवहार कम होता है जिससे समुदाय की उसके सदस्यों से की गयी आकांक्षायें मूर्त रूप ग्रहण करती हैं। इस प्रकार लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।
2. अन्य अभिकरणों से सहयोग-
समुदाय को चाहिए कि वह औपचारिक तथा अनौपचारिक सभी अभिकरणों से सहायता प्राप्त करे जिससे लैंगिक भेदभावों, दुर्व्यवहारों, असमानताओं की समाप्ति की शिक्षा प्रभावी बन सके। समुदाय या कोई भी अभिकरण भले ही वह सम्प्रभुतासम्पन्न राज्य ही क्यों न हो, यह कार्य अकेले नहीं कर सकते। अतः समुदाय को परिवार, विद्यालय, समाज तथा राज्य आदि से सहयोग प्राप्त कर लैंगिकता के समापन की शिक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।
3. स्त्रियों की उन्नति हेतु प्रयास—
लैंगिक भेदभावों को कम करने के लिए समुदाय स्त्रियों की सर्वतोन्मुखी उन्नति का प्रयास करना चाहिए। विभिन्न समुदायों में पृथक् व्यायामशाला, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, वाचनालय तथा मेलों इत्यादि में स्त्रियों को रचनात्मकता का स्थान दिया जाता है, जिससे स्त्रियों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक इत्यादि उन्नति हो रही है। इस प्रकार समुदाय स्त्रियों की समग्र उन्नति द्वारा उन्हें समान धारा में लाने का कार्य कर रहा है।
4. सामाजिक बुराइयों का अन्त-
लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय को चाहिए कि वह सामाजिक बुराइयों का अन्त करने के लिए दृढ़संकल्प रहे। सामाजिक बुराइयों जिसमें अन्धविश्वास, कुरीतियाँ, जड़ परम्परायें इत्यादि आती हैं, जिससे समाज गतिहीन हो जाता है। सामाजिक बुराइयाँ भेदभाव लाती हैं, वह जाति, लिंगादि आधारों पर होता है। समुदाय सामाजिक नियंत्रण प्रभावी रूप से करता है और समुदाय लैंगिकता की शिक्षा में अपनी भूमिका को तभी प्रभावी बना सकता है जब वह स्त्रियों और महिलाओं के प्रति व्याप्त संकीर्ण दृष्टिकोण और सामाजिक बुराइयों का अन्त करे। इस प्रकार समुदाय लैंगिकता की शिक्षा में प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है।
5. जागरूकता—
लैंगिकता की शिक्षा हेतु समुदाय को अपने सदस्यों में जागरूकता का संचार करना चाहिए। जागरूकता के कारण समुदाय में स्त्री-पुरुषों दोनों के प्रति समानता का भाव, स्त्री-शिक्षा का प्रचार-प्रसार, सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी, जिससे एक स्वस्थ समाज की स्थापना होगी। समुदाय की जागरूकता अत्यावश्यक है, किसी भी अच्छे कार्य के प्रसार हेतु, समानता तथा न्याय की स्थापना के लिए। इस प्रकार समुदाय अपने सदस्यों में जागरूकता लाकर लैंगिक भेदभावों की समाप्ति में प्रभावी भूमिका निर्वहन कर सकता है।
6. शिक्षा का प्रसार –
समुदाय का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वह शिक्षा का प्रसार करे, इस हेतु विद्यालयों की स्थापना और विशेषतः स्त्रियों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में लोकतांत्रिक आदर्शों तथा मूल्यों की स्थापना पर बल देना चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, स्त्रियों की व्यावसायिक उन्नति के प्रयास करने चाहिए। शिक्षा का प्रसार जैसे- जैसे होगा वैसे-वैसे स्त्रियों की भागीदारी और भूमिका सशक्त होती जायेगी। इस प्रकार समुदाय शिक्षा के प्रसार द्वारा लैंगिकता हेतु शिक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जब समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षित होगा तो स्त्रियों और बालिकाओं की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।
7. स्त्री-
शिक्षा का प्रसार समुदाय को विशेषतः स्त्री-शिक्षा के प्रसार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभ्य समुदाय का मानक वहाँ की शिक्षित स्त्रियाँ होती हैं। अतः स्त्री-शिक्षा के प्रसार हेतु बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्त्रियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करने से भी स्त्री-शिक्षा की उन्नति होगी, जिसका परिणाम लैंगिक भेदभावों में कमी के रूप में देखा जा सकता है।
8. स्त्रियों की शैक्षिक उन्नति हेतु विशेष प्रबन्ध –
समुदाय लैंगिकता हेतु शिक्षा में प्रभावी भूमिका निर्वहन स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्धों द्वारा कर सकता है, जैसे जिन घरों से बालिकायें पढ़ने नहीं जातीं, जिन घरों में निरक्षर महिलायें हैं, उन घरों में जाकर पढ़ाई के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए तथा स्त्रियों और बालिकाओं की शिक्षा को महत्त्वपूर्ण मानकर सामुदायिक सहयोग प्राप्त कर व्यक्तिगत प्रयासों में वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार समुदाय स्त्रियों की शैक्षिक उन्नति हेतु विशेष प्रबन्धों द्वारा लैंगिक दुर्भावनाओं को कम करने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है
9. व्यावसायिक शिक्षा पर बल समुदाय को चाहिए कि वह शिक्षा व्यवस्था को उपयोगिता और व्यवसाय आधारित बनाये, जिससे सामाजिक गतिशीलता आयेगी और गतिशील समाज में लैंगिक भेदभाव कम होंगे। व्यावसायिक शिक्षा का दूसरा लाभ यह है कि यह शिक्षा प्राप्त का स्त्रियाँ आत्मनिर्भर बनेंगी, जिससे वे पारिवारिक सरोकारों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति पुरुषों की भाँति कर सकेंगी। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा द्वारा लैंगिक भेदभावों में कमी तथा लैंगिकता की समानता के मुद्दे को प्रभावी बनाया जा सकता है।
10. लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास — समुदाय को अपनी परम्पराओं; मान्यताओं, रीति- रिवाजों और सम्पूर्ण ताने-बाने को लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित करना चाहिए। लोकतन्त्र में स्त्री- पुरुष सभी समान हैं और दोनों को ही स्वतन्त्रता प्राप्त है जिसमें स्त्रियों को धर्म, अभिव्यक्ति तथा शिक्षादि ग्रहण करने की स्वतन्त्रता प्राप्त है। इस प्रकार लोकतान्त्रिक मूल्यों के विकास द्वारा समुदाय स्त्री-पुरुषों में समानता का भाव लायेगा, जिससे लैंगिकता हेतु शिक्षा प्रभावी होगी।
प्रश्न 3 (i) लैंगिक असमता (विषमता) का अर्थ बताइए। इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए।
अथवा
लैंगिक असमता (असमानता) की संकल्पना बताइए। लैंगिक असमता के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
अथवा
लिंग असमता का अर्थ बताइए। लिंग असमता के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
ANSWER–
वर्तमान में लैंगिक असमता किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है बल्कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय हो गया है, क्योंकि आधुनिक समय में विश्व का आकार छोटा होता जा रहा है। वैश्वीकरण (Globalization) एवं उदारीकरण (Liberalization) की प्रक्रियाओं ने सभी राष्ट्रों की समस्याओं को एकबद्ध कर दिया है। अतः समाजशास्त्र जैसे विषय में लिंग सम्बन्धी असमता एवं समस्याओं का अध्ययन और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। यह विषय इस तथ्य पर बल देता है कि शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष तथा स्त्री के मध्य विद्यमान प्राकृतिक असमानताओं को तो स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार पर पुरुष तथा स्त्री में मतभेद करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा करना मानवता तथा मानव अधिकारों की धारणा के नितान्त विपरीत है। संयुकत राष्ट्र संघ के अनुसार पूरे विश्व में स्त्रियाँ यद्यपि विश्व जनसंख्या के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा सम्पूर्ण कार्य के दो-तिहाई भांग को पूरा करती हैं, परन्तु इनके पास विश्व की सम्पत्ति का केवल दसवाँ भाग ही है। विश्व बैंक के द्वारा प्रतिपादित सद्शासन के सिद्धान्त का भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में जोरदार प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है। विधि का शासन लिंग पर आधारित भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। यह कानून (विधि) के समक्ष सभी प्राणियों की समानता के विचार का समर्थन करता है।
लैंगिक असमता का अर्थ–
लिंग तथा लैंगिकता हेतु आंग्ल भाषा में Gender तथा Sex शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लिंग (Gender) का प्रयोग हम व्यक्तियों तथा आस-पास की वस्तुओं के नामों में भी प्रयुक्त करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य के दो रूप सृष्टि के समुचित परिचालन हेतु बनाये, जिसमें एक है स्त्री और दूसरा पुरुष। स्त्री तथा पुरुष ही अपनी प्रारम्भ अवस्था में बालिका और बालक से सम्बोधित किये जाते हैं। हमारे आस-पास के पर्यावरण में हम जो कुछ भी देखते हैं उसे किसी-न-किसी नाम से जानते हैं और इन नामों में ही उनका लिंग छुपा होता है।
पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग एक जैवकीय तथ्य है। यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड़ दी जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य बन जाता है जिसे लैंगिक असमता कहा जाता है। ‘लिंग’ (Gender) शब्द का प्रयोग पुरुषों तथा स्त्रियों के गुणों के कुलक तथा उनके समाज द्वारा उनसे अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान इन्हीं अपेक्षाओं से होती है ! ये अपेक्षाएँ इस विचार पर आधारित हैं कि कुछ गुण, व्यवहार, लक्षण, आवश्यकताएँ तथा भूमिकाएँ पुरुषों के लिए ‘प्राकृतिक’ हैं, जबकि कुछ अन्य गुण एवं भूमिकाएँ स्त्रियों के लिए प्राकृतिक हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि लिंग केवल जैवकीय नहीं है क्योंकि लड़का या लड़की जन्म के समय यह नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, क्या सोचना है अथवा किस प्रकार से प्रतिक्रिया करनी है। प्रत्येक समाज में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के रूप में उनकी लैंगिक पहचान तथा सामाजिक भूमिकाएँ समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से निश्चित की जाती हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा उन्हें उन सांस्कृतिक अपेक्षाओं का ज्ञान दिया जाता है जिनके अनुसार उन्हें व्यवहार करना है। ये सामाजिक भूमिकाएँ एवं अपेक्षाएँ एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में अथवा एक ही समाज के भिन्न युगों में भिन्न- भिन्न होती हैं।
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि लिंग असमता वर्तमान समय में जीवन का सार्वभौमिक तत्त्व बन गया है। विश्व के अनेक समाजों में, विशेषकर विकासशील देशों में, स्त्रियों के साथ समाज में प्रचलित विभिन्न कानूनों, रूढ़िगत नियमों के आधार पर विभेद किया जाता है तथा उनको पुरुषों के समान राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। स्त्री या फेमिनिस्ट विद्वानों के अनुसार लैंगिक असमता को स्त्री-पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन तथा स्त्री-पुरुष के मध्य असमान सम्बन्धों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है |
लैंगिक असमता के प्रकार अथवा रूप —
प्रत्येक समाज में लैंगिक असमता अनेक रूपों में विद्यमान रहती है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के अनुसार, “लैंगिक असमता विश्व के सभी देशों— जापान से जाम्बिया, यूक्रेन से संयुक्त राज्य अमेरिका-में पाई जाती है, परन्तु पुरुषों एवं स्त्रियों में असमता अनेक रूपों में होती है। यह एक सजातीय प्रघटना न होकर अनेक अन्तर्सम्बन्धित समस्याओं से जुड़ी प्रघटना है।” लैंगिक असमता के निम्नलिखित प्रकार हैं-
(1) मर्त्यता असमता-विश्व के अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों एवं पुरुषों में असमता का एक बर्बर प्रकार सामान्यतया स्त्रियों की उच्च मर्त्यता दर में परिलक्षित होता है, जिसके परिणामस्वरूप कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है। मर्त्यता असमता अत्यधिक मात्रा में उत्तरी अफ्रीका तथा एशिया (चीन एवं दक्षिण एशिया सहित) में देखी जा सकती है
(2) घरेलू असमता-परिवार अथवा घर के अन्दर ही लैंगिक सम्बन्धों में अनेक प्रकार की मौलिक असमानताएँ पाई जाती हैं। घर की सम्पूर्ण देख-रेख से लेकर बच्चों के पालन-पोषण का पूरा दायित्व महिलाओं का होता है। अधिकांश देशों में पुरुष इन कार्यों में स्त्रियों की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करते हैं। पुरुषों का कार्य घर से बाहर काम करना माना जाता है। यह एक ऐसा श्रम- विभाजन है जो स्त्रियों को पुरुषों के अधीन कर देता है।
(3) मौलिक सुविधा असमता-मौलिक सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक देशों में पुरुषों एवं स्त्रियों में असमता स्पष्टतया देखी जा सकती है। कुछ वर्ष पहले तक अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर पाबन्दी थी। एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों के साथ-साथ लैटिन अमेरिका में लड़कियों को लड़कों की तुलना में शिक्षा सुविधाएँ बहुत कम उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य मौलिक सुविधाओं के अभाव के कारण स्त्रियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाते हैं और न ही वे समुदाय में अनेक कार्यक्रमों में सहभागिता कर सकती हैं।
(4) प्रासूतिक असमता – गर्भ में ही बच्चे के लिंग को ज्ञात करने सम्बन्धी आधुनिक तरीकों की उपलब्धता ने लैंगिक असमता के इस रूप को जन्म दिया है। लिंग परीक्षण द्वारा यह पता लगाकर कि होने वाला शिशु लड़की है, गर्भपात करा दिया जाता है। अनेक देशों में, विशेष रूप से पूर्व एशिया, चीन एवं दक्षिण कोरिया में, साथ-ही-साथ सिंगापुर तथा ताइवान के अतिरिक्त भारत एवं दक्षिण एशिया में भी यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह उच्च तकनीकी पर आधारित असमता है।
(5) विशेष अवसर असमता – यूरोप तथा अमेरिका जैसे अत्यधिक विकसित एवं अमीर देशों के साथ-साथ अधिकांश अन्य देशों में उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण में लैंगिक पक्षपात स्पष्टतया देखा जा सकता है।
(6) व्यावसायिक असमता-व्यावसायिक असमता भी लगभग सभी समाजों में पाई जाती है। जापान जैसे देश में, जहाँ जनसंख्या को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं अन्य सभी प्रकार की मौलिक तुलना सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ पर भी रोजगार एवं व्यवसाय प्राप्त करना स्त्रियों के लिए पुरुषों की मैं काफी कठिन कार्य माना जाता है।
(7) स्वामित्व असमता – अनेक समाजों में सम्पत्ति पर स्वामित्व भी पुरुषों एवं स्त्रियों में असमान रूप से वितरित है। मौलिक घरेलू एवं भूमि सम्बन्धी स्वामित्व में भी स्त्रियाँ पुरुषों की तुलना में काफी पिछड़ी हुई हैं। इसी के परिणामस्वरूप स्त्रियाँ वाणिज्यकीय, आर्थिक तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं से वंचित रह जाती हैं।
प्रश्न 3 (ii) लैंगिक असमता (असमानता) क्या है? भारत में लैंगिक असमता के कारण एवं सुझावों का वर्णन कीजिए।
अथवा
भारत में लैंगिक असमता किस रूप में पायी जाती है? व्याख्या कीजिए।
अथवा
लैंगिक असमानता क्या है? समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को स्पष्ट कीजिए।
ANSWER-
पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग एक जैवकीय तथ्य है। यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड़ दी जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य बन जाता है जिसे लैंगिक असमता कहा जाता है। ‘लिंग’ (Gender) शब्द का प्रयोग पुरुषों तथा स्त्रियों के गुणों के कुलक तथा उनके समाज द्वारा उनसे अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान इन्हीं अपेक्षाओं से होती है। ये अपेक्षाएँ इस विचार पर आधारित हैं कि कुछ गुण, व्यवहार, लक्षण, आवश्यकताएँ तथा भूमिकाएँ पुरुषों के लिए ‘प्राकृतिक’ हैं, जबकि कुछ अन्य गुण एवं भूमिकाएँ स्त्रियों के लिए प्राकृतिक हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि लिंग केवल जैवकीय नहीं है क्योंकि लड़का या लड़की जन्म के समय यह नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, क्या सोचना है अथवा किस प्रकार से प्रतिक्रिया करनी है। प्रत्येक समाज में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के रूप में उनकी लैंगिक पहचान तथा सामाजिक भूमिकाएँ समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से निश्चित की जाती हैं।
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाएँ एवं संस्थाएँ उन मूल्य व्यवस्थाओं एवं सांस्कृतिक नियमों द्वारा सुदृढ़ होती हैं, जो स्त्रियों की हीन भावना की धारणा को प्रचारित करती हैं। प्रत्येक संस्कृति में अनेक प्रथाओं के ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं, जो स्त्रियों को दिए जाने वाले निम्न मूल्य व स्थिति को परिलक्षित करते हैं। पितृसत्तात्मकता स्त्रियों को अनेक प्रकार से शक्तिहीन बना देती है। इनमें स्त्रियों के पुरुषों की तुलना में निम्न होने, उन्हें साधनों तक पहुँचने से रोकना तथा निर्णय लेने वाले पदों में सहभागिता को सीमित करने जैसी परिस्थितियाँ प्रमुख हैं। नियन्त्रण के यह स्वरूप स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं से दूर रखने में सहायता प्रदान करते हैं। स्त्रियों की अधीनता, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति (जैसे उनके स्वास्थ्य, आय एवं शिक्षा का स्तर) तथा उनके पद अथवा स्वायत्तता एवं अपने जीवन पर नियन्त्रण के अंश के रूप में देखी जा सकती है।
भारत में लैंगिक असमता
भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पुरुष प्रधान एवं पितृसत्तात्मक समाज है। इसमें अन्य सभी समाजों की तरह जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों एवं स्त्रियों में लैंगिक असमता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अतः भारत में स्त्रियों एवं पुरुषों में लैंगिक असमता निम्नलिखित रूपों में देखी जा सकती है-
(1) लिंग-भेदभाव – प्रत्येक पितृसत्तात्मक परिवार का यह सामान्य लक्षण है कि वहाँ पुरुष की प्रधानता होती है और स्त्री का अवमूल्यन होता है। भारतीय समाज में इसका रूप अत्यन्त कठोर है। लड़की का जन्म ही अपने में अभिशाप है। पुत्र मुक्तिदाता, बुढ़ापे का सहारा और घर की पूँजी है, हो जाता है। जबकि पुत्री का जन्म एक दायित्व और कर्जा है। इसलिए जन्म से ही लिंग-भेदभाव शुरू इनके लालन-पालन के तौर-तरीके बिल्कुल अलग-अलग हैं। के.एम. पणिक्कर (K.M. Panikkar) ने स्पष्ट लिखा है कि हिन्दू सामाजिक जीवन की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक हिन्दू संयुक्त परिवार में स्त्री को प्रदान की जाने वाली प्रस्थिति है। आधारभूत रूप से हिन्दू सामाजिक व्यवस्था यह मानकर चलती है कि पुत्री परिवार का भाग नहीं है। वह तो एक ऐसा आभूषण है जो गिरवी रखा है और जब उसका कानूनी मालिक आएगा और उसकी माँग करेगा, तो उसे दे दिया जाएगा। ‘यास्क निरुक्त’ लेकर कन्या में स्पष्ट घोषणा है कि लड़की तो अन्य को दी जाती है। देने के तीन तरीके हैं—दान, विक्रय तथा उत्सर्ग। दान विवाह के समय कन्यादान के रूप में होता है, विक्रय से आशय वधू-मूल्य बेचना है जबकि उत्सर्ग का आशय उसे त्याग देना है, जैसे—मन्दिर में देवदासी के रूप में देवी या देवता के चरणों में समर्पित कर देना। ईसाइयों में वे मठ में एक नन के रूप में रहती हैं। ऐसी स्थिति में नारी का लालन-पालन कैसे होता होगा, वह तो अपने आप ही स्पष्ट है।
(2) स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सुविधाओं में असमता-
स्त्रियों के अस्वास्थ्य और कुपोषण की भी भारी समस्या है। बचपन से ही लड़कियों को वह पोषक पदार्थ नहीं दिए जाते जो लड़कों को दिए जाते हैं। वे स्वयं ही अपने शरीर की रक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत कम ध्यान देती हैं। प्रायः घर में वही स्त्री, जो अपने पति और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा भोजन बनाती हैं, बाद में जो बच जाता है उसे खाती हैं और अगर बासी भोजन रखा है तो पहले उसे खाती हैं। मातृत्व का भार भी उस पर सबसे ज्यादा है। शारीरिक व्यायाम की तो उन्हें शिक्षा ही नहीं दी जाती। ज्यादातर उनमें खून की कमी रहती है। एक ओर गरीब निर्धन स्त्रियों को तो उचित चिकित्सा एवं पोषण मिलना ही दुश्वार है तो, दूसरी ओर, धनी स्त्रियों के लिए समस्या इससे उल्टी है। वहाँ अत्यधिक दवाइयों का सेवन या आलसी जीवन एक समस्या बन गया है।
यहाँ परिवार नियोजन की दृष्टि से भी इस बात पर जोर दिया जाना जरूरी है कि हमारे समाज में परिवार नियोजन का प्रमुख लक्ष्य स्त्रियों को ही बनाया गया है। विदेशों में जो जन्म-निरोध के तरीके खतरनाक घोषित किए जा चुके हैं, वे भी यहाँ चलाए जा रहे हैं। यदि हम नसबन्दी या बन्ध्याकरण के आँकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि स्त्री बन्ध्याकरण का प्रतिशत कहीं ज्यादा ऊँचा है। लूप लगवाने से रक्त स्राव बढ़ जाता है और कभी-कभी गर्भाशय में अनेक रोग पैदा हो जाते हैं, परन्तु फिर भी स्त्री ही इन तरीकों का इस्तेमाल करती है। इसी तरह, गर्भ निरोधक गोलियों का लगातार सेवन बहुत हानिकारक है। अब एक नया इंजेक्शन आविष्कृत हुआ है जो गर्भ निरोध करने में समर्थ है।
(3) शिक्षा में असमता अथवा विषमता-प्रारम्भिक वैदिक साहित्य से हमें यह पता चलता है कि वैदिक युग में लड़की का भी उपनयन संस्कार होता था और वह भी लड़कों की भाँति आश्रमों में शिक्षा के लिए जाती थी। धीरे-धीरे उसे शिक्षा से दूर किया जाता रहा और उसके लिए एकमात्र संस्कार विवाह ही माना जाने लगा। धर्मशास्त्रों तक आते-आते यह प्रक्रिया पूरी हो गई। मुस्लिम काल में तो स्त्री पूर्णतः निरक्षर थी। नई दिल्ली स्थित ‘भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्’ (ICSSR) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि 1971 ई. में साक्षर स्त्रियाँ 18.4 प्रतिशत थीं, 1981 ई. में यह प्रतिशत 25 था, जबकि 1991 ई. तथा 2001 ई. की जनगणनाओं के ANKARसार यह क्रमश: 39.42 तथा 54.16 प्रतिशत हो गया है। वास्तव में, यह प्रगति नगरीय क्षेत्रों में के बीच अधिक हुई हैं।
(4) रोजगार में असमता अथवा विषमता-
1981 ई. की जनगणना के अनुसार स्त्री श्रम सहभागिता 20.85 प्रतिशत थी। 1991 ई. में भी इसमें कोई विशेष उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में, स्त्री श्रम की भी अजब कहानी है। उसको गृहस्थी का कार्य, जो वह प्राय, सबसे पहले उठकर प्रारम्भ करती है और देर रात तक समाप्त करती है, अनुत्पादक माना जाता है। वह कार्य राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता। जो वह घर से बाहर तथा कथित उत्पादक कार्यों में लगी है वहाँ भी वह निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रही है-
(i) कृषि क्षेत्र में, जहाँ कि 80 प्रतिशत स्त्रियाँ काम कर रही हैं, स्त्री श्रम को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है तथा वहाँ भी वे असंगठित हैं और मौसमी रोजगार के उच्चावचन से पीड़ित हैं।
(ii) घरेलू उद्योगों; जैसे अगरबत्ती, बीड़ी या दियासलाई बनाना, चटाई बनाना, पापड़ उद्योग, आदि में न तो रोजगार की सुरक्षा है और न निश्चित दर पर मजदूरी है। वहाँ के काम के घण्टे अधिक हैं और श्रम कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, वहाँ उनके यौन शोषण का भी भय बना रहता है।
(5) दहेज के कारण उत्पीड़न- भारतीय समाज में स्त्री के लिए विवाह में दहेज अनिवार्य है। इसलिए दहेज की समस्या एक भयंकर समस्या बनती जा रही है। आए दिन समाचार-पत्रों में दहेज की शिकार अभागी स्त्रियों के जलाने की घटनाओं का विवरण छपा होता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है और दहेज का समाज के प्रत्येक समुदाय में प्रसार भी होता जा रहा है। इसके विरुद्ध हाल ही में कठोर कानून भी बनाए गए हैं, पर पति के परिवार में अकेली स्त्री क्या करे? पिता या भाई भी कब तक विवाहित बेटी या बहन को अपने घर पर रखें। कहीं-कहीं आर्थिक कठिनाई उन्हें मजबूर करती है कि वे उसे पति के घर वापस भेज दें और कहीं-कहीं सामाजिक निन्दा उन्हें मजबूर करती है कि वे बेटी के लालची ससुराल वालों के साथ समझौता करने का प्रयत्न करते रहें। परिणाम अभागी स्त्री की मृत्यु ही होता है। यह कुप्रथा तभी समाप्त की जा सकती है जब इसके विरुद्ध युवा लड़के-लड़कियों में एक जागरण अभियान चलाया जाए। लड़कियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाया जाए और उनमें यह संकल्प जाग उठे कि वे ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेंगी जो दहेज की माँग करता है। गाँधीजी ने कहा था कि “विवाह तो पारस्परिक प्रेम व सहमति पर आधारित होना चाहिए, न कि दहेज पर आधारित हृदयहीन विवाह। उनकी राय में लड़कियों का अविवाहित रह जाना अच्छा है बनिस्बत उन पुरुषों के साथ विवाह करना, जो दहेज की माँग करते हैं।”
(6) तलाक का उत्पीड़न – पति-पत्नी के वैवाहिक सम्बन्धों का कानूनी दृष्टि से विच्छेद किया जाना तलाक है। तलाक के विभिन्न समुदायों में भिन्न-भिन्न आधार हैं, परन्तु तलाक स्त्री के लिए पुरुषों की अपेक्षा अधिक कष्टकारी और आघातपूर्ण घटना है। अदालत की लम्बी प्रक्रिया, बच्चों का प्रश्न, स्वयं के जीवन निर्वाह का प्रश्न, सामाजिक अप्रतिष्ठा और निन्दा का सामना – यह सब स्त्री को भुगतना पड़ता है, पुरुष को नहीं। तलाक प्राप्त स्त्री भारतीय समाज में अप्रतिष्ठा का विषय है और उसके पुनर्विवाह की समस्या भी कठिन है। इसलिए स्त्री के लिए तलाक एक महँगा सौदा है। परन्तु ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आ जाती हैं; जैसे पति द्वारा क्रूर यातना दिया जाना, उसका व्यभिचार लिप्त होना या घर छोड़कर कहीं चले जाना, आदि जो तलाक को ही एकमात्र हल के रूप में प्रस्तुत करती हैं। इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि स्त्रियों की पारस्परिक सहायता, स्त्री संगठनों का सहयोग और स्त्री की आर्थिक स्वतन्त्रता ही उसे तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिला सकती है।
(7) स्त्रियों के प्रति हिंसा-स्त्री अनेक रूपों में आज हिंसा का शिकार है। यह हिंसा दो रूपों में देखी जा सकती है—प्रथम, घरेलू हिंसा तथा द्वितीय, घर से बाहर हिंसा। पहले रूप का सम्बन्ध घर-गृहस्थी में स्त्री का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। विवाह के समय स्त्री सुनहरे स्वप्न देखती है कि अब प्रेम, शान्ति व आत्म-उपलब्धि का जीवन प्रारम्भ होगा, परन्तु इसके विपरीत सैकड़ों विवाहित स्त्रियों के यह सपने क्रूरता से टूट जाते हैं। वे पति द्वारा मार-पीट और यातना की अन्तहीन लम्बी अँधेरी गुफाओं में अपने आपको पाती हैं जहाँ उनकी चीख-पुकार सुनने वाला कोई नहीं। दुःख तो यह है कि ऐसी मार-पीट का जिक्र करने में भी उन्हें लज्जा अनुभव है और यदि वे शिकायत भी करें तो खुद उन्हें ही दोषी माना जाता है या उन्हें भाग्य के सहारे चुपचाप सहने की सलाह दी जाती है।
(8) यौन-शोषण तथा उत्पीड़न — पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति के परिणामस्वरूप उनकी सबसे प्रमुख समस्या उनका यौन शोषण और यौन उत्पीड़न है। जैसे- वेश्यावृत्ति, देवदासी, अश्लील चित्र, विज्ञापन, चलचित्र, कैबरे नृत्य तथा छेड़छाड़ आदि ।
(9) महिला हत्या—स्त्री हत्या वह हत्या कही जा सकती है जो उस समय हो जबकि वह माँ के गर्भ में है या जन्म लेने के बाद स्त्री-शिशु हत्या के रूप में है और चाहे जलती बहू या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न से मारने के रूप में है। इतना ही नहीं. इसमें ऐसी घटनाएँ भी शामिल हैं जिनमें ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी गई हों कि स्त्री ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली हो। ऐसी घटनाएँ स्त्री के उत्पीड़न की बड़ी दर्दनाक कहानियाँ प्रस्तुत करती हैं और वे इक्का-दुक्का घटनाएँ नहीं हैं कि जिन्हें अपवाद समझकर टाल दिया जाए। यह तो एक राष्ट्रीय खोज का विषय है।
लैंगिक असमानता को कम करने हेतु सुझाव
लैंगिक असमानता एवं महिला संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं—
(1) मातृत्व का मौलिक अधिकार —
प्रत्येक स्त्री को मातृत्व का मौलिक अधिकार मिले, चाहे वह विवाहित दायरे में हो या उससे बाहर। यह उसका नैसर्गिक अधिकार है, इसे संवैधानिक किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, उसे निरपेक्ष रूप से दैहिक अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। उसकी देह पर उसे ही स्वामित्व मिले। किसी अन्य को, चाहे वह कोई भी हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध स्त्री के दैहिक उपयोग का अधिकार नहीं है।
समुदाय
(2) वैधानिक सुधार- स्त्री संगठनों की सहभागिता व सलाह से स्त्री सम्बन्धी एक भारतीय स्त्री अधिनियम पारित हो जो विवाह, उत्तराधिकार, सम्पत्ति, यौन, सन्तानोत्पत्ति आदि विषयों पर स्पष्ट आदेश प्रदान करें। भारत की प्रत्येक वयस्क स्त्री को यह अधिकार दिया जाए कि वह बिना धर्म, जाति, के भेदभाव के अपने लिए इस अधिनियम को ग्रहण कर सकती है, इसका लाभ उठा सकती है।
(3) स्त्री-शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार – स्त्री-शिक्षा न केवल अनिवार्य की जाए वरन् निर्धन परिवारों की कन्याओं को छात्रवृत्तियाँ भी दी जाएँ। स्त्री छात्रावासों की व्यवस्था की जाए। इस शिक्षा का आधुनिक अर्थों में व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए। स्कूलों के साथ ही एक उत्पादन केन्द्र भी हो तो और भी अच्छा है। स्त्री-शिक्षा का उद्देश्य स्त्री को आर्थिक रूप में आत्म-निर्भर बनाना होना चाहिए।
(4) रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन — स्त्रियों में अधिक-से-अधिक रोजगार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को आरक्षण व सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति अपनानी चाहिए। स्त्रियों को वे सब सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों व जनजातियों को मिल रही हैं।
(5) महिला संगठन को प्रोत्साहन एवं सहायता – स्त्रियों को स्थानीय स्तर पर अपने संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनके संगठनों को सहायता दी जानी चाहिए।
(6) महिला सशक्तिकरण – लैंगिक असमता को दूर करने के लिए स्त्री सशक्तिकरण एक सबल उपाय माना जाता है। आज सभी राष्ट्रों में इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
वर्ष 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ‘महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव समाप्ति से सम्बद्ध घोषणा’ एवं सदस्य देशों में अपने देशों की महिला प्रस्थिति पर प्रतिवेदन की अनुशंसा पर वर्ष 1971 में भारत सरकार की समाज कल्याण राज्यमन्त्री फूलरेणु गुहा के नेतृत्व में ‘भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति’ (सीएसडब्ल्यूआई) का गठन किया गया है। इस समिति ने वर्ष 1974 में अपने प्रतिवेदन ‘टुवार्ड्स इक्वालिटी’ सरकार को प्रस्तुत किया।
प्रश्न 3 (iii) विद्यालय से आप क्या समझते हैं? समाज के लिए विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्त्व का वर्णन कीजिए।
अथवा
विद्यालय का अर्थ बताइए। समाज में विद्यालय के स्थान की व्याख्या कीजिए।
ANSWER–
विद्यालय का अर्थ —
‘स्कूल’ शब्द की उत्पत्ति ‘Schola’ या ‘Skhole’ नामक यूनानी शब्द से हुई, जिसका अर्थ है—’अवकाश’ (Leisure)। यह बात कुछ विचित्र-सी जान पड़ती है। इसका स्पष्टीकरण करते ए.एफ. लीच ने लिखा है- “वाद-विवाद या वार्ता के स्थान, जहाँ एथेन्स के युवक अपने अवकाश के समय को खेल-कूद, व्यबसाय और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे, धीरे-धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गये। एकेडेमी के सुन्दर उद्यानों में व्यतीत किये जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ।”
विद्यालय की परिभाषा —
विद्यालय की परिभाषा विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों ने निम्न रूप में दी है-
टी.पी. नन के अनुसार — “विद्यालय को मुख्य रूप से इस प्रकार का स्थान नहीं समझा जाना चाहिए, जहाँ किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, वरन् ऐसा स्थान जहाँ बालकों को क्रियाओं के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है, जो इस विशाल संसार में सबसे महान् और सबसे अधिक महत्त्व वाली हैं।”
रॉस के अनुसार — “विद्यालय वे संस्थाएँ हैं, जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सहायता मिले।” जॉन ड्यूवी के अनुसार – “विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है, जहाँ जीवन के कुछ गुम्नों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो।”
विद्यालय की विशेषताएँ —
विद्यालय की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—
(i) विद्यालय को बालकों के भावी जीवन की तैयारी के हेतु स्थापित किया जाता है।
(ii) विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केन्द्रबिन्दु होना चाहिए।
(iii) विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जिसमें बालकों के वांछित विकास के लिए विशिष्ट गुणों, क्रियाओं तथा व्यवसायों की व्यवस्था की जाती है।
(iv) विद्यालय वह स्थान है जहाँ संसार की महान् एवं महत्त्वपूर्ण क्रियाओं को स्थान दिया जाता है।
(v) विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। ऐसा विचार जनतंत्र में पाया जाता है और समाज की सभी क्रियाएँ विद्यालय में ही करायी जाती हैं जिसमें सभी छात्र भाग लेते हैं। डीवी महोदय ने कहा भी है, “प्रजाति की सामाजिक चेतना में व्यक्ति के भाग लेने से ही सारी शिक्षा आगे बढ़ती है।’
(vi) विद्यालय का वातावरण विशेष ढंग का होता है। विद्यालय का वातावरण छात्र, अध्यापक, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संग्रहालय, क्रीड़ास्थल आदि के कारण विशेष रूप का होता है। डीवी ने ऐसे वातावरण को सरलीकृत, शुद्ध और सन्तुलित रूप में होना बताया है। ऐसा वातावरण संकीर्णताओं से दूर होता है। बालकों का दृष्टिकोण व्यापक होता है।
समाज में विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्त्व —
समाज में विद्यालय का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए निम्नलिखित कारण हैं-
(1) विशाल सांस्कृतिक विरासत-आज की सांस्कृतिक विरासत बहुत विशाल हो गई है। इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान, कुशलताओं और कार्य करने की विधियों का समावेश हो गया है। ऐसी विरासत की शिक्षा देने में व्यक्ति अपने को असमर्थ पाते हैं। अतः उन्होंने यह कार्य विद्यालय को सौंप दिया।
(2) जीवन की जटिलता—
आज का जीवन प्राचीन काल के जीवन के समान सरल और सुखमय नहीं है। उस समय मनुष्य के पास अपनी सब आवश्यकताओं के स्वयं पूर्ण करने और अपने बच्चों की शिक्षा की स्वयं देखभाल करने के लिए समय था। आज जनसंख्या की वृद्धि, आवश्यकताओं की अधिकता और वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य के कारण जीवन बहुत कठिन हो गया अपने कार्यों से इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा की देखभाल कर सके इसलिए उसने यह कार्य विद्यालय को सौंप दिया है।
(3) व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास-घर, समाज, धर्म आदि शिक्षा के अच्छे साधन हैं। पर इनका न तो कोई निश्चित उद्देश्य होता है और न पूर्व-नियोजित कार्यक्रम। फलतः कभी-कभी बालक के व्यक्तित्व पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत, विद्यालय का एक निश्चित उद्देश्य और पूर्व-नियोजित कार्यक्रम होता है। परिणामस्वरूप, इसका बालक पर व्यवस्थित रूप में प्रभाव पड़ता है और उसके व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है।
(4) समाज की निरंतरता व विकास- ‘विद्यालय’ एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक होने के कारण विद्यालय सामुदायिक जीवन का वह स्वरूप है, जिसमें समाज की निरन्तरता और विकास के लिए सभी प्रभावपूर्ण साधन केन्द्रित होते हैं। विद्यालय के इसी महत्त्व के कारण टी.पी. नन (T.P.Nunn) ने लिखा है- “विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन् समस्त मानव-समाज का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। ”
(5) विद्यालय घर की अपेक्षा उत्तम साधन है— ‘विद्यालय’ घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान है। कारण यह है कि विद्यालय में विभिन्न आदतों, रुचियों और दृष्टिकोणों के बालक आने हैं। अतः परस्पर सम्पर्क के कारण बालक उन बातों को सीखते हैं, जिन्हें वे घर की चारदीवारी के अन्दर नहीं सीख सकते हैं। यदि बालकों को संसार के ढंगों से परिचित कराना है, यदि उनको सामाजिक शिष्टाचार और सहानुभूति सिखानी है, यदि उनको निष्पक्षता और सहयोग के महत्त्व को बताना है, तो उनको घर से बाहर विद्यालय में भेजना अनिवार्य है।
(6) शिक्षित नागरिकों का निर्माण-विद्यालय ही एकमात्र वह साधन है, जिसके द्वारा शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। यदि एक देश के समस्त बालकों को एक निश्चित आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, तो वे स्थायी रूप से साक्षर हो जाते हैं। साक्षर होने के साथ-साथ उनमें धैर्य, सहयोग, उत्तरदायित्व आदि गुणों का विकास होता है। इस प्रकार, बड़े होकर बालक राज्य के उपयोगी नागरिक सिद्ध होते हैं।
(7) घर व विश्व को जोड़ने वाली कड़ी-बालक की शिक्षा में घर का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। घर में रहकर वह अनुशासन, सेवा, सहानुभूति, निःस्वार्थता आदि गुणों को सीखता है। पर घर की चारदीवारी में बँधे रहने के कारण उनके ये गुण अपने परिवार के व्यक्तियों तक ही सीमित रहते हैं। फलतः उसका दृष्टिकोण संकुचित होता है। विद्यालय में विभिन्न वर्गों और सम्प्रदायों के बालकों के सम्पर्क में आकर उसका दृष्टिकोण विस्तृत होता है। साथ ही बाह्य समाज से उसका सम्पर्क स्थापित हो जाता है। इस प्रकार ‘विद्यालय’ घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। रेमॉण्ट का कथन है— “विद्यालय बाह्य जीवन के बीच की अर्द्धपारिवारिक कड़ी है जो बालक की उस समय प्रतीक्षा करती है, जब वह अपने माता-पिता की छत्रच्छाया को छोड़ता है।”
इकाई – II
प्रश्न 4 (i) शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय का वर्णन कीजिए।
अथवा
विद्यालय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। विद्यालय के कार्यों का वर्णन कीजिए।
अथवा
“विद्यालय एक प्रमुख शिक्षा संस्था है।” व्याख्या कीजिए। आज के परिप्रेक्ष्य में उसके महत्त्वपूर्ण कार्यों की विवेचना कीजिए।
अथवा
शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय के अर्थ एवं महत्त्व की व्याख्या कीजिए।
ANSWER–
‘विद्यालय’ शब्द दो शब्दों ‘विद्या’ और ‘आलय’ से बना है, जिसका अर्थ है ‘विद्या का घर’ या ‘विद्या का स्थान’ अर्थात् वह स्थान जहाँ विद्या ग्रहण की जाय। अंग्रेजी शब्द School (स्कूल) के उद्भव का सही पता नहीं चलता है। परन्तु यूनानी शब्द Scole तथा लैटिन शब्द Skole से इस बात का संकेत मिलता है कि स्कूल शब्द सम्भवतः इन्हीं शब्दों से सम्बन्धित रहा होगा। यूनानी शब्द ‘स्कोल’ का अर्थ ‘अवकाश’ होता है, इससे यह ध्वनित होता है कि एक स्थान विशेष पर लोग अवकाश में आते थे और उसका प्रयोग ज्ञानार्जन आदि से होता था। इस सन्दर्भ में स्कूल ‘अवकाशालय’ कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।
विद्यालय का अर्थ संस्था के रूप में ही लिया जाना चाहिए। संस्था होने के नाते विद्यालय का अर्थ केवल किसी स्थान पर बने हुए शिक्षा भवन से नहीं होता है और न तो केवल उसमें पढ़ने-पढ़ाने वालों से होता है बल्कि किसी निश्चित स्थान पर बने हुए भवन में पढ़ने-पढ़ाने वालों एवं प्रशासन करने वालों और शिक्षण क्रिया में सहयोग देने वाले अन्य व्यक्तियों के क्रिया-कलाप एवं उससे उत्पन्न वातावरण से होता है, जो ‘संस्था’ की अभिकल्पना पूरी करते हैं। ऐसी दशा में विद्यालय के बारे में डीवी के विचार उपयुक्त लगते हैं। उनका कहना है कि “विद्यालय का तात्पर्य एक विशेष वातावरण से है जहाँ जीवन के एक निश्चत गुण तथा कुछ निश्चित प्रकार की क्रियाएँ और व्यवसाय इस लक्ष्य से सिखाये जाते हैं कि वांछित दिशाओं में बालक का विकास हो सके।”
परिभाषा
(i) टी.पी. नन के अनुसार – “किसी राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग होते हैं।”
(ii) एम.एल जैक्स के अनुसार – “विद्यालय एक प्रकार से घर का विस्तार होता है।”
विद्यालय एक अभिकरण के रूप में—
प्रत्येक समाज अपने सदस्यों की शिक्षा का दायित्व स्वयं अपने ऊपर लेता है। वह इस दायित्व का निर्वाह निम्नलिखित साधनों से पूरा करने का प्रयास करता है-
• औपचारिक या नियमित शिक्षा के साधनों द्वारा
• अनौपचारिक या अनियमित शिक्षा के साधनों द्वारा,
औपचारिकेतर शिक्षा के साधनों द्वारा ।
विद्यालय अपने पारम्परिक तथा संकुचित रूप में शिक्षा का औपचारिक एवं सक्रिय साधन है। यह औपचारिक इस रूप में है कि इसका अपना निश्चित उद्देश्य, निश्चित कार्य, निश्चित कार्यक्रम, निश्चित स्थान, निश्चित कर्मचारीगण आदि होते हैं। इस कारण भी इसे पारम्परिक एवं संकुचित कहा जाता है। आधुनिक युग में इसके स्वरूप और कार्यों में बदलाव आया है। जब यह साधन (विद्यालय) सामुदायिक केन्द्र (Community Centre) के रूप में कार्य करता है, तब यह अनौपचारिक शिक्षा के साधन के रूप में कार्य करता है। जब यह ‘राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय’ के रूप में कार्य करता है, तब यह
औपचारिकेतर शिक्षा (Nonformal Education) का महत्त्वपूर्ण साधन बन जाता है। शिक्षा के साधन के रूप में इसके विभिन्न कार्य हैं जिनका नीचे वर्णन किया जा रहा है।
विद्यालय के कार्य
विद्यालय के निम्नलिखित दो प्रमुख कार्य हैं-
(1) औपचारिक कार्य
(2) अनौपचारिक कार्य
( 1 ) विद्यालय के औपचारिक कार्य
विद्यालय के औपचारिक कार्य निम्नलिखित हैं-
(i) चरित्र-निर्माण और आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का प्रशिक्षण देना ।
(ii) अतीत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना और इसे अधिक मूल्यवान बनाकर आने वाली पीढ़ी को हस्तान्तरित करना।
(iii) छात्रों में सोचने और निर्णय करने की शक्तियों का विकास करना, जिससे कि वे अपनी स्वतन्त्र विचार-शक्ति को सोचने, समझने और कार्य करने के लिए प्रयोग कर सकें।
(iv) छात्रों में कार्य को प्रारम्भ करने और नेतृत्व के गुणों का विकास करना, जिससे कि ये प्रजातन्त्र के अच्छे नागरिकों के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक कर सकें।
(v) छात्रों को ऐसा प्रशिक्षण देना, जिससे कि वे समाज और अन्य शक्तियों पर भार बने बिना सम्मानपूर्ण ढंग से अपनी जीविका की समस्या को हल कर सकें।
ब्रबेकर के अनुसार विद्यालय के निम्नलिखित कार्य है-
(i) संरक्षण कार्य –
हमारी सामाजिक संस्कृति बहुत मुसीबतों और बलिदानों द्वारा प्राप्त की गई है। यदि भावी पीढ़ी को न बता सकने के कारण इसका कोई भी अंश नष्ट हो गया तो यह बहुत दुःख की बात होगी। अतः विद्यालय को इसकी शिक्षा देकर इसे सुरक्षित रखना चाहिए। सांस्कृतिक आदर्श विद्यालय द्वारा ही सुरक्षित रखे जाते हैं। इसलिए भी विद्यालय सांस्कृतिक संरक्षण के कार्य की उपेक्षा नहीं कर सकता है।
(ii) प्रगतिशील कार्य – प्रगतिवादियों का मत है कि यह सोचना कि विद्यालय, संस्कृति को • नष्ट होने से बचा सकता है, उतना मूर्खतापूर्ण है, जितना कि यह सोचना कि औषधि, मनुष्य को मरने से बचा सकती है। अतः उनका कथन है कि विद्यालय संस्कृति को सुरक्षित रखने की अपेक्षा समाज को प्रगति की ओर ले जाने का कार्य करे। विद्यालय नये विचारों और कार्यक्रमों को अपनाकर समाज के ढाँचे और आदर्शों को समय के अनुसार परिवर्तित कर सकता है।
(iii) निष्पक्ष कार्य-कुछ व्यक्तियों का मत है कि विद्यालय को निष्पक्ष कार्य करने चाहिए। उसे सांस्कृतिक सुरक्षा, नवीन विचारों, राजनीति आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। उसका स्थान सांस्कृतिक मामलों से ऊपर है। उसका प्रमुख कार्य अनन्त मूल्यों और सत्यों की शिक्षा देना है, अतः उसे किसी मामले के पक्ष या विपक्ष में शिक्षा नहीं देनी चाहिए।
विद्यालय के अनौपचारिक कार्य —
विद्यालय के अनौपचारिक कार्य निम्न प्रकार हैं-
(i) समाज-सेवा, सामाजिक उत्सवों आदि का आयोजन करके छात्रों को सामाजिक प्रशिक्षण देना
(ii) सक्रिय वातावरण का निर्माण करके छात्रों की रुचिकर और रचनात्मक क्रियाओं को प्रोत्साहित करना।
(iii) खेल-कूद, स्काउटिंग, सैनिक शिक्षा, स्वास्थ्य कार्य आदि की व्यवस्था करके छात्रों को शारीरिक प्रशिक्षण देना।
(iv) वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, चित्र-कलाओं, प्रदर्शनियों, संगीत-सम्मेलनों और नाटकों का प्रबन्ध करके बालक और बालिकाओं को भावात्मक प्रशिक्षण देना।
टॉमसन के अनुसार विद्यालय के निम्नलिखित कार्य हैं-
(i) मानसिक प्रशिक्षण – मानसिक प्रशिक्षण का अर्थ है— पुस्तकीय ज्ञान और तर्क-शक्ति का विकास। विद्यालय का यह कार्य संकुचित तो है, पर साथ ही आवश्यक भी।
(ii) चारित्रिक प्रशिक्षण – चारित्रिक प्रशिक्षण विद्यालय का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है। प्राचीन समय के सरल समाज में समाज द्वारा चारित्रिक प्रशिक्षण दिया जाना सम्भव था, पर आज के जटिल समाज में यह सम्भव नहीं है। अतः यह कार्य प्रशिक्षण द्वारा किया जाना चाहिए।
(iii) सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण-विद्यालय को सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण देना चाहिए। अतः विद्यालय ऐसा वातावरण प्रदान करे, जिसमें रहकर छात्र स्वाभाविक जीवन व्यतीत कर सकें।
शिक्षा में विद्यालय का महत्त्व
विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपना औपचारिक महत्त्व अवश्य रखता रहा है। आज भी औपचारिकता से शिक्षण-क्रिया को मुक्त करने की सोचने वाले लोग विद्यालय के वातावरण एवं महत्त्व को हटा नहीं पाये हैं। विद्यालय के महत्त्व उसकी उपयोगिता को भी प्रकट करते हैं और उसकी आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं।
1. औपचारिक ढंग से शिक्षा देने का सबसे प्रमुख साधन होने के विचार से- विद्यालय जीवन के सभी ज्ञान विधिवत एवं औपचारिकता के साथ देता है। सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार के ज्ञान विद्यालय में मिलते हैं। शिक्षा एक प्रयोजनपूर्ण क्रिया होती है, जिसे क्रमबद्ध रूप से विद्यालय में ही कराया जाना सम्भव होता है। इससे बिना अपव्यय के शिक्षा की जटिल क्रिया परी होती है। विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम को एक विशेष वातावरण में विद्यालय छात्रों को पढ़ाता है। विद्यालय बालक को उसके सर्वांगीण विकास के लिए विविध प्रकार के ज्ञान अनुभव देता है।
2. घर की शिक्षा देने की कमी को पूरा करने के विचार से- विद्यालय का महत्त्व उस दशा में भी मिलता है, जहाँ घर ज्ञान प्रदान करने में असफल रहता है। अतएव यह साफ मालूम होता है कि विद्यालय समाज के लोगों को शिक्षित करने का एक अत्यन्त आवश्यक साधन है तथा घर के कार्यों को पूरा करने वाला होता है। आधुनिक युग में विद्यालय विशेष शिक्षा देकर अधिक जिम्मेदार हो गया है और उसे निर्वाह कर रहा है।
3. समाज की संस्थाओं से परिचित कराने के विचार से- अमरीका की एक शैक्षिक टीम ने लिखा है- “विद्यालय प्रयोगशालाओं के समान होने चाहिए जिसमें आदर्श सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण एवं पुनराभिनय हो । उसके लिए विद्यालय समुदाय के साथ चले और समुदाय को विद्यालय में आना चाहिए। जनतन्त्र में यह और भी जरूरी है। इस प्रकार से समाज की संस्थाओं के बारे में तथा उनके प्रयोग के लिए जरूरी ज्ञान प्रदान करने के विचार से विद्यालय का महत्त्व होता है।
प्रश्न 4 (ii) विद्यालय एवं समुदाय से आप क्या समझते हैं? विद्यालय एवं समुदाय की पारस्परिक निर्भरता की व्याख्या कीजिए।
ANSWER–
विद्यालय तथा समुदाय के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये दोनों अपनी-अपनी उन्नति एवं स्थायित्व के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना करता है जिनके द्वारा समाज के विचारों, मान्यताओं, आदर्शों, क्रिया-कलापों, मानदण्डों तथा परम्पराओं को आने वाली पीढ़ी को प्रदान किया जा सके। इस तथ्य की पुष्टि हम फ्रैंकलिन (Franklin) के शब्दों से कर सकते हैं- “समाज, शिक्षा-संस्थाओं को अपने सदस्यों में ऐसे ज्ञान, कौशलों, आदतों तथा आदर्शों का प्रसार करने एवं सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है जो उसके स्वयं के स्थायित्व एवं निरन्तर विकास के लिए परमावश्यक है।”
विद्यालय, समुदाय के जीवन एवं उसकी प्रगति पर बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय अपने विचारों एवं कार्यों द्वारा समुदाय का पथ-प्रदर्शन करके उसे प्रगति की ओर ले जाता है। हम इस तथ्य की पुष्टि हॉवर्थ (Howerth) के इन शब्दों द्वारा कर सकते हैं- “विद्यालय, समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं यह विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर निर्भर रहता है।”
समुदाय का विद्यालय पर प्रभाव
सामान्यतः लोग ‘समुदाय’ (Community) तथा ‘समाज’ (Society) का एक ही अर्थ लगाते हैं, परन्तु इनके अर्थ में विभिन्नता है। इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए आर. जी. कॉलिंगवुड (R.G Collingwood) ने लिखा है- “समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति, प्रौढ़ एवं बच्चे, सामाजिक तथा असामाजिक व्यक्ति सभी आते हैं जो एक निश्चित भू-भाग पर रहकर सामान्य जीवन में भाग लेते हैं, परन्तु वे सभी उसके संगठन या अभिप्राय के प्रति सचेत या जागरूक नहीं रहते हैं। समाज एक प्रकार का समुदाय या समुदाय का अंश है, जिसके सदस्य सामाजिक रूप से सचेत होकर उसके सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं और वे समान उद्देश्यों तथा मान्यताओं के फलस्वरूप एकता में बँधे रहते हैं । ”
समुदाय अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं आदि की पूर्ति के लिए विद्यालयों की स्थापना करता है। इस कारण समुदाय का विद्यालय पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। विद्यालय पर समुदाय के प्रभाव को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है-
(i) समुदाय के आदर्शों, मान्यताओं व आवश्यकताओं का प्रभाव – प्रत्येक समुदाय के अपने आदर्श, मान्यताएँ तथा आवश्यकताएँ होती हैं। वह इनकी पूर्ति एवं स्वयं को जीवित रखने के लिए विद्यालय की स्थापना करता है। इस कारण समुदाय के आदर्शों, मान्यताओं तथा आवश्यकताओं का विद्यालयों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण-विधि, आदि में देखने को मिलता है। समुदाय की आवश्यकताओं एवं माँगों के बदलते रहने के कारण शिक्षा के इन क्षेत्रों में भी परिवर्तन होता रहता है; उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में भारतीय समुदाय की आवश्यकताएँ एवं माँगें परिवर्तित हो चुकी हैं। आज का भारतीय समुदाय औद्योगीकरण की माँग कर रहा है। इस कारण भारतीय समुदाय के विद्यालयों में ‘कार्य-अनुभव’ (Work Experience) को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। साथ ही समुदाय विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना कर रहा है।
(ii) समुदाय की राजनीतिक दशाओं का प्रभाव – समुदाय की राजनीतिक दशाओं का विद्यालय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी समुदाय में शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? इसका उत्तर उस समुदाय की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करता है; उदहरणार्थ, भारतीय समुदाय ने लोकतान्त्रिक प्रणाली को अपनाया है। इसकी सफलता के लिए योग्य नागरिकों की आवश्यकता है। अतः विद्यालयों का एक प्रमुख कार्य है— योग्य नागरिकों का निर्माण करना। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए विद्यालय का लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के अनुसार संगठन एवं संचालन किया जाता है। साथ ही विद्यालय वातावरण में स्वतन्त्रता, समानता एवं भ्रातृत्व नामक मूलाधारों को स्थान प्रदान किया जाता है।
(iii) समुदाय के गुणों व दोषों का प्रभाव – प्रत्येक समुदाय में गुण एवं अवगुण पाये जाते हैं। भारतीय समुदाय विभिन्न सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त है। इनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालयों पर पड़ता है। भारतीय समुदाय के साम्प्रदायिक विद्यालय (Communal Schools) इसके स्पष्ट उदहारण हैं।
विद्यालय का समुदाय पर प्रभाव —
समुदाय पर विद्यालय के प्रभाव का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जाता है—
(i) समुदाय की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण- प्रत्येक समुदाय के अपने रीति-रिवाज, परम्पराएँ, विश्वास, नैतिकता, नियम, साहित्य आदि होते हैं जिनको उस समुदाय ने प्राचीन समय से लेकर आज तक अर्जित किया है। शिक्षा, समुदाय की इस सांस्कृतिक विरासत को बनाये। रखने तथा विकसित करने की प्रक्रिया है। विद्यालय इस सांस्कृतिक विरासत को आने वाली सन्तति । को प्रदान करके, उसको बनाये रखते हैं। साथ ही वे आने वाली सन्तति को इस योग्य भी बनाते हैं कि वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार उस विरासत को अपना योगदान कर सकें। विद्यालयों के अभाव में इस जटिल एवं विस्तृत तथा विशाल विरासत को थोड़े-से जीवनकाल में सीखना सम्भव नहीं है ।
(ii) समुदाय की आवश्यकताओं व माँगों की पूर्ति – प्रत्येक समुदाय की अलग-अलग आवश्यकताएँ एवं माँगें होती हैं। विद्यालय अपनी योजना तथा कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके समुदाय की माँगों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
(iii) समुदाय की व्यावसायिक व औद्योगिक प्रगति – विद्यालय समुदाय की व्यावहारिक एवं औद्योगिक प्रगति को भी प्रभावित करता है। समुदाय के व्यवसायों को पाठ्यक्रम में किसी-न-किसी रूप में स्थान मिलता है। महात्मा गाँधी ने भारतीय समुदाय की आर्थिक दशा के सुधार के लिए बेसिक शिक्षा पर बल दिया था। उन्होंने स्कूल के पाठ्यक्रम में समुदाय के प्रमुख हस्त शिल्पों को स्थान प्रदान किया। साथ ही, उन्होंने बुनियादी शिल्प पर आधारित शिक्षा की नींव डाली, जिससे समुदाय के लोग स्वावलम्बी बन सकें।
प्रश्न 5.विद्यालय को शिक्षा का प्रभावी अभिकरण बनाने के उपायों का वर्णन कीजिए।
ANSWER–
विद्यालय को शिक्षा का प्रभावी अभिकरण बनाने के उपाय निम्नलिखित हैं-
(1) घर या परिवार से सहयोग-शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए विद्यालय को घर से सहयोग करना चाहिए। माता-पिता को अपने बच्चों की आदतों, रुचियों, गुणों और अवगुणों को शिक्षकों को बताकर सहयोग देना चाहिए। इन बातों को जानकर शिक्षक अच्छी प्रकार से छात्रों का पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी ओर, माता-पिता भी अपने बच्चों के बारे में शिक्षकों के विचारों से लाभ उठा सकते हैं। शिक्षकों और अभिभावकों में निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है-
(i) अभिभावक संघ-अभिभावकों और शिक्षकों को एक-दूसरे के सम्पर्क में लाने के लिए अभिभावक-संघ स्थापित किये जाने चाहिए। संघ की बैठकों का कार्यक्रम बदलता रहना चाहिए। जैसे—अभिभावकों और शिक्षकों में बच्चों की शिक्षा के बारे में विचार-विमर्श, नई शिक्षण विधियों की व्याख्या या प्रदर्शन, शिक्षा में नई प्रवृत्तियों पर भाषण इत्यादि। इन सब बातों से अभिभावकों के ज्ञान में वृद्धि होगी और वे शिक्षकों को महत्त्वपूर्ण सहयोग दे सकेंगे।
(ii) अभिभावक दिवस – प्रत्येक विद्यालय में प्रतिवर्ष एक या दो बार अभिभावक दिवस मनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर अभिभावकों को अपने बच्चों के खेल-कूद, नाटक, प्रदर्शनी, आदि को देखने का अवसर दिया जाना चाहिए।
(iii) प्रगति – पत्र – अभिभावकों के पास उनके बच्चों के प्रगति-पत्र अवश्य भेजे जाने चाहिए। इससे वे जान सकेंगे कि उनके बच्चे विद्यालय में उन्नति कर रहे हैं या नहीं।
(2) सामाजिक जीवन से सम्पर्क-आमतौर पर शिकायत की जाती है कि विद्यालय का सामाजिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। फलतः जब बालक शिक्षा समाप्त करके जीवन में प्रवेश करता है, तब वह कठिनाई का अनुभव करता है। वास्तव में विद्यालय का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए।
उसे बाहर के बड़े समाज का छोटा रूप होना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधोलिखित उपाय काम में लाये जा सकते हैं-
(i) समाज-सेवा में भाग–समुदाय की भलाई के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग लेना चाहिए। विद्यालय को छात्रों में समाज-सेवा के आदर्शों और इच्छाओं को कूट-कूटकर भरने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही, उसे छात्रों को समाज सेवा के अवसर और सुविधाएँ देनी चाहिए।
–
(ii) समाज के सदस्यों को आमन्त्रण-विद्यालय को समाज के ऐसे सदस्यों को समय- समय पर आमन्त्रण देना चाहिए, जो विभिन्न उपयोगी कार्यों में लगे हुए हों। ये सदस्य अपने भाषणों द्वारा छात्रों को अपने कार्यों के बारे में बताएँ। वे यह भी बताएँ कि उनके कार्यों का समाज में क्या स्थान है और इन कार्यों की कठिनाइयाँ और अच्छाइयाँ क्या हैं? इस प्रकार, छात्रों में समाज का ज्ञान बढ़ेगा।
(iii) प्रौढ़ शिक्षा का केन्द्र-विद्यालय को प्रौढ़-शिक्षा का केन्द्र होना चाहिए। इससे भारत देश की निरक्षरता की समस्या कुछ सीमा तक हल हो सकती है। इसके अतिरिक्त, विद्यालय के सम्पर्क में रहने के कारण प्रौढ़ व्यक्ति विद्यालय की प्रगति में रुचि लेने लगेंगे।
(3) राज्यों का संरक्षण – नेपोलियन (Napoleon) ने एक बार कहा था – “जन-शिक्षा सरकार का प्रथम कार्य होना चाहिए।”
“Public instruction should be the first object of Government.
”
18वीं शताब्दी में कही गई यह बात आज भी सत्य है। इसलिए, सभी उन्नतशील देशों में जन- शिक्षा का भार सरकार पर है, परन्तु भारत में स्थिति हास्यपूर्ण है। सरकार अपने विद्यालयों पर तो आँख बन्द करके धन व्यय करती है और प्रबन्ध-समितियों द्वारा स्थापित विद्यालयों के साथ सौतेली माँ के जैसा व्यवहार करती है। जब तक सरकार देश के सभी विद्यालयों का भार अपने ऊपर नहीं लेगी, तब तक वह अपनी योजनाओं पर अरबों-खरबों रुपया व्यय करके भी देश की उन्नति नहीं कर सकेगी। अतः आवश्यक है कि सरकार निम्नलिखित उपायों को काम में लाये-
(i) अच्छे विद्यालयों की स्थापना -अच्छे विद्यालय वे हैं, जो सरकार द्वारा निश्चित किये गये शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक-से-अधिक योग देते हैं। बड़े दुःख की बात है कि हमारी सरकार ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।
(ii) योग्य शिक्षकों की नियुक्ति-शिक्षण कार्य के लिए उतने ही योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है, जितने कि किसी सरकारी कार्य, उद्योग या व्यवसाय के लिए। इस प्रकार के व्यक्ति तभी मिल सकते हैं, जब उनको उतना ही वेतन और वैसी ही सुविधाएँ मिलें जैसी कि उनको और कहीं कार्य करने पर मिल सकती हैं।
(iii) विद्यालयों का नियन्त्रण व निरीक्षण-सरकार को स्कूल इंस्पेक्टरों की संख्या बढ़ाकर विद्यालयों पर अपना नियन्त्रण कड़ा करना चाहिए। इंस्पेक्टरों को आज्ञा दी जाय कि वे समय- समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करें और उनकी समस्याओं को सुलझाएँ ।
(iv) ट्रेनिंग कॉलेजों का पुनर्गठन -आज देश के अधिकांश ट्रेनिंग कॉलेज अंग्रेजों के समय की लकीर को पीट रहे हैं। इनमें से कितने ही छात्रों को डिग्री दिलाने की दुकानें बन गये हैं। इनकी ओर ध्यान देने का सरकार को स्वतन्त्रता के इस लम्बे समय में अभी अवकाश नहीं मिला है। यह अति आवश्यक है कि भारत की वर्तमान आवश्यकताओं और शिक्षा की आधुनिक प्रवृत्तियों एवं सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर सरकार इनका पुनर्गठन करे। अब इस ओर ‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्’ (NCTE) महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है, परन्तु उसने स्ववित्तपोषित ट्रेनिंग कॉलेजों की स्थापना कराकर बी. एड. को मजाक तथा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है।
विद्यालय के बारे में काफी कहा जा चुका है। फिर भी अपने देश के सामान्य विद्यालयों का चित्र प्रस्तुत करना अनुपयुक्त न होगा। सैयदेन का कथन है- “अपने सर्वोत्तम रूप में ये विद्यालय ऐसे स्थान हैं, जहाँ पढ़ना-लिखना सीखना आदि में; या इतिहास, भूगोल और विज्ञान आदि में औपचारिक शिक्षा दी जाती है। अपने निम्नतम रूप में वे ऐसे स्थान हैं, जहाँ बच्चों के उल्लास और कार्य के प्रति प्रेम का गला घोंटा जाता है।”
इकाई-III
प्रश्न 6 (i) भारत में सह-शिक्षा की अवधारणा बताइए। सह-शिक्षा के गुण-दोषों की व्याख्या कीजिए।
अथवा
भारत में सह-शिक्षा को परिभाषित कीजिए। इससे लाभ एवं हानि की स्पष्ट व्याख्या कीजिए ।
अथवा
सह-शिक्षा विद्यालय से क्या तात्पर्य है? सह-शिक्षा विद्यालयों की ताकत एवं कमजोरी क्या है? व्याख्या कीजिए।
ANSWER–
भारत जैसे देश में जहाँ नारी को देवी जैसा पद दिया गया है, वहाँ पर नारी को
बहुत-सी समस्याओं से गुजरना इसके सांस्कृतिक मूल्यों और यथार्थ के बीच के अन्तर को स्पष्ट करता है। आज के परिवेश में जहाँ पर नारी और गरीब लोगों की सामाजिक सुरक्षा दाँव पर लगी है और वहाँ के तथाकथित नेता अपने घोटालों और सुखभोग में व्यस्त हों वहाँ पर इन मुद्दों के बारे में सोचना और विचार करना अति आवश्यक हो जाता है।
बचपन से ही लड़के और लड़कियों का भेद उनमें एक-दूसरे के प्रति जिज्ञासु बना देता है। शिक्षण संस्थानों को भी लिंग आधारित बना देना इसको और बढ़ा देता है। सह-शिक्षा के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं, जिन्हें निम्न परिभाषाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ब्रिटेनिका विश्वकोश के अनुसार सह शिक्षा का अर्थ है- “लड़के तथा लड़कियों को एक ही समय, एक ही स्थान पर, एक ही अधिकारी द्वारा, एक ही शासन के अधीन, एक ही तरीके से, एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। ” माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) के शब्दों में, “समता के आधार पर एक ही संस्था में लड़के एवं लड़कियों को शिक्षा देना सह शिक्षा कहलाता है।” इस प्रकार कहा जा सकता है कि सहशिक्षा संस्थाओं में लड़के एवं लड़कियाँ साथ-साथ पाठ्यचर्या को पूर्ण करते हैं।
सह-शिक्षा व्यवस्था भारत के लिए नई नहीं है। वैदिक काल में लड़के एवं लड़कियाँ गुरु के आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। स्वतन्त्रता के पश्चात् सहशिक्षा संस्थाओं में द्रुत गति से विकास हुआ है, विशेषकर पब्लिक स्कूल प्रणाली में । विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) का विचार था कि लोगों की राय ऐसी मालूम होती है कि 13 या 14 वर्ष की आयु से लगभग 18 वर्ष की आयु तक लड़के-लड़कियों के विद्यालय अलग-अलग होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) का विचार है- “ऐसा जान पड़ता है कि सहशिक्षा के सम्बन्ध में हमारे स्कूलों की शिक्षा प्रणाली उस समुदाय की सामाजिक पद्धति से आगे नहीं बढ़ सकती है, जिसमें कि स्कूल स्थापित किये जाने चाहिए। हमार विचार है कि जिन स्थानों पर सम्भव हो वहाँ लड़कियों के पृथक स्कूल हों क्योंकि ये मिश्रित स्कूलों की अपेक्षा उनकी शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विशेषताओं के विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान करेंगे और सभी राज्यों को ऐसे स्कूल पर्याप्त संख्या में खोलने चाहिए। परन्तु ये उन लड़कियों के लिए खोले जाने चाहिए, जिनके अभिभावकों को मिश्रित स्कूलों की सुविधाओं से लाभ उठाने में आपत्ति हो।” इसी प्रकार शिक्षा आयोग (1964-66) ने सहशिक्षा के सम्बन्ध में अपने सुझाव देते हुए कहा है कि “कॉलेज के स्तर पर स्थानीय ऐतिहासिक परम्पराएँ और सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि यह निर्धारित करती हैं कि वहाँ महिलाओं के लिए पृथक् कॉलेज हों या मिश्रित कॉलेज हों। शिक्षा के स्तर के लिए सहशिक्षा की समरूपी नीति आवश्यक नहीं है, परिस्थिति प्रत्येक राज्य में भिन्न है। …. अतएव इस स्तर पर सहशिक्षा सम्बन्धी नीति का निर्णय प्रत्येक राज्य की सरकार को करना होगा।” पूर्व स्नातक स्तर पर यदि स्थानीय माँग हो तो महिलाओं के लिए पृथक् कॉलेज स्थापित कियो जा सकते हैं। शिक्षा आयोग के विचार में स्नातकोत्तर स्तर पर महिलाओं के लिए पृथक् शिक्षा संस्थाओं का कोई औचित्य नहीं है।
सह-शिक्षा के गुण
सह-शिक्षा के निम्नलिखित गुण हैं-
सहशिक्षा के समर्थन में तर्क दिया जाए तो तीन तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रथम,
आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की कम जनसंख्या होने के कारण अलग स्कूल या कॉलेज खोलना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है। विशेषकर यह परिस्थिति ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों ही गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न कर देती है। वही भवन, वही साधन-सामग्री, पुस्तकालय तथा अन्य सुविधाएँ लड़कियों के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती हैं। अतः अतिरिक्त वित्तीय भार और अनावश्यक वृद्धि अपव्ययपूर्ण होगी। द्वितीय दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक है, जिसमें नारी-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति का कथन है- “पारस्परिक सम्पर्क जिज्ञासा की उस भावना का अन्त कर देता है, जो अजनबीपन के कारण उत्पन्न हो जाती है और जो लिंगों के अलगाव और पृथकता की विशेषता है।” ऐसा समझा जाता है कि केवल साथ रहने से ही प्राकृतिक भावनाओं की समझ व आत्मविश्वास की भावना आ सकती है।
सहशिक्षा के विरोध में अनेक विद्वानों ने स्वर मुखरित किया है। विरोधस्वरूप अनेक तथ्य प्रस्तुत किये हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर—प्रथम, सहशिक्षा बालक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। द्वितीय, सहशिक्षा संस्थाओं में कामुकता की भावना का विकास होता है। सहशिक्षा संस्थाओं में कई प्रकार का यौन उल्लंघन होना पाया गया है। नैतिक स्तर पर नये रोमांस या दुस्साहस की भावना उत्पन्न होने का भय बना रहता है। एक नवयुवक नैतिकता की उपेक्षा करके पतन की ओर अग्रसर हो सकता है। इसी प्रकार भावनात्मक सन्तुलन सहशिक्षा संस्थाओं में पाया जाता है— सहशिक्षा संस्थाओं से कई बार नवयुवक एवं नवयुवतियाँ भावुकता की दृष्टि से दीवालिए होकर निकलते हैं। वे अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। कई बार सहशिक्षा संस्थाओं में अध्यापक एवं विद्यार्थी लिंग-भावना के आकर्षण से ग्रस्त हो जाते हैं।
सह-शिक्षा के दोष (अवगुण )
सहशिक्षा के अवगुण निम्नलिखित हैं-
1. कुछ व्यक्तियों का यह कहना है कि पुरुष छात्र और महिला छात्र सह-शिक्षा के माध्यम से जब एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं तो वे एक-दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं और एक-दूसरे के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से दोनों व्यक्तियों का भावी गृहस्थ जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है।
2. छात्र में छात्रा की अपेक्षा हीन भावना होती है। पुरुष, महिला के सम्पर्क में आते ही उसके सम्मुख आत्महीनता का शिकार हो जाता है। इस प्रकार पुरुष छात्र का व्यक्तित्व विकास की स्थिति में न रहकर हीन भावना से पूरित हो जाता है। यदि शारीरिक रचना में पुरुष की अपेक्षा महिला कम सुन्दर होती है तो उसके विपरीत महिला में ही हीनभावना जाग्रत हो जाती है और उसके व्यक्तित्व पर अवांछनीय प्रभाव पड़ने लगता है।
कभी-कभी आत्महीनता की भावना पुरुष अथवा महिला विद्यार्थी को यौन आकर्षण से दूर हटाकर शैक्षिक क्षेत्र की सफलताओं के प्राप्त कराने में सहायक हो जाती है। ऐसा व्यक्ति एकाकी जीवन व्यतीत करना पसन्द करता है और उसकी क्षति की पूर्ति वह अध्ययन में लगाकर दूसरे की अपेक्षा उच्च स्तर प्राप्त करने का प्रयास भी करता है।
3. सह-शिक्षा क्षेत्र में यह बात देखने को मिलती है कि छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व उनके शुद्ध ‘स्वरूप में नहीं रह पाते। अधिकांशतः पुरुष स्त्रियों के गुण और स्त्री पुरुषों के गुण ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा करने से पुरुष का पौरुष हीन होने लगता है तथा स्त्री में लज्जा तथा स्त्रीत्व का अभाव होने लगता है।
कुछ व्यक्ति इस पक्ष के हैं कि पुरुषों को अच्छे शिष्टाचार को सीखने के लिए शिक्षित स्त्रियों के मध्य जाना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष की झिझक और अशिष्ट व्यवहार नहीं रहेंगे। इसका कारण यह बतलाया जाता है कि पुरुष विरोधी यौन वर्ग के व्यक्ति (महिला) को अपने व्यवहारों से प्रसन्न रखना चाहता है। अतः वह वैसा ही व्यवहार करने का प्रयास करता है जो उसे रुचिकर प्रतीत होता है। इसी प्रकार स्त्रियों को पुरुषों के मध्य रहकर स्वतन्त्र वातावरण मिलता है जिसमें वे आनन्द का अनुभव करते हुए निर्भीक बन जाती हैं।
प्रश्न 6 (ii) स्त्री-शिक्षा के पाठ्यक्रम की व्याख्या कीजिए।
अथवा
सह-शिक्षा के अन्तर्गत स्त्री-शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए।
ANSWER–
हमारे समाज में अभी भी बालक-बालिकाओं की सह-शिक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाया है। सह-शिक्षा के विषय में लोगों के मन में तरह-तरह की भ्रान्तियाँ हैं और सरकार सभी स्तरों पर आर्थिक दृष्टि से बालिकाओं के लिए पृथक् शिक्षण संस्थानों की स्थापना नहीं कर सकती। अतः अभिभावक सुरक्षात्मक कारणों और संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण सह-शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेजते हैं। परिणामस्वरूप उनकी परन्तु औपचारिक शिक्षा बाधित हो जाती है। प्राचीन काल तथा विहारों में सह-शिक्षा का प्रचलन था, मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों की सह-शिक्षा का पतन हुआ। ब्रिटिश काल में 1942 में 48 प्रतिशत बालक तथा बालिकाओं ने सह-शिक्षा प्राप्त की, परन्तु धीरे-धीरे सामाजिक तथा सुरक्षात्मक कारणों से सह-शिक्षा के प्रति मोह भंग हुआ है। लीकॉक महोदय ने सह-शिक्षा के दोषों का वर्णन इन शब्दों में किया है – “मनुष्य उस समय अध्ययन कर ही नहीं सकते, जब उनके चारों ओर महिलायें हों। यदि महिलाओं को प्रवेश दे दिया जाता है तो वे किसी भी प्राध्यापक के चारों ओर आने लगती हैं। प्राध्यापक उनमें से किसी के साथ विवाह कर लेता है और उसकी उच्च विचारों तथा अनुसंधान कार्यों से छुट्टी हो जाती हैं। ”
स्त्री-शिक्षा के पाठ्यक्रम —
प्रत्येक शिक्षा आयोग ने अपनी संस्तुतियों में यही कहा है कि स्त्रियों के लिए पुरुषों के समान सामान्य पाठ्यक्रम तथा एक-एक पृथक् विशिष्ट पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। इस विशिष्ट पाठ्यक्रम में गृह-विज्ञान, गृह- अर्थशास्त्र और गृह प्रबन्ध जैसे विषय, ललित कलाएँ (संगीत, चित्रकला और नृत्यकला) रखी जानी चाहिए।
वास्तव में स्त्री-शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य स्त्रियों को योग्य गृहणी, योग्य माता और योग्य पत्नी बनाना ही है। इसके अतिरिक्त वे भारत के सामान्य नागरिकों की भाँति पुरुषों के समान कर्त्तव्यों और अधिकारों का निर्वाह कर सकती हैं। भारतीय संविधान में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हैं।
कोठारी आयोग ने सुझाव दिया है कि स्त्रियों को स्त्रियोचित पाठ्यक्रम तो अवश्य मिलना चाहिए; परन्तु वह इस बात में स्वतन्त्र होनी चाहिए कि वह किस पाठ्यक्रम का चयन करती है। उस पर गृह-विज्ञान, गृह-प्रबन्ध और गृह- अर्थशास्त्र लादा नहीं जाना चाहिए, परन्तु हाईस्कूल स्तर तक उपर्युक्त गृह-विज्ञान सम्बन्धी विषयों के माध्यम से गृह-व्यवस्था का जानना आवश्यक है। अतः इस स्तर तक इन विषयों को अनिवार्य बनाया जा सकता है।
उच्च माध्यमिक स्तर तथा उच्च शिक्षा-स्तर पर उन महिलाओं के लिए जो नियमित रूप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकतीं, घर पर ही पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए ‘पत्राचार शिक्षण व्यवस्था’ तथ ‘सेवा-कालीन’ शिक्षा-व्यवस्था उपयुक्त रहेंगी। महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से परीक्षाओं में बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि महिलाएँ भी पुरुषों के पाठ्यक्रम ग्रहण करके कुशल शिक्षक, कुशल चिकित्सक, योग्य अभियन्ता, नेता और समाज सुधारक बन सकती हैं। अतः उन्हें विषय चयन की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।
निर्धारित महिलाएँ शिक्षा निदेशक अपनी सहायतार्थ मण्डलों (Regions) की सीमा निर्धारित करके विद्यालयों की मण्डलीय निरीक्षिका की नियुक्ति कराती हैं। एक मण्डल के सभी कन्या विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था का प्रशासनिक तथा आर्थिक उत्तरदायित्व उपयुक्त निरीक्षक के माध्यम से सम्पन्न होता है। इस प्रकार बालिका-शिक्षा माध्यमिक स्तर तक दोहरे शासन में रहती है। बालिका शिक्षा- संस्थाओं को अन्य पुरुष छात्र विद्यालयों के समान प्रशासनिक तथा नियन्त्रण की दृष्टि से जिला विद्यालय निरीक्षक (District Inspector of Schools) के आदेशों का पालन करना होता है तथा दूसरी ओर आर्थिक और व्यवस्थापक नियन्त्रण की दृष्टि से उन्हें जिले की सह-निरीक्षिका (Deputy Inspectors of Schools) के आदेशों का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार बालिका-शिक्षा के विकास में दोहरी बाधा उत्पन्न होती है।
बालिका की शिक्षा का प्रशासन शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशकों और महिला उपशिक्षा निदेशक के हाथों में होने से उचित व्यवस्था नहीं हो पाती। 1958 ई. में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय नारी समिति (National Women Committee) की नियुक्ति की थी और उसके सुझावानुसार 1959 ई. में राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परिषद् (National Council of Girl Education) का गठन तथा नियुक्ति की गयी। इस परिषद् ने सुझाव दिया था कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय में एक पृथक् बालिका शिक्षा विभाग खुले जो बालिका-शिक्षा के विकास की योजना कार्यक्रम और नीति निर्धारित करे। इसी प्रकार राज्यों में भी शिक्षा विभागों के अन्तर्गत बालिका शिक्षा उप-विभाग स्थापित किया जाए और संयुक्त शिक्षा निदेशकों (Joint Director of Education) की नियुक्ति की जाए। एक स्त्री-शिक्षा परामर्शदात्री समिति बनाकर राज्य स्तर पर बालिका-शिक्षा की नीति संचालित होनी चाहिए। यह योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।
प्रश्न 7 (i) स्त्री-शिक्षा का संगठन किस प्रकार होता है?
अथवा
स्त्री-शिक्षा के प्रशासन एवं नियन्त्रण की व्याख्या कीजिए।
ANSWER–
वैदिक काल में स्त्री-शिक्षा व्यवस्था ‘तपोवनों’ में संचालित होती थी। इन तपोवनों में महिलाओं तथा पुरुषों के लिए शिक्षा-व्यवस्था न होकर कुमारियों और कुमारों जिन्हें ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी कहकर पुकारा जाता था, के लिए होती थी। कुमार आश्रम बहुत दूरी पर पृथक्-पृथक् हुआ करते थे जिनकी व्यवस्थाएँ पुरुष व्यवस्थापकों (ऋषियों) तथा स्त्री व्यवस्थापिकाओं (विदुषियों) के हाथों में होती थीं। परन्तु गुरु-आश्रमों में यदि गुरु कोई कन्या रखता था तो वह कुमार-विद्यार्थियों के साथ अध्ययन कर लेती थी। गुरु के आश्रम में कुमार और कुमारी छात्राएँ भाई-बहन के सम्बन्ध स्थापित करके अध्ययनशील रहते थे। पुराने काल में कुमार और कुमारी को जीवन के लिए तैयार किया जाता था। अतः इनका ब्रह्मचर्य-काल शक्ति-संचय का काल होता था। इस शक्ति को संचित करके वे कठोर जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्याश्रम पूर्ण करते थे और बाद में गृहस्थाश्रम का उपभोग करके योग्य सन्तान उत्पन्न करते थे। इसलिए आधुनिक गुरुकुल प्रणाली जिसे युग प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्थापित किया था, इसी धारण से चलायी थी कि कुमार और कुमारी पृथक्-पृथक् रहकर शिक्षार्जन काल में ब्रह्मचर्यपूर्वक रह सकें और शक्ति संचित करके अपने भावी जीवन में आने वाले प्रत्येक जीवन संघर्ष को झेलकर सफलता प्राप्त कर सकें। परन्तु आज की शिक्षा-व्यवस्था में पुरातन सांस्कृतिक परम्पराओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता। न तो अभिभावक ही और न शिक्षा-व्यवस्थापक एवं प्रशासक ही कुमार और कुमारियों के लिए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। उनका शिक्षा से तात्पर्य केवल साक्षरता ग्रहण करके विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेना है और प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना है जो उन्हें नौकरी दिला सके। समझदार व्यक्ति अब भी ब्रह्मचर्य को जीवन के विकास तथा जीवन की तैयारी का प्रमुख साधन मानते हैं तथा अपने बालक-बालिकाओं को पृथक्-पृथक् विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर पढ़ाते हैं।
आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और आर्थिक समस्या ने कुमार और कुमारियों को साथ- साथ पढ़ने के लिए बाध्य कर दिया। सरकार तथा समाज पुरुष छात्रों के समान महिला छात्राओं के लिए शिक्षालय स्थापित नहीं कर सकता। अतः कुमार और कुमारियों के सम्मिलित रूप में पढ़ाने की प्रथा को स्वीकार करते हुए सह-शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ी।
स्त्री-शिक्षा के प्रशासन एवं नियंत्रण —
शिक्षा राज्यों के उत्तरदायित्व का विषय है जिसका विकास राज्यों को ही करना होता है, केन्द्रीय सरकार राज्यों का विकासात्मक अनुदान प्रतिवर्ष दिया करती है। इस प्रकार स्त्री-शिक्षा के सभी विद्यालय प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक चार प्रशासकों के नियन्त्रण में हैं-
1. केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में
2. राज्य सरकार के प्रशासन में,
3. स्थानीय परिषदों के प्रशासन में, तथा
4. व्यक्तिगत अथवा सामाजिक प्रशासन में ।
केन्द्रीय सरकार स्त्री-शिक्षा की कोई पृथक् व्यवस्था नहीं करती, वह इस शिक्षा को भी शिक्षा मन्त्रालय के माध्यम से सामान्य शिक्षा की भाँति व्यवस्थित करती है। परन्तु ‘राष्ट्रीय महिला शिक्षा- परिषद्’ की संस्तुति पर वह विशिष्ट आयोग या समिति नियुक्त करके उसकी स्थिति का सर्वेक्षण करा लेती है और स्त्री-शिक्षा के विकास की संस्तुतियाँ स्वीकार करके एक राष्ट्रव्यापी नीति बना लेती है जिसकी सूचना राज्य सरकारों को दे दी जाती है। राज्य सरकारें उस नीति का पालन करके स्त्री-शिक्षा की व्यवस्था करती हैं।
राज्य सरकारें प्रदेश में शिक्षा-विभाग की सहायता से सभी स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था, प्रशासन और नियन्त्रण करती हैं। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा का संचालन शिक्षा-विभाग, (प्रान्तीय) करता है। स्त्री-शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रदेश के शिक्षा विभाग में महिला शिक्षा निदेशक ही उत्तरदायी होती है। निर्धारित महिलाएँ शिक्षा निदेशक अपनी सहायतार्थ मण्डलों की सीमा निर्धारित करके ‘विद्यालयों की मण्डलीय निरीक्षिका’ की नियुक्ति कराती हैं। एक मण्डल के सभी कन्या विद्यालयों की शिक्षा-व्यवस्था का प्रशासनिक तथा आर्थिक उत्तरदायित्व उपर्युक्त निरीक्षक के माध्यम से सम्पन्न होता है। इस प्रकार स्त्री-शिक्षा माध्यमिक स्तर तक दोहरे शासन में रहती है।
प्रश्न 7 (ii) स्वतंत्रता के उपरांत स्त्री-शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालिए।
ANSWER-
स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्री-शिक्षा का जो विकास हुआ है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बालिका शिक्षा की ओर हमारा दृष्टिकोण ही बदल गया। स्त्रियों को पुरुषों के समान स्तर पर लाने के लिए आवश्यक सामाजिक, आर्थिक और कानूनी परिवर्तन किये गये और एक नये युग का शुभारम्भ हुआ। भारत का संविधान पुरुष और नारी दोनों के लिए समान अधिकार देता है। कुछ विशेष विधान स्त्रियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर को ऊँचा उठाने हेतु हैं।
अनुच्छेद 15 (1), 16 (1), 16 (2) में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। सरकार ने नारी उत्थान के लिए श्रीमती जयन्ती पटनायक की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन की स्थापना की। स्त्रियों के उत्थान के लिए यह कमीशन एक अच्छा अस्त्र साबित होगा, ऐसी आशा की गयी।
स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्री-शिक्षा के सन्दर्भ में आयोगों एवं समितियों ने निम्न कार्य किये-
राधाकृष्णन कमीशन (1948-49), जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ने स्त्री- शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि “शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते।” इस आयोग ने स्त्री-शिक्षा के विकासार्थं कुछ सुझाव दिये-
1. नारी को सुमाता तथा सुगृहिणी बनाने की शिक्षा दी जाये।
2. स्त्रियों के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाय।
3. स्त्रियों को गृह प्रबन्ध अध्ययन की प्रेरणा और अवसर दिये जायें।
4. अध्यापिकाओं को समान कार्यों के लिए अध्यापकों के बराबर वेतन दिया जाये!
5. ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाये जो बालिकाओं को समाज में समान स्थान दिला सके।
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने नारी शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक उत्साह का प्रदर्शन किया। नये संविधान का उद्देश्य भारत में एक ऐसे संविधान की संरचना करना है जो सब नागरिकों को बिना धर्म, जाति अथवा लिंग भेद के न्याय एवं समानता पर आधारित हो, इसीलिए सरकार द्वारा स्त्री-शिक्षा के लिए प्रभावशाली कदम उठाये गये। वर्ष 1949-50 के प्राथमिक स्कूलों में बालिकाओं की संख्या का प्रतिशत मात्र 28 था।
योजना आयोग द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्त्री-शिक्षा के विकास हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किये गये उसके परिणामस्वरूप स्कूल जाने वाली 6-11 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं की संख्या का प्रतिशत वर्ष 1955-56 में 40 प्रतिशत तक पहुँच गया जो कि वर्ष 1950-51 में मात्र 23.3 प्रतिशत था। योजना आयोग द्वारा अत्यन्त पिछड़ी बालिकाओं तथा महिलाओं को शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु शिक्षा के आवश्यक लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से उन्हें शिक्षित करने हेतु पूरे प्रयास किये गये।
इस अवधि में बालिका शिक्षा संस्थाओं की संख्या 61 लाख से बढ़कर 81 लाख हो गयी। इस संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि का कारण बालिकाओं का सहशिक्षा में प्रवेश लेना था। केवल बालिकाओं की शिक्षा देने वाली संस्थाओं की संख्या इस अवधि में 16,814 से बढ़कर 18,671 तक पहुँच गयी जबकि अध्ययनरत बालिकाओं की संख्या इस अवधि में क्रमशः 64.7 लाख से 93 लाख तक पहुँच गयी जो कि लगभग 42.6 प्रतिशत थी।
वर्ष 1951-1956 योजना काल में स्त्री-शिक्षा के विकास हेतु सरकार द्वारा पारित कानूनों तथा वैवाहिक जीवन में मधुरता तथा समरसता बनाये रखने के लिए 1955 में बना ‘हिन्दू विवाह अधिनियम’ और 1952 में बना ‘विशेष विवाह अधिनियम’ मुख्य हैं जिसमें अन्तर्जातीय विवाह को वैध घोषित किया गया तथा वर व कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु 21 व 18 वर्ष निश्चित की गयी। 1954 में जब यू. जी. सी. बिल संसद में पेश किया गया तो मिस जयश्री तथा श्री डी.सी. शर्मा ने महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी विद्यालयों में प्रवेश, शिक्षकों की भर्ती आदि समस्त पहलुओं पर समान रूप से नामित किया जाना चाहिए।
योजना आयोग द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना काल में महिला शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था की गयी क्योंकि महिला शिक्षकों के अभाव में शिक्षा का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा था। इय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली स्त्रियों के लिए मकान आदि की सुविधाएँ दिये जाने पर विशेष ध्यान दिया गया। बालिकाओं को शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ एवं विभिन्न राज्यों में स्त्रियों को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी-
(1) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों के लिए निःशुल्क आवासीय व्यवस्था ।
(2) स्कूलों में आया की नियुक्ति हेतु व्यवस्था ।
राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958) को हम दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जानते हैं महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य स्त्री-शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए सुझाव देना था।
समिति ने 1959 में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये –
(1) कुछ वर्षों तक बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता तथा स्त्रियों के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
(2) ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री-शिक्षा के विकास हेतु सरलीकृत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
सन् 1983 में बना आपराधिक दण्ड संहिता अधिनियम तथा महिला का अश्लील प्रस्तुतीकरण विरोध कानून, 1986 का प्रचार प्रसार तेज करना चाहिए। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि जितना विशाल यह कार्य है, उसके लिए यही पर्याप्त नहीं है कि इस क्षेत्र में केवल सरकारी मशीनरी ही कार्य करे. इसके लिए यह भी आवश्यक है कि स्वयंसेवी संस्थाएँ आगे आयें और स्त्रियों को उन कानूनों के प्रावधानों से अवगत करायें जिनके लाभ उन्हें मिल सकते हैं।
बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निम्नलिखित उपाय सुझाये गये—
(1) बालिकाओं की शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण करना।
(2) औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा के लिए सुविधाएँ बढ़ाना।
(3) वर्तमान कार्यक्रम का विस्तार एवं अनेक सहायता कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया जाये जिससे बालिकाओं का स्तर बढ़ाया जा सके।
प्रोफेसर राममूर्ति समिति (1991) के बालिका शिक्षा पर निम्नलिखित सुझाव हैं—
(1) अध्यापिकाओं की अधिक-से-अधिक नियुक्ति की जाये।
(2) विद्यालयों में पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल विकास का समावेश किया जाये।
(3) विभिन्न स्तरों पर महिला अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना की जाये।
इकाई – IV
प्रश्न 8 (i) शैक्षिक अवसरों की समानता के सन्दर्भ में स्त्री-शिक्षा का वर्णन कीजिए।
अथवा
भारतीय शिक्षा में स्त्री-सशक्तिकरण के लक्ष्यों का वर्णन कीजिए।
अथवा
बालिका शिक्षा हेतु प्रेरणा का वर्णन कीजिए।
ANSWER–
शैक्षिक अवसर की समानता की बात करते समय अनेक सन्दर्भों में असमानता पायी जाती है। बालिका को हम समाज में वह दर्जा नहीं दे पाते जो बालक को देते हैं। जन्म के बाद बालक-बालिका में कुछ लोग भेद करते हैं। बालिकाओं को समाज का एक वर्ग पढ़ाना ही नहीं चाहता है यदि पढ़ने भेज देता है तो बीच में ही पढ़ाई को रोक देता है। वर्तमान में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति निम्न प्रकार है-
महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करना शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्रता से ही एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। 1951 तथा 1981 के बीच महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता 7.93 प्रतिशत से बढ़कर 24.82 प्रतिशत हो गयी है तथापि काफी संख्या में इस अवधि के दौरान निरक्षर महिलाओं की संख्या (असोम को छोड़कर) 15.87 करोड़ से बढ़कर 24.17 करोड़ हो गयी है। निरक्षर जनसंख्या में से महिलाएँ 57 प्रतिशत हैं तथा स्कूल स्तर पर दाखिल न किये गये बच्चों में से 70 प्रतिशत लड़कियाँ हैं। अब तक किये गये प्रयासों के बावजूद शिक्षा प्रणाली महिलाओं की समानता के प्रति पर्याप्त योगदान नहीं कर सकी है।
लक्ष्य —
(क) लड़कियों के प्रति प्रारम्भिक शिक्षा का समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम, विशेषकर 1990 तक प्राथमिक स्तर तक तथा 1995 तक प्रारम्भिक स्तर तक ।
(ख) 1995 तक 15-35 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए (जिनकी संख्या 68 करोड़ आँकी गयी है) प्रौढ़ शिक्षा का एक समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम ।
(ग) व्यावसायिक, तकनीकी, वृत्तिक शिक्षा तथा विद्यमान और उभरती प्रौद्योगिकी में महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाना।
भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत में वर्ष 2001 में 102 करोड़ 70 लाख 15 हजार और 257 व्यक्ति थे, उनमें से 49.57 करोड़ स्त्रियाँ थीं। भारत में स्त्रियों में साक्षरता 54.1% है जबकि पुरुषों में यह 75.9% है। मुस्लिम और घुमन्तू समुदायों की स्त्रियों में असाक्षरता दर अन्य धार्मिक समुदायों से कहीं अधिक है। ग्रामीण स्त्रियों में शहरी स्त्रियों की अपेक्षा असाक्षरता दर बहुत अधिक है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्त्रियों में असाक्षरता दर बहुत अधिक है। 1996 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित National Policy on Education 1986- Programme of Action में यह स्वीकार किया गया था कि शिक्षा व्यवस्था स्त्रियों की समानता की दिशा में पर्याप्त योगदान नहीं कर पायी है। अतः सरकार ने इस दिशा में निम्नांकित कार्य करने की नीति बनायी-
(1) लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा की योजना बनायी जाये।
(2) स्त्रियों के लिए (आयु वर्ग 15-35 जिनकी संख्या 1995 तक अनुमानतः 6.8 करोड़ होने वाली थी) प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम बनाया जाये।
(3) लड़कियों/स्त्रियों को व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा दिलवायी जाये।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह प्रस्तावित किया था कि भारतीय स्त्रियों की दशा में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को हस्तक्षेप करना होगा। यह तय किया था कि-
(1) शिक्षा को हस्तक्षेप करने की भूमिका (Interventionist role) निभानी होगी।
(2) पाठ्यक्रमों और पुस्तकों की पुनः रचना करनी होगी जिससे नये मूल्यों का विकास हो सके।
(3) व्यावसायिक, तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा में स्त्रियों के प्रवेश का विस्तार किया जायेगा।
स्त्रियों का सशक्तीकरण –
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह कहा गया कि भारतीय स्त्रियों का सशक्तीकरण करना होगा जिसके निम्नांकित लक्ष्य या आवश्यक तत्त्व होंगे-
* स्त्रियों में एक धनात्मक स्वचित्रण और आत्मविश्वास का निर्माण करना (Building a positive self-image and self-confidence)।
* उनमें आलोच्य ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना ( Developing ability to think critically)।
* सामूहिक एकता का निर्माण करना और उनमें निर्णय लेने और कार्य करने की शक्ति का निर्माण करना (Building up group cohesion and fostering decision-making and action)।
सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में समान भागीदारी को सुनिश्चित करना उपर्युक्त स्त्री सशक्तीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए NBP 1986- Programme of Action में निम्नांकित कदमों को उठाने पर जोर दिया गया था-
1. प्रत्येक शिक्षा संस्थान 1995 तक महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम करेगा।
2. सभी शिक्षकों और अनौपचारिक/प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों (Instructors) को स्त्री सशक्तीकरण के अभिकर्ता (Agents of women Empowerment) बनने के लिए प्रशिक्षण प्रदान
किया जाना चाहिए। सभी सम्बन्धित शीर्ष शिक्षा संस्थाएँ और SCERT, DIET, SRC, UGC आदि ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करेंगे |
3. अनौपचारिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा की शिक्षिकाओं और अनुदेशिकाओं को विशेष प्रकार से प्रशिक्षण देना होगा ताकि वे महिला समानता की दिशा में एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभा सकें।
4. पाठशालीय स्तर तक स्त्री शिक्षकों को नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।
5. स्त्रियों की नयी पदस्थिति के अनुसार Common Core Curriculum में आवश्यक मूल्यों का समावेश किया जायेगा। एन. सी. ई. आर. टी. का महिला प्रकोष्ठ (Women’s Cell) इस दिशा
में विशेष कार्यक्रम करेगा
6. NIEPA (National Institute of Educational Planning and Administration) और राज्य स्तरीय सभी उपयुक्त संस्थाएँ शिक्षकों, प्रशिक्षकों, आयोजकों (Planners) और प्रशासकों की
स्त्रियों की समस्याओं के बारे में चैतन्यता बढ़ायेंगे।
7. विश्वविद्यालयों में महिला-अध्ययन केन्द्र (Women Studies Centres) खोले जायेंगे।
सुझाव–
शिक्षा के द्वारा स्त्रियों का सशक्तीकरण होना सम्भव है। इसके लिए लेखिका के निम्नांकित महत्त्वपूर्ण सुझाव हैं—
* पाँचवीं कक्षा तक कौशलों का प्रशिक्षण (Skill training) दिया जाना चाहिए।
* माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को निम्नांकित विषयों को चुनने देना चाहिए— गृह अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, फाइनेंसियल एकाउण्टिंग, फ्लोरीकल्चर, पोटरी और सेरेमिक्स, कम्प्यूटर कुशलताएँ, शिशु देख-रेख व शिक्षा, टेलीफोन, फैक्स, इन्फॉर्मेशन सेण्टर, डॉक्यूमेण्टल वर्क को कर पाना, टूरिज्म, गाइडेंस और काउंसलिंग, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेण्ट बुकिंग काउण्टर बालकों के क्लब, ब्यूटीशियन कोर्स, साइंटिफिक टेम्पर डवलपमेण्ट कोर्स, एडवरटाइजिंग. इन्स्ट्रक्शन एण्ड प्रिपरेशन यूनिट्स, रिपेयर एण्ड मेण्टीनेंस ऑफ इलैक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एण्ड सेल्स प्रमोशन यूनिट्स, लाइब्रेरी कार्य आदि।
* एक अलग निदेशालय की स्थापना हो जिसका कार्य स्त्रियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रमों की आयोजना, प्रबन्धन, मूल्यांकन करना और उपयुक्त डिप्लोमा प्रदान करना होना चाहिए।
प्रश्न 8 (ii) महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले प्रयास एवं आवश्यक सुझाव दीजिए।
अथवा
लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले प्रयास एवं आवश्यक सुझाव दीजिए।
अथवा
महिलाओं के विशेष संदर्भ में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।
Answer–
लड़कियों को प्रोत्साहित करने वाले सरकारी प्रयास निम्नलिखित हैं—
1. भारत में कई राज्यों में प्राथमिक स्तर तक, कुछ में माध्यमिक स्तर तक, कुछ में उच्च माध्यमिक स्तर तथा कुछ में कॉलेज स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का सरकारी प्रावधान लागू किया गया है। हरियाणा में 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा को निःशुल्क बनाया गया है। आप अपने राज्य के द्वारा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने हेतु दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में सरकारी शिक्षा विभाग में मुख्य कार्यालयों व जिला कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करें।
2. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पाठशालाओं की छात्राओं को होस्टल तथा बोर्डिंग (भोजन) की सुविधाएँ केन्द्रीय सरकार की ओर से दी जा रही हैं। अनुसूचित जातियों/जनजातियों की छात्राओं के लिए प्रतिवर्ष प्रति छात्रा रु. 10,000 होस्टल व बोर्डिंग के रूप में अनुदान दिया जाता है और पुस्तकों, फर्नीचर, बर्तनों, मनोरंजन के साधनों के लिए एकमुश्त सहायता भी दी जाती है।
3. दिनांक 23 सितम्बर, 2005 के ‘The Times of India’ में यह समाचार छपा था कि दिनांक सितम्बर, 2005 को भारत सरकार ने यह महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है कि—
* प्रत्येक परिवार की एकमात्र लड़की को कक्षा VI से XII तक निःशुल्क शिक्षा (Free Education) वर्तमान सत्र 2005-06 से प्राप्त हो पायेगी।
* सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली (CBSE) से मान्यता प्राप्त सभी पाठशालाओं को प्रत्येक ऐसी छात्रा की पूरी फीस माफ करनी पड़ेगी जो अपने माता-पिता की एकमात्र लड़की है।
* विश्वविद्यालय आयोग (UGC) को भी ऐसी व्यवस्था करने को कहा गया है कि उससे सम्बद्ध प्रत्येक कोर्स व कॉलेज को एक परिवार की एकमात्र लड़की को, जो उस संस्था/कोर्स की छात्रा है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी।
* ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स की ऐसी छात्रा को, जो अपने परिवार की एकमात्र लड़की है, स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) प्रदान की जायेगी।
• मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सों को छोड़कर अन्य सभी ग्रेजुएट कोर्सों में रु. 500 प्रतिमाह की स्कॉलरशिप ऐसी छात्रा को दी जायेगी और मेडिकल या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की छात्रा को रु. 1000 प्रतिमाह की स्कॉलरशिप मिलेगी तस्था इनके पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स की छात्रा को रु. 2000 प्रतिमाह की स्कॉलरशिप मिलेगी।
उपर्युक्त सुविधाओं का व्यय उन संस्थाओं को स्वयं वहन करना होगा।
(CBSE) बारहवीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम के आधार पर 550 स्कॉलरशिपें (प्रत्येक रु. 500 प्रतिमाह की) अण्डरग्रेजुएट स्तर (बी. ए. स्तर) तक संस्था ऐसी छात्रा को प्रदान करेगी।
आवश्यक सुझाव –
लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं-
1. ‘दी टाइम्स ऑफ इण्डिया’ दिनांक 19 सितम्बर, 2005 में छपे समाचार के अनुसार नई दिल्ली की एक प्रगतिशील संस्था FICCI Ladies Organization ने ‘Towards Education for Every Girl Student: Issues and Challenges’ विषय पर एक पेनल डिस्कशन सितम्बर, 2005 में आयोजित किया था। उसमें अग्रांकित महत्त्वपूर्ण सुझाव विद्वानों द्वारा दिये गये थे-
“शिक्षा, जीवन तथा समाज को परिवर्तित करने का एक साधन हैं। यदि शिक्षा अभिनति (Biases) या राग-द्वेष से लड़ने के लिए आपको तैयार करती है तो इसके पाठशालाओं में और अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति करके तथा स्थानीय लोगों को पाठशालाओं की देखभाल करने की शक्तियाँ देकर लड़कियों की शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। यदि स्थानीय क्षेत्र के लोगों- विद्यार्थियों के माता-पिता, सेवानिवृत्त अधिकारियों, स्त्रियों आदि की एक कमेटी बनायी जाये और एक पाठशाला में शिक्षिकाओं की नियुक्ति और वहाँ के अन्य कार्यों को करवाने में उनको शामिल किया जाये, तो विद्यार्थियों की शिक्षा में बेहतरी होगी।”
उक्त पेनल वार्तालाप में ध्यान आकर्षित कराया गया कि निम्नांकित कारक लड़कियों की शिक्षा में अवरोधक (रुकावट) का कार्य करते हैं-
• प्रायः घरों से पाठशालाएँ काफी दूरी पर हैं, लड़कियों को उन तक पहुँचना कठिन होता है
• लड़कियों को अपने घर पर छोटे भाई-बहनों की देखभाल (Sibling care) करनी पड़ती है।
• कई विद्यालयों और अधिकतर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लड़कियों के साथ यौन- सम्बन्धी छेड़छाड़ की जाती है और उनके यौन शोषण का प्रयास (बलात्कार आदि) होता है जिसमें न केवल
पुरुष विद्यार्थी अपितु पुरुष शिक्षक, प्रशासक और अन्य कर्मचारी होते हैं। इस प्रकार की यौन प्रताड़ना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई वर्षों पूर्व यह आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों और पाठशालीय शिक्षा विभागों में यौन प्रताड़ना को रोकने के लिए एक कमेटी बनायी जानी अनिवार्य है जो महिला-विद्यार्थियों व महिला शिक्षकों की यौन प्रताड़नाा सम्बन्धी सभी शिकायतों को सुने और निर्णय करके व दण्ड प्रदान करने की सिफारिशें उच्च अधिकारी को दे। सभी शिक्षा संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है, उसे बनाया जाना चाहिए।
• किशोर आय वर्ग की तथा वयस्क छात्राओं और शिक्षिकाओं को छेड़छाड़ करने वाले तथा यौन प्रताड़ना देने वालों से सुरक्षित होने के लिए आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि आजकल सभी स्थानों पर ऐसी असामाजिक घटनाएँ बढ़ रही हैं। दिल्ली राज्य के शिक्षा विभाग ने वर्ष 2005 में कई पाठशालाओं की युवा शिक्षिकाओं को एक ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करवाया है। उस प्रशिक्षण को ‘प्रोजेक्ट रक्षा’ नाम दिया गया है।
• यह हर्ष का विषय है कि आज भारत में प्रत्येक धर्म, जाति, समुदाय के लोग लड़कियों को पढ़ाने के इच्छुक
हैं और प्रयत्नशील हैं और केन्द्रीय व राज्य सरकारें और कई गैर-सरकारी संगठन (NGOs) भी उनके लिए कई उपयोगी कार्यक्रम और योजनाएँ चला रहे हैं। इनके फलस्वरूप आज भारतीय लड़कियाँ सभी क्षेत्रों व व्यवसायों में आशानुसार प्रगति कर रही हैं और सफलताएँ प्राप्त कर रही हैं। सभी लड़कियों को ऐसी सुविधाएँ दिलवायी जानी चाहिए। लड़कियों के सशक्तीकरण होने से ही महिलाओं का सशक्तीकरण हो सकता है।
प्रश्न 8 (iii) बालिका शिक्षा हेतु प्रमुख आयोगों का वर्णन कीजिए।
अथवा स्वतन्त्रता के उपरांत स्त्री-शिक्षा हेतु आयोगों का अवलोकन कीजिए।
ANSWER-
स्वतन्त्र भारत में नारी की सामाजिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है। जिन बन्धनों में वह बँधी हुई थी, वे शनैः-शनैः ढीले होते जा रहे हैं। जिस स्वतन्त्रता से उसे वंचित कर दिया गया था, वह उसे पुनः प्राप्त हो रही है। उसके सम्बन्ध में पुरुषों का दृष्टिकोण बदल रहा है, उनकी मान्यताएँ भी बदल रही हैं। ‘भारतीय संविधान’ ने भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया है— “राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।”
स्वतन्त्रता के उपरांत स्त्री-शिक्षा के विकास हेतु प्रमुख आयोगों का वर्णन निम्नलिखित है— स्वतन्त्रता के पश्चात् डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग 1948 ई. को नियुक्त हुआ जिसने स्त्री-शिक्षा को पर्याप्त महत्त्व दिया—
(1) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948)
इस आयोग के द्वारा स्त्री-शिक्षा के विकास के लिए निम्न सुझाव दिये गये—
(i) स्त्रियों के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाये।
(ii) स्त्रियों के पाठ्यक्रम को पुनर्गठित किया जाये।
(iii) स्त्रियों को सुयोग्य गृहिणी तथा सुमाता बनाने की शिक्षा दी जाये।
(iv) स्त्रियों के लिए गृह अर्थशास्त्र तथा गृह प्रबन्ध का प्रबन्ध किया जाये।
(2) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53 )
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्त्री-शिक्षा के विकास के लिए निम्न सुझाव दिये-
(i) 11 से 16 वर्ष की आयु की बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
(ii) बालिकाओं के लिए गृह-विज्ञान के शिक्षण की सुविधायें प्रदान की जायें।
( 3 ) स्त्री-शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति
सन् 1958 ई. में केन्द्रीय सरकार ने ‘स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति की । इस समिति की अध्यक्षा दुर्गाबाई देशमुख थीं। स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में समिति ने निम्न सुझाव दिये-
(i) स्त्री-शिक्षा को राष्ट्र की प्रमुख समस्या मानकर उसको वरीयता प्रदान की जाये।
(ii) केन्द्र सरकार स्त्री-शिक्षा के व्यय को वहन करे और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करे।
(iii) केन्द्रीय सरकार स्त्री-शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक योजना का निर्माण करें और इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करे। कोठारी आयोग (1966)
इस आयोग ने स्त्री-शिक्षा के समबन्ध में अपने अग्रलिखित सुझाव दिये हैं—
(1) स्त्री तथा पुरुषों की शिक्षा में, किसी प्रकार की विषमता नहीं होनी चाहिए। दोनों को विकास के लिए समान अवसर तथा सुविधायें प्रदान की जायें।
(2) लड़कियों तथा महिलाओं को भी विज्ञान के अध्ययन की प्रेरणा देनी चाहिए।
(3) गृह-विज्ञान तथा ललित कला महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए।
(4) बालिकाओं को व्यावसायिक प्रबन्ध एवं प्रशासन की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाय ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) तथा स्त्री-शिक्षा
महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करना शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। 1951 तथा 1981 के बीच महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता 7.93 प्रतिशत से बढ़कर 24.82 प्रतिशत हो गई है। अब तक किये गये प्रयासों के बावजूद शिक्षा-प्रणाली महिलाओं की समानता के प्रति पर्याप्त योगदान नहीं कर सकी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की समानता के लिए निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये-
1. लड़कियों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा का समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम ।
2. सन् 1995 तक 15-35 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा का एक समयबद्ध- चरणबद्ध कार्यक्रम।
आचार्य राममूर्ति समिति (1990) तथा स्त्री-शिक्षा
आचार्य राममूर्ति समिति ने महिला शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नांकित महत्त्वर्ण सिफारिशें की हैं-
1. शिशु देखभाल तथा शिक्षा केन्द्र प्राथमिक विद्यालयों के समीप स्थापित किये जाने चाहिए, साथ ही इनकी समयावधि को विद्यालयों की समयावधि के साथ समायोजित किया जाय।
2. कक्षा 1 से 3 का पाठ्यक्रम शिशु शिक्षा केन्द्रों के अनुकूल बनाया जाय।
3. आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों तथा विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित किया जाय।
4. 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जायें। महिला समाख्या (1989)
महिला समाख्या के उद्देश्य
इस कार्यक्रम के निम्नांकित उद्देश्य हैं—
1. महिलाओं की आत्मछवि एवं आत्मविश्वास को बढ़ाना।
2. ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाएँ वह ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सकें जो उन्हें समाज में रचनात्मक भूमिका निभाने में सहायता दे सकें।
3. प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण तथा भागीदारी वाला तरीका स्थापित करना।
महिला संघ वह केन्द्र-बिन्दु है जहाँ सभी गतिविधियों की योजना बनायी जाती है और जहाँ महिलाएँ मिल-बैठकर अपनी समस्याओं पर विचार करती हैं। दो या अधिक महिलाओं के दल को, जिसे सखी या सहायकी कहा जाता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये दल महिलाओं को एकत्र करने, संगठित करने का कार्य करते हैं और संघ में विचार-विमर्श को बढ़ावा देते हैं। संघ के लिए निर्धारित राशियाँ बैंक/डाकखाने में जमा की जाती हैं। इस धन का उपयोग महिलाओं के द्वारा तीन वर्ष तक सामूहिक कार्यों के लिए किया जाता है। सहयोगिनियाँ जो दस गाँवों के समूह को देखती हैं, संघ के प्रेरक, समर्थक एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं।
प्रश्न 9 (i) लिंग असमानता की चुनौतियों में पाठ्यक्रम की भूमिका का विवेचन कीजिए।
ANSWER-
कक्षाओं में कुछ शिक्षाविदों का मत है, पाठ्यक्रम में लिंग के आधार पर अन्तर रखना चाहिए। पाठ्यक्रम में लिंग असमानता के प्रश्न पर श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद् द्वारा नियुक्त समिति ने विशेष रूप से जाँच की। कोठारी आयोग ने इस समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया है-
1. जिस प्रजातन्त्रात्मक और समाजवादी आदर्श पर आधारित समाज की कल्पना की गई है, उसमें शिक्षा ऐसी व्यक्तिगत क्षमताओं, अभिवृत्तियों और रुचियों से सम्बन्धित होगी जिसका वास्तव में लिंग-भेद से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः ऐसे समाज की शिक्षा के लिए लिंग-भेद के आधार पर पाठ्यक्रम में अन्तर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
2. वर्तमान संक्रमणकारी अवस्था में पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच मनोवैज्ञानिक अन्तर और इस अन्तर पर आधारित सामाजिक कार्यों के विभाजन को स्वीकार करना होगा तथा बालक- बालिकाओं के पाठ्यक्रम निर्माण का व्यावहारिक आधार बनाना होगा। ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना होगा कि कालान्तर में जो मूल्य एवं अभिवृत्तियाँ अत्यावश्यक हैं, उनका स्त्रियों एवं पुरुषों में अत्यधिक निर्माण हो रहा है और ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे वर्तमान अन्तर हमेशा बना रहे या अधिक हो जाए।
कोठारी आयोग ने इन सुझावों पर सहमति प्रदान की और कहा कि कक्षा दस तक के छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए।
आयोग ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया है—
1. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान पाठ्यक्रम एक ऐच्छिक विषय होगा। यह एक सर्वप्रिय विषय है फिर भी इसे बालिकाओं के लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए।
2. संगीत तथा ललित कला भी बालिकाओं के प्रिय विषय हैं। माध्यमिक स्तर पर इन विषयों की शिक्षा की सामान्य व्यवस्था है। इन विषयों को विस्तृत पैमाने पर सिखाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
3. गणित एवं विज्ञान महत्त्वपूर्ण विषय हैं और विश्वविद्यालय स्तर पर उनसे सम्बन्धित विशिष्ट पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त तैयारी होनी चाहिए। अतः बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर गणित तथा विज्ञान पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने और इन विषयों की शिक्षिकाएँ तैयार करने के सम्बन्ध में विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।
विद्यालयीय पाठ्यक्रम में लिंग असमानता की चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए-
1. बालिकाओं की भूमिका को उभारना चाहिए और इतिहास में महिला लिंग की छवि को सकारात्मक रूप से व्यक्त करना चाहिए। विशेष रूप से भारतीय समाज के सन्दर्भ में महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलनों में दिये गये उनके योगदानों की चर्चा करना आवश्यक है। ऐसे सभी विषयों को अध्यापकों और प्रशासकों के प्रशिक्षण तथा नवीनीकरण में सावधानी से सम्मिलित किया जाना चाहिए।
2. बालिकाओं में गणित तथा विज्ञान शिक्षा को अधिक प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। बालिकाओं के स्कूलों में गणित तथा विज्ञान को आज की अपेक्षा अधिक महत्त्व देना चाहिए।
3. बालक तथा बालिकाओं की पाठ्यवस्तु में अन्तर रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
4. ऐसी आधारभूत कानूनी सहायता तथा सूचनाएँ जो बच्चों तथा महिलाओं को संरक्षण प्रदान करती हों तथा उनके अधिकारों से उन्हें परिचित कराना चाहिए। शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
5. बालिकाओं का कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें विद्यालय में रोकने की योजनाएँ बनानी चाहिए।
6. कक्षाओं के पाठ्यक्रम में लिंग सम्बन्धी पाठ्यवस्तु को सम्मिलित करना चाहिए।
7. पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालिकाओं को आत्मरक्षा के उपायों की जानकारी दी जानी चाहिए।
8. कक्षा दस तक बालिकाओं को किसी-न-किसी हुनर में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कक्षा 6 से 8 के मध्य होना चाहिए।
प्रश्न 9 (ii) कक्षा में जेण्डर की समानता के लिए किये जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए।
अथवा
कक्षा में लिंग समानता के लिए किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए।
ANSWER-
मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट सन् 1995 के अनुसार महिला शिक्षा, महिला समानता तथा महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के वर्तमान कार्यक्रम तथा उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं-
(1) बालिकाओं के नामांकन तथा उन्हें कक्षा में रोके रखने पर बल दिया जा रहा है।
(2) ग्रामीण अध्यापिकाओं की नियुक्ति तथा पाठ्यचर्या से लैंगिक पक्षपात को हटाये जाने पर बल दिया जा रहा है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के संशोधित नीति-निर्धारण में यह शर्त है कि भविष्य में नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों में कम से कम 50% महिलाएँ होंगी।
(3) मन्त्रालय ने अनौपचारिक शिक्षा की योजना के अन्तर्गत 90% सहायता ऐसे केन्द्रों को दी है जो केवल बालिकाओं के लिए हैं। केवल बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा सह- शिक्षा वाले अनौपचारिक केन्द्रों के अनुपात को 25:75 से बढ़कर 40:60 करके हाल ही में इस योजना को संशोधित किया गया है जिससे बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए और अधिक सुविधाएँ प्राप्त हों और वे अधिक शिक्षित हो सकें।
(4) बालिकाओं को विद्यालय (IX से XII) से रोके रखने हेतु छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की एक योजना प्रारम्भ की गई है। कक्षा IX से XII की छात्रावासों में रह रही छात्राओं के भोजन, फर्नीचर, बर्तन, मनोरंजन सम्बन्धी सामग्री आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस योजना में 3.580 बालिकाओं को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।
(5) यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत प्रयास किये जायेंगे कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों में से एक-तिहाई बालिकाएँ अवश्य हों।
(6) सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों में महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों में महिलाओं का नामांकन सामान्यतः हर स्थान पर 60% से अधिक है।
(7) उच्च शिक्षा के सामान्य तथा तकनीकी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों में असाधारण वृद्धि हुई है। समाज, उद्योग और व्यापार की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वविद्यालय तथा कॉलेज स्तर पर महिला शिक्षा को उनके अनुकूल बनाया गया है। उच्च शिक्षा के कुल नामांकन में महिलाओं का नामांकन जो वर्ष 1992-93 में 15.90 लाख था सन् 1993-94 के प्रारम्भ में 16.64 लाख हो गया। स्नातकोत्तर स्तर पर छात्राओं का नामांकन सम्पूर्ण नामांकन का 34.9 प्रतिशत था।
(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को लैंगिक समानता, महिलाओं के स्वावलम्बन, बालिका शिक्षा, जनसंख्या सम्बन्धी पहलुओं, मानवाधिकार आदि के क्षेत्र में शोध परियोजना प्र करने, पाठ्यचर्या, प्रशिक्षण और विस्तार का विकास करने के लिए सामाजिक और शैक्षिक विकास के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में अध्ययन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित
करने के लिए वित्तीय सहायता देता आ रहा है।
(9) महिला समाख्या (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा) डच सहायता से अप्रैल, सन् 1989 में प्रारम्भ की गई। इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश इन चार राज्यों में 15 जिलों में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 1752 ग्रामों को सम्मिलित किया जा चुका है। पेयजल तक पहुँच, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, जवाहर रोजगार योजना में आरक्षण सुनिश्चित होना तथा घरेलू एवं सामाजिक हिंसा से जुड़ी समस्याओं से निपटने में महिलाएँ सक्षम हो गई हैं। गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश के जिलों में महिला समाख्या ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में उल्लिखित भूमिका निभाई है। कर्नाटक में महिला समाख्या का केन्द्रबिन्दु देवदासी की कुप्रथा का समाप्त करना तथा स्वास्थ्य देख-रेख रहा है। उत्तर प्रदेश में पेयजल तथा अनौपचारिक शिक्षा, आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक न्याय तथा सरकारी योजनाओं तक पहुँच तथा गुजरात में साक्षरता मुख्य बिन्दु रहे हैं।
(10) +2 स्तर पर केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्यमशीलता पर बल देते हुए व्यावसायिक कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं।
(11) तकनीकी और व्यावसायिक धारा में भी महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। इन्जीनियरों और प्रौद्योगिकी धाराओं में (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा पॉलिटेक्निकों में) भी छात्राओं की संख्या मात्र 40 (0.3%) थी जो वर्ष 1993-94 में 78.3 हजार (13.1%) हो गई।
प्रश्न 9 (iii) लिंगीय समानता हेतु किये गये प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए ।
अथवा
लैंगिक समानता हेतु विभिन्न शासकीय योजनाओं का उल्लेख करें।
लिंगीय समानता हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक इत्यादि क्षेत्रों में गम्भीरतापूर्वक किया गया है। लिंग की समानता हेतु कुछ योजनाएँ निम्न प्रकार हैं-
1. लैंगिक समानता हेतु संविधान का दृढ़ संकल्प। संविधान की धारा 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29 के द्वारा स्त्री तथा पुरुष दोनों की समानता हेतु उपबन्ध किये गये हैं।
2. संविधान की धारा 45 के द्वारा 14 वर्ष तक के बालकों तथा बालिकाओं की अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।
3. स्वतन्त्रता के पश्चात् गठित आयोगों तथा समितियों, जैसे— राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, हंसा मेहता समिति इत्यादि द्वारा स्त्री शिक्षा और समानता के लिए शिक्षा हेतु सारगर्भित सुझाव दिये गये हैं।
4. स्त्री-शिक्षा के पाठ्यक्रम को जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक बनाने के लिए योजना का निर्माण । 5. लिंगीय समानता हेतु निःशुल्क शिक्षा, छात्रावासों की व्यवस्था, छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन ।
6. सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बालिका शिक्षा पर बल देकर लिंगीय समानता हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
7. पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना द्वारा स्त्री-शिक्षा के प्रसार और लिंगीय समानता की योजना पर कार्य किया जा रहा है।
8. महिलाओं, बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वालों को सरकार द्वारा सहायता तथा प्रोत्साहन प्रदान करना।
9. महिलाओं की शिक्षा द्वारा ही वे समानता का अधिकार पा सकती हैं इसीलिए बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा का प्रसार अधिक हो सके, अतः मानकों में भी कुछ ढील दी गयी है।
10. पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा योजनाबद्ध रूप से महिलाओं की शिक्षा और समानता के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
11. सातवीं पंचवर्षीय योजना द्वारा कार्यरत मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए ‘सचल शिशु सदनों’ की स्थापना की गयी है, जिससे लिंगीय समानता में वृद्धि होगी।
12. लिंगीय समानता हेतु महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण राजनीति में प्रदान किया गया है। 13. महिलाओं को मुख्य धारा में लाने और आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए नौकरियों में भी उनको आरक्षण प्रदान किया जा रहा है
14. कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश प्रदान करके उन्हें पुरुषों के समकक्ष खड़ा किया जा रहा है।
15. समान कार्य हेतु समान वेतन प्रदान करके महिला समानता और लिंगीय विभेदों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
16. लिंगीय समानता के लिए महिला थानों तथा 24 x 7 महिला हैल्प लाइन की व्यवस्था की गयी है।
17. महिलाओं को स्वस्थ बनाने, मातृ तथा शिशु मृत्यु-दर में कमी कर लिंगीय समानता को सुनिश्चित करने हेतु CARE, NHRM इत्यादि के द्वारा योजनाएँ चलायी जा रही हैं।
18. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2006 के द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने तथा लिंगीय समानता के प्रयास किये गये हैं।
19. धारा 366, 494, 498, 498 (a), 306, 294, 509,376, 313 इत्यादि के द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने पर सख्त सजा का प्रावधान करके लिंगीय समानता के लिए प्रयास किया गया है।
20. लिंगीय भेदभावों को कम करके महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु 1985 में ‘महिला समाख्या’ कार्यक्रम का प्रारम्भ किया गया, जिसके द्वारा ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा तथा उनको अधिकार सम्पन्न करने का ठोस कार्यक्रम बनाया गया। ‘महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा’ के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जागरूक करने, उनमें आत्मविश्वास की भावना भरने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश तथा असोम के 9,000 गाँवों में किया गया। इस योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार थे-
(i) महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि करना ।
(ii) ऐसे वातावरण का सृजन करना जहाँ महिलाएँ ज्ञान और सूचनाएँ प्राप्त कर सकें।
(iii) महिलाओं की औपचारिक तथा औपचारिकेतर शिक्षा कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करना।
(iv) शिक्षा प्रदान कर महिलाओं को समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने में मदद देना। इन नीतियों के परिणामस्वरूप 1981 में जहाँ देश में लगभग चार करोड़ बालिकाएँ अध्ययनरत थीं, वहीं 1991 में इनकी संख्या बढ़कर 6.2 करोड़ हो गयी। स्त्री-पुरुष के मध्य लिंगीय भेदभाव को कम करने में इस योजना का योगदान सराहनीय है।
21. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया, उन जिलों में जहाँ स्त्रियों की साक्षरता दर कम है।
22. जुलाई, 2004 से कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना (KGBVP) का प्रारम्भ किया। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन होने पर उन्हें 75% आरक्षण प्रदान किया जायेगा, बाकी का 25% प्रतिशत स्थान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं के लिए आरक्षित रहेगा। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर मुस्लिम आबादी को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे 86 विद्यालय प्रारम्भ किये जायेंगे। दसवीं पंचवर्षीय योजना के तथा राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात से वित्तीय खर्च वहन करेंगी। यह योजना 20 राज्यों में गयी है। आन्ध्र प्रदेश ने अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए 94 विद्यालयों की स्थापना की, झारखण्ड और मध्य प्रदेश द्वारा क्रमशः 74 और 70 विद्यालय खोले गये।
प्रश्न 9 (iv) भारत में बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों का मूल्यांकन कीजिए।
ANSWER–
बालिकाओं की शिक्षा के लिए निम्न कार्यक्रम हैं-
‘समानता की ओर’ रिपोर्ट 1975
यह रिपोर्ट “Towards Equality” जो कि CSWI द्वारा प्रस्तुत की गई थी, महिलाओं के अधिकारों पर विमर्श में एक ऐतिहासिक दस्तावेज थी। इसने समाज की विभिन्न आर्थिक स्तर की महिलाओं के विभिन्न अनुभवों द्वारा उनके जीवन में व्याप्त असमानताओं पर जोर दिया। इसने निष्कर्ष दिया कि महिलाओं की उत्पादक भूमिका को विभिन्न नीतियों में कोई ध्यान नहीं दिया गया जिससे उनकी आवश्यकताओं को भी अनदेखा किया गया। समिति ने जोर दिया कि सामाजिक वास्तविकताओं, मूल्यों एवं अभिवृत्तियों के अनुरूप औपचारिक शिक्षा ने किसी भी परिवर्तन को जन्म नहीं दिया, बल्कि आजादी के उपरान्त शिक्षा ने वर्ग संघर्ष को और गहरा ही किया है।
समिति ने ‘महिलाओं के लिये प्रासंगिक ज्ञान’ देने के विचार पर भी प्रश्न उठाया है। महिलाओं * की स्थानीय तथा विशिष्ट आवश्यकताओं के सम्बन्ध से ज्ञान की परिभाषा को व्यापक बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा को महिलाओं को घरेलू जिन्दगी के लिये तैयार करने के उद्देश्य ने महिलाओं के उत्पादक क्षेत्रों में उनकी महत्त्वपूर्ण भागीदारी को नकारा है।
श्रम शक्ति रिपोर्ट (1988) या (National Commission on Self Employed Women and Women of the Informal Sector) ये पहली समिति थी जिसने अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका एवं भागीदारी को स्पष्ट किया। इस क्षेत्र की महिलाओं की विशिष्ट एवं विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इसने शिक्षा की आवश्यकता महसूस की थी। कमीशन ने महसूस किया कि समानता के लिये सबको समान अवसर प्रदान करने के साथ ही सफलता के लिये जरूरी परिस्थितियाँ भी मुहैया कराई जानी चाहिये। इसने सुझाव दिया कि ग्रामीण बच्चों के पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक बनाया जाये तथा उन्हें इतिहास व विज्ञान के साथ ही प्रायोगिक विषय जैसे पशुपालन तथा पशु देखभाल जैसे विषय भी पढ़ाये जा सकते हैं। महिलाओं को केन्द्र में लाने के लिये पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया जाना चाहिये।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (National Policy on Education) एक महत्त्वपूर्ण डॉक्यूमेंट साबित हुआ क्योंकि इसने राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के पुनः संगठन की बात की जिससे “महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभायी जा सके…..तथा पुनः संशोधित पाठ्यक्रम, पुस्तकों, शिक्षकों के प्रशिक्षण, नीति-निर्माताओं आदि के द्वारा नये मूल्य का विकास किया जायेगा तथा विश्वास एवं सामाजिक पुनर्निर्माण किया जायेगा।”
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE 1986) ने नारी आन्दोलनों के आलोक में अपना विजन प्रस्तुत किया जिसने “शिक्षा को महिलाओं के स्तर में मूलभूत परिवर्तन लाने वाले कारक रूप” में स्वीकार किया। NPE के सुझावों के आधार पर पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया गया। एन.सी.ई.आर.टी ने भी पाठ्यक्रम के जरिये जेन्डर समानता लाने हेतु अध्यापक हैंड बुक्स की सीरिज जारी की।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) के बाद की पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि संशोधन बहुत नाममात्र के एवं दिखावटी ही अधिक थे।
शैक्षिक तथा विशेषकर पाठ्यक्रमीय प्रक्रियाओं में लड़कियों की शिक्षा के लिये कोई विशेष परिवर्तन नहीं किये गये थे और न ही जेन्डर एवं समानता के मुद्दों को ही देखा गया था। रा. शि. नीति की पुनरावलोकन (NPE Review Committee) समिति ने चिन्हित किया कि यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने जेन्डर समानता को शिक्षा में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया था फिर भी “स्कूल शिक्षा के सन्दर्भ तथा प्रक्रिया” वाले पूरे अध्याय में ‘जेन्डर’ के बारे में कुछ नहीं कहा गया सिवाय इसके कि 10 कोर पाठ्यक्रम क्षेत्र में एक ‘सेक्स की समानता’ (equality of the sexes) होगा। वास्तव में रिव्यू कमेटी ने सुझाव दिया कि समस्त पाठ्यक्रम में जेन्डर दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से होना चाहिए यहाँ तक छिपे पाठ्यक्रम (Hidden Curriculum) में भी।
इस प्रकार देखने में आता है कि भारत में शिक्षा नीतियों में जेन्डर तथा स्कूली ज्ञान पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया, जबकि सभी ने पाठ्यपुस्तक रिवीजन (पुनर्लेखन) पर जोर दिया है। हालाँकि पाठ्यपुस्तकों को महिलाओं की उपलब्धियों का विवरण देते हुए तथा दिखाई देने वाले जेन्डर बायस (gender bias) को हटाते हुये पुनर्लेखन करने का अधिक महत्त्व नहीं है। फिर भी 1970 के बाद ऐसा पाया गया कि शिक्षा के केवल विकास के सन्दर्भ से देखने के नजरिये में फर्क पड़ा है तथा शिक्षा को अब जेन्डर समानता लाने हेतु वाद-विवाद को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में 3 देखा जाने लगा है। हालाँकि नीतियाँ इस बारे में अधिक प्रकाश नहीं डालतीं कि इस प्रकार के दृष्टिकोण से कितना गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन आया है।
शिक्षा में जेन्डर मुद्दे पर नीतियों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ पाया है। सम्भवतः इसका कारण महिला आन्दोलनों एवं अध्ययनों का शिक्षा क्षेत्र के मुद्दों से बाहर रहना है। महिला आन्दोलनों ने भी अपना ध्यान अधिकतर जमीनी मुद्दों; जैसे—स्वास्थ्य, हिंसा तथा जीवनयापन के मुद्दों पर ही केन्द्रित रखा। महिला कार्यकत्ताओं ने मुख्य धारा के स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकताओं पर शायद ही कभी ध्यान दिया हो। महिला अध्ययन भी अधिकतर महिला आन्दोलनों से ही काफी हद तक जुड़े रहे तथा किसी भी नियोजित तरीके से शिक्षा विभाग से नहीं जुड़े। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा में इन मुद्दों पर केवल औपचारिक रूप से ही विचार किया गया तथा किसी भी प्रकार का व्यावहारिक जुड़ाव नहीं दिखाई पड़ता । शिक्षा में इस बात पर कभी विचार नहीं किया गया कि इन मुद्दों से किस प्रकार वर्तमान में जारी व्यवहारों एवं कार्य करने की शैली में व्यावहारिक बदलाव लाया जा सकता है। इसलिये सशक्तीकरण का विचार शिक्षा क्षेत्र के केन्द्रीय महत्व में न परिलक्षित होकर किशोर लड़कियों तथा महिलाओं के लिये महिला समाख्या जैसे कार्यक्रम के निर्माण में दिखता है।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
भारत में बाल लिंगानुपात (0-6 आयु वर्ग) में गिरावट की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 1991 में बाल लिंगानुपात 945 था, जो वर्ष 2001 में 927 जबकि वर्ष 2011 की जनगणना में अपने न्यूनतम स्तर 918 तक पहुंच गई है। समाज में कन्या भ्रूण हत्या की कुरीति को जड़ से खत्म करने व बेटियों को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के प्रयास के तहत भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रलाय की संयुक्त पहल के रूप में देश के 100 निम्न लिंगानुपात वाले जिलों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से प्रारंभ किया। गया। योजना की सफलता को देखते हुए वर्तमान में यह योना भारत के समस्त जिलों तक विस्तारित हो चुकी है।
उद्देश्य-
(i) लिंग आधारित भेदभाव तथा लिंग चयन का उन्मूलन
(ii) बालिकाओं की उत्तरजीविता और सुरक्षा सुनिश्चित करना
(iii) बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करना
लक्ष्य—कार्यक्रम के प्रथम फेज में आठ लक्ष्य चुने गए थे। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—
1. निम्न बाल लिंगानुपात वाले चयनित 100 जिलों में एक वर्ष में जन्म लिंगानुपात (SRB: Sex Ratio at Birth) में 10 अंकों की वृद्धि लाना ।
2. माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को वर्ष 2013-14 के 76 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2017 के अंत तक 79 प्रतिशत करना।
3. 5 वर्ष से कम आयु की न्यून भार (Under Weight) तथा रक्ताल्पता पीड़ित बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना ।
4. कम बाल लिंगानुपात वाले 100 जिलों के प्रत्येक स्कूल में वर्ष 2017 तक महिला शौचालयों की व्यवस्था करना।
5. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में ‘लैंगिक अंतराल’ को वर्ष 2011 के 8 अंक से कम करके वर्ष 2017 तक 4 अंक तक पहुँचाना।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के विस्तार के साथ-साथ इसके लक्ष्यों को भी विस्तारित किया गया। वर्तमान में इस योजना के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं-
1. चयनित जिलों में एक वर्ष में जन्म के समय लिंगानुपात में दो अंकों का सुधार करना।
2. प्रत्येक वर्ष बाल मृत्यु-दर (पांच वर्ष से कम आयु) में 1.5 अंक की कमी लाना।
3. प्रति वर्ष संस्थागत प्रसव में 1.5% की वृद्धि करना।
4. वर्ष 2018-19 तक माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाकर 82% करना।
5. प्रत्येक स्कूल में शौचालय की व्यवस्था करना।
6. बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार करते हुए 5 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं में रक्ताल्पता एवं कम भार की समस्या में कमी लाना।
जिलों के चयन के मापदंड
प्रथम चरण में जिलों के चयन में तीन मापदंड अपनाए गए थे, परंतु वर्तमान में योजना के अंतर्गत समस्त 640 जिलों (2011) को सम्मिलित कर लिया गया है। प्रथम 100 जिलों के चयन का आधार इस प्रकार था-
(i) 87 जिलों को उन 23 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से चुना गया था, जिनका बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था।
(ii) 8 जिलों को उन 8 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से चुना गया था, जिनका बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से तो अधिक था, परंतु उसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही थी।
(iii) 5 जिलों को उन 5 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से चुना गया था, जिनका बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक था और उसमें सुधार की प्रवृत्ति देखी जा रही थी, इनके चुनाव का प्रमुख कारण देश के अन्य हिस्सों को प्रेरणा प्रदान करना था।
बजट – यह योजना वर्ष 2014-15 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार, 100 करोड़ रूपये की आरंभिक राशि द्वारा शुरू की गई थी। वर्ष 2018-19 के बजट में इस योजना हेतु 280 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वर्ष 2017-18 के लिए इस योजना हेतु आवंटित राशि (200 करोड़ रुपये) की तुलना में 40% अधिक है।
प्रगति-यह कार्यक्रम बाल लिंगानुपात के गिरते स्तर को रोकने हेतु एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के कुछ सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में पहली बार बाल लिंगानुपात में वृद्धि देखने को मिली है। इसी अवधि में राजस्थान में भी बाल लिंगानुपात में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई, जो कि वर्ष 2001 के 909 से गिरकर वर्ष 2011 में 888 पर आ गई थी।
7 मार्च, 2018 को जारी आधिकारिक आंकड़ों में वर्ष 2015-16 से 2016-17 की अवधि में 104 चयनित जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार दर्ज किया गया। इसी अवधि में 146 जिलों में संस्थागत प्रसव की स्थिति में सुधार भी देखा गया।
विश्लेषण – स्वस्थ एवं प्रगतिशील समाज हेतु अनिवार्य शर्तों में संतुलित लिंगानुपात भी है। भविष्य में संतुलित लिंगानुपात के स्तर को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब वर्तमान में बाल लिंगानुपात में संतुलन हो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान भारत में बेटियों के संरक्षण एवं अनेक सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है। इसके तहत जागरूकता के माध्यम से भविष्य के भारत के निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। निश्चित रूप में इसका दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
प्रश्न 9 (v)बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु किये गये प्रयासों को रेखांकित कीजिए।
अथवा
भारत में राज्यों ने बालिका शिक्षा हेतु किस-किस प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की है? स्पष्ट कीजिए।
ANSWER–
स्वतन्त्रता के बाद से ही भारतीय समाज में बालिका-शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। बालिका- शिक्षा के महत्त्व को स्वीकारते हुए राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा भी बालिका-शिक्षा हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं। दिसम्बर, 2002 में हुए 86वें संविधान संशोधन के उपरान्त 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राष्ट्रीय संकल्प भारत के प्रत्येक बालक-बालिका का एक मूल अधिकार बन गया है।
सर्व शिक्षा अभियान (SSA) सबके लिए शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को साक्षर करने के सरकारी प्रयत्नों का एक केन्द्रीय तत्त्व विद्यालय जाने वाली या विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं तक शिक्षा की पहुँच को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम शिक्षा के लिए न केवल शिक्षा-प्रणाली में वरन् सामाजिक मान्यताओं व दृष्टिकोणों में व्यापक परिवर्तन लाने के महत्त्व व आवश्यकताओं को स्वीकार करते हैं। इसी कारण अब भारत के सभी राज्यों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु द्वि-बिन्दु प्रयत्न किए जा रहे हैं-
(1) प्रथम, लड़कियों की शिक्षा तक पहुँच व ठहराव को विभिन्न प्रकार के उपाय करके बढ़ाया जा रहा है।
(2) द्वितीय, प्रशिक्षण व अभिप्रेरण के द्वारा समाज में लड़कियों की शिक्षा की माँग को सृजित किया जा रहा है।
सभी को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक योजनाओं का नियोजन व कार्यान्वयन किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं-
(1) विद्यालय त्याग चुकी बालिकाओं हेतु स्कूल की ओर अभियान चलाना ।
(2) बालिकाओं के लिए समरूप अधिगम अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षकों को संवेदनशील बनाना।
(3) विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति व ठहराव के सुनिश्चित करने के लिए नवाचारी उपाय करना।
(4) विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय बनवाना ।
(5) अधिक उम्र वाली बालिकाओं हेतु ब्रिज पाठ्यक्रम चलाना ।
(6) जन समर्थन व सहयोग प्राप्त करने के लिए सघन अभियान चलाना ।
(7) कक्षा 8 तक सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें देना ।
(8) पाठ्य-पुस्तकों सहित सभी शिक्षण अधिगम सामग्री को यौन संवेदनशील बनाना।
सर्व शिक्षा अभियान के साथ-साथ प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम. महिला समाख्या, पूर्व बाल्यकाल परिचर्या व शिक्षा एवं एकीकृत बाल विकास सेवा जैसे विविध कार्यक्रमों के द्वारा कन्या-शिक्षा के विविध पक्षों को सुदृढ़ करके बालिकाओं तक शिक्षा के प्रकाश को पहुँचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पूर्व बाल्यकाल परिचर्या व शिक्षा जहाँ बालिकाओं को अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल से विमुक्त करके उनके विद्यालय जाने व वहाँ रुकने का मार्ग प्रशस्त करता है, वहाँ एकीकृत बाल विकास सेवा के द्वारा आँगनबाड़ी कार्यकर्मियों, प्राथमिक स्कूल शिक्षकों व स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करके पूर्व विद्यालय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। प्रारम्भिक स्तर पर बालिका-शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई है जिनका मुख्य उद्देश्य दुर्गम क्षेत्र विशेषतः अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों की शिक्षा के लिए गुणवत्तापरक आवासीय शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। सभी कार्यक्रमों का केन्द्रीय पक्ष है— वस्तुतः समाज में बालिका-शिक्षा की माँग को सृजित करना, बालिका शिक्षा में जनसमुदाय विशेषकर महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना तथा बालिका-शिक्षा को सुनिश्चित करने वाले दबाव कारकों को उत्पन्न करना।
इस कार्य में समाज, माता-पिता की अभिप्रेरणा व सजगता, विद्यालय क्रियाकलापों व समितियों में महिलाओं व माताओं की बढ़ती भूमिका व स्कूल शिक्षकों व समुदायों के परस्पर सम्बन्ध का सुदृढ़ीकरण जैसे उपाय आवश्यक व महत्त्वपूर्ण हैं। केन्द्र व राज्यों को सरकारों के इन प्रयत्नों से हमारे देश में बालिका-शिक्षा का तीव्र गति से प्रसार हुआ है।
लिंग विद्यालय एवं समाज BOOK -1 PDF
लिंग विद्यालय एवं समाज BOOK -2 PDF
(3) लिंग विद्यालय एवं समाज पिछले साल के प्रश्न
LING VIDYALALAY EVAN SAMAAJ QUESTION
| विषय | लिंग विद्यालय एवं समाज प्रश्न
Ling vidyaalay evan Samaaj Question Paper |
| SUBJECT | Gender, School and Society Question |
| पेपर कोड | 103 |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय |
| कोर्स | बी.एड |
| सेमेस्टर | प्रथम |
| FULL MARKS | |
| lnfo | यहाँ महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड प्रथम सेमेस्टर के पेपर -103 लिंग विद्यालय एवं समाज प्रश्न दिया गया है | |