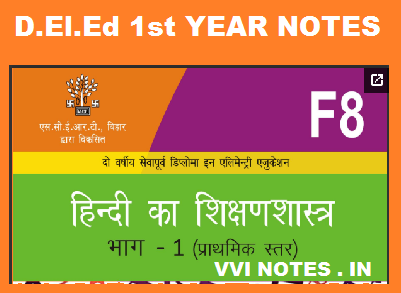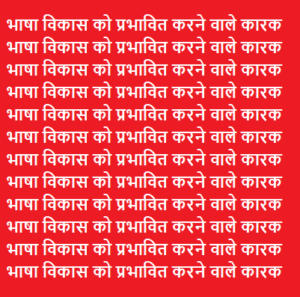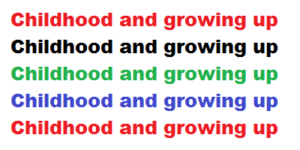हिंदी का शिक्षण शास्त्र -1 (प्राथमिक स्तर )
Hindi Ka Shikshan Shastra -1 (Parathmik Star )
| विषय | हिंदी का शिक्षण शास्त्र -1 (प्राथमिक स्तर ) |
| SUBJECT | Hindi Ka Shikshan Shastra -1 (Parathmik Star ) |
| COURSE | BIHAR D.El.Ed. 1ST YEAR |
| PAPER CODE | F-8 |
VVI NOTES के इस पेज में बिहार डी.एल.एड 1st ईयर पेपर F-8 ” हिंदी का शिक्षण शास्त्र -1 (प्राथमिक स्तर ) ” से सम्बन्धित महत्वपर्ण प्रश्नों के उत्तर जोड़े गये है | साथ ही इस विषय से सम्बन्धित नोट्स, बुक, गाइड के pdf भी सामिल किया जयेगा |
हिंदी का शिक्षण शास्त्र -1 (प्राथमिक स्तर ) नोट्स
महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर
(01 ) प्रश्न – भाषा, लिपि तथा हिंदी भाषा की प्रकृति को परिभाषित करें।
उत्तर –
भाषा –
भाषा शब्द संस्कृत के ‘भाष’ धातु से बना है। जिसका अर्थ है- बोलना । कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता-पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार, छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान-प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु-पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता ।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान-प्रदान करता है।
दूसरे शब्दों में – जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावो को समझ सके उसे भाषा कहते है। यह उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग भावों, विचारों का आदान प्रदान करते हैं।
लिपि –
लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग । ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, वही लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीजें होती हैं। भाषा वो चीज होती है जो बोली जाती है, लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है -लिखित या चित्रित करना । ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, वही लिपि कहलाती है। हिन्दी की लिपि देवनागरी है। हिन्दी के अलावा -संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएँ भी देवनागरी में लिखी जाती है।
प्रकृति- मानव स्वभाव की तरह भाषा का भी अपना स्वभाव होता है। उसका यह स्वभाव प्रकृति, भौगोलिक परिवेश, जीवन पद्धति, ऐतिहासिक घटनाक्रम, सामाजिक, सांस्कृतिक और विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले विकास आदि के अनुरूप बनता और ढलता है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण-अवगुण होते है। भाषा एक सामाजिक शक्ति है, जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूवर्जो से सीखता है और उसका विकास करता है।
भाषा की प्रकृति निम्नलिखित है
क. सामाजिकता- भाषा के लिए समाज का होना आवश्यक है। समाज के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः भाषा एक सामाजिक संस्था है ।
ख. अर्जन – भाषा संस्कार रूप में ग्रहण करते है। व्यक्ति अनुकरण, व्यवहार, अभ्यास से भाषा को ग्रहण करता है।
ग. परिवर्तनशीलता – भाषा निरंतर परिवर्तनशील रहती है। कुछ परिवर्तन प्रयोग से घिसने तथा बाहरी प्रभाव के कारण आते हैं।
घ. गतिशीलता – भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। वह सदा गतिमान रहकर विकास करती है। भाषा को ‘बहता नीर’ कहा गया है।
ड़. कठिनता से सरलता की ओर- भाषा कठिन से सरलता की ओर चलती है। कठिन लगने वाली ध्वनियां भाषाओं में कम होती है। आदमी आसानी चाहता है। कम से कम शब्दों में काम चलाना चाहता है।
च. भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सीमा- प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा किसी विशेष काल से आरंभ होकर इतिहास के निश्चित काल तक व्यवहार में रहती है ।
छ. निजी संरचना – प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग-अलग होती है। लिंग, वचन, कारक के अतिरिक्त वाक्य गठन आदि क्षेत्रों में हर एक भाषा अपनी निजी विशेषता लिए होती है, आदि।
प्रश्न (02) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 के विशेष सन्दर्भ में हिन्दी भाषा शिक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डालें।
उत्तर- प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में उसकी मातृभाषा की अमूल्य और आध रभूत भूमिका होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 विशेष रूप से इसे मानती है। साथ ही हिंदी भाषा के उद्देश्यों के समझ भाषाई कौशलों (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) के समुचित विकास के लिए प्रयत्नशील है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 के विशेष सन्दर्भ में हिन्दी भाषा शिक्षण के उद्देश्य
1.भाषा शिक्षण बहुभाषी होना चाहिए। केवल कई भाषाओं के शिक्षण के अर्थ में ही नहीं बल्कि रणनीति तैयार करने के लिहाज से भी ताकि बहुभाषी कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जाए। इससे उच्च स्तरीय भाषा कौशल का हिंदी में सरलतापूर्वक स्थानांतरण किया जा सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम विद्यालय स्तर पर यथासंभव प्रयास करें जिससे भाषा में सतत् शिक्षा को पूर्णत: विकसित किया जा सके।
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने माना है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे अपनी भाषाई ज्ञान को आरंभ में विद्यालय परिवार के साथ थोड़ी झिझक के साथ रखते हैं। इसका कारण है विद्यालय और उनके परिवेश की भाषा के बीच का मानक स्तर। इस भाषाई विविधता और बहुभाषिकता का उपयोग एक भाषा शिक्षक विभिन्न क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों की मदद से बच्चों के भाषाई कौशलों को विकसित करने के संदर्भ में कर सकता है।
3. गैर हिंदी भाषी राज्यों में बच्चे हिंदी सीखते हैं। हिंदी प्रदेशों के मामले में बच्चे वह भाषा सीखें जो उस इलाके में नहीं बोली जाती है।
4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आलोक में हिंदी शिक्षण का उद्देश्य तनाव से मुक्त, सुरक्षित और भयहीन होना चाहिए। जिससे बच्चे की अधिगम प्रक्रिया उसके स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधित ना कर सके। बच्चे की भाषा कौशलों का विकास इस स्तर पर समृद्ध होना चाहिए जिससे कि वे अपने परिवेश को आसानी से समझ सकें, आदि ।
विचारों के आदान-प्रदान के लिए मनुष्य निम्न चार प्रकार की क्रियाएँ करता हैं सुनना, बोलना,और लिखना। आदान अर्थात् ग्रहण करना, सीखना। प्रदान अर्थात् अभिव्यक्ति करना।
आदान में सुनना व पढ़ना क्रिया होती है।
प्रदान में—बोलना तथा लिखना क्रिया होती है।
इन चारों क्रियाओं में (सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना) कुशलता अर्जित करना ही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ये ही भाषा के मूल उद्देश्य कहलाते हैं।
A. सुनना:
1. भाषा के सभी ध्वनि-रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझना ।
2. विषय-वस्तु में आए विचारों, भावों, घटनाओं, तथ्यों आदि में प्रसंगानुसार सम्बन्ध स्थापित करने हुए समझना ।
3. विषय-वस्तु, केन्द्रीय भावों, प्रमुख विचारों और निष्कर्षों को समझना।
4. सुनने के शिष्टाचार का पालन करने की क्षमता का विकास करना।
शिष्टाचारपूर्वक सुनने में बालक की निम्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक स्थिति होती है—
1. श्रोता बालक वक्ता की ओर मुँह करके बैठे।
2.श्रोता चुपचाप ध्यानपूर्वक अर्थग्रहण करते हुए सुनें।
3. सुनते समय मुँह फेरकर बैठना, साथी से वार्तालाप, वाद-विवाद नहीं करें।
4. श्रोता वक्ता के सम्मान का ध्यान रखें।
5. वक्ता को अनावश्यक परेशान न करे।
B. बोलना :
1. शुद्धता, स्पष्टता, उतार-चढ़ाव व उचित हाव-भाव का निर्वाह करते हुए समूह में अलग से सहज रूप में प्रभावी ढंग से बोलने की क्षमता का विकास करना।
2. परिचित विषय, घटना तथा परिस्थिति का अपने ढंग से वर्णन/विवरण करने की क्षमता का विकास करना।
3.समय-समय पर प्रसंगानुसार बोलने के शिष्टाचार का पालन करते हुए मौलिक रूप से तर्कपूर्ण विचार प्रकट करने की क्षमता का विकास करना।
4. अभिनय अथवा भूमिका निर्वाह करते हुए पात्रानुसार संवाद बोलने के कौशल का विकास करना।
C. पढ़ना:
1.भाषा तत्वों को प्रसंगानुसार विश्लेषण करते हुए समझना।
2. विषय-वस्तु में आए विचरों, भावों, घटनाओं, तथ्यों आदि में प्रसंगानुसार सम्बन्ध स्थापित करते हुए सझना।
3. विषय-वस्तु के सारांश, केन्द्रीय भावों और निष्कर्षों को समझना ।
4. मुद्रित व हस्तलिखित सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित यति-गति, आरोह-अवरोह, विराम-चिह्नों के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हुए स्वाभाविक रूप से वाचन करने की क्षमता का विकास करना ।
5.बाल शब्दकोश को समझने की क्षमता का विकास करना।
6. स्तरानुकूल पाठ्येत्तर कहानियाँ, सचित्र पुस्तकें आदि साहित्य को समझकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना।
D. लिखना:
1. अक्षरों व शब्दों के सही आकार, उचित क्रम, पर्याप्त अन्तर को समझने-लिखने की क्षमता का विकास करना।
2. देखकर और सुनकर सुस्पष्ट सुन्दर, शुद्ध रूप में उचित विराम चिह्नों का ध्यान रखते हुए लिखने की क्षमता का विकास करना ।
3. सरल प्रारूपों, प्रार्थना-पत्रों, निबन्ध, वर्णन, विवरण आदि को सरल अनुच्छेदों में रचना करते हुए लिखने की क्षमता का विकास करना।
4. मौलिक रूप से तथा तर्कपूर्ण ढंग से सरल वर्णन, विवरण, निबन्ध, प्रश्नोत्तर, सारांश, कहानी, कविता, आदि को लिखने की क्षमता का विकास करना।
////////////
प्रश्न – सुनने और बोलने का अर्थ बच्चों के भाषायी कौशल के विकास के संदर्भ में स्पष्ट करें।
अथवा
भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने के महत्व की चर्चा कीजिए।
उत्तर –
सुनना –
जब हम स्वयं या अन्य कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो हम उसके द्वारा उच्चारित ध्वनियों, वाक्यों संवादों आदि का श्रवण करते हैं। यह प्रक्रिया सुनना कहलाती है। सुनना मात्र कही गई बातों को श्रवण कर लेना नहीं है, बल्कि सुनकर उस कहे गए कथन के प्रति एक संप्रत्यय के साथ समझ स्थापित करना है। बच्चे विद्यालय आने के पूर्व से ढेरों शब्दों के बारे में सुनकर उनके प्रति अपने मन में एक छवि विशेष का निर्माण कर लेते हैं। भाषा शिक्षण में सुनना और बोलना काफी हद तक एक दूसरे पर निर्भर है।
बोलना —
जब हम किसी बात/शब्द को सुनकर उसके विषय में कोई विचार बना कर अपनी अभिव्यक्ति को शाब्दिक / मौखिक रूप से प्रकट करते हैं यह प्रक्रिया बोलना कहलाती है। बोलने के क्रम में कई प्रकार की मानसिक संक्रियाएं होती है- विचारों का निर्माण, तर्कों की खोज करना, वैचारिक क्रमबद्धता, शब्द निर्माण, वाक्यों का सही चयन, ध्वनियों का उचित अनुमान, शारीरिक हावभाव आदि ।
सुनना और बोलना शारीरिक रूप से सक्षम होने पर एक स्वाभाविक गुण है। पर भाषाई दक्षता के दृष्टि से मात्र बोल लेना या सुन लेना पर्याप्त नहीं है जब तक इसके साथ ‘समझ’ भी ना जुड़ी हो। अर्थात सुनकर ‘समझना’ और समझकर ‘बोलना’ ही भाषाई कौशल कहलाते हैं। समझ के बिना सुनने और बोलने का कोई अर्थ नहीं होता। उदाहरण के लिए हम किसी अपरिचित भाषा में कही गई बात को सुन तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते तो क्या कहा जा सकता है कि हम उस भाषा को सुनने का कौशल नहीं रखते? इसी प्रकार बिना सोचे समझे कुछ भी अनर्गल प्रलाप करना भी बोलना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना तो सुनने वाले को और ना ही बोलने वाले को पता होता है कि वह क्या बोल रहा है? उसका आशय क्या है?
सुनना और बोलना मौखिक रूप से अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौशल है। बच्चे एक-दूसरे की बातों को सुनते-सुनते ही बोलने का प्रयास करते हैं और इसी प्रक्रिया में धीरे-धीरे अपने विचारों और भावों (अपनी आवश्यकताओं को भी) व्यक्त करने लगते हैं। सुनने और बोलने की सामान्य परस्पर प्रक्रिया बातचीत कहलाती है। इसी के अन्य रूप चर्चा, परिचर्चा, भाषण, वाद-विवाद, संगोष्ठी आदि के रूप में देखने को मिलते हैं। ये सब बच्चों में सुनने-बोलने के कौशल विकास में सहायक होते हैं।
भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कौशल सुनना है। अगर किसी भाषा को हम सीखना चाहते हैं तो उसे सुनने और बोलने का मौका मिलने पर हम आसानी से उस भाषा को सीख सकते हैं। इसके लिए बच्चे को कहानी सुनने और बालगीत सुनने और बोलने का मौका दिया जा सकता है। इससे बच्चे के मन में हिंदी भाषा का व्याकरण अपने आप बनता जाएगा।
किसी घटना का वर्णन, क्लास के दोस्तों के साथ बातचीत, कहानी कहना, नाटक आयोजित करना, बातचीत (संवाद), सवाल-जवाब सत्र, शब्दों का खेल, डिबेट प्रतिस्पर्धा, गीत व संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन। खुद से सीखने की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को उनकी रुचि की किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित आदि करने में सुनने और बोलने के कौशल शामिल होते हैं। इसके अलावा भाषा शिक्षण में चित्रों वाली किताबों का उपयोग, ऐसे जो संवाद और बातचीत पर आधारित हों सुनने और बोलने के कौशल का विकास कर बच्चों की भाषा को समृद्ध करते हैं। अतः भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने के कौशल से संबंधित ऐसी गतिविधियां बच्चों के भाषाई कौशल विकास के लिए बहुत उपयोगी साबित होती हैं।
प्रश्न 11. सुनने और बोलने को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें ।
उत्तर –
प्रत्येक व्यक्ति का श्रवण कौशल भिन्न -भिन्न होता है। निम्नलिखित कारकों से सुनने का कौशल प्रभावित होता है –
क. भाषिक ध्वनियों का ज्ञान ना होना सुनना की सुनने की क्रिया को प्रभावित करता है |
ख. शब्दावली पर अधिकार न होना सुनाए गए विषयों के समझने में बाधक होता है।
ग. क्रम को समझने की योग्यता ना होने से घटना, कहानी सुनने में विषय से संबंध बनाने और सुनकर समझने में सहायता नहीं मिलती है।
घ. स्मरण योग्यता न होने से क्रम को समझने में कठिनाई होती है।
ड़. उपयुक्त वातावरण सुनने की क्षमता को बढ़ाता है और अनुपयुक्त वातावरण बाधक बनता है।
च. अरुची और उदासीनता श्रवण में बाधा उत्पन्न करते हैं।
छ. अस्वस्थता के कारण सुनने के प्रति अनिच्छा, शिथिलता होती है।
ज. श्रोता एवं वक्ता के बीच तालमेल, विश्वास ना होने पर सुनने की क्रिया सार्थक नहीं होती है।
झ. श्रोता के अनुभव के दायरे में विषय को कहने / समझने की संभावना सुनने को सहज बनाती है।
ञ. वक्ता के मनोभावों, उद्देश्य, प्रयोजन, को समझ पाना ‘सुनने’ को समझने की शर्त है ।
ट. सुनने को संभव बनाने के लिए श्रोता को ‘परिचित’ विषय से ‘अपरिचित’ विषय की ओर जाना, समझाना श्रवण कौशल को प्रभावित करता है।
ठ. श्रोता के व्यक्तित्व में धैर्य, ग्रहणशीलता का गुण ना होना सुनने की क्रिया को प्रभावित करता है।
ड. श्रवण इंद्रियों में दोष सुनने की क्रिया में बाधक होता है
ढ. शिक्षक के अशुद्ध उच्चारण का शिक्षार्थी पर गलत प्रभाव पड़ता है। अतः उसका उच्चारण शुद्ध और मानक होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी को प्रेरणा मिले।
बोलने के कौशल का विकास सुनने के द्वारा ही होता है। सुनने के कौशल में कमी या बाधा रह जाने पर बोलने के कौशल का विकास भी प्रभावित होता है। बोलने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन निम्नलिखित हैं।
क. शुद्ध उच्चारण करने में सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल हो पाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसके भाषा संबंधी कौशल में निखार आता है।
ख. मस्तिष्क की बनावट भी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। भाषा बोलने तथा समझने के लिए स्नायु तन्त्र, तथा वाक-यन्त्र की आवश्यकता होती है। बहुत हद तक इनकी बनावट तथा कार्य शैली तथा स्नायु नियन्त्रण भाषा को प्रभावित करते हैं।
ग. भाषा सम्बन्धी बोलने के कौशल विकास पर व्यक्ति जिस स्थान और परिस्थिति में रहता है, आचरण करता है, विचारों का आदान-प्रदान करता है उससे बोलने का विकास होता हैं। उदाहरण स्वरूप निम्न श्रेणी के परिवार व समाज के लोगों में भाषा का विकास कम होता है क्योंकि उन्हें दूसरों के सम्पर्क में आने का अवसर कम मिलता है, इसी प्रकार परिवार में कम व्यक्तियों के होने पर भी भाषा संकुचित हो जाती है।
घ. ऐसे बहुत से व्यवसाय हैं जिनमें भाषा का प्रयोग अत्यधिक होता है। उदाहरणस्वरूप अध्यापन, वकालत, व्यापार कुछ ऐसे व्यवसाय है जिनमें बोले बिना कोई कार्य नहीं चल सकता। अतएव वातावरण के अन्तर्गत इनको भी सम्मिलित किया गया है।
ड़. ध्वनि की मात्राओं के ज्ञान में कमी, सही उच्चारण बोध में अपूर्णता, दोषपूर्ण श्रवण शक्ति, अशुद्ध वर्तनी लिखकर याद रखना, ध्वनि के अनुसार उतार-चढ़ाव, सुर, बलाघात आदि का प्रयोग ना कर पाना, कुशल और दक्ष मार्गदर्शन में कमी, मौखिक (मुँह के अंगों) में दोष बोलने को प्रभावित करते हैं।
च. बालक द्वारा स्वयं यंत्रों पर नियंत्रण ना रख पाने के कारण भाषा दोष उत्पन्न होता है। जैसे ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्रता स्पष्ट वाणी आदि ।
प्रश्न 12. प्राथमिक स्तर के बच्चों के सुनने और बोलने की क्षमताओं का विकास किस प्रकार करेंगे?
उत्तर –
प्राथमिक स्तर के बच्चों को सुनने और बोलने की क्षमताओं का विकास निम्नलिखित प्रकार से करेंगे
क. कक्षा में आज की बात, बातचीत, अपने बारे में बात करना, स्कूल अनुभवों पर बात करना ।
ख. आंखों देखी घटना या सुनी हुई घटनाओं के बारे में अभिव्यक्ति करना ।
ग. बालगीत, कविता सुनना-सुनाना –
कविता अपने आप को अभिव्यक्त करने तथा जीवन से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। नियमित रूप से कविताएं और गीत सुनकर बच्चे भाषा की बुनियादी संरचनाएं ग्रहण कर लेते हैं। जैसे- कविता में आए नए शब्दों का अर्थ पकड़ लेते हैं, कविता के लय को बिना बिगाड़ के तुकबंदी भी कर लेते हैं। साथ ही कविता बच्चों को अपने अनुभवों से भी जोड़ती है। अगर एक ही कविता दो अलग-अलग बच्चों द्वारा पढ़ी जाएगी तो दोनों ही उस कविता को अपने-अपने अनुभवों से जोड़ते हुए समझेंगे।
घ. कहानी सुनना सुनाना – कहानियां सुनना-सुनाना प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को भाषा सीखने में बहुत मदद करता है। कहानी सुनना बच्चों के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ उनके सृजनात्मकता को भी बढ़ाने वाला होता है। कई बार बच्चे सुनी हुई कहानी में मनचाहा बदलाव करके अपने मित्रों को सुनाते हैं। इसके द्वारा बच्चे ना केवल शब्दों के अर्थ बल्कि विभिन्न घटनाओं को भी समझने लगते हैं और साथ ही यह बच्चों की कल्पनाशीलता को भी बढ़ाती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कहानियां उनको भावी जीवन के लिए तैयार करने में भी मददगार होती है।
ड़. चित्र वर्णन – चित्र एक ऐसा माध्यम है जिससे हम प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के साथ बातचीत एवं चर्चा की बहुत सारी संभावनाएं खोज सकते हैं। छोटी कक्षाओं में बच्चों को चित्रों में बहुत ही रुचि होती है और उन्हें चित्र देखने और बनाने में मजा आता है। किसी किताब में चित्र सबसे पहले बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। उनके साथ चित्र पर सहज बातचीत करना आसान होता है। बच्चे चित्रों का बारीकी से अवलोकन भी करते और उस पर सारी बातचीत भी करते हैं। चित्रों से जुड़े प्रश्न बच्चों को चीजों को ढूंढने, उनके बारे में तर्क करने, कल्पना करने, भविष्यवाणी करने व चीजों और घटनाओं का अपने अनुभवों से संबंध बैठाने के लिए प्रेरित करते हैं |
च. रोलप्ले करवाना –
अभिनय को रोजमर्रा की कक्षा की गतिविधि में शामिल करने से बच्चों को आजादी और आनंद की अनुभूति होती है। इसके लिए प्राथमिक स्तर पर किसी ऐसी घटना, कहानी या कार्टून को लिया जा सकता है जो बच्चे अपने आसपास देखते हैं नाटक में बच्चों को स्वयं छोटे-छोटे समूह में नाटक के विषय चुनने, उसके संवाद लिखने एवं अभिनय करने से बच्चों में भाषाई क्षमता बढ़ेगी व उनका शब्द भंडार समृद्ध होगा ।
छ. दिए गए शब्दों से कहानी सुनाना
ज. सुने हुए विचारों को संक्षिप्त व विस्तारित कर पाना
झ. परिचित समसामयिक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना
ञ. बच्चों को कहानी, कविता, नाटक आदि रचने, उसे बढ़ाने तथा प्रस्तुत करने के अवसर देना, इत्यादि ।
प्रश्न 13. हिंदी भाषा सीखने के संकेतकों को सुनने, बोलने और पढ़ने के संदर्भ में स्पष्ट करें।
उत्तर –
संकेतक –
संकेतक का शाब्दिक अर्थ है – चिह्न, सूचक । अर्थात जो किसी विशेष कार्य अथवा बात की ओर इंगित करें उसे संकेतक कहते हैं। इस प्रकार सीखने के संकेतक से अभिप्राय ऐसे प्रतिमानों, सूचकों से है, जो सीखी गई बात अथवा कार्य की ओर इशारा करें। दूसरे शब्दों में सीखने के संकेतक शिक्षण-अधिगम (सीखने-सिखाने) प्रणाली एवं सीखने की प्रक्रिया में आई प्रगति के चिह्न रूप है
संकेतक एवं पाठ्यक्रम एक दूसरे से पूर्णतया संबद्ध है। वस्तुतः जैसे संकेतक होंगे वैसा ही पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, जैसा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को दिया जाएगा वैसा ही वह सीख पाएंगे। इसीलिए अभिष्ट संकेतों का निर्धारण अभिष्ट पाठ्यक्रम की अपेक्षा रखता है ।
सुनने और बोलने के कौशल में दक्षता से आमतौर पर यही माना जाता है कि बच्चे पढ़े और सुने को ज्यों का त्यों बोल दे। परंतु सुनने और बोलने में ‘समझ’ की प्रक्रिया को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे किसी बात पर प्रतिक्रिया ना करने वाले (ना सुनने वाले के अर्थ में) को हम यही कहते हैं कि अरे आप मेरी बात सुन नहीं रहे। स्पष्ट है कि यहां समझ के बिना सुनने का और बोलने का कोई मतलब नहीं। यह समझ ही है जो सुनने और बोलने को सार्थकता प्रदान करती है। यहां यह बात अवश्य है कि जैसे-जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसके सुनने और बोलने के दौरान समझ शक्ति का विकास होता जाता है और वह सुनने अथवा किसी भी बात पर बोलने से पहले चिंतन करने लगता है। भाषा के संकेतको का निर्धारण इसी पक्ष को ध्यान में रखकर किया गया है।
प्राथमिक स्तर पर सुनने और बोलने के संदर्भ में भाषा सीखने के संकेतक
क. दूसरों के विचार को ध्यान से और धैर्य के साथ सुनकर अपनी सोच विकसित
ख. किस्से कहानियां सुनकर आनंद प्राप्त करना ।
ग. ऐतिहासिक घटनाएं सुनकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानना ।
घ. कविताएं सुनकर उनके अर्थ एवं भाव को समझना एवं आनंद की अनुभूति करना ।
ड़. नए शब्दों को सुनकर उनके अर्थ समझना ।
च. रोचक कहानी, कविता आदि सुनकर अपने अनुभव में वृद्धि करना।
छ. सुने गए भावों-विचारों पर चिंतन करना ।
ज. सहज रूप से अपनी बात कह पाना ।
झ. परिस्थिति एवं अवसर के अनुरूप अपनी बात कह पाना ।
ञ. सशक्त रूप से अपनी बात कहना ।
ट. बोलने के शिष्टाचार का पालन करना ।
ठ. गीत, कविता आदि को लय ताल के साथ गाना ।
ड. गति एवं हाव-भाव के अनुसार बोलना ।
ढ. प्रश्न बनाना व पूछना ।
ण. घर, परिवेश एवं विद्यालय की भाषा में तालमेल बिठाकर अपने अनुभव व्यक्त
त. सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहना ।
थ. पढ़ी गई सामग्री को अपने शब्दों में कहना ।
द. गीत, कविता, कहानी व अपने विचारों को अकेले तथा समूह में प्रस्तुत करना ।
ध. सुने हुए गीत, कविता, कहानी, वार्तालाप आदि में अपने अनुभवों को जोड़कर अपनी बात कहना |
न. अपने घर, परिवार, विद्यालय एवं परिवेश में होने वाली समूह चर्चा में भाग लेना और अपने विचार प्रस्तुत करना इत्यादि ।
‘पढ़ना’ कौशल में दक्षता का सीधा अर्थ है – दी गई लिखित सामग्री को पढ़ना और उसे पढ़कर समझना। पढ़ना यांत्रिक पाठन ना हो कर एक युक्ति परक एवं सुसंस्कृत क्रिया है । दी गई सामग्री का मूल भाव, लेखन शैली, हाव-भाव आदि सब का ध्यान पठन के समय रखना पड़ता है। पढ़ना पढ़कर समझने और उस पर प्रतिक्रिया करने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पढ़ना बुनियादी तौर से अर्थवान गतिविधि है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मुद्रित अथवा लिखित सामग्री से कुछ संदर्भ अनुमान के आधार पर अर्थ पकड़ने की कोशिश ‘पढ़ना’ है। जैसे-जैसे बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से गुजरता है वह पढ़ने की इस कला को अर्जित करते हुए प्रवीण होता जाता है।
प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के संदर्भ में भाषा सीखने के संकेतक
क. अनुमान लगाकर पढ़ना एवं अर्थ खोजना।
ख. बच्चे द्वारा शब्दों और वाक्यों को वर्ण जोड़कर पढ़ने के बजाय इकाई के रूप में समझ कर पढ़ना ।
ग. अपने परिवेश में उपलब्ध सामग्री को अनुमान लगाकर समझते हुए पढ़ना जैसे दीवार, श्यामपट्ट, साइन बोर्ड आदि ।
घ. परिवेश में उपलब्ध संदर्भों, चित्रों का छपी हुई सामग्री को पढ़कर समझना ।
ड़. शब्दों में आपसी सहसंबंध स्थापित करते हुए प्रसंग के अनुसार पढ़ना ।
च, पढ़ने के प्रति रुचि होना। पढ़ते समय परिचित शब्दों का संदर्भ के आधार पर अनुमान लगाना ।
छ. साहित्य की विभिन्न विधाओं यथा कहानी, गीत, संवाद, निबंध आदि से परिचित होकर उन विधाओं की अन्य पुस्तकें पढ़ना ।
ज. पठन द्वारा आनंद प्राप्ति में समर्थ होना। दूसरों के विचारों को पढ़कर समझना ।
झ. पाठ में निहित मूल भाव, विचार या बिंदु को समझना ।
ञ. विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों का अर्थ जानना। नए शब्दों के अर्थ शब्द कोष में ढूंढना ।
ट. विभिन्न विधाओं के माध्यम से बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ना ।
ठ. परिवेश में उपलब्ध पाठ्यसामग्री के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना ।
ड. पाठ्य सामग्री द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होना ।
ढ. पाठ्य सामग्री, अखबार पत्र-पत्रिका आदि को पढ़कर समझना व उनपर प्रतिक्रिया व्यक्त करना ।
–
ब. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (जैसे टीवी, इंटरनेट, मोबाइल), परिवेश में उपलब्ध विज्ञापन आदि को पढ़कर समझ विकसित होना, इत्यादि ।
प्रश्न 14. पढ़ने का अर्थ स्पष्ट करें। शुरुआती पढ़ना क्या है? शुरुआती पढ़ने की चरणबद्ध प्रक्रिया की समझ विकसित करें।
उत्तर –
पढना लिखित / छपे चिह्नों को पढने और उनसे अर्थ गढ़ने की प्रक्रिया है । पठन प्रक्रिया के दौरान पाठक लिखित चिह्नों (अक्षरों, विरामचिह्नों, शब्दों के बीच में दिया गया स्थान, हाव-भाव) को देखकर शब्दों और वाक्यों के रूप में उनसे अर्थ ग्रहण करते हैं। पढ़ना एक विस्तृत प्रक्रिया है। इसके केवल अक्षरों व मात्राओं को पढ़ पाना ही नहीं बल्कि लिखी हुई पूरी सामग्री से अर्थ समझना भी शामिल है। पठन प्रक्रिया को तभी पूर्ण माना जाता है जब पाठक लिखित सामग्री का अर्थ समझ सके ।
पढ़ना एक समेकित प्रक्रिया है। इसमें अक्षरों की आकृतियां, उनसे जुड़ी ध्वनियाँ, वाक्य विन्यास, शब्दों और वाक्यों के अर्थ तथा अनुमान लगाने का कौशल शामिल है। पढ़ने का अर्थ है लिखित सामग्री से धारणाओं को गढ़ना, विचारों को आपस में जोड़ पाना और उन्हें अपनी स्मृति में रखना। अर्थात स्पष्ट है कि पढ़ना अनेक कुशलताओं का एक समूह है जो लिखी या छपी भाषिक सामग्री को अर्थ से जोड़ने में हमारी मदद करता है। पढ़ना कौशल की सभी परिभाषा में जिस बिंदु पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वह है – ‘अर्थ’ । अर्थात पढ़ने का लक्ष्य ही पढ़कर अर्थ समझने से है ।
शुरुआती पढ़ना –
शुरुआती पढ़ना, पढ़ना सीखने की शुरुआत है जो बच्चे स्मृति चिन्ह बना कर करते हैं। पढ़ना सीखने की शुरुआत सार्थक शब्दों और रुचिकर संदर्भों से होती है। उदाहरण के लिए यदि बच्चों को ‘घर’ का चित्र और चित्र के नीचे लिखा ‘घर’ शब्द दिखाते हैं तो बच्चा चित्र के बिना पर लिखा गया ‘घर’ शब्द पहचान जाता है। भले ही वह ‘घ’ व ‘र’ जैसे अक्षर नहीं पहचानता हो। एक बार जब बच्चे साथ में दिए गए चित्रों या शिक्षक के साथ बातचीत के सहारे कई शब्द पहचानने लगते हैं तब उन शब्दों में आए अक्षरों की ओर ध्यान दिलाया जाता है। मात्राओं को भी बच्चे स्वयं पहचानने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर पढ़ना सीखने की शुरुआत में अक्षर बच्चों के लिए सार्थक नहीं होते। हर अक्षर की आकृति और ध्वनि को बच्चे की स्मृति में बिठाने के लिए काफी समय और श्रम लगता है। वर्णमाला और बारह खड़ी को पूरा करते-करते महीनों बीत जाते हैं।
शुरुआती ‘पढ़ना’ की चरणबद्ध प्रक्रिया –
क. शुरुआती पढ़ना किताबों से करना कहीं अच्छा होता है। अक्षरों या रेखा चित्रों या तस्वीरों से सजाई गई कोई कहानी संग्रह, पढ़ना सीखने की शुरुआत में मददगार हो सकती है। जिसमें कविताएं, गीत, बच्चों के लिए खेल-गीतों का संग्रह हो ।
ख. चित्रों के द्वारा बातचीत के सहारे शब्दों को पहचानने और शब्दों में अक्षरों की ओर ध्यान दिलाना ।
ग. तरह-तरह के फ्लैश कार्ड, चार्ट रबर के अक्षरों जैसी प्रचलित सामग्री का उपयोग करना ।
घ. कहानी तथा कविताओं को बार-बार सुनाने से बच्चे पहले से सुनी कविता, कहानी अनुमान लगाते-लगाते पढ़ना सीख जाते हैं। वे जल्दी पढ़ भी लेते हैं। अक्षर, शब्द एवं वाक्य की पहचान भी सहज हो जाती है।
ड. अनुमान लगाते हुए पढ़ने से बच्चे लिपि पहचानने, वाक्यों में निहित अर्थ समझने एवं कहानी, कविता के प्रसंगों पर प्रतिक्रिया देने, कहानी को पढ़कर उसका सार प्रस्तुत करने की चरणबद्ध प्रक्रिया से बच्चे शुरुआत में पढ़ना सीखते हैं।
प्रश्न 15. पढ़ने की प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों के तात्पर्य और महत्व का वर्णन करें।
उतर –
पढ़ना एक आरंभिक प्रक्रिया है जो बच्चों के पास उपलब्ध किताबों के माध्यम से संभव हो पाती है और उनकी पुस्तकों के कारण बच्चों की जिज्ञासा, लगाव, झुकाव, आकर्षण, आदि स्वतः पढ़ने को प्रेरित करने लगती है। विभिन्न प्रकार के रोचक और मनोरंजक चित्र बच्चों को पढ़ते समय उनकी किताबों से बांधे रखते हैं। प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि बच्चों से चित्रों के विषय में वार्तालाप करके हम उनके पढ़ने-लिखने का विकास कर सकते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया से आशय उन गतिविधियों से है जिनके माध्यम से छात्र पढ़ने के संबंधित क्रिया को पूर्ण करता है। पढ़ने संबंधी सपनों का क्रमबद्ध एवं आवश्यक रूप से अनुकरण करने से पठन का कार्य उचित रूप से संपन्न होता है। इसलिए पठन की क्रिया को संपन्न करने के पूर्व पठन के सोपानों का ज्ञान छात्र एवं शिक्षक दोनों को अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पढ़ने की प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपान है
क. किताबें उलटना-पलटना
बच्चों द्वारा किताबों का उलटना-पलटना पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। यह बच्चों में किताबों के प्रति जिज्ञासा एवं पढ़ने की इच्छा को प्रदर्शित करता है। जब कोई बच्चा ऐसा कर रहा होता है तो पूछे जाने पर उसका जवाब यही होता है कि वह किताब पढ़ रहा है। साथ ही वह इसके संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दे पाता है। बच्चों की पहुंच में ढेर सारी ऐसी रंग-बिरंगी किताबों का होना उनमें किताबों से लगाव उत्पन्न करेगा। किताबों से लगाव होना पढ़ने की नींव है।
ख. चित्र पठन –
बच्चे चित्रों को ध्यान से देखते हैं और चित्र के बारे में मन में उठने वाले अपने सवालों क्या, कौन, कहां आदि का जवाब अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ढूंढने में लग जाते हैं। बच्चे के साथ बच्चों का यह कार्यकलाप चित्र पठन कहा जाता है। बच्चों से चित्र पठन करवाते हुए उनसे दिए गए चित्र के संबंध में बातचीत करके उनके सुनने, बोलने और लिखने के कौशलों का विकास किया जा सकता है ।
ग. अनुमान लगाते हुए पढ़ना –
हमने प्रायः देखा है कि बच्चे कविता पठन के समय कविता की पंक्तियों पर उंगलियां फेरते हैं। ऐसा बच्चे द्वारा अनुमान लगाकर पढ़ने की प्रक्रिया के द्वारा संभव होता है। इस प्रक्रिया में शब्दों के उच्चारण, पंक्तियों पर अंगुलियों की स्थितियों में वास्तविक सामंजस्य का कभी-कभी अभाव होता है। परंतु अनुमान लगाकर पढ़ना, पढ़ने के कौशल की कुंजी है। एक दक्ष पाठक एक शब्द के सारे अक्षरों या एक वाक्य के सारे शब्दों को नहीं देखता है, बल्कि पढ़ते समय उसकी आंखें मुद्रित सामग्री के एक छोटे अंश पर ही गौर करती हैं। शेष भाग वह अनुमान के आधार पर ग्रहण कर लेता है। अनुमान का आधार होता है अक्षर की आकृतियां, शब्द एवं उनके अर्थ व संयोजन और पाठक का पूर्व ज्ञान ।
घ. लिपि पहचानना –
पढ़ने की प्रक्रिया के इस सोपान में लिपियों को पहचानना, उससे जुड़ी ध्वनियों के उच्चारण एवं उसके मानसिक बिंब की रचना करना सम्मिलित हैं। शब्द के रूप, ध्वनि एवं अर्थ तीनों मिलकर हमारे मस्तिष्क में शब्द का एक चित्र या बिंब का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क में शब्द से संबंधित चित्र या बिंब का निर्माण होना हमारे पूर्व अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे-जैसे कलम अर्थात कलम पढ़ते समय हमारे मस्तिष्क में कलम का ही चित्र उभर कर आता है ना कि किसी अन्य वस्तु का । मस्तिष्क में शब्दों के चित्रों के निर्माण में दक्षता प्राप्त कर लेने के बाद पाठक शब्दों को अक्षरों में तोड़ कर उन लिपि चिह्नों की भी पहचान सुगमतापूर्वक कर सकता है।
ड़. अर्थ समझना –
अर्थ की समझ के बिना पठन ‘वाचन’ की श्रेणी में आता है। अतः अर्थ समझना पठन की प्रथम और अनिवार्य शर्त है । पठन सामग्री के साथ संवाद कर के अनुभवों विचारों और सैद्धांतिक संरचना के रूप में अर्थपूर्ण समझ प्रदान करना ही पढ़ना है। अर्थ ग्रहण की दक्षता पाठक के पूर्व अनुभव पर निर्भर करती है। साथ ही यह पाठक से चिंतन-मनन की भी अपेक्षा रखती है। पठन के क्रम में अर्थ ग्रहण के साथ-साथ व्याख्या एवं विश्लेषण भी चलती रहती है ताकि पाठक वहीं पहुंचे जहां लेखक उसे ले जाना चाहता है।
च. प्रतिक्रिया देना –
मानव एक चिंतनशील प्राणी है। स्वाभाविक है कि पढ़ने की सामग्री के अर्थ ग्रहण के उपरांत वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। एक अच्छा पाठक पढ़ने के साथ-साथ विभिन्न दृष्टिकोण से पठित सामग्री का मूल्यांकन करते हुए उसके प्रति अपना विचार प्रकट करता जाता है। साथ ही साथ उसके मन में कुछ भावनाएं भी उत्पन्न होती है जिससे वह अपने हाव-भाव से प्रदर्शित करता है। किसी साहित्य को पढ़कर उसके रस का अनुभव एक अच्छा पाठक ही कर सकता है और उसके उपरांत वह प्रतिक्रिया भी अवश्य देगा । प्रतिक्रिया से पता चलता है कि पाठक द्वारा किस स्तर तक अर्थ ग्रहण किया गया है। पढ़ने के बाद बच्चों को किसी कहानी को संक्षेप पर सुनाने या कहानी की घटनाओं के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रेरित करने पर उनमें अर्थ ग्रहण एवं चिंतन-मनन द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है।
छ. पढ़कर सार प्रस्तुत करना –
जब किसी मुद्रित सामग्री के पठन के फलस्वरुप उसमें निहित जिस भाव आदर्श अथवा मूल्य से हम सहमत हो उसे आत्मसात कर लें, पठन का उद्देश्य तभी पूरा माना जाता है। एक पाठक की किसी मुद्रित सामग्री को पढ़कर उसकी विषय वस्तु को लेखक की भावना के अनुरूप ग्रहण कर लेता है एवं उसकी अभिव्यक्ति संक्षिप्त रूप से कर सकने में समर्थ होता है तो पठन को सफल समझा जाता है। बच्चों को पढ़ी गई कविता एवं कहानियों को संक्षिप्त रूप में अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करने से बच्चों के गहन पठन की क्षमता का विकास होता है।
प्रश्न 16. पढ़ने के विभिन्न प्रकारों एवं सीखने में इनके महत्व का वर्णन करें।
क. सस्वर पठन पढ़ना-
सीखने की यह आरंभिक स्थिति है । सस्वर पठन का अर्थ है बोलकर उच्चारण सहित स्पष्ट रूप से पठन। आरंभिक कक्षा के छात्रों को सस्वर पठन करने पर बल दिया जाता है। कक्षा में बच्चों का विभिन्न कहानियों, कविताओं का हाव-भाव एवं लय के साथ सस्वर पठन करने के कार्य दिए जाते हैं जिससे कि उनमें शब्दों की सही समझ, उच्चारण, स्पष्टता का भाव विकसित हो।
(03) प्रश्न
(04) प्रश्न
(05) प्रश्न
(06) प्रश्न
(07) प्रश्न
(08) प्रश्न
(09) प्रश्न
(10) प्रश्न
Note- यह वेबसाइट Under construction है जल्द ही सभी प्रश्नों के उत्तर जोड़ दिये जायेगे|
हिंदी का शिक्षण शास्त्र -1 (प्राथमिक स्तर ) SCERT BOOK PDF
F-8 हिंदी का शिक्षण शास्त्र -1 (प्राथमिक स्तर ) Book pdf
F-8 Hindi Ka Shikshan Shastra -1 (Parathmik Star ) Book pdf
vvi notes. in के इस पेज में बिहार डी.एल.एड फर्स्ट ईयर पेपर -F-8 (Bihar D.El.Ed first year paper F-8) हिंदी का शिक्षण शास्त्र -1 (प्राथमिक स्तर ) से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये |