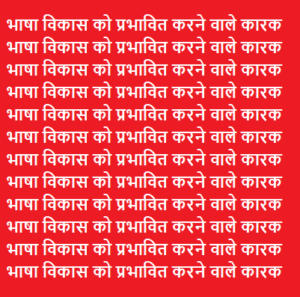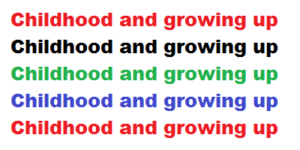ज्ञान और सूचना में अन्तर एवं समानता
अथवा
ज्ञान एवं सूचना के विस्तार से विभेद
प्रत्येक ज्ञान के साथ एक ज्ञाता व एक ज्ञेय जुड़ा होता है और जब ज्ञाता का ज्ञेय के साथ इन्द्रियों के माध्यम से सम्पर्क होता है तो ज्ञेय को पदार्थ के सम्बन्ध में एक चेतना होती है जिसे ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रियों से जो प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभव होता है, उसे भी ज्ञान कहते हैं। ज्ञान इन्द्रियों तक ही सीमित नहीं होता अपितु इन्द्रियों से परे भी जो अनुभूतियाँ होती हैं उसे भी ज्ञान कहां जाता है।
ज्ञान के स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान का अर्थ जानना आवश्यक है। ज्ञान का स्वरूप किसी वस्तु के सम्बन्ध में जानकारी है जिसे सूचना भी कहा जा सकता है। जब हम किसी वस्तु के सम्बन्ध में यह कहते हैं कि हमें उसकी जानकारी है तो हम यह मानकर चलते हैं कि यह जानकारी सत्य है। अतएव ज्ञान की धारणा में पहले तो यह बात निहित है कि ज्ञान को अवश्य सत्य होना चाहिये। इसी प्रकार ज्ञान के अर्थ में तीन बातें आती हैं—सत्यता, सत्यता में विश्वास तथा सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण आदि। प्रायः ज्ञान के स्वरूप को मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक क्रिया, जैसे—जानना, करना और अनुभूति करना माना जाता है। यही तीन तत्त्व मनुष्य के व्यवहार में भी दृष्टिगत होते हैं तथा यह कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति को इस कार्य का अच्छा ज्ञान है। इसी प्रकार ज्ञान का पक्ष वस्तु के गुणों में भी सम्बन्धित होता है जो इस बात का प्रतीक है कि जब व्यक्ति किसी वस्तु के गुणों को वास्तविक रूप से देख ले तभी उसे उस वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है |
‘ज्ञान’ जिसका अंग्रेजी रूपान्तर नॉलेज है, को समानार्थी ही प्रयुक्त किया जाता है परन्तु पाश्चात्य मत में मिली ‘नॉलेज’ शब्द की विवेचना तथा ‘भारतीय मतानुसार’ ‘ज्ञान’ शब्द की दार्शनिक विवेचना में अन्तर है। ‘नॉलेज’ सिर्फ सत्य होता है जबकि ‘ज्ञान’ का सत्य व असत्य दोनों ही रूपों में पाया जाना नियत है। पाश्चात्य तर्कनिष्ठ अनुभववादी परम्परा में ‘असत्य ज्ञान’ एक स्वतोष्या घाती पद और ‘सत्य ज्ञान’ एक पुनशक्ति है जबकि भारतीय परम्परा या पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में आधारभूत भेद है। अतः दोनों शब्दों को एक-दूसरे की भाषा में अनूदित या रूपान्तरित नहीं किया जा सकता।
ज्ञान की अवधारणा के सन्दर्भ में एक तथ्य और है कि ज्ञान केवल अनुभूति मात्र नहीं है। अनुभूति मात्र बाह्य स्वरूप की होती है परन्तु जब वस्तु के बाह्य स्वरूप को देखने के बाद हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो यह स्थिति संभवतः ज्ञान की कही जा सकती है। ऐसा ज्ञान प्राप्त होने की स्थिति को ही ज्ञान चक्षु का खुल जाना कहा जा सकता है। शिक्षा यदि हमारे ज्ञान चक्षु खोल दे तो वह ज्ञान इन्द्रियों के अनुभव तक ही सीमित नहीं रहता है अपितु इन्द्रियों से प्राप्त अनुभूतियों से भी छात्र को ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसके लिए कर्म, ज्ञान व भक्ति में समन्वय आवश्यक है।
ज्ञान व सूचना में समानता
सामान्यतः हम या हमारा समाज ज्ञान व सूचना के बीच भेद नहीं करता, ज्ञान में अन्तर्निहित और मौन विशेषतायें होती हैं जो सूचना की अपेक्षा सूक्ष्म किस्म की होती हैं और इस प्रकार हम ज्ञान व धर सूचना के बीच भेद न करके समाज में से आलोचनात्मक चिन्तन को दर किनार करते जा रहे हैं। यह केवल जन-सामान्य के कारण नहीं बल्कि हमारे समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा भी नजरअन्दाज किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर सैम पित्रोदा की (Knowledge commission) की रिपोर्ट में भी इस अन्तर को नजरअन्दाज किया गया है।
इस समाज में दो प्रकार के बुद्धिजीवी होते हैं, लोक बुद्धिजीवी और नीति बुद्धिजीवी। हमें यह समझना होगा कि दोनों के कार्यक्षेत्र पृथक् न होकर एक हैं। लोकनीति एक सम्पूर्ण विषय-वस्तु है जहाँ नीति बुद्धिजीवी अपने ज्ञान को केवल एक लिखित और सैद्धान्तिक वस्तु मानकर रूपरेखा तैयार कर देते हैं वहीं लोक बुद्धिजीवी किसी तथ्य को गहराई से समझने का यत्न करते हैं। ये नीतियों के तथ्यों और नैतिकता के सापेक्ष रखते हैं। समस्या यह है कि 90 के दशक के बाद से भारत में लौक बुद्धिजीवियों की अपेक्षा नीति बुद्धिजीवियों का आधिक्य हो गया है जिसके कारण आज भारत ज्ञान का उपभोक्ता मात्र बनकर रह गया है। यह केवल ज्ञान को आत्मघात करने की चेष्टा करता है, स्वयं इसकी व्याख्या या नए खोज में रुचि नहीं रखता और यही कारण है कि भारत अन्य देशों की अपेक्षा काफी पीछे रह गया है।
हम नीतियों में कुछ बदलाव करके स्वयं को पंडित समझने लगते हैं। ये अधूरा ज्ञान और सूचना को ज्ञान समझना एक महान भूल है।
वर्तमान समय में जब शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठ रहे हैं तो यह कहना गलत न होगा कि लोक नीति के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा जो ज्ञान प्राप्त करने का मूल आधार है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, अगर कमोवेश ध्यान दिया भी जाता है तो गुणवत्ता मजबूत करने को बहुत कम सोचा जाता है।
यह ध्यान रखना होगा कि शिक्षा केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है ज्ञान शिक्षा जो हमें देते हैं और उस सूचना में व्यावहारिकता, अनुभव, परिमार्जन आदि का समावेश करने के पश्चात् सूचना का अन्तरण ज्ञान में होता है।
यदि हम ज्ञान व सूचना से सम्बन्धित विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि दोनों प्रत्ययों में सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ सूचना का निष्कर्षण मूल आँकड़ों में होता है और ज्ञान का उदगम आँकड़ों से होता है। इस प्रकार दोनों ही प्रत्ययों हेतु मूल स्रोत आँकड़े ही हैं। नितेकी दोनों प्रत्ययों की व्याख्या निम्न वाक्यों द्वारा की Information is knowledge affects और Knowledge is information processed with a point of nice through representation. । जिससे पता चलता है कि ज्ञान व सूचना एक ही है परन्तु ज्ञान सूचना का अधिक विकसित रूप है। इसके भव्य है यह तथ्य कि ज्ञान व सूचना दोनों की पहचान अवलोकन में ही होती है, इसके द्वारा भी ज्ञान व सूचना को समान माना जा सकता है।
ओटन ने इन दोनों सम्प्रत्ययों का वर्णन इसकी प्रक्रियाओं के आधार पर इस प्रकार किया है- सूचना के अर्जन की प्रक्रिया में इसका हस्तान्तरण ज्ञान में होता है व ज्ञान का सम्मिलित एक सामान्य समझ में व अंततः बुद्धि में होता है।’
इससे स्पष्ट है कि आँकड़ों के निरन्तर सम्बन्धों में सूचना मानव मस्तिष्क का एक भाग बन जाती और इसे आनुभविक तौर पर अर्जित किया जा सकता है, प्रायोगिक रूप में वर्णित किया जा सकता और दार्शनिक रूप से व्याख्यायित किया जा सकता है जो कि हर प्रक्रिया सूचना-ज्ञान प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है।
**** *** *** ** ** ** *** *** ****
@@ @@ @@ @@ @@ @@@
(related question)
- ज्ञान और सूचना में अन्तर एवं समानता
- ज्ञान एवं सूचना के विस्तार से विभेद
- gyan soochana ke vistaar se vibhed
- gyan aur soochana mein antar evan samaanata
- Differences and similarities between knowledge and information
- Differentiation by extension of knowledge and information