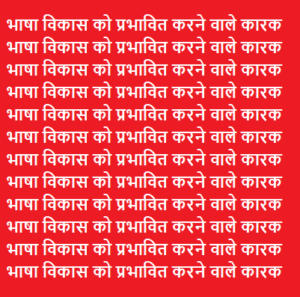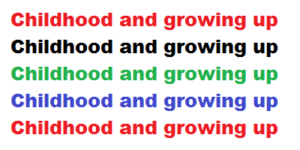ज्ञान प्राप्ति की विधियां
मानवीय ज्ञान व इसका भण्डार अनन्त होता है व निरन्तर गतिशील रहने के कारण इसमें निरन्तर परिवर्तन व परिवर्द्धन भी होता रहता है। सामान्यतः मानवीय ज्ञान की तीन अवस्थायें क्रमशः (i) ज्ञान का संचयन, (ii) ज्ञान का अन्तरण व (iii) ज्ञान का सृजन होती है। प्रथम अवस्था के अन्तर्गत स्मरण, लेखन, मुद्रण, भंडारण आदि के विभिन्न तरीकों के द्वारा उपलब्ध ज्ञान का संचय किया जाता है। द्वितीय अवस्था में विभिन्न संचरण माध्यमों की सहायता से उपलब्ध संचित ज्ञान को भावी पीढ़ी को प्रदान किया जाता है। तृतीय अवस्था में नवीन ज्ञान का सृजन करके ज्ञान भंडार को समृद्ध किया जाता है। इस प्रकार निःसन्देह प्रदत्तों व सूचनाओं की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त सार्थक निष्कर्ष ही ज्ञान के अंग होते हैं व इनके द्वारा प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है। इस वास्तविक/ यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने की निम्नलिखित विधियाँ हैं-
वास्तविक/ यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने की विधियाँ
- (i) विश्लेषणात्मक दर्शन-
- (ii) ज्ञान की वैयक्तिक अनुभव विधि
- (iii) ज्ञान की अधिकारिता विधि
- (iv) ज्ञान की निगमन तर्क विधि
- (v) ज्ञान की आगमन तर्क विधि
- (vi) वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल
(i) विश्लेषणात्मक दर्शन-
यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में विश्लेषणात्मक दर्शन का बहुत योगदान होता है। यह दर्शन भाषागत तथा तार्किक विश्लेषण की विधि को अपनाता है तथा अपनी प्रकृति में वैज्ञानिक है। तार्किक विश्लेषण, शैक्षिक अवधारणाओं के सन्दर्भ में अनुमानों, आलोचनाओं, स्पष्टीकरण एवं परीक्षण करके तथा उनमें जो तार्किक दोष हैं, उन्हें सामने लाकर ऐसे ज्ञान की ओर ले जाता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यथार्थ का संकेत देता है।
(ii) ज्ञान की वैयक्तिक अनुभव विधि-
ज्ञानार्जन का एक प्रमुख साधन इन्द्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव होते हैं। प्राचीन काल से ही आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा को पाँच ज्ञानेन्द्रियों के रूप में स्वीकार किया गया है जिनके द्वारा मनुष्य तरह-तरह के अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार के वैयक्तिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को अनुभव जनित ज्ञान कहते हैं जो निःसन्देह ज्ञान प्राप्ति का सबसे प्राचीन स्रोत भी है। दिन-प्रतिदिन में भी हम प्रायः देखते हैं कि जन्म लेते ही प्रत्येक प्राणी- मानव, पशु व पक्षी इस विधि का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं व इसी अनुभव द्वारा मनुष्य कई प्रकार के सामान्य ज्ञान जैसे हानिकारक व लाभदायक वस्तुओं की जानकारी, ऋतुएँ बदलने के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन व और भी कई बातें जान लेते हैं। परन्तु इस अनुभवजन्य ज्ञान के बारे में एक बात और भी अच्छी तरह समझनी होगी कि केवल एक या दो अनुभव प्रायः ज्ञान प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं अथवा एक या दो अनुभवों से प्राप्त सूचना सदैव ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखी जाती है वरन अनुभवों की एक लम्बी श्रृंखला से प्राप्त सूचना की बारम्बार पुष्टि ही ज्ञान का स्वरूप बनती है। अनुभवजन्य ज्ञान की वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता तथा वैधता का निर्धारण करना भी प्रायः एक कठिन कार्य होता है तथा यदि किसी प्रकार से यह विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठता हासिल भी कर ली जायें तो इसकी वैधता का निर्धारण प्रायः कठिन ही होता है व इसमें सन्देह बना रहता है। यही कारण है कि ज्ञान के स्रोत के रूप में वैयक्तिक अनुभवों को वर्तमान में मान्य स्वीकार नहीं किया जाता है एवं इससे प्राप्त ज्ञान निम्नकोटि का कहलाता है। अतः ये वैयक्तिक अनुभव व्यक्ति की निजी जानकारी या सूचना के साधन तो हो सकते हैं परन्तु इसे यथार्थ बात नहीं माना जा सकता।
(iii) ज्ञान की अधिकारिता विधि-
अनादिकाल से यह परम्परा रही है कि कोई भी व्यक्ति, किसी समस्या, कठिनाई या जिज्ञासा के उत्पन्न होने पर, अपने से श्रेष्ठ, मान्य या जानकार व्यक्तियों से परामर्श करता है क्योंकि हम उनके प्रति आस्था, श्रद्धा व विश्वास का भाव रखते हैं। इसी श्रेष्ठ मान्य या जानकार व्यक्ति/संस्था/वस्तु के द्वारा दिये गये परामर्श, उत्तर या ज़ानकारी को अधिकारिता मत कहा जाता है एवं इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने की विधि अधिकारिकता विधि कहलाती है। बाढ़ क्यों आती है? नदी की गहराई क्या है? बिजली क्यों चमकती है अथवा कड़कती है? सूर्यग्रहण / चन्द्रग्रहण क्यों पड़ता है? जैसे अनेक प्रश्नों का उत्तर आदिकाल से व्यक्ति अपने से अधिक वयोवृद्ध व जानकार लोगों से प्राप्त करता रहता था। यह माना जाता था कि कुछ वरिष्ठ व्यक्तियों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करने तथा अध्ययन-मनन व चिन्तन करने का अधिक अनुभव है एवं उन्होंने उसके बारे में एक स्पष्ट व स्वीकार्य धारणा बना ली है। परिणामस्वरूप इस प्रकरण / समस्या विशेष पर वे उनकी राय बिना बात किसी अतिरिक्त चिन्तन-मनन या परीक्षण के यथावत् सत्य रूप में स्वीकार कर ली जाती थी।
(iv) ज्ञान की निगमन तर्क विधि-
इस विधि के विकास में प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक सुकरात व उसके सहयोगियों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। यह विधि तर्क के रूप में ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाकर ज्ञान प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। इस विधि को निरपेक्ष न्याय वाक्य नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिज्ञप्तियों के आधार पर न्याय वाक्यों को चार वर्गों अर्थात् निरपेक्ष न्याय वाक्य वैकल्पिक न्याय वाक्य, परिकल्पित न्याय वाक्य एवं नियोजक न्याय वाक्य में विभक्त किया जा सकता है।
इस विधि की भी कुछ सीमाएँ हैं जैसे—पूर्व स्थापित ज्ञान के आधार पर किसी परिस्थिति विशेष के बारे में नवीन ज्ञान का सृजन सटीकता से न हो पाना, शब्दों व संकेतों का अर्थ अलग-अलग होना जिससे प्राप्त निष्कर्ष में त्रुटि आ सकती है तथा वैधता व प्रामाणिकता को सिद्ध न कर पाना आदि जिसके कारण 17वीं शताब्दी तक आते-आते इस विधि का प्रयोग काफी सीमित हो गया है।
(v) ज्ञान की आगमन तर्क विधि-
ज्ञानार्जन की इस विधि के प्रणेता फ्रांसिस बेकन थे। इसलिए इसे बेकोनियन विधि के नाम से भी जाना जाता है। निगमन तर्क के विपरीत आगमन विशिष्ट से सामान्य की ओर प्रवृत्त होता है। इस विधि के अन्तर्गत व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार के अनेकों तर्क दृष्टान्तों का संकलन करके उनमें निहित समानता को पहचानने का प्रयास करता है और इस प्रक्रिया में वह नवीन ज्ञान के अर्जन की ओर अग्रसर होता है। जहाँ एक ओर इस विधि को निगमन विधि की विपरीत विधि कहा जाता है तो वहीं दूसरी ओर इसे निगमन विधि की पूरक विधि भी कहा जा सकता तर्क विधि के दो प्रकार पूर्ण आगमन तथा अपूर्ण आगमन भी हो सकते हैं। पूर्ण आगमन विधि में जहाँ अध्ययन क्षेत्र के सभी दृष्टान्तों के अवलोकन के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष निकाले जाते हैं वहीं अपूर्ण आगमन में कुछ चुने दृष्टान्तों के आधार पर प्रायिकता निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दोनों ही प्रकार की विधियों में निःसन्देह विशिष्ट स्थितियों के सामान्यीकरण द्वारा ही निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। कालान्तर में इस विधि को भी छोड़ दिया गया एवं बौद्धिक क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्ति की एक नवीन विधि की आवश्यकता महसूस की गई
(vi) वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल-
पीयर्स महोदय के अनुसार वैज्ञानिक पहुँच का सबसे अच्छा मार्ग एक दर्शन की स्थापना करना है। फीगल का भी कुछ ऐसा ही विचार है। वह विज्ञान और मानववाद के बीच के सम्बन्ध पर बल देते हैं और वैज्ञानिक विधि की मूल विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। वे विज्ञान के उद्देश्यों की पहचान वर्णन, व्याख्या एवं पूर्वानुमान के रूप में करते हैं जिससे विज्ञान को इसका प्रगतिशील रूप और प्रयोगात्मकता के निश्चित होने का भाव मिलता है। फीगल का यह भी विश्वास है कि विज्ञान द्वारा और अच्छे मूल्य सम्बन्धी निर्णयों को लेने की क्षमता मिलती है।
अतः ज्ञान प्राप्त करने की इस वैज्ञानिक विधि का आरम्भ कठिनाई या समस्या के अभाव होने से शुरू होकर समाधान खोजने पर समाप्त होता है। समस्या के परिभाषीकरण द्वारा समस्या को व्यावहारिक कार्यरूप में प्रस्तुत करके सुस्पष्ट किया जाता है। समस्या के चिन्हित व स्पष्ट हो जाने के उपरान्त उसके निदान हेतु कुशल अनुमान लगाकर तत्सम्बन्धी परिकल्पना बनाई जाती है तथा बाद में इस परिकल्पना के परीक्षण हेतु आवश्यक साक्ष्यों को संकलित करके उनका संश्लेषण-विश्लेषण किया जाता है। इसी के आधार पर अर्थात् साक्ष्यों के संश्लेषण-विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों से परिकल्पना को स्वीकार, अस्वीकार या परिमार्जित किया जाता है। वैज्ञानिक विधि का उद्देश्य परिकल्पना को शत-प्रतिशत प्रमाणित करना या निरस्त करना नहीं होता है वरन् यह देखना होता है कि साक्ष्य किस सीमा तक उसकी पुष्टि कर रहे हैं।
*********************
**************************
(Related question)
- ज्ञान प्राप्ति की विधियां
- methods of acquiring knowledge
- ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न विधियों
- Knowledge acquiring process