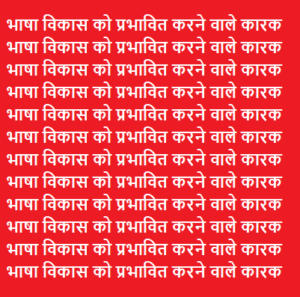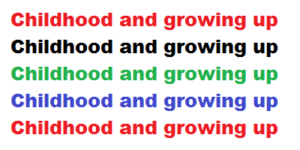Childhood and growing up
| विषय | Childhood and growing up |
| SUBJECT | Childhood and growing up B.Ed. Notes |
| COURSE | B.Ed. 1st Year |
| PAPER | 01 (First) |
VVI NOTES के इस पेज में B.Ed. 1st YEAR Paper -1 Childhood and Growing Up से सम्बन्धित Childhood and growing up B.Ed. Notes , Childhood and growing up B.Ed. 1st year Notes , Childhood and growing up b-ed Notes pdf free download , Childhood and growing up assignment इत्यादी को सामिल किया गया है |
Childhood and growing up B.Ed. Notes in hindi
| B.Ed first Year Paper -1 Childhood and Growing Up के यहाँ पर नोट्स और असाइनमेंट दिया गया है | |
प्रश्न -1 वृद्धि एवं विकाश से क्या समझते है ? विकास के प्रमुख अवस्थाओ का वर्णन करे
उत्तर –
वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं?
वृद्धि (Growth) और विकास (Development) दोनों मानव जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है।
1. वृद्धि (Growth):
वृद्धि से आशय शारीरिक परिवर्तन या परिमाणात्मक (quantitative) वृद्धि से है, जैसे – ऊँचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, शरीर के अंगों का आकार बढ़ना आदि। यह मापी जा सकती है।
विशेषताएँ:
- यह शारीरिक होती है।
- मापी जा सकती है (जैसे किलोग्राम में वजन, सेंटीमीटर में ऊँचाई)।
- एक निश्चित उम्र तक ही होती है (जैसे युवावस्था तक)।
- यह केवल शरीर के बाहरी परिवर्तन को दर्शाती है।
2. विकास (Development):
विकास से आशय व्यक्ति के समग्र और सतत परिवर्तन से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक पक्ष शामिल होते हैं। यह गुणात्मक (qualitative) होता है और जीवन भर चलता रहता है।
विशेषताएँ:
- यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि सभी पहलुओं से जुड़ा होता है।
- इसे मापा नहीं जा सकता, केवल देखा या अनुभव किया जा सकता है।
- यह जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता है।
- यह परिपक्वता और समायोजन की प्रक्रिया है।
विकास की प्रमुख अवस्थाएँ
(Stages of Development)
(01) जन्मपूर्व अवस्था (Prenatal Stage):
- अवधि: =गर्भधारण से जन्म तक
- विशेषता: =भ्रूण का शारीरिक और मानसिक आधार तैयार होता है।
(02) शैशवावस्था (Infancy):
- अवधि:= जन्म से 5 वर्ष तक
- विशेषता:= शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है, इंद्रियों का विकास, चलना-फिरना, बोलना शुरू करना।
(03) बाल्यावस्था (Childhood):
- अवधि: = 5 से 12 वर्ष तक
- विशेषता: = सामाजिक व्यवहार सीखना, भाषा विकास, विद्यालयी शिक्षा की शुरुआत।
(04) किशोरावस्था (Adolescence):
- अवधि: = 12-13 से 18-19 वर्ष तक
- विशेषता: = यौवनारंभ, आत्म-चेतना, भावनात्मक अस्थिरता, पहचान की खोज।
(05) युवा अवस्था (Early Adulthood):
- अवधि: = 20 से 40 वर्ष तक
- विशेषता: = करियर निर्माण, विवाह, परिवार की जिम्मेदारियाँ।
(06) मध्यम अवस्था (Middle Adulthood):
- अवधि: = 41 से 60 वर्ष तक
- विशेषता: = सामाजिक स्थिति में स्थिरता, बच्चों का पालन-पोषण, आत्ममूल्यांकन।
(07) प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था (Old Age):
- अवधि: = 60 वर्ष के बाद
- विशेषता: = शारीरिक क्षीणता, सेवानिवृत्ति, सामाजिक एवं भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता।
प्रश्न -2 किशोरों की मुख्य समस्या क्या है ?किशोरों की समस्या समाधान में शिक्षक परिवार एवं समुदाए की भूमिका का वर्णन ?
उत्तर –
किशोरावस्था (13-19 वर्ष) एक चुनौतीपूर्ण दौर होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इस उम्र में किशोरों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं:
🌱 किशोरों की मुख्य समस्याएँ
किशोरावस्था (Teenage/Adolescence) जीवन का ऐसा चरण है जो बचपन और वयस्कता के बीच का होता है। यह समय शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से बहुत सारे बदलावों का होता है। इस समय किशोर कई समस्याओं से जूझते हैं, जैसे:
1. पहचान की तलाश (Identity Crisis)
किशोर यह समझने की कोशिश करते हैं कि वे कौन हैं, क्या बनना चाहते हैं।
2. शारीरिक परिवर्तन
हार्मोनल बदलावों के कारण शरीर में बहुत बदलाव आते हैं जिससे आत्म-संदेह या शर्म की भावना उत्पन्न हो सकती है।
3. भावनात्मक अस्थिरता
मूड स्विंग्स, गुस्सा, चिड़चिड़ापन आम हैं।
4. अभिभावकों और शिक्षकों से मतभेद
आत्मनिर्भरता की चाह और विचारों में टकराव अक्सर तनाव का कारण बनता है।
5. सामाजिक दबाव और मित्र समूह का प्रभाव (Peer Pressure)
किशोर अक्सर गलत संगत या गलत निर्णय ले लेते हैं।
6. नशे की आदतें, सोशल मीडिया की लत
ध्यान भटकने या अवसाद के कारण किशोर गलत राह पकड़ सकते हैं।
7. सामाजिक दबाव –
दोस्तों के समूह में फिट होने की चिंता, बुलिंग या अकेलापन।
8. शैक्षिक तनाव –
परीक्षा, करियर चुनाव और अभिभावकों की उम्मीदों का दबाव।
9. पारिवारिक टकराव –
स्वतंत्रता चाहत और अभिभावकों के नियंत्रण के बीच संघर्ष।
10. डिजिटल दुनिया का प्रभाव –
सोशल मीडिया की लत, अनुचित सामग्री या साइबर बुलिंग।
🧩 किशोरों के समस्या समाधान में शिक्षक, परिवार एवं समुदाय की भूमिका
1. 👨👩👧 किशोरों के समस्या समाधान में परिवार की भूमिका:
• सकारात्मक संवाद बनाए रखना – बच्चों से खुलकर बात करना, उनकी बातें सुनना और समझना।
• समर्थन और मार्गदर्शन – बिना डांट-डपट के सलाह देना और निर्णय में उनका साथ देना।
• उचित अनुशासन – स्वतंत्रता देने के साथ-साथ सीमाएँ तय करना।
• मूल्य और संस्कार देना – नैतिक शिक्षा और सही व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना।
•
2. 🧑🏫 किशोरों के समस्या समाधान में शिक्षकों की भूमिका:
• मित्रवत व्यवहार – शिक्षक अगर दोस्ताना और समझदार होंगे तो किशोर अधिक खुलकर अपनी समस्याएँ साझा करेंगे।
• काउंसलिंग और मार्गदर्शन – शिक्षा के साथ जीवन मूल्यों और करियर के बारे में सलाह देना।
• प्रेरणा देना – किशोरों में आत्मविश्वास भरना और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
• सकारात्मक माहौल बनाना – कक्षा में समानता, सहिष्णुता और सहयोग की भावना का विकास करना।
3. 🏘️किशोरों के समस्या समाधान में समुदाय/समाज की भूमिका:
• युवाओं के लिए सकारात्मक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना – जैसे खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वयंसेवी कार्य आदि।
• किशोरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम – स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, यौन शिक्षा आदि पर खुली चर्चाएँ।
• संवेदनशीलता और सहयोग – समाज को किशोरों की समस्याओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष:
किशोरावस्था एक संवेदनशील लेकिन विकासशील चरण है। यदि इस समय किशोरों को सही मार्गदर्शन, समर्थन और समझ मिल जाए तो वे भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। इसके लिए परिवार, शिक्षक और समुदाय — सभी को मिलकर काम करना होगा।
प्रश्न 3 – भाषा विकास के मुख्य अवस्था एवं कारको उल्लेख करे
उत्तर –
भाषा विकास (Language Development) बाल विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो शिशु के जन्म से ही आरंभ हो जाती है और अनुभव, पर्यावरण, एवं संप्रेषण के माध्यम से क्रमशः विकसित होती है। इसमें बच्चा धीरे-धीरे ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ को समझने व प्रयोग करने लगता है।
भाषा विकास की मुख्य अवस्थाएँ
(Stages of Language Development)
1. 👶 प्रारंभिक ध्वनि अवस्था (0-6 माह):
o बच्चा रोकर, चीखकर या कुछ ध्वनियाँ निकालकर अपनी भावनाएँ प्रकट करता है।
o कूइंग (Cooing) और बबलिंग (Babbling) जैसे ध्वनि प्रयोग होते हैं (जैसे “अ”, “ऊ”, “गु”, “गा”)।
2. 🍼 बोलचाल पूर्व अवस्था (6-12 माह):
o ध्वनियों में दोहराव (जैसे: “मामा”, “पापा”) होता है।
o बच्चा दूसरों की आवाज़ पर प्रतिक्रिया देने लगता है।
o कुछ सामान्य शब्दों को समझने लगता है।
3. 🗣️ शब्द प्रयोग अवस्था (1-2 वर्ष):
o पहला शब्द बोलता है (जैसे “माँ”, “पानी”)।
o धीरे-धीरे शब्दों का भंडार बढ़ने लगता है।
o एक-एक शब्द से भाव प्रकट करता है।
4. 💬 वाक्य गठन अवस्था (2-3 वर्ष):
o दो से तीन शब्दों के वाक्य बनाने लगता है (जैसे “माँ पानी दो”)।
o सरल वाक्यों में बात करने की कोशिश करता है।
5. 🧒 व्याकरणिक भाषा अवस्था (3-6 वर्ष):
o भाषा में व्याकरणिक संरचना का प्रयोग करने लगता है।
o प्रश्न पूछता है, भाव व्यक्त करता है, कहानियाँ सुनाता है।
6. 🧍 प्रौढ़ भाषा अवस्था (6 वर्ष एवं आगे):
o भाषा में परिपक्वता आती है।
o भाव, विचार, तर्क आदि को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने लगता है।
o लेखन और औपचारिक भाषा का प्रयोग सीखता है।
🧩 भाषा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक
(Factors Influencing Language Development)
1. 👪 पारिवारिक वातावरण:
o बातचीत और संवाद का स्तर जितना अच्छा होगा, बच्चा उतनी जल्दी भाषा सीखेगा।
2. 🏫 शैक्षणिक वातावरण:
o विद्यालय और शिक्षक की भाषा प्रेरणादायक होनी चाहिए।
3. 🧬 बौद्धिक क्षमता (Mental Ability):
o बालक की संज्ञानात्मक (cognitive) क्षमता भाषा सीखने की गति को प्रभावित करती है।
4. 🗣️ अनुकरण (Imitation):
o बच्चे अपने आसपास की भाषा की नकल करके सीखते हैं।
5. 📺 मीडिया और तकनीक:
o टी.वी., मोबाइल, किताबें इत्यादि भाषा विकास में मदद या बाधा बन सकते हैं, इस पर निर्भर करता है कि इनका प्रयोग कैसे हो रहा है।
6. 💞 प्रेरणा और सामाजिक संबंध:
o सामाजिक सहभागिता जितनी अधिक होगी, बच्चा उतनी जल्दी और बेहतर भाषा सीखेगा।
7. 🧠 श्रवण क्षमता:
o सुनने की क्षमता ठीक होने पर ही बच्चा सही रूप से भाषा सीख सकता है।
निष्कर्ष:
भाषा विकास एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न अवस्थाओं और कारकों के प्रभाव में होती है। यदि बच्चे को अनुकूल वातावरण, संवाद, और सहयोग मिले तो वह भाषा को आसानी से और प्रभावी ढंग से सीख सकता है।
अगर तुम चाहो तो मैं इस विषय पर एक चार्ट या पॉइंट-फॉर्म प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकता हूँ।
****प्रश्न – भाषा विकास क्या
भाषा विकास
(LANGUAGE DEVELOPMENT)
भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है इस नाते उसे निरन्तर अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है अतः भाषा और विचारों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक सुन्दर और सुगम माध्यम है। एक गूंगा व्यक्ति दूसरों के सामने स्वयं को कितना असहाय महसूस करता है जब वह अपने विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट नहीं कर पाता है। यद्यपि वह अपने हाव-भाव तथा अंग संचालन द्वारा अपनी बात को कहने का प्रयास करता है किन्तु उसमें इतनी स्पष्टता नहीं होती है। अतः भाषा के माध्यम से विचारों को प्रकट करने पर उनमें स्पष्टता आ जाती है। अतः प्रत्येक बालक के विकास क्रम में भाषा विकास होना परम आवश्यक है। भाषा विकास बालकों के मानसिक और सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करता है। भाषा के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान करने से व्यक्ति की सामाजिकता का विकास होता है। इसी प्रकार पढ़ने, लिखने, सीखने आदि सभी क्रियाओं में भी भाषा विकास माध्यम का कार्य करता है। भाषा विकास के कारण ही मानव दूसरे जीवों से श्रेष्ठ माना जाता है। मानव की सभ्यता व संस्कृति का विकास भी भाषा की ही देन है।
वाणी और भाषा में अन्तर
(DIFFERENCE BETWEEN SPEECH AND LANGUAGE)
सामान्यतः वाणी और भाषा इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है जबकि इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग-अलग है।
वाणी (speech) का एक रूप ध्वनि और शब्दों (sound and words) के माध्यम से अर्थ को दूसरों पर स्पष्ट किया जाता है। जब बालक के उच्चारण केवल ध्वनि संकेतों के रूप में रहते हैं तो उन्हें वाणी नहीं कहा जा सकता है। स्पष्ट व नियन्त्रित ध्वनि को ही वाणी कहा जाता है। बालकों का वाणी विकास प्रारम्भ में अस्पष्ट होता है किन्तु जैसे-जैसे स्नायुमण्डल का विकास होता जाता है उसकी वाणी स्पष्ट होती जाती है।
बालक की प्रत्येक ध्वनि वाणी नहीं होती है। जब बालक के द्वारा उच्चारित किये गये शब्दों का अर्थ बालक को ज्ञात होता है साथ ही जिस वस्तु के लिए शब्दों का उच्चारण किया गया है उनसे सम्बन्ध भी ज्ञात होता है। तभी उसके द्वारा उच्चारित ध्वनि को वाणी कहा जाता है। जैसे-यदि प्रारम्भ में बालक बाबा ध्वनि का उच्चारण करता है किन्तु वह बाबा से अपने सम्बन्ध को नहीं जानता है तो यह उच्चारित ध्वनि वाणी नहीं कही जा सकती है।
इसी प्रकार वे ध्वनियाँ जिन्हें बालक के आसपास रहने वाले सभी व्यक्ति आसानी से समझ सकें तो उसे वाणी कहा जाता है। यदि बालक द्वारा उच्चारित ध्वनि और शब्दों को केवल माता-पिता ही समझ पाते हैं तो उसे वाणी विकास नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार ध्वनियों और शब्दों के सम्मिलित रूप को वाणी कहते हैं।
”
इसके विपरीत भाषा, वाणी का विस्तृत रूप है। इसके अन्तर्गत विचारों तथा भावों को प्रकट करने के सभी साधन; जैसे-बोलना, पढ़ना, लिखना, हावभाव, संकेत तथा कलात्मक अभिव्यक्तियाँ आती हैं। भाषा के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सकता है।
अतः भाषा विकास वाणी विकास का ही विस्तृत रूप है। बालकों में वाणी विकास से ही भाषा विकास की शुरुआत होती है। जन्म के पश्चात् कुछ माह तक शिशु अपनी वाणी के माध्यम से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शब्दों का उच्चारण करता है। ये शब्द अर्थहीन होते हैं किन्तु इनके उच्चारण से माता-पिता उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं। आयु वृद्धि के साथ जैसे-जैसे भाषा विकास होता जाता वैसे-वैसे भाषा के माध्यम तथा वाक् चातुर्य से बालक अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने लगता है।
बालकों का भाषा विकास एक लम्बी व जटिल प्रक्रिया है। बालकों का भाषा विकास जन्म के तुरन्त बाद उनके प्रथम क्रन्दन से ही प्रारम्भ हो जाता है। फिर जन्म के बाद भी यह क्रन्दन भूख लगने पर, बिस्तर गीला होने या अधिक गर्मी या सर्दी लगने पर प्रदर्शित होता रहता है। 4-5 माह की अवस्था में शिशु अस्पष्ट ध्वनियों क उच्चारण करने लगता है फिर इसी क्रम में धीरे-धीरे अर्थहीन शब्दों का उच्चारण प्रारम्भ कर देता है। धीरे-धीरे इन शब्दों की संख्या बढ़ती जाती है और फिर वह कुछ निश्चित ध्वनियों को ही उच्चारित करता है जो कि सारयुक्त होती हैं, धीरे-धीरे शब्दों से वाक्यों तक पहुँचकर बालक के भाषा विकास में परिपक्वता आ जाती है तथा अन्य विभिन्न प्रकार का साहित्य भाषा की ही देन है।
संस्कृति के हस्तान्तरण में सहायक-
भाषा किसी भी व्यक्ति, समुदाय, समाज तथा राष्ट्र की सभ्यता व संस्कृति का दर्पण होती है। भाषा विकास किसी देश की सभ्यता व संस्कृति को उत्कृष्ट बनाता है। प्रत्येक समुदाय तथा समाज के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसके द्वारा उस समाज की सामाजिक तथा सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित होती रहती है।
भाषा विकास के प्रमुख सिद्धान्त
(THEORIES OF LANGUAGE DEVELOPMENT)
वैज्ञानिकों का मानना है बालकों के प्रथम क्रन्दन से ही उनका भाषा विकास प्रारम्भ हो जाता है किन्तु उसका भाषा विकास कुछ सिद्धान्तों के अनुसार ही होता है, ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-
1. बोलने के लिए प्रेरणा (Motivation of Speak ) – प्रारम्भ में प्रत्येक बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शब्दों का उच्चारण करता है। अतः बालक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बोलना सीखता है। यदि उसकी आवश्यकताओं के उसके संकेतों और हावभाव को देखकर ही पूरा कर दिया जायेगा तो उसका भाषा विकास कुंठित हो जायेगा। अतः माता-पिता तथा संरक्षकों को चाहिए कि प्रारम्भ से ही बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें तथा बालक को उसकी विभिन्न आवश्यकताओं से सम्बन्धित शब्दों का उच्चारण करके बतायें जिससे उसके भीतर शब्द भण्डार का क्रमशः विकास हो। अतः जब बालकों को बोलने के लिए उचित प्रोत्साहन व प्रेरणा मिलती है तो प्रारम्भ में उसके शब्द भण्डार में उन्हीं शब्दों का बाहुल्य होता है जो उसकी आवश्यकताओं से सम्बन्धित होते हैं। अतः बालक का भाषा विकास प्रेरणाओं पर आधारित होता है। प्रेरणा के अभाव में उसका भाषा विकास या तो कुंठित हो जाता है या देर से होता है।
2. अनुकरण की प्रणाली (Mechanism of Imitation)—बालक के भाषा विकास के सम्बन्ध में अनेक बाल-मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किये और वे सभी इस बात को मानते हैं कि भाषा विकास में अनुकरण का हाथ सबसे अधिक होता है। हरलॉक का मानना है कि बालक अनुकरण द्वारा ‘हकलाना’ (stammering) तथा गलत उच्चारण करना भी सीखता है।
प्रत्येक बालक अपने भाषा विकास क्रम में माँ तथा अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों द्वारा बोले गये शब्दों की ध्वनियों और उच्चारण का अनुकरण करता रहता र है। प्रारम्भ में शिशु स्वरों का अनुकरण करता है फिर जैसे-जैसे स्वर यन्त्र परिपक्व होता जाता है वह व्यंजनों का भी उच्चारण करने लगता है। अतः यह आवश्यक है कि बालकों के शुद्ध तथा स्पष्ट शब्दों का उच्चारण किया जाये क्योंकि एक बार जब बालक अनुकरण द्वारा बोलने लगता है तो उसे अपने द्वारा उच्चारित शब्दों से आनन्द की प्राप्ति होती है कि वह उन्हें बार-बार दुहराता है। बार-बार शब्दों का उच्चारण करने से वह गलत, सही सभी शब्दों के उच्चारण में दक्षता प्राप्त कर लेता है।
इस सम्बन्ध में स्ट्रेचर का मत है कि जब बालक अनुकरण द्वारा सीखता है तो उसे उच्चारण से सम्बन्धित सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए।
3. स्वरयंत्र की परिपक्वता (Maturation of Larynx) –बालकों के बोलने की क्रिया में कई अंग एक साथ कार्य करते हैं, जैसे-गला, जीभ, फेफड़े, स्वरयन्त्र आदि । इन अंगों की परिपक्वता पर ही बालक का भाषा विकास निर्भर करता है। ये सभी अंग जब तक अपने परिपक्वता स्तर को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक बालक का भाषा विकास सम्भव नहीं है। जैसे-जैसे इन अंगों में परिपक्वता आती जाती है वैसे-वैसे भाषा परिष्कृत और परिपक्व होती जाती है अतः बिना स्वरयन्त्र के परिपक्व हुये भाषा विकास सम्भव नहीं है
4. सम्बद्धता की प्रणाली (Conditioning)—बाल-मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक का भाषा विकास सम्बद्धता की प्रणाली पर आधारित होता है। भाषा विकास क्रम में पहले बालक अर्थहीन और निरर्थक शब्दों को उच्चारण करता है किन्तु जब उसके द्वारा उच्चारित शब्दों के साथ किसी वस्तु को उसके सामने प्रदर्शित किया जाता है तो वह अपने द्वारा उच्चारित शब्दों के अर्थ का सम्बन्ध वस्तु के साथ जोड़ लेता है। जैसे यदि बालक के सामने दूध की बोतल या गिलास ले जाकर दूध शब्द का उच्चारण किया जाता है तो वह धीरे-धीरे यह समझने लगता है कि बोतल या गिलास का दूध के साथ सम्बन्ध है। अतः जब-जब उसके सामने दूध शब्द का उच्चारण किया जाता है तो वह उसका सम्बन्ध जोड़ लेता है और फिर स्वयं ही भूख लगने पर दूध शब्द का उच्चारण करने लगता है।
मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सम्बद्धता की प्रणाली द्वारा बालक भाषा विकास के अतिरिक्त अपने वातावरण के साथ आसानी से समायोजन कर लेता है तथा स्वयं में
अनेक कौशलों का विकास करता है।
भाषा का स्नायुविक आधार (Neural Base of Language)-भाषा विकास के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किये उनके अनुसार भाषा विकास स्नायु तन्त्र की परिपक्वता तथा कार्यों पर निर्भर करता है।
भाषा विकास का महत्व
(IMPORTANCE OF LANGUAGE DEVELOPMENT)
भाषा विचारों और भावों के प्रकटीकरण का माध्यम है। इसके द्वारा प्राणी को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक सभी क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है।
1. सामाजिक सम्बन्धों के निर्माण में सहायक-किसी भी सामाजिक समूह का अंग बनने में भाषा एक सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति समूह के सदस्यों के बीच अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की बहुत-सी बातों को अपने जीवन में अपनाता है और समाज के रीति-रिवाजों, आदर्शों, परम्पराओं तथा नियमों को सीखता है। भाषा के माध्यम से ही प्रत्येक व्यक्ति समाज में व्यक्तियों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करता है। जो बालक बहिर्मुखी होते हैं वे समाज व समूह के साथियों के बीच अधिक लोकप्रिय होते हैं। इसके विपरीत अन्तर्मुखी बालक जो हमेशा शान्त रहते हैं वे अनेकानेक प्रतिभायें होने पर भी समाज में लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं। भाषा के द्वारा कोई भी व्यक्ति समूह का नेतृत्व पा सकता है क्योंकि वाकचातुर्य में दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है अतः भाषा सामाजिक सम्बन्धों के निर्माण में सहायता प्रदान करती है।
एलिस (Ellis) के अनुसार-“भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है।”
2. सामाजिक समायोजन में सहायक-भाषा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपना स्थान बनाता है और सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण करता है जिससे उसका सामाजिक समायोजन आसान हो जाता है। गूंगे व्यक्ति जो भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान-प्रदान नहीं कर पाते हैं उनको समायोजन करने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार वे व्यक्ति जो अपने प्रान्त की भाषा का ही ज्ञान रखते हैं जब वे किसी दूसरे प्रान्त में जाते हैं तो उन्हें दूसरे प्रान्त की भाषा का ज्ञान न होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः भाषा के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति आसान हो जाने से समायोजन में कठिनाई नहीं होती है। इसी प्रकार वे बालक आसानी से सामाजिक समायोजन स्थापित कर लेते हैं जिनमें विचारों की अभिव्यक्ति की निपुणता पायी जाती है।
3. नेतृत्व के विकास में सहायक-भाषा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति समूह का नेता बन सकता है। विचारों को जो व्यक्ति कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त कर लेते हैं उनकी वाणी व्यक्तियों को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर लेती है अतः नेतृत्व गुणों के विकास में भाषा सहयोग प्रदान करती है।
4. स्व-मूल्यांकन में सहायक – कोई भी बालक जब समाज के बीच रहकर भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान-प्रदान करता है तो समाज के व्यक्ति उसके विचारों और भावों से उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं जो बालक समूह के बीच लोकप्रिय हो जाता है। वह स्वयं ही अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लेता है कि समाज में उसका क्या स्थान है और समाज के सदस्य उसके बारे में क्या सोचते हैं ? स्व-मूल्यांकन से बालक के अन्दर स्व-प्रत्यय (self-concept) का निर्माण होता है जो उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है।
5. शैक्षणिक उपलब्धि में सहायक-शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए भाषा ज्ञान आवश्यक है। बालक कैसे बोलता है? क्या बोलता है, उसका शब्द-भण्डार कितना है,उसका वाक्य विन्यास कैसा है ? इन सभी बातों से उसकी शैक्षणिक उपलब्धियाँ प्रभावित होती हैं। जिस बालक का शब्द-भण्डार बड़ा होता है, वाक्य विन्यास अच्छा होता है तथा भाषा के प्रस्तुतीरकण में सौन्दर्य व मधुरता होती है उन बालकों की शैक्षणिक उपलब्धियाँ सामान्य बालकों से अधिक होती हैं। इस सम्बन्ध में गैरीसन (Garrison) ने लिखा है कि, “एक बालक का शब्द-भण्डार कितना है इससे इस बात का निर्धारण करता है कि उस बालक का विद्यालय में प्रगति स्तर किस प्रकार का होगा, वह विद्यालय में प्रगति करेगा या सामान्य प्रगति में असफल रहेगा।”
अतः शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए बालक के शब्द-भण्डार का विस्तृत होना आवश्यक है। किसी भी बालक का शब्द भण्डार जितना अधिक विस्तृत होता है उसे अपने वातावरण को समझने में उतनी ही अधिक सुविधा होती है।
6. मानव विकास में सहायक-भाषा मानव विकास की आधारशिला है। जो बालक अपने विचारों का प्रकटीकरण सीमित, सन्तुलित तथा प्रभावशाली भाषा में करते हैं वे जीवन में विकास की ओर अग्रसर होते हैं तथा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करते हैं।
7. साहित्य के सृजन में सहायक- किसी भी देश की भाषा ही वहाँ के साहित्य का सर्जन करती है। भाषा ने ही हमें अनेकों महान ग्रंथ दिये हैं-वेद, उपनिषद्, कथायें । मानव मस्तिष्क के दो भाग होते हैं-दायाँ भाग और बायाँ भाग । मस्तिष्क का बायाँ भाग भाषा विकास को प्रभावित करता है किन्तु अध्ययनों में यह भी देखा गया कि यदि किसी कारण वश जन्म के समय मस्तिष्क का बायाँ भाग कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उनके भाषा विकास को दायाँ भाग नियन्त्रित कर लेता है किन्तु जन्म के बाद 2-3 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क का बायाँ भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो निश्चयपूर्वक बालक का भाषा विकास अन्य बालकों के समान नहीं होता है। अतः भाषा विकास स्नायुतंत्र की संरचना तथा कार्यों पर निर्भर करता है।
भाषा विकास की अवस्थायें या भाषा विकास के चरण
(STAGES OF SPEECH DEVELOPMENT OR STEPS OF LANGUAGE DEVELOPMENT)
बालकों का भाषा विकास एकाएक नहीं होता है। यह तो एक लम्बी और जटिल प्रक्रिया है जिसके कई सोपान हैं। वैसे जन्म के बाद प्रथम क्रन्दन को ही भाषा विकास की प्रारम्भिक अवस्था माना जाता है किन्तु इस समय उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि उसका क्रन्दन किस कारण से है। बालक का वास्तविक भाषा विकास तभी माना जाता है जब वह स्वयं द्वारा उच्चारित शब्दों का अर्थ समझ सके तथा शब्दों का व्यक्तियों तथा वस्तुओं से सम्बन्ध जोड़ सके। अतः बालकों के भाषा विकास की अवस्थाओं को पाँच भागों में बाँटा जाता है-
1. बोलने की तैयारी-क्रन्द्रन, बलबलाना, हावभाव,
2. आकलन शक्ति का विकास,
3. शब्द प्रयोग,
4. वाक्य प्रयोग,
5. शुद्ध उच्चारण ।
1. बोलने की तैयारी (Preparation for Speech) — भाषा विकास की प्रारम्भिक अवस्था ही “बोलने की तैयारी है” है। यह अवस्था जन्म के बाद से प्रारम्भ होकर 13 से 14 महीने तक रहती है। भाषा विकास की इस प्रक्रिया के दौरान बालक क्रन्दन द्वारा, बलबलाहट द्वारा तथा हावभाव द्वारा अपनी वाणी को प्रकट करने का प्रयास करता है।
(i) क्रन्दन (Crying)—प्रत्येक सामान्य शिशु के जीवन का प्रारम्भ उसके क्रन्दन से होता है। मनोवैज्ञानिकों ने क्रन्दन को ही भाषा विकास का प्रारम्भिक स्वरूप माना है। बालकों की यह क्रिया एक सहज क्रिया है इसका बालक से कोई बौद्धिक या संवेगात्मक सम्बन्ध नहीं होता है। जन्म के बाद प्रथम क्रन्दन तो एक प्राकृतिक क्रिया है। जन्म के बाद प्रथम दो सप्ताह तक भी बालकों का रोना उद्देश्यहीन तथा अनियमित होता है किन्तु आयु वृद्धि के साथ-साथ शिशु का क्रन्दन उसकी आवश्यकताओं से जुड़ता जाता है। तीन-चार सप्ताह के शिशु के क्रन्दन से यह स्पष्ट होने लगता है कि या तो वह भूखा है, उसे कोई पीड़ा है, या उसके वस्त्र व बिस्तर गीला हो गया है।
शिशु क्रन्दन के कारण-जन्म के पश्चात् दो सप्ताह तक तो शिशु क्रन्दन की क्रिया निरर्थक होती है लेकिन दो सप्ताह बाद शिशु का क्रन्दन परिस्थितिजन्य हो जाता है। शिशु क्रन्दन के उसके आन्तरिक व बाह्य कारण हो सकते हैं; जैसे-भूख, थकान, पीड़ा, गीले वस्त्र, तीव्र ध्वनियाँ, तीव्र प्रकाश, भय आदि । जैसे-जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है उनके रोने के कारणों में वृद्धि होती जाती है। तीन-चार माह का बालक अपने आसपास दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति को समझने लगता है। अतः उसका क्रन्दन दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी होने लगता है। चार-पाँच माह का शिशु अपरिचित व्यक्तियों को देखकर रोने लगता है। 6-7 माह के शिशु अपनी प्रिय छीन लेने पर रोते हैं यदि उनकी क्रियाओं में बाधा उत्पन्न की जाती है तो भी रोने लगते हैं। 1 वर्ष का बालक भय, अपरिचित व्यक्ति व परिस्थिति, कसे वस्त्र, भूख-प्यास तथा पीड़ा की स्थिति में रोता है। वे बालक अन्य बालकों की तुलना में अधिक रोते हैं जो क्रन्दन को अपनी आवश्यकता पूर्ति का साधन समझते हैं।
शिशु क्रन्दन में शारीरिक स्थितियाँ-सभी बालकों का रोने का स्वरूप समान नहीं होता है, कुछ बालक अधिक रोते हैं जबकि कुछ बालक कम। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो गर्भवती मातायें गर्भावस्था में संवेगात्मक रूप से अस्थिर रहती हैं जन्म के पश्चात् उनके शिशुओं के क्रन्दन की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसके विपरीत संवेगात्मक रूप से सन्तुलित गर्भवती माताओं के शिशु कम रोते हैं। रोते समय बालकों की आन्तरिक तथा बाह्य शारीरिक स्थितियों में परिवर्तन आ जाता है जो बच्चे जितनी अधिक तेजी से रोते हैं उनकी शारीरिक क्रियायें, जैसे-हाथ-पैर पटकना, शरीर को पलटना, उतनी ही तीव्र होती है इसके अतिरिक्त रोते समय चेहरा लाल हो जाता है, साँस की गति अनियमित तथा अनियन्त्रित हो जाती है। एक माह से अधिक आयु शिशु की आँखों से आँसू भी निकलते हैं। आयु वृद्धि के साथ-साथ बालक के क्रन्दन में कमी आती जाती है।
शिशु क्रन्दन से लाभ व हानि-
भाषा-विकास क्रम में रोने का अपना महत्व है क्योंकि इसी से भाषा विकास प्रारम्भ होता है किन्तु रोने को आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम जब बालक बना लेता है तो वह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए अधिक रोते हैं वे चिड़चिड़े व जिद्दी हो जाते हैं। फलस्वरूप अधिक रोने से उनका शरीर दुर्बल हो जाता है।
शिशु का सामान्य रोना स्वास्थ्य के लिए व्यायाम का कार्य करता है। रोने से शिशु की माँसपेशियों की वृद्धि होती है उनमें क्रियाशीलता आती है। इसके साथ ही रोने से शिशु के संवेगों का प्रकटीकरण होता है ।
शिशु का अधिक रोना प्रत्येक अवस्था में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः जब शिशु भाषा का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दे तो उसके रोने में कमी आ जानी चाहिए। बालक की रोने की आदत बन जाना अहितकर है। इससे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक सभी प्रकार का विकास प्रभावित होता है अतः आयु वृद्धि के साथ-साथ बालक के क्रन्दन में कमी आनी चाहिए। जब बालक पाँच वर्ष का हो जाये तो उसका अनावश्यक रोना बन्द हो जाना चाहिए ।
(ii) बलबलाना (Babbling) – आयु वृद्धि के साथ-साथ बच्चों का रोना कम हो जाता है किन्तु उनके स्थान पर शिशु अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालने लगता है जिसे ‘बलबलाना’ कहते हैं। बलबलाने से ही बालक में शब्दोच्चारण का विकास होता है। पहले माह में अन्त से ही बालक कुछ सरल ध्वनियाँ निकालने लगता है। स्पष्ट बलबलाहट दो माह की आयु से प्रारम्भ हो जाती है और लगभग 12 वर्ष की आयु तक चलती रहती है। बलबलाने से बालक का स्वरयन्त्र (larynx) परिपक्व होता है।
बलबलाने की प्रारम्भिक अवस्था में बालक एक ही ध्वनि की पुनरावृत्ति करता है। प्रारम्भ में बालक स्वरों को फिर बाद में व्यंजनों को उच्चारित करता है। ध्वनियों का उच्चारण बालक अन्य लोगों द्वारा बोले गये शब्दों को सुनकर करता है। प्रारम्भ में जब वह स्वरों को दुहराता है तो उसे आनन्द की अनुभूति होती है; जैसे- वह प्रारम्भ में बा, भा, पा, ना आदि स्वरों को दुहराता है तो उन्हीं से बाद में बाबा, मामा, पापा, नाना आदि शब्दों का विकास होता है |
बलबलाने की क्रिया अनुकरण पर आधारित होती है। बालक अपने माता-पिता तथा आसपास रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा बोले गये शब्दों का निरन्तर अनुकरण करता रहता है और फिर स्वयं भी उन्हीं ध्वनियों को दोहराता है। धीरे-धीरे सम्बद्धता (conditioning) के आधार पर इन शब्दों का अर्थ भी समझने लगता है।
कुछ विद्वानों का मानना है कि बलबलाने की क्रिया बालक अनुकरण द्वारा नहीं करता वरन इसलिए करता है कि उसके द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ उसे प्रिय लगती हैं अतः वह खेल की तरह बलबलाने का कार्य करता है।
बालकों की बलबलाने की क्रिया का कोई तात्कालिक महत्व नहीं होता है किन्तु भाषा विकास में इसका दीर्घगामी परिणाम देखा जा सकता है। बलबलाने की क्रिया से शिशु का स्वरयन्त्र परिपक्व होता है। बलबलाने से ही शब्दोच्चारण को आधार मिलता है और धीरे-धीरे भाषा-विकास होता है।
(iii) हावभाव (Gestures) –हावभाव से तात्पर्य है कि अपने विभिन्न शारीरिक अंगों के माध्यम से अपने विचारों को प्रदर्शित करना। बालक के भाषा विकास में हावभाव भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बालकों द्वारा हावभाव का प्रदर्शन भाषा के पूरक के रूप में किया जाता है। बच्चों में हावभाव की उत्पत्ति बलबलाने के साथ-साथ ही हो जाती है। बच्चा अपने हावभावों का प्रदर्शन, मुस्कराकर, हाथ फैलाकर, उँगली दिखाकर, मूक भाषा में व्यक्त करता है। अतः बच्चों के लिए हावभाव, विचारों की अभिव्यक्ति का एक सुगम साधन है जो शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है।
`
हावभाव का प्रदर्शन बड़े बालकों द्वारा भी किया जाता है किन्तु बच्चों और बालकों के हावभाव के प्रदर्शन में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। बच्चों का प्रदर्शन मूक होता है जबकि बालकों का प्रदर्शन शब्दों के उच्चारण के साथ उनके अनुसार होता है। जैसे-जैसे बालक का भाषा विकास होता जाता है हाव भाव का प्रदर्शन कम हो जाता है।
शिशु के जीवन में हावभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि हावभाव के अभाव में शिशु अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान वयस्कों को नहीं करा सकता है। भाषा विकास के साथ हावभावों में कमी आ जाती है किन्तु ये पूर्णतः समाप्त नहीं होते हैं।
2. आकलन शक्ति का विकास (Development of Comprehension)—–बालकों की वह क्षमता जिसके द्वारा वह दूसरों की क्रियाओं तथा हावभाव का अनुकरण कर लेता है ‘आकलन शक्ति’ कहलाती है। हरलॉक के मतानुसार बालकों में आकलन शक्ति का विकास शब्दों के प्रयोग से पहले प्रारम्भ हो जाता है वह शब्दों को समझना पहले सीखता है और बोलना बाद में।
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिशुओं में तीन चार माह की आयु से आकलन शक्ति का विकास प्रारम्भ हो जाता है। चार माह का शिशु माँ को पहचानकर मुस्कराने लगता है। 7-8 माह का बालक शब्दों का अनुसरण करने लगता है और एक वर्ष का बालक सरल निर्देशों को समझने लगता है। पाँच वर्ष की अवस्था में आकलन शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है।
बालकों की आकलन शक्ति में शब्दों के साथ-साथ हावभाव भी होते हैं। बालक उन वाक्यों और शब्दों को जल्दी शीघ्रता से सीखता है जिनके साथ हावभाव भी सम्मिलित रहते हैं।
बालक के बौद्धिक विकास तथा आकलन शक्ति का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। तीव्र बुद्धि बालकों की आकलन शक्ति अधिक होती है।
3. शब्द प्रयोग (Vocabulary) – आयु वृद्धि और आकलन शक्ति के विकास से बालक का शब्द भण्डार बढ़ता है। प्रारम्भ में वह संज्ञाओं (nouns) का प्रयोग करता है। दो वर्ष का बालक लगभग 50% संज्ञा शब्द बोल लेता है। ये संज्ञा शब्द खिलौनों, खाने-पीने की चीजों, वस्त्रों और व्यक्तियों से सम्बन्धित होते हैं। सबसे पहले बालक साधारण क्रिया-सूचक शब्दों; जैसे-आओ, जाओ, खाओ, लो, दो का प्रयोग करता है। शिशु केवल इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं करता अपितु उनका अर्थ भी समझता है। डेढ़ वर्ष की अवस्था में वह विशेषण शब्दों (adjectives) का प्रयोग भी करने लगते है। ये विशेषण शब्द भोज्य पदार्थों और खिलौनों से सम्बन्धित होते हैं। प्रारम्भ में बालकों द्वारा अच्छा, बुरा, गरम, ठंडा आदि विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बालक तीन वर्ष की अवस्था में करने लगता है। प्रारम्भ में मैं, मेरा, तू, तेरा, यह, वह, तुम, तुझे, उसका, उसे आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है किन्तु प्रारम्भ में उसे यह ज्ञान नहीं होता है कि उसे कौन-सा शब्द कब बोलना चाहिए। अन्य प्रकार के शब्दों का प्रयोग वह पाँच-छ: वर्ष की अवस्था में करता है।
बालक की शब्दावली के विकास के साथ-साथ उसके शब्द-भण्डार में भी वृद्धि होती है। 1 वर्ष की आयु में बालक की शब्दावली में केवल कुछ शब्द रहते हैं। इसके बाद शब्द भण्डार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। शब्द भण्डार की वृद्धि के दौरान वह केवल नये शब्द ही नहीं सीखता बल्कि पहले सीखे गये शब्दों का नया अर्थ भी सीखता है। बालक द्वारा बोले गये प्रथम शब्द ‘होलोफ्रेसस’ (holophrases) कहलाते हैं क्योंकि एक शब्द में बालक का सम्पूर्ण आशय निहित होता है।
स्मिथ, शर्ली, गैसेल तथा थम्पसन आदि वैज्ञानिकों ने बालकों के शब्द भण्डार तथा शब्द चयन के लिए अध्ययन किये और बताया कि डेढ़ वर्ष के बालक का शब्द भण्डार 10 शब्द, दो वर्ष के बालक का शब्द-भण्डार 272 शब्द, ढाई वर्ष में 450 शब्द, तीन वर्ष की अवस्था में 900 शब्द तथा चार वर्ष की अवस्था में 1500 शब्दों का हो जाता है। पाँच वर्ष में यह बढ़कर 2000 तथा छः वर्ष में लगभग 2500 हो जाता है। इस प्रकार दिन-प्रतिदिन उसका शब्द भण्डार बढ़ता जाता है।
अध्ययनों में यह भी देखा है कि बालिकाओं का शब्द भण्डार सभी अवस्थाओं में बालकों की अपेक्षा अधिक रहता है।
बालकों के शब्द-भण्डार के रूप-बालकों का शब्द-भण्डार दो प्रकार का माना गया है-
(1) सामान्य शब्द-भण्डार (General Vocabulary)
(2) विशिष्ट शब्द-भण्डार (Special Vocabulary)
(1) सामान्य शब्द-भण्डार (General Vocabulary) बालक सामान्य परिस्थितियाँ में जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे उसके सामान्य शब्द कहलाते हैं। ये शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया सम्बन्धी होते हैं, जैसे-लेना, देना, आना, जाना, अच्छा, बुरा, मामा, नाना, पापा आदि।
(2) विशिष्ट शब्द-भण्डार (Special Vocabulary)–विशिष्ट शब्द-भण्डार के अन्तर्गत वे शब्द आते हैं जिन्हें बालक विशेष अवसरों पर बोलता है। अधिकांशतः तीन चार वर्ष की आयु में बालक विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करने लगता है। पाँच-छ: वर्षों में विशिष्ट शब्दावली का काफी मात्रा में विकास हो जाता है। बालकों की विशिष्ट शब्दावली अनेक रूपों में प्रकट होती है।
(i) शिष्टाचार के शब्द (Etiquette Vocabulary)—जैसे-आप, जी, श्रीमान, साहब, महाशय, कृपया, धन्यवाद आदि। इन शब्दों को बालक स्कूल जाने पर अधिक मात्रा में सीखता है। इन शब्दों द्वारा बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करता है।
(ii) संख्यात्मक शब्द (Number Vocabulary)—जैसे-गिनती, पहाड़े आदि । (iii) रंगों से सम्बन्धित शब्द (Colour Vocabulary) – जैसे-लाल, हरा, नीला, पीला आदि । चार वर्ष की आयु तक बालक तीन प्राथमिक रंगों-लाल, पीला, नीला उच्चारित करने लगता है।
(iv) समय सम्बन्धी शब्द (Time Vocabulary) – जैसे-सुबह, शाम, रात, आज, कल, परसों, दिन, वर्ष, माह आदि ।
(v) धन से सम्बन्धित शब्द (Money Vocabulary)—विभिन्न सिक्कों से सम्बन्धित शब्दों का उच्चारण बालक पाँच वर्ष की अवस्था तक सीख जाता है
(vi) अशिष्ट शब्द (Slong Vocabulary)—जैसे-गाली-गलौज के गंदे शब्दों का उच्चारण करना बालक पाँच से आठ वर्ष की अवस्था में सीख जाता है। संवेगात्मक तनाव व अस्थिरता की अवस्था में बालक अशिष्ट शब्दों का उच्चारण करता है।
4. वाक्य निर्माण (Sentence Formation)—वाक्य निर्माण भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि वाक्यों के द्वारा बालक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। वाक्य निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में बालक केवल एक शब्दीय वाक्य बोलता है। यह शब्द या तो संज्ञा या फिर क्रिया होता है। उदाहरण के लिए यदि ‘बालक पापा शब्द का प्रयोग करता है तो उसका अर्थ है वह पापा के पास जाना चाहता है। इसी प्रकार यदि वह दूध की बोतल देखकर कहता है दे दो, इसका तात्पर्य है वह दूध पीना चाहता है। ऐसे शब्द बालक एक से डेढ़ वर्ष की अवस्था के बीच अधिक बोलता है। एक शब्दीय वाक्यों के साथ बालक हावभावों का भी प्रदर्शन करता है; जैसे- दूध की बोतल की ओर उँगली करके कहता है दे दो। तीन चार वर्ष की अवस्था में बालकों के वाक्यों में शब्दों की संख्या बढ़ जाती है मैकार्थी (McCarthy) के अनुसार तीन वर्ष का बालक, तीन और चार वर्ष का बालक चार या पाँच शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करता है। ऐसे वाक्यों में संज्ञाओं, क्रियाओं और विश्लेषणों का मिश्रण होता है। इस अवस्था को ‘अपूर्ण वाक्य की अवस्था’ या ‘लघु वाक्य की अवस्था’ कहा जाता है। जैसे-बालक कहता है पापा ऑफिस गये, मैंने दूध पिया आदि। इसी प्रकार विकास क्रम में पाँच-छः वर्ष का बालक 10 शब्दों तक का प्रयोग अपने वाक्यों में कर लेता है।
बालकों के वाक्य निर्माण में यह देखा गया है कि पहले बालक साधारण वाक्यों (simple sentence) को बोलते हैं। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों का प्रयोग पाँच-छ: वर्ष की अवस्था में कर पाते हैं।
5. शुद्ध उच्चारण (Correct Pronunciation) — शुद्ध उच्चारण भाषा विकास की अन्तिम अवस्था है। इसमें बालक अपने व्याकरण सम्बन्धी दोषों को सुधारता है और उच्चारण शुद्ध करता है। तीन वर्ष की आयु तक बालक की भाषा में बहुत अधिक व्याकरण सम्बन्धी दोष पाये जाते हैं। विशेषकर बच्चे सर्वनाम शब्दों के प्रयोग, वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्यकाल के प्रयोग में त्रुटि करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके संज्ञाओं के लिंग तथा वचन के प्रयोग में भी त्रुटि होती है। अतः यह आवश्यक है कि ठीक समय पर ही इन त्रुटियों का सुधार कर दिया जाये अन्यथा वे गलत शब्दों का उच्चारण करने लगते हैं। बच्चे व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियाँ भी अपनी भाषा में करते हैं किन्तु इस त्रुटि का निवारण धीरे-धीरे स्कूल जाने पर हो जाता है। कुछ बालक शब्दोच्चारण में भी त्रुटि करते हैं जैसे श को स बोलते हैं। इसका कारण घर में माता-पिता तथा अन्य व्यक्तियों का गलत शब्दोच्चारण करना होता है। कभी-कभी स्वरयन्त्र में खराबी होने से भी शब्दों का उच्चारण सही नहीं हो पाता है। छः-सात वर्ष की अवस्था में स्वरयन्त्र भी पूर्ण परिपक्व हो जाता है तथा बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति भी इतनी अधिक विकसित हो जाती है कि वह शुद्ध उच्चारण द्वारा सुन्दर और शुद्ध भाषा का विकास कर सकता है।
बाल भाषा की सामग्री
(CONTENTS OF CHILDREN’S SPEECH)
बालक जब स्पष्ट उच्चारण करना सीख जाते हैं तब भी उनकी भाषा में कुछ विशेषतायें परिलक्षित होती हैं। ये विशेषतायें बाल भाषा की सामग्री कहलाती है। ये विशेषतायें अग्रलिखित हैं-
1. अहं की भावना (Ego-Centricity) छोटे बालकों की बातचीत का अधिकांश भाग स्वयं उनसे सम्बन्धित होता है क्योंकि यह अवस्था ‘स्वप्रेम की अवस्था’ होती है। अतः उनकी भाषा में मै, मेरा, मुझको आदि शब्दों की बहुलता होती है। कुछ बड़े हो जाने पर वे दूसरों के विषय में भी बातचीत करते हैं किन्तु उस समय भी उनकी बातों में अहंभाव की अधिकता पायी जाती है। अतः वे अपनी भाषा में आज्ञा-सूचक तथा प्रश्न-सूचक शब्दों का प्रयोग अधिक करते हैं।
2. प्रश्नों की अधिकता (Excess of Questions)—बालकों की बातचीत में प्रश्नों की अधिकता होती है क्योंकि नवीन वातावरण से समायोजन करने के पूर्व वह अपनी जिज्ञासा को शान्त करना चाहता है। कभी-कभी बालक दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी प्रश्न करता है। ऐसा देखा गया है कि बालक अधिकांश प्रश्न अपने माता-पिता से ही करता है क्योंकि माता-पिता उसकी जिज्ञासाओं को अच्छी तरह शान्त कर देते हैं।
3. भावात्मक सामग्री (Emotional Contents) – बालकों की भाषा में भावात्मक सामग्री की बहुलता होती है। वे अपनी बातों में अपने संवेगों का प्रदर्शन अधिक मात्रा में करते हैं वे या तो प्रसन्नतापूर्वक बातचीत करते हैं या दुखी होकर सुख, दुख के संवेगों के अलावा उनकी भाषा में क्रोध, भय, प्रेम, घृणा, आशा, निराशा आदि संवेग भी सम्मिलित रहते हैं।
4. शब्दों की पुनरावृत्ति (Repetition of Words) – बालकों की भाषा में प्रायः एक ही शब्द की पुनरावृत्ति अधिक होती है। ऐसा इस कारण से होता है कि बच्चे की अनुभव क्षमता और आयु दोनों ही कम होती हैं। वह अपने विचारों को जब स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है तो एक ही शब्द को बार-बार दुहराता है। डेविस ने इस सन्दर्भ में अध्ययन किया और बताया कि बोले गये प्रत्येक चार शब्दों में से एक शब्द बालकों द्वारा अवश्य दुहराया जाता है। बातचीत में कुशल न होने के कारण ही बालक शब्दों तथा वाक्यांशों को दोहराता है जब वह किसी विचार को आदेश में तीव्रता के साथ व्यक्त करता है और उसे यह समझ नहीं आता है कि आगे क्या बोलना है तो तुरन्त बोले गये शब्द को दोहरा देता है।
भाषा दोष
(SPEECH DEFECTS)
बालकों का भाषा विकास धीमी गति से व क्रमिक होता है। प्रारम्भ में बालक बोलना सीखता है तो स्वरयंत्र पूरी तरह परिपक्व न होने के कारण उसकी भाषा में कई प्रकार के दोष पाये जाते हैं; जैसे-अस्पष्ट बोलना, शब्दों का सही उच्चारण न करना, तुतलाना आदि। किन्तु ऐसा नहीं है कि ये दोष स्थायी हों और आयु वृद्धि के साथ इनमें वृद्धि हो। यदि इन दोषों का सुधार प्रारम्भिक अवस्था में ही कर दिया जाता है तो इनका निराकरण हो जाता है और यदि सुधार नहीं किया जाता है तो ये दोष स्थायी रूप लेते हैं जो बालकों में हीन-भावना का विकास करते हैं और उसके व्यक्तित्व के विकास को कुंठित कर देते हैं। भाषा दोष से पीड़ित बालकों के सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई होती है क्योंकि वे समूह के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपहास का पात्र बनते हैं। अतः माता-पिता संरक्षकों और अभिभावकों का यह दायित्व है कि यदि भाषा दोष जन्मजात नहीं है तो उनका निराकरण तुरन्त कर दें।
भाषा दोष के सम्बन्ध में हरलॉक ने लिखा है कि, “दोषपूर्ण भाषा अशुद्ध भाषा है। अधिकांशतः दोषपूर्ण शब्द का प्रयोग उच्चारण सम्बन्धी दोषों के लिए किया जाता है। लेकिन विस्तृत अर्थों में इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के भाषा दोष के लिए किया जाता है। विकार शब्द का प्रयोग उच्चारण के गम्भीर दोषों के लिए किया जाता है।”
भाषा दोष के प्रकार
बालकों के कई प्रकार के भाषा दोष पाये जाते हैं, ये निम्नलिखित हैं-
1. भ्रष्ट उच्चारण (Lisping)-भ्रष्ट उच्चारण बच्चों में पाया जाने वाला एक सामान्य दोष है। यह दोष बालकों में कई रूपों में देखने को मिलता है। इसका एक रूप यह है कि बालक अक्षरों की ध्वनियों को बदल देता है जैसे कुछ बच्चे ‘र’ को ‘ल’ उच्चारित करते हैं। कुछ बालक ‘स’ को ‘श’ और ‘श’ को ‘स’ बोलते हैं। बच्चे कुछ ‘स’ को ‘फ’ बोलते हैं। और ‘रोटी’ को ‘लोटी’ ‘समय’ को शमय, ‘शीला’ को ‘सीला’ आदि बोलते हैं, कुछ बच्चे ‘ड’ को ‘र’ बोलते हैं जैसे ‘गुड़’ को ‘गुर’ कहते हैं-
कारण-भ्रष्ट उच्चारण के कई कारण होते हैं-
(i) जबड़ों, दाँतों और ओठों की रचना ठीक न होना।
(ii) बालक द्वारा शैशवावस्था की भाषा दुहराने पर माता-पिता द्वारा आनन्द प्राप्त करना और बच्चे को उन्हीं शब्दों को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना ।
(iii) माता-पिता द्वारा भ्रष्ट उच्चारण करना ।
(iv) कभी-कभी बच्चों में यह भाषा दोष उस समय भी उत्पन्न हो जाता है जब बच्चे के सामने के दाँत टूट जाते हैं और बीच में रिक्त स्थान हो जाता है।
2. अस्पष्ट उच्चारण (Slurring)–अस्पष्ट उच्चारण में बालक शब्दों का उच्चारण इस प्रकार करते हैं कि उनका अर्थ ही समझ नहीं आता है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक बच्चों में यह भाषा दोष स्वतः ही दूर होने लगता है और यदि दूर नहीं होता है या नहीं किया जाता है तो यह स्थायी रूप ले लेता है। अस्पष्ट उच्चारण में बालक कभी-कभी किसी शब्द के किसी अक्षर को छोड़कर उच्चारण करता है; जैसे- कुछ बच्चे ट्रेन को टेन कहते हैं, आलूबुखारा को आलूबुखार आदि । बालकों में अस्पष्ट उच्चारण के कई कारण हो सकते हैं।
कारण-
(1) होठ, जीभ तथा जबड़े की माँसपेशियों की क्रियाशीलता में कमी।
(ii) अत्यधिक भय और संवेगात्मक तनाव।
(iii) अत्यधिक उत्तेजना के कारण जल्दी-जल्दी बोलना।
(iv) स्वरयन्त्र का अविकसित होना या लकवे के प्रभाव के कारण गतिविहीन होना।
3. तुतलाना (Sluttering)—इस भाषा दोष में बालक या तो बोलते-बोलते किसी शब्द का उच्चारण करने से पूर्व रुकावट का अनुभव करता है या किसी शब्द के प्रथम अक्षर या अक्षर समूह को कई बार दुहराता है। अतः इस भाषा दोष में बालक की वाणी असांमजस्यपूर्ण और पुनरावृत्ति वाली होती है। जैसे—वह कहना चाहता है, “मम्मी पानी दे दो तो वह कहेगा मममम मम्मी पपपप पानी दददद दे दो। अतः स्पष्ट है कि तुतलाने में बालक प्रथम अक्षर की पुनरावृत्ति कई बार करता है। तुतलाने का भाषा दोष जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में ही शुरू हो जाता है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि अधिकांश बालकों में यह भाषा दोष 22 वर्ष की अवस्था से ही प्रारम्भ हो जाता है। हरलॉक (Hurlock) के मतानुसार बालकों में तुतलाना 21⁄2 से 31⁄2 वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ होता है।
ब्लैन्टन ( Blanton) ने बालकों के तुतलाने सम्बन्धी भाषा दोष के कारण और हानि को जानने के लिए 400 बालकों तथा व्यक्तियों को प्रयोग का माध्यम बनाया और अनुसंधानों के पश्चात् बताया कि अधिकांश बालकों में तुतलाना 22 वर्ष की अवस्था से प्रारम्भ हो गया था किन्तु कुछ बालकों में तुतलाना छः वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ हुआ। इन दोनों ही अवस्थाओं में बालकों को सामाजिक समायोजन स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव हुआ।
कारण-बालकों के तुतलाने का कोई निश्चित कारण नहीं होता है। कुछ बच्चे केवल अपने माता-पिता के सामने ही तुतलाते हैं जबकि कुछ अजनबी व्यक्तियों और समूह के साथ समायोजन स्थापित न कर पाने की स्थिति में अज्ञात भय और घबराहट के कारण तुतलाते हैं।
4. हकलाना (Stammering) -आमतौर पर हकलाना और तुतलाने में कोई विशेष अन्तर नहीं माना जाता है जबकि हकलाना तुतलाने से भिन्न होता है। तुतलाने में किसी शब्द को बार-बार दोहराया जाता है जबकि हकलाने में एक शब्द उच्चारित करने पर व्यक्ति आगे की बात थोड़ी देर में कह पाता है। जैसे यदि वह कहना चाहता है कि “तुम कब जाओगे” तो वह ‘तुम कब’ कहकर आगे का शब्द बोलने की कोशिश करेगा किन्तु जल्दी बोल नहीं पायेगा। कुछ देर बाद जब वह तनाव मुक्त होता है तो फिर शेष शब्दों का उच्चारण करता है।
कारण-वैज्ञानिकों का मानना है कि हकलाने का कारण भी बालकों का भय और घबराहट है। इसके अतिरिक्त स्वरयन्त्र, गला, जीभ, फेफड़ा तथा होंठ सभी का सन्तुलन ठीक न होने पर बालकों में यह दोष उत्पन्न हो जाता है।
ट्रेविस (Travis) के मतानुसार, हकलाने का कारण मस्तिष्क में श्रवण एवं वाक् केन्द्रों (Auditory and Speech Centres) का विकृत हो जाना है।
हकलाने की क्रिया में बालक के चेहरे में तथा शारीरिक स्थितियों में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं क्योंकि जिन शब्दों को वह बोल नहीं पाता है उन्हें जोर डालकर बोलने के प्रयास में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं; जैसे-माथे पर लकीरें पड़ जाना, मुँह टेड़ा हो जाना, आँखें झपकाना आदि। जब बालक तीन वर्ष का होता है तो उसमें हकलाने की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है।
हकलाना बालक के समायोजन तथा विकास को प्रभावित करता है। जो बालक हकलाते हैं उन्हें सामाजिक समायोजन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि भाषा दोष के कारण उनका उपहास होता है। फलस्वरूप उनमें हीनभावना का विकास होता है जो उनके सामान्य विकास को अवरुद्ध कर देती है।
भाषा दोषों को दूर करने के उपाय-
भाषा दोष बालकों में हीनभावना को उत्पन्न करते हैं। यह भावना उनके स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है। अतः माता-पिता तथा शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों में भाषा दोषों को विकसित न होने दें। इसके लिए निम्न उपाय किये जा सकते हैं-
1. जिन बालकों में भाषा दोष हों उनका उपहास नहीं करना चाहिए ।
2. बालकों को प्रारम्भ से ही सही उच्चारण का प्रशिक्षण देना चाहिए।
3. बालकों की तोतली भाषा सभी को प्रिय लगती है किन्तु माता-पिता को चाहिए कि वे बालक की इस प्रवृत्ति को बढ़ावा न दें। इससे आयु बढ़ने पर उनका अस्पष्ट उच्चारण स्वतः ही समाप्त हो जायेगा ।
4. बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति पायी जाती है वे वही शब्द बोलते हैं जिन्हें अपने माता-पिता तथा आसपास रहने वाले व्यक्तियों से सुनते हैं। अतः वयस्क व्यक्तियों को बालक के सामने गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए। जैसे- माँ लाड़ में कहती है “मेरा बेता त्या थायेगा” जबकि उसके कहने का तात्पर्य है कि “मेरा बेटा क्या खायेगा” ।
5. बालकों कठोर नियन्त्रण में नहीं रखना चाहिए। कठोर नियन्त्रण से उनमें संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है फलस्वरूप भय और घबराहट में वे अपनी बात स्पष्ट प से नहीं कह पाते हैं। अतः बालकों के मन से उनके भय, घबराहट तथा संवेगात्मक तनाव की दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
.
6. बालकों को अपनी उम्र के बच्चों के साथ उठने-बैठने तथा खेलने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए जिससे यदि उनमें भाषा दोष है तो वह अपनी कमियों से अवगत हों तथा अपने हम उम्र बालकों की भाषा का अनुकरण कर स्पष्ट उच्चारण करना सीखें।
भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व
(FACTORS AFFECTING LANGUAGE DEVELOPMENT)
सभी बालकों में भाषा विकास की मात्रा और गति समान नहीं होती है। कोई बालक जल्दी बोलना सीखता है तो कोई देर से । इसी प्रकार कुछ बालकों को सीमित शब्दों की जानकारी होती है जबकि कुछ का शब्द-भण्डार अत्यधिक विकसित होता है। शब्दोच्चारण में भी कोई बालक शुद्ध उच्चारण करता है जबकि कुछ में भाषा सम्बन्धी दोष पाये जाते हैं। इस प्रकार देखा गया है कि बालकों के भाषा विकास में काफी अन्तर पाया जाता है। इस अन्तर के विभिन्न कारण होते हैं जिन्हें भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कहा जा सकता है। ये तत्व निम्नलिखित हैं-
1. शारीरिक स्वास्थ्य (Physical Health)—ऐसा देखा गया है कि जो बालक स्वस्थ व निरोगी होते हैं उनका भाषा विकास उन बालकों की तुलना में शीघ्र होता है जो अक्सर बीमार और अस्वस्थ रहते हैं। अस्वस्थ्य और बीमार बालकों का भाषा विकास इसलिए मन्द गति से होता है क्योंकि वे सीमित मात्रा में ही अपने मित्रों व साथियों के सम्पर्क में आ पाते हैं जिससे अनुकरण द्वारा सीखने का अवसर कम मिल पाता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक अस्वस्थता के कारण बालक अधिकांशतः शान्त रहता है और कम बोलता है। फलस्वरूप बोलने का अभ्यास कम होता है जिससे वह भाषा विकास में स्वस्थ बालकों की तुलना में पीछे रहता है।
2. शरीर रचना (Bodily Structure ) -बालक के स्वास्थ्य के साथ-साथ उसकी शरीर रचना भी इसके भाषा विकास को प्रभावित करती है। शरीर रचना से तात्पर्य स्वर-यंत्र, जीभ, तालू, दाँत आदि की बनावट से है क्योंकि ये अंग ही बोलने की क्रिया में सहायक होते हैं। यदि बालक का स्वरयन्त्र परिपक्व होता है, जीभ की माँसपेशियाँ क्रियाशील होती हैं, दाँतों की रचना सामान्य होती है तो ऐसे बालक जल्दी और स्पष्ट बोलते हैं किन्तु जिन बालकों के स्वरयन्त्र में कोई खराबी होती है वे देर से बोलते हैं और स्पष्ट भी नहीं बोल पाते हैं।
3. लिंग भेद (Sex Difference) -मनोवैज्ञानिकों के इस क्षेत्र में किये गये प्रयोगों में यह देखा गया है कि भाषा विकास लिंग भेद से प्रभावित होता है। इस क्षेत्र में मैकार्थी (McCarthy) ने अपने अध्ययनों के पश्चात् प्रमाणित किया कि समान आयु के बालक-बालिकाओं में बालिकाओं की भाषा जल्दी समझ में आ जाने योग्य होती है।
अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार भी लड़कियाँ लड़कों की तुलना में शीघ्र बोलना प्रारम्भ करती हैं, उनका शब्द-भण्डार भी लड़कों से अधिक होता है। बालिकाओं के उच्चारण में भी शुद्धता होती है जबकि बालकों में भाषा दोष अधिक पाये जाते हैं।
4. बुद्धि (Intelligence)—बुद्धि और भाषा विकास में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। इस सम्बन्ध में किये गये बुद्धि परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि जो बालक उत्कृष्ट बुद्धि के होते हैं वे जल्दी बोलना शुरू करते हैं। इसके विपरीत मन्द बुद्धि बालकों में बोलने की क्षमता देर से विकसित होती है। बुद्धिमान बालकों का शब्द-भण्डार विस्तृत, शब्द चयन उत्तम, शुद्ध उच्चारण और वाक्य रचना की अधिक क्षमता पायी जाती है।
5. सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति (Socio-Economic Status)—जिन परिवारों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उन परिवारों में बालकों का भाषा विकास अच्छा होता है। जो माता-पिता शिक्षित तथा अच्छी सामाजिक व आर्थिक स्थिति वाले होते हैं उनके बालकों का शब्द-भण्डार सुन्दर होता है तथा उच्चारण शुद्ध होता है। वे अपनी भाषा में गन्दे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि उनकी भाषा में कोई दोष आ भी जाता है तो शिक्षित माता-पिता उसके निराकरण का प्रयास शीघ्रता से करते हैं। इसके विपरीत अशिक्षित माता-पिता भाषा विकास को महत्व नहीं देते हैं। माँ बाप स्वयं भी गंदे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो अनुकरण से उनके बच्चे भी भ्रष्ट उच्चारण करने लगते हैं।
6. परिपक्वता (Maturation ) — जिस प्रकार क्रियात्मक विकास के लिए शारीरिक अंगों का परिपक्व होना आवश्यक है उसी प्रकार भाषा विकास के लिए फेफड़े, गला, जीभ, होंठ, दाँत, स्वर-यंत्र तथा मस्तिष्क के भाषा केन्द्र का पूर्ण परिपक्व होना आवश्यक है। जब तक ये सभी अंग परिपक्वता प्राप्त नहीं करते हैं तब तक बच्चों को चाहे किसी भी प्रकार का बोलने का प्रशिक्षण क्यों न दिया जाये उसका भाषा विकास नहीं हो सकता है। जैसे-जैसे ये अंग परिपक्वता प्राप्त करते जाते हैं उसी क्रम से भाषा विकास होता जाता है।
7. सीखना तथा अनुकरण (Learning and Imitation)—जब बालक के भाषा विकास सम्बन्धी अंग परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं तो बालक का भाषा विकास फिर वातावरण सम्बन्धी तत्वों के अधीन हो जाता है। ये वातावरण सम्बन्धी तत्व (i) सीखने के अवसर और (ii) अनुकरण की प्रवृत्ति है। स्नायुविक परिपक्वता तथा भाषा विकास सम्बन्धी अंगों में परिपक्वता आ जाने पर सीखने और अनुकरण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाते हैं तो बालक का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। जिन घरों में कई बालक होते हैं तो वहाँ छोटा बालक बड़ों का अनुकरण कर जल्दी बोलना सीखता है। इसी प्रकार यदि बालक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो वहाँ भी उसे वयस्कों से भाषा विकास के लिए पर्याप्त सीखने तथा अनुकरण करने का अवसर प्राप्त होता है। चूँकि बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास जन्म के 9-10 महीने पश्चात् से ही हो जाता है। अतः माता-पिता तथा अन्य वयस्क व्यक्तियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे बालकों के समक्ष भ्रष्ट भाषा का प्रयोग न करें।
8. प्रेरणा (Motivaiton) बालकों का बोलना सीखने में प्रेरणा का बड़ा महत्व होता है। प्रेरणा से बालक को प्रोत्साहन मिलता है। माता-पिता को चाहिए कि वह बालक की संकेतात्मक भाषा पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न करें बल्कि उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे बालक जब थोड़ा-थोड़ा उच्चारण प्रारम्भ कर दे तो जो शब्द वह उच्चारित करता है उसी से सम्बन्धित शब्दों के बारे में उससे प्रश्न करना चाहिए। जैसे-यदि वह पापा शब्द बोल लेता है तो पापा शब्द का ही उच्चारण और अधिक शुद्ध कराने के लिए उससे जा सकता हैं। बेटे के लिए खिलौना कौन लाया ? तो वह उत्तर स्वरूप संक्षिप्त शब्दों में कहेगा पापा। इसी प्रकार दूध की बोतल दिखाकर पूछा जा सकता है कि बेटा क्या पियेगा ? तो वह कहेगा दूध। इस प्रकार जब बालक बार-बार शब्दों को बोलने लगता है तो उसे स्वयं ही स्वः उच्चारित शब्दों को सुनकर आनन्द आने लगता है और फिर वह बार-बार उन शब्दों की पुनरावृत्ति करता है।
9. निर्देशन (Guidance)—भाषा विकास के लिए प्रेरणा के साथ-साथ निर्देशन की भी आवश्यकता होती है। भाषा विकास के लिए यह जरूरी है कि जो शब्द बोले जायें उनके मॉडल भी बच्चे के सामने प्रस्तुत किये जायें जिससे वह बोले गये शब्द की सही तस्वीर अपने मस्तिष्क में अंकित कर सके। जैसे यदि गुड़िया दिखाकर उसके सामने गुड़िया शब्द का उच्चारण किया जाता है तो धीरे-धीरे गुड़िया शब्द और उसकी आकृति बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है जिससे भविष्य में जब कभी वह गुड़िया देखता है तो स्वतः ही गुड़िया शब्द का उच्चारण करने लगता है अतः उचित निर्देशन से बालक जल्दी बोलना सीखता है।
10. पारिवारिक सम्बन्ध (Family Relationship) – बच्चे के पारिवारिक सम्बन्ध उसके विकास को प्रभावित करते हैं। जिन बच्चों के पारिवारिक सम्बन्ध अच्छे होते हैं वे बच्चे अच्छी प्रेरणा पाकर जल्दी बोलना सीख जाते हैं। बच्चे के भाषा विकास पर पारिवारिक सम्बन्धों के प्रभाव जानने के लिए कई बाल मनोवैज्ञानिकों जिनमें स्पिज, मैकार्थी, थॉमसन आदि का नाम प्रमुख है, ने अनाथालय के बालकों का अध्ययन किया क्योंकि यहाँ पारिवारिक सम्बन्धों का अभाव था। अध्ययन के पश्चात् उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक सम्पर्क से अलग रहने वाले बच्चे रोते अधिक हैं और बबलाते कम हैं। उनके मुँह से निकलने वाली ध्वनियों की संख्या भी कम होती है। अतः उनका भाषा विकास देर से होता है। इसके बीच जो बालक परिवार के साथ रहते हैं वे जल्दी तथा शुद्ध बोलना सीख जाते हैं।
कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिवार के सदस्यों की संख्या तथा आकार का प्रभाव भी भाषा विकास पर जानने के लिए अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि जिन परिवारों में अधिक बच्चे होते हैं या जहाँ संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ बालकों को अनुकरण के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं जिससे बालकों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है।
11. व्यक्तिगत विभिन्नतायें (Individual Differences) – वैज्ञानिकों के मतानुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव भाषा विकास पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो बालक बहिर्मुखी (extrovert) तथा उत्साही होते हैं उनमें भाषा विकास अन्तर्मुखी (introvet) तथा शान्त बालकों की तुलना में शीघ्रता से होता है।
12. कई भाषाओं का प्रयोग (Bilingualism)—जिन परिवारों में माता-पिता कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं वहाँ बालकों का भाषा विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है क्योंकि माता-पिता द्वारा बच्चे के सामने एक ही वस्तु के लिए दो अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दो अलग-अलग शब्दों को याद रखना बालक के लिए कठिन होता है जिससे उसके उच्चारण में भाषा सम्बन्धी दोष आ जाते हैं। अतः यदि परिवार में कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो बालक का भाषा विकास धीमी गति से होता है।
विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास
(LANGUAGE DEVELOPMENT IN DIFFRENT STAGES)
शैशवावस्था में भाषा विकास
(LANGUAGE DEVELOPMENT DURING INFANCY)
शिशु का प्रथम क्रन्दन उसकी भाषा विकास की शुरुआत होती है। इस समय उसे स्वर और व्यंजनों का ज्ञान नहीं होता है। लगभग चार माह तक शिशु जो ध्वनियाँ निकालता है उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। लगभग 10 माह की अवस्था शिशु एक शब्द का उच्चारण करता है और उसी शब्द की पुनरावृत्ति बार-बार करता है। लगभग 1 वर्ष तक शिशु की भाषा अस्पष्ट होती है केवल उसके माता-पिता ही अनुमान स्वरूप उसके शब्दोच्चारण का अर्थ निकाल सकते हैं। लगभग 12 वर्ष की आयु में उसकी कुछ-कुछ भाषा समझ में आने लगती है।
शैशवावस्था में बालक की वाक्य रचना केवल एक शब्द की होती है; जैसे दूध के लिए वह बू-बू शब्द का उच्चारण करता है। इसी प्रकार वे अन्य वस्तुओं के लिए भी एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं।
स्मिथ (Smith) ने शैशवावस्था के भाषा विकास क्रम को निम्न सारणी के अनुसार प्रस्तुत किया है-
आयु — ——– शब्द
जन्म से 8 माह —-0
10 माह —-1
1 वर्ष —- 3
1 वर्ष 3 माह —-19
1 वर्ष 6 माह —-22
1 वर्ष 9 माह —-118
2 वर्ष —-212 ARI
बाल मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शैशवावस्था में शिशु के भाषा विकास पर उसके परिवार की संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव पड़ता है । सभ्य और सुसंस्कृत परिवार के बच्चों की भाषा सुसंस्कृत और उच्चारण शुद्ध होता है।
वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि शैशवावस्था में लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की तुलना में शीघ्रता से होता है किन्तु जिन बालकों में गूंगापन, हकलाना, तुतलाना आदि भाषा दोष पाये जाते हैं उनका भाषा विकास धीमी गति से होता है।
बाल्यावस्था में भाषा विकास
(LANGUAGE DEVELOPMENT DURING CHILDHOOD)
जैसे-जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है वैसे-वैसे उसके स्वर-यन्त्र तथा स्नायुविक अंगों में परिपक्वता आती जाती है फलस्वरूप धीरे-धीरे उसका भाषा विकास तीव्र गति से होने लगता है। बाल्यावस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य निर्माण की क्रिया में दक्षता प्राप्त कर लेता है।
बाल मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बाल्यावस्था में भी बालिकाओं का भाषा विकास बालकों की तुलना में तीव्र गति से होता है तथा लड़कों की अपेक्षा उनके वाक्यों में शब्दों की संख्या अधिक होती है। इसके अतिरिक्त भाषा प्रस्तुतीकरण में भी बालिकायें बालकों से तेज होती हैं। प्रथम छः वर्षों तक यह गति तीव्र रहती है फिर मन्द हो जाती है।
बाल्यावस्था में भाषा विकास पर घर, विद्यालय, समूह के साथी, परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति तथा उचित निर्देश का प्रभाव पड़ता है।
सीशोर ने बाल्यावस्था के भाषा विकास को निम्न सारणी के माध्यम से स्पष्ट किया है।
सीशोर के अनुसार बाल्यावस्था में भाषा विकास
आयु वर्षों में —शब्द
4 वर्ष 5,600
5 वर्ष 9,600
6 वर्ष 14,700
7 वर्ष 21,200
8 वर्ष 26,300
10 वर्ष 34,300
बालकों के शब्द-भण्डार पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता बालक का वातावरण जितना विस्तृत होगा, शब्द-भण्डार उतना ही विस्तृत बनता है।
जैसेल के मतानुसार-चार वर्ष की आयु में लगभग पचास प्रतिशत बालक छोटे शब्दों; जैसे- कुर्सी, गुड़िया, पापा, पानी आदि शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में सही अर्थ में कर सकते हैं।
स्मिथ के अनुसार-पाँच-छ: वर्ष के बालक अपने वाक्यों में कभी-कभी एक शब्द भूल से छोड़ देते हैं, कभी-कभी क्रिया के प्रयोग में त्रुटि करते हैं किन्तु वे स्वयं ही उसे सुधारने का प्रयास करते हैं।
उत्तर बाल्यावस्था में भाषा विकास
(LANGUAGE DEVELOPMENT DURING LATE-CHILDHOOD)
जैसे-जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उसकी भाषा में गुणात्मक और परिमाणात्मक सुधार आता जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों के शब्द-भण्डार, वार्तालाप की सामग्री, बोले तथा लिखे गये वाक्यों की जटिलता व लम्बाई तथा भाषा की अभिव्यक्ति के ढंग में अन्तर आ जाता है। उत्तर बाल्यावस्था की भाषात्मक विशेषतायें निम्नलिखित हैं-
(1) शब्द-भण्डार-शब्द-भण्डार दो प्रकार का होता है-
(i) सामान्य शब्द-भण्डार,
(ii) विशिष्ट शब्द-भण्डार ।
सम्पूर्ण बाल्यावस्था में सामान्य शब्द-भण्डार का विकास तीव्रता से होता है क्योंकि बालक का स्कूल जाने के कारण सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। सामाजिक सम्पर्क व्यापक हो जाने के उसे अनेक नये शब्द सुनने व समझने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी उसके शब्द-भण्डार को विकसित करती हैं।
इस अवस्था में विशिष्ट शब्द-भण्डार भी विकसित होता है। शिष्टाचार सम्बन्धी, संख्यात्मक, कालसूचक शब्दों का विकास भी बड़ी तीव्रता से होता है
बालक इस अवस्था में क्रोध आने पर गाली के शब्दों का प्रयोग करते हैं और अत्यधिक प्रयोग के कारण वे उनकी दैनिक भाषा का अंग बन जाते हैं। यह शब्द वह परिवार, पड़ौस या समूह से सीखता है। बालिकायें गाली का प्रयोग कम करती हैं।
इस अवस्था में गुप्त भाषा का प्रयोग भी देखने को मिलता है। जिसे बालक अपने रहस्यों के आदान-प्रदान के लिए स्वयं ही विकसित कर लेता है। अपनी
गुप्त बातों को अपने मित्रों तक पहुँचाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में इसका प्रयोग अधिक देखा जाता है।
हरलॉक के अनुसार-इसका प्रयोग बालक केवल अपने घनिष्टतम मित्रों के लिए ही करता है।
गुप्त भाषा केवल लिखित या मौखिक ही नहीं होती है बल्कि, हावभाव, हाथ, उँगलियों व आँखों के माध्यम से भी गुप्त भाषा का प्रकटीकरण किया जाता है। बोलने में बालक गलत उच्चारण द्वारा भी गुप्त भाषा प्रकट करता है।
वाक्य तथा उच्चारण-
उत्तर बाल्यावस्था मे बालकों के वाक्य लम्बे व जटिल होते हैं। उनके वाक्य मिश्रित व संयुक्त प्रकार के होते हैं। वे एक ही वाक्य को कई प्रकार से लिख सकते हैं व बोल सकते हैं अर्थात् इस समय उनकी भाषा में अपने विचारों का भी समावेश हो जाता है। व्याकरण की दृष्टि से भी इस समय भाषा परिष्कृत हो जाती है। अब वह प्रश्नसूचक, आदेशात्मक, विस्मयबोधक तथा निषेधात्मक वाक्यों में अन्तर अच्छी तरह समझने लगता है।
भाषा सामग्री – बालकों की भाषा सामग्री दो प्रकार की होती है-
(i) स्वकेन्द्रित (Ego-cetric speech) तथा
(ii) समाज केन्द्रित (Socialized speech)।
छोटे बालकों की भाषा अधिकांशतः स्वकेन्द्रित होती है। वे अधिकांशतः अपनी वस्तुओं, रुचियों तथा परिवार की बातें करते हैं । किन्तु उत्तर बाल्यावस्था में जैसे-जैसे सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे उसकी बातें अन्य व्यक्तियों से सम्बन्धित होती जाती हैं। अतः इस अवस्था में उनकी भाषा स्वकेन्द्रित कम समाज केन्द्रित ज्यादा हो जाती है जिससे उनमें आलोचना की प्रवृत्ति का भी विकास होता है।
किशोरावस्था में भाषा विकास
(LANGUAGE DEVELOPMENT DURING ADOLESCENCE)
भाषा विकास की दृष्टि से भी किशोरावस्था अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समय वह अपने वयस्कों द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करता है। उसकी भाषा में सूक्ष्मता और बौद्धिकता की झलक मिलती है। इस समय उसकी भाषा का स्वरूप स्व-निर्धारित होता है। उसके शब्दों में भावों की गहनता तथा शब्दों की जटिलता होती है। उच्चारण में शुद्धता आ जाती है और व्याकरण का प्रयोग सन्तोषजनक होता है।
इसके अतिरिक्त किशोरावस्था में जो संवेगों की बहुलता होती है इससे भी भाषा विकास प्रभावित होता है। कल्पना शक्ति का बाहुल्य होने के कारण इसी अवस्था में वे कवि, कहानीकार, चित्रकार, नाटककार, अभिनेता, विचारक आदि बनने की सोचते हैं। जिसमें भिन्न-भिन्न रूपों में उनकी भाषा का परिष्कृत रूप प्रकट होता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने पर उनकी भाषा में सौन्दर्य माधुर्य झलकता है।
इस समय उनका शब्द-भण्डार विस्तृत हो जाता है। निश्चित भाषा-शैली का विकास होता है। भाषा में प्रौढ़ता होती है।
किशोरों का भाषा विकास उनके सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान करता है। किशोर चिन्तनशील तथा संवेदनशील प्राणी होता है। वह अपने चिन्तन व संवेगों को के बीच भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। भाषा के उचित प्रयोग से वह समूह अपना एक स्थान बना पाता है जिससे सामाजिक समायोजन में सहायता मिलती है।
Childhood and growing up Book pdf Download
Childhood and Growing Up Book pdf
Childhood and Growing Up Book pdf
| Childhood and Growing Up – B.Ed first Year Childhood and growing up के Book pdf दिया गया है |आप इसे download कर सकते है | |
Childhood and growing up Handwritten Notes
| Childhood and Growing Up – B.Ed first Year Childhood and growing up के यहा पर Handwritten Notes नोट्स दिया गया है |आप Childhood and growing up Handwritten Notes download कर सकते है | |
Childhood and growing up guide
| Childhood and Growing Up – B.Ed first Year Childhood and growing up के यहा पर Guide का pdf दिया गया | आप इसे Download कर सकते है | |
Childhood and growing up Ignou book pdf
| Childhood and Growing Up – B.Ed first Year Childhood and growing up के यहा पर Ignou book pdf दिया गया है | आप Childhood and growing up Ignou book pdf download कर सकते है | |
Childhood and growing up Assignment
| Childhood and Growing Up – B.Ed first Year Childhood and growing up के यहा पर Assignment दिया गया है | आप Childhood and growing up Assignment pdf download कर सकते है | |
| डी.एल.एड. बी.एड सम्बन्धी न्यूज नोट्स pdf के लिए ग्रुप एवं चैनल को ज्वाइन करे | |
| डी.एल.एड (व्हाट एप ग्रुप) |  |
| बी.एड (व्हाट एप ग्रुप) |  |
| टेलीग्राम (व्हाट एप ग्रुप) |  |
| CTET (व्हाट एप ग्रुप) |  |
| ALL IN ONE- व्हाट एप चैनल |  |
| Instagram Join |  |
- Childhood and growing up B.Ed 1st Year Full Marks ,
- Childhood and growing up B.Ed 1st Year Pass Marks ,
- Childhood and growing up B.Ed 1st Year Pratical marks ,
- Childhood and growing up B.Ed 1st Year book pdf download ,
- Childhood and growing up B.Ed 1st Year guide pdf download ,
- Childhood and growing up B.Ed 1st Year notes ,
- Childhood and growing up B.Ed 1st Year notes Hindi Medium ,
- Childhood and growing up B.Ed 1st Year English Medium ,
- Childhood and growing up assignment ,
- Childhood and growing up assignment in Hindi ,
- Childhood and growing up assignment in English ,
- Childhood and growing up B.Ed 1st Year notes in english ,
- Childhood and growing up B.Ed 1st Year notes in hindi ,
- Childhood and growing up assignment in Hindi pdf ,
- Childhood and growing up ignou notes ,
- Childhood and growing up ignou pdf ,
- Childhood and growing up book pdf free download ,
- Childhood and growing up assignment ,
- Childhood and growing up b.ed book pdf in english ,
- Childhood and growing up b.ed 1st year notes ,
- Childhood and growing up b.ed notes in hindi pdf ,