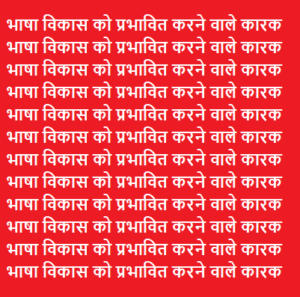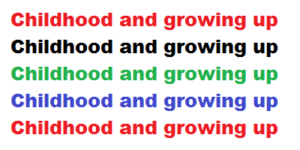भाषा विकास में बाधाएँ
(Hazards in Language Development)
भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें बालकों को दूसरे की बोली को समझना तथा साथ-ही-साथ ऐसे शब्दों में बोलना भी होता है कि दूसरे लोग उनकी बोली को समझ सकें। अतः, यह स्वाभाविक है कि इस जटिल प्रक्रिया के रास्ते में कुछ बाधाएँ
(hazards) उत्पन्न हो जाएँ। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि बालकों के भाषा विकास में कई तरह की बाधाएँ उत्पन्न होती हैं जिनसे उनका भाषा विकास काफी मंदित हो जाता है। इन बाधाओं में निम्नांकित प्रमुख हैं-
-
- (1) अत्यधिक रुदन (Excessive crying )
- (2) समझने में कठिनाइयाँ (Diefficulties in comprehension)
- (3) विलंबी वाक् (Delayed speech)
- (4) दोषपूर्ण वाक् (Defective speech)
- (5) वाक् विकार (Speech disorder)
- (i) तुतलाना (Hisping)
- (ii) अस्पष्ट उच्चारण करना (Slurring )
- (iii) हकलाना (Stuttering or stammering)
- (iv) क्षिप्रोच्चारण दोष या संकुल ध्वनि (Cluttering)
- (v) स्-स् करना (Hissings)
- (6) बातचीत करने में कठिनाई (Difficulties in conversing)
(1) अत्यधिक रुदन (Excessive crying ) –
जब कोई बालक अपनी उम्र के हिसाब से सामान्य से ज्यादा रोता है, तब इसे अत्यधिक रुदन की संज्ञा दी जाती है। जिन बालकों का रुदन अत्यधिक न होकर सामान्य
(normal) होता है, उनमें तो इस सामान्य रुदन से फायदा ही होता है; क्योंकि इससे उनकी मांसपेशियों (muscles) का व्यायाम (exercise) हो जाता है जो उनमें भूख जगाता है तथा गहरी नींद भी लाता है। लेकिन, यदि रुदन अधिक मात्रा में और अधिक समय तक होता है तो इससे बालकों में शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह की हानि होती है जो भाषा विकास को मंदित करता है। अत्यधिक रुदन से बालकों में शारीरिक शक्ति की कमी, पेट में गड़बड़ी, असंयत मूत्रता (enuresis or bed wetting) तथा मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। इतना ही नहीं, अत्यधिक रुदन करनेवाले बालकों के प्रति माता-पिता की मनोवृत्ति (attitude) ठीक नहीं रहती है और वे ऐसे बालकों का सामाजिक तिरस्कार (social rejection) करना प्रारंभ कर देते हैं। इन सबका परिणाम यह होता है कि बालकों में हीनता की भावना विकसित हो जाती है और उनमें सामाजिक निपुणता भी कम हो जाती है। फलतः, उनका भाषा विकास मंदित हो जाता है।
(2) समझने में कठिनाइयाँ
(Diefficulties in comprehension) —
भाषा विकास के लिए यह आवश्यक है कि बालक दूसरों की भाषा को ठीक ढंग से समझें। जो बालक दूसरों की भाषा को समझ नहीं पाते, उन्हें दूसरों से अलग-थलग रहना पड़ता है और इस तरह उनमें सामाजिक अकेलापन (social isolation) का गुण विकसित हो जाता है जिससे उनमें हीनता की भावना (feeling of inferiority) तथा अनुपयुक्तता की भावना (feeling of inadequacy) विकसित होती है जो बालकों के भाषा विकास को अवरुद्ध कर देती है। फ्रिडलैण्डर (Fridlander, 1970) के अनुसार जो बालक दूसरों की भाषा नहीं समझ पाते, उनमें सीमित शब्दावली (limited vocabulary) होती है तथा उनमें ध्यानपूर्वक दूसरों की आवाज न सुनने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है।
(3) विलंबी वाक् (Delayed speech) –
कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनका भाषा विकास अपनी उम्र के लिए बने मानक (norms) से काफी पीछे होता है। इस तरह के भाषा विकास को विलंबी भाषा विकास
(delayed speech development) कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने विलंबी भाषा विकास के कई कारण बताए हैं जिनमें बालकों में कम बुद्धि का होना, उनमें शब्दों तथा वाक्यों को सीखने की प्रेरणा में कमी तथा माता-पिता द्वारा शब्दों को सीखने के लिए उपयुक्त प्रेरणा (stimulation) आदि प्रधान बताए गए हैं। बुक तथा टुकर (Bruck & Tucker, 1974) के अनुसार विलंबित भाषा विकास से सिर्फ बालकों का व्यक्तिगत तथा सामाजिक अभियोजन (social adjustment) ही नहीं बल्कि शैक्षिक समायोजन (educational adjustment) भी बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। इससे बालकों में पढ़ने की क्षमता, शब्दों के हिज्जे (spelling) करने की क्षमता तथा उनका अर्थ याद रखने की क्षमता आदि काफी कम हो जाती है जो अपने-आपमें भाषा विकास के लिए एक प्रमुख समस्या बन जाती है।
(4) दोषपूर्ण वाक् (Defective speech) –
अयथार्थ वाक् (inaccurate speech) को दोषपूर्ण वाक् (defective speech) कहा जाता है। वाक् (speech) में दोष (defects) तीन तरह के हो सकते हैं- शब्दों के अर्थ में दोष (defects in word meanings), शब्दों के उच्चारण में दोष (defect in pronunciation) तथा वाक्यों की बनावट में दोष (defect in sentence structure)। शब्दों के अर्थ में दोष का कारण दो भिन्न अर्थवाले शब्दों का एक ही ढंग से बोला जाना होता है। जैसे पानी-पाणि तथा दिन-दीन ऐसे शब्द हैं जिन्हें लगभग एक ही ढंग से बोला तो जाता है परंतु इनके अर्थ भिन्न-भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों से बालकों को सही-सही संचार (communication) करने में दिक्कत होती है जिससे इनका भाषा विकास अवरुद्ध हो जाता है। शब्दों के उच्चारण (pronunciation) में दोष होने से भी भाषा विकास अवरुद्ध हो जाता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो 4 साल की उम्र के बाद भी उच्चारण में त्रुटियाँ करते हैं। हरलॉक (Hurlock, 1978) के अनुसार ऐसे बालक शैक्षिक अवसर (educational opportunities) का पूरा-पूरा फायदा नहीं उठा पाते और वे अक्सर अवरस्तर के उपलब्धक (underachiever) बन जाते हैं जिनसे उनका आगे का भाषा विकास और भी अवरुद्ध हो जाता है। वाक्यों की बनावट में व्याकरण-संबंधी त्रुटियों (grammatical errors) से बालकों का भाषा विकास अवरुद्ध हो जाता है। सामान्यतः 3 साल से अधिक उम्र के बालकों को भाषा के व्याकरण पर नियंत्रण बढ़ जाता है तथा त्रुटियाँ कम हो जाती हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि यदि ऐसी त्रुटियाँ बालकों में 5-6 साल या इससे अधिक उम्र होने पर होती है तो इससे बालकों के भाषा विकास पर बुरा असर पड़ता है।
(5) वाक् विकार (Speech disorder) –
शब्दों के उच्चारण में होनेवाले गंभीर दोष (serious defect) को वाक् विकार (speech disorder) कहा जाता है। वाक् विकार वैसे परिवार में अधिक पाया जाता है जिसमें माता या पिता या दोनों में ही तंत्रिकातापीय लक्षण (neurotic symptoms) होता है, जहाँ माता-पिता तथा बालकों का संबंध ठीक तथा घनिष्ठ नहीं होता है, जहाँ माँ अधिक प्रबल (dominant) तथा पिता अधिक दब्बू (submissive) होते हैं, जहाँ माँ बालकों पर ध्यान नहीं देती है या नहीं दे पाती है, जहाँ बालकों से माता-पिता काफी अधिक उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों ने वाक् विकार (speech disorder) को अपर्याप्त समायोजन का एक संलक्षण (syndrome of poor adjustment) माना है। ऐसे वाक् विकार (speech disorder) व्यक्ति की जिंदगी में कभी हो सकते हैं परंतु इस तरह का वाक् विकार प्राक् स्कूली अवस्था
(pre school age) में, जब बालक बोलना सीखते हैं, अधिक होता है। इस तरह के वाक् विकार (speech disorder) में अग्रांकित प्रमुख हैं-
(i) तुतलाना (Hisping) –
बोलने की प्रक्रिया में किसी शब्द के सही अक्षर का किसी दूसरे अक्षर द्वारा प्रतिस्थापन (substitution) को तुतलाना कहा जाता है। ऐसे तो प्रतिस्थापन का कोई नियम नहीं है परंतु अकसर ऐसा देखा गया है कि हिन्दी बोलने वाले बालक ‘ल’ अक्षर का प्रतिस्थापन ‘र’ से करते हैं। जैसे वह ‘लाल’ को अकसर ‘राल’ या ‘लार’ बोलता है। ऐसी तुतलाहट का कारण प्रायः बालकों में जबड़े (jaws), दाँत, होंठ आदि में कुछ विकृतियाँ हैं ।
(ii) अस्पष्ट उच्चारण करना (Slurring ) —
किसी शब्द का अस्पष्ट उच्चारण करना भी एक प्रकार का प्रमुख भाषा विकार (speech disorder) है। प्रायः जबड़ों, होंठ या जीभ का आंशिक रूप से कार्य करना या पूर्ण रूप से कार्य करने की असमर्थता के कारण बालक शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट ढंग से करते हैं। संवेगात्मक उत्तेजना (emotional stimulation) की स्थिति में भी बालक जल्दी-जल्दी बोलना प्रारंभ कर देते हैं और वे अकसर शब्दों का अस्पष्ट उच्चारण करते हैं।
(iii) हकलाना (Stuttering or stammering) –
हकलाना एक संकोचित (hesitant) तथा आवृत्तिपूर्ण (repetitious) बोली को कहा जाता है जो अकसर वाक् मांसपेशियों (speech muscles) के अंशत: एवं पूर्णतः असामंजस्य (incoordination) से उत्पन्न साँस लेने और छोड़ने में गड़बड़ी से पैदा होता है। इसमें बोलते समय एक शब्द को बालक रुक-रुककर उसे कई बार दुहराता है। हकलाना 21⁄2 से 32 वर्ष के बालकों में सामान्य रूप से देखा जाता है परंतु उम्र बढ़ने से यह अपने-आप समाप्त हो जाता है। परंतु, किसी-किसी बालक में हकलाने की क्रिया में उम्र बीतने के साथ कोई कमी नहीं दीखती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि हकलाना एक आनुवंशिक प्रक्रिया (hereditary process) है परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि हकलाने की प्रक्रिया उन बालकों में अधिक होती है जिनके माता-पिता द्वारा उन्हें अतिरक्षण (overprotection) मिलता है तथा माता-पिता स्वयं पूर्णतावाद (perfectionism) में विश्वास रखनेवाले होते हैं। माता-पिता के इस ढंग के व्यवहार के कारण ऐसे बालक अधिक चिंतित रहते हैं तथा दूसरों को गलत समझने की प्रवृत्ति रखनेवाले होते हैं।
(iv) क्षिप्रोच्चारण दोष या संकुल ध्वनि (Cluttering) –
वैसी बोली जो तीव्र (rapid), संभ्रांति (confused) तथा अव्यवस्थित (jumbled) होती है, उसे क्षिप्रोच्चारण दोष या संकुल ध्वनि कहा जाता है। यह दोष बहुत कुछ हकलाना (stuttering) से मिलता-जुलता है परंतु एक अर्थ में भिन्न है और वह यह है कि क्षिप्रोच्चारण दोष को बालक ध्यान देकर दूर कर सकता है लेकिन हकलाना को वह ध्यान देकर भी दूर नहीं कर सकता । क्षिप्रोच्चारण दोष से ग्रसित बालकों में कुछ क्रियात्मक व्यग्रता (motor awkwardness) तथा विलंबी भाषा विकास
(delayed speech development) के लक्षण भी पाए जाते हैं।
(v) स्-स् करना (Hissings) –
कुछ बालकों में ‘श’ या ‘स’ प्रत्येक शब्द के साथ जोड़कर बोलने की एक आदत-सी बन जाती है। ऐसे भाषा विकार (speech disorder) का मूल कारण गले से निकलती हुई वायु पर अनियंत्रण का होना होता है। सारासन (Sarason, 1979) के अनुसार यह भाषा विकार उन बालकों में अधिक पाया जाता है जिनमें संवेगात्मक तनाव अधिक होता है।
(6) बातचीत करने में कठिनाई (Difficulties in conversing) –
अधिकतर बालक बातचीत करने में दो तरह की कठिनाई महसूस करते हैं। पहली कठिनाई बातचीत की मात्रा (amount of talk) से संबंधित होती है और दूसरी कठिनाई, किस चीज के बारे में बातचीत की जाए (what to talk about) से संबंधित है। पहली कठिनाई से संबंधित दो तरह के बालक होते हैं— कुछ बालक बहुत अधिक बोलते हैं और कुछ बालक बहुत कम बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है। कि इन दोनों तरह के बालकों का सामाजिक एवं आत्मगत समायोजन (social and personal (adjustment) अपर्याप्त (inadequate) होता है जो स्वस्थ वाक्-विकास (healthy speech development) के लिए एक बाधा सिद्ध होता है। अधिक बोलनेवाले बालकों को लोग आत्मकेंद्रित (egocentric) समझते हैं तथा कम बोलने वाले बालकों को लोग मूर्ख (stupid) समझते हैं। बालकों के प्रति इस तरह की मनोवृत्ति (attitude) उनमें भाषा विकास (language development) के लिए हानिकारक होती है। वेलकोविज (Welkowitz, 1976) ने एक अध्ययन किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपनी उपलब्धियों (achievements), अभिरुचियों के बारे में अधिक बातचीत करते हैं और ऐसे होते हैं जो यौन (sex) तथा अपने माता-पिता के अवगुणों के बारे में अधिक बातचीत करते हैं। पहले तरह के बालकों को लोग घमंडी एवं आत्मकेंन्द्रित (egocentric) समझने लगते हैं और दूसरे तरह के बालकों के प्रति लोग सामाजिक तिरस्कार (social rejection) दिखाते हैं। इन दोनों तरह की भावनाएँ (feelings) बालकों में स्वस्थ भाषा विकास के मार्ग में बाधाएँ (hazards) उत्पन्न करती हैं।
इस तरह हम देखते हैं कि बालकों के भाषा विकास में बाधाएँ (hazards) कई कारणों से उत्पन्न हो जाती हैं। इन कारकों में वाक् विकार (speech disorder) की समस्या शिक्षा मनोवैज्ञानिकों को सबसे अधिक चुनौती देनेवाली समस्या है।
भाषा विकास में बाधाएँ |Hazards in Language Development |Bhasha Vikas Me Badhaye
भाषा विकास में बाधाएँ – Hazards in Language Development.