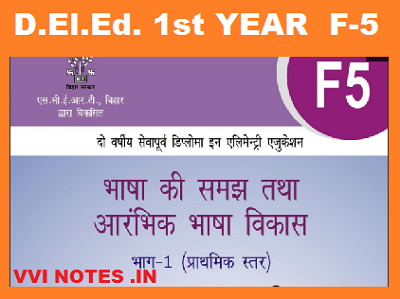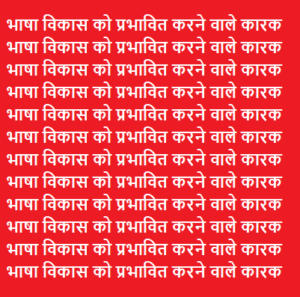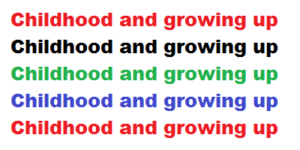भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास
Bhasha Ki Samajh Tatha Aarambhik Bhasha Vikas
Understanding Of Language And Early Language Development
| विषय | भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास |
| SUBJECT | Bhasha Ki Samajh Tatha Aarambhik Bhasha Vikas |
| SUBJECT | Understanding Of Language And Early Language Developmentn |
| Course | D.El.Ed. 1st YEAR |
| Paper Code | F-5 |
VVI NOTES के इस पेज में बिहार डी.एल.एड 1st ईयर पेपर F-5 भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास सिलेबस , भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास नोट्स ,भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास क्वेश्चन पेपर ,भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास क्वेश्चन बैंक ,भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास बुक पीडीऍफ़ ,भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास गाइड को शामिल किया गया है |
Bihar D.El.Ed 1st Year Paper F1 Bhasha Ki Samajh Tatha Aarambhik Bhasha Vikas Syllabus , Bhasha Ki Samajh Tatha Aarambhik Bhasha Vikas notes , Bhasha Ki Samajh Tatha Aarambhik Bhasha Vikas Question Paper ,Bhasha Ki Samajh Tatha Aarambhik Bhasha Vikas Book pdf Download
भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास सिलेबस
Bhasha Ki Samajh Tatha Aarambhik Bhasha Vikas syllabus
इकाई 1 : भाषा की प्रकृति
इकाई 2 : भाषायी विविधता वहुभाषिकता
इकाई 3 : बच्चों का आरम्भिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा
भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास का सिलेबस विस्तार से
इकाई 1 : भाषा की प्रकृति
* भाषा का अर्थ
* भाषा : प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के रूप में,
–समझ के माध्यम के रूप में,
–सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में।
* मानव भाषा और पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों की भाषा में अन्तर।
* भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था : ध्वनि संरचना, शब्द संरचना, वाक्य संरचना, प्रोक्ति (संवाद) संरचना।
* भाषा की विशेषताएँ।
इकाई 2 : भाषायी विविधता वहुभाषिकता
* भारत का बहुभाषिक परिदृश्य : भारत में भाषाएँ एवं भाषा-परिवार।
* बिहार का बहुभाषिक परिदृश्य।
* भाषा और बोली।
* बहुभाषिकता के आयाम : बौद्धिक आयाम, शिक्षणशस्त्रीय आयाम।
* भाषाओं के सन्दर्भ में संवैधानिक प्रावधान : अनुच्छेद 343-351, आठवीं अनुसूची।
* बहुभाषिक कक्ष और केस स्टडी।
इकाई 3 : बच्चों का आरम्भिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा
* बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता तथा बच्चों के भाषाई ज्ञान को समझना
-विद्यालय आने से पहले बच्चों की भाषायी पूँजी।
* बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? (स्किनर, चॉमस्की, वायगोत्सकी और पियाजे के विशेष सन्दर्भ में)।
* भाषा अर्जित करने और भाषा सीखने में अन्तर।
* विद्यालय में भाषा-विषय के रूप में माध्यम भाषा के रूप में।
* भाषा सीखने-सिखाने के उद्देश्यों की समझ : कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, संवेदनशीलता।
* भाषा के आधारभूत कौशलों-सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने का विकास। -शुरुआती पढ़ना-लिखना।
* लिपि और भाषा।
भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास नोट्स
Bhasha Ki Samajh Tatha Aarambhik Bhasha Vikas Notes
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. ‘सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में भाषा’ इस बिन्दु पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
उत्तर—
भाषा के उच्चरित रूप का व्यवहार हम अपनी बोलचाल में प्रतिदिन करते हैं। भाषा सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में विज्ञान ने भाषा के उच्चारित अथवा मौखिक रूप को कुछ स्थायित्व दिया है। नभ वाणी (Radio) तथा दूरदर्शन (Television) द्वारा हम दूर बैठे भी किसी की बात को सुन सकते हैं। सीतावाद्य (Gramophone) तथा ध्वनिलेय (Tape-recorder) के द्वारा हम मौखिक या उच्चारित भाषा को बहुत समय तक सुरक्षित रख सकते हैं |
प्रश्न 2. भाषा को प्रतीकात्मक या सांकेतिक साधन क्यों कहा जाता है?
उत्तर—
भाषा : एक सांकेतिक साधन है
भाषा को एक सांकेतिक साधन कहा गया है। जब तक भाषा की भिन्न-भिन्न ध्वनियों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भिन्न-भिन्न संकेतों को प्रयोग में लाते थे; जैसे—सिर को ऊपर-नीचे अथवा दायें-बायें हिलाना और नेत्रों को टेढ़े-तिरछे घुमाना । परन्तु केवल आंगिक संकेतों के सहारे हम अपने सभी विचारों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर सकते । इसलिए कालान्तर में भाषा का आविष्कार हुआ।
पहले हम जब अपने विचारों को प्रकट करना चाहते तो आंगिक संकेतों का प्रयोग करते थे; परन्तु बाद में भाषा के आविष्कार के पश्चात् भाषा के माध्यम के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होने लगी। भाषा भी एक प्रकार का संकेत ही है; परन्तु अन्तर केवल इतना ही है कि वह शारीरिक अथवा आंगिक संकेत न होकर, ध्वन्यात्मक संकेत है शारीरिक अथवा आंगिक संकेतों की कोई-न-कोई सीमा होती है, परन्तु ध्वन्यात्मक संकेतों की सीमा नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त आंगिक संकेतों के द्वारा कुछ गिने-चुने भावों का ही स्पष्टीकरण हो सकता है, जो मनुष्य को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य करते हैं। अपने परम्परागत विचारों की अमूल्य निधि को सुरक्षित रखने की बात तो दूर रही, हम अपने ही समय के लोगों के विचारों को इन शारीरिक संकेतों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते। परन्तु ध्वन्यात्मक संकेतों में वह क्षमता है कि अनन्तकाल तक, मानव के कोटि-कोटि मनोभावों को सुरक्षित रखते हुए, एक युग से दूसरे तक पहुँचाते रहें।
प्रश्न 3. रूपान्तर के आधार पर शब्दों के भेद बताइये।
उत्तर—
रूपान्तर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं-
(i) विकारी, (ii) अविकारी ।
जो शब्द लिंग, कारक तथा वचन आदि के प्रभाव से अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उन्हें ‘विकारी’ शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं- संज्ञा – सर्वनाम – विशेषण और क्रिया ।
जिन शब्दों पर लिंग, वचन तथा कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अविकारी’ शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं—–क्रिया-विशेषण, सम्बन्ध समुच्चबोधक तथा विस्मयादिबोधक |
प्रश्न 4. वाक्य विन्यास किसे कहते हैं?
उत्तर—वाक्य-विन्यास हमें यह बतलाता है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का परस्पर सम्बन्ध क्या है, वे एक-दूसरे पर कहाँ और किस सीमा तक आधारित हैं और वे किस क्रम में प्रयोग में लाए गए हैं। वाक्य-विन्यास के
तीन प्रधान तत्व हैं—
(i) अन्वय, (ii) अधिकार, (iii) क्रम ।
दो शब्दों में पारस्परिक वचन, कारक, लिंग, पुरुष और काल की समानता रहती है, वह ‘अन्वय’ कहलाती है । ‘अधिकार’ शब्दों का वह सम्बन्ध है जिससे किसे एक शब्दों की रचना, उनके अर्थ और सम्बन्ध के विचार से की जाती है, इसे ‘क्रम’ कहते हैं।
प्रश्न 5. वाक्य के अर्थ सम्बन्धी भेद बताइये ।
उत्तर—
अर्थ के आधार पर आठ प्रकार के वाक्य होते हैं-
(i) विधिवाचक वाक्य
(ii) निषेधवाचक वाक्य
(iii) आज्ञावाचक वाक्य
(iv) प्रश्नवाचक वाक्य
(v) विस्मयबोधक वाक्य
(vi) इच्छाबोधक वाक्य
(vii) सन्देहसूचक वाक्य
(viii) संकेतार्थक वाक्य ।
प्रश्न 6. हिन्दी भाषा में क्रिया के आधार पर वाक्य के कौन-कौनसे भेद किए जाते हैं? सोदाहरण वर्णन कीजिए।
उत्तर—
क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद
क्रिया के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए जा सकते हैं—
(क) कर्तृ-प्रधान,
(ख) कर्म-प्रधान और
(ग) भाव-प्रधान।
इन तीनों का संक्षिप्त वर्णन नीचे की पंक्तियों में किया जा रहा है।
(क) कर्तृ-प्रधान वाक्य
इन वाक्यों में कर्ता और कर्म अपने-अपने स्थान पर स्थित होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक कर्तृवाचक वाक्य में कर्म हो ही; यथा—
(i) भाई परमानन्द ने हिन्दू-संगठन पर भाषण दिया ।
(ii) रमण महर्षि सोते हैं।
(ख) कर्म प्रधान वाक्य
ऐसे वाक्यों में कर्म का होना नितान्त आवश्यक है। इन वाक्यों में क्रिया कर्म प्रधान होती है; यथा—
(i) स्वामी विवेकानन्द द्वारा अमरीका में हिन्दू धर्म की व्याख्या की गई।
(ii) रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्वामी विवेकानन्द को भगवान के दर्शन कराए गए।
(ग) भाव-प्रधान वाक्य
इस प्रकार के वाक्यों में स्वयं क्रिया ही प्रधान रहती है; यथा-
(i) पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं की हत्या का समाचार सुनकर मुझसे खाया नहीं गया।
(ii) विदा के समय उससे बोला नहीं गया।
प्रश्न 7. वाक्य के विभिन्न अंगों का सोदाहरण परिचय दीजिए ।
उत्तर-
वाक्य के अंग
वाक्य के प्रधान रूप से दो ही अंग होते हैं—
(क) ‘उद्देश्य’ और
(ख) ‘विधेय’।
इनकी संक्षिप्त व्याख्या आगे दी जा रही है—
(क) उद्देश्य
वाक्य में जिसके सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है, उसे वाक्य का ‘उद्देश्य’ कहते हैं;
यथा—
“स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की ।”
इस वाक्य में लेखक अथवा वक्ता ने जो कुछ भी कहा है या लिखा है, वह स्वामी श्रद्धानन्द के सम्बन्ध में है। इसलिए इस वाक्य में “स्वामी श्रद्धानन्द’ ही ‘उद्देश्य’ है।
(ख) विधेय
उद्देश्य के सम्बन्ध में जो कहा जाये, वह ‘विधेय’ कहलाता है। उपर्युक्त वाक्य में “गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की ”—यह विधेय है, क्योंकि यह कथन उद्देश्य (स्वामी श्रद्धानन्द) के सम्बन्ध में कहा गया है।
प्रश्न 8. स्वर और व्यञ्जन को स्पष्टतः परिभाषित कीजिए ।
उत्तर—
स्वर-जिन अक्षरों का उच्चारण फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर, कण्ठ से झंकारता हुआ तथा मुखावरोध से सर्वथा स्वतन्त्र है। प्रत्येक स्वर अन्य किसी स्वर या व्यंजन के स्पर्श या सम्पर्क के बिना स्वतन्त्र रूप से उच्चरित होता है। स्वर के अनेक अर्थों में एक अर्थ स्वतन्त्र भी होता है, स्वर कहते हैं।
व्यंजन- जो ध्वनियाँ पूर्ण रूप से व्यक्त होती हैं, उन्हें ‘व्यंजन’ कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वर के रूप में होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट ध्वनि के रूप में होता है। प्रत्येक उच्चारण स्वर और ध्वनि के रूप में अथवा स्वर और व्यंजन के रंग में रंगा होता है, इसलिए अक्षरों को ‘वर्ण’ भी कहते हैं।
प्रश्न 9. स्वर व व्यंजनों में कोई एक अन्तर बताइये।
उत्तर—
स्वर स्वतन्त्र अथवा स्वयं स्वरित होते हैं। लेकिन कोई भी व्यंजन किसी एक स्वर की सहायता के बिना व्यक्त नहीं होता है। व्यंजन के स्पष्ट उच्चारण के लिए व्यंजन के पीछे या पहले किसी एक स्वर की अपेक्षा होती है। मुखाकाश में वायु के संचरण मात्र के स्वरों का स्वरण होता है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए मुखाकाश में वायु और जिह्वा को परस्पर विविधतया घात, अज्ञघात, प्रत्याघात व्याघात करना पड़ता है।
प्रश्न 10. संध्याक्षर क्या है? व्याख्या कीजिए।
उत्तर—
स्वरों में संध्याक्षर—वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में ए, ऐ, ओ, औ को संध्याक्षर माना गया है। इनके उच्चारण भी एक के स्थान पर दो कहे गए हैं—जैसे—ए, ऐ का कण्ड-तालु तथा ओ, औ का कण्ठोष्ठ। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका उच्चारण दो स्वरों के समान होता रहा होगा। इसीलिए उन्हें संध्याक्षर कहते हैं । लेखक को अच्छी प्रकार याद है कि जब उसने वर्णमाला सीखी थी तो उसे ‘ए’, ‘औ’ उच्चारण क्रमशः ‘अई’, ‘अऊ ́ सिखाया गया था ‘ए’ तथा ‘ओ’ का विवरण ऊपर दिया जा चुका है, ‘ऐ’ तथा ‘औ’ को आगे दिया जा रहा है-
ऐ—यह ‘अ’ तथा ‘ए’ के संयोग से बना है। इसका उच्चारण भी शीघ्रतापूर्वक ‘अ’ से ‘ए’ पर आ जाता है।
औ—यह ‘अ’ तथा ‘ओ’ की सन्धि से बना है। इसका उच्चारण भी शीघ्रतापूर्वक ‘अ’ से ‘ओ’ पर आ जाता है।
प्रश्न 11. विराम चिह्न कौन-कौनसे हैं ? संक्षिप्त में बताइए।
उत्तर—
विराम चिह्न
‘विराम’ का अर्थ-
आराम, ठहरना, विश्राम आदि इसका शाब्दिक अर्थ है, अर्थात् जब हम बोलते हैं तो बोलते समय बीच-बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस प्रकार बोलते समय रुकना, ठहरने की क्रिया को ही ‘विराम’ कहते हैं। वाक्यों को लिखते समय इस ठहराव या विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ‘विराम चिह्न ́ कहते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि विराम चिह्न वाक्यों में लगाये जाने वाले वे चिह्न हैं जो ठीक-ठीक ठहराव के साथ वाक्यों को बोलने में सहायक होते हैं। उनके पदों, वाक्यांशों तथा खण्ड वाक्यों में परस्पर सम्बन्ध सूचित कर वाक्यों के अर्थ को भलीभाँति स्पष्ट करें। अतः विराम चिह्न लिपि के सशक्त अनुशासन का आध र है। कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में, “शब्दों तथा क्यों का परस्पर सम्बन्ध बताने वाले तथा किसी बात को भिन्न-भिन्न भागों में बाँटने और यथास्थान रुकने के लिए लेखन में जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिह्न कहते हैं।”
भाषा में विराम चिह्नों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता तथा वाक्यों के भाव समझने में सुविधा होती है। केवल विराम चिह्न ही वाक्यों को स्पष्टता प्रदान करने में सहायक होता है, विराम चिह्नों का प्रयोग भाषा को प्रवाहपूर्ण तथा सार्थक व्यंजन देता है।
हिन्दी भाषा में विराम चिह्न निम्न प्रकार के हैं-
(1) अल्प विराम (.)
(2) अर्द्ध विराम (;)
(3) पूर्ण विराम (1) अंग्रेजी में (.)
(4) प्रश्न चिह्न (?)
(5) विस्मयसूचक या आश्चर्य चिह्न या भावादिबोधक तथा सम्बोधन चिह्न ( ! )
(6) निर्देशक चिह्न (डेश) (-)
(7) कोष्ठक (), {},
(8) अवतरण चिह्न या उद्धरण चिह्न (‘ ‘), (‘ ‘)
(9) विवरण चिह्न (:-)
(10) अपूर्ण विराम कोलन [:]
(11) संक्षेप सूचक (.)
(12) योजक या संयोजक चिह्न (-)
प्रश्न 12. भाषा की संरचनात्मक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए ।
उत्तर—
संरचना या वाक्य-संरचना
मानक भाषा हिन्दी की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह संरचना या वाक्य रचना की दृष्टि से उत्तर भारत की पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, उड़िया, बिहारी, बंगाली आदि से साम्य रखती है इसलिए समान प्रकृति की इन भाषाओं में परस्पर अनुवाद – कार्य नितान्त सरल है। पारस्परिक बोधगम्यता की अनेक सम्भावनाएँ इस संरचना-साम्य में सर्वदा सुरक्षित हैं। जहाँ तक शब्दावली के साम्य की बात है, पूरे भारत की उत्तरी तथा दक्षिणी भाषाओं में लगभग साठ प्रतिशत शब्दावली तो संस्कृत की ही पाई जाती है। मलयालम में तो संस्कृत शब्दावली का प्रतिशत और भी अधिक है।
प्रश्न 13. शब्द – भण्डार किसे कहा जाता है ?
उत्तर-
शब्द-भण्डार –
शब्द-भण्डार की दृष्टि से भी मानक भाषा हिन्दी अत्यन्त सम्पन्न भाषा है। संस्कृत के विपुल शब्द-भण्डार के साथ ही इसमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी शब्दों तथा देशज शब्दावली की भी प्रचुरता है। अब यह प्रादेशिक भाषाओं की शब्दावली को आत्मसात् करके अपने शब्द-भण्डार में और भी वृद्धि कर रही है।
हिन्दी में ज्ञान-विज्ञान के अनेक पारिभाषिक शब्द-कोश प्रकाशित हो चुके हैं। अब मानक भाषा हिन्दी में मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजविज्ञान, भौतिकी आदि विषयों की
शिक्षा का माध्यम बनने की क्षमता है। अनेक विश्वविद्यालयों के अनेक विज्ञान-विभागों के अध्यापक अब हिन्दी में एम.एस-सी. तक अध्यापन करा रहे हैं। कुछ शोधक हिन्दी में विज्ञान विषयों पर शोध-प्रबन्ध भी लिखने लगे हैं।
प्रश्न 14. ध्वनि का अर्थ और ध्वनि संरचना को समझाइए। अथवा, ध्वनि संरचना को भाषिक संरचना का महत्त्वपूर्ण तथ्य कहा जाता है। स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-ध्वनि का अर्थ-
ध्वनि शब्द ध्वन् धातु में इण् (इ) प्रत्यय जुड़ने से बना है। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ है-आवाज करना। आज भाषा विज्ञान में ध्वनि के लिए ‘स्वन’ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि- “ध्वनि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है।” ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सामान्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को ‘वर्ण’ कहते हैं। इसके पुनः खण्ड (टुकड़े) नहीं हो सकते। उदाहरण के रूप में अ क् त् प् च् आदि ध्वनियाँ (लिखित रूप में वर्ण) हैं और इनके खण्ड नहीं हो सकते।
यों तो मानव अपने मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ध्वनि से हमारा अभिप्राय उच्चारण-अवयवों की सहायता से उत्पन्न की गई भाषिक ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनियाँ भाषा के शब्दों का निर्माण करती हैं। अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सार्थक ध्वनियों के प्रयोग से ही शब्दों का निर्माण होता है। अतः ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जा सकती है, जिसके खण्ड नहीं हो सकते। कुछ विद्वान ध्वनि तथा ध्वनि चिह्न दोनों के लिए वर्ण का प्रयोग करते हैं। अतः ध्वनियाँ मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों की प्रतीक हैं। ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण से शुद्ध लेखन प्रक्रिया सम्भव है।
ध्वनि संरचना मानक हिंदी की ध्वनि-संरचना मौलिक है। नासिक्य ध्वनि के बाद का व्यंजन जिस वर्ण का है, उसी का पंचम वर्ण नासिक्य ध्वनि के रूप में उस व्यंजन से संयुक्त किया जाता है, यथा-रङ्क दण्ड, दन्त, पम्पा आदि। अब प्रयत्न लाघव तथा टंकण, मुद्रण की सुविधा को ध्यान में रखकर अधिकतर नासिक्य ध्वनियों को अनुस्वार से ही अंकित करने का प्रचलन बढ़ रहा है। नासिक्य ध्वनियों की पूर्णता अपूर्णता को दर्शाने के लिए बिन्दु (.) के साथ चंद्र-बिन्दु ( ँ) की व्यवस्था है, यथा- हंस और हँसना । यह हिन्दी मानक भाषा की मौलिक विशेषता है।
ध्वनियों के संयुक्त रूपों के लेखन की संरचना के कारण उनका उच्चारण शुद्ध रूप में हो पाता है; यथा—केन्द्रित, साम्प्रदायिक, उच्चरित आदि ।
सभी स्वर मौखिक भी होते हैं और अनुनासिक भी; जैसे—पूछ- पूँछ ओकार- ओंकार, टकार टंकार। मानक हिन्दी में उच्चारण को शुद्ध रूप में सुरक्षित रखने की विरल क्षमता है। जैसा बोला जाता है, वैसा ही लिखा जाता है।
विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी हिन्दी में उनके मूल उच्चारण में लिखने के लिए नए लिपि चिह्नों की व्यवस्था की गई है; यथा-नॉलेज, फरेब, दिमाग आदि।
अन्य भाषाओं में या तो स्वर हैं या व्यंजन ध्वनियाँ हैं, किन्तु हिन्दी में अन्तस्थ वर्ण भी हैं, जो व्यंजनों में परिगणित हैं, किन्तु उच्चारण की दृष्टि से अर्द्ध स्वर हैं, क्योंकि ये स्वरों के योग से ही निर्मित हैं;
यथा इ + अ = य्, उ + अ = व ।
प्रश्न 15. वाक्य -विन्यास का महत्त्व बताइये।
उत्तर-
वाक्य-विन्यास का महत्त्व
वाक्य- विन्यास की दृष्टि से मानक भाषा हिन्दी में विशेष लचीलापन है। यही कारण है कि अंग्रेजी जैसी सर्वथा भिन्न प्रकृति की भाषा से भी हिन्दी में अनेक सफल अनुवाद किए गए हैं, जो मौलिक लेखन का आभास कराते हैं। हिन्दी की वाक्य-संरचना की नमनीयता के कारण ही विदेशी भाषाओं से हिन्दी में किए गए अनुवादों को आशातीत सफलता मिली है। इस दृष्टि से साहित्य अकादमी द्वारा कराए गए विविध विषयों के ग्रन्थों के अनुवाद हिन्दी वाक्य-विन्यास का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तथा हिन्दी भाषा की अभूतपूर्व क्षमता का बोध कराते हैं।
प्रश्न 16. भाषा एक समझ का माध्यम है। संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
उत्तर—
भाषा की एक विशेषता उसका समझ का गुण है। यद्यपि मूलतः भाषा सम्प्रेषण का माध्यम है, किन्तु व्यावहारिक रूप से यह समझ का सम्प्रेषण भी है। जब वक्ता मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति कर रहा होता है तब उसका प्रयोजन अपने मन्तव्य को श्रोता को समझाना होता है और श्रोता का प्रयोजन वक्ता के मन्तव्य को भली-भाँति एवं सटीक रूप में समझना होता है। यदि भाषा वक्ता के मन्तव्य को श्रोता को पूर्णतः समझने में सहायक होती है तो इसी में भाषा की सार्थकता होती है। इसीलिए भाषा को समझ के माध्यम के रूप में भी परिभाषित किया जाता है।
प्रश्न 17. प्रोक्ति या सम्वाद संरचना क्या है?
उत्तर—प्रोक्ति या सम्वाद भाषा का वह रूप है जिसके माध्यम से सम्प्रेषण का प्रयोजन पूर्ण होता है। वक्ता अपने भावों, विचारों, अनुभवों आदि को अभिव्यक्त करने के लिए सम्वादों की रचना करता है। ये सम्वाद सार्थक वाक्य या वाक्य समूह होते हैं जिनके माध्यम से सम्प्रेषण पूर्णता को प्राप्त होता है। श्रोता वक्ता के आशय को हृदयगम कर पाता है। एकांकी, नाटक आदि साहित्यिक विधाएँ प्रोक्ति या सम्वादों पर ही आधृत होती हैं।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
(Long Answer Type Questions)
प्रश्न 1. भाषा को अर्थ सहित परिभाषित कीजिए ।
उत्तर-
भाषा का अर्थ एवं परिभाषाएँ
भाषा शब्द की रचना संस्कृत के ‘भाषा’ शब्द से हुई, जिसका अर्थ है—’व्यक्तायां वांचि’ । धातु के अर्थ की दृष्टि से यदि भाषा की परिभाषा की जाये तो वह यह होगी— “विचारों, भावों तथा इच्छाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने वाले वर्णात्मक प्रतीकों की समष्टि को भाषा कहते हैं।” वागेन्द्रियजनित और अवागेन्द्रियजनित भेद में
(02) प्रश्न
(03) प्रश्न
भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास Book pdf
Bhasha Ki Samajh Tatha Aarambhik Bhasha Vikas Book pdf
भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास क्वेश्चन पेपर
Bhasha Ki Samajh Tatha Aarambhik Bhasha Vikas Question Paper
Understanding Of Language And Early Language Development
VVI NOTES के इस पेज में बिहार डी.एल.एड फर्स्ट ईयर पेपर -F-5 (Bihar D.El.Ed first year paper F-5) भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास से सम्बन्धित पिछले साल का प्रश्न |
BIHAR D.El.Ed WHAT AAP & TELIGRAM GROUP
Bhasha Ki Samajh Tatha Aarambhik Bhasha Vikas vvi question answer
भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर , (Short Answer Type Questions )