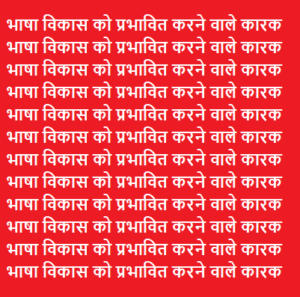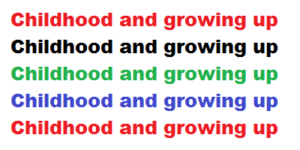बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ बताइए
| प्रश्न | बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ बताइए |
| विश्वविद्यालय नाम | महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय |
| सेमेस्टर | प्रथम -01 |
| संछिप्त जानकारी | इस पेज में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड के प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य के बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ बताइए उतर दिया गया है | |
| VVI NOTES.IN के इस पेज में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड के प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य सिलेबस , शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य प्रश्न -बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ बताइए। अथवा बौद्ध दर्शन के शैक्षिक अभिप्रायों का उल्लेख कीजिए तथा आधुनिक भारतीय शिक्षा हेतु उनकी सार्थकता का परीक्षण कीजिए। अथवा मूल्यों के शिक्षण के सन्दर्भ में बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ की विवेचना कीजिए। को शामील किया गया है | | |
प्रश्न 3 (i) बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ बताइए।
अथवा
बौद्ध दर्शन के शैक्षिक अभिप्रायों का उल्लेख कीजिए तथा आधुनिक भारतीय शिक्षा हेतु उनकी सार्थकता का परीक्षण कीजिए।
अथवा
मूल्यों के शिक्षण के सन्दर्भ में बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ की विवेचना कीजिए।
उत्तर –
बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ
महात्मा बुद्ध एवं उनके शिष्यों-अनुयायियों ने संसार के लोगों को दुःखों से मुक्ति का सन्देश, उपदेश, शिक्षा दी। जो भी शिक्षा दी उस पर मनन-चिन्तन किया तथा विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये। ये सिद्धान्त बौद्ध दर्शन के नाम से पुकारे गये। इन्हीं सिद्धान्तों को शिक्षा – ज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त करके तत्सम्बन्धी विचार निकर्ष निकाले गये जिन्हें बौद्ध शिक्षा दर्शन कहा गया। बौद्ध शिक्षा दर्शन प्रत्यक्षवादी कहा जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य मालुक्यपुत्र को कहा था कि सिद्धान्तों के विवेचन से दुःखी मानवता का दुःख दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि दुःखों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए, दुःख मुक्ति के मार्ग निकालना चाहिए। यही सिद्धान्त उपदेश रूप में बौद्ध दर्शन बने और उनका व्यावहारिक रूप बौद्ध शिक्षा दर्शन कहा जा सकता है।
बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ –
महात्मा बुद्ध ने अपने युवा जीवन में तीन दृश्य देखे- वृद्ध की दुर्दशा, मृत व्यक्ति के लिए विलाप, संन्यासी की स्थिति। इनसे प्रभावित होकर वह ‘सत्य ज्ञान’ की खोज में निकले। महात्मा बुद्ध का विचार था कि ‘मुझमें भी श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति और प्रज्ञा है, मैं स्वयं धर्म का साक्षात्कार कर सकता हूँ।’ यह आत्मबोध या आत्मज्ञान ही वास्तव में शिक्षा है, इसीलिए महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व कहा जाता है।
बोध से क्या तात्पर्य है? इस ओर भी देखना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन के चार आर्य सत्य बताये हैं-दुःख, दुःख समुदय, दुःख निरोध और दुःख निरोधगामी प्रतिपदा। इस संसार में दुःख ही दुःख है। समस्त संसार जब आग में जल रहा है तब उसमें आनन्द का अवसर कहा? अन्धकार (अज्ञान) से व्यक्ति देख नहीं पाता है (धम्मपद)। अतः अज्ञान और उससे प्राप्त दुःखों को दूर करने का मार्ग जानना ही बोध है अथवा शिक्षा है। अतः बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुःख है और शिक्षा इन दुःखों को दूर करने का मार्ग बताती है। शिक्षा दुःखों का ज्ञान है और दुःखों को दूर करने का अष्टांग प्रदान करती है। जब यह बोध या अनुभूति और प्रयत्न होता है तो वही शिक्षा हो जाती है। अतः शिक्षा व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में आर्य सत्य (ज्ञान) देने वाली और सद्मार्ग की ओर ले जाने वाली क्रिया है।
महात्मा बुद्ध ने ‘भग्गानं अट्ठांग को सेट्ठी’ अर्थात् अष्टांग मार्ग को सभी मार्गों में श्रेष्ठ कहा है। इस मार्ग पर चलने के लिए शील, समाधि और प्रज्ञा प्राप्त करना जरूरी है। शील पापों, अकर्मों, तृष्णाओं का निरोध हैं, समाधि कुशल चित्त की एकाग्रता और प्रज्ञा अविद्या का नाश है। सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि, समाधि में तथा सम्यक् दृष्टि और सम्यक् संकल्प प्रज्ञा में अन्तर्भूत पाये जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा अष्टांग मार्ग का अनुशीलन है जिससे व्यक्ति अर्हत्व की प्राप्ति करता है। अस्तु, शिक्षा अर्हत्व की प्राप्ति का साधन है, उसकी कठिन प्रक्रिया है।
आधुनिक भारतीय शिक्षा की सार्थकता
जिस अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन और अनुमोदन महात्मा बुद्ध ने किया है और जैसी शिक्षा उन्होंने दी उसके आधार पर हम शिक्षा के अग्रलिखित आठ कार्य भी निश्चित कर सकते हैं जो आगे दिये जा रहे हैं-
1. सम्यक् दृष्टि के आधार पर अविद्या, अज्ञान, मिथ्या दृष्टि दूर करना तथा वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को पहचानने की क्षमता प्रदान करना। इससे दुःख, दुःख का कारण, दुःख के परिणाम दूर होते हैं।
2. सम्यक् संकल्प के आधार पर राग-द्वेष- तृष्णारहित, अहिंसा, त्याग, दया से पूर्ण जीवन व्यतीत करने का निश्चय करना। इससे व्यक्ति में पवित्र जीवन का विचार दृढ़ होता है, अभ्यास होता है।
3. सम्यक् वाचा के अनुसार पर अप्रिय, मिथ्या, अशुभ, अप्रिय, असंयमित, निन्दनीय वाणी का प्रयोग न करना, जिससे दूसरों को दुःख या कष्ट हो। इसमें भाषा प्रयोग पर नियन्त्रण होता है।
4. सम्यक् कर्मान्त के आधार पर अहिंसा, अस्तेय, सत्य, संयम, शीलता, भद्रता जैसे गुणों का विकास करना जो तदनुकूल व्यवहार-कर्म के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। शुद्धाचरण के लिए यह आवश्यक कहा जाता है।
5. सम्यक् आजीव के आधार पर उचित साधनों एवं उपायों से जीविका प्राप्ति करना और अनुचित मार्ग, साधन एवं उपाय का अनुसरण न करके जीवन निर्वाह करना। इससे शुद्ध वृत्ति व अध्यवसाय के लिए प्राणी प्रयत्न करता है और धन के लोभ का संवरण करता है
6. सम्यक् व्यायाम के आधार पर सद् प्रयास या पुरुषार्थ का पालन करना, अकुशल धर्म का त्याग करना, कुशल धर्मों का उपार्जन करना, पुराने बुरे भाव-विचारों से दूर रखना, नये बुरे विचार- भाव न आने देना, मन में शुभ धारणा बनाये रखना।
7. सम्यक् स्मृति के आधार पर अच्छे उपदेशों, ज्ञान, धर्म को बार-बार स्मरण करना, जागरूक रहना और सावधान रहना जिससे निर्वाण प्राप्त होता है।
8. सम्यक् समाधि के आधार पर चित्त को एकाग्र करना तथा क्रोध, आलस्य, उद्धतता, पश्चाताप, सन्देश आदि से विगत होना, सांसारिक लोभ से अडिग रहना, दुःख-सुख में पूर्ण शान्त रहना ।
शिक्षा के ये कार्य व्यक्ति को पूर्ण शिक्षित-सभ्य बनाते हैं। इन गुणों से युक्त व्यक्ति मनसा, वाचा, कर्मणा से अनुशासित होता है। अनुशासित होने से ही व्यक्ति अपना सम्यक् विकास करने में समर्थ होता है। इस प्रकार शिक्षा का कार्य व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास बौद्ध दर्शन के अनुसार कहा जा सकता है।
बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य
बौद्ध शिक्षा का कार्य व्यक्ति का मनसा, वाचा, कर्मणा विकास करना कहा जा सकता है, अतएव शिक्षा के उद्देश्य भी तद्नुकूल निर्धारित किये जा सकते हैं जो निम्नलिखित कहे जा सकते हैं-
1. सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास-
बौद्ध शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य सम्यक् विकास कहा जा सकता है। व्यक्ति के तीन पक्ष हैं-संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। ये तीनों पक्ष सम्यक् दृष्टि, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि के अष्टांग मार्ग में मिलते हैं। इन मार्गों में वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों पक्ष शामिल पाये जाते हैं। ऐसी दशा में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य समन्वित एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। ज्ञान, भाव और क्रिया सभी का विकास बौद्ध शिक्षा का लक्ष्य है।
2. नैतिक एवं आचरणिक विकास–
बौद्ध धर्म एवं दर्शन दोनों में नैतिक एवं शुद्ध आचरण पर जोर दिया गया है। उचित कर्म नैतिकता की मुख्य कसौटी है जो व्यक्ति राष्ट्र या समुदाय के सम्बन्ध में सही है। सामाजिक कल्याण औचित्य के अभ्यास या उचित कर्म के अनुपालन पर ही निर्भर करता है। “बौद्ध धर्म-दर्शन के अनुसार उचित ज्ञान, उचित प्रयोजन और उचित वाणी के परिणामस्वरूप ही उचित कर्म या निष्काम कर्म होता है।” यह उपदेश स्वरूप बौद्ध शिक्षा है। अतः बौद्ध शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक एवं आचरणिक विकास करना कहा जाता है। बुद्ध मुख्यतया एक धार्मिक सुधारक तथा आचार के शिक्षक थे, इसलिए उनका ‘आचार मार्ग’ का सूत्र था-
सव्व पापस्य अकरणं कुसलस्य उपसम्पदा ।
सचित्तपरियोदपनं एतं बुननं सासनं । (धम्म पद 14/5 )
3. सांस्कृतिक विकास–
बौद्ध धर्म के प्रचार से भारतीय संस्कृति का भी प्रचार हुआ। योगी अरविन्द ने तो यहाँ तक कहा है कि संसार में भगवान बुद्ध के समान क्रियाशील पुरुष आज तक उत्पन्न नहीं हुआ है। तत्कालीन धर्म के क्रियाकाण्डों का उन्होंने खण्डन किया और नव धर्म शिक्षा को सामने रखा। पूजा-पाठ, यज्ञ-योग, जादू-टोना, पशुबलि आदि का विरोध किया गया जिससे इनके शुद्ध रूप बौद्ध धर्म के पतन के बाद पुनः शुरू किये गये। वेद, शास्त्र, उपनिषद् आदि की आलोचना ने जहाँ बौद्ध संस्कृति का विकास किया वहीं प्राचीन भारतीय संस्कृति (हिन्दू संस्कृति) का पुनरुत्थान भी किया। अब स्पष्ट है कि बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य सांस्कृतिक विकास भी था।
4. निर्वाण की प्राप्ति-
बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य है। निर्वाण की प्राप्ति । निर्वाण का तात्पर्य ‘अनन्त शान्ति’ है जिससे तृष्णा, काम, भोग, जरा-मरण के क्लेश-दुःख की शान्ति हो जाती है तथा अनन्त सुख-आनन्द की अनुभूति होती है। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा में सांख्य और वेदान्त की मुक्ति की धारणा का मेल पाया जाता है। “हीनयानी निर्वाण सांख्य की मुक्ति के समान है और महायानी निर्वाण वेदान्त की मुक्ति का प्रतीक है।” अतएव निर्वाण या दुःख का नाश और सुख की प्राप्ति बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य कहा जाता है।
5. सामाजिक विकास-
बौद्ध धर्म सामाजिक आचार-विचार की शिक्षा देता है। अतः बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य लोगों में सामाजिक योग्यता एवं कुशलता का विकास करना था। बौद्ध भिक्षु स्वयं समाज में जाकर दीक्षा देते थे, देश-विदेश में भ्रमण भी करते थे। इससे उनमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भावना का भी विकास होता था। बौद्ध शिक्षा इस प्रकार व्यापक परिप्रेक्ष्य में दी जाती थी और यह व्यापक दृष्टिकोण सामाजिक विकास के उद्देश्य से उत्पन्न होता था। ‘शील’ या उचित जीवन ‘आत्मगत विशुद्धता’ है और मुक्ति प्राप्ति के लिए आवश्यक गुण है जो व्यवसाय और कार्य के आदर्श सम्पादन करने वाले समाज के सदस्य में होता है। बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य इसीलिए सामाजिक भावना का विकास व्यापकतम परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है। सामाजिक विकास में जनतान्त्रिक जीवन एवं दृष्टिकोण का भी विकास अन्तर्निहित कहा जाता है।
प्रश्न 3 (i) बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ बताइए। अथवा बौद्ध दर्शन के शैक्षिक अभिप्रायों का उल्लेख कीजिए तथा आधुनिक भारतीय शिक्षा हेतु उनकी सार्थकता का परीक्षण कीजिए। अथवा मूल्यों के शिक्षण के सन्दर्भ में बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ की विवेचना कीजिए। को शामील किया गया है }