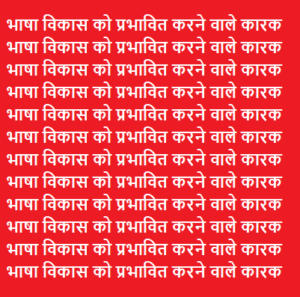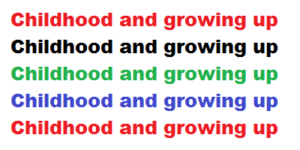असमानता का तात्पर्य क्या है?
प्रश्न – असमानता का तात्पर्य क्या है ? What does inequality mean?
उत्तर
प्रकृति में हम कई प्रकार की असमानता पाते हैं। अपने विश्व-देश-समाज में भी हमें विविध प्रकार की असमानता दृष्टिगोचर होती है। यह अपमानता आर्थिक तथा भौतिक सुख-सुविधाओं, शैक्षिक अर्हताओं, सामाजिक हितों और स्थितियों से भी संबंधित हो सकती हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति, वर्ग या समुदाय के सशक्तिकरण करने में एक-दूसरे को पुष्ट करती हैं। सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण या जन्मजात असमानताओं के कारण सामर्थ्यसूचक विशेषताओं या गुणों को नकारना ही असमानता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में जातिप्रथा और लिंग आधारित भेदभाव में विश्वास करने की परम्परा है। इसी तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों और सभी वर्गों की लड़कियों की शैक्षिक स्थिति तो वर्गों के बीच की खाई की कहानी ब्यान करती है।
ऊपर जिस खाई की चर्चा की गई है उसे पाटने या मजबूत बनाने में समाज की विचारधारा या उसकी अर्थव्यवस्था प्रमुख भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई समाज लोकतंत्र में विश्वास करता है और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को स्वीकार करता है तो वह समाज वर्णव्यवस्था और लिंग आधारित विभेद को पनपने नहीं देगा तथा कुछ ही हाथों में संपत्ति और सत्ता को संकेंद्रित नहीं होने देगा। यह निर्विवाद सत्य है कि समाज की जैसी विचारधारा होगी, वहाँ के सभी संस्थाओं (सरकार, परिवार, न्यास, संगठन समितियाँ आदि) का ढाँचा और स्तरण भी उसी के अनुरूप होगा। लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की विचारधारा होगी तो समाज में पाए जाने वाले कृत्रिम विभेद और वर्ग विशेष की सत्ता और सामर्थ्य के महल को उठाना उस समाज का लक्ष्य होगा। इस लक्ष्य के निर्धारित हो जाने के बाद समाज की उपर्युक्त सभी संस्थाएँ अपनी-अपनी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रक्रियाओं में सुधार कर अपने सुविधावंचित व्यक्तियों, वर्गों या समुदायों की स्थिति में सुधार करने के काम में जुट जाएँगी ताकि उनमें भी वे सभी अच्छे और सकारात्मक गुण विकसित हो सकें तथा अंततोगत्वा सभी को अवसरों की समानता वाला लक्ष्य प्राप्त हो सके। संक्षेप में, विचराधारा, संस्थाएँ और सामाजिक प्रक्रिया ही वे प्रमुख कारक हैं जो असमानता को बनाए रखने या उसमें सुधार कर धीरे-धीरे उसे पूरी तरह से मिटा देने की भूमिका निभाते हैं। हम अपने इन आयामों की सीमा शैक्षिक प्रक्रिया के चौखटें परिसीमित कर रहे हैं। परन्तु यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि शैक्षिक प्रक्रिया की विशेषताएँ आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों को भी प्रभावित करती हैं। इसका वास्तविक कारण यह है कि शिक्षा हमारी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए, यदि कोई बालक स्कूल नहीं जाता और यदि जाता भी है तो वही न्यूनतम अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं करता तो इसके पीछे आर्थिक कारण होते हैं। इससे उसकी भावी सामाजिक व्यवस्था और स्कूल का तात्कालिक वातावरण भी प्रभावित होता है। हो सकता है, गरीबी ही वह कारक हो जिसकी वजह से वह बच्चा स्कूल न जाकर अपने परिवार की परवरिश के काम में लगने के लिए मजबूर हुआ हो। इसी तरह, यदि कोई बालक न्यूनतम अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं कर पाता, तो सभी उस स्कूल पर दोष मढ़ने लगते हैं और इस तरह से स्कूल के वातावरण पर तत्काल बुरा प्रभाव पड़ने लग जाता है।
”
असमानता की संकल्पना ऐतिहासिक प्रकृति की है। ऐतिहासिक प्रतिमान देश और काल से सम्बद्ध होता है। हम इस बात के पर्याप्त उदाहरण दे चुके हैं कि किस प्रकार से ऐतिहासिक ताकतों ने हमारे समाज में असमानताओं की जड़ें मजबूत कीं। जब हम ‘असमानता’ के ऐतिहासिक प्रकारों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय दो प्रकार के उन कारकों में भेद करना होता है जो इस परिघटना के पीछे काम करते हैं। ये कारक हैं
1. वर्जित कारक
2. अंतर्जात कारक
1. वर्जित कारक
ये वे कारक हैं जो शिक्षा-व्यवस्था से बाहर वाले हैं जैसे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक कारक। इन कारकों से पूरी शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रसार की कोई प्रणाली विशेष सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित होती दिखाई पड़ती हैं।
2. अंतर्जात कारक—
ये वे कारक हैं जो शिक्षा-व्यवस्था में से ही उभर कर असमानता को जन्म देते हैं। हम ऐसे कुछ कारकों का उल्लेख कर चूके हैं। जैसे समाज में स्कूल- शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध न होना, या स्कूल शिक्षा का पूरा का पूरा व्यवस्थागत ढाँचा बिगड़ा होना जहाँ बच्चे की शिक्षा अरूचिकर, अनुपयोगी, निरर्थक लगने लगे, स्कूली शिक्षा का व्यवस्थागत ढाँचा कमजोर होगा तो इससे पलायनशीलता बढ़ेगी, अर्थात् बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाएँगे, नए बच्चे भर्ती ही न होंगे या जो पढ़ रहे होंगे, उनमें से भी कई बीच में ही पढ़ाई छोड़ बैठेंगे।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकारों को नकारने से असमानता जन्म लेती है। असमानता की यह संकल्पना देश और काल से जुड़ी होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी समाज विशेष में असमानता की जड़ें उस समाज के ऐतिहासिक विकास-क्रम में निहित होती हैं। असमानता के आयाम समाज की विचारधारा, विश्वास तथा शासन के अनुरूप हो सकते हैं। साम्यवाद, समाजवाद या पूँजीवाद आदि राजनैतिक विचारधाराएँ हैं। इन विचारधाराओं की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएँ समाज में असमानता को बढ़ाती, मिटाती या कम करती है। इस प्रकार हर समाज में पाई जानेवाली असमानताओं की जननी और धात्री उसकी विचारधारा प्रक्रिया और संस्थाएँ होती हैं। कार्य-कारण- संबंध-सूचक ये सारे कारक भी दो प्रकार के होते हैं—बर्हिजात कारक कहलाते हैं, जबकि अंतर्जात कारक व्यवस्था के अंदर से ही उभरते हैं। इसके सिवाय, असमानताएँ गुणात्मक भी हो सकती हैं और मात्रात्मक भी। गुणात्मक असमानताओं में सामाजिक बाधाएँ, कुपोषण, मार्गदर्शन का अभाव आदि सम्मिलित हैं तथा मात्रात्मक असमानताओं में निम्न आय, निम्न उपलब्धि स्तर आदि आते हैं।