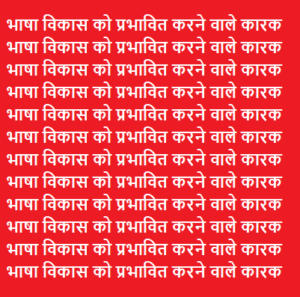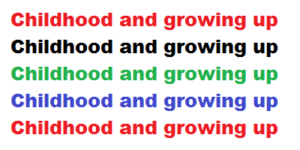मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषाएँ, क्षेत्र, विशेषताएँ, एवं उद्देश्य
Meaning Definitions Scope Characteristics and Aims of Evaluation
| Meaning of Evaluation, Definitions of Evaluation,Scope of Evaluation, Characteristicsof Evaluation, Aims of Evaluation, moolyaankan ke paribhaashaen , moolyaankan ke kshetr, moolyaankan ke visheshataen, moolyaankan ke evan, moolyaankan ke uddeshy, |
| VVI NOTES के इस पेज में मूल्यांकन के अर्थ ,मूल्यांकन के परिभाषाएँ ,मूल्यांकन के क्षेत्र ,मूल्यांकन के विशेषताएँ ,मूल्यांकन के उद्देश्य को शमिल किया गया है | |
मूल्यांकन का अर्थ Meaning of Evaluation
मूल्यांकन हमारे सामान्य शब्दकोश का एक सामान्य (Common) भाग बन चुका है। बिना मूल्यांकन के न तो किसी वस्तु, तथ्य या व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं और न वांछित सुधार। घर के छोटे-छोटे कार्यों से लेकर विद्यालय, समाज आदि के कार्यों में मूल्यांकन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाहित है। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए श्वांस की आवश्यकता होती है और श्वांस प्रक्रिया के सन्दर्भ में हमें अनुभव भी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार मूल्यांकन प्रक्रिया तो निरन्तर चलती रहती है, किन्तु उसका इतना सामान्यीकरण हो गया है कि हम उसका अनुमान नहीं लगा पाते कि कहाँ और कब मूल्यांकन प्रक्रिया सम्पादित की जा रही है। मात्र औपचारिकता में ही इसका अनुमान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित रेखाचित्र के माध्यम से शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन की संस्थिति को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। शाब्दिक विश्लेषण की दृष्टि से मूल्यांकन दो शब्दों का सम्मिलन है – प्रथम मूल्य द्वितीय अंकन। इस प्रकार मूल्य का अंकन करना ही मूल्यांकन है, अर्थात् मूल्यांकन में इस सत्य का निर्णय किया जाता है कि कौन-सी चीज अच्छी है और कौन-सी बुरी ? और अच्छी सत्य के क्या कारण हैं ? कहने का आशय यह है कि जब हम किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण दोषों के सन्दर्भ में उसका अवलोकन करते हैं, तो वहाँ मूल्यांकन निहित होता है। शिक्षा के क्षेत्र में मुल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। इसकी प्रक्रिया के अन्तर्गत न केवल छात्रों की विषय विशेष सम्बन्धी योग्यता की ही जानकारी प्राप्त होती है बल्कि यह भी जानने का प्रयत्न किया जाता है कि उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्त्व का विकास किस सीमा तक हुआ है ? साथ ही शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ आदि की सफलता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी मूल्यांकन प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। संक्षेप में मूल्यांकन एक निर्णयात्मक एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत विषय-वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय लिया जाता है, जो बुद्धिमत्तापूर्ण एवं परिपक्व होता है। उपर्युक्त के आधार पर मूल्यांकन के अर्थ को निम्नलिखित विश्लेषण द्वारा और अधिक सरलतम रूप से स्पष्ट किया जा सकता है- (1) मूल्यांकन = छात्रों का मात्रात्मक विवरण + मूल्य निर्णय (2) मूल्यांकन = छात्रों का गुणात्मक विवरण + मूल्य निर्णय ( 3 ) मूल्यांकन = मात्रात्मक विवरण + गुणात्मक विवरण + मूल्य निर्णय ।
मूल्यांकन के परिभाषाएँ
Definitions of Evaluation
विभिन्न विद्वानों द्वारा मूल्यांकन के सम्बन्ध में दी गयी परिभाषाएँ निम्नलिखित प्रकार है-
1. टारगर्सन तथा एडम्स के अनुसार –
” मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना । इस प्रकार शैक्षणिक मूल्यांकन से तात्पर्य है- शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की प्रक्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के विषय में निर्णय देना ।”
2. क्विलिन तथा हन्ना के अनुसार —
“छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किये गये परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना एवं उनकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है ।
3. जे. डब्ल्यू. राइटस्टोन के अनुसार –
” मूल्यांकन सापेक्षिक रूप से नवीन प्राविधिक पद है, जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परम्परागत जाँचों एवं परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में व्यक्त करने के लिये किया गया है । • मूल्यांकन में व्यक्तित्व सम्बन्धी परिवर्तन एवं शैक्षिक कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों पर बल दिया जाता है । इसमें केवल पाठय-वस्तु की निष्पत्ति ही निहित नहीं, वरन् वृत्तियों, रुचियों, आदर्शों, सोचने के ढंग, कार्य करने की आदतों तथा वैयक्तिक एवं सामाजिक अनुकूलन भी निहित है ।’
“Evaluation is a relatively new technical term introduced to designate a more comprehensive concept of measurement than applied in conventional tests and examinations…..The emphasis in measurement is upon single aspects of subject matter achievement or specific skills and abilities but……….. The emphasis in evaluation is upon broad personaltiy changes and major objectives of an educational. These include attitudes. interests, ideals way of thinking, work-habits and personal and social adaptability.”
– J. W. Wrightstone
4. के. पी. पाण्डेय के अनुसार –
” मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी तथा शिक्षा के अन्य सभी पक्षों की पारस्परिक निर्भरता तथा उनकी उपादेयता की जाँच होती है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थी की उपलब्धि के आधार पर केवल विद्यार्थी की ही जाँच नहीं होती, बल्कि शिक्षक, शिक्षण पद्धति, पाठ्य-पुस्तक तथा अन्य शैक्षणिक साधनों की उपयोगिता की जाँच भी होती है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में इन सभी का पारस्परिक योगदान मालूम किया जाता है और शिक्षण क्रिया को शिक्षार्थी की दृष्टि से और अधिक महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी बनाने की कोशिश की जाती है ।”
मूल्यांकन का क्षेत्र
Scope of Evaluation
मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । आर. एस. वर्मा के शब्दों में, “मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं । दूसरे शब्दों में, किसका मूल्यांकन किया जाय — प्रश्न का उत्तर ही मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारित करना है । मूल्यांकन द्वारा हम व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों (Dimension) का पता लगाते हैं । ये आयाम शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा नैतिक क्षेत्रों से सम्बन्धित हो सकते हैं ।” संक्षेप में मुल्यांकन का सम्बन्ध केवल छात्र की बौद्धिक उपलब्धि से न होकर उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व से हैं जैसा कि रेमर्स व गेज (Remmers & Gage) ने एक स्थान पर लिखा है, “मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का
मूल्यांकन के क्षेत्र के अन्तर्गत छात्र के व्यक्तित्व के निम्नलिखित प्रमुख पक्ष आते हैं-
- (1) ज्ञान (Knowledge),
- (2) बोध या अवबोध (Comprehension),
- (3) सूचना ( Information),
- (4) कुशलताएँ (Skills),
- (5) प्रवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ एवं मूल्य (Tendencies, Attitudes & Values),
- (6) छात्र की त्रुटियाँ (Mistakes of Student),
- ( 7 ) शारीरिक स्वास्थ्य (Physical Health ) ।
1. ज्ञान (Knowledge)
मूल्यांकन में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि छात्र ने विषय-वस्तु के सम्बन्ध में कितना ज्ञान अर्जित किया है
2. बोध या अवबोध-(Comprehension)
बोध से तात्पर्य है कि छात्र सीखी हुई सामग्री की कितनी प्रकार से व्याख्या करने की क्षमता रखता है |
3. सूचना-( Information)
छात्र ने ज्ञान के सम्बन्ध में कितनी सूचना का संकलन किया है 1
4. कुशलताएँ (Skills)
कुशलताओं का सम्बन्ध पाठ्य-विषय से सम्बन्धित कुशलताओं से है
5. प्रवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ एवं मूल्य (Tendencies, Attitudes & Values)
– यह देखना कि छात्र की अपने विषय में, अपने विद्यालय में क्या प्रवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ एवं मूल्य हैं ।
6. बुद्धि-
यह ज्ञात करना कि कुछ छात्र क्यों भूल करते हैं तथा त्रुटियों की क्यों पुनरावृत्ति करते हैं ?
7. योग्यताएँ –
छात्रों की योग्यताओं का ज्ञान करना । योग्यताएँ सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की होती हैं।
8. रुचियाँ—
इनका सम्बन्ध किसी वस्तु, विषय या क्रिया को पसन्द करने या न करने से है, अभिरुचि परीक्षणों का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है ।
9. छात्रों की त्रुटियाँ —
मूल्यांकन के द्वारा छात्र की इस बात की जाँच हो जाती है कि वह त्रुटियाँ क्यों कर रहा है । त्रुटियों का ज्ञान हो जाने पर उनके निराकरण के प्रयास किये जाते है ।
10. शारीरिक स्वास्थ्य –
शारीरिक स्वास्थ्य का मापन करना मूल्यांकन के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । इसके लिये ‘प्रश्नावली’, ‘स्वस्थ इतिहास’ तथा ‘निरीक्षण पद्धतियों’ का प्रयोग किया जाता है । वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य भी एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, जिसका मापन किये बिना कोई भी मूल्यांकन पद्धति अधूरी रह जायेगी ।
मूल्यांकन की विशेषताएँ
Characteristics of Evaluation
मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
- (1) मूल्यांकन एक व्यापक पद है जिसमें जाँच एवं मापन दोनों आ जाते हैं ।
(2) मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होता है । यह छात्र के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के सम्बन्ध में मूल्य का अंकन करता है ।
(3) मूल्यांकन के अन्तर्गत बालक के सभी पक्ष – शारीरिक, मानसिक, नैतिक आदि आ जाते हैं ।
(4) मूल्यांकन निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है ।
(5) मूल्यांकन, संख्यात्मक तथा वर्णनात्मक दोनों प्रकार का होता है ।
(6) क्विलिन तथा हन्ना (Quillen & Hanna) के अनुसार, “मूल्यांकन सम्पूर्ण शिक्षण एवं अधिगम का अभिन्न अंग है ।”
(7) मूल्यांकन का शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इस प्रकार यह सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली का अंग है।
(8) छात्र व्यवहार के परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिये मूल्यांकन में सामग्री एकत्र करने के समस्त साधन निहित रहते हैं ।
(9) मूल्यांकन का प्रमुख सम्बन्ध छात्र के विकास से है ।
(10) मूल्यांकन एक प्रकार से सहयोगी कार्य है, जिसमें छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है 1
(11) मूल्यांकन का स्वरूप सुधारात्मक होता है । यह छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का ही मापन नहीं करता ।
(12) मूल्यांकन परिणामों के आधार पर किसी छात्र के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्त्व के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है 1
(13) किस सीमा तक किसी उद्देश्य की प्राप्ति हुई है ? शिक्षण में जो उद्देश्य निश्चित किये जाते हैं, उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, इस बात का पता मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा चलता है ।
(14) कक्षा के अन्दर जो सीखने के अनुभव उत्पन्न किये गये, वे प्रभावशाली रहे या नहीं—इस तथ्य की जाँच मूल्यांकन के अन्तर्गत की जाती है।
मूल्यांकन के उद्देश्य
Aims of Evaluation
विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य बताये हैं-
(1) मापन के अनेक गम्भीर दोषों को दूर करना ।
(2) मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य “बालकों के बहुमुखी विकास को अधिकतम गतिशील बनाये रखना । ”
(3) यह जाँचना कि बालक ने रुचियों, समझदारी, वृत्तियों, कुशलताओं, गुणों आदि को किस सीमा तक ग्रहण कर लिया है ।
(4) पाठ्यक्रम में परिस्थिति और आवश्यकतानुसार संशोधन के आधार प्रस्तुत करना । (5) शिक्षण की उपयोगिता की जाँच करके उसे छात्रोपयोगी बनाना ।
(6) शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जाँच करना ।
(7) यह देखना कि विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य-पुस्तकें उपयुक्त हैं
( 8 ) अध्यापक की शिक्षण – कुशलता एवं सफलता की जाँच करना ।
(9) अध्यापक को शिक्षण विधियों के प्रभाव एवं परिणाम की जाँच के अवसर देना ।
(10) छात्रों की दुर्बलताओं एवं सद्गुणों को समझाने में सहायता देना ।
(11) छात्रों को उचित एवं व्यावसायिक निर्देशन देने में सहायता प्रदान करना । (12) शैक्षिक कार्यक्रम की जाँच करना ।
(13) छात्रों को अपनी समस्याओं को समझाने में सहायता देना ।
(14) जो छात्र सामान्य ढंग से प्रगति नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी कठिनाइयों को हल करने के लिये परामर्श देना ।
(15) छात्रों की विभिन्न व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना ।
( 16 ) छात्रों की प्रगति एवं वर्गीकरण के लिये आवश्यक आधार प्रस्तुत करना ।
(17) छात्रों को इस प्रकार के निर्देशन देना जो शैक्षिक, सामाजिक, व्यावसायिक एवं संवेगात्मक समस्याओं का निदान कर सकें।
@@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @ @@ @@@ @@ @@ @@ @ @@ @@ @@ @@@ @@ @@ @@@ @@ @@ @@ @@@ @@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
| Meaning of Evaluation, Definitions of Evaluation,Scope of Evaluation, Characteristicsof Evaluation, Aims of Evaluation, moolyaankan ke paribhaashaen , moolyaankan ke kshetr, moolyaankan ke visheshataen, moolyaankan ke evan, moolyaankan ke uddeshy, |
| VVI NOTES के इस पेज में मूल्यांकन के अर्थ ,मूल्यांकन के परिभाषाएँ ,मूल्यांकन के क्षेत्र ,मूल्यांकन के विशेषताएँ ,मूल्यांकन के उद्देश्य को शमिल किया गया है | आप इस टॉपिक से सम्बन्धित कोई भी प्रश्न निचे कमेंट क्र पूछ सकते है | |