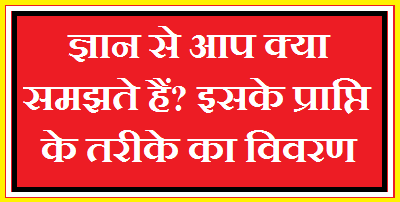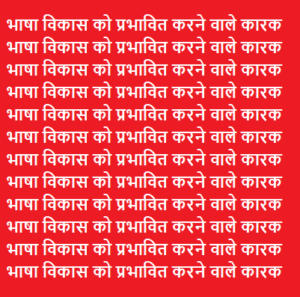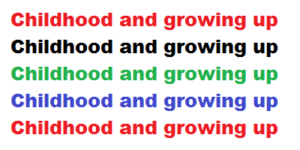ज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसके प्राप्ति के तरीके का विवरण दीजिए।
Gyaan se aap kya samajhate hain? Gyaan praapti ke tareeke
ज्ञान पद का अनुवाद ‘नालेज’ पद से किया जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार ‘ज्ञान’ का अर्थ समझने से पूर्व सत्य की वस्तुनिष्ठता, ज्ञान की सार्थकता, ज्ञान की सत्यता तथा तार्किक प्रतिज्ञप्ति सत्यता से लगाया जाता है।
इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-
- (i) ज्ञान की सत्यता हेतु उसकी वस्तुनिष्ठता का आंकलन किया जाना आवश्यक है।
- (ii) ज्ञान के अस्तित्व में कोई संशय नहीं होना चाहिए।
- (iii) ज्ञान की सत्यता की पुष्टि की सन्देहरहित होनी चाहिए।
- (iv) तार्किक प्रतिज्ञप्ति भी सत्य होनी चाहिए।
ज्ञान की अवधारणा स्पष्ट करते हुए यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या ज्ञान का स्वरूप परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है। यह प्रश्न भी जटिल है ज्ञान के सम्मिलित तथ्य, विचार प्रत्यय, नियम और निष्कर्ष आदि ज्ञान के श्रव्य हैं अर्थात् जब अध्यापक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है तो इन सभी तत्त्वों को बताता और समझाता है। अब जहाँ तक ज्ञान के तत्त्वों के बदलने या न बदलने का प्रश्न है तो इसमें सन्देह नहीं है कि ज्ञान के कुछ तत्त्व नहीं बदलते या इनके परिवर्तन की दर इतनी धीमी होती है कि उनका बदलाव महसूस नहीं होता। वहीं अनेक तथ्य, प्रत्यय व नियम ऐसे भी हैं जो लगभग नहीं बदलते। ज्ञान के यही तत्त्व शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। बहुत से जीवन मूल्य ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। शिक्षा छात्रों के मन में उनके प्रति आस्था उत्पन्न करती है और यह शिक्षा का दायित्व भी है। इसके विपरीत ज्ञान के कुछ तत्त्व परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक खोजों से भी ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, उसमें परिवर्तन आता है। उदाहरणार्थ पहले शिक्षक द्वारा छात्रों को यह ज्ञान दिया जाता था कि सूर्य प्रातःकाल पूर्व दिशा से चलना आरम्भ करता है और शाम को पश्चिम दिशा में अपनी यात्रा समाप्त करता है। परन्तु अब छात्रों को यह बताया जाता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। इस रूप में यदि देखा जाये तो पुरातन ज्ञान अज्ञान था। एक और उदाहरण द्वारा भी इसे समझा जा सकता है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठने पर हमें पेड़ चलते हुए प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तव में चलती स्थिति में तो रेलगाड़ी ही है। पृथ्वी की गति का ज्ञान हो जाने से भूगोल की शिक्षा में परिवर्तन आया। अतः शिक्षा को ज्ञान के तत्त्वों में आने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि रखनी होगी। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक ड्यूवी ने ज्ञान को अनुभव की सतत पुनर्रचना कहा है। विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी समय-समय पर कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। सत्य के अन्वेषण से जो नये नियम और सिद्धान्त प्रकाश में आते हैं, वे ज्ञान के स्थूल रूप में परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं।
ज्ञान की अवधारणा/संकल्पना
ज्ञान की अवधारणा के सन्दर्भ में एक तथ्य और है कि ज्ञान केवल अनुभूति मात्र नहीं है। अनुभूति मात्र बाह्य स्वरूप की होती है परन्तु जब वस्तु के बाह्य रूप को देखने के बाद हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो यह स्थिति संभवतः ज्ञान की कही जा सकती है। ऐसा ज्ञान प्राप्त होने की स्थिति को ही ज्ञान चक्षु का खुल जाना कहा जा सकता है। शिक्षा यदि हमारे ज्ञान चक्षु खोल दे तो वह अर्थात् हमारी शिक्षा का इस प्रकार भारतीय दर्शन के अनुसार चेतना को ही ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ज्ञान इन्द्रियों के अनुभव तक ही सीमित नहीं है, अपितु इन्द्रियों से प्राप्त अनुभूतियों द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसके लिए कर्म, ज्ञान व भक्ति में समन्वय आवश्यक है।
ज्ञान के स्रोत या तरीके
ज्ञान प्राप्ति के मूल रूप से निम्नलिखित पाँच प्रकार हैं–
- (a) इन्द्रिय अनुभव
- (b) साक्ष्य
- (c) तार्किक चिन्तन
- (d) अन्तः प्रज्ञा तथा अन्तः प्रज्ञावाद
- (e) सत्ता अधिकारिक ज्ञान
(a) इन्द्रिय अनुभव –
ज्ञान का एक प्रमुख साधन इन्द्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव का प्रत्यक्षीकरण है। मनुष्य की पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा उसे क्रमशः देखकर सुनकर, सूँघकर, स्वाद लेकर तथा स्पर्श करके सांसारिक वस्तुओं के बारे में तरह-तरह का ज्ञान प्रदान करती हैं। ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से मनुष्य ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही संसार की वस्तुओं के सम्पर्क में आता है तो एक प्रकार की संवेदना उत्पन्न होती है, यह सब देना ज्ञानेन्द्रियों को प्राप्त उत्तेजना में ही होती हैं तथा वस्तु का ज्ञान प्रदान करती है। इसे प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। यह प्रत्यक्षीकरण ही हमें उस वस्तु की जानकारी देता है।
(b) साक्ष्य –
जब हम दूसरों के अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तो इसे साक्ष्य कहा जाता है, साक्ष्य में व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता। वह दूसरों के निरीक्षण पर ही तथ्य का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार साक्ष्य दूसरों के अनुभव पर आधारित ज्ञान है। हम प्रायः अपने जीवन में साक्ष्य का बहुत उपयोग करते हैं। हमने स्वयं बहुत से स्थानों को नहीं देखा है किन्तु जब दूसरे उनका वर्णन करते हैं तो हम उन स्थानों के अस्तित्व में विश्वास करने लगते हैं।
(c) तार्किक चिन्तन–
तार्किक चिन्तन ऐसी मानसिक प्रक्रिया/योग्यता है जिसके बिना कोई भी ज्ञान सम्भव नहीं है। हमारा अधिकांश ज्ञान तर्क पर ही आधारित होता है। हमें अनुभव द्वारा जो संवेदनायें प्राप्त होती हैं उनको तर्क द्वारा संगठित करके ज्ञान का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार यह अनुभव पर काम करता है और हमें ज्ञान में परिवर्तन करता जाता है।
इन्द्रियों से प्राप्त अनुभवों के द्वारा हम-रंग, स्वाद तथा गन्ध आदि से सम्बन्धित कुछ संवेदनाएँ प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु जब वस्तुओं में भेद करने का प्रश्न आता है, वहाँ हमें तार्किकता की आवश्यकता होती है जिसमें अमूर्त चिन्तन निहित होता है। अतः ज्ञान का आधार तर्क बुद्धि ही है।
(d) अन्तः प्रज्ञा तथा अन्तः प्रज्ञावाद –
यह भी ज्ञान प्राप्ति का एक मुख्य स्रोत है। यह एक प्रकार का आन्तरिक बोध है जिसमें ज्ञान की स्पष्टता निहित होती है। अन्तः से हमारा तात्पर्य है किसी तथ्य को अपने मन में जानना। इसके लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इसके अन्तः अचानक ज्ञान के प्रकाश की किरण उत्पन्न होती है जिसे हम ज्ञान की संज्ञा देिते हैं। इस प्रकार के ज्ञान का एकमात्र प्रमाण यह है कि उसकी निश्चितता तथा वैधता में सन्देह नहीं होता तथा हम उस ज्ञान पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्तःप्रज्ञा हमारे अन्दर निहित वह सद्धत क्षमता है जो कभी अचानक ही क्रियाशील होकर हमें आलोकित करती है।
परन्तु इस अन्तःप्रज्ञा के साथ कभी-कभी आत्मनिष्ठता का ऐसा गुढ़ा आबद्ध हो जाता है कि यदि हम इस यथार्थ ज्ञान का साथ मान भी लें तो फिर इस ज्ञान में वस्तुनिष्ठता तथा सार्वजनिकता जैसी चीज नहीं रह जायेगी और हम यह दावा नहीं कर सकेंगे कि कौन-सी प्रतिज्ञप्ति सत्य है और कौन-सी असत्य है।
(e) सत्ता अधिकारिक ज्ञान–
उच्च शिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान को सत्ता अधिकारिक ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। मनोविज्ञान ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि मानव समाज में व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं। कुछ मनुष्य अत्यन्त प्रतिभाशाली हैं, जिनकी संख्या कम होती है, वे ही ज्ञान क्षेत्र में नई बातें जोड़ते हैं। इनके द्वारा दिया गया ज्ञान आर्ष या प्रति ज्ञान कहलाता है। शिक्षा का समस्त पाठ्यक्रम इन महान व्यक्तियों द्वारा जीवन के अनुभवों का भार है। अतः इन महान् व्यक्तियों को सत्ता माना जाना चाहिए। परन्तु इस तथ्य में एक कमी है कि इनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान के प्रति हमें इतना भी अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए कि हमारा ज्ञान संकीर्ण हो जाये व उस ज्ञान से हमारे विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाये।
***** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** ***
(सम्बन्धित प्रश्न )
- ज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसके प्राप्ति के तरीके
- ज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसके प्राप्ति के तरीके का विवरण दीजिए
- gyaan se aap kya samajhate hain? gyaan praapti ke tareeke
- What do you understand by knowledge? ways of acquiring knowledge