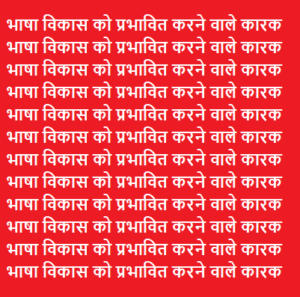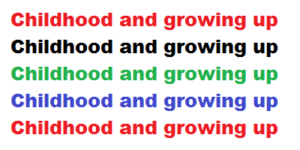S-9A TO S-9I DElEd 2nd Year Pedagogy Of All Subject Notes , Book , Guide pdf
इस पेज में बिहार डी.एल.एड सेकेण्ड ईयर पेपर S9-a , s9-b ,s9-c , s9-d , s9-e , s9-f , s9-g , s9-h , s9-i तक सभी पेपर के नोट्स , बुक ,गाइड पीडीएफ ( Pedagogy Of all subject Notes , Book , Guide pdf ) दिया गया है |
VVI NOTES .IN के इस पेज में FULL Marks , PASS MARKS , PRACTICAL MARKS की भी जानकारी दी गयी है , जिनसे विद्यार्थी को BIHAR D.El.Ed 2nd YEAR PAPER S9-a , s9-b ,s9-c , s9-d , s9-e , s9-f , s9-g , s9-h , s9-i Pedagogy Of all subject के बारे में सभी जानकारी हो जायेगी |
| Topic in Hindi | डी.एल.एड. सेकेण्ड ईयर S9 -A से S9 – i सभी विषय के नोट्स , बुक ,गाइड पीडीएफ |
| Topic in English | BIHAR D.El.Ed 2nd YEAR PAPER S9-a , s9-b ,s9-c , s9-d , s9-e , s9-f , s9-g , s9-h , s9-i Pedagogy Of all subject |
| Course | Bihar D.El.Ed. |
| Paper Code | S9-a , s9-b ,s9-c , s9-d , s9-e , s9-f , s9-g , s9-h , s9-i |
| Paper Name hindi | डी.एल.एड. सेकेण्ड ईयर S9 -A से S9 – i सभी विषय के नोट्स , बुक ,गाइड पीडीएफ |
| Paper Name Math | Pedagogy Of all subject Notes , Book , Guide pdf |
| Credit | 02 ( Pedagogy Of all subject ) |
| FULL MARKS | 50 ( Pedagogy Of all subject ) |
| Theory | 35 ( Pedagogy Of all subject ) |
| Hnternal | 15 ( Pedagogy Of all subject ) |
| PASS MARKS | 45% ( थ्योरी एवं प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग 45 % मार्क्स आना चाहिए )
( Pedagogy Of all subject ) |
| डी.एल.एड. सम्बन्धी न्यूज नोट्स pdf के लिए ग्रुप को ज्वाइन करे | |
| व्हाट एप ग्रुप |  |
| टेलीग्राम लिंक |  |
S-9a Pedagogy Of all subject scert Notes , Book , Guide pdf Download
S-9a Pedagogy Of Hindi Notes
S-9 हिंदी का शिक्षण शास्त्र नोट्स
Q. 1. भाषा विज्ञान के स्वरूप पर प्रकाश डालें।
अथवा, भाषा विज्ञान क्या है? भाषा विज्ञान कला है अथवा विज्ञान?
उत्तर : भाषा-विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा-विज्ञान, भाषा के स्वरूप, अर्थ और सन्दर्भ का विश्लेषण करता है। भाषा के दस्तावेजीकरण और विवेचन का सबसे प्राचीन कार्य 6ठी (छठी) शताब्दी के महान भारतीय वैयाकरण पाणिनी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘अष्टाध्यायी’ में किया है।
भारतीय मनीषियों ने शब्द को ब्रह्म की श्रेणी प्रदान कर भाषा की महत्ता को रेखांकित किया था। भाषा-विज्ञान के अध्येता भाषाविज्ञानी कहलाते हैं। भाषा-विज्ञान, व्याकरण से भिन्न है।
भाषा के व्यापक एवं संकुचित रूप में उसके स्वरूपों को समझने या निर्धारित करते समय हमें पक्षियों के कलरव से लेकर सर्पों की फुफकार, जानवरों की हुंकार, गार्ड की झण्डी, गूंगों के इशारों तक की ओर भी दृष्टिगोचर करनी पड़ती है। साथ ही वाणी के संकीर्ण स्वरूप का भाषा विज्ञान के अन्तर्गत अध्ययन करना पड़ता है। किन्तु दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु अन्य प्राणियों की बोली का परित्याग कर केवल मानव की भाषा तक ही सीमित रहना पड़ता है। इसमें भी अन्य उपांगों द्वारा निःस्त व्यवहारों का तिरस्कार कर केवल वाणी को ही अवलम्बन मानते हैं और सगर्व उसका ही अध्ययन करते हैं। नन्हें शैशवों की या भिखारी के मौन हाथों अथवा गूंगे को इंगित भाषा की भाषा विज्ञान में वैज्ञानिक अययन की कोई जरूरत नहीं, इसके अतिरिक्त वाणी से अभिव्यक्त सम्पूर्ण ध्वनियों का भी वैज्ञानिक अध्ययन में कोई महत्व नहीं, न हमें अट्टहास से जरूरत है और न क्रन्दन से, न घोड़े के संचालकों की टकाटक शब्द या किसी की आपत्ति में सहानुभूति और दयार्द्रचित्त चच-चच शब्द से, न गाड़ी की पें पें, न भेड़ों की में-में, या मेढ़कों की भंक-भैक से प्रयोजन है।”
यहाँ तो हमें मतलब है मनुष्य की वाणी द्वारा प्रयुक्त ऐसी ध्वनियों से जो अध्ययन के द्वारा विश्लेषण में आ जाय और जिनके इधर-उधर के हेरा-फेरी उलट पलट से कोई सार्थक शब्द का निर्माण हो सके। हमें तो प्रयोजन है ऐसी ध्वनियों से जिनके द्वारा एक मानव अन्य मानव पर अपने विचार को प्रकट कर सके जो सार्थक हो, मनुष्य द्वारा उच्चरित हो और जिससे दूसरा मानव भी अर्थ को ग्रहण कर सके। इस परिप्रेक्ष्य में हमें भाषा शब्द पर ही चिंतन करने के लिए विवश होना पड़ता है।
भाषा शब्द बहुत ही विस्तृत है। इसका विकास संस्कृत की ‘भाष्’ धातु से हुआ है जिसका प्रयोग व्यक्ति वांचि अर्थात् वाणी के लिए किया जाता है। इसमें पशु-पक्षियों की बोली से लेकर प्रकाण्ड पण्डितों तक की भाषा भी समाहित हो जाती है। लेकिन मनुष्य जिस भाषा का प्रयोग अपने बोलने अथवा विचार-विनिमय के लिए करता है वह अन्य प्राणियों की भाषा से इतर है। अतः हमें कहना पड़ता है कि विचार-विनिमय और भावाभियक्ति के सम्पूर्ण साधन भाषा के क्षेत्र में आते है। अतः भाषा विज्ञान के अन्तर्गत हम जिस भाषा का अध्ययन करते हैं उसका क्षेत्र बहुत ही संकुचित है। इसमें उसी सार्थक ध्वनि समूह को स्थान दिया जाता है जिसका अर्थ विश्लेषित हो सके।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः उसे हमेशा विचार-विनिमय की जरूरत पड़ती है। इस कार्य को वह अनेक प्रकार से सम्पन्न करता है। वास्तव में भाषा का रूप और भी सीमित हो जाता है। संसार के समस्त भाषा शास्त्रियों ने भाषा के विभिन्न शास्त्रीय अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। इनमें भारतीय और पाश्चात्य, प्राचीन और आधुनिक सभी वर्गों के विद्वान आते हैं। भाषा की परिभाषा को आबद्ध करने का अनादि काल से ही प्रयास होता चला आया है। यहाँ हम सर्वप्रथम पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पर ही विचार करेंगे।
प्लेटो के अनुसार- ‘विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, किन्तु जब वही ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं।
“वान्द्रिय महोदय ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि भाषा एक तरह का चिह्न से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनकी सहायता से मानव अपना विचार प्रदर्शित करता है। ये प्रतीक नेत्र ग्राह्य, श्रोत्र ग्राह्य या स्पर्श ग्राह्य इत्यादि अनेक प्रकार के होते हैं। और वास्तव में श्रोत्रग्राह्य प्रतीक भाषा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है । ”
भाषा विज्ञान की परिभाषा देते हुए स्रुतेवाँ के शब्दों में- “A Language is a system of arbitrary Voc. I Symbols by means of which members of a social group co-operate and interact.”
ए० ए० कार्डीनर के अनुसार — “विचाराभिव्यक्ति के लिये व्यक्त ध्वनि संकेत ही भाषा है।” भाषा की यथावत रूप से परिभाषा में देते हुए विश्वकोष (एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका) मे लिखा है कि Language may be defined as an arbitrary system of vocal symbols by means of which human beings, as members of a social group and participants in culture ineract and communicate.”
सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक जेस्पर्सन ने इस प्रकार भाषा विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है- ‘मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। मानव-मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरन्तर प्रयोग करता है। इस तरह के कार्य-कलाप को भाषा कहते हैं।”
हेनरी स्वीट के अनुसार Language is expression of humam thought by means of speech, sounds or articulate sounds.”.
महान दार्शनिक प्लेटो के कथनानुसार- “विचार और भाषा में बहुत थोड़ा ही अन्तर है, विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, परन्तु वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। (साफिस्ट)
मोरिया ए० पाइ तथा फ्रेंकग्यानोर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘डिक्शनरी ऑव लिंग्विस्टिक्स’ में भाषा की परिभाषा देते हुए इस प्रकार लिखा है-” भाषा उस सार्थक और विश्लेषण समर्थ मानवोच्चारित ध्वनियों को कहते हैं, जिनका प्रयोग मानव विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए करता है। ”
ब्लॉस और ट्रेगर के कथनानुसार – “भाषा ऐच्छिक वाक् प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग करता है। ”
उपरोक्त पाश्चात्य भाषाविदों के अतिरिक्त भारतीय मनीषियों ने भी भाषा – विज्ञान की परिभाषा अलग-अलग ढंग से दी है जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं— डॉ० श्याम सुन्दर दास के कथनानुसार – ” भाषा-विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट और उसके ह्रास की व्याख्या करता है।” भाषा-विज्ञान नामक अपनी कृति में वे इस तरह लिखते हैं-” भाषा-विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा शास्त्र के भिन्न-भिन्न अंगों ओर स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है—–सारांश यह है कि भाषा-विज्ञान की सहायता से हम किसी भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन, अध्ययन और अनुशीलन करना सीखते हैं। भाषा विज्ञान में ही एक अन्य जगह वे इस तरह स्पष्ट करते हैं- “मनुष्य-मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि-संकेतों का जो व्यवहार होता, उसे भाषा कहते हैं। ”
इस तरह उपरोक्त परिभाषाओं से भाषा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है और पूर्णतः सिद्ध होता है कि भाषा मनुष्य के सामाजिक व्यवहार साधन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि “भाषा-विज्ञान भाषा के अध्ययनार्थ एक गत्यात्मक विज्ञान है, जिसका विकासात्मक पल्लवन देश-काल के परिवेश में होता है। ”
भाषा – विज्ञान विज्ञान है या कला अथवा भाषा-विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों है।
कुछ लोग कहते हैं कि भाषा विज्ञान है क्योंकि उसमें विशिष्ट ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान का अर्थ ही है विशिष्ट या व्यवस्थित ज्ञान। अतः भाषा-विज्ञान, विज्ञान है क्योंकि इसमें विज्ञान की तरह ही निष्कर्ष ग्रहण के लिए वर्णन किया जाता है। इसमें स्थायी परिणामों या सिद्धांतों के संदर्भ में भौतिक एवं गणित की तरह परीक्षण भी संभव है। इसमें विज्ञान की तरह की उपचार पूर्णता, अतः संगति और लाघव इत्यादि भी होते हैं। अतः यह विज्ञान है।
कुछ अन्य विज्ञानों के अनुसार भाषा विज्ञान कला है क्योंकि इसमें सिद्धांत की अपेक्षा कल्पना को ही अधिक महत्व दिया जाता है, जिस प्रकार से दर्शनशास्त्र और राजनीतिशास्त्र में। अतः यह विज्ञान नहीं बल्कि कला है। भाषा को हम सिद्धांत रूप में तब तक प्रतिष्ठित नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसे कल्पना, अनुमान और तर्क से परिमण्डित नहीं किया जाय। दूसरी बात यह कि कला की भांति भाषा भी किसी क्षेत्र विशेष के अन्दर घिरी हुई नहीं है, जिस तरह विज्ञान का क्षेत्र होता है। अतः भाषा विज्ञान भी एक कला है। इस प्रकार विद्वानों के अपने-अपने विचार हैं। लेकिन कुछ अन्य लोग भी इस मत के हैं कि यह कला और विज्ञान दोनों है। क्योंकि इसमें कला की तरह कल्पना और विज्ञान की भाँति सिद्धांत दोनों ही समुपलब्ध होते हैं। भाषा समाज की सम्पत्ति है और कला मानवों द्वारा उद्धृत है। आधुनिक युग में अध्ययन के क्षेत्र को तीन वर्गों में बाँटा जाता है—
1. प्राकृतिक विज्ञान
2. सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र इत्यादि
3. मानविकी – चित्रकला और साहित्य-संगीत इत्यादि ।
इस प्रकार उपरोक्त आधारों के मुताबिक हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भाषा विज्ञान में दोनों का ही सामंजस्य एवं पूर्णता है। अतः भाषा-विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का ही वास्तविक आकार धारण करने वाला एक सशक्त आधार स्तम्भ है।
भाषा के बिना मानव सभ्यता और संस्कृति की प्रगति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वस्तुतः भाषा के सोपान पर ही मानव जाति की समस्त उपलब्धियाँ समाहित हैं।
Q. 2. भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप पर प्रकाश डालें।
Ans.
प्रत्येक भाषा का अपना स्वरूप होता है। जिस तरह हर संस्कृति व समाज का भाषा पर प्रभाव पड़ता है उसी तरह भाषा भी विकास व परिवर्तन के कालों से गुजरती रहती है। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है, जिसके स्वभाव को जानने से शिक्षण कार्य में आसानी होती है। भाषा के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए डॉ० बाबूराम सक्सेना का कथन है कि ‘जिन ध्वनि चिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनियमय करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं।” इस परिभाषा के आधार पर भाषा का निर्माण ध्वनियों से होता है। चाहे है। वह हिन्दी भाषा हो या अन्य कोई भाषा हो। ध्वनियों का अस्तित्व सभी में समाया हुआ सामान्य रूप से ध्वनि हवा तथा अन्य संबद्ध अणुओं में कंपन्न रूप में होती है लेकिन भाषा में प्रयुक्त ध्वनि वह लघुतम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व है। ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे क्, च्, अ, उ आदि ध्वनियाँ हैं। एक भाषा में ध्वनि का उच्चारण, उच्चारण स्थलों का ज्ञान, ध्वनियों का वर्गीकरण आदि विषय वर्ण-विचार में विवेचित किया जाता है। ध्वनियों के संयोग से ऐसे ध्वनि-समूहों की रचना की जाती है, जिनका कोई अर्थ होता है और ऐसी सार्थक ध्वनि या ध्वनि-समूह को शब्द कहलाते हैं। भाषा का शब्द-भंडार, शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण तथा शब्दार्थ का विश्लेषण शब्द-विचार के अंतर्गत किया जाता है। शब्दों से पदों का निर्माण एवं उनका वाक्य में प्रयोग, पद-निर्माण के विविध रूपों एवं नियमों आदि का अध्ययन पद-विचार में किया जाता है। भाषा को लिखने के लिए एक लिपि निर्धारित होती है। वह लिपि निर्धारित ध्वनियों का सार्थक समूह-शब्द के संयोग से लिखा वाक्य रूप नियमों के अंतर्गत धारण कर भाषा रूप में ढल जाती है। वही भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप कहलाता है। शब्द-विचार, वर्ण-विचार और वाक्य-विचार की दृष्टि से हिन्दी भाषा वैज्ञानिक है।
1. शब्द-विचार की दृष्टि से भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप : शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वाक्य में उसके अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं। उस स्थिति में शब्द को एक वैयाकरणिक रूप मिल जाता है और वह शब्द वाक्य निर्माण की दृष्टि से यथास्थान पर रखा जाता है। यदि उस शब्द को व्याकरण या वाक्य-रचना के नियम से दूसर स्थान पर रख दिया जाये तो उस शब्द का महत्व अपन आप में नगण्य हो जाता है। शब्द को ही पद कहा जाता है, क्योंकि वाक्य में वह विविध रूप धारण कर लेता है। शब्द व लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के कारण बदल जाते हैं, उन्हें विकारी कहते हैं और जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें अविकारी कहते हैं। इसके साथ ही भाषा अपना मूल रूप बनाये रखकर अन्य भाषाओं के शब्दों को अपने आगोश में समेट कर उन शब्दों से समृद्ध और विकसित होती है तो वह वैज्ञानिक ही मानी जा सकती है। भाषा में मूल तत्सम शब्दों के अलावा तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, अंत:करणात्मक शब्दों के ग्रहण द्वारा उसका विकास सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप होता है जो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस दृष्टि से यदि हिन्दी भाषा को देखा जाये तो हिन्दी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों का प्रयोग सामाजिक आवश्यकता के आधार पर सहज रूप में होता है। अतः हिन्दी भाषा का स्वरूप वैज्ञानिक है।
2. वर्ण-विचार की दृष्टि से भाषा का वैज्ञानिक रूप : ध्वनि, वर्ण और अक्षर भिन्न-भिन्न अवधारणाएँ हैं। हिन्दी भाषा या अन्य किसी भाषा में ध्वनियाँ अपने चिह्नित रूप में विद्यमान हैं। उन ध्वनियों या वर्णों का अपना अलग-अलग रूप है। उनका उच्चारण भी मुँह के अलग-अलग अवयवों के सहयोग से किया जाता है। निर्धारित ध्वनियों को स्वर और व्यंजन दो रूपों में देखा जाता है। भाषा को सीखने के लिए उसकी ध्वनियों तथा उनके लिपि चिह्नों को सरलता, शुद्धता से उच्चारित करना तथा उनका पढ़ना व लिखना आवश्यक होता है। यदि किसी भाषा की वर्णमाला सभी निर्धारित ध्वनियों को शुद्धता से प्रकट कर सकती है और उसकी लिपि सही ध्वनियों के लिखने में व उच्चारण में सहायक सिद्ध हो सकती है तो वह भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप की दृष्टि से उचित मानी जायेगी।
3. वाक्य-विचार की दृष्टि से भाषा का वैज्ञानिक रूप : व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना वाक्य है। वाक्य में अर्थवान् शब्दों को इस क्रम में रखा जाता है कि उससे पूरे विचार या भाव का ग्रहण हो जाता है। वाक्य -विचार में शब्दक्रम, उनका पारस्परिक संबंध, वाक्य के अंग, उनके भेद, वाक्य विश्लेषण आदि का विवेचन वाक्य नियमों के अंतर्गत होता है। यह भाषा का वैज्ञानिक रूप है। वाक्य में प्रयुक्त पद निश्चित लिपि में लिखे होने के कारण सरलता से पहचान लिये जाते हैं। हिन्दी भाषा की लिपि ‘देवनागरी’ है। इस लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हिन्दी जिस रूप में जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। हिन्दी या अन्य भाषा की रचना संबंधी कुछ निर्धारित नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के अंतर्गत भाषा की रचना और संचालन होता है, जो एक दृष्टि से भाषा की वैज्ञानिकता का द्योतक है।
इस संबंध में रमन बिहारीलाल का कथन है कि “प्रत्येक भाषा में रचना के कुछ नियम होते हैं। कुछ भाषायें तो ऐसी हैं जिनमें वाक्य-रचना के बड़े कठोर नियम है और कुछ भाषायें ऐसी हैं जिनमें वाक्य-रचना के पदक्रम में थोड़ा अंतर किया जा सकता है। हिन्दी दूसरे प्रकार की भाषा है। हिन्दी में वाक्य-रचना में पदों के क्रम एवं विभक्तियों के प्रयोग आदि के कोई कठोर नियम तो नहीं हैं लेकिन व्याकरण-सम्मत भाषा की वाक्य-रचना के कुछ सामान्य नियम हैं। ”
• उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि ‘वर्ण विचार’, ‘शब्द-विचार’, ‘वाक्य-विचार’ भाषा के वैज्ञानिक रूप हैं, क्योंकि इनकी संरचना, उच्चारण व लेखन निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही होता है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि हिन्दी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है।
Q. 3. भाषा के कार्यों का वर्णन करें।
Ans. भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राण है। भाषा का आविष्कार एवं विकास वस्तुतः मनुष्य का विकास है। मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भाषा के कार्यों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है-
1. अभिव्यक्ति (Expression) :
भाषा मनुष्यों के संवेगों, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। मनुष्य के मन में संवेग, भाव एवं विचार बाह्यजगत के साथ अंतःक्रिया करने पर अपने आप स्फुरित और व्यक्त होते रहते हैं। आत्माभिव्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही मनुष्य को भाषा सीखने के लिए उत्प्रेरित करती है। नवजात शिशु अपने मस्तिष्क में ध्वनि इकाइयों का संग्रह करता रहता है, जिनके सहारे वह नई शब्दावली सीखता और जोड़ता है। ये इकाइयां उच्चारण तथा अर्थ बोध संबंधी होती हैं, जो मस्तिष्क के स्नायु कोषों में अंकित हो जाती हैं। शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि के साथ-साथ इन इकाइयों में भी निरंतर वृद्धि होती चली जाती है और बालक को अपने संवेगों, भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की शक्ति प्राप्त होती है।
संवेगात्मक अभिव्यक्ति (Emotional Expression) :
संवेगात्मक अभिव्यक्ति का महत्व समझने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि संवेग क्या होते हैं और भाषा इनके विकास और नियंत्रण में कैसे सहायक होती है। सभी बालक जन्म से कुछ मूल्य प्रवृत्तियाँ लेकर आते हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों के फलस्वरूप वे बाह्य परिस्थितियों की वस्तुओं के साथ एक निश्चित संवेग धारण कर लेते हैं। जैसे कोई चीज न मिलने पर रोना, चिल्लाना। इसी प्रकार, जब बालक आनन्द का अनुभव करता है तब वह अपने अनुभवों को किसी के साथ बांटना चाहता है।
क्रोध बालक के व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक बाधक है। पर इसी संवेग को भाषा में वीर रस की कविताओं के माध्यम से देश के शत्रुओं के प्रति क्रोध में परिवर्तित किया जा सकता है। बुराइयों को समाप्त करने में भी उसकी इस प्रवृत्ति को लगा सकते हैं। अध्यापक विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा अपने संवेगों पर नियंत्रण पाने में बालक की सहायता कर सकता है। विविध बाल प्रतियोगिताओं के द्वारा ईर्ष्या को स्पर्धा में परिवर्तित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों को विविध परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके भी आप उचित दिशा में उनका संवेगात्मक विकास कर सकते हैं। शिक्षार्थियों को ऐसे वीरों की कहानियाँ भी सुनायी जा सकती हैं, जिन्होंने संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त करके यश प्राप्त किया।
संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए ‘रेचन’ नाम की प्रविधि सबसे सफल मानी गयी है। रेचन का तात्पर्य यह है कि बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान किये जायें कि वे अपने संवेगों की अभिव्यक्ति कर सकें। यही कल्पना के पंख लगाकर कहानियों का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार संवेगों को भाषा द्वारा एक खास दिशा दिखाई जा सकती है। जब बालक को स्वस्थ संवेगात्मक अनुभूति होती है तभी ऐसे भावों का जन्म होता है, जो साहित्य, कला, संगीत आदि विषयों में रचनात्मक कार्य का आधार बनते हैं। अतः बालक के विकास में संवेगों का विशेष महत्व होता है और संवेगों की उचित अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही
संभव है।
वैचारिक अभिव्यक्ति (Ideological Expression) :
पशु मूलप्रवृत्यात्मक प्रेरणा से, बिना परिणाम सोचे काम करते हैं, परन्तु मनुष्य कार्य का परिणाम सोचकर कार्य करता है। मनुष्य के लिए उसकी चिंतन शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी शक्ति से वह अपने को वातावरण के अनुकूल व्यवस्थित करता है। बालक को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें उसकी वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए।
वस्तुत: चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें पुराने अनुभवों के आधार पर सूक्ष्मतम विश्लेषण करते हुए भविष्य की चिंता की जाती हैं और किसी निश्चय पर पहुँचा जाता है। इस क्रिया को प्रत्ययात्मक चिंतन कहते हैं। प्रत्ययों का निर्माण संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण के आधार पर होता है। बच्चा घोड़े को देखकर अनुकरण में घोड़ा कहता है, पर अभी यह घोड़े और गधे में अंतर नहीं कर सकता। प्रत्यय ज्ञान के बाद बच्चा पदार्थ के गुणों का विश्लेषण करने लगता है। इसे प्रत्यय ज्ञान की दूसरी सीढ़ी माना गया है। पूर्णतः विश्लेषण करने के बाद बच्चा घोड़े के विषय में अपने ज्ञान का संश्लेषण करता है। विविध रंगों के होने के बाद सभी घोड़ों में एक समानता है। वे सभी एक से आकार के होते हैं। प्रायः एक जैसी सवारी का काम उनसे लिया जाता है, इसके बाद वह घोड़े, गधे, ऊँट आदि में अंतर समझने लगता है और उसका वर्गीकरण करने लगता है।
प्रत्यय ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है नामकरण, जब वह देखता है कि कुछ विशिष्ट गुणों के कारण एक पशु घोड़ा कहा जाता है, दूसरा बैल, तीसरा ऊँट आदि। इस प्रकार पशु विशेष का नाम लेने पर उसके न होने पर भी बालक उसका बोध भली प्रकार कर सकता है। इसलिए इस अवस्था में बालक को विभिन्न वस्तुओं को दिखाकर भाषा ज्ञान विकसित करना चाहिये। मांटेसरी विधि में भाषा शिक्षण के लिए इस प्रविधि का भरपूर उपयोग किया जाता है। तीन से चार वर्ष की आयु में बालक सरल वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। वह देश और काल से भी परिचित होने लगता है। चार वर्ष की आयु के पश्चात बच्चा केवल घटनाओं का दर्शक ही नहीं बना रहता, बल्कि वह उनका कारण भी जानना चाहता है। वह लंबे वाक्य बोलने लगता है, वह बड़े शब्दों को गढ़ना भी शुरू कर देता, जैसे दूधवाला, सब्जीवाला इत्यादि ।
बालक धीरे-धीरे बहुत से शब्दों को समझने लगता है परन्तु उनका प्रयोग नहीं कर पाता। इसके लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। बलक के मानसिक विकास का उसके भाषा विकास के साथ बहुत गहरा संबंध है। भाषा के अच्छे ज्ञान से वह अन्य विषयों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। कहानियाँ सुनाकर, चित्र दिखाकर उनका वर्णन करवाना, साधारण परन्तु उपयोगी वस्तुओं का वर्णन करने का अवसर प्रदान करना, शुद्ध उच्चारण सुनवाना तथा परस्पर बातचीत के अवसर सुलभ करवाना आदि गतिविधियों से बच्चों का मानसिक विकास होता है और वैचारिक अभिव्यक्ति भी सशक्त होती चली जाती है। बालक को मूर्त से अमूर्त का ज्ञान और निर्णय करने की क्षमता भाषा शिक्षण द्वारा ही संभव है।
2. सामाजिक अंतःक्रिया (Social Interaction) : भाषा हमारी संस्कृति का अंग होती है। नि:संदेह भाषा और संस्कृति में प्रगाढ़ संबंध है। भाषा को एक सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है, परन्तु भाषा संस्कृति का तत्व मात्र ही नहीं, बल्कि समस्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार है और इस कारण किसी भी समाज की विशेषताओं के अध्ययन के लिए उस समाज की भाषा का अध्ययन आवश्यक है।
लियोनार्ड ब्लूमफील्ड के शब्दों में, “भाषा की क्रिया ही प्रत्येक समुदाय के निर्माण का आधार है। भाषा सामाजिक क्रियाकलापों को समझने में सर्वाधिक प्रत्यक्ष अंतदृष्टि प्रदान करती है और उनको संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योग भी देती है। किसी भी मानव समुदाय को भलीभांति परखने के लिए हमें उसकी भाषा को समझना चाहिए। यदि हम किसी समुदाय की जीवन पद्धति और उसके ऐतिहासिक उद्गम का गहराई से अययन करना चाहते हैं तो हमें उसकी भाषा का व्यवस्थित विवरण प्राप्त करना होगा।”
3. सामाजिक और वैचारिक नियमन (Social and ideological regulations) :
भाषा का कार्य केवल विचारों का आदान-प्रदान ही नहीं है, बल्कि भाषा सामाजिक एवं वैचारिक विनियमन का एक साधन है। हम भाषा का प्रयोग दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने अथवा प्रभावित करने के लिए भी करते हैं। बर्नस्टीन व उसके साथियों ने बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में माता-पिता के विभिन्न प्रकार के नियामक व्यवहार का अध्ययन किया है और उन्होंने बड़े रोचक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। उसका एक उदाहरण है कि यदि कोई माता यह देखती है कि उसके बच्चे ने किसी दुकान से चुपके से कोई चीज उठा ली है तो वह भाषा की शक्ति का विभिन्न रूपों में उपयोग कर सकती है और बच्चे के मन में उनमें से प्रत्येक का भाषा की शक्ति के बारे मे अलग-अलग प्रभाव होगा।
उदाहरणतः वह कह सकती है—“तुम्हें उस चीज को नहीं उठाना चाहिए जो तुम्हारी नहीं है।” (वस्तुओं के स्वामित्व के आधार पर निषेध के माध्यम से नियमन) “यह उचित नहीं है” (नैतिकता के बोध द्वारा नियमन)। इस प्रकार की अकेली घटना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, किन्तु पुनरावृत्ति प्रबलन के माध्यम से नियामक व्यवहार के ये रूप बच्चे को व्यवहार नियंत्रक के रूप में भाषा की भूमिका का बोध कराते हैं। आगे चलकर बच्चा भी भाषा की इस भूमिका के बोध के प्रयोग अपने सम समूह और भाई-बहनों के व्यवहार का नियमन करने में करता है।
भाषा के नियामक प्रकार्य से ही जुड़ा भाषा का एक अन्य प्रकार्य है— उसका सामाजिक अंतःक्रियात्मक प्रकार्य। इससे आशय है कि स्वयं तथा दूसरों के बीच अंतःक्रिया में भाषा का प्रयोग। व्यक्ति का समस्त सामाजिक संपर्क, भाषा के माध्यम से ही होता। भाषा के द्वारा ही वह समाज से संबंध स्थापित करता है, अपने सुख-दुख, हर्ष-उल्लास में दूसरों को भागीदार बनाता है और दूसरों के सुख-दुख, हर्ष-उल्लास में अपनी भावनाओं को मूर्त रूप देता है।
व्यवहार की दृष्टि से भाषा के दो रूप हैं—उच्चरित रूप, लिखित रूप। लिखित रूप में भाषा का जो व्यवहार होता है, उसके भी दो पक्ष हैं—ग्रहण और अभिव्यक्ति अर्थात् पढ़ना और लिखना। भाषा एवं साहित्य को अक्षुण्ण बनाये रखने की दृष्टि से लिखित भाषा का महत्व है। सामाजिक संबंध बनाये रखने के लिए औपचारिक पत्र-व्यवहारों की आवश्यकता पड़ती है। वाणिज्य एवं व्यावसायिक कार्यों की संपन्नता के लिए भी हम पत्र-व्यवहार पर ही निर्भर करते हैं। सभी सम्मेलनों, समितियों, आयोगों आदि के प्रतिवेदन लिखित रूप में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। किसी भी कार्य के विवरण को स्थायी रखने के लिए हमें लिखित रूप का सहारा लेना पड़ता है। राष्ट्र का संविधान लिखित रूप में ही है। राष्ट्र के समस्त संसदीय, शासकीय न्यायिक, सैनिक आदि सभी कार्यों का संवहन लिखित संदेशों के द्वारा ही होता है। लिखित रूप को ही प्रामाणिक माना जाता है।
4.सृजनात्मकता (Creativity) :
प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मकता के तत्व निहित होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सृजनात्मकता के साथ उच्चकोटि की बौद्धिक क्षमता आवश्यक नहीं है। कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में सृजनात्मकता दिखा सकता है। जो बालक प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर कुछ आगे की ओर चिंतन करता है वह अपने कार्य तथा कार्य शैली में सृजनात्मकता दिखाता है।
सृजनात्मकता की योग्यता वाले बच्चे अपने विचारों से दूसरों को सरलता से प्रभावित कर लेते हैं। अतः प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मकता के विकास हेतु समुचित अवसर मिलना चाहिए। इस अवसर के मिलने पर वे बहुत-सी असफलताओं और कुण्ठाओं को सरलता से भूलकर मौलिकता की परिधि को विस्तृत कर सकते हैं। मानव जाति का इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक व्यक्ति अपनी कुण्ठाओं से ऊपर उठकर साहित्य, कला, विज्ञान, चित्रकला तथा संगीत आदि क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान कर पाये हैं। यदि कोई बालक किसी एक क्षेत्र में असफल होता है तो उसे दूसरे क्षेत्र में अपनी रचनाओं में सृजनात्मकता दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
सृजनात्मक लेखन से अभिप्राय बच्चे में चिंतन शक्ति और सृजनात्मक कल्पना का कवि बनाना नहीं है। भाषा शिक्षण में सृजनात्मक लेखन से अभिप्राय बच्चे में चिंतन शक्ति और सृजनात्मक कल्पना का विकास और उसके संवेगों और भावों को एक स्वस्थ समाजोपयोगी दिशा में परिवर्तित करके आत्म संतोष और गौरव की अनुभूति कराना है।
Q. 4. हिन्दी की व्यापकता पर प्रकाश डालें।
अथवा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी की स्थिति पर एक टिप्पणी लिखें।
Ans :
भारत के 18 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिन्दी है जबकि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिन्दी का इस्तेमाल द्वितीय भाषा के तौर पर करते हैं। यानी करीब 48 करोड़ लोग देश में सीधे तौर पर हिन्दी समझते-बोलते हैं। यही नहीं दुनिया के करीब 150 देश ऐसे हैं जहाँ हिन्दी भाषी लोग रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक होगी हिन्दी ।
शैक्षिक स्तर पर हिन्दी भाषा के अध्ययन-अध्ययन की स्थिति भी इतनी ही संतोषपद । भारत के बाहर लगभग 160 विश्वविद्यालयों या संस्थाओं में हिन्दी भाषा के अध्ययन की व्यवस्था है। दक्षिण अमेरिका में क्यूबा के हवाना विश्वविद्यालय और मंगोलिया के उलन बात्र ब्ला विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ायी जाती है। रूस, चीन आदि में हिन्दी अध्ययन की ओर प्रवृत्ति है। इंगलैंड, फ्रांस आदि में हिन्दी से संबंध शोध-कार्य हो रहे हैं।
क्या यह प्रच्छन्न स्वीकृति नहीं है कि भारत को समझने के लिए उसकी प्रमुख भाषा हिन्दी को समझना आवश्यक है। वे अन्य देश अक्सर मानते हैं कि हिन्दी के माध्यम से इस देश से सांस्कृतिक संबंध जोड़े जा सकते हैं। इसी प्रकार मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम तथा अन्य देशों के प्रवासी भारतीय भी अपनी मूल संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए इस भाषा को सुरक्षित रखना चाहते हैं।
कई भारतीयों के मन में यह प्रश्न उठता है कि हिन्दी विश्व की प्रमुख भाषाओं में एक है और इसके बोलने वालों की बड़ी संख्या है, फिर भी यह अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्यों नहीं बन पायी है। उत्तर देने से पहले हम कुछ जुड़े हुए सवालों पर भी दृष्टि डालना चाहेंगे, कुछ विषम स्थितियों की वार्ता करना चाहेंगे। मॉरिशस आदि देशों में जहां बहुसंख्यक प्रवासी भारतीय हैं, उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए उच्च स्तर पर हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की भी व्यवस्था नहीं हैं, किन्तु वहां हिन्दी साहित्य की कई विधाओं की रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं।
जहां तक अमेरिका, कनाडा आदि उन्नत देशों का सवाल है, तकनीकी विकास और संचार साधनों की उपलब्धि के कारण वहां के हिन्दी के कार्यकर्ता अधिक सक्रिय हैं, अधिक अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाते हैं। लंदन के रेडियो पर फोन के जरिये श्रोताओं से जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रस्तुत होता है, वह तो भारत में भी नहीं है। अमेरिका के टेलिविजन पर भारतीयों के लिए पेश किये जाने वाले कार्यक्रमों का स्तर देखकर विस्मय होता है।
सवाल है, दोनों प्रकार के देशों के प्रवासी भारतीय के सांस्कृतिक अस्मिता को सुरक्षित रखने का, हिन्दी की सृजानात्मक प्रतिभा को गति देने और इसके विकास को दिशा देने का, विचार और चिंतन को भाषा के रूप में हिन्दी को अपनाने का। स्थिति अनुकूल है, कार्यान्वयन की आवश्यकता है। अगर इन देशों में भी हिन्दी एक आधुनिक भाषा के रूप में विकसित हो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके प्रवेश में विलंब नहीं होगा।
Q.6. साहित्य की रचनाओं के उपयोग से व्याकरणिक तत्वों का संदर्भगत शिक्षण किस प्रकार करेंगे उदाहरण के साथ समझाएं।
अथवा, साहित्यिक रचनाओं का शिक्षण व्याकरण के तत्वों का संदर्भगत शिक्षा देने में सहायता करती है। कैसे? चर्चा करें।
Ans. किसी भी विषय वस्तु के अध्ययन हेतु विषय सामग्री का चयन कर पाना स्वयं में अति महत्वपूर्ण कार्य होता है। विषय सामग्री का समुचित चयन छात्रों के ज्ञान और अधिगम को विकसित करता है। ठीक इसी प्रकार हिंदी भाषा शिक्षण में साहित्य की रचनाओं का चयन न सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य की पूर्ति करता है बल्कि सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास के साथ-साथ भाषा के व्याकरणिक तत्वों का संदर्भगत विकास भी करता है। व्याकरण के तत्वों का संदर्भगत शिक्षण देने में साहित्य की पुस्तकें किस प्रकार सहायक सिद्ध होती है। हम निम्नांकित बिंदुओं के ऊपर विवेचना करते हुए समझ सकते हैं।
1.मात्राओं का सटीक प्रयोग—
बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी साहित्य की पुस्तक के अध्ययन से जोड़े रखती है। विशेषकर बच्चे तो मनोरंजन के उद्देश्य साहित्य की रचनाओं की ओर अधिक खींचे रहते हैं। इनके नियमित अध्ययन से बच्चों में मात्राओं की सही जानकारी प्राप्त होती है। इन मात्राओं के समुचित उपयोग सीख जाने से उनकी भाषा काफी समृद्ध हो जाती है।
2.विराम चिह्नों की सही जानकारी—
साहित्य की रचनाओं के उपयोग से बच्चों में विराम चिह्नों की सही जानकारी मिलने लगती है वह अपने लेखन एवं पठन में इनको सही प्रयोग में लाते हैं इस प्रकार उनकी भाषा शुद्ध सही और परिष्कृत होती चली जाती है। यही स्थिति आगे जाकर उनकी भाषायी की क्षमता के कौशलों में दक्षता प्रदान करती है।
3.शब्द-भंडारण-
साहित्य की रचनाओं के लगातार अध्ययन से लेखन और पाठन के साथ-साथ बच्चों में शब्द भंडारण भी काफी तेजी से बढ़ता है। वे नित्य नए-नए शब्दों के साथ स्वयं का परिचय पाते हैं और उनके अर्थ, संरचना एवं प्रयोग को भी जान पाते हैं।
4. वर्तनी की शुद्धता-
बच्चे जब साहित्य की रचनाओं को रुचि और आनंद के साथ पूरी तन्मयता से अध्ययन करते हैं, तब उनमें वर्तनी की शुद्धता काफी उत्कृष्ट और परिमार्जित होने लगती है। इससे अनेक लेखन में भाषागत अशुद्धियों के होने की संभावना शून्य होने लगती है और वे प्रभावी लेखन लिखने के लायक हो जाते हैं।
5. मानक लिपि से परिचय लिपि के मानक स्वरूप में नहीं हो पाने के कारण बच्चों का लेखन व्याकरणिक तौर पर अशुद्ध हो जाता है। इस समस्या का सरल, सहज और सशक्त समाधान है, बच्चों के बीच साहित्य की पुस्तकों का समुचित अध्ययन। बच्चें पुस्तकों के अध्यापन करते समय स्वयं जाँच लेते हैं कि किस वर्ण का मानक स्वरूप कैसा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि साहित्यिक पुस्तकों का अध्ययन मानक लिपि की अच्छी समझ प्रदान कर पाने में काफी प्रभावी तथा सहायक होती है।
6. भाषायी कुशलताओं का विकास भाषा के चारों आधारभूत कौशलों का विकास भी साहित्य की रचनाओं के सतत् अध्ययन से संभव है। बच्चे कविता कहानी चित्रकथा, गीत आदि का श्रवण, वाचन, पठन और लेखन बड़ी रुचि के साथ करना पसंद करते हैं। इनको उचित मार्गदर्शन देकर शिक्षक इनकी भाषायी कुशलताओं को विकसित कर सकता है।
7. व्याकरणिक नियमों की जानकारी-साहित्य की रचनाओं के सफल और ध्यान पूर्वक अध्ययन से बच्चों में व्याकरण के नियमों की जानकारी आसानी से हो जाती है। बच्चों में संधि के नियम उपसर्ग की जानकारी आसानी से हो जाती है। बच्चों में संधि के नियम उपसर्ग, प्रत्यय, रचना, लिंग, वचन, कारक, चिह्न विभक्ति, समास आदि के नियमों के गुण स्वतंत्र अध्ययन से ही आने शुरू हो जाते हैं।
इस प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं कि साहित्यिक रचनाओं का उपयोग बच्चों में व्याकरण की पारंगतता लाने में सहायता करती है। यह बच्चों को शुद्ध और मानक भाषा का प्रयोग, अशुद्ध भाषा की जाँच कर पाने, अपनी अभिव्यक्ति में शुद्धता लाने, लेखन में व्यवस्थापूर्ण रचना कर पाने, भाषा विश्लेषण की योग्यता प्राप्त करने, मानसिक अनुशासन को बनाए रखने आदि में काफी प्रभावी और सहायक है।
Q. 7. साहित्य की विभिन्न विधाओं का भाषा शिक्षण में उपयोग करने के क्या उद्देश्य हैं?
Ans.
कहानी शिक्षण के उद्देश्य:
1. साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना।
2. कहानी में निहित भावों, विचारों, नैतिक मूल्यों को ग्रहण करने की क्षमता. विकसित करना।
3. सृजनात्मक शक्ति का विकास करना।
4.शब्द, सूक्ति, मुहावरे आदि के भंडार को समृद्ध करना।
5. अंदाजा लगाने की क्षमता का विकास करना।
6. एकाग्रता को विकसित करना।
7. कहानी की रचनाशीलता का विकास करना।
8. कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास करना।
गद्य की अन्य विधाओं के शिक्षण के उद्देश्य-
1. साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना।
2. विधा की रचनाशीलता तथा एकाग्र होकर पाठ को आत्मसात करने की क्षमता का विकास करना ।
3. मंच पर अभिनय करने की क्षमता एवं अवसरानुकूल शब्दावली का प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना ।
4. ऐतिहासिक कथाओं, पौराणिक विचारों एवं सामाजिक कुरीतियों से परिचित कराना।
5. उचित यति-गति, हाव-भाव, आरोह-अवरोह तथा उतार-चढ़ाव के साथ उच्चारण की क्षमता विकसित करना।
6. निरीक्षण, कल्पना, बोध एवं विवेचन के गुण विकसित करना।
7. शब्द, सूक्ति, मुहावरे आदि के भंडार को समीक्षा करना।
8. अंदाजा लगाने की क्षमता का विकास करना।
9. कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास करना।
कविता (पद्य) शिक्षण के उद्देश्य-
1. कविता की पढ़ाई के
2. भावों, विचारों, नैतिक करना। दौरान सस्वर पठन की कुशलता विकसित करना। मूल्यों को ग्रहण करने तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास
3. कविता पढ़ने के बाद उसकी समीक्षा करने की योग्यता का निर्माण ।
4. कविता को उचित यति-गति, आरोह-अवरोह के साथ गाना।
5. कल्पना शक्ति विकसित करना।
6. पठित अथवा उच्चरित कविता के अर्थ, भाव एवं कल्पना को साथ-साथ ग्रहण करने और उनकी व्याख्या करने की योग्यता विकसित करना।
7. कविता रचने की आदत विकसित करना।
Q. 8. साहित्य की समझ (शब्द शक्ति एवं अन्य साहित्यिक तत्वों) का उपयोग विद्यार्थियों की भाषाई क्षमताओं को विकसित करने हेतु किस प्रकार करेंगे?
Ans.
साहित्य की समाज छात्रों को ना सिर्फ मनोरंजन आनंद देता है बल्कि यह छात्रों की भाषाई क्षमताओं को भी विकसित करता है। छात्र जब साहित्य की पुस्तकों को बार-बार मजे लेकर पढ़ते हैं तब वे स्वयं को उत्साहित अनुभव करते हैं किताबों के पन्नों को बार-बार पढ़ते है जिसमें बच्चों की दुनिया की झलक मिलती है साहित्य के अंतर्गत कविता, कहानी, नाटक, हास्य, व्यंग, रोमांच से भरी बातें, संस्मरण यह सभी कुछ आते हैं। जिसे पढ़कर छात्रों को आनंद की अनुभूति होती है।
साहित्य की समझ छात्रों की भाषायी क्षमताओं को विकसित करने हेतु निम्न प्रकार से मदद करता है-
1. छात्र जैसे-जैसे कहानी को आगे पढ़ते और सुनते हैं वे पीछे की घटनाओं को भी याद रखते चलते हैं। यदि ऐसा ना हो तो आगे की कहानी और उसकी अपनी कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस प्रकार यह छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास करने में सहायक है।
2. वैसे छात्र जो पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त साहित्य की किताबों से कविता, कहानी, लेख आदि को पढ़ते रहते हैं। उनका भाषाई उच्चारण काफी शुद्ध होता है। वे व्याकरणगत अशुद्धियों को कम करते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि इन बच्चों में साहित्य की समझ ना रखने वाले बच्चों की तुलना में समालोचनात्मक चिंतन की क्षमता अधिक होती है। यह आमतौर पर अच्छे लेखक या वक्ता बन सकते हैं।
3. विभिन्न अध्ययनों से भी यह पता चलता है कि जो बच्चे साहित्य का अध्ययन करते हैं उनका शब्द भंडारण काफी विस्तृत होता है और वे परिष्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं।
4. साहित्य की समझ छात्रों को मानव जीवन के उन पहलुओं के बारे में भी परिचय कराता है जिनसे उनको भविष्य में सामना करना पड़ता है। यदि कहा जाए कि साहित्य के कारण छात्र भविष्य के लिए तैयार होते हैं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।
5.साहित्य की सहायता से छात्र भिन्न-भिन्न परिवारों, परिवेशों परंपराओं, रीति-रिवाजों आदि से अवगत होते हैं। इस कारण छात्रों में सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता के गुण उभरते हैं और एक आदर्श व समरस समाज का निर्माण होता हैं।
6. साहित्य पढ़ने से छात्रों में कल्पनाशीलन बनने की क्षमता के साथ-साथ रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता का गुण भी विकसित होता है।
7. साहित्य छात्रों को समाज में प्रचलित और प्रतिस्थापित मानक व्यवहारों, विश्वासों आदि के विषय में एक तार्किक समझ विकसित करता है।
8. पढ़ना स्वयं में एक आनंददायी ही अनुभव है यह घंटों छात्रों को एक सार्थक गतिविधि में रमाए रखता है।
उपरोक्त बिंदुओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य की समझ का उपयोग ना केवल विद्यार्थियों की भाषायी क्षमता को विकसित करती है वरन् उनमें सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, धार्मिक गुणों से भी परिपूर्ण कर एक आदर्श और सफल नागरिक निर्माण हेतु दिशा प्रदान कराती है। यह छात्रों में कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, सृजनात्मक चिंतन के साथ-साथ स्वस्थ एवं सार्थक मनोरंजन का भी विकास कराती है।
Q.9. साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी कविता आदि का उपयोग कर विद्यार्थियों की भाषायी क्षमताओं का विकास किस प्रकार करेंगे?
उत्तर—
साहित्य के रस का स्वाद व्यक्ति को पठन एवं लेखन के प्रति अभिप्रेरित करता है। साहित्य की दो प्रमुख विधाएँ हैं गद्य और पद्य । गद्य शब्द संस्कृत के गद् धातु से बना है जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कथन। यह साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें लय, गति और संगीत का अभाव होता है। गद्य के अंतर्गत कहानी की विधा आती है दूसरी साहित्यिक विधा है, पद्य। यह मन के विचारों को लय एवं ताल के द्वारा अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करती हैं। मनुष्य के मानसिक भावों को प्रकट करने का यह नूतन साधन है पद्य के अंतर्गत कविता की विधा आती है।
भाषा शिक्षण में छात्रों की भाषा की कुशलताओं और क्षमताओं को विकसित करने में साहित्य की दोनों विधाओं कहानी और कविता का अपना विशेष स्थान है। प्रायः यह देखा जाता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अधिकांश पाठ कहानी और कविता के रूप में ही prstut रहते हैं।
कहानी—
कहानी जीवन के सत्य को उजागर करती है जीवन के किसी पक्ष क की विवेचना करती है। कहानी की सहायता से कहानीकार लक्ष्य की ओर बढ़ता है। कहानी में कसावट कम गुण होना चाहिए। कहानियों को पढ़ना और सुनना स्वयं में एक बड़ा ही आनंदपूर्ण अनुभव होता है। कहानी के आरंभ होते ही बच्चों का ध्यान एवं आकर्षण दोनों कहानी के नुक्से तक खिंचे चले आते हैं क्योंकि बच्चे खुद को कहानी में देखते हैं। कहानी में होने वाली घटनाओं से उनके आकर्षण को बल मिलता है।
जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है वैसे-वैसे छात्रों की कल्पना चिंतन और जिज्ञासा भी बढ़ती चली जाती है। कहानी के कारण छात्रों में श्रवण, वचन और पठन जैसी आधारभूत भाषायी कौशलों का विस्तार होता है। छात्रों की वैचारिक सृजनशीलता की सीमा बढ़ती है। मात्राओं का सटीक प्रयोग विराम चिह्न की सही जानकारी शब्द भंडारण में वृद्धि, उच्चारण और वर्तनी की शुद्धता मानक लिपि में निर्धारित वर्णों के स्वरूप की पहचान, शब्दों तथा वाक्य के निर्माण में संरचनात्मक तारतम्यता आदि गुणों का विकास कहानी शिक्षण की मदद से सरलता और सहजता के साथ प्रदान की जा सकती है। भाषिक गुणों में कुशलताओं की प्राप्ति के साथ-साथ छात्रों को नैतिक, चारित्रिक और वैचारिक गुणों को भरने के लिए भी कहानी एक सशक्त और प्रभावी साधन होती है। पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियाँ इसका जीवंत उदाहरण है।
कविता-कविता मन के भावों की स्वच्छंद श्रृंखला है। कविता में भाव कल्पना और बुद्धि तीनों का समावेश्न होता है। कविता द्वारा मानवीय सुख-दुख को अत्यंत सहज भाव से अभिव्यक्त किया जाता है। इसका अध्यापन सुर, लय एवं ताल के अनुरूप किया जाता है। इसके अध्यापन से छात्रों में उनकी आत्मिक और हार्दिक भावों को व्यक्त कर पाने की क्षमता का विकास होता है।
कविता के माध्यम से छात्रों में शब्द और स्पष्ट उच्चारण की क्षमता का विकास होता है। उचित भात्रानुकूल चेहरे की मनोदशा को विभिन्न मुद्राओं द्वारा व्यक्त कर पाने का गुण विकसित होता है। कल्पना शक्ति का सम्यक विकास होने के कारण छात्रों में सृजनात्मक और रचनात्मक गुणों का विकास हो पाता है। काव्य-सौंदर्य के विभिन्न पक्षों को स्वयं जाँच पाने की क्षमता बढ़ती है। कविता शिक्षण के कारण छात्रों में समुचित ध्वनि अनुतान, बलाघात, आरोह-अवरोह की समझ प्राप्त होती है यह छात्रों में राष्ट्रप्रेम, दया, सद्भाव, सहानुभूति, चरित्र निर्माण, विश्व बंधुत्व आदि की भावना भरने का भी कार्य करती है। यह भाव के अनुरूप स्वर, लय, ताल, गति आदि के समावेशन का अद्भुत दया, चरित्र निर्माण, विश्व बंधुत्व आदि की भावना भरने का भी कार्य करती है। यह भाव के अनुरूप स्वर, लय, ताल, गति, यति के समावेशन का अद्भुत एवं प्रभावी संयोजन होती है।
Q.10. साहित्य का उपयोग कर बच्चों में कल्पना करने, समझ, चिंतन करने अथवा व्यक्त करने हेतु स्थितियों की रचना के लिए रणनीतियों की चर्चा करें।
Ans. हिंदी भाषा शिक्षण के अनेक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य बच्चों की कल्पना शीलता, चिंतन क्षमता, वर्णन करने की क्षमता आदि का विकास करना। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ी गई सामग्री के बारे में चिंतन करते हैं कि क्या कहने का प्रयास किया गया है, क्या उचित है या अनुचित है। ठीक इसी प्रकार लेखन करते समय यह सोचते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं एवं किस तरह सटीक भाषा का प्रयोग करना है। इस प्रकार अन्य विषयों की भाँति हिंदी भाषा में भी चिंतन क्षमता का अपना विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पना करके एवं चिंतन करके ही बच्चे एक प्रभावी एवं अच्छे लेखक और वक्ता बनते हैं। हिंदी भाषा में कल्पना-शीलता का विकास एक मुख्य उद्देश्य है. जो बच्चों में भाषाई सृजनशीलता पर बल देता है। हम अनेक तरीकों से उनकी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। यह रणनीतियां निम्नांकित है-
1. बच्चों से किसी आँखों देखी घटना का वर्णन करने के लिए कहना या उनसे उनकी दिनचर्या के विषय में पूछना बातचीत जितनी अनौपचारिक होगी बच्चे इतने सहज और निःसंकोच भाव से अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर पाएंगे।
2. बच्चे से कल्पना शक्ति को बढ़ाने वाले प्रश्नों को पूछना उनसे ऐसे पूछा जाए कि “यदि आपके घर कोई बड़ी हस्ती पहुँच जाए तो अब आप क्या करोगे?” या “ अगर आप किसी प्रतियोगिता में एक लाख रूपए जीत जाए तो आप क्या करेंगे?”
3. बच्चों से यह पूछा जाए कि आप अपने आवास, आस-पड़ोस, विद्यालय आदि में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? इस प्रकार के प्रश्न द्वारा बच्चों में कल्पना-शीलन, चिंतन क्षमता एवं रचनात्मकता का विकास होता है।
4. बच्चों से किसी कहानी में परिवर्तन करके उस कहानि को फिर से सुनाने को कहें जैसे खरगोश और कछुआ की कहानी में यदि वह कछुआ सो गया होता तब क्या होता? शिक्षक स्वयं भी किसी कहानी को शुरू करके उसके मध्य एवं अंत को अलग-अलग बच्चों द्वारा पूरा कराएं ऐसी गतिविधियों के कारण बच्चे अपनी कल्पना शक्ति एवं चिंतन क्षमता द्वारा कहानी को आगे बढ़ाकर उसका अंत करेंगे।
5. बच्चों से पहेलियाँ बनवाई जाए और उन्हें पूछा जाए साथ ही उन्हें उनसे कहानियाँ बनाकर भी कहने को कहा जाए।
6. किसी विषय पर बच्चों को भाषण वाद-विवाद आदि करने के लिए भी कहा जाए। इससे उनकी मौखिक अभिव्यक्ति के साथ-साथ चिंतन और कल्पना शक्ति दोनों क्षमताओं का विकास होता है।
7. बच्चों को विषय देकर इनसे कविता, कहानी, निबंध, लेख, पत्र, विज्ञापन, संदेश,सूचना आदि लिखवाए जा सकते हैं।
8. बच्चों के साथ उनके घर, पड़ोस समाज शहर, राज्य, देश-विदेश आदि की सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण, व्यापारिक, समस्याओं जैसे विषयों तथा उनके समस्याओं के समाधानों पर भी चर्चाओं का सफल आयोजन किया जा सकता है।
Q.11. हिंदी शिक्षण के विभिन्न उपागम-व्यवहारवादी रचनात्मकता तथा आलोचनात्मक उपागम की समझ विकसित करें।
Ans. 1.
व्यवहारवादी उपागम-
व्यवहारवादी उपागम की अनुसार सीखना एक यांत्रिक व्यवस्था है। इसमें सीखने वालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपेक्षित व्यवहार का प्रदर्शन करें। जब तक वह अपेक्षित व्यवहार का प्रदर्शन ना करें तब तक उसके अनपेक्षित व्यवहारों को अस्वीकार किया जाता रहेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यह अपेक्षित व्यवहार क्या है, यह सिखाने वाला तय करेगा। इसमें सीखने वाले की सक्रिय भूमिका नहीं होती है बल्कि सिखाने वाला सीखने वाले के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। इसमें उन विधियों का उपयोग किया जाता है जिसमें सूचनाओं तथ्यों और विचारों का एकतरफा प्रभाव होता है जैसे-व्याख्यान विधि। इसमें ऐसा माना जाता है कि ज्ञान बाहर से सीखने वाले के भीतर प्रवेश करता है और आवश्यकतानुसार सीखने वाला उसी ज्ञान को संप्रेषित कर देता है। इसे माना जाता है कि किसी कविता, कहानी, घटना आदि की एक ही व्याख्या हो सकती है। इस अर्थ में व्यवहारवादी उपागम ज्ञान को एक रखिए मानता है। इसमें किसी कविता आदि की वहीं व्याख्या सही मानी जाएगी जिसे सिखाने वाला सही मानता है। इसलिए इस उपागम में सीखने वाले की सक्रिय भूमिका को स्वीकार नहीं किया जाता है। सीखने वाले के अनुभव, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति अथवा आर्थिक परिस्थिति, मनोदशा आदि के लिए इस उपागम में कोई स्थान नहीं होता है।
2. रचनात्मक उपागम—
रचनात्मक उपागम में सीखने वाले की सक्रिय भूमिका होती है। इसमें व्यवहारवादी उपागम की भांति सीखने वाला यांत्रिक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य नहीं होता है। इसमें सीखने वाले को चिंतन करने, अर्थ निकालने प्रतिक्रिया देने आदि की छूट होती है। इस प्रकार रचनात्मक उपागम में ज्ञान एक रखिए ना होकर बहुपक्षीय होता है। रचनात्मक उपागम में सीखने वाले के समक्ष जो तथ्य रखे जाते हैं, वह उन पर यांत्रिक ढंग से प्रतिक्रिया देने को बाध्य नहीं होते हैं। दूसरी ओर वे उन्हें तथ्यों पर चिंतन करते हैं और फिर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वे मानते हैं कि इंसान का सीखना इनपुट-आउटपुट सिद्धान्त के आधार पर नहीं चलता है। उनके अनुसार ज्ञान एकपक्षीय ना होकर बहुपक्षीय है अर्थात् एक कविता, कहानी, घटना के एक से अधिक अर्थ भी निकल सकते हैं। अर्थ का निकलना सीखने वाले के अनुभवों पर निर्भर करता है। इस उपागम में व्याख्यान विधि के स्थान पर गतिविधि आधारित शिक्षण को विशेष महत्व और स्थान दिया जाता है। रचनात्मक उपागम का उद्देश्य छात्रों के अंदर अर्थ निकालने और रचना के सृजन कर पाने की क्षमताओं का विकास करना है।
3. आलोचनात्मक उपागम—
आलोचनात्मक उपागम का स्रोत पूरी तरह आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है। यह शिक्षण शास्त्र मानता है कि शिक्षा की पूरी प्रक्रिया राजनीतिक होती है, अतः शिक्षा में शिक्षण के तरीके को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि पढ़ने के तरीके ऐसे हो कि जिन से छात्रों का ध्यान समाज में फैली हुई विषमताओं, अंधविश्वासों, अन्याय, मिथकों में अंतर्निहित शक्ति समीकरणों की ओर टिके और वे इन से टकराने के आवश्यक समझ और साहस का विकास कर सके। अतः इस उपागम में सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों पर आलोचनात्मक उपागम को शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाता है। आलोचनात्मक उपागम संवाद को शिक्षण प्रक्रिया की दूरी मानता है। यहाँ संवाद का अर्थ सामान्य बातचीत से नहीं है बल्कि संवाद का अर्थ कहीं जा रही बातों में विद्यमान माताओं को सामने लाना और उनमें निहित शक्ति समीकरणों को उजागर करना। उजागर करने के बाद उनके समतामूलक मनाने के बेहतर विकल्प प्रस्तुत करना है। आलोचनात्मक उपागम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को मुक्तिदायी बनाना है, जिसे एक आदर्श
समाज और लोक कलयाणकारी राष्ट्र का निर्माण हो सके।
Q.12. विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता, चिंतन क्षमता, वर्णन करने की क्षमता आदि का मूल्यांकन करने के पैमानों और तरीकों का उल्लेख करें।
Ans. विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता, चिंतन क्षमता, वर्णन करने की क्षमता आदि का मूल्यांकन करने के पैमाने- यह आकलन करना कि छात्र-
1. किसी वस्तु का वर्णन करती/करता है।
2. कल्पना व अनुभव से कहानी बनाती/बनाता और आगे बढ़ाती/बढ़ाता है।
3. किसी वस्तु के सामान्य उपयोग के अलावा अन्य उपयोग सोचती/सोचता है।
4. अनुपयोगी तथा कम वाली सामग्री का इस्तेमाल करते हुए मुखौटे आदि बनाती बनाता तथा अभिनय में उनका इस्तेमाल करती/करता है।
5. भाषा के सौंदर्य की सराहना करती/करता है।
6. आस-पास मौजूद पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों तथा लोगों के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखती/रखता है।
7. चीजों के व्यर्थ इस्तेमाल को रोकती/रोकता है।
हिंदी भाषा शिक्षण के अनेक देशों में से एक उद्देश्य है- बच्चों की कल्पनाशीलता, चिंतन क्षमता, वर्णन करने की क्षमता, आदि का विकास करना। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ी गयी सामग्री के बारे में चिंतन करते हैं कि क्या कहने का प्रयास किया गया है, क्या उचित है अथवा नहीं। उसी प्रकार जब हम लिखते हैं तो यह सोचते हैं कि क्या लिखना है, क्या नहीं एंव किस तरह सटीक भाषा का प्रयोग करना है। इस प्रकार अन्य विषयों की तरह हिंदी भाषा में भी चिंतन क्षमता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पना करके एवं चिंतन कर के ही बच्चे एक प्रभावी तथा बेहतर लेखक एवं वक्ता बनते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में कल्पनाशीलता का विकास एक मुख्य उद्देश्य है जो बच्चों में भाषायी सृजनशीलता पर बल देता है। कल्पना और चिंतन बच्चों को एक बेहतर तथा प्रभावी वक्ता एवं लेखक बनने में मदद करते हैं। हम अनेक तरीकों से उनकी इन क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं। जैसे-
1. बच्चों से किसी आँखों देखी घटना का वर्णन करने के लिए कहना या उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में पूछना। बातचीत जितनी अनौपचारिक होगी, बच्चे उतना ही निःसंकोच रूप से अपनी बात कहेंगे तथा वर्णन करेंगे।
2. बच्चों से कल्पना करने वाले सवाल पूछे। उनसे पूछे कि “यदि चाँद तुम्हारे आंगन में उतर जाए तो तुम क्या करोगे” या “तुम्हारे घर में कोई बड़ी हस्ती पहुँच जाए तो अब क्या करोगे? इससे उन्हें कल्पना करने का भरपूर अवसर मिलेगा।
3. बच्चों से पूछे कि तुम अपने घर स्कूल पास-पास में क्या बदलाव लाना चाहते हो? यह गतिविधि बच्चों में चिंतन क्षमता का विकास और आकलन करती है।
4. बच्चों से किसी कहानी में परिवर्तन करके उस कहानी को दोबारा सुनाने के लिए कहें। स्वयं कोई कहानी शुरू करके उसका विकास और अंत भी विभिन्न बच्चों से करवाया जा सकता है। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे अपनी कल्पनाशीलता एवं चिंतन क्षमता के द्वारा कहानी को आगे बढ़ाएंगे एवं उसका अंत करेंगे।
5. बच्चों से पहेलियां बनवायी या पूछी जा सकती है एवं उनसे कोई कहानी कहने के लिए भी कहा जा सकता है।
6. किसी विषय पर बच्चों को भाषण, वाद-विवाद आदि करने के लिए भी कहा जा सकता है जिससे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के साथ-साथ कल्पनाशीलता एवं चिंतन क्षमता दोनों का आकलन हो सकता है।
7. बच्चों को विषय देखकर उससे कहानी, कविता, निबंध, पत्र, विज्ञापन संदेश, सूचना आदि लिखवाए जा सकते हैं।
8. बच्चों के साथ उनके घर-मोहल्ले, गाँव-शहर, देश की विभिन्न समस्याओं और समाधानों पर चर्चा की जा सकती है, आदि।
Q. 13. विद्यार्थी के मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के पैमानों और तरीकों का उल्लेख करें।
Ans, विद्यार्थी के मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के पैमानें- यह आकलन करना कि छात्र-
1. सुनकर-समझकर, सोचकर बोलता है।
2. बात को धैर्य और ध्यान के साथ सुनती/सुनता है।
3. कविता/कहानी विवरण हाव-भाव एवं आवाज के उतार-चढ़ाव के साथ सुनाती/ सुनाता है।
4. क्या, कब, कहाँ, किससे, कैसे और क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में देती/ देता है।
5. नाटक एवं संवाद सुनकर प्रमुख तत्व ग्रहण करती/करता है।
6. परिचित परिस्थितियों के बारे में बातचीत करती/करता है।
7. बोलते समय लिंग, वचन का सामंजस्य रखती/रखता है।
8. हो रहे कार्य के संबंध के क्या, कब कैसे वाले प्रश्न पूछती/पूछता
9. दैनिक जीवन में विभिन्न संदर्भों में स्वयं को अभिव्यक्त करती/करता है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करने के कई ऐसे तरीके हैं जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान भी संपादित किया जा सकता है। जैसे कक्षा 8 की पुस्तक में पाठ 7 साइकिल की सवारी को पढ़ने के बाद बच्चों को उस पर बातचीत की ..जा सकती है। यह बातचीत केवल पाठ के अंत में दिए हुए सवालों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। हम उनसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिसमें उनकी चिंतन उनकी कल्पना व स्वअभिव्यक्ति को जगह मिल सके जैसे कि-
1. जब आपने साइकिल चलाना सीखा तब आपके साथ क्या-क्या हुआ? बताइए।
2. क्या आपकी साइकिल सीखने और लेखक के द्वारा साइकिल सीखने की प्रक्रिया में कोई अंतर है? कैसे?
3. क्या होता अग़र आपके सामने से कार आ रही होती?
4.क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जब भी कोई नई चीज सीखी जाती है तो मुश्किलें आती ही है? कैसे?
5. सड़क पर साइकिल या कोई अन्य वाहन चलाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों?
इसके अलावा हम निम्नलिखित तरीकों से बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं-
1. बच्चों से कह सकते हैं कि किसी कहानी को अपनी भाषा और अपने शब्दों में सुनाइए ।
2. गाने की शुरूआत किसी एक बच्चे से कराएं और बारी-बारी से उस कहानी को विभिन्न बच्चों द्वारा आगे बढ़ाते चलें।
3. बच्चों को किसी कहानी का मंचन करने के लिए भी कह सकते हैं जिससे विभिन्न परिस्थितियों वे सही तरीके से अपनी बात कहने की कुशलता विकसित कर सकेंगे।
4. बच्चों से किसी वस्तु, चित्र, आँखों देखी घटना, दृश्य, अनुभवों आदि का मौखिक वर्णन भी करवा सकते हैं।
5. बच्चों को शब्द अंताक्षरी के द्वारा भी मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। एक बच्चा जो शब्द कहेगा उसकी अंतिम आवाज से शुरू होने वाले कोई अक्षर से अगला शब्द दूसरे बच्चे का कहना होगा और इसी प्रकार अंताक्षरी आगे बढ़ती जाएगी।
Q. 14. हिंदी की बहुभाषिक विशेषताओं की समझ साहित्य की मदद से बच्चों में किस प्रकार विकसित करेंगे?
Ans.
साहित्य का अध्ययन करना हम बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी रोचक और आनंददायी होता है। गंभीर से गंभीर विषयवस्तु को भी हम साहित्य की मदद से बड़ी सरलता एवं सहजता के साथ आकर्षक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाल शिक्षा के क्षेत्र में तो साहित्य की समझ का होना एक प्रभावकारी व क्रांतिकारी साधन है। भाषा शिक्षण या विशेषकर हिंदी के संदर्भ में साहित्य की समझ का होना नितांत आवश्यक है।
हिंदी की बहुभाषिक विशेषता काफी समृद्ध और विस्तृत है। इस बहुभाषिक विशेषता की समस्याएँ बच्चों में साहित्य की सहायता से बड़ी आसानी से प्रदान कर सकते हैं। हिंदी की संपदा और इसकी प्रभावशीलता बहुभाषिकता से अछूती नहीं है। इस कारण बच्चों में हिंदी की भाषिक विशेषताओं की समझ का होना जरूरी है। इस समझ को प्रदान करने में साहित्य से बढ़कर कोई अन्य साधन और विकल्प उपलब्ध नहीं हो सकता है-
1. क्षेत्र विशेष अनुसार अनुदान या बलाघात परिवर्तन-
हम बिहार राज्य के संदर्भ में ही देख सकते हैं कि मैथिली, मगही, अंगिका, भोजपुरी आदि भाषाएँ प्रचलन में तो हिंदी के ही समान है परंतु इनकी अनुदान या बलाघात क्षेत्र विशेष के अनुसार परिवर्तित होती है। ध्वनियों के आरोह-अवरोह भी क्षेत्रीयता के प्रभाव से बच नहीं पाते हैं या स्थिति हिंदी की बहुभाषिक विशेषता को प्रदर्शित करती है।
2.अन्य भाषिक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग—
अध्ययनों से ऐसा पता चलता है कि जिन बच्चों में सीखने के क्रम में एक से अधिक भाषाओं में कुशलता का विस्तार करने का अवसर मिला है। उनमें रचनात्मक और सामाजिक सहिष्णुता आदि जैसे गुणों का विकास सीखने की प्रक्रिया के साथ-साथ चलती है। अतः अन्य भाषिक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करने वाले बच्चे स्वतः ही बहुभाषिक विशेषता के प्रभाव में आ जाते हैं।
3. सामाजिक परिस्थितियों में स्थापन—
हिंदी की बहुभाषिक विशेषताओं में विशेष विशेषता यह है कि बहुभाषिक बच्चों में स्वयं को विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में स्थापित करने की कुलशता आ जाती है बच्चे अलग-अलग प्रकार के सामाजिक परिवेश में प्रतिस्थापित सामाजिक, मूल्यों, व्यवहारों, परंपराओं, रीति-रिवाजों आदि की जानकारी साहित्य की मदद से बाते हैं। वे अपने सामाजिक जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में उनका उपयोग स्वयं को स्थापित कर पाने के लिए करते हैं।
4. भाषिक संपदा के रूप में साहित्य की सहायता से हम बच्चों में हिंदी की बहुभाषिक भाषा ही संपदा के रूप में उनकी हिंदी को काफी समृद्ध और परिमार्जित कर सकते हैं हिंदी के विभिन्न स्वरूपों जैसे- अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका आदि की अच्छी समझ प्रदान करा सकते हैं। इस प्रकार हम बच्चों की हिंदी के साथ-साथ उनके साहित्य की समझ को भी विस्तारित कर पाते हैं।
5. राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान-
हिंदी स्वयं में इतनी सामर्थ्यवान और शक्तिशाली है कि वह संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने में सक्षम है। बच्चों में साहित्य की मदद से हिंदी की बहुभाषिक विशेषताओं को बताते हुए हम एक दूसरे की भाषा को उचित सम्मान देने की शिक्षा दे सकते हैं। इसका प्रभाव शिक्षा के काफी संवेदनशील स्वरूप में दिखाई देगा। हिंदी की बहुभाषिका भरी विशेषता ना केवल बच्चे की अस्मिता को जन्म देती है अपितु या भारत की भाषा परिदृश्य का अद्भुत गुण प्रस्तुत करती है। यही बहुभाषिक विशेषता साहित्य के अध्ययन को करते-करते राष्ट्रीय एकता के भाव को भी प्रबल करती है।
Q. 15. हिंदी भाषा की विशेषताओं का वर्णन करें।
Ans.
हिंदी भाषा के निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-
1. हिंदी का उद्भव भाषाओं की जननी, देवभाषा संस्कृत से हुआ है जो आज भी तकनीकी क्षेत्र (कम्प्यूटर आधारित प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बौद्धिकता इत्यादि) में प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा मानी जा रही है।
की भाषिक विशेषताओं की समझ का होना जरूरी है। इस समझ को प्रदान करने में साहित्य से बढ़कर कोई अन्य साधन और विकल्प उपलब्ध नहीं हो सकता है-
1. क्षेत्र विशेष अनुसार अनुदान या बलाघात परिवर्तन- हम बिहार राज्य के संदर्भ में ही देख सकते हैं कि मैथिली, मगही, अंगिका, भोजपुरी आदि भाषाएँ प्रचलन में तो हिंदी के ही समान है परंतु इनकी अनुदान या बलाघात क्षेत्र विशेष के अनुसार परिवर्तित होती है। ध्वनियों के आरोह-अवरोह भी क्षेत्रीयता के प्रभाव से बच नहीं पाते हैं या स्थिति हिंदी की बहुभाषिक विशेषता को प्रदर्शित करती है।
2. अन्य भाषिक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग — अध्ययनों से ऐसा पता चलता है कि जिन बच्चों में सीखने के क्रम में एक से अधिक भाषाओं में कुशलता का विस्तार करने का अवसर मिला है। उनमें रचनात्मक और सामाजिक सहिष्णुता आदि जैसे गुणों का विकास सीखने की प्रक्रिया के साथ-साथ चलती है। अतः अन्य भाषिक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करने वाले बच्चे स्वतः ही बहुभाषिक विशेषता के प्रभाव में आ जाते हैं।
3. सामाजिक परिस्थितियों में स्थापन — हिंदी की बहुभाषिक विशेषताओं में विशेष विशेषता यह है कि बहुभाषिक बच्चों में स्वयं को विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में स्थापित करने की कुलशता आ जाती है बच्चे अलग-अलग प्रकार के सामाजिक परिवेश में प्रतिस्थापित सामाजिक, मूल्यों, व्यवहारों, परंपराओं, रीति-रिवाजों आदि की जानकारी साहित्य की मदद से बाते हैं। वे अपने सामाजिक जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में उनका उपयोग स्वयं को स्थापित कर पाने के लिए करते हैं।
4. भाषिक संपदा के रूप में साहित्य की सहायता से हम बच्चों में हिंदी की बहुभाषिक भाषा ही संपदा के रूप में उनकी हिंदी को काफी समृद्ध और परिमार्जित कर सकते हैं हिंदी के विभिन्न स्वरूपों जैसे- अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका आदि की अच्छी समझ प्रदान करा सकते हैं। इस प्रकार हम बच्चों की हिंदी के साथ-साथ उनके साहित्य की समझ को भी विस्तारित कर पाते हैं।
5. राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान- हिंदी स्वयं में इतनी सामर्थ्यवान और शक्तिशाली है कि वह संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने में सक्षम है। बच्चों में साहित्य की मदद से हिंदी की बहुभाषिक विशेषताओं को बताते हुए हम एक दूसरे की भाषा को उचित सम्मान देने की शिक्षा दे सकते हैं। इसका प्रभाव शिक्षा के काफी संवेदनशील स्वरूप में दिखाई देगा। हिंदी की बहुभाषिका भरी विशेषता ना केवल बच्चे की अस्मिता को जन्म देती है अपितु या भारत की भाषा परिदृश्य का अद्भुत गुण प्रस्तुत करती है। यही बहुभाषिक विशेषता साहित्य के अध्ययन को करते-करते राष्ट्रीय एकता के भाव को भी प्रबल करती है।
Q. 15. हिंदी भाषा की विशेषताओं का वर्णन करें।
Ans.
हिंदी भाषा के निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-
1. हिंदी का उद्भव भाषाओं की जननी, देवभाषा संस्कृत से हुआ है जो आज भी तकनीकी क्षेत्र (कम्प्यूटर आधारित प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बौद्धिकता इत्यादि) में प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा मानी जा रही है।
2. हिंदी भाषा का व्याकरण संस्कृत से ही अनुप्राणित है। स्वाभाविक रूप से इसके व्याकरणिक नियम प्रायः अपवाद-रहित हैं, इसलिए स्पष्ट हैं और आसान हैं।
3. हिंदी की वर्णमाला दुनिया की सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है। इसमें स्वरों और व्यंजनों को अलग-अलग व्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी वर्णों को उनकी उच्चारण स्थानादि की विशेषताओं के आधार पर रखा गया है।
4. हिंदी भाषा की लिपि (देवनागरी) विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें प्रत्येक / वनि के लिए एक निश्चित लिपि चिह्न का प्रयोग होता है और एक लिपि चिह्न एक ही ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है।
5. हिंदी की वर्णमाला ध्वन्यात्मक वर्णमाला है, जिसमें हर ध्वनि के लिए लिपि चिह्न हैं। इस प्रकार यह इतनी सामर्थ्यवान भाषा है कि हम जो कुछ भी बोल सकते हैं, वह सब, हिंदी में लिख भी सकते हैं।
6. हिंदी का शब्दकोष बहुत विशाल है जहाँ एक-एक वस्तु, कार्य, भाव आदि को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द विद्यमान हैं। हिंदी के शब्दकोश में शब्दों की संख्या 2.5 लाख से भी अधिक है और यह लगातार बढ़ती ही जा रही है।
7. हिंदी भाषा की विशेषता ये भी है कि इसने अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने में कभी कोई संकोच नहीं किया। जब और जहाँ आवश्यकता हुई, हिंदी भाषा में नए शब्द शामिल होकर हिंदी के अपने हो गये और हिंदी की समृद्धि बढ़ती गई।
8. हिंदी भाषा में जो लिखा जाता है वही (उसी रूप में) पढ़ा भी जाता है। इसमें गूँगे अक्षर’ (Silent letters) नहीं होते। अतः इसके लेखन और उच्चारण में स्पष्टता है।
9. हिंदी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि इसमें निर्जीव वस्तुओं (संज्ञाओं) के लिए भी लिंग का निर्धारण होता है।
Q. 16. विद्यार्थियों की पढ़ने की क्षमता का आकलन करने के पैमानों और तरीकों का उल्लेख करें।
Ans.
विद्यार्थियों की पढ़ने की क्षमता का आकलन करने के पैमाने- यह आकलन करना कि छात्र-
1. पढ़कर समझता, समझ व्यक्त करती/करता है।
2. परिवेश में उपलब्ध लिखित और मुद्रित सामग्री को पढ़कर समझती/समझता है।
3.सूचनाओं को पढ़कर समझती/समझता है।
4.पढ़ी गई सामग्री के प्रमुख तत्व ग्रहण करती/करता है।
5.संदर्भों में आये शब्दों का अर्थ समझकर उपयोग करती/करता है।
6.पुस्तकालय या अन्य स्रोतों से किताबें लेकर पढ़ती/पढ़ता है।
7.पाठ्यपुस्तक और उससे इतर सामग्री की रचनाओं में पाई जाने वाले विविधता को पहचान कर उसकी सराहना करती/करता है।
पढ़ने की क्षमता के माध्यम से बच्चे अपने ज्ञान का विस्तार तो करते ही हैं साथ ही पढ़ी गई सामग्री के बारे में समझ भी विकसित करते हैं। पढ़ना एक ऐसा कौशल है जिसका निरंतर विकास होता रहता है। पढ़ने की कुशलता के लिए बच्चों का लिपि से परिचय, भाषा से परिचय वाक्य संरचना एवं शैली से परिचय तथा विषय से परिचय होना जरूरी है। इसके अलावा शिक्षक निम्नलिखित तरीकों से उनकी पढ़ने की कुशलता का आकलन कर सकते हैं-
1. बच्चों से पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ को पढ़वा सकते हैं जैसे कक्षा 7 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में पाठ “सोना” को पढ़ने के लिए बच्चों को कह सकते हैं। जब बच्चे पढ़ रहे हो तो उनके पढ़ने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए कि वह सही भाव से पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ने में उचित प्रवाह है एवं अर्थ की दृष्टि से वे शब्दों, वाक्य आदि पर बल दे रहे हैं आदि।
2. यदि शब्दों पर अटक रहा है एवं पुनरावृत्ति कर रहा है तो समझना चाहिए कि बच्चा अर्थ को समझ रहा है एवं उसके द्वारा शब्द का अर्थ जब तक मेल नहीं खाता तो वह पुनः शब्द को पढ़ता है, बार-बार पढ़ता है, जब तक कि वह अर्थ से मेल न खा जाएं।
3. उसे पाठ के किसी अंश को संवादों में लिखने के लिए बोल कर उसका आकलन करेंगे।
4. पाठ की किसी पंक्ति का भाव उनसे पूछ सकते हैं जैसे कि “सोना” के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करें।
5. उनसे पाठ को अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहेंगे।
6.कक्षा के बाहर भी अनेक लिखित सामग्री होती है। शिक्षक उन सामग्री को भी पठन क्षमता के आकलन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए- विज्ञापन, छपी खबर, समाचार पत्र आदि ।
7. सस्वर पढ़ना और छात्रों से ऊँची आवाज में पढ़ने को कहना एक बहुत अच्छा अभ्यास है- वे बोलकर पढ़ सकते हैं एवं शिक्षक उन्हें सुन भी सकते हैं। इससे हम छात्रों के पठन कौशल को देख सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं।
8. पठन की कुशलता का मूल्यांकन कई तरह की स्रोत सामग्रियों पर आधारित होना चाहिए और इसमें विभिन्न गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए। जैसे कहानियाँ सुनना, कविताएँ दोहराना, किताबें बनाना और शब्दों को याद कर पढ़ना आदि।
Q. 17. विद्यार्थियों की लिखित अभिव्यक्ति का आकलन करने के पैमानों और तरीकों का उल्लेख करें।
Ans.
विद्यार्थियों की लिखित अभिव्यक्ति का आकलन करने के पैमाने- यह आकलन करना कि छात्र-
1. क्यों कब, कैसे वाले प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में लिखती/लिखता है।
2. शब्दों को उपयुक्त दूरी से सीधी लाइन में लिखती/लिखता है।
3. अपरिचित शब्दों का श्रुतिलेखन करती/करता है।
4. अनुच्छेद, विवरण लिखती/लिखता है।
5. अपने सामान्य और विशेष अनुभवों को लिखती/लिखता है।
6. साहित्य की विभिन्न विधाओं का लेखन करता/करती है।
लिखित अभिव्यक्ति का आकलन करते समय हमें कई बिन्दुओं पर ध्यान रखना होगा। हिंदी भाषा में अपनी बात व विचारों को प्रकट करने के लिए एक लिखित भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का आकलन उद्देश्य परक होना चाहिए। निम्नलिखित तरीकों से हम बच्चों के भाषा के लिखित रूप के प्रयोग की क्षमता का मूल्यांकन कर सकते हैं-
1. बच्चों को एकांकी को कहानी के रूप में लिखने के लिए देना।
2.पाठ के किसी अंश को कहानी के रूप में लिखने के लिए देना।
3. बच्चों को किसी एकांकी के घटनाक्रम को अधूरा लिखकर देना फिर उन्हें कहना कि वह अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर इसे आगे बढ़ाएं और पूरा करें।
4.गद्य को पद्य व पद्य को गद्य में रूपांतरित करने को देना ।
5. दिए गए निर्देशों के आधार पर कहानी, कविता, निबंध, पत्र आदि विधाओं की रचना करने को देना।
6. किसी आँखों देखी घटना का लिखित वर्णन करने को कहना व उनके भाषा प्रयोग की बारीकियों का विश्लेषण करना ।
7.बच्चों को कल्पना के आधार पर किसी समस्या अथवा घटना के बारे में लिखने के लिए कहना । जैसे- उनसे कहना कि ऐसी घटना के बारे में लिखिए जब आपने भी ऐसे ही परिस्थिति में किसी को देखा हो।
8.बच्चों को किसी स्थिति अथवा घटना को देखकर या पढ़कर उसके बारे में संक्षेप में लिखने के लिए कहना, आदि।
Q. 18. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के उन मानकों का उल्लेख करें जिससे विद्यार्थियों की भाषाई क्षमताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है और उनकी क्षमताओं को समझा जा सकता है। इसे कक्षा प्रक्रियाओं में किस प्रकार शामिल करेंगे?
Ans.
भाषा में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जाना चाहिए-
A. मौखिक परीक्षण-
मौखिक परीक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। यहाँ अनौपचारिक का मतलब है कक्षा में पढ़ाते-पढ़ाते किसी विद्यार्थियों से कोई प्रश्न पूछ दिया या किसी शब्द का अर्थ बताने को पूछ दिया।
1.प्रश्न-उत्तर का सत्र चलाया जाए।
2.कहानी कथन का सत्र चलवाया जाए।
3.विद्यार्थी को बोल बोलकर पढ़ाया जाए। ऐसा करवाने से विद्यार्थी द्वारा किया गया शुद्ध या अशुद्ध उच्चारण शिक्षक के साथ-साथ सभी विद्यार्थियों तक पहुँचता है तथा एक दूसरे को अपनी त्रुटियों से अवगत कराते हैं।
4.विद्यार्थी द्वारा देखी या सुनी बात का वर्णन करवाया जाए।
B. लिखित परीक्षा- लिखित परीक्षा में सिर्फ प्रश्नों का उत्तर ले लेना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें निम्नलिखित युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे-
1. श्रुतलेख- इसमें एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा व्यक्ति सुनकर लिखता है। ऐसा करने से हम विद्यार्थी के श्रवण तथा लेखन क्षमता का आकलन कर लेते हैं।
2. आपूर्ति परीक्षण- जिसे हम अंग्रेजी में क्लोज टेस्ट कहते हैं इसमें हम किसी कहानी या निबंध से कोई अनुच्छेद ले सकते हैं। फिर उन अनुच्छेदों में से कुछ-कुछ शब्द निकालकर विद्यार्थियों के सामने रखते है फिर विद्यार्थियों को भरने के लिए कहा जाता है कि उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऐसा करने से हम विद्यार्थी के व्याकरण क्षमता, शब्द भंडार, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन कर लेते हैं।
3. कहानी का अपनी मातृभाषा में पुनर्लेखन – इसमें हम विद्यार्थी द्वारा पहले से पढ़ा गया पाठ को हम उनकी मातृभाषा में पुनर्लेखन को कहते हैं यहाँ हम उनकी लेखन क्षमता की जाँच कर लेते हैं। साथ ही साथ हम एक भाषा से दूसरी भाषा में उनके द्वारा अनुवाद करने का क्षमता का भी आकलन कर लेते हैं।
4. कहानी का शीर्षक लिखना- इसमें हम विद्यार्थी को किसी निबंध, उपन्यास तथा अनुच्छेद का शीर्षक लिखने को कह कर हम उनके पठन की समझ क्षमता का आकलन कर लेते हैं।
5. कहानी से प्रश्न बनाना- ऐसा करने से हम विद्यार्थी के प्रश्न बनाने की क्षमता का आकलन कर लेते हैं।
6. नाटक का मंचन एवं संवाद लेखन- ऐसा करने से हम पाते हैं कि विद्यार्थी को कहाँ तक समझ आया कि वह किस अभिनयकर्ता को किस समय पर क्या प्रस्तुत करना है नाटक का मंच कैसा हो? आदि के बारे में आकलन कर लेते हैं।
7. कविता की व्याख्या या उसका भावार्थ लेखन, आदि।
अतः मूल्यांकन करते समय परीक्षण विद्यार्थी की भाषा, ज्ञान एवं क्षमता का आकलन एवं मूल्यांकन करने वाला होना चाहिए ना कि उनकी स्मरण शक्ति का। दूसरी बात आकलन करते समय हमें विद्यार्थी के मात्र कमजोर पक्षों को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि उनकी कारण को भी ढूंढना चाहिए जिनके कारण विद्यार्थी की अपेक्षित पहलू कमजोर है। मूल्यांकन इन मानकों पर करने पर विद्यार्थियों की भाषाई क्षमताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है।
Q. 19. यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा बोलते और लिखते समय अनेक प्रकार की त्रुटियां करता है तो उसे किस प्रकार फीडबैक दी जानी चाहिए और क्यों?
Ans.
फीडबैक वह जानकारी है, जो हम किसी बच्चे को इस बारे में देते हैं कि एक दिये गये लक्ष्य या अपेक्षित परिणाम के सापेक्ष उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है। प्रभावी ढंग से दिए गए फीडबैक से बच्चों को:
1. क्या हुआ है इसकी जानकारी मिलती है।
2. कोई क्रिया या कार्य कितनी अच्छी तरह किया गया इसका मूल्यांकन पता लगता है।
3. इस बारे में मार्गदर्शन मिलता है कि उनका प्रदर्शन किस प्रकार सुधारा जा सकता है।
4. जब हम प्रत्येक छात्र को फीडबैक देते हैं, तो इससे उन्हें यह जानने में मदद मलनी चाहिए कि :
5. वे वास्तव में क्या कर सकते हैं।
6.वे अभी क्या नहीं कर सके।
7.दूसरों की तुलना में उनका काम कैसा है।
8.वे इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं।
छात्रों के लेखन पर फीडबैक देते समय एक बार में केवल एक या दो पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित करें। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि वे अत्यधिक सुधारों के कारण निराश नहीं होंगे या अत्यधिक फीडबैक के कारण परेशान नहीं होंगे। पहले लेखन या बोलने पर फीडबैक देते समय छात्रों के संघटन के प्रयासों की तारीफ करना महत्वपूर्ण है। क्या छात्र के पास कहानी के लिए कोई बढ़िया विचार था? क्या छात्र ने रोचक संवाद लिखे थे? क्या छात्र ने रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को लिखना याद रखा था? क्या छात्र ने सही-साथ हिंदी में लिखने व बोलने का अच्छा प्रयास किया था?
भले ही आपकी कक्षा बड़ी हो, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम हर एक छात्र को अलग-अलग फीडबैक दें। फीडबैक देने या टिप्पणी करने का कोई एक तरीका नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि फीडबैक से लेखनया बोलने के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बने। उदाहरण के लिए-
मैंने छात्रों को पाठ्यपुस्तक से डिक्टेशन दिया। जब छात्रों ने अपना काम मुझे सौंपा, तो मैंने इसकी समीक्षा की और देखा कि दस वर्ष की एक लड़की ने ‘पेंसिल’ और ‘कर्तव्य’ शब्दों की स्पेलिंग इस प्रकार लिखी थी: पेनसिल, करतव्य ।
मेरी पहली प्रतिक्रिया इन गलतियों को सुधारने की थी। लेकिन मैं देख सकता था कि वह लड़की हिंदी शब्दों की शुरूआती ध्वनियों को जानती थी। वह ध्वनियों के आधार पर शब्द लिख सकती थी। मैं देख सकता था कि वह हिंदी के अपने मौखिक ज्ञान का उपयोग करके स्पेलिंग लिखने का अच्छा प्रयास कर रही थी, हालांकि लेखन में यह हमेशा सही नहीं था।
मैंने उसके प्रयासों की तारीफ की। लेकिन साथ ही उसे कहा कि वह अपने लिखे को ध्यान से पढ़े और एक शब्दकोश का उपयोग करके अपने शब्दों के मात्राओं की जाँच करे। मैंने उसे ज्यादा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि वह हिन्दी में जितना ज्यादा पढ़ेगी, उसकी शब्दों में मात्राओं की समझ भी उतनी ही बेहतर बनेगी।
फीडबैक चाहे मौखिक हो, या छात्रों की वर्कबुक में लिखकर दिया जाए, यदि इसके लिए निम्नलिखित दिशार्निदेशों का पालन किया जाता है, तो यह अधिक प्रभावी बन जाता है।
1. प्रशंसा और सकारात्मक भाषा का उपयोग करना— जब हमारी प्रशंसा की जाती है और हमें प्रोत्साहित किया जाता है तो आमतौर पर हम उस समय के मुकाबले बेहतर महसूस करते हैं, जब हमारी आलोचना की जाती है या हमारी गलती सुधारी जाती है। सुदृढ़ीकरण और सकारात्मक भाषा समूची कक्षा और सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायक होती है।
2. संकेत देने के साथ-साथ सुधार का उपयोग करना— शिक्षक जब बच्चों के साथ जो बातचीत करते हैं, उससे उन्हें सीखने में मदद मिलती है। यदि हम उन्हें सिर्फ यह बताते है कि कोई उत्तर गलत है और बात वहीं खत्म कर देते हैं, तो सोचने और कोशिश करने में उनकी मदद करने का मौका गँवा देंगे। यदि हम बच्चों को कोई संकेत देते हैं और उनसे आगे भी प्रश्न पूछते हैं, तो इससे हम उन्हें ज्यादा गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही उन्हें उत्तर ढूँढ़ने तथा खुद के अधिगम की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी प्रेरित करते हैं।
Q. 20. शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के उद्देश्य और विधियों की तारतम्यता को समझना क्यों आवश्यक है?
अथवां,
कौन-से उद्देश्य के लिए कौन-सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त होगी इनके बीच के रचनात्मक संबंध व तारतम्यता को समझना एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है?
Ans.
प्रत्येक विषय में प्रदत्त पाठ के शिक्षण अधिगम में सरलता सूस्पष्टता एवं बोधगम्यता लाने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। परंतु यहाँ आवश्यकता इस बात की होती है कि कौन-से शिक्षण उद्देश्य के लिए कौन-सी शिक्षण सहायक सामग्री का चयन पाठ शिक्षक करें कि जिससे पाठ की रोचकता, रचनात्मकता के साथ सीखने वाले शिक्षार्थियों की जिज्ञासा और तारतम्यता बनी रहे। इस नितांत आवश्यक जानकारी का होना एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, इसे हम निम्न उदाहरणों के माध्यम से सरलतापूर्वक समझ सकते हैं।
माना कि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में ग्लोब और मानचित्र दोनों उपलब्ध हैं। अब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा इनका उपयोग भौगोलिक आकृतियों, राजनीतिक सीमाओं, पड़ोसी देशों की स्थितियां स्पष्ट करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा। यहाँ दूसरी स्थिति में एक भाषा शिक्षक (हिंदी शिक्षक) अपनी कक्षा में इन्हीं शिक्षण सहायक सामग्रियों को भाषाई विविधता, क्षेत्रीय भाषा के व्यावहारिक क्षेत्रों, अन्य भाषाओं के क्षेत्रों आदि को प्रदर्शन करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है, परंतु भाषा के शिक्षक के लिए इस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सरल नहीं रहेगा और भाषाई विविधता के क्षेत्र बच्चों को मानचित्र के माध्यम से दिखाने पर बच्चे उससे व्यवहारिक तौर पर जुड़ नहीं पाएंगे और उनकी जिज्ञासा कम हो जाएगी। इसकी जगह पर कुछ व्यवहारिक स्थितियों का उपयोग कर शिक्षार्थियों की जिज्ञासा एवं तारतम्यता को बनाए रखा जा सकता है।
विद्यालय के प्रत्येक कक्षा-कक्ष में श्यामपट्ट की उपस्थिति विद्यालय और शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता है। श्यामपट्ट का भी उपयोग शिक्षण-अधिगम में शिक्षकों द्वारा मुख्य रूप से शिक्षण सहायक सामग्री के उपकरण के तौर पर किया जाता है। गणित के
शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट के एक भाग को गणितीय सक्रियाएं को हल करते समय रफ कार्य हेतु किया जाता है तो वहीं दूसरी ओर भाषा शिक्षकों द्वारा उसी भाग का उपयोग कठिन शब्द संधि-विच्छेद, लिंग निर्णय आदि के रूप में पाठ पढ़ाते समय किया जा सकता है। उपरोक्त उदाहरणों पर ध्यान पूर्वक दृष्टिपात करने से हमें यह पता चलता है कि एक विशेष प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग मात्र एक ही पाठ्य विषय में नहीं किया जा सकता है। उसे उसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता के अनुरूप अन्य शिक्षक भी अपने पाठ के विषय वस्तु में छात्रों की समझ और अधिगम को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करने हेतु उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ बस आवश्यकता इस बात की है कि अमुक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाए गए शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण के विषय वस्तु के बीच किस प्रकार की रचनात्मक संबंध एवं तारतम्यता स्थापित हो रही है। यही समझ शिक्षक को अपनी कक्षा में प्रभावी, शिक्षण को अधिगम पूर्व और शिक्षार्थियों के ज्ञान को चिरस्थाई बनाने में सहायता करती है।
Q. 21. साक्षात्कार लेने और देने के समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
Ans.
साक्षात्कार लेते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए-
1. शब्दों का चयन सोच समझकर हो। कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल ना हो जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे या उसे आपत्ति हो ।
2. लंबे-लंबे वाक्यों के स्थान पर संक्षिप्त और सटीक वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए।
3.साक्षात्कार की शुरूआत अभिवादन से करे एवं साक्षात्कार देने वाले को सहज करें।
4. चिन का साक्षात्कार लेना है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उनसे कोई अटपटा सवाल नहीं पूछना चाहिए जिससे उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है।
5. जिन का साक्षात्कार लिया गया है उनकी बात पूरी होने तक उनको सुनना चाहिए उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न करना चाहिए।
6.साक्षात्कार लेते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे या कोई आपत्ति हो ।
साक्षात्कार देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए-
1.आत्मविश्वास बनाए रखें।
2.शिष्टाचार का ध्यान रखें।
3.अपनी वाणी को मधुर व संयम बनाए रखें।
4.प्रश्नों के समझकर उत्तर दें।
5.प्रश्न का उत्तर नहीं आने की स्थिति में गलत उत्तर ना दें बल्कि अपनी असमर्थता जाहिर कर दें।
6.जिस विषय का साक्षात्कार होना हो
7. जरूरत से ज्यादा बोलने से बचें।
8.उस विषय के बारे में पूरी जानकारी रखें।
अपने शब्दों और वाक्यों का चयन ध्यानपूर्वक करें। अत्यधिक विस्तार के फेर में
विषय से भटकाव हो सकता है।
Q. 22. विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी भाषा के स्वरूप का वर्णन करें।
Ans. सूचना संचार प्रणाली किसी भी व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दूसरी तरफ समाज के दर्पण के रूप में साहित्य भी तो संचार माध्यम ही है जो सूचनाओं का व्यापक संप्रेषण करता है। साहित्य की तुलना में संचार माध्यमों का ताना-बाना अधिक जटिल और व्यापक है क्यों कि वे तुरंत और दूरगामी असर करते हैं। भूमंडलीकरण ने उन्हें अनेक चैनल ही उपलब्ध नहीं कराए हैं, इंटरनेट और वेबसाइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीयता के नए अस्त्र-शस्त्र भी मुहैया कराए हैं। परिणामस्वरूप संचार माध्यमों की त्वरा के अनुरूप भाषा में भी नए शब्दों, वाक्यों, अभिव्यक्तियों और वाक्य संयोजन की विधियों का समावेश हुआ है।
इस सबसे हिंदी भाषा के सामर्थ्य में वृद्धि हुई है। संचार माध्यम यदि आज के आदमी को पूरी दुनिया से जोड़ते हैं तो वे ऐसा भाषा के द्वारा ही करते हैं। अतः संचार माध्यम की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने पर हिंदी समस्त ज्ञान-विज्ञान और आधुनिक विषयों से सहज ही जुड़ गई है। वह अदालतनुमा कार्यक्रमों के रूप में सरकार और प्रशासन से प्रश्न पूछती है, विश्व जनमत का निर्माण करने के लिए बुद्धिजीवियों और जनता के विचारों के प्रकटीकरण और प्रसारण का आधार बनती है, सच्चाई का बयान करके समाज को अफवाहों से बचाती है, विकास योजनाओं के संबंध में जन शिक्षण का दायित्व निभाती है, घटनाचक्र और समाचारों का गहन विश्लेषण करती है तथा वस्तु की प्रकृति के अनुकूल विज्ञापन की रचना करके उपभोक्ता को उसकी अपनी भाषा में बाजार से चुनाव की सुविधा मुहैया कराती है। अतः कहा जा सकता है कि वैश्विक संदर्भ में हिंदी की वास्तविक शक्ति को उभारने में संचार माध्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
एक तरफ साहित्य लेखन की भाषा आज भी संस्कृतनिष्ठ बनी हुई है तो दूसरी तरफ संचार माध्यम की भाषा ने जनभाषा का रूप धारण करके व्यापक जन स्वीकृति प्राप्त की है। समाचार विश्लेषण तक में कोडमिश्रित हिंदी का प्रयोग इसका प्रमुख उदाहरण है। इसी प्रकार पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, पारिवारिक, जासूसी, वैज्ञानिक और हास्यप्रधान अनेक प्रकार के धारावाहिकों का प्रदर्शन विभिन्न चौनलों पर जिस हिंदी में किया जा रहा है वह एकरूपी और एकरस नहीं है बल्कि विषय के अनुरूप उसमें अनेक प्रकार के व्यावहारिक भाषा रूपों या कोडों का मिश्रण उसे सहज जनस्वीकृत स्वरूप प्रदान कर रहा है। एक वाक्य में कहा जा सकता है कि संचार माध्यमों के कारण हिंदी भाषा बड़ी तेजी से तत्समता से सरलीकरण की ओर जा रही है। इससे उसे अखिल भारतीय ही नहीं, वैश्विक स्वीकृति प्राप्त हो रही है।
हिंदी के इस रूप विस्तार के मूल में यह तथ्य निहित है कि गतिशीलता हिंदी का बुनियादी चरित्र है और हिन्दी अपनी लचीली प्रकृति के कारण स्वयं को सामाजिक आवश्यकताओं के लिए आसानी से बदल लेती है। इसी कारण हिंदी के अनेक ऐसे क्षेत्रीय रूप विकसित हो गए हैं जिन पर उन क्षेत्रों की भाषा का प्रभाव साफ-साफ दिखाई देता है। ऐसे अवसरों पर हिंदी व्याकरण और संरचना के प्रति अतिरिक्त सचेत नहीं रहती बल्कि पूरी सदिच्छा और उदारता के साथ इस प्रभाव को आत्मसात कर लेती है। यही प्रवृत्ति हिंदी के निरंतर विकास का आधार है और जब तक यह प्रवृत्ति है तब तक हिंदी का विकास रुक नहीं सकता।
Q. 23. कविता या नाटक आदि का उपयोग करकं बच्चों में कल्पनाशीलता के विकास के लिए रणनीतियों का निर्माण एवं उपयोग किस प्रकार करेंगे?
Ans.
प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बच्चे आपस में कविता को गुजगुनाते रहते हैं या किसी चरित्र विशेष / पात्र विशेष का प्रदर्शन करते हुए मिलते हैं। ऐसी स्थिति बच्चों के कल्पनाशीलता के कारण प्रदर्शित होती है। कविता अथवा नाटक आदि का उपयोग करके बच्चों में कल्पनाशीलता के विकास के लिए हम निम्नलिखित प्रकार की रणनीतियों का निर्माण एवं उनका उपयोग कर सकते हैं-
कविता शिक्षण के समय-
A. प्रस्तावना—प्रस्तावना कविता शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। यह बच्चों की कल्पना क्षमता पर आधारित पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए इसकी प्रस्तुति निम्न प्रकारों से की जा सकती है-
1. कविता का परिचय देकर,
2. पार्टी कविता की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करके,
3. कविता की कुछ पंक्तियों को प्रस्तुत करके,
4. भाव के अनुसार उपयोगी वातावरण निर्माण करके,
B. उद्देश्य कथन— उद्देश्य कथन कविता या कवि की मूल भावना को स्पष्ट करता
C. उत्तम पाठ- कविता के उत्तम पाठ में भाव, गति, लय, बलाघात, छंद, उच्चारण आदि पर विशेष बल दिया जाता है। इसे छात्रों में शब्दों के प्रति स्पष्ट समाज स्थापित होती है।
D. केंद्रीय भाव की परीक्षा- छात्रों की कल्पनाशीलता एंव समाज की परीक्षा लेने हेतु केंद्रीय भाव से एक-दो प्रश्नों को पूछना जिसे स्पष्ट हो सके कि छात्रों का अधिगम कहाँ तक सुनिश्चित हो पाया।
E. कठिन शब्दों का शब्दार्थ बतलाना- कविता के रस को शब्दों के कारण बा न पहुँचे। इस बात को ध्यान में रखकर कठिन शब्दों के अर्थ को सीधा और स्पष्ट रूप से बता कर छात्रों की कल्पना को विकसित किया जा सकता है।
F. सौंदर्य बोध- ध्वनि सौंदर्य, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, शैली सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य, आदि कविता के सौंदर्य तत्व होते हैं। कविता में बसे सौंदर्य बोध से बच्चों का परिचय करवा कर हम छात्रों की कल्पनाशीलता को विकसित करके कविता का रसास्वादन भी करा सकते हैं।
नाटक शिक्षण के समय – नाटक का स्थान साहित्य की सभी विधाओं में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें अभिनय के साथ-साथ गायन, वादन, नृत्य, संवाद आदि विशेष रूप में होते हैं। भारतीय साहित्य में नाटक के महत्व को स्पष्ट करने हेतु ‘काव्येशु नाटक रम्या’ वाक्य की काफी है। नाटक कहानी की तरह किसी घटना का रसात्मक और संवादात्मक प्रस्तुति लिए हुए रहता है। नाटक शिक्षण को हम अपने कक्षा-कक्ष में छात्रों की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, प्रदर्शन कला आदि के साथ-साथ आत्म संयम, संतुलन, सहयोगी पर निर्भरता जैसे गुणों के विकास के लिए करते हैं।
नाटक शिक्षण की कक्षा अभिनय विधि का प्रयोग करके आवश्यक पाठ्यवस्तु के भागों पर चर्चा, भाषा-शैली, पात्रों का चरित्र-चित्रण, जीवन मूल्यों की स्थापना आदि को सूक्ष्म रूप से विश्लेषित कर सकते हैं। ऐसा करने से छात्रों में एकाग्रता, शब्दों को अवसरों के अनुकूल उपयोग करने, उचित हाव-भाव, मुद्रा, अनुदान बलाघात आदि के साथ शुद्धता पूर्ण उच्चारण की क्षमता का विकास होता है। ज्वलंत सामाजिक राजनीतिक आर्थिक धार्मिक विषयों को आकर्षक और रोचकता पूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने जैसी प्रदर्शन कला का विकास होता है। नाटक छात्रों में स्वमूल्यांकन, निरीक्षण, कल्पनाशक्ति, रचनात्मकता, बोध और विवेचन कर पाने की क्षमता का भी विकास कर सकने में सक्षम होता है।
Q. 24. शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? शिक्षण में इनके उपयोग के उद्देश्यों और उपयोग करने की विधियों की चर्चा करें।
Ans.
एक कक्षा-कक्ष में प्रदान किए जा रहे अधिगम में सहायता के लिए उपयोग में लाए गए वैसी सारी सामग्री जिससे अधिगम सरल, स्पष्ट, रोचक, प्रभावी और दीर्घकालीन बन सके, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा में हो रहे नित्य नवाचार प्रयोगों के कारण शिक्षण अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता और उसके प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि इन सहायक सामग्री की उपलब्धता एवं इनके उपयोगों को शिक्षक अपनी कक्षा में किस प्रकार करते हैं।
शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धता-
1. मात्र शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने वाले सामग्री का चयन किया जाए। जैसे यदि हम छात्रों में कल्पना के विस्तार से जुड़ी कोई गतिविधि कराना चाहते हैं तो वैसे शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करना चाहिए जो छात्रों के कल्पनाओं को विस्तार करने का अवसर दे सकें।
2. सामग्री ऐसी हो कि जिनका उपयोग छात्रों द्वारा मीना सावधानी बरतें, खुलकर और पूरी तरह किया जा सके।
3. सामग्री का चयन विभिन्न उपयोगों के आधार पर किया जाए ना कि मात्र एक उपयोग के आधार पर।
4. कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या और आवश्यकतानुसार सामग्री का चुनाव करना चाहिए।
5. सामग्री की उपलब्धता छात्रों के आस-पास के बाजार को ध्यान में रखकर करें इसे तकनीकि खराबी या कुछ कमी रहने पर सामग्री को वापस कर सकें। साथ ही यह भी ध्यान दें की सामग्री अधिक महंगी नहीं हो।
6. शिक्षक से आपसी विमर्श करके अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार स्पष्ट तौर पर प्राथमिकता वाले सामग्री को ही चुने, ना कि अनावश्यक सामग्री को ।
शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता-
–
1. सामग्री की उपलब्धता ससमय कराने पर छात्रों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, इसे उनकी रुचि और निरंतरता भी प्रभावित होने से बचती है।
2. छात्रों को ऐसा प्रतीत हो कि यह सारी सामग्री मात्र देखने की वस्तु ना होकर उनके लिए सीखने में सहायक सिद्ध होने वाली है।
3. यदि अलग-अलग सामग्रियों को उपयोग करना पड़ रहा हो तब उनके उपयोग के लिए एक सुनिश्चित योजना तैयार करनी चाहिए ।
4. सामग्री को वियोग में लाने के क्रम में वे टूट-फूट सकते हैं, नष्ट भी हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट नियम और निर्देश के साथ उपयुक्त स्थान को भी चयन करना चाहिए।
5. शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग में जैसे- लेने-देने, रखने प्रदर्शन करने आदि की प्रक्रिया में छात्रों को जिम्मेदार और भागीदार बनाना चाहिए।
6. इनके उपयोग में छात्रों की भूमिका सक्रिय रूप से होनी चाहिए, इससे उनकी जिज्ञासाओं और उत्कंठाओं का अंत होगा और अधिगम अस्पष्ट होगा शिक्षक का कार्य उचित मार्गदर्शक और नियंत्रक के रूप में रहे।
शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य-
हिंदी शिक्षण की कक्षाओं में चार्ट, चित्र, पोस्टर, मानचित्र, रेखाचित्र, खादी बोर्ड या फ्लैनल बोर्ड, श्यामपट्ट आदि को सहज रूप से शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इनकी सहायता से साहित्य का काल विभाजन, व्याकरण के शब्द भेद प्रक्रिया लिंग निर्णय आदि के साथ-साथ हिंदी भाषा के व्यवहरित क्षेत्र विशेष अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के चित्र आदि को प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। दूसरी और परिभाषाएं शब्द वर्तनी विराम चिह्नों के प्रयोगों के अलावा नवीन विचारों और अन्वेषणों को भी स्पष्ट स्वरूप दे सकते हैं। आधुनिक विज्ञान के नए-नए तकनीकी उपकरणों में टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र, कम्प्यूटर, दूरदर्शन, इंटरनेट, प्रोजेक्टर रेडियो आदि का भी उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में किया जा रहा है। इन सारे दृश्य श्रव्य उपकरणों की सहायता से शिक्षण में दीर्घकालिक और चिरस्थाई अधिगम के प्रभावों को देखने को मिलता है। इस प्रकार शिक्षण सहायक सामग्री छात्रों में पाठ के प्रति जागृति, अभिव्यक्ति, तारतम्यता के अतिरिक्त विषय वस्तु की स्पष्टता के उद्देश्यों की पूर्ति को निरंतर बनाए रखने में सक्षम होता है।
Q. 25. व्यवहारवादी तथा रचनात्मक उपागम की विभिन्न विधियाँ तथा रणनीतियाँ कौन-कौन सी हैं? वर्णन करें।
अथवा,
व्यवहारवादी तथा रचनात्मक उपागम की विभिन्न विधियाँ कौन-कौन सी हैं? इन्हें सिखाने की विभिन्न रणनीतियों की भी चर्चा करें।
Ans.
व्यवहारवादी उपागम की विभिन्न विधियाँ तथा रणनीतियाँ-
1. अभिक्रमित अधिगम —
यह शिक्षण-अधिगम का वह निकाय है जिसमें पूर्ण निर्धारित पाठ्यवस्तु को छोटे-छोटे और अलग-अलग चरणों में बाँट दिया जाता है। इन चरणों को ध्यानपूर्वक ऐसे तार्किक श्रेणियों में संगठित किया जाता है जिन्हें विद्यार्थी शीघ्रता से सीख सकें। प्रत्येक चरण अपने से पूर्व चरण के आधार पर निर्मित होता है और प्रत्येक चरण के उपरान्त प्रबलन दिया जाता है। प्रगति जाँच का प्रावधान इस प्रकार होता है कि यदि शिक्षार्थी की अनुक्रिया ठीक होगी तो वह आगे बढ़ पाएगा, यदि नहीं तो वह अगले चरण में प्रवेश मात्र उसी समय कर पाएगा जब वह सही उत्तर ढूँढ़ लें।
2. शिक्षण मशीन-
अधिगम के व्यवहारगत उपागम का यह दूसरा अनुप्रयोग है। शिक्षण मशीनों में विषयवस्तु को आवश्यक रूप से पूर्व निर्धारित अनुक्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को प्रस्तुत विषयवस्तु के प्रति अनुक्रिया करने दी जाती है और उसके तुरन्त पश्चात् उन्हें पुनर्निवेशन (प्रतिपुष्टि) दिया जाता है। शिक्षण मशीनें स्वचालित उपकरण होती हैं जो किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न अथवा उद्धीपन देते हैं और फिर अनुक्रिया करने का साधन प्रदान करते हैं। तत्पश्चात् उसे उसको उत्तर को सही या गलत होना बताती हैं। ग्रह कार्य वे अनुक्रिया के तुरंत पश्चात् करती हैं।
रचनात्मक या सृजनात्मक उपागम की विभिन्न तथा रणनीतियां-
1. अभिसारी (कन्वर्जेन्ट ) अभिसारी विधि ऐसी विधि है जिसमें ऐसी गतिविधियों की ओर निर्देशित किया जाता है जिससे सीधे उत्तर प्राप्त हो। जबकि अपसारी विधि में अधिक से अधिक विचारों और उनकी विभिन्नताओं पर जोर दिया जाता है। अपसारी विधि से शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी सूझबूझ से चिन्तन कर उत्तर या समाधान तक जाए। इस तरह विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो उनके मस्तिष्क में मौलिक विचार आते हैं। यही विचार उन्हें सृजनात्मकता की ओर अग्रसर करते हैं।
2. अपसारी (डाइवर्जेन्ट) मौलिकता डाइवर्जेन्ट चिन्तन से ही उत्पन्न होती है। विद्यार्थी जब डाइवरजेन्ट चिन्तन से समस्या के समाधान की तरफ आगे जाते हैं तो समस्या को नए नजरिए से देखने की कोशिश में मौलिकता की तरफ बढ़ते हैं। डाइवरजेन्ट चिन्तन से विचारों में मौलिकता आती है जो कि बहु-सुझावों या विचारों का ही परिणाम होती है जबकि अभिसारी विधि में स्मृति आधारित प्रश्नों की बहुलता होती है। यहाँ विविधता पर ध्यान नहीं दिया जाता परंतु इस तरह से भी विद्यार्थियों को विचार करने के लिए बिन्दु मिल जाते है। हम यह भी कह सकते है कि कनवर्जेन्ट और डाइवर्जेन्ट चिन्तन एक-दूसरे के पूरक हैं।
Q.26. बच्चों को विभिन्न स्थितियों में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए किस प्रकार तैयार करेंगे?
Ans.
प्रत्येक बच्चा जन्मजात भाषा क्षमता के साथ जन्म लेता है। प्रत्येक भाषा विशेष प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में अर्जित की जाती है। बच्चा स्वतः ही यह सीखता है कि क्या कहना है, कहाँ कहना है, किससे कहना है और यह विभिन्न आयु वर्ग के द्वारा विभिन्न संदर्भ में उसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। बच्चों को दोहराने और अनुकरण करने के लिए दबाव डालने पर उन्हें प्रभावशाली तरीके से कहने के लिए सिखाया नहीं जा सकता है। भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को विभिन्न प्रकार की स्थितियों में अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रयासों को किया जा सकता है-
1. व्याकरणिक ज्ञान प्रदान कर- व्याकरण का उचित और समृद्ध ज्ञान बच्चों के वाचन कला को अलंकृत और परिमार्जित करता है। यह बच्चों को मात्राओं के सही प्रयोग, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण आदि जैसे तत्वों की जानकारी देता है। व्याकरणिक ज्ञान साहित्य की समझ को भी दृढ़ता प्रदान करता है जिससे सामाजिक जीवन की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से बच्चे का परिचय हो जाता है।
2. भाषायी शुद्धता हेतु उचित अवसर देकर— बच्चों में भाषा वाचन कुशलता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हें भाषा की शुद्धता हेतु उचित अवसर देने की आवश्यकता है। जैसे- दुकानदार और ग्राहक, शिक्षक और छात्र, डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित होने वाले प्रश्नों के द्वारा बच्चों को विभिन्न प्रकार की स्थितियों में प्रभावी ढंग से बात कहने के लिए तैयार किया जा सकता है।
3. शब्दों के उचित अनुतान या बलाघात की जानकारी देकर— वाचन के समय ध्वनि में जो उतार-चढ़ाव होता है। वह अनुतान कहलाता है। इसे बलाघात भी कहते हैं। यह प्रायः वाक्य स्तर पर होता है, किंतु कभी-कभी शब्द के स्तर पर भी हो सकता है। जैसे- “ठीक है” का प्रयोग अनुतान के विभिन्न स्तर पर स्वीकारोक्ति, प्रश्न पूछने, विस्मय, स्वीकृति आदि के संदर्भ में अलग-अलग भाव व्यक्त करते हैं। इस कारण बच्चों के वाचन को प्रभावी स्वरूप देने के लिए शब्दों की उचित अनुदान या बालाघाट की संज्ञा सही जानकारी का होना अनिवार्य आवश्यकता है।
4. शब्द अनुरूप भाव-भंगिमा— अपनी बातों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए शब्दों के अनुरूप चेहरे की भाव और भंगिमा होनी चाहिए। कहाँ हास्य हो, कहाँ गंभीरता हो, कहाँ पर चंचलता हो आदि की जानकारी होना बच्चों के लिए अति आवश्यक है। शब्दानुकूल मुखाभिव्यक्ति हमारी बोली को अत्यंत प्रभावी बनाने का काम करती है।
5. आत्मविश्वास भरकर— बच्चे गलत हो जाने के भय से प्रयास करने में संकोच करते हैं। यह स्थिति उनको मानसिक स्तर पर संकुचित और वाचन में प्रवाह को रोकती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाएं और उन्हें अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कहने के उचित अवसर प्रदान करें। ऐसा करने से बच्चे प्रेरित होंगे और प्रयास करेंगे। यह निरंतर प्रयास ही उन्हें आगे भविष्य में सफलता की ओर अग्रसर करेगा।
6. पुनर्बलन करके संकोची एवं प्रयास नहीं करने वाले बच्चों के लिए पुनर्बलन कर प्रभावी उपचार होता है। भाषा शिक्षक अपने छात्रों को “ठीक है, प्रयास करें, बहुत अच्छा, एकदम ठीक” आदि जैसे शब्दों से पुनर्बलित करके उनमें ऊर्जा और उत्साह का नवीन संचार कर देते हैं। यह पुनर्बलन छात्रों को आशानुकूल प्रतिफल देने की ओर प्रेरित करता है।
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों को विभिन्न स्थितियों में अपनी बात प्रभावी ढंग से कहने के लिए उचित अवसर, व्याकरण की अच्छी समझ, भाषा की शुद्धता का ज्ञान, शब्दों के रूप मुखाभिव्यक्ति, आत्मविश्वास और अभिप्रेरणा, पुनर्बलन के साथ-साथ निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। उपरोक्त प्रयासों की मदद से अपनी बात को कहने के लिए तैयार कर सकते हैं।
Q. 27. किसी स्थिति का एक संक्षिप्त विवरण कैसे तैयार करेंगे?
Ans.
संक्षेपण अथवा सार-लेखन (अंग्रेजी Precis) का आशय है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना। किसी बड़े पाठ (निबन्ध, लेख, शोध प्रबन्ध आदि) में मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुत्तर आकार में प्रस्तुत करना संक्षेपण (critical precis writing) कहलाता है। इसकी संरचना भी निबन्ध जैसी ही होती है। सार लेखन की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता, शिक्षा आदि कई क्षेत्रों में पड़ती है।
संक्षेपण की प्रक्रिया-
1. संक्षेपण करते समय सबसे पहले मूल अनुच्छेद या विषय-वस्तु को एकाधिक बार ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। इससे मूल अनुच्छेद का भावार्थ समझ में आ जाएगा।
2. मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों, बातों तथा विचारों को रेखांकित कर लिया जाना चाहिए। रेखांकन करते समय मूल विषय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अंश नहीं छूटना चाहिए।
3. इसके बाद मूल में व्यक्त किए गए विचारों, भावों तथा तथ्यों को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए।
4. मूल अनुच्छेद का एक तिहाई में संक्षेपण करना चाहिए। इसमें संक्षेपक को अपनी ओर से कोई भी तर्क-वितर्क करने तथा किसी अतिरिक्त अंश को जोड़ने की अनुमति या छूट नहीं होती।
5. संक्षेपण तैयार करते समय मूल अनुच्छेद में वर्णित या उल्लिखित कहावतें, मुहावरे, वाक् प्रचार तथा अलंकार आदि को हटा देना चाहिए।
6. संक्षेपण तैयार करने के बाद उसके लिए सुयोग्य शीर्षक का चयन किया जाना चाहिए।
Q. 28. उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के क्या उद्देश्य है? इस स्तर पर हिंदी शिक्षण का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए?
Ans.
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य निम्नांकित हैं-
1. हिंदी को शुद्ध रूप में लिखना और बोल सकना।
2. अपने विचारों को शुद्ध, सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण भाषा में व्यक्त कर पाना भी हिंदी शिक्षण के उद्देश्य है।
3. दूसरे व्यक्तियों के लिखित और मौखिक विचारों, अभिव्यक्तियों, भावों आदि को समझने की योग्यता विस्तार करना।
4. छात्रों को उचित हाव-भाव और आरोहो एवं अवरोहों के साथ भावपूर्ण वाचन की कला बताना भी हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है।
5. हिंदी शिक्षण के द्वारा छात्रों के ज्ञान, विवेक, चरित्र नैतिकता आदि का विकास कराकर एक । आदर्श नागरिक का निर्माण कराना।
6. छात्रों की सृजनात्मकता तथा रचनात्मकता का विकास करना पुस्तकों में समाहित ज्ञान को अर्जन करना एवं स्वाध्याय की क्षमता को उत्पन्न करना हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है।
7. छात्रों को सद् साहित्य की रचना योग्य बनाना तथा मानव जीवन की विविध परिस्थितियों का अध्ययन करा कर उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करना ।
8. साहित्य से परिचय करवा कर अपने गौरवशाली सभ्यता व संस्कृति के संरक्षण एवं उसके प्रचार-प्रसार हेतु तैयार करना ।
9. विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय आदि की भावना से प्रेरित कराना।
इस प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य मात्र शैक्षिक/ औपचारिक नहीं होकर पूरी तरह व्यावहारिक और अनौपचारिक शिक्षक भी देना है। यह न केवल छात्र की भाषागत कुशलताओं को विकसित करती है वरन् छात्रों में सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, मानवीय गुणों को धारण करने की प्रेरणा भी देती है। छात्रों की कल्पनाशीलता, चिंतन क्षमता, सृजनात्मकता, तार्किकता और रचनात्मकता आदि को भी गति प्रदान करती है। इस कारण छात्रों में लेखन, वाचन, श्रवण, पठन आदि को भी गति प्रदान करती है। इस कारण छात्रों में लेखन वाचन श्रवण पठन आदि की कुशलताओं में भी प्रवीणता आती है।
Q. 29. लिखी हुई और कही गई बातों को समझने के क्या तरीके हैं?
अथवा,
लिखी और कही गई बातों को समझने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
Ans.
लिखी और कही गई बात को समझने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी-
1. कहीं गई या लिखी गई बात को ध्यान से सुनना या पढ़ना।
2. बात किस संदर्भ में कही गई है या लिखी गई है उसे समझना ।
3. बात की हर पक्ष का सूक्ष्म विश्लेषण करना।
4. यह जानने का प्रयास करना कि यदि बात की हर पहलू को जाँचा परखा जाए तो उसके और कितने अर्थ हो सकते हैं।
5. बात को पहले बेहतर तरीके से समझ लेना फिर अपना मंतव्य रखना ।
6. किसी भी बात का इस तरह से विश्लेषण करना कि उसे बिना पूर्वाग्रह के समझा जा सके।
7. लिखने और बोलने वाले की मनः स्थिति को समझने का प्रयास करना, उसके बाद ही उसके बारे में कोई निर्णय लिया लेना।
Q. 30. नीचे दिए गए उद्धरण का एक संक्षिप्त विवरण तैयार करें।
Ans.
” ऋतुराज वसन्त के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पतझड़ में पश्चिम- पवन ने जीर्ण-शीर्ण पत्रों को गिराकर लताकुंजों, पेड़-पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। वृक्षों और लताओं के अंग में नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गयी। कनेर, करवरी, मदार, पाटल इत्यादि पुष्पों की सुगन्धि दिग्दिगन्त में अपनी मादकता का संचार करने लगी। न शीत की कठोरता, न ग्रीष्म का ताप। समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक प्राणी की नस-नस में उत्फुल्लता और उमंग की लहरें उठ रही है। गेहूँ के सुनहरे बालियों से पवनस्पर्श के कारण रुनझुन का संगीत फूट रहा है। पत्तों के अधरों पर सोया हुआ संगीत मुखर हो गया है। पलाश-वन अपनी अरुणिमा में फूला नहीं समाता है। ऋतुराज वसन्त के सुशासन और सुव्यवस्था की छटा हर ओर दिखायी पड़ती हैं। कलियों के यौवन की अँगड़ाई भ्रमरों को आमन्त्रण दे रही है। अशोक के अग्निवर्ण कोमल एवं नवीन पत्ते वायु के स्पर्श से तरंगित हो रहे हैं। शीतकाल के ठिठुरे अंगों में नयी स्फूर्ति उमड़ रही है। वसन्त के आगमन के साथ ही जैसे जीर्णता और पुरातन का प्रभाव तिरोहित हो गया है। प्रकृति के कण-कण में नये जीवन का संचार हो गया है। आम्र मंजरियों की भीनी गन्ध और कोयल का पंचम आलाप, भ्रमरों का गुंजन और कलियों की चटक, वनों और उद्यानों के अंगों में शोभा का संचार- सब ऐसा लगता है जैसे जीवन में सुख ही सत्य है, आनन्द के एक क्षण का मूल्य पूरे जीवन को अर्पित करके भी नहीं चुकाया जा सकता है। प्रकृति ने वसन्त के आगमन पर अपने रूप को इतना सँवारा है, अंग-अंग को सजाया और रचा है कि उसकी शोभा का वर्णन असम्भव है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती।
संक्षेपण : वसन्त ऋतु की शोभा
वसन्तऋतु के आते ही शीत की कठोरता जाती रही। पश्चिम के पवन ने वृक्षों के जीर्ण-शीर्ण पत्ते गिरा दिये। वृक्षों और लताओं में नये पत्ते और रंग-बिरंगे फूल निकल आये। उनकी सुगन्धि से दिशाएँ गमक उठीं। सुनहरे बालियों से युक्त गेहूँ के पौधे खेतों में हवा से झूमने लगे। प्राणियों की नस-नस में उमंग की नयी चेतना छा गयी। आम की मंजरियों से
सुगन्ध आने लगी कोयल कूकने लगी फूलों पर भौरें मँडराने लगे और कलियाँ खिलने लगी । प्रकृति में सर्वत्र नवजीवन का संचार हो उठा।
(टिप्पणी- ऊपर मूल सन्दर्भ में वसन्तऋतु प्रकृति की शोभा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है, जिसमें साहित्यिक लालित्य भरने की चेष्टा की गयी है। संक्षेपण में सभी व्यर्थ शब्दों और वाक्यों को हटा दिया गया है और काम की बातों का उल्लेख कर दिया है, सीधी-सादी भाषा में। मूल वर्तमानकाल में लिखा गया है, पर संक्षेपण में सारी बातें भूतकाल में लिखी गयी हैं।)
Q. 31. उच्च प्राथमिक स्तर में क्या, कैसे और किसे पढ़ाना है इसका आकलन किस प्रकार करेंगे?
Ans.
छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करने के दो उद्देश्य हैं- योगात्मक आकलन (सीख का आकलन) और रचनात्मक आकलन (या सीखने के लिए आकलन)। क्या, कैसे और किसे पढ़ाना है इसका आकलन रचनात्मक आकलन के द्वारा किया जाता है। रचनात्मक मूल्याकन अधिगम को बढ़ाता है, क्योंकि सीखने के लिए, अधिकांश छात्रों को-
1. समझना चाहिए कि उनसे क्या सीखने की उम्मीद की जा रही है।
2. जानना चाहिए कि अपनी पढ़ाई में वे इस समय किस स्तर पर हैं।
3. समझना चाहिए कि वे किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं। (अर्थात् क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए) जानना चाहिए कि कब उन्होंने लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम हासिल कर लिए हैं।
यह पता लगाने के लिए प्रश्न पूछने का इस्तेमाल किया जाता है कि क्या विद्यार्थियों ने किसी चीज को समझा है या नहीं। उनके अनुभव किसी विषय के संबंध में क्या हैं, सीखने का स्तर क्या है, इस स्तर पर किसी विषयवस्तु को पढ़ाने के लिए किन-किन रणनीतियों और उपागम की आवश्यकता होगी, इसका आकलन कुछ प्रश्नों को पूछ कर और विषय से संबंधित कार्यों का अवलोकन करके किया जा सकता है। इस आकलन के परिणामों का फिर अगले अधिगम अनुभव को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। निगरानी और फीडबैक रचनात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है। विद्यार्थियों से सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार पढ़ाने से पहले, पढ़ाते समय और पढ़ाने के बाद आकलन किया जा सकता है।
1. पहले-पढ़ाने से पहले आकलन से यह जानने में मदद मिलती है कि छात्र क्या जानते हैं और पढ़ाने से पहले क्या कर सकते हैं। यह आधार-रेखा निर्धारित करता है. और शिक्षकों को अपनी शिक्षण योजना तैयार करने के लिए प्रारभिक बिंदु देता है।
2. पढ़ाते समय-कक्षा में पढ़ाते समय आकलन करने में यह देखना शामिल है कि छात्र क्या सीख रहे हैं और क्या सुधार हो रहा है। इससे शिक्षकों को अपनी शिक्षण पद्धति, संसाधनों और गतिविधियों का समायोजन करने में मदद मिलेगी। यह समझने में मदद करेगा कि छात्र वांछित उद्देश्य की दिशा में किस प्रकार प्रगति कर रहे है और शिक्षण कितना सफल है।
3. पढ़ाने के बाद शिक्षण के बाद किया जाने वाला आकलन पुष्टि करता है कि छात्रों ने क्या सीखा है और दर्शाता है कि किसने सीखा है और किसे अभी मदद की जरू रत है। इससे शिक्षक अपने शिक्षण लक्ष्य की प्रभाविता का आकलन कर सकेंगे।
Q. 32. उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी विषय के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों की समझ विकसित करें। इन्हें समझना एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है?
Ans. पाठ्यचर्या में उल्लिखित को ही पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। हिंदी विषय के पाठ्क्रम में जिन बिंदुओं का उल्लेख होता है वे सभी किसी ना किसी रूप में पाठ्यचर्या से जुड़े होते हैं। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का ही एक अंग है जिसमें विभिन्न अनुशासनों या विषयों के खास उद्देश्य, शिक्षण पद्धतियों और आकलन की चर्चा होती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा भी कहा जा सकता है कि पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम वस्तुतः यह बताता है कि किसी विषय विशेष को अध्यापन के उद्देश्य क्या है, किसी विषय की स्तरानुसार विषय वस्तु क्या होगी, उसे बेहतर तरीके से कैसे अध्यापन किया जा सकता है और उस विषय का आकलन करने के तरीके क्या होंगे। पाठ्यक्रम शिक्षकों को विषय अध्यापन के बारे में एक प्रकार से दिशा-निर्देश देता है कि पाठ्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों को आप किस प्रकार पूरा कर सकें।
वही पाठ्यपुस्तकों का निर्माण पाठ्यक्रम में वर्णित वर्गानुसार उद्देश्य, शिक्षण पद्धतियों और आकलन के तौर-तरीकों ध्यान में रखकर किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्यपुस्तकों का निर्माण पाठ्यक्रम को केंद्र में रखते हुए किया जाता है। पाठ्य पुस्तकें कक्षा में संपादित होने वाली गतिविधियों का आधार होती है। पाठ्य पुस्तकें स्तरानुसार बनाई जाती है। या शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए दिशा-निर्देशन का कार्य करती है कि किस विषय विशेष के अंतर्गत किस स्तर पर कितनी अवधारणाओं को स्थान दिया जाना है और किस प्रकार उन अवधारणाओं को छात्रों तक संप्रेषित किया जाना है। पाठ्यपुस्तकों में बच्चों के अनुभवों को भी समुचित स्थान दिया जाता है ताकि वे अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान की पुनर्रचना कर सके।
एक शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की समझ का होना शिक्षण-अधिगम की नितांत आवश्यक शर्त है। बिना इन दोनों के अच्छी समझ के शिक्षक कक्षा में स्तरीय और मानकीकृत शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा। बच्चों की शिक्षा के स्वरूप को तय करते समय राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों को पूरा करते हुए छात्रों में पारिवारिक, नैतिक, चारित्रिक गुणों के साथ आदर्श और सफल नागरिक के गुणों का समावेशन भी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में विद्यमान रहते हैं। इनके भीतर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, क्रियाकलापों, अभ्यासों आदि के माध्यम से एक शिक्षक छात्रों की अनेक प्रकार की क्षमताओं का विकास कराकर उन्हें सफल नागरक/व्यक्ति के रूप में प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करती है।
भाषाई शुद्धता, व्याकरण में परिमार्जित होना, भाषा की कुशलताओं की दक्षता, स्वयं की रचनात्मक क्षमता, प्रदर्शन कला द्वारा अभिव्यक्ति की शक्ति आदि जैसे गुणों को निखारने में शिक्षक (भाषा/हिंदी) के लिए पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों की उपस्थिति काफी मदद दायी होती है। पाठ्यक्रम के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति में, अधिगम की प्रक्रिया को रोचक बनाने में, छात्रों के ध्यान को पाठ्यवस्तु पर केंद्रित रख सकने में तथा अभ्यास द्वारा शिक्षण की सफलता को प्राप्त करने में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका को मात्र एक शिक्षक ही समझ सकता है।
Pedagogy Of Math Notes , Book , Guide pdf
Pedagogy Of Math Pdf download
scert Pedagogy Of Math Notes , Book , Guide pdf download
bihar deled s-9a Notes , Book , Guide pdf
गणित का शिक्षाशास्त्र Notes , Book , Guide pdf
deled s-9-a Notes , Book , Guide pdf , deled S-9a , s9-a DElEd 2nd Year ,
गणित का शिक्षाशास्त्र नोट्स , बुक ,गाइड पीडीएफ
S9- a Pedagogy of Math Notes , Book , Guide pdf
S9- b Pedagogy of science Notes , Book , Guide pdf
S9- c Pedagogy of social science Notes , Book , Guide pdf
S9- d Pedagogy of English Notes , Book , Guide pdf
S9- e Pedagogy of hindi Notes , Book , Guide pdf
S9- f Pedagogy of Urdu Notes , Book , Guide pdf
S9- g Pedagogy of Bangali Notes , Book , Guide pdf
S9- h Pedagogy of Math Notes , Book , Guide pdf
S9- i Pedagogy of Math Notes , Book , Guide pdf
 |
 |